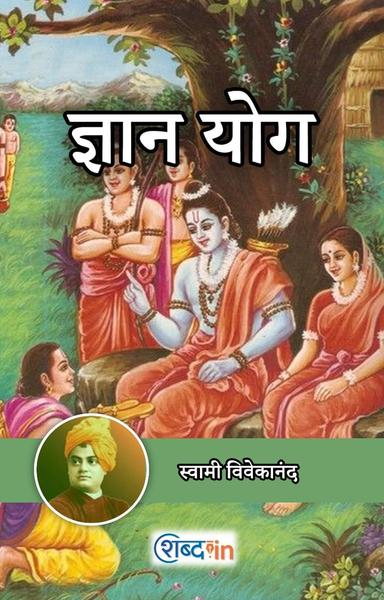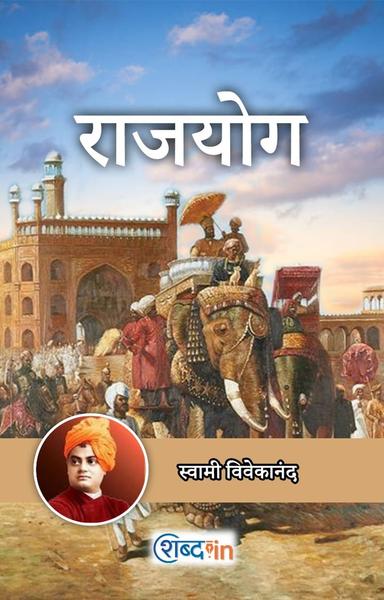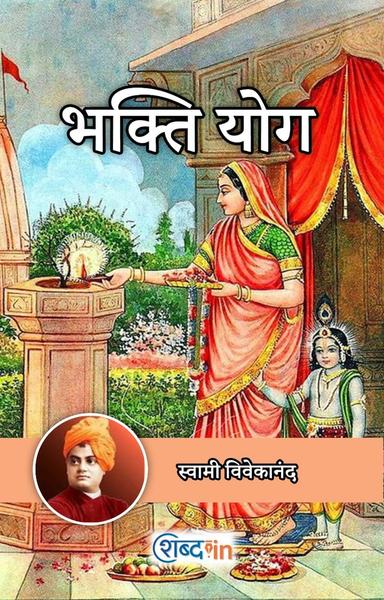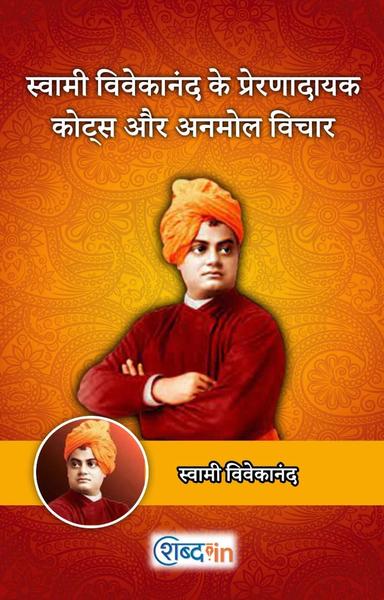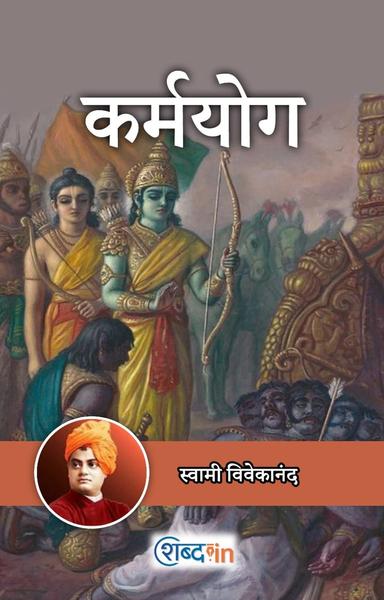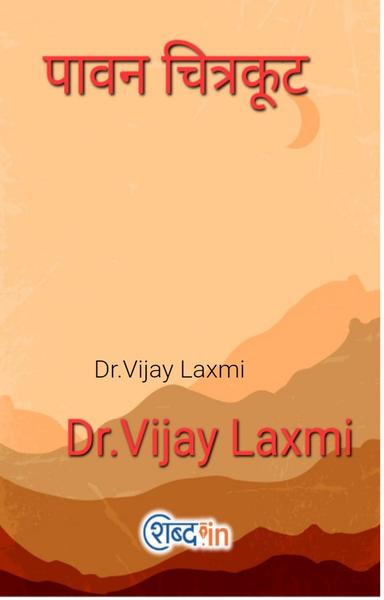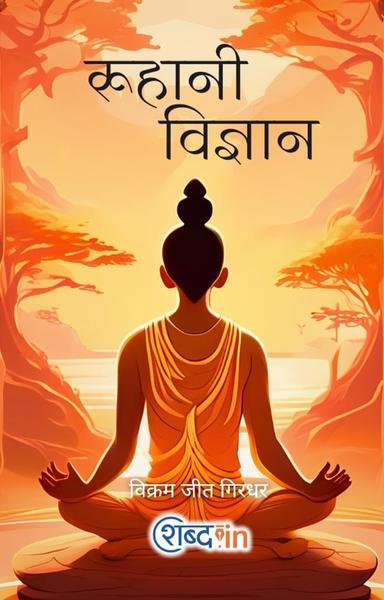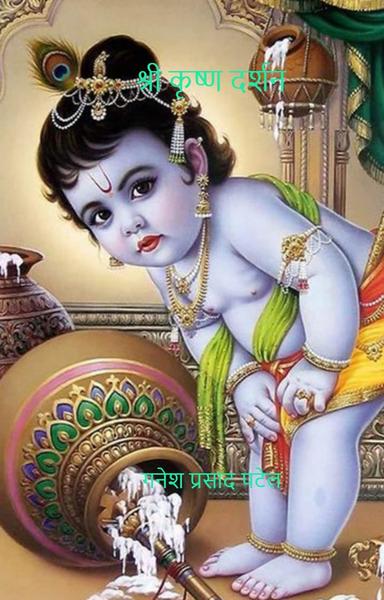तुममें से बहुतों ने मैक्समूलर की सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘वेदान्त दर्शन पर तीन व्याख्यान’को पड़ा होगा और शायद कुछ लोगों ने इसी विषय पर प्रोफेसर डॉयसन की जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक पढ़ी हो। ऐसा लगता है कि पश्चात देशों में भारतीय धार्मिक चिन्तन के बारे में जो कुछ लिखा या पढ़ाया जा रहा है, उसमें भारतीय दर्शन की अद्वैतवाद नामक शाखा प्रमुख स्थान रखती है । यह भारतीय धर्म का अद्वैतवाद-वाला पक्ष है और कभी कभी ऐसा भी सोचा जाता है कि वेदों की सारी शिक्षाएं इस दर्शन में सन्निहित हैं। खैर भारतीय चिन्तन-धारा के बहुत सारे पक्ष हैं और यह अद्वैतवाद तो अन्य वादों की तुलना में सब से कम लोगों द्वारा माना जाता है । अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत में अनेकानेक चिन्तन-धाराओं की परम्परा रही है और चूंकि शाखा विशेष के अनुयायियों द्वारा अंगीकार किये ‘जानेवाले मतों को निर्धारित करनेवाला कोई सुसंघटित या स्वीकृत धर्मसंघ अथवा कतिपय व्यक्तियों के समूह वहाँ कभी नहीं रहे, इसलिए लोगों को सदा से ही अपने मन के अनुरूप धर्म चुनने अपने दर्शन को चलाने तथा अपने सम्प्रदायों को स्थापित करने की स्वतंत्रता रही। फलस्वरूप हम पाते है कि चिरकाल से ही भारत में मत-मतान्तरों की बहुतायत रही है। आज भी हम कह नहीं सकते कि कितने सौ धर्म वहाँ फल रहे हैं और कितने नये धर्म हर साल उत्पन्न होते है । ऐसा लगता है कि उस राष्ट्र की धार्मिक उर्वरता असीम है ।
भारत में प्रचलित इन विभिन्न मतों को मोटे तौर पर दो भागो में विभक्त किया जा सकता है : आस्तिक और नास्तिक। जो मत हिन्दू धर्म ग्रन्थ वेदों को सत्य का शाश्वत प्रकाश मानते हैं, उन्हें आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों को न मानकर अन्य प्रमाणों पर आधारित हैं,उन्हें भारत में नास्तिक कहते हैं। आधुनिक नास्तिक हिन्दू मतों में दो प्रमुख हैं; बौद्ध और जैन। आस्तिक मतावलम्बी कोई कोई कहते है कि शाल हमारी बुद्धि से अधिक प्रामाणिक है, जब कि दूसरे मानते हैं कि शास्त्रों के केवल बुद्धिसम्मत अंश को ही स्वीकार करना चाहिए, शेष को छोड़ देना चाहिए।
आस्तिक मतों की भी फिर तीन शाखाएँ हैं : सांख्य न्याय और मीमांसा। इनमें से पहली दो शाखाएँ किसी सम्प्रदाय की स्थापना करने में सफल न हो सकीं, यद्यपि दर्शन के रूप में उनका अस्तित्व अभी भी है। एकमात्र सम्प्रदाय जो अभी भारत में प्रायः सर्वत्र प्रचलित है, वह है उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्त। इस दर्शन को ‘वेदान्त’ कहते हैं । भारतीय दर्शन की समस्त शाखाएँ वेदान्त, यानी उपनिषदों से ही निकली हैं, किन्तु अतिवादियों ने यह नाम खासकर अपने लिए रख लिया, क्योंकि वे अपने सम्पूर्ण धर्म ज्ञान तथा दर्शन को एकमात्र वेदान्त पर ही आधारित करना चाहते थे। आगे चलकर वेदान्त ने प्राधान्य प्राप्त किया। और भारत में अब जो अनेकानेक सम्प्रदाय है, वे किसी न किसी रूप में उसी की शाखाएँ हैं। फिर भी ये विभिन्न शाखाएँ अपने विचारों में एकमत नहीं हैं।
हम देखते है कि वेदान्तियों के तीन प्रमुख भेद है। पर एक विषय पर सभी सहमत हैं, वह यह कि ईश्वर के अस्तित्व में सभी विश्वास करते हैं। सभी वेदान्ती यह भी मानते हैं कि वेद शाश्वत आप्तवाक्य है, यद्यपि उनका ऐसा मानना उस तरह का नहीं, जिस तरह ईसाई अथवा मुसलमान लोग अपने अपने धर्मग्रंथों के बारे में मानते हैं । वे अपने ढंग से ऐसा मानते हैं । उनका कहना है कि वेदों में ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान सत्रिहित है और चूंकि ईश्वर चिरन्तन है, अतः उसका ज्ञान भी शाश्वत रूप से उसके साथ है । अतः वेद भी शाश्वत है । दूसरी बात जो सभी वेदान्ती मानते हैं, वह है सृष्टि सम्बधी चक्रीय सिद्धान्त। सब यह मानते हैं कि सृष्टि चक्रों या कल्पों में होती है। संपूर्ण सृष्टि का आगम और विलय होता है। आरम्भ होने के बाद सृष्टि क्रमशः स्थूलतर रूप लेती जाती है, और एक अपरिमेय अवधि के पश्चात् पुनः सूक्ष्मतर रूप में बदलना शुरू करती है तथा अन्त में विघटित होकर विलीन हो जाती है । इसके बाद विराम का समय आता है । सृष्टि का फिर उद्धव होता है और फिर इसी क्रम की आवृत्ति होती है। ये लोग दो तत्त्वों को स्वतः प्रमाणित मानते है : एक को ‘आकाश’ कहते है, जो वैज्ञानिकों के ‘इथर’ से मिलता-जुलता है और दूसरे को ‘प्राण’ कहते हैं, जो एक प्रकार की शक्ति है । ‘प्राण’ के विषय में इनका कहना है कि इसके कम्पन से विश्व की उत्पत्ति होती है। जब सृष्टीचक्र का विराम होता है, तो व्यक्त प्रकृति क्रमशः सूक्ष्मतर होते-होते आकाश-तत्त्व के रूप में विघटित हो जाती है, जिसे हम न देख सकते है और न अनुभव ही कर सकते हैं; किन्तु इसी से पुनः समस्त वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। प्रकृति में हम जितनी शक्तियाँ देखते हैं – जैसे, गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, विकर्षण अथवा विचार, भावना एवं स्नायविक गति – सभी अन्ततोगत्वा विघटित होकर प्राण में परिवर्तित हो जाती हैं और प्राण का स्पन्दन रुक जाता है। इस: स्थिति में वह तब तक रहता है, जब तक सृष्टि का कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं हो जाता। उसके प्रारम्भ होते ही ‘प्राण में पुनः कम्पन होने लगते हैं । इस कम्पन का प्रभाव ‘आकाश’ पर पड़ता है और तब सभी रूप और आकार एक निश्चित क्रम में बाहर प्रक्षिप्त होते है।
सब से पहले जिस ‘दर्शन कीं चर्चा मैं तुमसे करूँगा वह द्वैतवाद के ‘ नाम से प्रसिद्ध है। द्वैतवादी यह मानते हैं कि विश्व का स्त्रष्टा और शासक ईश्वर शाश्वत रूप से प्रकृति एवं जीवात्मा से पृथक् है। ईश्वर नित्य है, प्रकृति नित्य है तथा सभी आत्माएँ भी नित्य हैं । प्रकृति तथा आत्माओं की अभिव्यक्ति होती है, एवं उनमें परिवर्तन होते हैं, परन्तु ईश्वर ज्यों का त्यों रहता है । द्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर सगुण है; उसके शरीर नहीं है, पर उसमें गुण है। मानवीय गुण उसमें विद्यमान है; जैसे वह दयावान् है, वह न्यायी है, वह सर्वशक्तिमान् है, वह बलवान् है, उसके पास पहुँचा जा सकता है, उससे प्रार्थना की जा सकती है, उससे प्रेम किया जा सकता है, प्रेम का वह प्रतिदान देता है आदि-आदि। संक्षेप में वह मानवीय ईश्वर है – अन्तर इतना है कि वह मनुष्य से अनन्त गुना बड़ा है, तथा मनुष्य में जो दोष है, वह उनसे परे है। ‘वह अनन्त शुभ गुणों का भण्डार है’ – ईश्वर की यही परिभाषा लोगों ने दी है। वह उपादानों के बिना सृष्टि नहीं कर सकता। प्रकृति ही वह उपादान है, जिससे वह समस्त विश्व की रचना करता है। कुछ वेदान्तेतर द्वैतवादी – जिन्हें परमाणुवादी’ कहते हैं, यह मानते है कि प्रकृति असंख्य परमाणुओं के सिवा और कुछ नहीं है और ईश्वर की इच्छा- शक्ति इन परमाणुओं में सक्रिय होकर सृष्टि करती है । -वेदान्ती लोग इस परमाणु-सिद्धान्त को नहीं मानते। उनका कहना है कि यह नितान्त तर्कहीन है। अविभाज्य परमाणु रेखागणित के बिन्दुओं की तरह हैं, खण्ड और परिमणिण्हत। किन्तु ऐसी खण्ड और परिमाणरहित वस्तु को अगर असंख्य बार गुणित किया जाए, तो भी वह ज्यों की त्यों रहेगी। फिर, कोई वस्तु, जिसके अवयव नहीं ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती, जिसके विभिन्न अवयव हों। चाहे जितने भी शून्य इकट्ठे किये जाएं, उनसे कोई पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। इसलिए अगर ये परमाणु अविभाज्य हैं तथा परिमाणरहित हैं, तो इनसे विश्व की सृष्टि सर्वथा असम्भव है। अतएव वेदान्ती द्वैतवादी अविश्लिष्ट एवं अविभेद्य प्रकृति में विश्वास करते हैं, जिससे ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। भारत में अधिकांश लोग द्वैतवादी हैं मानव-प्रकृति सामान्यतः इससे अधिक उच्च कल्पना नहीं कर सकती । हम देखते है कि संसार में धर्म में विश्वास रखने वालों में नब्बे प्रतिशत लोग द्वैतवादी ही हैं। यूरोप तथा एशिया के सभी धर्म द्वैतवादी है, वैसा होने के लिए वे विवश है। कारण, सामान्य मनुष्य उस वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता, जो मूर्त न हो। इसलिए स्वभावतः वह उस वस्तु से चिपकना चाहता है, जो उसकी बुद्धि की पकड़ में आती है। तात्पर्य यह कि वह उच्च आध्यात्मिक भावनाओं को तभी समझ सकता है, जब ले उसके स्तर पर नीचे उतर आएँ। वह सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में ही ग्रहण कर सकता है। सम्पूर्ण विश्व में सर्वसाधारण का यही धर्म है। वे एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो उनसे पूर्णतया पृथक्, मानो एक बड़ा राजा, एक अत्यन्त बलिष्ठ सम्राट हो। साथ ही वे उसे पृथ्वी पर के राजाओं की अपेक्षा अधिक पवित्र बना देते है। उसे समस्त दुर्गुणों से रहित और समस्त सदुणों का आधार बना देते हैं । जैसे कहीं अशुभ के बिना शुभ और अन्धकार के बिना प्रकाश सम्भव ही!
सभी द्वैतवादी सिद्धान्तों के साथ पहली कठिनाई यह है कि असंख्य सदुणों के भाण्डार न्यायी तथा दयालु ईश्वर के राज्य में इतने कष्ट कैसे हो सकते हैं? यह प्रश्न हर द्वैतवादी धर्म के समक्ष है पर, हिन्दुओं ने कभी भी इसे सुलझाने के लिए शैतान की कल्पना नहीं की। हिन्दुओं ने एकमत, होकर स्वयं मनुष्य को ही दोषी माना और उनके लिए ऐसा मानना आसान भी था। क्यों? इसलिए कि, जैसा मैंने तुमसे अभी कहा, उन्होंने नहीं माना कि आत्मा की सृष्टि शून्य से हुई । इस जीवन में हम देखते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं; हममें से प्रत्येक हर रोज अगले दिन के निर्माण में लगा रहता है। आज हम कल के भाग्य को निश्चित करते हैं, कल परसों का, और इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए इस तर्क को हम यदि पीछे की ओर ले चले, तो भी यह पूर्णतः युक्तिसंगत होगा। अगर हम अपने ही कर्मों से भविष्य को निश्चित करते हैं, तो यही तर्क हम अतीत के लिए भी क्यों न लागू करें? अगर किसी अनन्त शृंखला की कुछ कड़ियों की पुनरावृत्ति होते हम बारम्बार देखें तो कड़ियों के इन समूहों के आधार पर हम समूची शृंखला की भी व्याख्या कर सकते हैं । इसी तरह इस अनन्त काल के कुछ भाग को लेकर अगर हम उसकी व्याख्या कर सकें और समझ सकें, तो यही व्याख्या समय की समूची अनन्त शृंखला के लिए भी सत्य होगी। यदि यह सत्य हो कि प्रकृति सर्वत्र एकरूप है, तो काल की सम्पूर्ण शृंखला पर यही व्याख्या लागू होगी। अगर यह सत्य है कि इस छोटी-सी अवधि में हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर यह सत्य है कि हर कार्य के लिए कारण अपेक्षित है, तो यह भी सत्य है कि हमारा वर्तमान हमारे सम्पूर्ण अतीत का परिणाम है । इसलिए यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के भाग्य के निर्माण के लिए मनुष्य के सिवा और किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कुछ भी अशुभ दीखता है, उसके कारण तो हम ही है। हम लोग ही सारे पापों की जड़ हैं। और जिस तरह हम यह देखते हैं कि पापों का परिणाम दुःखद होता है, उसी तरह यह भी अनुमान किया जा सकता है कि आज जितने कष्ट देखने को मिलते है, उन सब के मूल में वे पाप हैं, जिन्हें मनुष्य ने अतीत में किया है । इसलिए इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य ही उत्तरदायी है; ईश्वर पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वह, जो चिरन्तन परम दयालु पिता है, दोषी नहीं माना जा सकता। ‘हम जो बोते है, वही काटते हैं।’
द्वैतवादियों का एक दूसरा विचित्र सिद्धान्त यह है कि सभी आत्माएँ कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगी; कोई भी छूटेगी नहीं। नाना प्रकार के उत्थान-पतन तथा सुख-दुःख के भोग के उपरान्त अन्त में ये सभी आत्माएँ मुक्त हो जाएँगी। आखिर मुक्त किससे होंगी? सभी हिन्दू सम्प्रदायों का मत है कि इस संसार से मुक्त हो जाना है। न तो यह संसार, जिसे हम देखते तथा अनुभव करते हैं, और न वह जो काल्पनिक है, अच्छा और वास्तविक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही शुभ और अशुभ से भरे पड़े हैं। द्वैतवादियों के अनुसार इस संसार से परे एक ऐसा स्थान है, जहाँ केवल सुख और केवल शुभ ही है; जब हम उस स्थान पर पहुँच जाते है, तो जन्म-मरण के पाश से मुक्त हो जाते है। कहना न होगा कि यह कल्पना उन्हें कितनी प्रिय है, वहाँ न तो कोई व्याधि होगी और न मृत्यु; वहाँ शाश्वत सुख होगा और सदा वे ईश्वर के समक्ष रहते हुए परमानन्द का अनुभव करते रहेंगे। उनका विश्वास है कि सभी प्राणी – कीट से लेकर देवदूत और देवता तक – कभी न कभी उस लोक में पहुंचेंगे ही जहाँ दुःख का लेश भी नहीं होगा। किन्तु अपने इस जगत् का कभी अन्त नहीं होगा; तरंग की भांति यह सतत चलता रहेगा। निरन्तर परिवर्तित होते रहने के बावजूद इसका कभी अन्त नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करनेवाली आत्माओं की संख्या अपरिमित है। उनमें से कुछ तो पौधों में हैं कुछ पशुओं में, कुछ मनुष्यों में तथा कुछ देवताओं में हैं । पर सब के सब – उच्चतम देवता भी – अपूर्ण हैं, बन्धन में हैं। यह बन्धन क्या है? – जन्म और मरण की अपरिहार्यता। उच्चतम देवों को भी मरना पड़ता है । देवता क्या हैं? वे विशिष्ट अवस्थाओं या पदों के प्रतीक हैं। उदाहरणस्वरूप, इन्द्र जो देवताओं के राजा हैं, एक पद-विशेष के प्रतीक हैं। कोई अत्यन्त उच्च आत्मा इस कल्प में उस पद पर विराजमान है और इस कल्प के बाद वह पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी और इस कल्प में जो दूसरी उच्चतम आत्मा होगी, वह उस पद पर जाकर आसीन होगी। ठीक यही बात अन्य सभी देवताओं के बारे में भी है। वे विशिष्ट पदों के प्रतीक हैं, जिन पर एक के बाद एक करोड़ों आत्माओं ने काम किया है और वहाँ से उतरकर मनुष्य का जन्म लिया है । जो मनुष्य फल की आकांक्षा से इस लोक में परोपकार तथा अच्छे काम करते हैं और स्वर्ग अथवा यशप्राप्ति की आशा करते है; वे मरने पर देवता बनकर अपने किये का फल भोगते हैं। किन्तु यह मोक्ष नहीं है। मोक्ष, फल की आशा रखने से नहीं मिलता। मनुष्य जिस किसी भी चीज की आकांक्षा करता है, ईश्वर उसे वह देता है। आदमी शक्ति चाहता है पद चाहता है, देवताओं की भांति सुख चाहता है; उसकी इच्छाएँ तो पूरी हो जाती है, पर उसके कर्म का कोई शाश्वत फल नहीं होता। एक निश्चित अवधि के बाद उसके पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है – चाहे वह अवधि कितनी ही लम्बी क्यों न हो। उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तब वे देवता पुनः मनुष्य हो जाएँगे और उन्हें मोक्षप्राप्ति का दूसरा अवसर मिलेगा। निम्न कोटि के पशु क्रमशः मनुष्यत्व की ओर बढ़ेंगे, फिर देवत्व की ओर; और तब शायद पुनः मनुष्य बनेंगे, अथवा पशु हो जाएँगे। यह क्रम तब तक चलता रहेगा, जब तक वे वासना से रहित नहीं हो जाते, जीवन की तृष्णा को छोड़ नहीं देते और ‘मैं और मेरा’ के मोह से मुक्त नहीं हो जाते । यह ‘मैं और मेरा, ही संसार में सारे पापों का मूल है। अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो कि क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है, तो फौरन वह कहेगा – “यह तो ईश्वर का है; मेरी सम्पत्ति मेरी नहीं, बल्कि ईश्वर की है। “सब कुछ ईश्वर का है – ऐसा ही मानना चाहिए।
भारत में ये द्वैतवादी पक्के निरामिष तथा अहिंसावादी है। किन्तु उनके ये विचार बौद्ध लोगों के विचारों से भिन्न है। अगर तुम किसी बौद्ध से पूछो – “आप क्यों अहिंसा का उपदेश देते है?” – तो वह उत्तर देगा – “हमें किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है।” किन्तु अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो – “आप जीवहिंसा क्यों नहीं करते?” तो वह कहेगा – “क्योंकि सभी जीव तो ईश्वर के हैं।” इस तरह द्वैतवादी मानते हैं कि ‘मैं और मेरा’ का प्रयोग केवल ईश्वर के सम्बन्ध में ही करना चाहिए। ‘मैं’ का सम्बोधन केवल वही कर सकता है और सारी चीजें भी उसी की हैं। जब मनुष्य इस स्तर पहुँच जाए कि ‘मैं और मेरा’ का भाव उसमें न रहे, सारी चीजों को ईश्वरीय मानने लगे हर प्राणी से प्रेम करने लगे, और किसी पशु के लिए भी अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे – और ये सारे भाव बिना किसी प्रतिफल की आकांक्षा से हों, तो उसका हृदय स्वतः पवित्र हो जाएगा, तथा उस पवित्र हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। ईश्वर ही सभी आत्माओं, के आकर्षण का केन्द्र है। द्वैतवादी कहते हैं – “अगर कोई सुई मिट्टी से ढकी हो, तो उस पर चुम्बक का प्रभाव न होगा; पर ज्योंही उस पर से मिट्टी को हटा दिया जाएगा त्योंही वह चुम्बक की ओर आकृष्ट हो जाएगी।” ईश्वर चुम्बक है और मनुष्य की आत्मा सुई; पापरूपी मल इसको ढके रहता है । जैसे ही कोई आत्मा इस मल से रहित हो जाती है, वैसे ही प्राकृतिक आकर्षण से वह ईश्वर के पास चली आती है; और सनातन रूप से उसके साथ रहने लगती है, यद्यपि उसका ईश्वर से कभी तादात्म्य नहीं होता। पूर्ण आत्मा अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी रूप ग्रहण कर सकती है । अगर वह चाहे तो सैकड़ों शरीर धारण कर सकती है और चाहे तो एक भी नहीं; वह लगभग सर्वशक्तिमान हो जाती है अन्तर केवल इतना रहता है कि वह सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टि करने की शक्ति केवल ईश्वर ही की है । चाह कोई कितना भी पूर्ण क्यों न हो वह विश्वनियन्ता नहीं हो सकता, यह काम केवल ईश्वर ही कर सकता है । किन्तु जो आत्माएँ पूर्ण हो जाती हैं, वे सभी सदा आनन्द से ईश्वर के साथ रहती है। द्वैतवादी लोगों की यही धारणा है ।
ये द्वैतवादी और भी मत का प्रचार करते हैं। “प्रभु मुझे यह दो मुझे वह दो” – ईश्वर से इस तरह की प्रार्थना करने पर इन लोगों को आपत्ति है। ये समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को जागतिक कोई वस्तु माँगनी ही है तो वह ईश्वर से निम्नतर जीवों से – इन देवताओं, देवदूतों अथवा पूर्ण आत्माओं में से किसी से माँगे। ईश्वर केवल प्रेम के लिए है। यह तो निन्दनीय बात है कि हम ईश्वर से भी ‘मुझे यह दो वह दो’ ऐसा निवेदन करते है। इसलिए द्वैतवादी कहते है कि मनुष्य अपनी वासनाओं की पूर्ति तो निम्न कोटि के देवताओं को प्रसन्न करके कर ले, पर अगर वह मोक्ष चाहता है तो उसे ईश्वर की पूजा करनी होगी। भारतवर्ष में सर्वसाधारण का यही धर्म है।
असली वेदान्तदर्शन विशिष्टाद्वैत से प्रारम्भ होता है। इस सम्प्रदाय का कहना है कि कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं होता । कारण ही परिवर्तित रूप में कार्य बनकर आता है । अगर सृष्टि कार्य है और ईश्वर कारण, तो ईश्वर और सृष्टि दो नहीं है । वे अपना तर्क इस तरह आरम्भ करते है कि ईश्वर ही जगत का निमित्त तथा उपादान कारण है । अर्थात इस सृष्टि का ईश्वर ही स्वयं कर्ता है और वही स्वयं इसका उपादान भी है, जिससे सम्पूर्ण प्रकृति प्रक्षिप्त हुई है। तुम्हारी भाषा जो क्रियेशन (creation) शब्द है वस्तुतः संस्कृत में उसका समानार्थक शब्द नहीं है,क्योंकि भारत में ऐसा कोई सम्प्रदाय नहीं, जो पाश्चात्य लोगों की तरह यह मानता हो कि प्रकृति की स्थापना शून्य से हुई है । हो सकता है कि आरम्भ मैं कुछ लोग ऐसा मानते भी रहे हो पर शीघ्र ही उन्हें निरुत्तर कर दिया गया होगा। मेरी जानकारी में आज कोई ऐसा सम्प्रदाय नहीं है, जो इस धारणा में विश्वास करता हो । सृष्टि से हम लोगों का तात्पर्य है किसी ऐसी वस्तु का प्रक्षेपण, जो पहले से ही हो । इस सम्प्रदाय के अनुसार तो मारा विश्व स्वयं ईश्वर ही है । विश्व के वही उपादान है । वेदों में हम पढ़ते है, ‘जिस तरह ऊर्णनाभि (मकड़ी) अपने ही शरीर से तन्तुओं को निकालता है, उसी तरह यह सारा विश्व भी ईश्वर से प्रादुर्भूत हुआ है।’1
अब अगर कार्य कारण का ही दूसरा रूप है, तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर, जो चेतन और शाश्वत ज्ञानस्वरूप है, किस तरह इस भौतिक, स्थूल और अचेतन जगत का कारण हो सकता है? अगर कारण परम शुद्ध और पूर्ण हो, तो कार्य अन्यथा कैसे हो सकता है? ये विशिष्टाद्वैतवादी क्या कहते हैं? उनका एक विचित्र सिद्धान्त है । उनका कहना है कि ईश्वर प्रकृति एवं आत्मा एक हैं। ईश्वर मानो जीव है और प्रकृति तथा आत्मा उसके शरीर है । जिस तरह मेरे एक शरीर है तथा एक आत्मा है, ठीक उसी तरह सम्पूर्ण विश्व एवं सारी आत्माएँ ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर सारी आत्माओं की आत्मा है । इस तरह ईश्वर विश्व का उपादान कारण है। शरीर परिवर्तित हो सकता है – तरुण या वृद्ध, सबल या दुर्बल हो सकता है – किन्तु इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ही शाश्वत सत्ता शरीर के माध्यम से सदा अभिव्यक्त होती है । शरीर आता-जाता रहता है, पर आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। ठीक इसी तरह समस्त जगत ईश्वर का शरीर है और इस दृष्टि से वह ईश्वर ही है; किन्तु जगत में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे ईश्वर प्रभावित नहीं होता, जगद्रुपी उपादान से वह सृष्टि करता है और हर कल्प के अन्त में उसका शरीर सूक्ष्म होता है, वह संकुचित होता है; फिर परवर्ती कल्प के प्रारम्भ में वह विस्तृत होने लगता है और उससे विभिन्न जगत निकलते हैं।
फिर द्वैतवादी एवं विशिष्टाद्वैतवादी दोनों यह मानते है कि आत्मा स्वभावतः पवित्र है, किन्तु अपने कर्मों से यह अपने को अपवित्र बना लेती है। विशिष्टाद्वैतवादी इसको द्वैतवादियों की अपेक्षा अधिक सुन्दर ढंग से कहते हैं। उनका कहना है कि आत्मा की पवित्रता एवं पूर्णता कभी संकुचित हो जाती है, पर फिर ज्यों की त्यों हो जाती है। और हमारा प्रयास यह है कि उसकी अवस्था को बदलकर पुनः उसकी पूर्णता, पवित्रता एवं शक्ति की स्वाभाविक स्थिति में ले आएँ। आत्मा के अनेक गुण हैं पर उसमें सर्वशक्तिमत्ता या सर्वज्ञता नहीं है। हर पापकर्म उसकी प्रकृति को संकुचित कर देता है और पुण्य कर्म विस्तीर्ण। जिस तरह किसी प्रज्ज्वलित अग्नि से उसी जैसे करोड़ों स्फुलिंग निकलते है, उसी तरह इस अपरिमेय सत्ता (ईश्वर) से सभी आत्माएँ निकली है । सब का उद्देश्य एक ही है । विशिष्टाद्वैतवादियों का ईश्वर भी साकार है, अशेष गुणों का आकर है वह-विश्व की हर चीज में व्याप्त है । वह विश्व की हर वस्तु में हर जगह अन्तःप्रविष्ट है । जब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है, तो उनका तात्पर्य यही रहता है कि ईश्वर सब में व्याप्त है । उदाहरणतः ईश्वर दीवाल नहीं हो जाता, बल्कि वह दीवाल में, व्याप्त है । विश्व में कोई ऐसा कण नहीं, ऐसा अणु नहीं, जिसमें वह न हो। आत्माएँ सीमित हैं; वे सर्वव्यापी नहीं हैं। जब उनकी शक्तियों का विस्तार होता है और वे पूर्ण हो जाती हैं, तो जरा-मरण के चक्र से मुक्ति पा जाती हैं, और सदा के लिए ईश्वर में ही वास करती हैं ।
अब हम अद्वैतवाद पर आते हैं । मेरे विचार में अब तक विश्व के किसी भी देश में दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसका चरमतम विकास एवं सुन्दरतम पुष्प अद्वैतवाद में है। यहाँ मानव-विचार अपनी अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है और अभेद्य प्रतीत होने वाले रहस्य के भी पार चला जाता है। यह है, वेदान्त का अद्वैतवाद। अपनी दुरूहता और अतिशय उत्कृष्टता के कारण यह जनसमुदाय का धर्म नहीं बन पाया। पिछले तीन हजार वर्षों से जहाँ इसका एकछत्र शासन रहा है, जो इसका जन्मस्थान है, उस भारत में भी यह सर्वसाधारण तक पहुँचने में असमर्थ-ही रहा। आगे चलकर हम देखेंगे कि संसार के श्रेष्ठ विचारशील व्यक्तियों को भी इसको समझने में कठिनाई होती रही है। हमने अपने आप को इतना दुर्बल बना लिया है, इतना नीचे गिरा लिया है। हम बातें चाहे जितनी बड़ी-बड़ी करें पर सत्य तो यह है कि स्वभावतः हम किसी दूसरे का सहारा चाहते हैं। हमारी दशा उन छोटे और कमजोर पौधों की है, जो किसी सहारे कि बिना नहीं रह सकते। कितनी बार लोगों ने मुझसे ‘एक सुखकर धर्म’ की माँग की। कुछ ही लोग हैं जो सत्य की जिज्ञासा करते हैं, उससे भी कम सत्य को जानने का साहस कुरते- हैं और सब से कम सत्य को जानकर हर प्रकार से उसकी कार्यरूप में परिणत करते हैं । यह उनका दोष नहीं; बल्कि उनके मस्तिष्क का दोष है। हर नया विचार, खासकर उच्च कोटि का लोगों को अस्तव्यस्त कर देता है, उनके मस्तिष्क में नया मार्ग बनाने लगता है, और उनके सन्तुलन को नष्ट कर देता है । साधारणतः लोग अपने इर्द-गिर्द के वातावरण में रमें रहते हैं, और इससे ऊपर उठने के लिए उन्हें प्राचीन अन्धविश्वासों वंशानुगत अन्धविश्वासों वर्ग, नगर देश के अन्धविश्वासों तथा इन सब की पृष्ठभूमि में स्थित मानव-प्रकृति में सत्रिहित अन्धविश्वासों की विशाल राशि पर विजय प्राप्त करनी होती है। फिर भी कुछ तो ऐसे वीर लोग संसार में है ही, जो सत्य को जानने का साहस करते हैं, जो उसे धारण करने तथा अन्त तक उसका पालन करने का साहस करते हैं ।
अद्वैतवादी लोगों का क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर ईश्वर है, तो वह सृष्टि का निमित्त तथा उपादान कारण दोनों है। वह केवल स्त्रष्टा नहीं अपितु सृष्टि भी है। वह स्वयं ही विश्व है। पर यह कैसे सम्भव है? शुद्ध चित्तस्वरूप ईश्वर विश्व में कैसे परिणत हुआ है? हाँ! ऐसा ही प्रतीत होता है । जिसे अज्ञानी लोग विश्व कहते हैं, वस्तुतः उसका अस्तित्व है ही नहीं। तब तुम और मैं और ये सारी चीजें जिन्हें हम देखते हैं क्या है? मात्र आत्मसम्मोहन। सत्ता केवल एक, है और वह अनादि अनन्त और शाश्वत शिवस्वरूप है। उस सत्ता में ही हम ये सारे सपने देखते हैं। एक आत्मा ही है, जो इन सारी चीजों से परे हैं, जो अपरिमेय है, जो ज्ञात से तथा ज्ञेय से परे है । हम उसी में तथा उसी के माध्यम से विश्व को देखते हैं। एकमात्र सत्य वही है । वही यह मेज है, वही दर्शक है, वही दीवाल है, वही सब कुछ है; पर नाम और रूप से रहित । मेज में से नाम और रूप को हटा दो जो बचेगा वही वह सत्ता है । वेदान्ती उस सत्ता में लिंग-भेद नहीं मानते – लिंग तो मानव-मस्तिष्क से उत्पन्न एक कल्पना, एक भ्रम है – आत्मा का कोई लिंग नहीं। जो लोग भ्रम में है, जो पशु के सदृश हो गये है, वे पुरुष या स्त्री को देखते हैं; किन्तु जो जीते-जागते देवता है, वे नर या नारी में अन्तर नहीं जानते। जो सारी चीजों से ऊपर स्व चुके हैं, उसके लिए नर-नारी में भेद की भावना कैसे रह सकती है? हर व्यक्ति हर-वस्तु शुद्ध आत्मा है; जो पवित्र है, लिंगहीन है तथा शाश्वत शिव है । नाम रूप और शरीर ही, जो भौतिक है, सारी भिन्नताओं के मूल है । अगर तुम नाम और रूप के अन्तर को हटा दो, तो सारा विश्व एक है; दो की सत्ता नहीं है बल्कि सर्वत्र एक ही है। तुम और मैं एक हैं। न तो प्रकृति है न ईश्वर और न विश्व – बस, एक ही अपरिमेय सत्ता है जिससे नाम और रूप के आधार पर ये तीनों बने है। ज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है? वह नहीं जाना जा सकता। तुम अपने आपको कैसे देख सकते हो? तुम अपने को प्रतिबिम्बित भर कर सकते हो। इस तरह यह सारा विश्व एक शाश्वत सत्ता आत्मा की प्रतिच्छाया मात्र है । और चूंकि प्रतिच्छाया अच्छे या बुरे प्रतिफलक पर पड़ती है, इसलिए तदनुरूप अच्छे या बुरे बिम्ब बनते हैं । अगर कोई व्यक्ति हत्यारा है, तो उसमें प्रतिफलक बुरा है न कि आत्मा। दूसरी ओर अगर कोई साधु है, तो उसमें प्रतिफलक शुद्ध है। आत्मा तो स्वरूपतः शुद्ध है । एक वही सत्ता है, जो कीट से लेकर पूर्णतया विकसित प्राणी तक में प्रतिबिम्बित है । इस तरह यह संपूर्ण विश्व एक एकत्व एक सत्ता है; भौतिक मानसिक नैतिक आध्यात्मिक – हर दृष्टि से । इस एक सत्ता को ही हम विभिन्न रूपों में देखते है, अपने मन से अनेक बिम्ब इस पर अध्यस्त करते है। जिस प्राणी ने अपने को मनुष्यत्व तक ही सीमित रख लिया है, उसे ऐसा लगता है कि यह संसार मनुष्यों का है। किन्तु जो चेतना के उच्चतर स्तर पर है, उसे यह संसार स्वर्ग- सा दीखता है । वस्तुतः एक ही सत्ता या आत्मा अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । इसका न तो आना होता है, न जाना। न यह पैदा होती है, न मरती है और न पुनः अवतरित होती है । आखिर यह मर भी कैसे सकती है? यह जाए, तो कहाँ जाए? संसार और स्वर्ग आदि सारे स्थानों की व्यर्थ कल्पना तो हमने कर रखी है। न तो, वे कभी रहे है न अभी हैं और न भविष्य में कभी होंगे।
मैं सर्वव्यापी हूँ शाश्वत हूँ । मैं जा ही कहाँ सकता हूँ? मैं कहाँ नहीं हूँ? मैं तो प्रकृति की पुस्तक को पढ़ रहा हूँ । पृष्ठ पर पृष्ठ उलटता जा रहा हूँ, और जीवन का एक एक स्वप्न समाप्त होता जा रहा है। एक पन्ना पढ़ता हूँ, एक स्वप्न समाप्त होता है; और इसी तरह यह क्रम जारी है। जब सारी पुस्तक पढ़ डालूँगा तो उसे लेकर एक किनारे रख दूँगा – यही मेरे खेल का अन्त होगा। आखिर वेदान्तियों के इन सारे कथनों का तात्पर्य क्या है? आत्मा का श्रेष्ठत्व। संसार में जो देवता कभी पूजे जाते थे, या पूजे जाएँगे, उन्हें निकाल बाहर कर वेदान्तियों ने उनके स्थान पर मनुष्य की आत्मा को आसीन किया, वही आत्मा, जो चन्द्र, सूर्य और स्वर्ग की तो बात ही क्या, अखिल ब्रह्माण्ड से भी श्रेष्ठ है। सम्पूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होनेवाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। वह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है एकमात्र वही ईश्वर है, जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। इसलिए मैं किसी अन्य की नहीं, बल्कि अपनी ही पूजा करूँगा। ‘मैं अपनी आत्मा की पूजा करता हूँ – यही वेदान्ती कहता है। मैं किसे नमन करूँ? स्वयं को। मैं सहायता माँगू भी, तो किससे? कौन मुझ एकमात्र अपरिमेय सत्ता को सहायता देनेवाला है? ये सब केवल भ्रम और स्वप्न हैं । कब, किसने, किसकी सहायता की है? कभी नहीं। अगर तुम द्वैतवाद में विश्वास करनेवाले किसी कमजोर प्राणी को गिड़गिड़ाते और स्वर्ग से सहायता की भीख माँगते देखो, तो यही समझो कि वह व्यक्ति नहीं जानता कि स्वर्ग उसके भीतर ही है । यह ठीक है कि उसकी याचना सार्थक भी होती है, उसे सहायता मिलती है – पर वह सहायता स्वर्ग से नहीं, अपितु उसके अन्दर से ही आती है। भ्रमवश वह समझ लेता है कि वह बाहर से आती है। एक उदाहरण लो। कोई रोगी है। उसे किवाड़ खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है, वह जाकर किवाड़ खोलता है, पर उसे कोई नहीं दीखता। वह लौटकर आ जाता है। पर फिर खटखटाहट होती है और वह जाकर दरवाजा खोलता है। पर फिर कोई नहीं दीखता। इस बार वह आकर सोता है, तो पाता है कि वह खटखटाहट स्वयं उसके हृदय की धड़कन है। इसी तरह आदमी भ्रमवश अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्कर समाप्त होता है, तो वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वह दर दर भटकता रहा वन-प्रान्तर तथा मन्दिर-मस्जिद को छानता रहा, जिसे वह स्वर्ग में बैठकर संसार पर शासन करनेवाला मानता रहा, वह कोई अन्य नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा है। वह मैं है, और मैं वह। मैं ही (जो आत्मा हूँ) ब्रह्म हूँ, मेरे इस तुच्छ ‘मैं’ का कभी अस्तित्व नहीं रहा।
तथापि, किस प्रकार वह पूर्ण ब्रह्म भ्रमित हुआ है? वह भ्रमित नहीं हुआ। किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म स्वप्न देख सकता है? उसने कभी स्वप्न नहीं देखा। सत्य कभी स्वप्न नहीं देखता। यह प्रश्न ही कि आत्मा को भ्रम कैसे हुआ, बेतुका है। भ्रम से भ्रम की उत्पत्ति होती है। पर जैसे ही सत्य का दर्शन होता है, भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम सदा भ्रम पर आधारित रहता है; सत्य, ईश्वर तथा आत्मा कभी उसके आधार नहीं हो सकते। तुम कदापि भ्रम में नहीं हो; वही भ्रम है, जो तुममें तुम्हारे सम्मुख है। एक बादल है; दूसरा आता है और उसे हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है। फिर दूसरा आता है और पहले को हटा देता है। जैसे अनन्त नीले आकाश में रंगारंग बादल आते हैं, क्षण भर ठहरते हैं और अन्तर्हित हो जाते हैं । पर आकाश ज्यों का त्यों शाश्वत नील रूप से विद्यमान रहता है, वैसे ही तुम भी शाश्वत पूर्णता और शुद्धता के साथ विद्यमान हो, यद्यपि भ्रम के बादल आते-जाते रहते हैं। तुम्हीं वास्तविक विश्वदेवता हो, यही नहीं, दो की भावना ही अयथार्थ है – एक ही तो सत्ता है। ‘तुम और मैं’ कहना ही गलत है, केवल ‘मैं’ कहो। मैं ही तो करोड़ों मुँह से खा रहा हूँ, फिर मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो करोड़ों करों रो काम कर रहा हूँ, फिर मैं निष्क्रिय कैसे हो सकता हूँ? मैं ही समस्त विश्व का जीवन जी रहा हूँ, मेरे लिए मृत्यु कहां है? मैं जीवन और मृत्यु के परे हूँ। मैं मुक्ति की खोज कहाँ करूँ? मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूँ । मुझे इस विश्व के ईश्वर को – बांध कौन सकता है? संसार के धर्मग्रन्थ मानो छोटे छोटे नक़्शे है, जो मेरी महिमा को, मुझ अनन्तविस्तारी सत्ता को चित्रित करने का प्रयास करते हैं । ये पुस्तकें मेरे लिए क्या है? अद्वैतवादी इस प्रकार कहते हैं ।
‘सत्य को जान लो और क्षण भर में मुक्त हो जाओ। ‘सारा अज्ञान भाग जाएगा। जब एक बार मनुष्य विश्व की अनन्त सत्ता से अपने को एकीभूत कर लेता है, जब विश्व की सारी पृथक्ता विनष्ट हो जाती है, जब सारे देवता और देवदूत, नर-नारी, पशु और पौधे उस ‘एकत्व’ में विलीन हो जाते हैं – तब कोई भय नहीं रह जाता। क्या मैं अपने आपको चोट पहुँचा सकता हूँ? अपने को मार सकता हूँ? क्या मैं अपने को आघात पहुँचा सकता हूँ? डरना किससे? अपने आपसे डर कैसा? जब ऐसा भाव आ जाएगा, तब समस्त दुःखों का अन्त हो जाएगा। मेरे दुःख का कारण क्या हो सकता है? मैं ही तो समस्त विश्व की एकमात्र सत्ता हूँ । तब किसी से ईर्ष्या नहीं रह जाएगी; क्योंकि ईर्ष्या किससे? स्वयं से? तब समस्त अशुभ भावनाएँ समाप्त हो जाएँगी । किसके विपक्ष में मैं अशुभ भावना रख सकता हूँ? स्वयं के विरुद्ध? विश्व में मेरे सिवा और है कौन? और वेदान्ती कहता है कि ज्ञानप्राप्ति का यही एकमात्र मार्ग है। विभेद के भाव को विनष्ट कर डालो यह अन्धविश्वास कि विविधता, का अस्तित्व है, समाप्त कर डालो । “जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है, जो इस अचेतन जड़ पिण्ड में एक ही चेतना का अनुभव करता है एवं जो छायाओं के जगत में ‘सत्य’ को ग्रहण कर पाता है केवल उसी मनुष्य को शाश्वत शान्ति मिल सकती है और किसी को नहीं और किसी को नहीं ।”2
ईश्वर के सम्बन्ध में भारतीय दर्शन ने जो तीन कदम उठाये उनकी ये ही प्रमुख विशेषताएँ है। हमने देखा कि इसका प्रारम्भ ऐसे ईश्वर की कल्पना से हुआ, जो सगुण व्यक्ति है तथा विश्व से परे है । यह दर्शन बृहद ब्रह्माण्ड से सूक्ष्म ब्रह्माण्ड – ईश्वर – तक आया जिसे विश्व में अन्तर्व्याप्त माना गया। और अन्त में आत्मा ही को परमात्मा मानकर संपूर्ण विश्व में एक सत्ता की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया गया। वेदों की यही चरम शिक्षा है। इस तरह यह दर्शन द्वैतवाद से प्रारम्भ होकर विशिष्टाद्वैत से होता हुआ, शुद्ध अद्वैतवाद में विकसित होता है । हम जानते हैं कि संसार में बहुत कम लोग ही इस अन्तिम अवस्था तक आ सकते हैं या इसमें विश्वास करने का साहस रख सकते है, और इसे व्यवहार में लानेवाले तो उनसे भी विरल है । फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि सम्पूर्ण नीतिशास्त्र और आध्यात्मिकता का रहस्य यही है। क्यों सब लोग कहते हैं – “दूसरे की भलाई करो?” इसका कारण कहाँ है? क्यों सभी महान व्यक्ति मानवजाति में विश्वबस्त्व की शिक्षा देते है और महत्तर व्यक्ति समस्त प्राणियों में? कारण यह है कि चाहे वे जानें या न जानें, पर उनकी हर धारणा उनके हर तर्कहीन एवं वैयक्तिक अन्धविश्वास के मूल में निहित एक आत्मा का शाश्वत प्रकाश बार बार अपनी अनन्त व्यापकता को प्रकट करता है, अनेक रूपों में विद्यमान अपनी एक सत्ता का प्रतिपादन करता है ।
फिर भारतीय दर्शन अपनी चरमावस्था पर पहुँचकर विश्व की यों व्याख्या करता है : विश्व एक ही है, पर इन्द्रियों को यह भौतिक लगता है, बुद्धि को आत्माओं का संग्रह दीखता है और आध्यात्मिक दृष्टि से ईथर के रूप में प्रकट होता है । उस व्यक्ति को जो अपने ऊपर पापों का परदा डाले रहता है, यह गर्हिर्त लगेगा; किन्तु जो सतत आनन्द की खोज में है, उसे यह स्वर्ग सा लगेगा और जो आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः विकरित है, उसके लिए यह सब अन्तर्हित हो जाएगा उसे, केवल अपनी ही आत्मा का विस्तार प्रतीत होगा।
अभी वर्तमान समय में समाज की जैसी स्थिति है, उसमें दर्शन की इन तीनों अवस्थाओं की नितान्त आवश्यकता है; ये अवस्थाएं परस्परविरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। अद्वैतवादी अथवा विशिष्टाद्वैतवादी यह नहीं कहते कि द्वैतवाद गलत है। वे कहते हैं कि द्वैतवाद भी ठीक ही है, पर कुछ निम्न स्तर का। यह भी सत्य ही की ओर ले जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना जीवनदर्शन अपने विचारों के अनुसार निश्चित करने की स्वतन्त्रता है। तुम किसी को आघात मत पहुँचाओं, किसी की स्थिति को अस्वीकार मत करो; जिस स्थिति में वह है, स्वीकार करो और यदि तुम कर सकते हो, तो उसे अपने हाथों का सहारा दो और उसे एक उच्चतर स्तर पर ले जाओ, पर उसे हानि न पहुँचाओ और उसे विनष्ट मत करो। अन्त में तो सब को सत्य को पाना ही है। “जब सारी वासनाओं का अन्त हो जाएगा, तब वह नश्वर मानव ही अमर बनेगा”3 – तब यह मानव ही ईश्वर बन जाएगा।
मुण्डक उपनिषद १ । १ ।७
कठोपनिषद् २ । २ । १३
कठोपनिषद ;२ । ३ । १४