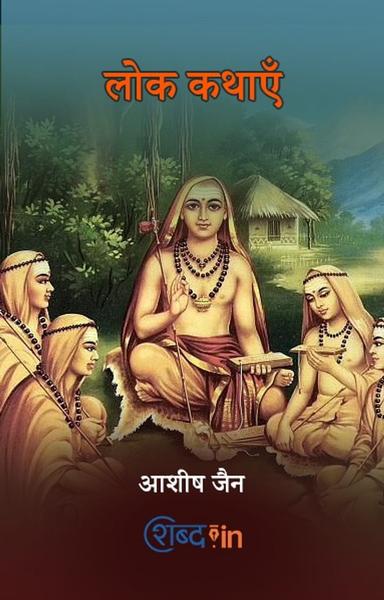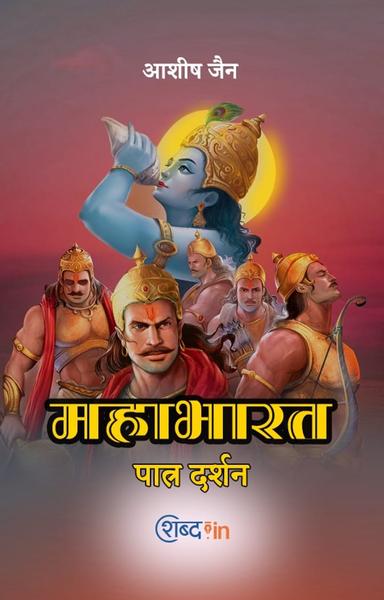मैं कृष्ण
मेरी माता देवकी मुझसे पहले हुए छः पुत्रों को दुलार करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकी थी। उसकी अदम्य इच्छा जानकर मैंने देव-साधना की, और इससे देवकी को आठवाँ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम गजसुकुमाल था।
सोमा नामक अति रूपवान ब्राह्मण कन्या के साथ मेरे प्यारे से छोटे भाई गजसुकुमाल का संबंध बाँधा गया था। परंतु परमात्मा नेमिनाथ जी की एक ही देशना को सुनकर संसार से अत्यंत विरक्त होकर गजसुकुमाल ने तुरंत ही माता देवकी को मनाकर दीक्षा ले ली थी। संयमजीवन के अल्पकाल में ही मुनि गजसुकुमाल सोमा के पिता सोमशर्मा के क्रोध की बलि चढ़ गये थे। सिर पर सुलगते अंगारे भरकर ध्यानस्थ गजसुकुमाल मुनि को उसने जिंदा सुलगा दिया था। मोक्ष की पघड़ी बाँधने वाले श्वसुर का उपकार मानते हुए वे मुनि कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में सिधारे थे। जिससे वैरागित होकर मेरी अनेक पट्टरानीयाँ और राजकुमारी राजीमती आदि हजारों आत्मायें संसार से विरक्त होकर दीक्षित बन गये थे।
मेरे पिता वसुदेव पूर्वभव में अपूर्व वेयावच्ची नंदिषेण मुनि थे। उस भव के तप-जप और वेयावच्च की अपूर्व साधना के बदले अंत समय में उन्होंने हजारों ललनाएँ अपने पीछे पागल हो जायें वैसे रूप की प्राप्ति का नियाणा बाँधकर जुआ खेला। इसीलिए ही वासुदेव अति सुंदर रूपवान राजकुमार थे। उनके पीछे हजारों युवतियाँ दीवानी रहती थीं। उनका पुत्र मैं कृष्ण और उनकी बहन कुन्ती मेरी बुआ लगती थी, जो पांड़वो की माता थी।
मैं कृष्ण :
इस भरत क्षेत्र में होने वाले आगामी तीर्थंकर देवों की चौबीसी में 12वें तीर्थंकर ‘अमम’ बनने का सौभाग्य मेरे सिर पर लिखा गया है। वर्तमान में मैं विशिष्ट कोटि का धर्मात्मा तो था ही, परंतु कुछ संयोगवश कर्मात्मा भी था। उभय स्वरूप मिश्रित मैं सम्यग्दृष्टि था। सम्यग्दर्शन भी उत्कृष्ट कक्षा के क्षायिकभाव का था।
मैं परमात्मा नेमिनाथ का परम भक्त होने के कारण मोक्ष पाने के एक मात्र लक्ष्यवाला था, और चारित्रधर्म जीवन का ही एक मात्र पक्षधर था। इस लक्ष-पक्ष के कारण एक बार मैंने अठारह हजार मुनिओं को वंदन किया था। मैंने मेरे राज्य में घोषणा करवाई थी कि माता पितादि की आजीविका की चिंता से यदि किसी धर्मात्मा की दीक्षा नहीं हो सकती हो तो उसे आजीविका की चिंता से सर्वथा मुक्त कर दूँगा।
इसके परिणाम से ढ़ेर सारे परिवारों में युवक-युवतियों की दीक्षा हुई थी।
यौवन की दहलीज पर कदम रखने वाली तमाम सुपुत्रियों को मैं सवाल करता था कि, ‘पुत्री ! तुझे रानी बनना है या दासी?’ बेटी कहती थी कि, ‘पिताजी ! मुझे तो रानी ही बनना होगा ना?’ ‘तो बेटी! तू परमात्मा नेमिनाथजी के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ले।’ ऐसा कहकर मैं हर एक सुपुत्री को संयम-मार्ग की ओर ले जाता था।
मैं आत्मश्लाघा नहीं करना चाहता, पर यदि आप मेरे जीवन में गहराइयों में झाँककर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैं असीम गुणों का स्वामी था। ये गुण भी मेरे गुणानुराग की वजह से मुझ में आये थे।
एक बार मैं हाथी पर बैठकर मैं राजमार्ग से गुजर रहा था। रस्ते पर मैंने एक मरी हुई, अत्यंत बदबूदार, भयंकर जुगुप्सनीय हड़काई कुत्ती का अस्थिपिंजर देखा, तो उसके दूध जैसे सफेद-मोतियों जैसे चमकते दांत देखकर आनंदविभोर होकर बोल पड़ा था कि ‘अहो! कितनी सुंदर दंतपंक्ति है!’ हकीकत में यह दैवी-माया थी। इसीलिए देव ने प्रसन्न होकर मुझ से कुछ माँगने को कहा, मैंने क्या माँगा, पता है?
‘रोगीजनों की रोगमुक्ति’
देव ने मुझे एक नगाड़ा दिया, जिसकी आवाज सुनने से रोगियों के रोग शांत प्रायः हो जायेंगे – ऐसा उसने कहा।
हर छः महीनों में यह नगाड़ा बजाने पर हजारों रोगियों के रोग शांत हो जाते थे। यह देखकर मेरी आत्मा आनंद से नाच उठती थी, मेरी आँखे हर्षाश्रु से छलक उठती थी।
तीर्थंकरों की आत्मा का यही तो स्वभाव होता है! वे दुःखीजनों को देखकर दुःखार्त हो जाते हैं, पापियों को देखकर उनको पापमुक्त कर देने की भावना से रच-पच हो जाते है। पूर्व भव के किसी भी भव में वे ऐसी असीम करूणा भावना से छलकते होते है
।मैं एक बार जंगल में हाथी पर बैठकर जा रहा था, वहाँ एक वृद्ध रस्ते से गुजर रहा। उसे अपना एक छोटा सा मकान बनाना था। गरीब होने के कारण एक-एक ईंट खुद उठाकर निश्चित जगह पर रखता था। लंबे अंतर के कारण वह अत्यंत हाँफ रहा था। उसे बार-बार बीच में विराम लेना पड़ता था। यह सब देखकर में दयार्द्र हो गया। त्रिखंडाधिपति के मेरे पद को भूलकर हाथी से उतरकर मैं खुद एक ईंट उठाकर चलने लगा। यह देखकर मेरे साथ के हजारों लोग एक-एक ईंट उठाकर चलने लगे। उस बूढ़े का काम पूरा हो गया। उसके चेहरे का आनंद देखकर मैं हर्षविभोर हो गया।
ऐसी विराट करूणा के कारण ही मैंने कुरुवंश के युद्ध को अंत तक रोकने के लिए सख्त प्रयत्न किये थे। यदि मैं पांड़वपक्ष में नहीं होता, मेरे दाव पेंचों की प्रचंड़ बुद्धिमत्ता नहीं होती तो मेरे बिना अर्जुन कर्ण को नहीं जीत सकता था। कृष्ण-नीति से ही, मतलब कि मेरी कुनेह से ही कर्ण को जीता गया था।
मेरे पास सम्यग्ज्ञान था, इसलिए युद्ध जनित संहार की कल्पना से मैं बराबर वाकिफ ही था, फिर भी नियति के आगे मुझे भी झुकना पड़ा। एक महासंहार (महाभारत) का तांड़व खेला गया।
सम्यग्दृष्टि जीवों को भोगों को भुगतना पड़ता है, युद्ध करने पड़ते हैं। लेकिन वे उनमें तीव्रता से आसक्त नहीं बनते, इसीलिए उन्हें अनासक्त कर्मयोगी कहते हैं।
बेशक ‘जैसे के साथ तैसा’, यह मेरी कृष्णनीति थी। अर्जुन के रथ के सफल सारथि के रूप में कुरुक्षेत्र में मैं पांडवों को विजय दिला सका था। पर अंदरोंदर यादवों के कलह को तो सख्त प्रयत्न करने के बाद भी मिटा नहीं सका था।
जीवन की ढलती संध्या में तो जैसे कि मेरा पुण्य खत्म ही हो गया था। द्वारिका का दहन हो गया, रथ में बैठकर भागने पर घोड़े की लगाम टूट गई, लाचार होकर माँ-बाप को भी बेसहारा छोड़ना पड़ा, बड़े भाई बलदेव को लेकर निकलना पड़ा। रस्ते में सख्त भूख लगी, तो बलदेव ने हाथ में पहने हुए कड़े को बेचकर भोजन का प्रबंध किया। भोजन के साथ क्षार प्रधान सूरा का सेवन करने से पानी की सख्त प्यास लगी। बलदेव पानी की तलाश में निकले। उस दरमियान मैं सफेद कंबल ओढ़कर किसी वृक्ष के नीचे पैर पर पैर चढ़ाकर सो गया। और, मेरे ही चचेरे भाई जराकुमार ने मुझे हरिण समझकर ज़हर लेपित बाण मुझ पर छोड़ा, जो मेरे पैर के आर-पार हो गया।
सख्त पानी की प्यास और सख्त पीड़ा के बीच द्वैपायन ऋषि के द्वारा सुलगायी हुई द्वारिका नजर समक्ष छाने लगी। द्वैपायन के पेट को चीरकर उसके उदर में से द्वारिका की ऋद्धि को बाहर लाने के रौद्रध्यान और कृष्ण लेश्या के बीच मेरी करूण मौत हो गई। कैसी बेमौत !
त्रिखंडाधिपति तीसरी नरक में पहुँच गया।
धर्मात्मा, भावी तीर्थंकर की आत्मा को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा।
क्या पता! कुरुक्षेत्र के मैदान पर गीता की रचना हुई थी या नहीं? जो हुआ वो। परंतु एक बात तय है कि, उस गीता के द्वारा जगत को दो जबरदस्त उपदेश मिले। मानवजगत के लिए यह अत्यंत उपयोगी भी है।
⇒ पहला उपदेश : अहंकार छोड़ने के द्वारा यशकीर्ति की आसक्ति का त्याग करना चाहिये।
⇒ दूसरा उपदेश : सहजता से स्वधर्म का पालन करना चाहिये। यही गीता का सार है !
जीव में दो प्रकार की आसक्ति होती है। रावण की तरह “पर में आसक्ति” और दुर्योधन की तरह “स्व में आसक्ति”। अपने ऊपर आसक्ति ‘मद’ से आती है, और दूसरों पर आसक्ति ‘मदन’ से आती है। जिसमें अहंकार है वो ही खुद में आसक्त होता है। उनको अपनी छवि बहुत प्यारी होती है। ऐसे इन्सान अपने स्वधर्म का अच्छी तरह पालन नहीं कर सकते।
स्वधर्म यानि औचित्य। उनका पालन सभी को करना चाहिये। पिता के रूप में पुत्र के लिए जो औचित्य होता है उसे पिता को पालना ही चाहिये। इस प्रकार पति-पत्नी, माँ-बेटी, साधु-संसारी, अतिथि, राजा-प्रजा, गुरु-शिष्य, शेठ-नौकर आदि सभी के स्वधर्म होते हैं। स्वधर्मों से भ्रष्ट नहीं होना चाहिये, यह बहुत बड़ा अधर्म है।
- स्वधर्मों का पालन करना लौकिक सौंदर्य है, धर्म की बुनियाद है।
- धर्म का आचरण, लोकोत्तर सौंदर्य है, जो मोक्ष की बुनियाद है।
- स्वधर्म प्रथम है, भले ही धर्म मुख्य हो।
श्री कृष्ण (मैंने) ने गीता द्वारा अर्जुन को दो बातें बतायी:
♦ तेरी ‘छवि’ (यश) की आसक्ति को तोड़ ड़ाल।
♦ क्षत्रिय के रूप के तेरे स्वधर्म का पालन कर।
इन दो चीजों के निराकरण के लिए, कहा जाता है कि जो उपदेश 700 श्लोकों में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिया वही ‘गीता’ है। धर्म तो बेशक श्रेष्ठ है, पर इससे स्वधर्मों की उपेक्षा थोड़े ही कर सकते हैं ! प्राथमिक कक्षा का धर्म तो स्वधर्मों का पालन ही है। उसके बिना लोकोत्तर सौंदर्य कैसे प्राप्त हो सकता है ?
‘संभवामि युगे युगे’ का प्रण लेकर बैठे हुए कृष्ण !
आप कहाँ अवतार लेते हैं ? धरती के सैंकड़ों अर्जुन आप के बिना हतप्रभ होकर, सर पर हाथ रखकर, दूर-सुदूर क्षितिज पर, आँखे तककर, निराश वदन से बैठे हैं। बेशक, आपके अवतरण होने में एक बहुत बड़ा विघ्न तो खड़ा ही है। कहीं आपका गर्भपात ना हो जाये।
पर इस अर्जुन को हिम्मत देने वाले श्री कृष्ण ! आप स्वयं हिम्मत मत हार जाना। वर्ना हम सभी की क्या हालत होगी !