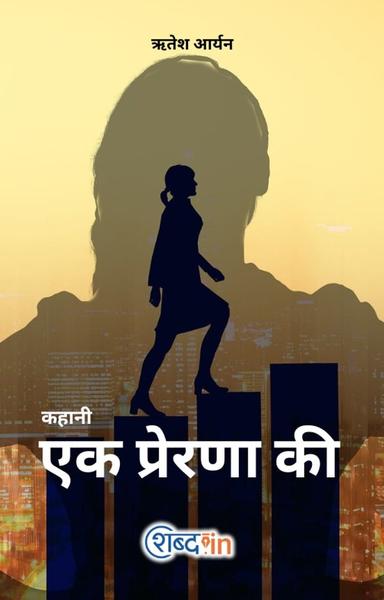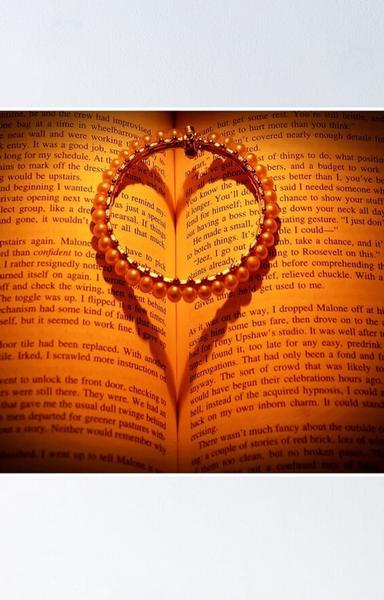याद हो आती है वो पहली फ़िल्म जिसे देखने के दौरान मानो शरीर की सुध बुध तक खो गयी थी । कथानक की बढ़ती गति में नायिका राधा का नई नवेली दुल्हन के रूप में अवतरण और घर की जिम्मेवारियों को निभाते हुए एक कुशल गृहणी की तरह परिवर्तित हो जाना ,मानो सब कुछ अपने घर के भीतर ही घटित हो रहा था । राधा के रूप में अभिनेत्री नरगिस जिंदगी के तमाम थपेड़ो से दो चार होते हुए नारी व्यक्तित्व के नए आयामों को स्पर्श करती हैं । एक नवयुवती से लेकर एक मां बनने के साथ साथ मदर इंडिया के रूप में उसका व्यक्तित्व एक मिसाल की तरह आज भी प्रासंगिक हो उठता है , भारतीय संस्कृति के आदर्शों के व्यावहारिक रूप की इतनी सुंदर प्रस्तुति विरले ही मिलती है ।समूची फ़िल्म पचास साठ के दशक के जिंदगी की जद्दोजहद को तो दर्शाती ही है लेकिन ये भी जतलाती है कि जिंदगी धूप में तपकर और छांव में साधकर ही निखरती है । अंधेरे और उजाले का चक्र एक निष्णात सच्चाई है ।
जंजीर , शोले ,दीवार से लेकर अस्सी और नब्बे के दशक में बदलती सिनेमाई तस्वीर एकल नही थी ये अपने साथ समाज को भी बदल रही थी या दूसरे शब्दों में कहे तो समाज का ही प्रतिविम्बन कर रही थी । अस्सी के दशक के राजनीतिक भूचाल और व्यवस्था के प्रति आक्रोश का प्रस्फुटन जहां अमिताभ बच्चन , विनोद खन्ना सरीखे नायक प्रदर्शित कर रहे थे । तो नब्बे के दशक में उदारीकरण और वैश्वीकरण ने निर्माता निर्देशकों को विश्व दर्शन करवाने के लिए खिड़कियां खोल दी थी । शिफॉन की साड़ी में नृत्यरत नायिका और सुटधारी नायक स्विट्ज़रलैंड में दृश्यमान होकर व्यवसायिक सफलता की गारन्टी माने जाने लगे थे ।
,
अदाकारों का पूरा चरित्र समाज पर और समाज के लोगों पर इस तरह प्रभाव छोड़ता आया है कि जहां केश सज्जा और वस्त्र परिधान समाज के एक व्यापक हिस्से द्वारा अनुसरित किया जाता रहा है वही नायक की मानवीय कमजोरियों को भी खुद में ढाल कर पूजित किया गया , देवदास के नायक का सीने पर हाथ रख कर खाँसना भी एक ट्रेंड बन कर छा जाना सोचने और विवश कर देता है ।
हर कालखंड का सिनेमा कॉमर्शियल और क्लासिकल यानी कल्पना और यथार्थ का संश्लेषण दर्शाता है । कल्पना उस कल्पित भविष्य की जिसमे अंधेरे का नामोनिशान ना हो सर्वत्र उजाला पसरा रहे तो यथार्थ उस कठोर भूतल से अवगत कराता है जिसमें बिना अंधेरों के उजाला एक स्याह झूठ की मानिंद प्रतीत होता है , वर्तमान शिल्पकारों में करन जौहर कल्पना तो अनुराग कश्यप यथार्थ के इन दो धाराओं के शीर्षतम प्रस्तुतिकर्ता के रूप में देखे जा सकते हैं ।
चाहे जो भी हो , हिंदुस्तान की पहली फ़िल्म आलम आरा और सत्यवादी हरिश्चन्द्र से शुरू हुई इस यात्रा ने अपने तकरीबन सौ सवा सौ काल के दरमियान समाज को करीब से ना सिर्फ बदलते देखा है बल्कि स्वयं भी इस बदलाव को जीया है । और समाज का कोई तबका इससे अछूता रहा हो ऐसा कोई भी चरित्र विरले ही देखने को मिलता है , गैंग ऑफ वासेपुर के प्रबल चरित्र रामाधीर भी "मैं सिनेमा नही देखता" बोलने के लिए सिनेमाई पर्दे के सहारा ले रहे होते हैं । यहां तक कि युग प्रवर्तक मोहनदास गांधी की के अबोधता के ऊपर भी पहली फ़िल्म हरिश्चन्द्र के नायक चरित्र ने बोधता की गहरी छाप छोड़ी थी ।
आज सिनेमा ने स्वयं को कई अन्य आयामों में विस्तारित कर लिया है । इंटरनेट पर भी वेब सीरीज का एक समानांतर स्वरूप विस्तृत हो रहा है , सेक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर , रंगबाज़ , अपहरण , असुर आदि आदि , अभिव्यक्ति के किस पहलू को ये धारा स्पर्श कर रही है । ये देखना वाक़ई दिलचस्प होगा । ये प्रश्न ठीक वैसे ही है जैसे भोजपुरी विद इस भाषा के अश्लील शब्दों की प्रस्तुति को लेकर ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं कि इसे भाषा और संस्कृति का प्रचार समझा जाये या दुष्प्रचार .... ? ...ये पहलू अलग विमर्श की मांग करता है ...
वास्तव में सिनेमा और समाज के इस संश्लेषण का विश्लेषण उस दौर के गुजरने के बाद विश्लेषित किया जाता रहा है ।
बहरहाल सूचनाएं व्यापक स्वरूप अख्तियार कर रही है । इन प्रवाहों की वास्तविक दशा क्या होगी ये तो आने वाला वक़्त ही निर्धारित करेगा । सिनेमा वस्तुतः एक अभिव्यक्ति है समाज की , व्यक्ति की । ये अभिव्यक्ति यदि नैसर्गिक रहे तो आने वाला समाज ऋणी रहेगा अपनी पूर्व संततियों के लिए ,हम पूर्वजों के लिए , एक ऐसी धरोहर के लिए जिसमे समाज की वास्तविक सच्चाई विद्यमान रही , जो निर्मुक्त रही अपने कालखंड की राजनीति से , निर्बाध रूप से जिसने समाज के हर पहलू को सलीके से स्पर्श किया । ठीक वैसे जैसे साहित्य भी रहा है । वरना लोदी के समय मे कबीर का राग ना सुना जा पाता, मुग़लिया खंड मे तुलसी और नानक मुखर ना हुए होते । अंग्रेजी शासन में प्रेमचंद और निराला अभिव्यक्त नही हो पाते । हालांकि कुछ तस्वीरें अभी भी धुँधली और स्याह है ,जिनसे गुजरते वक़्त यूँ भान होता है कि अभिव्यक्ति का गला घोंटा गया है उसके नैसर्गिक बहाव को अवरोधित किया गया है । कुछ पन्ने फाड़े गए कुछ इबारतें स्याह कर दी गयी है ।
सिनेमा की विधा समाज से एक सरल संवाद करती हुई विधा है । इन अर्थों में इसकी जिम्मेवारी भी काफी बड़ी हो जाती है , यह विधा इन उत्तरदायित्वों को अपने कंधो पर ढो लेगी इसका पूरा विश्वास हम सभी को है । हम सभी को भी ऐसा समाज निर्मित करना होगा । चलचित्र से कल का चित्र सुंदर और मनोहारी निर्मित होगा ऐसा यकीन सुधिजनों को भी है ~
Writer - Ritesh Ojha
Place - Delhi
Contact - aryanojha10@gmail.com