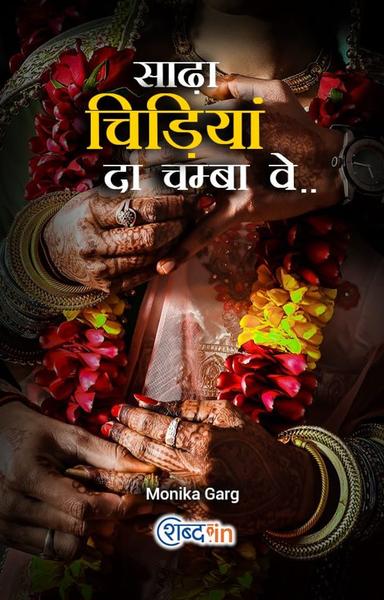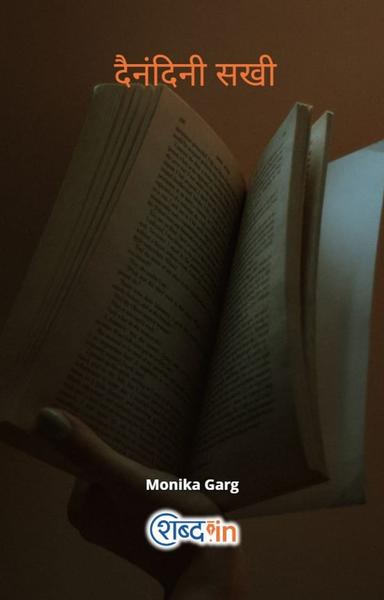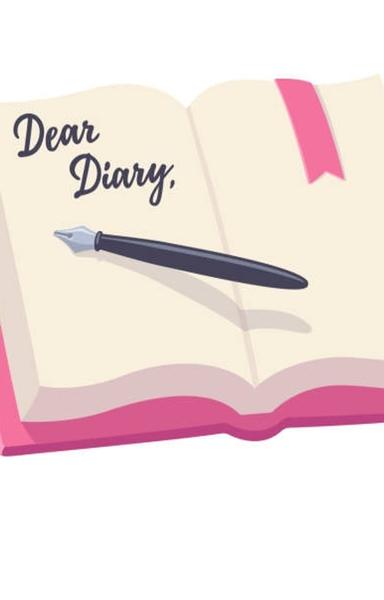प्रिय सखी ।
कैसी हो ।हम अच्छे है ये महीना तो तुम्हारी हमारी मुलाकात का आखिरी महीना है।चल मन की बातें मन लगाकर करेंगे।
आज का विषय:- पाश्चात्य संस्कृति:- वरदान या अभिशाप
पाश्चात्य संस्कृति विदेशी नववधू की तरह है।
विदेशी नववधू के आकर्षण ने कुछ ऐसा जादू किया कि हम जन्म देनेवाली, पाल- पोसकर बड़ा करनेवाली अपनी माँ को ही भूल बैठे । पाश्चात्य सभ्यता के प्रकाश में हमारी चकाचौंध बुद्धि ने अपना सर्वस्व उसी के चरणों में न्योछावार कर दिया ।
प्रत्येक देश का अपना एक वातावरण होता है; उसकी अपनी एक प्रकृति होती है और उसी के अनुकूल वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा होती है । पाश्चात्य देशवासियों ने ठंडे देश में उत्पन्न होने के कारण कोट-पैंट-टाई से शरीर कोअधिक-से-अधिक कसने में ही अपना कल्याण देखा और उन्होंने ठीक ही किया, किंतु उष्ण देश के निवासी भारतीयों ने उनका अपने स्वास्थ्य और धन का अपव्यय ही किया; पिछलग्गू बनने की उपाधि से अपने आपको विभूषित किया । बहरहाल, इस पहनावे को भारतवासी अब आत्मसात् कर चुके हैं ।
प्राचीन मनीषियों ने हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो अचूक नुस्से बनाए थे, वे भारतीय मिट्टी से मेल खाते हैं । वे यहाँ की जलवायु के अनुकूल भी हैं । उनमें हमारे पूर्वजों के सारे संस्कार निहित हैं । वे सभी प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी हैं । उनसे श्रेयस और नि: अयस दोनों की प्राप्ति हो सकती है । स्वास्थ्य ही संसार में सारे सुखों का मूल है । इसी क्षेत्र में, आयुर्वेद में बताए गए नुस्से या औषधियाँ कम खर्च में तैयार होती हैं ।
वे हमारे स्थायी स्वास्थ्य का सृजन करती हैं, क्योंकि वे यहाँ के वातावरण और जलवायु के अनुकूल हैं । वे रोग को समूल नष्ट कर स्थायी प्रभात छोड़ती हैं, किंतु विदेशी रंग में रँगे हम लोगों ने क्षणिक उत्तेजना देनेवाली अस्थायी प्रभाव से युक्त, महँगी विदेशी वस्तुओं और औषधियों को स्वीकार कर अपना स्वास्थ्य और धन ही नष्ट नहीं किए अपितु अपने आर्थिक ढाँचे को भी अस्वस्थ, असंतुलित और जर्जर बना डाला ।
विदेशी इंजेआनों को अपने शरीर के रक्त-मांस में आत्मसात् करवाकर विदेशी चरणों में अपना मस्तिष्क भी बेच दिया । विदेशी धन- धान्य से संपन्न हो गए और हम अपने अज्ञान से भूखों मरने लगे । हमने अपना स्वास्थ्य खोया, धन खोया, अपनी अमूल्य संस्कृति और सभ्यता खोई, फिर भी हम मिथ्याभिमान में तने रहे । हम सरीखा वज्र मूर्ख दूसरा कौन होगा ? हमने महँगी विदेशी शिक्षा लेकर तर्कवाद के माध्यम से अपनी ही संस्कृति के सिर धूल डाली ।
उसे मृत घोषित किया; हृदय का पल्ला छोड्कर हम जितना ही मस्तिष्क की ओर खिंचते गए उतने ही सभ्य और शिष्ट बने । जितना ही अधिक हमने पड़ा उतनी ही मात्रा में छल, मिथ्याभिमान और बुद्धिवाद के सहारे सही को गलत सिद्ध करने की योग्यता हममें आती गई । हम बुद्धिवाद के स्वामी बने, भले ही व्यावहारिक, नैतिक और सात्विक ज्ञान में शून्य रहे ।
पाश्चात्य आदर्शो की भित्ति एकमात्र विज्ञान पर टिकी हुई है । विज्ञान के ही बल पर वह इतराती है, किंतु सुख और सुविधा के नाना साधनों के होते हुए भी वह चंचल और अशांत है । भोग से परे भी कोई वस्तु है, यह उसे सोचने की फुरसत ही नहीं । मोटर, महल, रेडियो, टी.वी. वीडियो, मोबाइल, कंप्यूटर, रेल, सिनेमा, हवाई जहाज, बड़े-बड़े अस्पतालों, कारखानों और ज्ञानराशि के होते हुए भी हम छिछले हैं; विषण्ण है । ऐसी कोई वस्तु है, जो हमें नहीं मिल रही है ?
आज के युग का मानव सड़कों पर दौड़ रहा है, वह अपने रुकने की जगह जानता ही नहीं । जब हम इतिहास के माध्यम से अपने पूर्वजों के जीवन के विषय में पढ़ते हैं तब हमें महान् आश्चर्य इस बात पर होता है कि जितनी सुविधाएँ आज हमें प्राप्त हैं, उनकी शतांश भी उन्हें प्राप्त न थीं, फिर भी वे जीवन से संतुष्ट थे और अपने आप में भरे-पूरे थे । उनका अपना एक ध्येय था ।
वे शांति को पा चुके थे तथा अपने लक्ष्य-सीमाओं को समेटकर बैठे थे । जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान इस जीवन मंत्र को पचाकर अपने अंतःकरण में उतार चुके थे, किंतु विज्ञान-युग के पाश्चात्य आदर्शो में पले हम तरंगों में बहे जा रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे की जमीन गायब है ।
हम देखते हैं कि टेलीफोन और टेलीविजन के संयोजन से दूराउई की बाधा को तोड़कर मनुष्य-मनुष्य की आवाज ही नहीं सुन सकते हैं, बल्कि वे परस्पर एक-दूसरे को देख भी सकते हैं । मिलने के ऐसे सुलभ साधनों के होते हुए यदि मानव के बीच हार्दिक और आत्मिक मिलन नहीं हो पा रहा है तो यह महान् आश्चर्य की बात है ।
पाश्चात्य आदर्शो ने जितना हमें ज्ञान दिया है उतना ही व्यस्त रहना भी सिखा दिया है । ‘शांति’ नाम की चीज हम सुनते भर हैं, कभी अनुभव करने का अवसर नहीं पाते और न उसकी कुछ आवश्यकता ही समझते हैं । हलचल और शोरगुल से भरे हुए नगरों में प्रलोभन और मन-बहलाव के जो लाखों उपकरण उपलब्ध हैं, वे मनुष्य को चौबीस घंटे एकांत से अलग उस भीड़ में व्यस्त रखते हैं, जिसकी विशेषता यह है कि उसे सोचने और चिंता करने की कमी कभी अनुभव ही नहीं होती ।
मन के भीतर जो आत्मा नाम का देवता है, दिन भर का हिसाब-किताब देने के लिए हमने उसकी बैठक में जाना छोड़ दिया है । हमारे पुरखे पाप करते हुए भी डरते थे, क्योंकि पाप को वे ‘पाप’ समझते थे, किंतु हम पाप-पुण्य को नहीं मानते ।
हमने उस युग के नीतिशास्त्र को त्रुटिपूर्ण और अव्यावहारिक समझकर एक पृथक् नीतिशास्त्र का निर्माण कर लिया है, जिसमें बुद्धि का प्राधान्य है । ‘आत्मा’ नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा हमारा विश्वास हो गया है । अत: हमने उसका पूर्णतया बहिष्कार भी कर दिया है और इसीलिए हम लंदन के चौक पर के घड़ियाल की तो आवाजें रेडियो पर सुन लेते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी की आह और कराह हमें सुनाई नहीं पड़ती ।
इसलिए कहती हूं सखी अपनी जमीन और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना ही हम भारतीयों के खून मे है।अब चलती हूं सखी अलविदा।