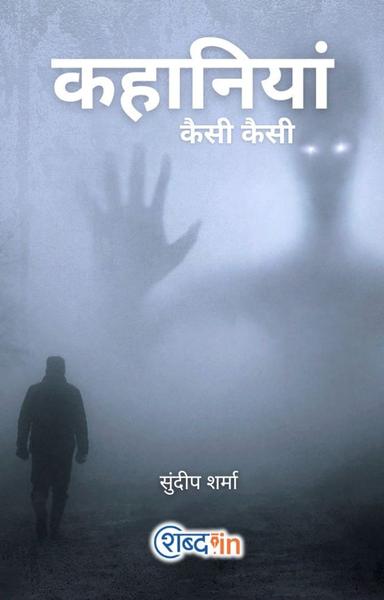शीर्षक:- आज़ाद या महज ख़्वाब।।
उसने उसको बंद पिंजरे से निकाल,
ऐसा खुला समंदर दिखाया, जिसका कोई आसमां तक न था,
था तो खुलापन काफी ,बेहद काफी, पर टुकड़ा जमीं का जरा पास तक न था।।
वो खुश तो थी बहुत आकर पिंजरे से बाहर,
पर बे मतलब की उड़ान, आकाश के पार जाकर भी सुकून का कतरा न दे पाई,,
वहां थी जो रोशनी वो भी थी सब की सब अंधेरे मे ही समाई।।
और उसे बड़ी चतुराई से बताया गया कि तुम कैद हो, तुम्हे खुलना होगा,,उड़ना होगा,तुम्हे बंधन तोड़,मुक्त होना होगा,,।।
कितना भला था न खेलना उसके जज़्बातों के साथ, बता कर यह सच दिखने वाला खास का राज।।
वह भोली, समझ अपना हमजोली, फिर छली गई, जो थी सम्मान की पूज्या वो उपभोग की वस्तु अंततः बना दी क्या थी गई।।
पहले उसने उसे वसन से मुक्त कराया,
अश्लीलता की परिभाषा बदल सैक्सी का नया आदर्श समझाया,
फिर वासनात्मक नजरिए को खुलापन कह, उसको खूब रिझाया।।
जो पहले अश्लील के मायने था,अब उसे सुंदर व आधुनिक बताया,
इतना ही नही,उस पर किरदार हल्का करने को विचारों मे भी ज़हर मिलाया।।
आधुनिक,
जी हाँ अध्यात्मिक से अत्याधुनिक का चोला उड़ाया, और फिर सरेआम, करने को उपभोग, उसे बाज़ार का स्वाद बाज़ार मे लाकर चखाया।।
स्वाद भी कैसा,उन्मुक्तता का सबब ऐसा,
जिसकी खेह नही,
अब छोटे कपड़ो मे भी छिपती उसकी देह नही,,
और फैशन बता उसके सभी रंगो से सजा मेला,
जिसके लिए खर्च करने होते थे ढेरों पैसे,
उससे पाकर निजात, सरेबाजार उसके ही जज़्बात व अंगों तक से खूब खेला।।
और भी देखिए, जब यह हवस, वयस्क से बाल्यकाल की और आई,तो बच्चियां तक न रही महफूज तो गुड टच,बैड टच की बात आई।।
पर कभी सोचा यह नौबत ही क्यू आई।।
यहां पूज्या थी,बच्चियां कंजक के रूप मे,
यौवन खेलता था,आंगन महफूज से,
वहा वहशत चली ही कैसे आई।।?।।
न ,सोचा न,अभी शायद आधुनिकता, बाक़ी है,
जी यह आधुनिकतम फूहड़ता,की जो स्वतंत्रता है, यह नाकाफ़ी है।।
असल मे पर कटे पंछी की कैद जिसके बदन नग्न और जिस्म की हो सैर,
ऐसे मुकाम, लकीरो से खींचने थे,
तन पर जो सजते थे वस्त्र, वो चीथड़ो मे बदल दरअसल उसके निज अंग भींचने थे।।
उसी की जद्दोजहद को आसान कर दिया,
रे नारी देख तुझे तेेरे पिंजरे से कैसे आज़ाद कर दिया।।
माहौल का माखौल है,सोने से पीतल होती,का अफसोस है,
क्या बंद तब थी बंधन मे,जब रीति-रिवाज के नाम ,हर घर तुम्हारी हँसी गूंजती थी,
सलाह लेनी होती पिता से तो बच्चो की माँ पिता से यूँ पूछती थी।।
"अरे सुनते हो यह मुनिया कुछ कहती है। "
दबी आवाज सही पर उसमे उसकी सहमति सम्मति सजी रहती है।।
यही था आजाद ख्याल का खुलापन, जिसमे नम्रता के साथ विश्वास था,उन्मुक्त था ,जिसे बताया गया कारावास क्या उपयुक्त था।?।
और इधर अब ,जब बदल कर हद, सूटकेसो मे,छद्म वेषों मे,तुम्हारे खुद के टुकड़े देख औरत के न ऑसू सूखते है,
यह कैसी है आजादी, यहां तेरे टुकड़े तेरे ही आज़ाद कराने वाले बीनते है।।
चिल्लाती चींख के भी कान बोलते क्यो नही है,
यह तेरी स्वतंत्रता के परिणाम सोचते क्यो नही है।?।
तुम क्या थी,
आज क्या हो,?
बंद तब थी,
या कि आज हो,?,
माना कमाना मजबूरी थी,पर कीमत क्या लगी कोई पूरी थी,।?।
सवाल कौंधता है,
पर भेड़चाल मे कौन, बोलता है।।
कभी सोचना क्या पाया क्या ,अपार पैसा भी जो तो कर गया पराया ।।
माना तुम स्वछंद हो गई हो,पर जानती भी हो किसकी अनुबंध हो गई हो।?।
प्रकृति को तुुम ठुकरा नही सकती, और वापिस अब तुम जा नही सकती,
ऐसे मे कोई हल हो तो सोचना,
कारण, भोक्ता बैठा है उपभोक्ता बन कर,तुम्हे खुद ही खेत अपना है जोतना।।
मेरी मानों ,तो ,शक्ति हो, तुम तो ,अपना विस्तार करो,
जो सजाए ख़्वाब, तुम्हारे,अपने ,उनका ,आगाज करो,
पहले सोचो और फिर,जोरदार, वार करो।।
और शक्ति बनी हो तो, पुरुष को स्वीकार करो,
पोषण करो उसका ऐसा कि जो चाहो जैसा चाहो वैसा सहर्ष स्वीकार करो।।
अरे कोई तो विवेकानंद तैयार करो।।
तुम जननी हो,जनती हो आकाश से लेकर दो बूंद, सजती हो,इसी सुसज्जित
सुसंस्कृत संस्कृति का निर्माण करो,,और
इसी सज्जा का सम्मान करो,।।
हरकोई तुम्हे पूजे ऐसे पुरुष तुम खुद ही करा कर स्तनपान, असली पुरुषत्व तैयार करो।।(3)
=/=
मौलिक रचनाकार,
संदीप शर्मा।।
देहरादून उत्तराखंड।