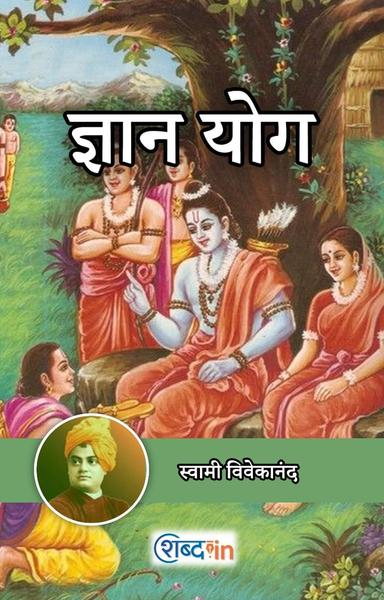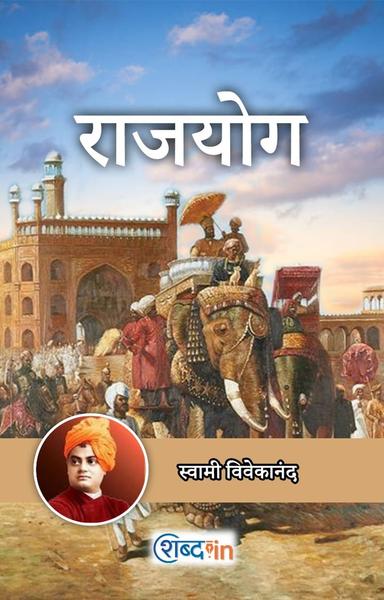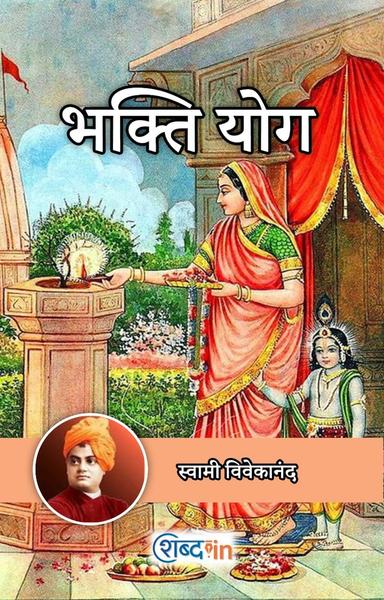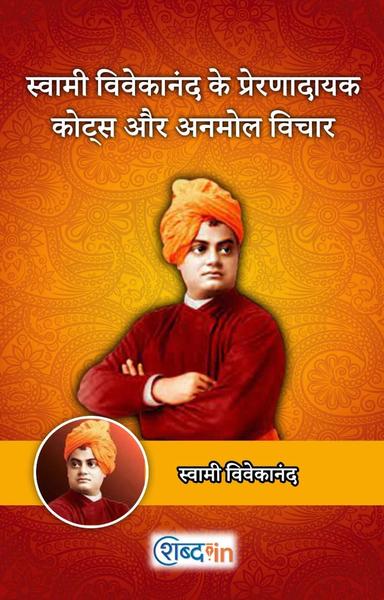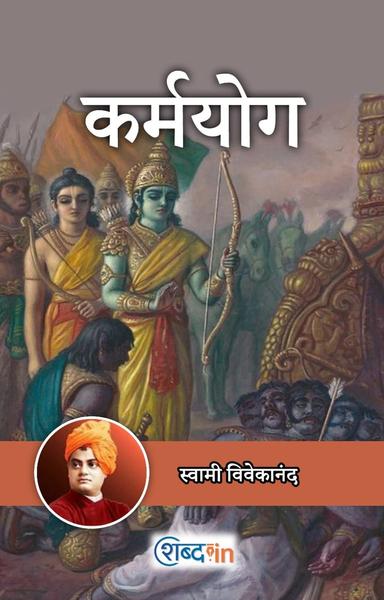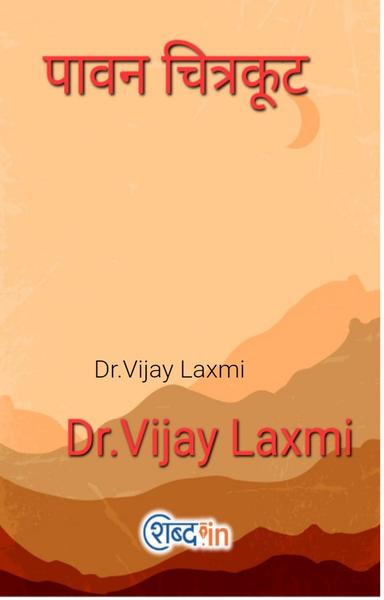“ईश्वर का स्वरूप” नामक स्वामी विवेकानंद कृत भक्ति योग का यह तीसरा अध्याय है। इसमें स्वामी जी बता रहे हैं कि भक्ति के लिए ईश्वर का स्वरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही इस अध्याय में वे विभिन्न भारतीय दार्शनिक धाराओं के अनुसार ईश्वर के स्वरूप की विवेचना कर रहे हैं।
ईश्वर कौन हैं? “जिनसे विश्व का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है,”1वे ही ईश्वर हैं। वे “अनन्त, शुद्ध, नित्यमुक्त, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परमकारुणिक और गुरुओं के भी गुरु हैं,” और सर्वोपरि, “वे ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूप हैं।”2
यह सब व्याख्या अवश्य सगुण ईश्वर की है। तो क्या ईश्वर दो हैं? एक सच्चिदानन्दस्वरूप, जिसे ज्ञानी ‘नेति नेति’ करके प्राप्त करता है और दूसरा, भक्त का यह प्रेममय भगवान? नहीं, वह सच्चिदानन्द ही यह प्रेममय भगवान है, वह सगुण और निर्गुण दोनों है। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि भक्त का उपास्य सगुण ईश्वर, ब्रह्म से भिन्न अथवा पृथक् नहीं है। सब कुछ वही एकमेवाद्वितीय ब्रह्म है। पर हाँ, ब्रह्म का यह निर्गुण स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण प्रेम व उपासना के योग्य नहीं। इसीलिए भक्त ब्रह्म के सगुण भाव अर्थात् परम नियन्ता ईश्वर को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करता है। उदाहरणार्थ, ब्रह्म मानो मिट्टी या उपादान के सदृश है, जिससे नाना प्रकार की वस्तुएँ निर्मित हुई हैं। मिट्टी के रूप में तो वे सब एक हैं, पर उनका बाह्य आकार अलग अलग होने से वे भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं। उत्पत्ति के पूर्व वे सब की सब मिट्टी में गूढ़ भाव से विद्यमान थीं। उपादान की दृष्टि से अवश्य वे सब एक हैं, पर जब वे भिन्न भिन्न आकार धारण कर लेती हैं और जब तक आकार बना रहता है, तब तक तो वे पृथक् पृथक् ही प्रतीत होती हैं। एक मिट्टी का चूहा कभी मिट्टी का हाथी नहीं हो सकता, क्योंकि गढ़े जाने के बाद उनकी आकृति ही उनमें विशेषत्व पैदा कर देती है, यद्यपि आकृतिहीन मिट्टी की दशा में वे दोनों एक ही थे। ईश्वर उस निरपेक्ष सत्ता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, या यों कहिये, मानव-मन के लिए जहाँ तक निरपेक्ष सत्य की धारणा करना सम्भव है, बस वही ईश्वर है। सृष्टि अनादि है, और उसी प्रकार ईश्वर भी अनादि हैं।
वेदान्तसूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में यह वर्णन करने के पश्चात् कि मुक्तिलाभ के उपरान्त मुक्तात्मा को एक प्रकार से अनन्त शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यासदेव एक दूसरे सूत्र में कहते हैं, ‘पर किसी को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति प्राप्त नहीं होगी’, क्योंकि यह शक्ति केवल ईश्वर की ही है।3 इस सूत्र की व्याख्या करते समय द्वैतवादी भाष्यकारों के लिए यह दर्शाना सरल है कि परतन्त्र जीव के लिए ईश्वर की अनन्त शक्ति और पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना नितान्त असम्भव है। कट्टर द्वैतवादी भाष्यकार मध्वाचार्य ने वराहपुराण से एक श्लोक लेकर इस सूत्र की व्याख्या अपनी पूर्वपरिचित संक्षिप्त शैली से की है।
इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार रामानुज कहते हैं, “ऐसा संशय उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा को जो शक्ति प्राप्त होती है, उसमें क्या परम पुरुष की जगत्सृष्टि-आदि असाधारण शक्ति और सर्वनियन्तृत्व भी अन्तर्भूत हैं? या कि उसे यह शक्ति नहीं मिलती और उसका ऐश्वर्य केवल इतना ही रहता है कि उसे परम पुरुष के साक्षात् दर्शन भर हो जाते हैं? तो इस पर पूर्वपक्ष यह उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा का जगन्नियन्तृत्व प्राप्त करना युक्तियुक्त है; क्योंकि शास्त्र का कथन है, ‘वह शुद्धरूप होकर (परम पुरुष के साथ) परम एकत्व प्राप्त कर लेता है’ (मुण्डक उपनिषद्, ३।१।३)। अन्य स्थान पर यह भी कहा गया है कि उसकी समस्त वासना पूर्ण हो जाती है। अब बात यह है कि परम एकत्व और सारी वासनाओं की पूर्ति परम पुरुष की असाधारण शक्ति जगन्नियन्तृत्व बिना सम्भव नहीं। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि उसकी सब वासनाओं की पूर्ति हो जाती है तथा उसे परम एकत्व प्राप्त हो जाता है, तो हमें यह मानना ही चाहिए कि उस मुक्तात्मा को जगन्नियन्तृत्व की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस सम्बन्ध में हमारा उत्तर यह है कि मुक्तात्मा को जगन्नियन्तृत्व के अतिरिक्त अन्य सब शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जगन्नियन्तृत्व का अर्थ है – विश्व के सारे स्थावर और जंगम के रूप, उनकी स्थिति और वासनाओं का नियन्तृत्व। पर मुक्तात्माओं में यह जगन्निन्तृत्व की शक्ति नहीं रहती। हाँ, उनकी परमात्मदृष्टि का आवरण अवश्य दूर हो जाता है और उन्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभूति हो जाती है – बस यही उनका एकमात्र ऐश्वर्य है। यह कैसे जाना? शास्त्रवाक्य के बल पर। शास्त्र कहते हैं कि जगन्नियन्तृत्व केवल परब्रह्म का गुण है। जैसे – ‘जिससे यह समुदय उत्पन्न होता है, जिसमें यह समुदय स्थित रहता है और जिसमें प्रलयकाल में यह समुदय लीन हो जाता है, तू उसी को जानने की इच्छा कर – वही ब्रह्म है।’ यदि यह जगन्नियन्तृत्व-शक्ति मुक्तात्माओं का भी एक साधारण गुण रहे, तो उपर्युक्त श्लोक फिर ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जगन्नियन्तृत्व-गुण से ही उसका लक्षण प्रतिपादित हुआ है। असाधारण गुणों के द्वारा ही किसी वस्तु की व्याख्या होती है, उसका लक्षण प्रतिपादित होता है। अतः निम्नलिखित शास्त्रवाक्यों में यह प्रतिपादित हुआ है कि परमपुरुष ही जगन्नियमन का कर्ता है, और इन वाक्यों में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं, जिससे मुक्तात्मा का जगन्नियन्तृत्व स्थापित हो सके। शास्त्रवाक्य ये हैं – ‘वत्स, आदि में एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही था। उसमें इस विचार का स्फुरण हुआ कि मैं बहु सृजन करूँगा। उसने तेज की सृष्टि की।’ ‘आदि में केवल ब्रह्म ही था। उसकी उत्क्रान्ति हुई। उससे क्षत्र नामक एक सुन्दर रूप प्रकट हुआ। वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान – ये सब देवता क्षत्र हैं।’ ‘पहले आत्मा ही थी; अन्य कुछ भी क्रियाशील नहीं था। उसे सृष्टिसृजन का विचार आया और फिर उसने सृष्टि कर डाली।’ ‘एकमात्र नारायण ही थे, न ब्रह्म थे, न ईशान, न द्यावापृथ्वी, नक्षत्र, जल, अग्नि, सोम और न सूर्य। अकेले उन्हे आनन्द न आया। ध्यान के अनन्तर उनके एक कन्या हुई – दश-इन्द्रिय।’ ‘जो पृथ्वी में वास करते हुए भी पृथ्वी से अलग हैं, . . . जो आत्मा में रहते हुए . . . ’ इत्यादि।”4दूसरे सूत्र की व्याख्या करते हुए रामानुज कहते हैं, “यदि तुम कहो कि ऐसा नहीं है, वेदों में तो ऐसे अनेक श्लोक हैं, जो इसका खण्डन करते हैं, तो वास्तव में वेदों के उन-उन स्थानों पर केवल निम्न देवलोकों के सम्बन्ध में ही मुक्तात्मा का ऐश्वर्य वर्णित है।”5 यह भी एक सरल मीमांसा है। यद्यपि रामानुज समष्टि की एकता स्वीकार करते हैं, तथापि उनके मतानुसार इस समष्टि के भीतर नित्य भेद है। अतएव यह मत भी कार्यतः द्वैतभावात्मक होने के कारण, जीवात्मा और सगुण ब्रह्म (ईश्वर) में भेद बनाये रखना रामानुज के लिए कोई कठिन कार्य न था।
अब इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध अद्वैतवादी का क्या कहना है, यह समझने का प्रयत्न करें। हम देखेंगे कि अद्वैतमत द्वैतमत की समस्त आशाओं और स्पृहाओं की किस प्रकार रक्षा और पूर्ति करता है, और फिर साथ ही किस प्रकार ब्रह्मभावापन्न मानवजाति की परमोच्च गति के साथ सामंजस्य रखते हुए अपने भी सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। जो व्यक्ति मुक्तिलाभ के बाद भी अपने व्यक्तित्व की रक्षा के इच्छुक हैं – भगवान से स्वतन्त्र रहना चाहते हैं, उन्हें अपनी स्पृहाओं को चरितार्थ करने और सगुण ब्रह्म का सम्भोग करने का यथेष्ट अवसर मिलेगा। ऐसे लोगों के बारे में भागवत-पुराण में कहा है, “हे राजन्, हरि के गुण ही ऐसे हैं कि समस्त बन्धनों से मुक्त, आत्माराम ऋषिमुनि भी भगवान की अहैतुकी भक्ति करते हैं।”6
सांख्य में इन्ही लोगों को प्रकृतिलीन कहा गया है; सिद्धिलाभ के अनन्तर ये ही दूसरे कल्प में विभिन्न जगत् के शासनकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं। किन्तु इनमें से कोई भी कभी ईश्वर-तुल्य नहीं हो पाता। जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गये हैं, जहाँ न सृष्टि है, न सृष्ट, न स्रष्टा, जहाँ न ज्ञाता है, न ज्ञान और न ज्ञेय, जहाँ न ‘मैं’ है, न ‘तुम’ और न ‘वह’, जहाँ न प्रमाता है, न प्रमेय और न प्रमाण, जहाँ ‘कौन किसको देखे’ – वे पुरुष सब से अतीत हो गये हैं और वहाँ पहुँच गये हैं, जहाँ ‘न वाणी पहुँच सकती है, न मन’ और जिसे श्रुति ‘नेति, नेति’ कहकर पुकारती है। परन्तु जो इस अवस्था की प्राप्ति नहीं कर सकते, अथवा जो इच्छा नहीं करते, वे उस एक अविभक्त ब्रह्म को प्रकृति, आत्मा और इन दोनों में ओत-प्रोत एवं इनके आश्रयस्वरूप ईश्वर – इस त्रिधा-विभक्त रूप में देखेंगे। जब प्रह्लाद अपने आपको भूल गये, तो उनके लिए न तो सृष्टि रही और न उसका कारण; रह गया केवल नाम-रूप से अविभक्त एक अनन्त तत्त्व। पर ज्यों ही उन्हें यह बोध हुआ कि मैं प्रह्लाद हूँ, त्यों ही उनके सम्मुख जगत् और कल्याणमय अनन्त गुणागार जगदीश्वर प्रकाशित हो गये। यही अवस्था बड़भागी, नन्दनन्दन-गतप्राणा गोपियों की भी हुई थी। जब तक वे ‘अहं’ज्ञान से शून्य थीं, तब तक वे मानो कृष्ण ही हो गयी थीं। पर ज्यों ही वे कृष्ण को उपास्य-रूप में देखने लगीं, बस त्यों ही वे फिर से गोपी की गोपी हो गयी, और तब “उनके सम्मुख पीताम्बरधारी, माल्याविभूषित, साक्षात् मन्मथ के भी मन को मथ देनेवाले मृदुहास्यरंजित कमलमुख श्रीकृष्ण प्रकट हो गये।”7
अब हम आचार्य शंकर की बात लें। वे कहते हैं, “अच्छा, जो लोग सगुण ब्रह्मोपासना के बल से परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, पर साथ ही जिनका मन अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रखता है, उसका ऐश्वर्य ससीम होता है या असीम? यह संशय आने पर पूर्वपक्ष उपस्थित होता है कि उनका ऐश्वर्य असीम है, क्योंकि शास्त्रों का कथन है, ‘उन्हें स्वाराज्य प्राप्त हो जाता है’, ‘सब देवता उनकी पूजा करते हैं’, ‘सारे लोकों में उनकी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।’ इसके उत्तर में व्यास कहते हैं, ‘हाँ, जगत् की सृष्टि आदि की शक्ति को छोड़कर।’ मुक्तात्मा को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति से अतिरिक्त अन्य सब अणिमादि शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। रहा जगत् का नियन्तृत्व, वह तो केवल नित्यसिद्ध ईश्वर का होता है। कारण कि शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर सृष्टि आदि की बात आयी है, उन सभी स्थानों में ईश्वर की ही बात कही गयी है। वहाँ पर मुक्तात्माओं का कोई प्रसंग नहीं है। जगत् के परिचालन में केवल उन्हीं परमेश्वर का हाथ है। सृष्टि आदि सम्बन्धी सारे श्लोक उन्हीं का निर्देश करते हैं। ‘नित्यसिद्ध’ विशेषण भी दिया गया है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि अन्य जनों की अणिमादि शक्तियाँ ईश्वर की उपासना तथा ईश्वर के अन्वेषण से ही प्राप्त होती हैं। ये शक्तियाँ असीम नहीं हैं। अतएव, जगन्नियन्तृत्व में उन लोगों का कोई स्थान नहीं। फिर वे अपने मन का पृथक् अस्तित्व बनाये रखते हैं, इसलिए यह सम्भव है कि उनकी इच्छाएँ अलग अलग हों। हो सकता है कि एक सृष्टि की इच्छा करे, तो दूसरा विनाश की। यह द्वन्द्व दूर करने का एकमात्र उपाय यही हैं कि वे सब इच्छाएँ अन्य किसी एक इच्छा के अधीन कर दी जायँ। अतः सिद्धान्त यह निकला कि मुक्तात्माओं की इच्छाएँ परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं।”8
अतएव भक्ति केवल सगुण ब्रह्म के प्रति की जा सकती है। “देहाभिमानियों को अव्यक्त गति कठिनता से प्राप्त होती है।” हमारे स्वभावरूपी स्रोत के साथ सामंजस्य रखते हुए भक्ति प्रवाहित होती है। यह सत्य है कि ब्रह्म के मानवी भाव के अतिरिक्त हम किसी दूसरे भाव की धारणा नहीं कर सकते। पर क्या यही बात हमारी ज्ञात प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में भी नहीं घटती? संसार के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक भगवान कपिल ने सदियों पहले यह दर्शा दिया था कि हमारे समस्त बाह्य और आन्तरिक विषय-ज्ञानों और धारणाओं में मानवी ज्ञान एक उपादान है। अपने शरीर से लेकर ईश्वर तक यदि हम विचार करें, तो प्रतीत होगा कि हमारे अनुभव की प्रत्येक वस्तु दो बातों का मिश्रण है – एक है यह मानवी ज्ञान और दूसरी है एक अन्य वस्तु – फिर यह अन्य वस्तु चाहे जो हो। इस अवश्यम्भावी मिश्रण को ही हम साधारणतया ‘सत्य’ समझा करते हैं। और सचमुच, आज या भविष्य में, मानव-मन के लिए सत्य का ज्ञान जहाँ तक सम्भव है, वह इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं। अतएव यह कहना कि ईश्वर मानवधर्मवाला होने के कारण असत्य है, निरी मूर्खता है। यह बहुत-कुछ पाश्चात्य विज्ञानवाद (Idealism) और सर्वास्तित्ववाद (Realism) के झगड़े के सदृश है। यह सारा झगड़ा केवल इस ‘सत्य’ शब्द के उलट-फेर पर आधारित है। ‘सत्य’ शब्द से जितने भाव सूचित होते हैं, वे समस्त भाव ‘ईश्वरभाव’ में आ जाते हैं। ईश्वर उतना ही सत्य है जितनी विश्व की अन्य कोई वस्तु। और वास्तव में, ‘सत्य’ शब्द यहाँ पर जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उससे अधिक ‘सत्य’ शब्द का और कोई अर्थ नहीं। यही हमारी ईश्वरसम्बन्धी दार्शनिक धारणा है।
1. जन्मादि अस्य यतः – ब्रह्मसूत्र, १।१।२
2. स ईश्वर अनिर्वचनीयप्रेमस्वरूपः।
3. जगद्व्यापारवर्जम्, प्रकरणात् असन्निहितत्वात् च। ब्रह्मसूत्र ४।४।१७
4. किं मुक्तस्य ऐश्वर्यम् जगत्सृष्ट्यादि परमपुरुषअसाधारणम् सर्वेश्वरत्वम् अपि, उत तद्रहितम् केवलपरमपुरुषानुभवविषयम् इति संशयः। किम् युक्तम्? जगदीश्वरत्वम् अपि इति। कुतः? “निरञ्जनः परमम् साम्यम् उपैति” इति परमपुरुषेण परमसाम्यापत्तिश्रुतेः सत्यसंकल्पत्वश्रुतेः च। न हि परमसाम्य-सत्यसंकल्पत्वे सर्वेश्वरासाधारणजगन्नियमनेन विना उपपद्येते; अतः सत्यसंकल्पत्व-परमसाम्योपपत्तये समस्तजगन्नियमनरूपम् अपि मुक्तस्य ऐश्वर्यम इति। एवम् प्राप्ते प्रचक्ष्महे – जगद्व्यापारवर्जम् इति। जगद्व्यापारः – निखिलचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदनियमनम् तद्वर्जम् निरस्तनिखिलतिरोधानस्य निर्व्याजब्रह्मानुभवरूपम् मुक्तस्य ऐश्वर्यम्। कुतः? प्रकरणात् – निखिलजगन्नियमनम् हि परम् ब्रह्म प्रकृत्य आम्नायते – “यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्त्यभिसविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व, तत् ब्रह्म” इति। यदि एतत् निखिलजगन्नियमनम् मुक्तानाम् अपि साधारणं स्यात्, ततः च इदम् जगदीश्वरत्वरूपम् ब्रह्मलक्ष्मणम् न संगच्छते; असाधारणस्य हि लक्षणत्वम्। तथा “सत् एव सौम्य इदम् अग्रे आसीत् एकम् एव अद्वितीयम्, तत् ऐक्षत बहु स्याम् प्रजायेय इति, तत् तेजः असृजत” “ब्रह्म वा इदम् एकम् एव अग्रे आसीत्, तत् एकम् सत् न व्यभवत्, तत् श्रेयोरूपम् असृजत क्षत्रम् – यानि एतानि देवक्षत्राणि, – इन्द्रः, वरुणः, सोमः, रुद्रः, पर्जन्यः, यमः, मृत्युः, ईशानः इति” “आत्मा वा इदम् एकः एव अग्रे आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत, स ऐक्षत लोकान् नु सृजा इति, स इमान् लोकान् असृजत” “एकः ह वै नारायणः आसीत्, न ब्रह्मा, न ईशानः, न इमे द्यावापृथिवी, न नक्षत्राणि, न आपः, न अग्निः, न सोमः, न सूर्यः, स एकाकी न रमेत, तस्य ध्यानान्तस्थस्य एका कन्या दश इन्द्रियाणि” इति आदिषु, “यः पृथिव्याम् तिष्ठन् पृथिव्याः अन्तरः” इति आरभ्य “यः आत्मनि तिष्ठन्” इति आदिषु च निखिलजगन्नियमनम् परमपुरुषम् प्रकृत्य एव श्रूयते। असन्निहितत्वात् च – न च एतेषु निखिलजगन्नियमनं प्रसंगेषु मुक्तस्य सन्निधानम् अस्ति, येन जगद्व्यापारः तस्य अपि स्यात्। – ब्रह्मसूत्र, रामानुज भाष्य, ४।४।१७
5. “प्रत्यक्षोपदेशात् इति चेत् न, अधिकारिमंडलस्थोक्तेः।” इस सूत्र (ब्रह्मसूत्र ४।४।१८) का रामानुज भाष्य देखिये।
6. आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे। कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थंभूतगुणो हरिः॥ श्रीमद्भागवत, १।७।१०
7. तासाम् आविरभूत् शौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः। पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथमन्मथः॥ श्रीमद्भागवत, १०।३२।२
8. ये सगुणब्रह्मोपासनात् सह एव मनसा ईश्वरसायुज्यं व्रजन्ति, किम् तेषाम् निरवग्रहम् ऐश्वर्यम् भवति, आहोस्वित् सावग्रहम् इति संशयः। किम तावत् प्राप्तम्? निरङकुशम् एव एषाम् ऐश्वर्यम् भवितुम् अहर्ति – “आप्नोति स्वाराज्यम्” “सर्वे अस्मै देवाः बलिम् आवहन्ति” “तेषाम् सर्वेषु लोकेशु कामचारः भवति” इत्यादि श्रुतिभ्यः। इति एवं प्राप्ते पठति – “जगद्व्यापारवर्जम्” इति। जगदुत्पत्त्यादिव्यापारम् वर्जयित्वा अन्यत् अणिमादि-आत्मकम् ऐश्वर्यं मुक्तानाम् भवितुम् अर्हति। जगद्व्यापारः तु नित्यसिद्धस्य एव ईश्वरस्य। कुतः? तस्य तत्र प्रकृतत्वात्, असन्निहितत्वात् च इतरेषाम्। परः एव हि ईश्वरः जगद्व्यापारे अधिकृतः, तम् एव प्रकृत्य उत्पत्त्यादि-उपदेशात् नित्यशब्दनिबन्धनत्वात् च। तदन्वेषण-विजिज्ञासनपूर्वकम् तु इतरेषाम् अणिमादि ऐश्वर्यम् श्रूयते। तेन असन्निहिताः ते जगद्व्यापारे। समनस्कत्वात् एव च एषाम् अनैकमत्ये कस्यचित् स्थितिअभिप्रायः, कस्यचित् संहार अभिप्राय इति एवम् विरोधः अपि कस्यचित् स्यात्। अथ कस्यचित् संकल्पम् अनु अन्यस्य संकल्पः इति अविरोधः समर्थ्येत। ततः परमेश्वराकूतन्त्रत्वम् एव इतरेषाम् इति व्यवतिष्ठते। – ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य ४।४।१७