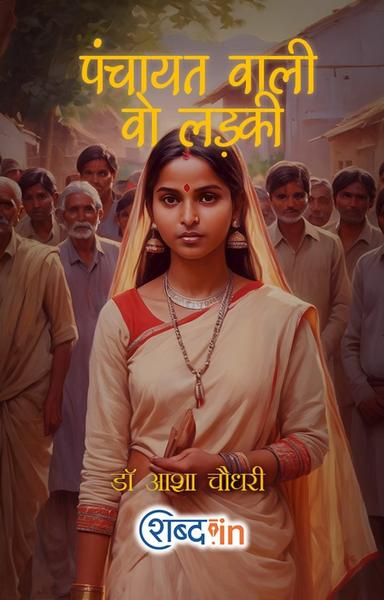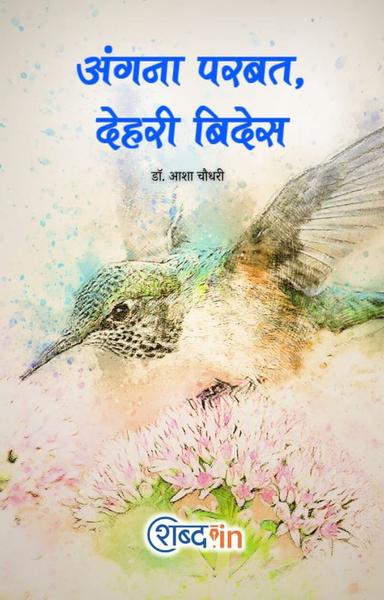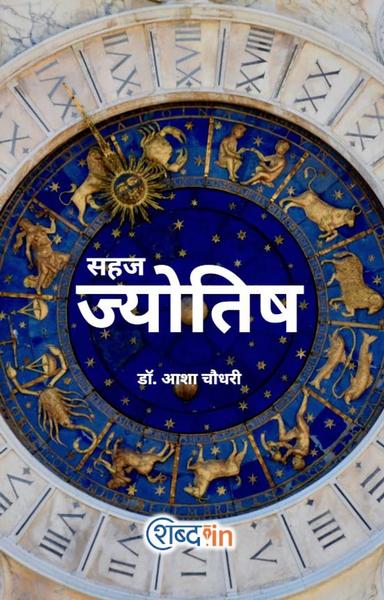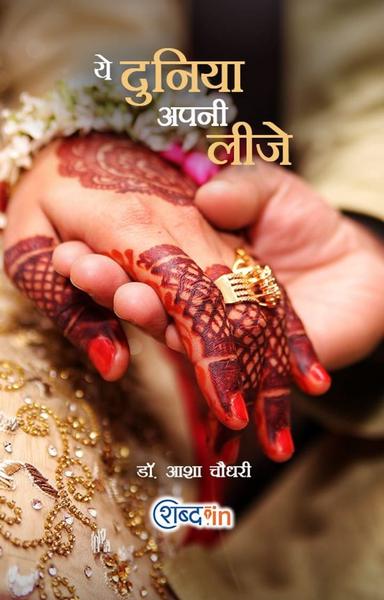अंगना परबत, देहरी बिदेस
डॉ आशा चौधरी
1-
ट्रेन के पूरी रात के सफर के दौरान अनगिनत स्मृतियाँ और बस् अवसाद ! मानो ये ही उसके साथ थे। लखनऊ मेल से दिल्ली का फासला रहता भी रात ही रात का था। ट्रेन छूटते ही उसने अटैंडेंट से बेड रोल ले लेने के बाद जो मुंह ढाँपा तो सुबह दिल्ली आने पर ही उघाड़ा था। इतने बरसों के अबोल, अदेखे के बाद भी अपनों की पहचान में मन कहाँ देर करता है। चट् से पहचान लिया था उसने स्टेशन पर अनमने से खड़े प्रेम भैया को। प्रेम भैया अकेले ही आए थे उसे लिवाने, वही प्रेम भैया जो उसे बचपन में अक्सर छेड़ा करते थे-
‘रत्नों, बना दे मेरा स्वेटर जल्दी, नहीं तो अपने नाम के आगे चोपड़ा लगा लूंगा !’
वे तो घर में किसीको भी छेड़ने से बाज न आते थे।
’चाची, जल्दी लाओ नाश्ता नहीं तो चोपड़ा.......’
’मम्मी, पाॅकेट मनी बढ़ाओ प्रेम चोपड़ा आता है .......’
स्मृतियाँ भी कैसी-कैसी कोई ओर नहीं, कोई छोर नहीं .......
शायद वे भी ऐसी ही किन्हीं स्मृतियों की पकड़ में थे, सो सामान के नाम पर उसके एकमात्र बैग की उठाई-धराई, टिकिट चैक कराना-धराना सब मशीन की मानिंद किये जाते थे, वरना वे ऐसे चुप्पे तो कतई न थे।
‘मुझे पहले अस्पताल ही ले चलो भैया !’
उसकी डूबती आवाज ही का असर था कि भैया ने कार अस्पताल की ओर ही मोड़ ली थी जो कि एक भव्य पंचसितारा होटल की तरह की लुक दे रहा था। आलीशान अस्पताल के कैपंस में दाखिल हो जब कार विशाल पोर्च में रुकी तब तक भी आँसू उसके थे कि रुकने का नाम ही न लेते थे। जब भैया उसे हाथ से सहारा दे वार्ड की ओर ले चले तो आँसू और इठला गए थे। आखिर भाई का सहारा जो था ! मगर जब वह वार्ड में पहुँची तो बेड पर निश्चल, निश्चेष्ट तमाम नलियों-मशीनों के जंगल-जाल से में फंसे असहाय पड़े पापाजी को देख न जाने आँसू कहाँ बिला गए ! मानो गंगा में कुछ बचा ही न था बहने को। क्या तो, कुछ कितना तो सूख सा गया था भीतर-बाहर।
कहाँ चली गई थी पापाजी के चेहरे की वो अपनत्व भरी चमक ? वक्त ने क्या तो, कैसी तो असमर्थता की लकीरें खींच दी थीं उस चेहरे पर जो कभी उनकी खुशमिजाजी का आईना ही हुआ करता था। कितना तो बुढ़ापा आ उतरा था उन पर !
उम्रदराजी के साथ-साथ हर झुर्री में जैसे कोई भीतरी असहायता इस तरह रच-बस गई थी कि उनका पूरा चेहरा मानो उस दर्द भरी असहायता का साक्षात बयान ही कर रहा प्रतीत होता था। वह मूक खड़ी निर्निमेष निहारती थी।
सब खाली-खाली हो आया एकबारगी। वीराना, एकाकी, धुर सन्नाटा सा खिंच आया था उसके आस-पास। भैया का उसके लिये कुर्सी खींचना, उसे बिठाना। नर्स का आना, टेबल पर खट-पट करना, चार्ट देखना, सब मानो किसी और लोक की घटनाओं जैसा हो आया।
वो चाहे तो भी पापाजी को छू न सके। ऐसी मजबूरी ! पैर कैसे छुए ? वे मानो नींद में थे और, सोते के पैर नहीं छुए जाते ! वो इतने अर्से बाद आई है, आई क्या है बुलाई गई है और बिना उनके पैर छुए खड़ी है ! माथे पर हाथ नहीं फेर सकती डर के मारे कि कहीं अगल-बगल लगी तमाम नलियाँ इधर-उधर न हो रहें। वो क्या करे ?
आँसू भी मानो इस ऊहा-पोह की स्थिति से बचने को पहले ही विदा ले चुके थे। भैया, डाॅक्टर के आने पर उनसे कुछ बात कर रहे थे। एक-दो और डाॅक्टरों ने आ कर थोड़ा दिलासा दिया था। और वे क्या दे सकते थे ? उसी में से थोड़ा दिलासा भैया ने उसे अपनी नजर के वापस चलने के इशारे के साथ दे दिया।
अब चलना होगा उस घर में कि जिसे छोड़े लगभग् पंद्रह-सोलह वर्ष बीत चले। पापाजी के पास, उस अपने जन्मदाता के पास चंद लम्हा रुकने से ही फर्ज पूरा हो गया ? उसे लगा वह क्या-क्या न करने लगे। बचपन की तरह ! कुछ
बेतरतीब से पड़े पापाजी को तरतीब से सुला दे। ये तकिया जरा ऊँचा है पापाजी इतना ऊँचा तकिया तो कभी नहीं लेते थे। चादर थोड़ा नीचे लटक रही है। पापाजी चादर को पैरांे में दबा कर सोते थे। यूं नीचे लटकते कपड़े उन्हें अच्छे नहीं लगते थे।
‘तू चल ! सब नर्स का काम है वो करेगी !’
भैया ने उसका मंतव्य भाँप पापाजी की सार-संभाल को उठ रहे उसके हाथों को थाम उसे दरवाजे की तरफ मोड़ लिया। वो चित्रखचित सी चली आई। लंबे-लंबे गलियारे, दवाओं की गंध, गहरे हरे परदों से ढके अनेक दरवाजे-खिड़कियाँ पार करती वह भैया के साथ खुले बरामदे में चलती चली आई, जहाँ से दिख रहा था अस्पताल का एल शेप वाला भवन, उसके साथ फैले बेहद खूबसूरत हेज, लाॅन, क्यारियाँ। क्यारियों में खिले अनगिनत प्रकार के अनगिनत फूल, सड़क के किनारे लंबे पेड़ांे की कतारें सांस रोके सतर मुद्रा में अटेंशन खड़ी सी लगती थी। भैया उसे सड़क के एक ओर खड़ा रहने का इशारा कर, अपने लिये सलाम-सैल्यूट को उठे अनेक हाथों को उदासीनता से लेते हुए कार लाने चले गए।
अब उसने ध्यान से देखा प्रेम भैया को। फ्रेंकफर्ट में खासे जमे-जमाऐ कारोबार ने जहाँ एक ओर अथाह दौलत दी थी उन्हें, वहीं अच्छा भरा हुआ धनपति शरीर भी दे डाला था। कभी कितने दुबले पतले हुआ करते थे यही प्रेम भैया।
मम्मी कहा करतीं थीं -
’खाया कर ठीक से कुछ ! कोई लड़की पसंद नहीं करेगी रे तुझे सींकिया सुल्तान।’
मम्मी का डर लेकिन निर्मूल ही तो निकला। प्रेम भैया पापाजी के मेडिकल इक्विपमेंट्स के बिजनेस की धुरी से होते गए और उनकी उन तमाम आर्थिक सफलताओं से अभिभूत हो जात-बिरादरी में सच् ही मानों उनके लिये लड़की वालों ने लाइन लगा दी ! मगर.......
मगर उन्हें पसंद भी आई तो अपनी जाति-समाज के बाहर की कभी अपनी क्लासमेट रही कमलिनी ! जो सिर्फ नाम की कमलिनी थी। गठा हुआ शरीर और फटा हुआ गला ! न जाने कैसे कभी कुछ रिश्ते विधाता यूं ही अपने हँसी-मजाक के निमित्त तो नहीं जोड़ देता ?
‘मम्मी के सींकिया सुल्तान को पहलवान मिल गया!’
परिवार में हंसी-ठठ्ठा होता रहा, होता रहा, लेकिन जाने क्या जादू की छड़ी सी फेर दी थी कमलिनी भाभी और उनके परिवार वालों ने कि लाल पाई, आने, धेले के हिसाब-किताब बराबर रखने वाले भैया ने उनके बाद और कोई प्रस्ताव आने ही न दिया ! पापाजी रस्मो-रवाज के पक्के थे, जुबान के धनी थे। गांठ के भी पूरे पक्के थे। घर में कोई कमी
न थी। सो दहेज न आया तो न सही, भाभी को तो खुले दिल के परिवार ने अपना ही लिया था। वे थीं भी ऐसी मुंहफट कि उनका सामना करने में अच्छी-अच्छी लड़ाकाऐं, मुंहलगी नौकरानियाँ शर्मा जातीं ! सो भाभी के मुंह लगने का साहस किसी से न हुआ। एक दो बार मम्मी ने अवश्य ‘सासपन’ दिखलाना चाहा तो उन्हें भी भाभी के तब, उन दिनों भारी हो चुके पैरों की खुशखबरी तथा भैया के उनके प्रति बेहद फेवरेबल बिहेवियर ने पस्त कर दिया था।
रत्ना देख रही थी इन बीते वर्षों में शायद अब कहीं जा कर प्रेम भैया कमलिनी भाभी के जोड़ के हो पाए थे। काफी मुटा गए थे। भाभी की दिन भर तले-गले से जुगाली करते-कराते रहने की आदत का ही करिश्मा हो सकता है यह ! जो भी हो, जरुर मम्मी की आत्मा स्वर्ग से इस बात के लिये कमलिनी भाभी को भरपूर असीसती होगी कि उनके सींकिया सुल्तान को पहलवान बना दिया ! उसे एक बोझिल सी हँसी आने को भी मगर होठों पर नहीं आई।
पिछले ही वर्ष तो मम्मी का भी देहांत हुआ फ्रेंकफर्ट में। प्रेम भैया, भाभी फ्रेंकफर्ट में ही सेटल हो गए हैं यह उसे पता था। यह भी पता चला था कि मम्मी को वे अपने साथ लिवा ले गए थे। शायद यह आठ-दस साल पुरानी बात है। मम्मी ने एक बार उसे सबसे छुप-छुपा कर पत्र लिखा भी था कि ’मैं यहाँ आ तो गई हूँ रत्ने, पर इन दोनों के रंग-ढंग मुझे नहीं भाते ! फ्रिज में मीट रखा है। किचन में मीट बनता है। मेरे लिये थोड़ा भी इंतजाम नहीं। क्या करुं, कैसे करुं ? अन्न, मांस, मच्छी इन्हें तो एक साथ रखा-बना सब हजम है। मेरा तो मन तैयार नहीं होता। कमलिनी से तो कोई उम्मीद नहीं, प्रेम भी उसी के रंग में रंगा है। ये लोग दोनों अपने में रमें हैं। बच्चे पढ़ाई में, मुझे बच्चों को संभालना होता है।
मुझसे इतनी देख-भाल अब नहीं होती। कमलिनी से कुछ कहो तो वह तो इतना बतंगड़ बना डालती है कि सहा नहीं जाता, और प्रेम मुझसे इतना चुप्पा-चुप्प रहता है कि उससे भी कुछ कहा नहीं जाता।’
तब समझ में आ गया था कि क्यों कमलिनी भाभी अपनी सास को जिन्हें वह छुपा-छुपे या मजाक-मजाक में किसी भी तरह ’गले की फास’ कहने से नहीं चूकती थीं खुशी-खुशी अपने साथ फ्रेंकफर्ट ले गई थीं। वहीं पिछले साल ह्दयाघात से मम्मी नहीं रहीं। सब क्रिया-कर्म वहीं हो गया। पापाजी और बाकी भाई लोग गए थे। रत्ना को तो कोई कुछ समझता हो परिवार की, तब तो बताता ! उसका तो नाम लेना तक प्रतिबंधित किया हुआ बताया जाता था घर में ! सब-कुछ हो हवा जाने के बाद ही खबर दे कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई ! समय पर खबर हो भी जाती तो भी क्या कर
पाती वह ! बस् उनके मोक्ष की कामना ही तो कर सकती थी।
बेटे ने जाति से बाहर ब्याह किया था तो वह तो सबको मंजूर था। मगर घर की बेटी ने जाति से बाहर ब्याह का फैसला किया तो सब पराए हो गए थे। उसने भाई-भावजों के रवैये को भांप कर कोर्ट-शिप करने में ही खैर समझी थी ! उसे पता था भाभियाँ बेहद खुश थीं मन ही मन, क्योंकि अंटी से कुछ माल ढीला न करना पड़ा था, साथ ही आगे का व्यवहार भी भरसक बंद ! उसे गाहे-बगाहे किसी प्रकार किसी किसी से पता चला करता था कि भाभियाँ मम्मी-पापाजी के कान भरने से बाज न आती थीं कि-
‘इतनी लाड़ की, इकलौती ने यूं नाक काट दी ! ऐसी बेटी का तो सात जन्मों मुंह न देखे कोई !’
मम्मी अवश्य उनकी बातों में आ जाया करती थीं, तभी उसे कभी न बुलाया। या कि कोई दबाव था उन पर किसीका ? किसका ? भाभी लोगों का ? या, बेटों पर प्राण छिड़कतीं यूपी, पंजाब की आम माँओं की तरह वे स्वयं ही बेटी से विरत हो रही थीं ? हालांकि मम्मी ने जब उसे माफ करने का मन बनाया तब तक उनकी चला-चली की बेला आ लगी थी। पर पापाजी ? पापाजी कैसे इतने निष्ठुर हो रहे जीवन भर कि इतने वर्ष पर वर्ष बीतते गए उसे कभी याद नहीं किया, कभी तलब नहीं किया ? क्या सचमुच उसका अपराध इतना बड़ा था ? किससे पूछे वह आज ? जिससे पूछना था वह तो बेसुध था। भाइयों से पूछने का कोई मतलब न था।
पिता की आसन्न मौत की घड़ी में भी उसे विचारों का महा मकड़जाल घेरे था। क्या मन कभी घड़ी भर को भी विचार विहीन नहीं रह सकता ?
ऐसी ही कुछ उथल-पुथल प्रेम भैया के मनस् में भी मची होगी तभी न वे यूं चुपचाप ड्राइव किये जाते थे ? पहले तो उसे छेड़-छेड़ कर रुला न दें तो वे प्रेम भैया ही नहीं। कोई काना-कुबड़ा दिखा नहीं कि देख ’रत्ना तेरा वर !’ या लंगूर दिखा नहीं कि -
’देख तेरे ससुर जी ! देख-देख कैसे कमर खुजला रहे हैं !’ पूरा घर तो घर, नौकर-चाकर तक मजे लेते थे भाई-बहन की चुहल के। ये तो खैर वक्त ही नहीं चुहल का लेकिन क्या वैसे भी प्रेम भैया इतने चुप्पे इतने गंभीर हो गए होंगे ? कैसे तो, उन्हीं परिचित रास्तों पर अजनबी से बने बैठे थे।
दिल्ली आना उसे पड़ता था कई बार, काँफ्रेंस, सेमिनार आदि अनेक कारणों से। मगर वो पहले वाली बात नहीं रही। अपने घर की ओर की दिशाएं, वो राहें तो सोच में भी जी ही दुखाती थीं .......।
जिन अपनों ने बिसरा दिया उन्हें बिसूरने से क्या लाभ था ? बस मम्मी और पापाजी ही बेतरह याद आते थे। न जाने किस मिट्टी के बने थे मगर वे लोग कि अपनी इकलौती, बड़ी लाड़ली बताई जाने वाली बेटी के लिये फिर कभी कोई राह खुली न रखी इधर आने की। और उसके आने की जुगत भी लगी तो तब जब पापाजी महायात्रा की ठान चुके समझे जा रहे हैं .......!
कार कब घर के विशाल गेट को पार कर भीतर प्रवेश कर गई उसे भान तक न हुआ। अरे, ये सब कितना बदल गया। पहले तो मात्र यही कोठी थी। आसपास विशाल फैला मैदान, गगन चुंबी अशोक के वृक्षों, हरी मुलायम घास और चारों ओर चारदीवारी से घिरा, प्रकृति के संग साक्षात बतियाता-खिलखिलाता घर था, जिसे ऊँची-ऊँची चारदिवारी के बावजूद दूर से देखा जा सकता था। आज तो इसके इर्द-गिर्द ये कितनी गगनचुंबी अट्टालिकाएं अपने दामन में अनेक फ्लेट ही फ्लेट समेटे सीमेंट-कांक्रीट के जंगल के नमूने के रुप में आधुनिक समय की मजबूरियों व फैशन की प्रतीक बन खड़ी हैं। जिधर नजर उठाती थी उधर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग ! वो, अपने वो बगीचे, वो खेतनुमा बाग कहाँ गए बड़े-बड़े ? उसकी हैरान नजरों के प्रश्न भांप लिये थे प्रेम भैया ने .......
’चल अंदर चल। इतनी जमीन खाली रखने से कोई फायदा नहीं था। सो मल्टी स्टोरी बना-बना कर कुछ फ्लेट्स सेल कर दिये, कुछ किराए पर हैं !’
वह हक्की-बक्की सी उस तमाम स्थल को एक पल याद करती सी, तो अगले पल भूलने का प्रयास करती सी, अजनबी सी कार से उतरने को थी। भैया ने कार पोर्च में रोकी ही थी, कि उसके देखते ही देखते एक ड्राइवर तेजी से आ कर कार का डोर खोल रही उसके पैरों में फटाक् से झुक आया। पूरा शोफर की यूनिफॅार्म में था। दूसरे, इतने वर्षों का अंतराल कुछ कम नहीं होता। इस बीच अनेक चेहरे, शख्सियतें बदल, बिगड़-सुधर जाती हैं।
‘ये अपने यहाँ शुक्ला काम करती है न उसी का बेटा है ....’ भैया ने उसके असमंजस को दूर किया।
‘अरे ! ये इत्ता बड़ा हो गया ? कहाँ तो रें रें पें पें करता, नाक सुड़कता शुक्ला चाची के पीछे-पीछे घूमता था .... । क्या नाम था रे तेरा .... ?’
शुक्ला अवश्य ही घर की काम वाली बाई थी, पर मम्मी सबसे आत्मीयता भरे भैया, दीदी, चाचा-चाची, काका-काकी के भाव से काम ले कर सबको खुश व संतुष्ट रखती थीं। लेकिन उसने विस्मृति की गर्त झाड़ने के प्रयास के साथ ही महसूस किया कि भैया के चेहरे व शब्दों में निहायत ही भोथरा सा भाव था शुक्ला चाची और उसके बेटे के लिये।
‘जी मेरा नाम हरनाम है।’
‘ओ, हरनाम ..... ! भैया इसे ही मम्मी मीता कहती थीं न ? क्योंकि मम्मी का नाम भी हरनाम कौर था ... ’
‘हाँ हाँ चल अंदर तो चल .....’
हरनाम की आँखों की चमक को अनदेखा करके भैया उसे भीतर ले चले थे।
‘क्या तू भी आते ही नौकरों-शोफरों से बतियाने लगी .... ’
एक अजब सी हिकारत भरा था भैया का स्वर। उसे भी स्वयँ पर पल भर के लिये कुछ ऐसा ही भाव हो आया। सच तो है यह कोई वक्त है नौकरों से बोलने बतियाने का, कि जब अभी तो सारे परिवार से मिलना बाकी था। पापाजी सीरियस हैं, भला नौकरों से दुआ-सलाम, पूछ-ताछ अभी ही होनी है ? उसे कुछ झेंप सी हो आई लेकिन अभी तो बहुत सी स्थितियाँ ऐसी आनी बाकी थीं जिनमें वह झेंपने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी, कौन जाने ? होंठ काटती उसने अंदर
प्रवेश किया।
‘‘अंगना तो परबत भया,
देहरी भई बिदेस’’
न जाने क्यों उसे अमीर खुसरो की ये पंक्तियां बरबस याद आऐ जाती थीं। अंगने का परबत हो जाना देखने ही शायद आई थी। देहरी तो कभी की बिदेस हो चुकी थी या कि सप्रयास बिदेस बना दी गई थी उसके लिये उसीके किन्हीं अपनों के द्वारा। अब,
ब्याह के इतने बरसों बाद प्रथम प्रवेश था मायके में उसका बिना किसी अगवानी के, मम्मी होतीं तो शगुन का एक टीका ही सही लेकिन शगुन करतीं जरूर, मगर ये वक्त यह सब सोचने का था क्या ? क्यों उसे ये बेहूदा ख्याल घेर लेते थे ? क्या हो गया है उसे ? अपने ही घर में जाते समय कितनी हिचक, ठिठक, कैसा संकोच सा, कुंठा सा उस पर तारी हुआ जाता था।
भीतर घुसते ही उसकी नजरें न चाहते हुए भी मुआयना सा किये जाती थीं। मम्मी के समय का साफ-सुथरा बेहतरीन डनलप के सोफों व डबल परदों से सजा रहने वाला ड्राइंगरुम और भव्य हो चुका था, मगर अस्त-व्यस्त सा था। क्यों न
हो, पापाजी के जानने वालों की कोई कमी थी ? जिसे खबर मिली दौड़ा-दौड़ा आया होगा, सो ड्राइंगरुम का व्यवस्थित रहना नामुमकिन ही था।
सीढ़ियों के पास वाली दाहिनी दीवार पर मम्मी की फोटो थी जिस पर न जाने कब की सूखी माला पड़ी थी। जिसके फूल भी बीच-बीच में, कहीं-कहीं झर गए थे। उसे सिसकी सी हो आई। मम्मी की वही ममतामय मुस्कुराहट, वही सुखी गृहस्थिन और योग्य, क्षमतावान माँ वाली आँखों की चमक अभी-अभी जैसे सीधे उसके ह्दय में प्रवेश किये जाती थी। क्या माँ ! क्या पड़ी थी बाकी बच्चों, पति व घर को भूल कर, तज कर अपने प्रिय बेटे के साथ फ्रेंकफर्ट जा रहने की ? आखिर क्या गल्ती हो गई थी सबसे ? पापाजी का, बाकी सबका, घर का मोह फिर कभी वापस खींच ही न पाया आपको ? और मेरे पास तो आप आ ही नहीं सकती थी न ? मैं तो बेटी हूँ न ! बेटियों के घर का तो आप ने पानी तक नहीं पीना था ! और बेटी भी वो जिसने अपनी इच्छा से अपना वर चुना था !
‘चलो बीबीजी, कब तक बिसूरोगी? कैसा रहा आपका सफर ? रेल के सफर की थकान-शकान दूर करो जी, फ्रेश
हो लो। फिर नाश्ता-वाश्ता बनवाते हैं, अब क्या धरा है यहाँ .......?’
’अरे पुनीता भाभी!’ .....
कितनी बदल गई थीं भाभी ? दबा हुआ रंग खासा निखर आया था मगर सुतवां नैन-नक्श पर चरबी की परत-दर-परत में सारा रूप मोटापे की बलि चढ़ गया था। जो हो, मालिकिन के जैसे एक रौब से चमकता था उनका चेहरा। एक ओर, वह पुलकती थी अपनों को देख कर, फिर, दूसरे क्षण सीरियस पड़े पापाजी का ख्याल उसे सहमा जाता था। काश ! एक बार वे आँखें खोल कर उसे देख लेते, अपना हाथ उठा कर उसे असीस देते बस् !
‘देखो न क्या करुं अब तो गठिया भी आ धरा लगता है। अरे भई तुम तो वैसी की वैसी ही रहीं ! क्या हमारे ननदोई
जी कुछ खिलाते-पिलाते नहीं ?’
पुनीता भाभी अपना भारी बदन शकर के थैले सा झुलातीं, शनैः-शनैः, अशक्तों की तरह सीढ़ियों के बाजू वाले कमरे से निकल उसके नजदीक आ खड़ी हुईं थीं।
फीकी सी हँसी हंस कर रह गई थी वह। शुरु से ही एस्थमेटिक थी। नपा-तुला खा कर ही आज तक जिंदा है ये बात घर के किसी सदस्य से छिपी न थी। इसी बीमारी की उग्रता की वजह से ही तो उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पाता था। जहाँ होता भी था वहाँ बड़े घर की, तीन भाइयों पर इकलौती बेटी के लिये दिये जाने वाले अपेक्षित दहेज के अनुमान से तीनों भाभियाँ कसमसा जाया करती थीं। सो, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने, अगलों के पास उसकी बीमारी की सूचना बढ़-चढ़ कर पहुँच ही जाया करती थी।
‘आज-कल तो लड़कियाँ खुद ही अपना वर चुन लेती हैं।’
’वैसे लव मैरिज करके माता-पिता की चिंता दूर कर देना कुछ बुरा भी नहीं ?’
तब, ये पुनीता भाभी ही निकलते-बढ़ते, मौका लगते अपनी अनमोल राय छेकती रहती थीं। और कमलिनी भाभी भी उनकी हाँ में हाँ मिलातीं मगर अक्सर ही फिकरेबाजी भी करती थीं सो अलग ......
‘हाँ सो तो है। मगर लव मैरिज के लिये खुद में कुछ होना भी तो चाहिये। बीमार-शीमार से, सूखी-संट्टी से कोई क्या लव-शव कर लेगा ?’ जलेबी की तरह या कि सूई की तरह सीधी कही-समझी जाने वाली वे एक से बढ़ कर एक अनोखी संरचनाऐं उसीके परिवार में कैसे, कहां से और क्यों कर आ जुटी थीं भगवान् ?
उनकी फिकरेबाजी और कसमसाहट को क्या कभी भुलाया जा सकता था ?
‘अरे भैया, मेरी भाभीजी ने तो साफ-साफ कह दिया था मेरे भैया को कि ’नंद गले की फंद’ के साथ नहीं रहूंगी ! पर अपन को देख लो यहां, रह ही रहे हैं ना, कुछ कहा कभी ? कभ्भी नहीं बाब्बा......।’
ओह! उसे ठंडे तीरों से बींध-बींध कर मानो लव मैरिज के लिये प्रेरित किया जाता ......। उसके ही घर में उसका रहना उनसे सहा न जाता था।
अकूत दौलतमंद पापाजी इसी तरह एक रोज कन्यादान के अधिकार से वंचित कर दिये गए थे ! दिखने को लगा कि बेटी कृतघ्न थी ! सारी शिक्षा-दीक्षा, कुल की मान-मर्यादा, गौरव पर पानी फेर गई......मगर निसंदेह भाभियों को यह पता था कि सच् कुछ और ही था ! और शायद भैया लोग भी जानते रहे हों कुछ-कुछ......
उसने स्वयँ में एक निहायत ठंडापन महसूस किया था पुनीता भाभी के गले लगते हुए, वैसा ही भाव कुछ उधर भी
था ‘जीती रहो ,सदा फलो फूलो.....’ नुमा आर्शीवाद देते समय। साथ ही उन्होंने अपनी बला दूसरों पर भी ठेल दी थी।
‘अरे आओ भई सब लोग, देखो रत्ना बीबीजी आ गईं !’
वे खुद जा कर मखमली सोफे में वजनी पत्थर सी पूरी की पूरी धंस गईं । बड़े-बड़े उसाँस लेती वे उसे अपनी दृष्टि में बनाए रखे थीं।
‘कौन कहेगा बीबीजी आप के दो बच्चे हैं ? पेट तो कहीं है ही नहीं। अरे मैं कहूँ के कहीं किसीके उठाई-धराई के तो ना पाल-पोस दिये ?’ ही ही ही। भाभी हँसी थीं।
उसे लग रहा था सब बेचैन होंगे पापाजी को ले कर । मगर ......
प्रीती भाभी पुनीता भाभी के पीछे-पीछे अवतरित र्हुइं, फिर कमलिनी भाभी ,फिर फिर ......,
फिर वे उसके सब अपने, छोटे-बड़े, कुछ जवान हो रहे, कुछ जवान हो चुके। स्नेहिल मुस्कान से भरे, कुछ अनमने से, शरमाते से, ‘प्रणाम बुआजी’, कुछ ‘चरण स्पर्श’ कहते करते उसके वे सब अपने जिन्हें उसने इस लंबे अर्से के दौरान केवल अपनी कल्पनाओं में ही देखा था ! अपनी मर्जी से ब्याह क्या कर लिया था मानों एक सड़े अंग की तरह काट कर फेंक दी गई थी।
क्या इतनी नाकारा थी वह ?
प्रीतो भाभी का वही बनावटीपन, पैनी नजरों से सामने वाले को तौलते हुए बात करना अब भी न गया था।
’पता नहीं भैय्या! लोग कैसे इत्ता नप्पे-तुले रह लेते हैं। जाने भगवान् कैसे किसीको ऐसे सांन्चे में ढाल के भेजता है। कितना ही कुछ होता-हवाता रहे मगर आप को क्या फर्क पड़ने का।’ उनके नश्तर इतने अर्से के बाद भी वैसे ही टनाटन थे।
वह चुप की चुप्प न रह जाए तो क्या करे ? जवाब वह उन लोगों को पहले भी नहीं दे पाती थी, अब भी जवाब देने तो नहीं ही आई थी। मम्मी इन्हीं प्रीती भाभी के लिये ही तो हँसी-हँसी में कहा करती थीं कि इसे बना कर तो विधाता ने इसका साँचा ही तोड़ दिया होगा !
‘अब यहीं देख लो, हमारी बीबीजी को ही देख लो। अब भला कुछ खाती-पीती ना होंगी ऐसा तो है नहीं। पर देख लो भई इन्हें। ये तो वैसी की वैसी ठहरीं सूखे छुहारे सी, बारीक सेव सी! इधर हमें देखो, स्साला पानी भी पियें तो घी बन-बन के लगता है !’
उन्हें अफसोस क्यों ना हो कि उनकी इस इकलौती ननद का शरीर अब भी चरबी-शून्य क्यों ? कहीं भूल कर भी चरबी-शरबी नहीं ! जबकि वे सब कमलिनी भाभी की ही तरह गोभी का फूल हो चुकी थीं। वो देख पा रही थी कि ठेठ आलीशान लेकिन कुल जमा दो मंजिले उस बंगले में भी, लिफ्ट लगवा ली गई थी। भाभियों के फलते-फूलते शरीरों
का बहुत कुछ भौतिक इलाज।
यद्यपि कमलिनी भाभी पहले भी कुछ कम न थीं ! अब तो उनके शरीर का पोर-पोर साड़ी-ब्लाउज से झाँक पड़ने को बावला सा लगता था। गनीमत है कि अब भी वे साड़ी ही पहने थीं न जाने किस कारण से। वरना उसे कोई आश्चर्य न हुआ होता जो वे उसे किसी अल्ट्रा माॅर्डन वेशभूषा में दिखतीं। घने घुघंराले कंधे तक कटे बाल अभी भी वैसे ही थे जिनके कारण वे कभी सिर न ढंकती थीं। वैसी ही उनकी भंगिमाएं, अपनी फैली-थुलथुल, बेलौस-बेभाव फैली काया का बेहिचक मुक्त दर्शन करवातीं वे मानो शरीर के मुद्दे पर जरा भी जागरुक न थीं। जैसा है, वैसा है। कैसा होना चाहिये इससे मानो उन्हें कोई सरोकार कभी रहा ही न था।
’ओहो! रत्ना बीजी ने तो जैसे कसम ही खा रखी है कभी मोट्टी-शोट्टी न होने की ! भला इत्ती स्लिम बने रहने की कोई वजह भी तो हो ? दूसरी शाद्दी करनी है कोई ?’
वे उसकी नपी-तुली काया देख बौरा ही तो गईं लगती थीं ! किसे नहीं पता था कि शादी के लिये प्रेम भैया को खुद उन्होंने ही फाँसा था, मगर अपने मामा पक्ष के दम पर विधिवत तय करके की गई शादी के कारण नाक उठाए फिरती थीं। अब भी हाल वही के वही दिखते थे उनके-
’अब क्या करते भई! माँ-बाप ने कान पकड़ कर शादी जहाँ कर दी वहीं गाय से जा बंधे ! कोई आशिक-वाशिक होता तो अपन भी छमिया दिखने की कोशिश करते......! हा हा हा हा......’
छिः ! कितने घटिया विचार ! उन अपने-अपने विचारों को मगर उच्चारें वो और घड़ों पानी रत्ना पर पड़े जाता था जैसे ! वह क्या किसी आशिक के कारण स्लिम ठहरी ? और फिर, यह कोई वक्त है इस तरह की बातों का ?
मम्मी आप की बहुएँ कहलाने के लायक कौन है इनमें से ? वह अगर अभी भी दुबली-पतली दिखती है तो इसमें उसकी ही गलती है ? कभी वे उसे इसी दुबलेपन के कारण मरियल-शरियल, छड़ी-शड़ी न जाने क्या-क्या तो सुना देती थीं। और अब ?
अब सूखा छुहारा, बारीक सेव और न जाने क्या-क्या। और ये आज सब अपनी-अपनी कायाओं की तुलना अचानक ही उससे क्यों करने लगी हैं ? कोई और बात नहीं मिली इन्हें बातचीत के लिये ? काश्। कोई भैया ही यहाँ आ जाऐं
कम से कम थोड़ी लगाम तो लगे इन छुट्टी-बिदकी घोड़ियों को।
‘बीबीजी चाय ......।’
अदरक व तुलसी की गंध ने उसका ध्यान खींचा था। अरे ये तो शुक्ला चाची थी ! अभी तक यहीं काम कर रही है बेचारी !
’कैसी हो चाची? पैरी पाना चाची।’
’जुग-जुग जियो बिटिया- बच्चों को ले आतीं तो देख तो लेते हम.....’
’कहाँ चाची? दोनों एक ही क्लास में हैं। दोनों के टेंथ बोर्ड के एक्जाम हैं।’
’हाँ भई! नौकरी वालों को तो नौक्कर-शौक्कर ही बनाने होंगे बच्चे। तुम खुद आ र्गइं यही क्या कम है ?’
पुनीता भाभी के लिये मम्मी नाहक ही नहीं कहती थीं कि ’जब देखो तब मुंह में बस् अंगारे ही भरे रहती है ! जहाँ चाहा उगल दिये। जो चाहे तो पूरे के पूरे समंदर को राख में बदल कर रख दे मिनटों में !’ वो तो देख रही थी कि तीनों ही भाभियां हालांकि पहले से ही खासी निपुण रही थीं, मगर इतने अर्से में तो उन सबने ऐसी किसी कला में पूरी-पूरी निपुणता हाँसिल कर ली थी। सो, इतना सब कुछ होते हुए भी, अर्सा बाद आई ननद को देखते ही न जाने क्यों वे सब पोर-पोर से भुने-सुलगे जाती थीं ? वह क्या खुद आई है ? आप ही लोगों के बुलाए तो आई है। और, वह यहाँ कितना रहेगी ? कोई हमेशा के लिये तो आई नहीं है !
’कैसा चल रहा है तुम्हारा इस्कूल-विस्कूल?’
‘अजी स्कूल ना कहो, बीब्बीजी तो काॅलेज, ना ज्जी ना, यूनिवर्सिटी वाली ठहरीं!’
पुनीता भाभी की गल्ती सुधारी थी प्रीतो भाभी ने या कहें कि अपने गहन ज्ञान का ही प्रदर्शन किया था !
’हँज्जी वही, काॅलिज-शाॅलिज कहो के इस्कूल, सब एक ही बात है!’
उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह इन वाचाल, मुंहलगी सी हो चुकी महिलाओं की इस प्रकार की बातों से कोई वास्ता न रखेगी, तभी पापाजी के साथ चंद दिनों रह पाएगी ! ये छुट्टी साँडनियों सी हो चुकी हैं, इन्हें किसी पर, कारण-अकारण कैसा भी आघात करने में कोई लाज-हिचक नहीं।
भैया उसका सामान उस रुम में रखवा रहे थे जो कि कभी सब बच्चों का पढ़ने-लिखने का ही नहीं बल्कि धींगा-मुश्ती करने का भी प्रिय कमरा हुआ करता था। जिसकी सारी खिड़कियाँ बाग की ओर ही खुलती थीं क्योंकि मम्मी का
मत था कि पढ़ते बच्चों के लिये ताजी हवा आनी जरूरी है। यह आजकल शायद गेस्टरूम बनाया जा चुका था। भैया की उपस्थिति में भाभियों ने बातचीत का विषय बदल दिया। अब फौरन पापाजी की चर्चा थी ! कब से कोमा में हैं ! कैसे क्या हुआ ! सुबह बस् नीबू पानी लेकर न्यूज पेपर पकड़ा ही था कि चकरा कर गिर पड़े ! पेपर छूट गया हाथ से ! वो तो शुक्र है वाहे गुरु का कि प्रीतो भाभी पेपर पढ़ने की आतुरता में उधर आई थीं, उन्होंने देख फौरन शोर मचाया। वरना न जाने क्या हो जात्ता ! बीब्बीजी हम तो लुट जात्ते, उनकी छत्तरछाया से वंचित हो जात्ते !
इस बीच रुम में उसका सामान सैट होने तक मझले व छोटे भैया भी आ चुके थे, उन्होंने आते ही उसे लिपटा लिया।
’कैसा चल रहा है तेरा यूनिवर्सिटी में सब ?’
दमाद अच्छा है हमारा ? भान्जे कैसे हैं ? बाकी सब ठीक ?’ उसके सिर पर हाथ फेरते थे वे बरसों पहले कभी बिछड़े उसके अपने, उसे लगा कि हां ! कोई सूत्र है जो अभी भी बाकी है। सारे तार अपनत्व के टूटे नहीं थे !
‘तू फ्रेश हो कर नाश्ता-वाश्ता करके थोड़ा आराम-शाराम कर ले, फिर दोपहर को वापस नर्सिंग होम चलेंगे।’
‘चलो रे भगो सब कबूतरों यहाँ से, ज्यादा भीड़ मत लगाओ,
’अब थोड़ा आराम करने दो कबूतरों की बुआजी को ......’
भैया लोग अपनी मन माफिक भाषा में बच्चों की चिल्लरपार्टी को आगाह करने लगे थे।
‘नहीं भैया, रहने दीजिए इन्हें मेरे साथ । मेरे कहाँ नसीब थे’ ....... वह रुआँसी हो आई।
‘अजी नसीब की बात ! मैं तो कहूं के आफत के इन पिटारों को साथ ही लेती जाना बिब्बीजी आप तो . . .’ कमलिनी भाभी के कहने के साथ ही......
‘चुप भी करो। आई है नहीं कि जाने की बात करने लगीं तुम . . .. ।’
प्रेम भैया ने कमलिनी भाभी को टोका था तो उसे मन ही मन क्यों न गर्व हो आना था अपने भाइयों पर। भाभियाँ तो आखिर कही ही ‘परजाई’ जाती हैं। कम से कम भाई अभी भी भाई के ही रुप में थे। संबंधों की व्यावसायिक
व्याख्या उन्होंने नहीं अपना ली दीखती थी !
वह कुछ संतुष्ट सी थी भीतर ही भीतर। ’बुआजी, बुआजी’ का शोर, एक आग्रह अब उसे चने के झाड़ पर चढ़ाए दे रहा था मानो ! उसे ये ख्याल मात्र भी न रहा कि ये इतने अप्रतिम अपनत्व, लाड़-भाव को पूरे पिछले वर्षों में जागने से कौन रोकता था, क्यों उसे इस सबसे वंचित रखा गया ?
बहरहाल बच्चे वैसे भी उसके लिये हमेशा फस्र्ट प्रायॅरिटी थे, यहाँ भी बच्चों ने बाजी मार ली। उनमें से कुछ वे थे जो उसके जाने के समय दो-तीन वर्ष के रहे थे। अब तो वे पहचाने ही न जाते थे। भीगी मसें, व्यवस्थित क्लीनशेव्ड जवान-जवान से, जवानी की देहलीज पर खड़े, मगर अपनी माँओं से ठीक विपरीत सुशिक्षित, मृदुल व्यवहार कहाँ से पाया उन्होंने ? सकून से भर गई थी वह !
उनमें से कई वे थे जो उसके चले जाने के बाद इस परिवार के सदस्य बने। वह नहीं देख पाई उनका ठेठ बचपन, उनका उठना-गिरना-पड़ना, ठुमक-ठुमक चलना, तुतलाना मगर अब कि जब उन सबने उसे बुआजी बुआजी कह कर संबोधित किया तो वह अपने भीतर-बाहर सब तरफ आनंद से सराबोर हो उठी। कोई बात नहीं जो वह पापाजी की महाप्रयाण बेला के बहाने से यहाँ आ पाई . . . . . कोई गम नहीं। धन्यवाद पापाजी कि किसी भी कारण से उसे अपने खून सेरुबरु होने का मौका तो मिला।
‘आप क्यों नहीं आते थे बुआजी? कभी नहीं देखा आपको, बस् आपके बारे में सुनते रहते थे हम लोग !’
‘अच्छा! तो मेरी चर्चा होती थी यहाँ ? कौन बताता था तुम्हें मेरे बारे में ?’ . . . . ऐसे गमगीन माहौल में भी एक तसल्ली भरी खुशी संभाले नहीं संभली थी उससे पल भर को तो।
‘दादाजी बताते थे। वो बहुत बातें करते थे आपकी!’
फिर से उसे अचंभे ने घेर लिया। कैसे कभी भाभी लोग उसे फोन पर बतियाती थीं कि ‘पापाजी ने तो आपके नाम से गंगा स्नान कर लिया है बीबीजी ! वे तो नाम तक नहीं सुनना चाहते आपका ! रत्ना नाम से ऐसे चिढ़ गए हैं कि रत्नों की बात भी हो तो नहीं उच्चारते यह नाम ! वे इस नाम के लिये भी ‘पत्थर’ कहते हैं पत्थर। रतना नाम तक लबों पर नहीं लाते अपने !’
यदि ऐसे पत्थर दिल हो गए थे पापाजी तो क्यों अपने पोतों-पोतियों से उसकी चर्चा किया करते थे ? याद करते थे उसे ! वे भुला नहीं पाए थे उसे ! उसे कोई मौका भी तो न दिया किसी ने कि अपनी वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करा पाती ! एक क्षण में उसका खून विह्ल होता, तो अगले क्षण वह मानो सूख जाता। पापाजी क्यूं किसीके बहकावे में आए हुए थे ? या कि,
भाभियों के साथ बुढ़ापा गुजारने में अपने हिसाब-किताब बदलना उनकी कोई अव्यक्त सी मजबूरी थी ? या कि फिर कौन था, कौन था उसके और पापाजी के बीच की दूरियों को बनाने व बढ़ाने वाला ?
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
2-
‘वाला नहीं वालियाँ थीं! तुम्हारे ब्याह के बाद टूटे-बुझे तुम्हारे पापाजी को तीनों बहुओं ने भड़काने में कोई कसर न रखी। उल्टे अविजित तक को लफंगा, गया-बीता सिद्ध कर-कर के उन्हें तुम लोगों से मोड़ दिया गया !’ दोपहर को वकील मामा हौले-हौले उसे बता ही रहे थे कि प्रीतो भाभी ने आ कर अपना आसन जमाने में तनिक देर न की थी।
‘भई क्या खुसुर-फुसुर हो रही है? हम भी तो सुनें !’ वे बिना किसी की परवाह के छूट मुंहफट तरीके से बोलने के लिये परिचितों में विख्यात थी हीं। रत्ना ने महसूस किया कि जब तक भी वकील मामा उसके पास रहे किसी न किसी बहाने,
कोई न कोई भाभी किसी न किसी पूरे मकसद से वहाँ जमी रहीं !
आखिरकार थकी-माँदी, आशंकाओं-कुशंकाओं से, अनेक नवीन अनुभवों से भरी सुबह उदास दोपहर में बदली। आने जाने वालों की गहमा-गहमी और इतने काम थे भाईयों भाभियों पर कि फोन पर ही पापाजी के हाल-चाल पूछ लिये गए। पेड़ों की फुनगी पर उतरती सिंदूरी शाम के रुप में दिन एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर कर समाप्त होने के नजदीक
आ लगा था।
कितना कुछ आज पाया था उसने, कितना कुछ गंवाया था, कितना कुछ बीत जाने का अहसास उसे मथ रहा था। कुछ बीतते ही जाने का एक अजीब सा पारदर्शी अवसाद सा उसका साथ न छोड़ता था। कई क्षणों तक यूं लगता पापाजी पड़े रहो यूं ही ! मुझे ये अनमोल क्षण तो मिले ! अगले क्षण ऐसे भी होते कि जब वह क्लांत हो स्वयँ को धिक्कारती रह गई कि जन्मदाता के प्रति ये भाव ! तुम्हें सब के बीच रहने का सुख मिले इसके लिये जन्मदाता के दुख की कामना ! हद है !
वह अपने कक्ष में अपने विचारों में गुम थी। भाई लोग सब अपने-अपने कामों से गए हुए थे। बच्चे बाहर लाॅन में क्रिकेट का मजा ले रहे थे। गहराती साँझ धुंधलके की चादर ओढ़ने लगी थी। पास ही के बाग में अब चिड़ियों का शोर थमने सा लगा था। उजाला-अंधेरा कुछ-कुछ घुल-मिल कर ढलती साँझ की धुंधली चादर के पीछे से गहराती रात को तारों भरे कजरारे आचलँ से सजाने-संवारने चला आ रहा था।
’साँझ पड़े नहीं सोते’,
’साँझ ढले दीया-बाती हो जानी चाहिये’ मम्मी अक्सर कहा करती थीं लेकिन उसकी इच्छा नहीं हुई बिस्तर से उठ कर कमरे का स्विच आॅन करने की। रह-रह कर कमलिनी भाभी के भोथरे ठहाके उसे काफी देर से सुन पड़ रहे थे। शायद उन्हीं के मिजाज की कुछ उनकी पुरानी सहेलियाँ आई हुई थीं। उनके स्वसुर के हाल-चाल पूछने नहीं, वरन खुद कमलिनी भाभी सालों बाद स्वदेश लौटी हैं, सो उनके खुद के हाल-चाल जानने उनकी परिचिताएं, उनकी रिश्तेदारिनें सुबह से ही दो जाती हैं तो और चार चली आ रही थीं।
कमलिनी भाभी के व्यवहार में यूरोप रिटर्न होने का रौब-दाब खासा देखने लायक हो गया है। सोच कर वह सहज ही मुस्कुरा दी। अपनी अभावों भरी, सौतेली माँ की फटकार भरी पिछली बेनूर जिंदगी को कितनी तरतीब से भूल चुकी दिखती हैं भाभी। बात-बात पर यूं जतलाती हैं मानो वे राई-रत्ती कभी किसी तकलीफ से दो चार न हुई हों, रईसी चोंचलों में ठेठ लाड़ली बिटिया की ही तरह पाली गई हों अपने मायके में ! जबकि उसे पता है अपने मायके में सादे फर्शी लगे कमरों का उन्हें झाड़ू-पोंछा तक लगाना पड़ता था। पर यहाँ आ कर उन्होंने एकदम ही स्वयँ को राजकुमारियों की लिस्ट में शामिल कर लिया था।
मम्मी की खास इच्छा रहती थी कि प्रायः हर पूजा-परब के अवसर पर प्रसाद घर की बहू ही के हाथों बने। मगर एक-दो बार के बाद ही भाभी ने दो टूक सुना दिया था।
‘ना मम्मीजी। मेरे तो हाथों में छाल्ले आ जाते हैं इत्ता सारा हलवा घोंटने से !’
और थोड़ा सा प्रासाद इस घर में बनता नहीं था। सो कमलिनी भाभी इसी प्रकार बहू के हर फर्ज से शनैः-शनैः खुद को बचा कर ले जाती गईं !
और यह क्या भूलने की बात थी कि ...... एक से एक खानदानी लड़कियों की लिस्ट लिये प्रेम भैया की बस् एक हाँ सुनने को अकुलाए फिरतीं मम्मी को शाॅक ही तो लगा था ! मगर बड़े कलेजे वाली थीं ! सो सह ही गईं थीं शांत भाव से वह सब, कि जिसे तब इतनी आसानी से सह जाने का जमाना न था। भैया की जिद के आगे हार कर मम्मी ने हथियार डालते हुए वही कुछ कहा था न ...... कि-
‘चलो ठीक है। कहते हैं के अपने स्तर से नीचे के परिवार की लड़की आएगी तो निभ के तो चलेगी ! अकड़-फों तो नहीं दिखाएगी ज्यादे !’
खुद भी हथियार डालते हुए उन्होंने पापाजी को भी अपने ऐसे ही तर्कों से निरूत्तर करते हुए मना लिया था। परंतु उसे ताज्जुब पर ताज्जुब होता कि कैसे छोटे स्तरों के परिवारों की कुछ अनोखी लड़कियां अपने से बड़े परिवारों में ब्याही जा कर, इधर ब्याह हुआ नहीं कि उधर उन परिवारों को अपनी अंगुलियों पर नचा डालने की अनोखी, अकूत सामथ्र्य से भर उठती हैं ! कई तो इस अनूठी संपदा को जैसे दहेज की तरह साथ लेकर आती हैं ! वे पहले ही मानो अपने से उच्चतर उस परिवार से एक आंतरिक शत्रुता पाले रखती हैं। वे ससुराल नहीं वरन् एक युद्ध के मोरचे पर जाती हैं मानो। और आने के साथ ही अपने तरकश के सारे तीर बगटुट प्रयोग में लाने लगती हैं।
कितनी भोली थीं मम्मी कि जो सोच बैठी थीं कि निम्न आर्थिक-पारिवारिक स्तर की बेटी आ कर उनके परिवार से झुककर, निभकर चलेगी ! सबको अपना समझेगी, सबकी मान-मर्यादा रखेगी ! भाभी ने तो आने के साथ ही अपने स्तर का प्रदर्शन करना शुरु कर सबको नाकों चने चबवा दिये थे। अभी भी हाल उनके वही के वही दिखते थे।
‘देख लेना लिनी! ये तेरे ससुर इतनी आसानी से सटकने के नही ! ये तुझसे अच्छे-खासे पापड़ बिलवाऐंगे !’ कोई थीं कमलिनी भाभी की हम स्तर, वे उन्हें ठठ्ठा करती हुई समझा रही थीं-ही ही ही ही- - -
’मेरे ससुर ना भैया! उन्हें पैरालिसिस हुआ। ऐसे ही कोमा में गए। पूरे छै महीने बिस्तर तोड़ा उन्होंने !’
छिः ! उसे न जाने कैसी घिन सी हो आई ।
उधर, ’हो हो हा हा ’ करती भाभी की मोटी खुरदुरी हँसी से उनका सर्कल गुलजार हो रहा था !. . .
’रहने भी दे, रहने भी दे। मसखरी छोड़! कोई कितना ही पलंग तोड़े अपन तो बाब्बा जितने दिन की छुट्टी पर आए हैं, उसके एक दिन पहले उड़ जाएंगे !’
’और जायदाद बंटवारा! ?’ भाभी की किसी व्यवहार कुशल, स्मार्ट दोस्त का चिंतित स्वर था . . . .
‘वो तो पापाजी के हाथ से सब पहले ही लिया जा चुका है। कुछेक एकड़ की जमीन भर बची है जो शायद अपनी इकलौती सुपुत्री को देना चाहता था डोकरा पर . . .. हो होहोहो . . . मुझे नहीं लगता कि ननदरानी ले पाएगी। मम्मी का थोड़ा सोना-चाँदी दे दिला कर उसका मुंह भर देंगे बस्।’
’तो फिर ननदरानी को इत्ता पहले बुलाने की क्या पड़ी थी? बाद में शोक पत्रिका दे देते!’
’अरे बाब्बा, समझो तो सही, अभ्भी उसके सिग्नेचर कहाँ हुए हैं?’
ओह् ! रत्ना के बुझे-बुझे दिल में आस की कोई बची-खुची किरण भी दम तोडती, उसे आईना दिखा़ चलती बनी थी। तो इसलिये बुलाई गई है वह !
बहक-बहक कर अंधेरा कमरे में खिड़की के अधखुले पल्लों से, अधखुले रौशनदान से, कहीं न कहीं से, धुस ही पड़ा, पसर गया था पूरे कमरे में। केवल उसके कमरे में ही नहीं, उसकी मनःस्थली पर, पूरे का पूरा आ उतरा था अपने काले डेने फैलाए ! न जाने क्यूं एक गहरा अवसाद नस-नस में खून के साथ जैसे बहने सा लगा था। न जाने आँसू कब यूं बह चले कि बस् थमते न थे। न जाने क्यों वह बस् रोए जाती थी चुपचाप ! न जाने क्यों वह खुद को एक टापू में तबदील होती पा रही थी। कोई नहीं था उसके आसपास। मानो कोई नहीं था उसका अपना। स्वार्थ में गिचगिचा, घिनौना, उफनता समुद्र और बीच में वह स्वयँं को असहाय, निस्तब्ध सी हो गई पा रही थी। कैसे पूछे भाभी से ? उनके खुद के पापाजी के प्रति भी क्या भाभी ऐसी दर्दहीन घिनौनी हँसी हँसती रह सकती थीं।
ऐसे ही जुमले तब भी छोड़तीं क्या वे ? या संभव है वे ऐसा कर सकती थीं क्योंकि उनके पिता ने सौतेली माँ के हाथों में उन्हें घर की नौकरानी सी बना कर रख छोड़ा था। लेकिन यहाँ ? यहाँ तो उनके ससुर ने उनसे एक ग्लास पानी का भी कभी उठवाया हो ! कहीं कोई स्पंदन नहीं बचा है मानो जो उसे यहाँ रोके रखे। चल, यहाँ से चल ही दे। यहाँ क्या रखा है अब ? लेकिन उसे याद आ गया फाइवस्टार होटल के जैसे दिखते अस्पताल के उस पाश वार्ड में अपनी ठहरती-बिसरती सांसें गिनता वह अपने समय का, पूरे परिवार का नायक, अपने ही बेटे-बहू जिसके पीठ फेरते ही उसकी कमाई दौलत के लिये खल पात्रों में बदल कर पूरी जाँबाजी से मानसिक कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं।
क्या सिर्फ पापाजी के लिये ही उसे नहीं रुकना चाहिये ? सूटकेस जमाने को तत्पर हो रहे मनस को बड़े जतन से रोकती है वह। उसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पापाजी की खातिर रहना है। इन अमानुषों-बनमानुषों के कारण वह क्यों अपने पापाजी से निगाहें फेर ले ? वो रहेगी यहाँ तब तक जब तक संभव होगा। ये लोग हैं क्या, जिनके कारण वह
पापाजी की छत्रछाया से अब इतने सालों के बाद आते ही फिर परे हो जाए ! मन के किसी कोने में इस परिवार की इकलौती बेटी होने का दर्प भरा अहसास अभी जीवित था। उसीने उसे निराशा के दावानल से कुंदन की भाँति उबार लिया।
बोझिल कदमों से उसने उठ कर बाथरूम में जा ठीक से मुंह धोया, पानी के छींटे दे-दे कर रोने-धोने के निशान मिटाए चेहरे से और कमरे में आ कर स्विच आॅन कर दिया।
उजली रौशनी से नहा उठा कमरा। इसी के साथ पास के ड्राइंगरुम से आ रहे बेदर्द से, जहरीले से ठहाकों पर विराम सा लग गया।
’अरे उठ गईं बीबीजी? मैं तो आने ही वाली थी आपको उठाने, कि मम्मी कहती थीं साँझ पड़े नहीं सोते।’ प्रीतो भाभी मम्मी को याद कर रही थी! हुंह फोटो पर जमी धूल पोंछने की, सूखी , पुरानी पड़ चुकी माला बदलने तक की तो किसी को फुरसत नहीं ! खैर। बैठे-ठाले याद तो किसी भी सूरत में किया ही जा सकता है ! अपनी मेहमानों को बिदा करने निकली भाभियों के सुर अब गिरगिट से रंग बदले हुए थे। रत्ना ने होंठ काट लिये, कहीं कुछ अप्रिय न निकल जाए उसके मुंह से। क्यों इन उम्मीद भरी महिलाओं के दिल तोड़े जाएं ? अपने हिस्से की माँग न कर बैठे ननद, इस चिंता में ये सब की सब मोटी-झोंटी, कद्दू की कद्दू अपनी कायाओं को भरसक खींचती-ढोती, बेचारियाँ नाहक अपनी क्षमताओं से बढ़-बढ़ कर मानसिक-शारीरिक, अधिकृत-अनधिकृत कसरतें किये जाती थीं !
‘अरे लो। मैं कब से राह देख रही थी बीबीजी उठें, तो साथ चाय-शाय हो जाए। आप तो अच्छी सोईं! लो जी नींद हो तो ऐस्सी। यहाँ पाप्पाजी की चिंता में आँखें नहीं लगतीं। इधर बीब्बीजी हमारी तो नींद के मामले में किस्सी की नहीं !’ कहती हुई फटाका सी कमलिनी भाभी दरवाजे के पास खड़ी प्रीती भाभी को ठेलतीं, झमाझम पारदर्शी इम्पोर्टेड साड़ी, परफ्यूम से लदी महकती-गमकती कमरे में समा गईं।
उसने भरपूर नजर उन्हें देखा। बस् देखा। भीतर छिपा हर भाव इस देखने में साफ नजर आ गया होगा घर में अभी-अभी दाखिल हुए प्रेम भैया को, जो भाभी के पीछे ही पीछे उसके रूम में चले आए थे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपलक उसकी चितवन का व्यंग्य क्या भाभी के सहयात्री की अनुभवी दृष्टि से छिपा रह पाया होगा ?
वह देख रही थी कि भाभी की कमर का घेरा मानो ट्रक के टायर की तरह था। बेहतरीन मँहगी शिफाॅन साड़ी निरीह, बड़ी बेरहमी से उस कमर नामक कमरे पर कस-कसा कर बांधी गई थी यद्यपि, मगर वह तो मुई, एक तरफ तो उनके भारी भरकम कूल्हों की उतनी ही चुगली कर रही थी जितनी कि उनके पेट पर पड़े असंख्य स्ट्रेचमाक्र्स को छुपा सकने में नाकामयाब थी। उधर, यही हाल स्लीवलैस नन्हें से ब्लाउज गरीब का था जो डीपनेक रूपी आतंकी से
डरा-सिकुड़ा बलहीन सिक्योरिटी गार्ड सा उनके वक्षों के असीमित उभार रूपी वीवीवीआईपीज को संभाल पाने में जरा भी सक्षम न दीखता था। या, कौन जाने कि उसे मिले किसी ऐसे ही आंतरिक आदेश के पालन में जी-जान एक करता मुस्तैदी से जुटा था बेचारा ! मँहगी डायमंड ज्वैलरी, मँहगे वस्त्र, सब कुछ मँहगी-मँहगा, इतना खर्च करके भी कुल मिला कर भाभी के ढंकने योग्य बदन को छुपा सकने में पूरी तरह असमर्थ था सब मँहगा सरंजाम। या, कि ढंकना किसने था ?
नख से शिख तक थुल-थुल चरबी ही चरबी से पटे पड़े उस चरबी के ढेर में कहाँ तो ढूंढ लेती वह अपनी किसी कमलिनी नामधारिणी भाभी को ? हालांकि वे पहले भी कोई कम ’हैल्दी’ न थीं मगर अब तो वे जरा इधर-उधर मुड़तीं थीं तो फैशनेबल छोटे से, पिद्दू से, कहो कि बित्ते भर के ब्लाउज से पीठ पर झाँकती दिखे जाती थी एक व्हाइट लाइन, आगे पेट पर असंख्य सिल्वर लाइन, फैले घुंघराले पगलाए से कई-कई शेड दे कर रंगे बाल, और मुंह में जोजो-सोसो तो ! उसने भैया की नजरों में नजरें डाल ही तो दी थीं !
भैया इधर-उधर न करने लगते तो और क्या करते ? .......... उसे हमेशा सलीके से कपड़े पहनने की सलाहें दिया करते थे कभी यही भैया ! कितना तरसती रह जाती थी वह स्लीवलैस ड्रेस के लिये ! पर, इन्हीं भैया की जिद थी कि कपड़े शरीर की शान बढ़ाने वाले होने चाहिये।
‘मैं नहीं ले जाउंगा तुझे कहीं भी अपने साथ!’
‘ऐसे कपड़े तुझे सूट नहीं करते! जो मुझे राखी बाँधनी हो रत्नोंबाला, तो खबरदार जो ऐसे-वैसे, बेढंगे कपड़े पहने, सुन लिया ना रतनारानी !’
पता नहीं भैया भाभी को रोकते-टोकते नहीं या उनकी रोक-टोक भाभी पर चलती नहीं या.......फिर यही तो, कि भैया को भाभी से कोई राखी थोड़े ही ना बंधवानी है ! उसे अनायास ही हँसी सी आने लगी थी जो लाख रोकने के बावजूद
भी प्रकट हो ही गई थी। उसकी उस हल्की सी हँसी में छिपा व्यंग्य न समझ पाएं ऐसे बेवकूफ उसके भैया तो कम से कम नहीं ही थे !
’ये क्या तुम लिनी? कुछ तो वक्त-बेवक्त देखा करो। क्या लाद रखा है ? क्या लटका रखा है ? कैसी लग रही हो !
लोग आ रहे हैं कि पापाजी बीमार हैं और तुम यूं घूम रही हो जैसे यहाँ किसी की शादी में आई हो !’
भाभी ने आग्नेय नैत्रों से रत्ना को घूरा था। ना,
रत्ना ने कुछ ना कहा था ! जो कुछ कहा था भैया ने ही तो कहा था। फिर वह धधकती निगाह उस पर क्यों ?
’मैं तो ऐस्से ही रहूंगी जैस्से रहती हूँ। हाँ! कोई मरेगा तो मैं उसके साथ मर जाऊँ क्या ? अरे तुम्हें जाना है तो जाओ। मम्मी मरे थे तब भी तुम यही सब बकते रहते थे। अब फिर वही किच-किच। जब देखो मेरा मूड आॅफ करते हो। ऐसा ही था तो मैंने आ कर गल्ती की। तुम कल का ही मेरा टिकट बनवा दो, मैं वापस चली जाती हूं !’
बिफरती भाभी समय, परिस्थिति, सामने उपस्थित व्यक्ति, उसकी मजबूरियाँ, उसके हालात आदि कुछ भी तो देखने-समझने को कभी तैयार न थीं। अभी भी तो जैसे उन्होंने भैया के साथ आ कर एहसान किया हो। यूं तैश दिखा रही थीं कि जरा चूं-चपड़ की तो वे अपना एयरबैग उठाएंगी और फ्रेंकफर्ट चली जाएंगी सीधी। जैसे फ्रेंकफर्ट में ही जन्मी हों ! उसे यह भाँपते जरा देर नहीं लगी कि भैया अपने गले पड़ गए ढोल को बस् किसी तरह जैसे-तैसे ढोए जा रहे थे। भैया को आहत देखना उसे नहीं पोसाता। लेकिन, आश्चर्य कि-
प्रेम भैया और इतने लाचार ? जो भी हो, थे तो उसके भैया ही, वही भैया जो बचपन में कभी गधे के रेंकने पर अपनी मुट्ठियों में फूंकते हुए उसे छेड़ते थे.........
’रत्नो, वाह वाह, तेरे देवर ने तो क्या गला पाया है! चल जरा कोई मीठी चीज खिला दे।’
वह गुस्से से भर कर धमाधम उन पर अपने मुक्कों की बौछार कर डालती ,वे बचने का ढोंग करते सबको हंसाया करते ......... हंसा-हंसा कर दोहरा कर दिया करते।
’ऐ पगलू, मुक्के नहीं मिठाई खिलाने को कह रहा हूं मैं। क्या सुरीली तान थी तेरे देवर की रे !’
’पगली। तू क्यों गुस्सा करती है?’ मम्मी उसे समझातीं। ‘गुस्सा करती है, चिढ़ जाती है तभी तो भाई लोग छेड़ते हैं। तू चिढ़ मत। उल्टे कह दे कि वो मेरा देवर है तो तुम्हारा भी तो कुछ लगता है।’ पर प्रेम भैया कहाँ हार मानने वाले होते ? ’क्या करें जब ऐसे रिश्तेदार हों तो?’ भाई-बहन की नोंक-झोंक कभी तो बंद होती हो !
’भाभी, आप गुस्सा करते हो, चिढ़ जाते हो न, इसीसे भैया आपको चिढ़ाते हैं। मत किया करो इतना गुस्सा ।’......... उसने मम्मी की ही तरह बीच में पड़ना चाहा था, भैया की अचकचाई नजर ने जैसे एकदम ही उससे पूछा था सच्!
सच् ! क्या तुझे वह सब याद है ? हां, उसे कुछ न भूला था। सब कुछ तो याद था-
शुरू-शुरू में भाभी जब आई-आईं ही थीं तब भी वे ऐसे ही उफनती थीं। मम्मी उन्हें किसी न किसी प्रकार समझाने के प्रयास करती थीं। चाहती थीं मम्मी बेचारी कि सभ्य घर की बहू ऐसे बात-चीत किया करे कि घर के बाहर तो क्या, एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी आवाज न जाए। मगर भाभी ने तो अपनी ’सास गले की फांस’ से किसी तरह कुछ ना सीखने की कसम खा रखी थी मानो ! हाँ नव धनाढ्यों के जैसे सारे तौर-तरीके चुटकियों में सीख डाले थे बिना किसी के सिखाऐ ! वहीं, अपने उठने-बैठने के, बोलने-बतियाने के पारिवारिक संस्कार एक-आध इंच भी न भुला सकी थीं। आज तक वैसी की वैसी ही थीं !
‘मैं कहाँ गुस्सा करती हूँ? ये तो बस् बात-बात पर मुझे ऐसे सुनाते हैं जैस्से बस् मैं ही अपराधी हूँ ! अब जरा अच्छे से पहन-ओढ़ लो तो आफत, नहीं पहनो-आढ़ो तो भी आफत ही आफत ! सारे तौर-तरीके क्या तुम्ही लोगों को आते हैं ? ऐसा ही है तो क्यों लाए थे ब्याह कर के ? या अभी भी छोड़ क्यों नहीं देते ?’ इल्जाम लगाना, जली-कटी सुनाना, धमकी-चमकी देना कुछ भी नहीं छूटा था भाभी से तो !
‘ओफ्ओ, अब रहने भी दीजिये न दीदी! अपन ही तो ठहरे छोटे घर के !’
प्रीतो भाभी बड़ी भाभी को बड़े अदब से संभालती थीं एक तरफ, दूसरी तरफ रत्ना की भी लू जबरन उतारे लेती थीं-एक पंथ दो काज !
’मैं तो कहूं भैया, कि बेट्टी भले ही छोट्टे घर में दे दो वो चलेगा! वहाँ नखरे उठवाती ठाठ्ठों से अपना मायका-शायका भूली रहेगी, पर भैया ! अपने से बड़े घर में बेट्टी ब्याहो तो चार उलाहने हर साँस में सहने का कलेजा दहेज में दे कर ही ब्याहो !’ प्रीतो भाभी को कब कहां ससुर-जेठ का कोई लिहाज रहा ?
रत्ना के बोल तो उनके सामने मुंह में जमे ही रहते थे, भैया भी निरूत्तर से हो कर पास रखे राॅकर पर ढह ही तो गए थे। झुलईंयाँ लेता राॅकर उनकी अंदरूनी बेचैनी को स्पष्ट उजागर कर रहा था मगर भाभियों में किसे थी परवाह ?
‘चलिये छोड़िये, बीबीजी को कुछ खिला-पिला तो दें, जब से आई हैं कुछ लिया नहीं है ठीक से।’ प्रीतो भाभी जबरदस्ती कमलिनी भाभी का हाथ पकड़ खींचती उन्हें डाइनिंग हाॅल की ओर ले चली थीं।
‘शिट्। किसीको खाना है खाऐ, मरना है मरे, मैं क्यों परेशान होऊँ ? एक तो सुबह-सुबह से यहाँ आने-जाने वाले नाक में दम कर देते हैँ , दूसरे इत्ता सब सुनो-झेलो इन सबको, वो अलग ! कैसा है ये परिवार बाब्बा रे ! कैस्से कोई रह सकता है यहाँ !’
‘कैसे नहीं रहेंगे ? कहाँ जाएंगे भला ? हमें तो रहना ही पड़ता है न यहाँ ! आप तो वहाँ जर्मनी में ऐश कर रही हैं। हमें तो कोई निजात नहीं। रह ही रहे हैं न ?’
प्रीतो भाभी और कमलिनी भाभी दोनों में से कोई किसी से कम होने को तैयार नहीं। एक छुरी तो दूजी कटार !
भैया राॅकर की पुश्त पर सिर टिकाए छत पर न जाने क्या घूरते थे चुपचाप, जैसे कुछ न सुना हो ! वह अपराधी सी दुपट्टे का किनारा अंगुली में खोलती-लपेटती समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे , .......... भैया का उखड़ा मूड देख
पापाजी के बारे में भी कुछ पूछने की हिम्मत न हुई थी। सब जस का तस ही होगा। अच्छा या कि बुरा, सुधार या कि बिगाड़ होने पर ही तो सबको खबर दी जाएगी।
दरवाजे पर ठक् ठक् की आवाज करती, जरूरत से ज्यादह ही वैलमैनर्ड बनने का स्वांग सा करती पुनीता भाभी अपनी मनों-टनों वजनी काया को किसी तरह खींचती-ढकेलती आ गईं थीं खाने के लिये इसरार करती उसे लिवाने। इनकी ही कमी थी। जैसे भैया ने एक हल्की सी उसाँस छोड़ी थी और उठ खड़े हुए थे।
‘तूने कुछ खाया नहीं? हें ? इस तरह भूखे रहने से पापाजी ठीक हो जाएंगें क्या ? ’ भैया ने लाड़ से उसे झिड़का था। न जाने क्यों वह इतने से लाड़-प्यार से रोवनियां होने लगती थी इन दिनों। और वैसे भी भैया को यह कौन याद दिलाऐ कि यूं मेहमान बना कर गेस्टरूम में जिसे ठहरा दिया है वह उनकी बहन मम्मी के कहे सदा मंगलवार का व्रत करती आई है, और व्रत न भी रखा हो तो, कब अपने आप ले कर खाती थी कभी ?
जब आप ही भूल गए तो भाभियों ने याद रख कर क्या करना था वह सब ?
मत करो, मत करो, मत दिखाओ अब कोई इतना लाड़-मनुहार ! उसका हृदय हिलक-हिलक उठा था। कहीं कुछ टूटता दरकता था भीतर ही भीतर चुपचाप का चुपचाप।
‘कहें तो बीब्बीजी खाना यहीं लगवा दें आपका ?’
यह कोई आज की बात नहीं, वह अपने बचपन से ही देखती आई थी कि भरपूर खाने की उम्र में भी एक दो बार के छिटपुट से, मुठ्ठी भर इधर-उधर की चीजों से ही उसका पेट यूं भर जाता था कि जब-तब मम्मी अफसोस सा करती रहती थीं कि-
‘पेट के नाम पर तो रत्नों, तू बस् एक छोटी सी कटोरी ही ले कर आई है !’
अब कुछ वैसा तो था नहीं जिसे भूख कहते हैं पर नहीं कुछ खाने से भी न जाने भाभियों के दिलों पर क्या बीते, जिस सबको वे भाईयों पर ही तो उंडेलेंगी। वैसे भी वो थोड़ा सबके बीच, खास कर बच्चा पार्टी के बीच रहने की अपनी दिली इच्छा दिल ही दिल में न दबा पाई।
‘नहीं भाभी, मैं बस् आती हूँ।’ यही सोच कर कि बच्चों में जी अच्छा बहल जाएगा वह फटाफट फ्रेश हो कर डाइनिंग हाॅल पहुंच गई थी।
मगर क्या था वहाँ जी बहलने जैसा कुछ ? बच्चे जो कि कुछ बड़े हो चुके थे उनका डिनर उनके कमरों में भेजा जा चुका था। उनमें से कुछ पहले ही खा-खिला के अपने-अपने बेडरूम में भेजे जा चुके थे। न जाने किस बात से बचने को अजब सी खामोशी में, ऊहा-पोह में लिपटे भाई लोग, न जाने कैसी तो उधेड़-बुन में, तुक-ताँय में उलझी-उलझी सी भाभियों के साथ उससे तो कुछ ठीक से खाया न जाता था।
शुक्ला चाची बेचारी इसरार कर-कर के थकी जाती थी। उसका नाम दरअसल सुकला था सु-कला, लेकिन होते-होते वह कब शुक्ला हो गई थी खुद उसे भी नहीं पता होगा। कितने सलीके से रहने लगी थी अब वह ! लगता था उसे ऐसे रहने को भाभी लोगों का कुछ आदेश सा ही रहता होगा वरना कहाँ शुक्ला चाची और कहाँ उसका ये सधा हुआ
रंग-ढंग ! वह तो यूं लबड धों-धों थी कि मम्मी आए दिन उस पर बरजा करती थीं-
‘मरी शुक्ली, थोड़ा तो सामना-सूमना ढाँक-ढूंक लिया कर! अरे तुझसे नहीं संभलती तो क्यों लपेटे फिरती है साड़ी ? ले चल मेरे कुछ सलवार सूट ले जा, शुरू कर दे पहनना। कम से कम तेरा शरीर तो निगोड़ा कुछ ढँका-दबा रहेगा री..........’
मगर कहाँ ले गई मम्मी से कभी कोई सूट शुक्ला चाची ?
‘ना बीजी ना, हमसे तो ना छोड़ा जाएगा अपना पेहनावा। आँचरा बिना लाज कहाँ ढंके है ?’
‘ओहो में तो वारी जाउं तेरी लाज पे! पर ये बता, के भला कहीं से ढंकती भी है तेरी ये साड़ी, तेरी उस लाज को ?’
शुक्ला चाची बस् सिर पर पल्ला भर रखे रहती। फिर और क्या चाहिये था उसे ? सिर पे पल्ला रहना चाहिये, भले ही पीछे से पीठ पर ऊँचे चढ़े जाते ब्लाउज से, कभी किसी जमाने में सफेद कही जा सकने वाली, निहायत मैली-कुचैली अंर्तवस्त्र की पट्टी सी झांके या काम-काज निबटाने की धुन में उसकी साड़ी का पल्लू सामने से हमेशा ही इधर-उधर ढलका रहे ! बस् सिर ढँक लिया तो सब जायज है इन लोगों में। इसी से मान-सम्मान लिया-दिया जा सकता है !
हम बच्चों ने जब एक रोज उसके सिर ढँके रहने पर टिप्पणियों की अति ही अति कर डाली तब उसने बड़े गर्व से हमें बताया था ‘यूं कहे हैं कि महाभारत में जब द्रौपदी की लाज लुटी ही तब उसके सारा बदन नंगा हो गया हा, पर सिर से कपड़ा ना हटा हा।’
ओफ ! कितनी आसानी से ये भोले लोग धर्मग्रंथों की भी मनमानी व्याख्या करके अपना जीवन चला लेते हैं ! उनका चल भी जाता है बेखटके ! आज भी सिर पर साड़ी संभाले मुस्तैद दिख रही थी। कभी उसका पति भैंस खरीदने के लिये पापाजी से कुछ रुपये लेकर जो गया तो फिर वापस आया ही नहीं था। तब वो रकम बड़ी रकम हुआ करती थी।
जिसे ले कर वह न जाने कहाँ, न जाने क्यों चला गया था। सारे थाने-दीवाने करके, गुमशुदगी के इश्तेहार आदि दे दिला के उसकी तसल्ली का सब कर-कराके देख लिया था पापाजी ने। तब से बेचारी सिंकती-सीझती, सिसकती, झेलती वह एक मजबूर औरत अपने एक बेटे के साथ हमारे घर के कोने-कचरे की हो रही थी।
महाभारत काल में उस द्रौपदी के पतियों ने उसे दाँव पर लगा दिया था। इस युग में इस के पति ने मानो उन कुछेक रुपयों में उसे हमारे यहाँ बंधक रख दिया ! यह बात और है कि उसे परिवार की जरुरतों व संस्कारों के चलते कभी बंधक नहीं समझा गया। मम्मी उससे हमेशा ढंग से व्यवहार करती थीं। उसे पूरी पनाह दिये रहतीं। उससे क्या उनका तो सभी नौकर-चाकरों से ऐसा ही व्यवहार होता था कि वे बेखौफ यहाँ शरण पाए रहते। कमलिनी भाभी ने आ कर थोड़ी नाक-भौं-चढ़ाई थीं। उन्हें नौकरों को इंसान समझने से कुछ गुरेज सा था, इन संर्दभों में मगर मम्मी को
बदलना ग्लोब को चौकोर करने की तरह असंभव कार्य था। सो इस मामले में भाभी की उनके आगे एक ना चली।
‘शुक्ला चाची पानी ..........
‘चाची सलाद ..........
‘चाची दही, ..........’
‘शुक्ला चाची स्पून, .......... चाची, चाची और शुक्ला चाची.......... !
कभी मजबूरी में इसे रखना पड़ा था क्योंकि उसके पति के द्वारा लिया गया कर्ज चुकाना उसके काम करने की मजबूरी थी, उसकी जरुरत थी। धीरे-धीरे वह इस परिवार की जरुरत बन चुकी थी। हालांकि अब उसका ’ओहदा’ और बढ़ चुका लगता था। अब वह मानो नौकरों की मैनेजर थी। उसकी मदद को अनेक नौकर थे जिनसे काम
करवाने की, घर की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उसीकी थी। सब कुछ उसीके भरोसे था। क्षण-क्षण खनकते चम्मचों-क्राकरी की मिली-जुली आवाज में ‘शुक्ला चाची-शुक्ला चाची’ की आवाज भी मिली जुली थी ! बिना उसके मानो कैसे क्या होता ? यह नाम राम नाम की तरह रटा जा रहा था। बस् एक माला और दे दो हाथों में !
सरल-तरल ह्दया मम्मी के साए में उसकी सारी जवानी मानो उन्हीं की नपी-तुली, सुघड़ संतुलित देख-रेख में बीत गई थी, तब वह इतना सलीका न सीख पाई थी कभी। अब वृद्धावस्था दस्तक देती आ लगी थी उसके शरीर से। जरुर भाभियों की धौंस ने ही उसे इस उमर में इतना सलीका सिखा दिया होगा।
रत्ना को समझ में नहीं आता था कि उसे चकित होना चाहिये या खुश होना चाहिये या दुखी। . . . . . . .किसी किसी के
साफ-सुथरे, सलीके वाले परिधानों से भी उसके मटमैले दुख आखिर क्यों इतना झांकते हैं ?
थोड़ी-थोड़ी देर सूजे पैरों की, गठिया के जोड़ों के दर्द की दुहाई दे-दे कर आराम कुर्सी पर सोफों, दीवानों पर ढुलक-ढुलक जाती भाभियों की तुलना में वह बेचारी अनवरत फिरकनी सी घूमती-फिरती खड़ी-खड़ी ही दिखी है। उसे क्या आराम की इच्छा न पकड़ती होगी ? उसके जोड़ों में इस उमर में भी दर्द नहीं होता ? क्या उसके पैर नहीं सूजते होंगे ?
सूजते भी हों तो किसे दिखा सकती है ? कहाँ आराम के दो क्षण निकाल पाती होगी बेचारी ?
एक-एक निवाला निगलते मानों गले में कुछ फंस-फंस जाता लगता था रत्ना के। यह शुक्ला चाची का दर्द था कि पापाजी की असहायता से उपजा दुख व किसी आसन्न घड़ी की प्रतीक्षा का या, इतने अंतराल के बाद मायके में बदल चुकी परिस्थितियों से अपने भीतर ही भीतर चल रही जद्दो-जहद का ही मिला-जुला असर था जो रह-रहकर उसे दुख के भाव, आँसुओं को गटकने जैसी स्थितियों से दो चार किये जाता था।
‘तो बीबीजी आप भी सोने की कोशिश करो जी ननदोई जी की याद को लेकर...!’
कमलिनी भाभी ने भैयाओं की उपस्थिति भी नहीं सोची-देखी.... वे नींबू पानी के बाउल में अंगुलियाँ धो रही थीं। ’हमें तो खाने-पीने के बाद भई बिस्तर चाहिये हम तो चले ...... ’ बाकी भाभियों ने थोड़ी फाॅर्मेलिटी पूरी की। फिर वे भी एक के पीछे एक सरक लीं थीं। भाइयों के साथ यद्यपि अब जा कर गिले-शिकवे दूर करने का समय मिला लगता था मगर, दिन भर की दौड़-धूप की थकान से क्लाँत उनके चेहरों पर ऐसी कोई उत्कंठा न थी।
’सुबह मिलते है रत्नों, सो जा अब’
मंझले व छोटू भैया बड़े भैया यानि प्रेम भैया से पापाजी के बारे में कुछ बतिया रहे थे मगर उनकी भाषा चिकित्सकीय अधिक थी। पापाजी के व्यवसाय का ही असर था यह कि वे डाॅक्टरों के बीच रहते-रहते मानो आधे डाॅक्टर हो चुके लगते थे। उसे लगा कि वे या तो कुछ स्पष्ट जानते न हों या बताना नहीं चाहते थे। . . . .
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
3-
उसे जैसे भैया ने आदेश सा दे दिया था। अतः उसे वहाँ रुकना गैर जरुरी लगा। उसके भारी कदम उसे अपने रुम में खींच ले गए। जबकि अभी नींद तो कोसों दूर थी। कुछ पढ़े बिना तो उसे वैसे भी नींद नहीं आती थी। यहाँ तो कुछ पढ़ने को था भी नहीं। आराम कुर्सी पर निढाल वह क्या कर सकती थी दूर लखनऊ में बैठे अपने पति व बच्चों की याद करने के सिवाय ? अपने मोबाइल से उन लोगो से बातें तो कर सकती थी। पापाजी की स्थिर हालत के बारे में बता सकती थी। चलो कर लो यह भी। फिर,
सिवाय सोने के अब कोई काम बचा न दीखता था, सो आँखें मूंद तो ली थीं पर नींद थी कि कोसों दूर थी .......। इस हाल में, अपने ही घर-आंगन में, न जाने कैसा क्या खो गया, बिछड़ गया था कि कहीं किसी सूत्र से स्वयँ को जोड़ नहीं पा रही थी।
दरवाजे के धीरे से खुलने की आवाज होने पर उसने मुंदी पलकें भरसक खोल कर देखा तो शुक्ला चाची को चाँदी की ट्रे में चाँदी के कप में कॅाफी और बगल में कोई पत्रिका लिये खड़े पाया। चाची के चेहरे पर घिर आई झुर्रियां उसकी ममत्व भरी मुस्कान को और बढ़ा ही रही थीं। कम तो क्या कर पातीं !
वही उसका चाँदी वाला सेट क्या अब तक याद है चाची को ? और ....और....
‘हमें पता था बिटिया, मम्मीजी के लाख मना करने के बाद भी काॅफी पिये बिना, कुछ पढ़े बिना सोती नहीं थीं तब ? अब भी पीती हो न ?’
‘............’
‘हम ने तो केह दई तिवारी खानसामे से, के तिवारीजी और जो कछु बी करना हो करलेव, पर जे काॅफी तो हमींसे बनेगी !’
वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही चाची इतने सारे कामों के पहाड़ के पहाड़ से दबी हुई भी कैसे काॅफी रुपी उसकी तात्कालीन संजीवनी बूटी को याद रख पाई आज तक ? उसने तो कभी का काॅफी-शाॅफी पीना छोड़ दिया लेकिन चाची का मन क्यों तोड़ना ? कितने अरमान से बेचारी उसके लिये वही, उसी तरीके से घोंट-घोंट कर काॅफी बना कर लाई है। अब,
जब, कि उसे पता था कि सब सोने ऊपर जा चुके हैं, अब उसे किसी का डर न था सो साड़ी फिर वैसे ही लतरती हुई, कंधे व पल्लू से लगी पिन हटने से बेतरतीब। अब लगी उसे शुक्ला चाची वही पुरानी चाची, वही अपनी-अपनी सी। उसे काॅफी थमाते वह कारपेट पर धम्म से बैठ गई।
‘अरे चाची, यहाँ बैठो मेरे पास !’ उसने पास रखे स्टूल की तरफ इशारा किया।
उसे याद है मम्मी के समय वह मम्मी से नीचे बैठकर ही बतियाती थी किंतु उसके अनुरोध पर अवश्य उसके पलंग के पैताने बैठ जाया करती थी।
‘नहीं बिटिया अब हमें मजबूर मत करो। मम्मी जी के बाद आप ही हमारे लिये हो। थोड़ा-तनिक हमारी भी मान लो ............’
उसका जी लरज आया। गऐ हुओं की इतनी याद भी अच्छी नहीं होती। पढ़ा था उसने कहीं कि जितना हम उन लोगों की याद कर-करके रोते-दुखी होते हैं उन्हें भी उस लोक में कहीं ज्यादा दुख पहुँचाते हैं। बनिस्बत इसके, यदि उनकी आत्मा की शांति, उन्नति के लिये सच्ची प्रार्थना करें तो वे मोक्ष-पथ में ऊँचे उठते जाते हैं। यहाँ, हमारे द्वारा की गई दुआएं, उनकी उस दुनिया की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होती है। न जाने कैसा यकीन सा हो उठा था उसे इस सबमें कि रोने-धोने के बदले अपने तमाम दुख को, उनके अभाव के दुख को अपनी हार्दिक प्रार्थनाओं में ही बदल डालने को तत्पर रहती थी।
पीड़ाओं के दहक भरे आँवे में, कहो कि धीरे-धीरे बढ़ाई जाती आँच में तप-तप कर बना कोई मिटटी का बरतन थी वह मानो। शिल्पकार की साधना, उसी का दिया रुपाकार सब उसमें राई-रत्ती रचा-बसा था। ताप से निकल धीरे-धीरे ठंडे हो गए बरतन में शीतल जल भरने पर वह वातावरण से ठंडक खींच लेता है। ऐसे ही था उसका तरह-तरह से तपाया जा चुका हृदय जो वातावरण से दर्द के कण कण अपने भीतर जज्ब कर लेता था।
मम्मी के साए में ऐसे ही पाला गया था उसे। लाखों लाड़-प्यार के बीच भी यह अहसास उसमें भर दिया गया था कि वह लड़की है ! और मम्मी के ज्ञान के दायरे का यह अलिखित, अनकहा दस्तूर था कि लड़की को तमाम दर्द सहने आने चाहिये !
पापाजी जब बिजनेस टूर से वापस लौटते थे तो भी तो वे सब भाई-बहन कितनी-कितनी रात गए तक पूरी शिद्दत से जागते रहते थे। क्या इतने दिनों के बाद आज यह रस्म थोड़ी बहुत ही सही निबाही नहीं जा सकती थी ?
मगर मम्मी के दिये संस्कारों ने ही उसे जज्ब करना सिखाया। वहीं,
वह धीरे-धीरे अपने अनुभवों से यह सीखती गई कि एक मिट्टी, एक हाथ, एक ही आंवे से निकले तमाम बरतन एक ही ताप नहीं सह सकते, एक जैसी ठंडक नहीं दे सकते। कई बार इसका फैसला परिस्थितियाँ, समय और खुद बरतन की हैसियत करती हैं कि कौन सा बरतन कितना ताप सहेगा !
वह आने के समय से ही महसूस कर रही थी कि भाभियाँ आँखों में अनेक प्रश्न लिये अपने-अपने पतियों को किन्हीं अजब सी निगाहों से देखती मिलती थीं कई बार, जैसे वे जानना चाहतीं हों कि क्या बात हुई ? कुछ बनी बात ? और भाई लोग ?
लोग उससे खुलने से झिझक रहे हैं। उसी अपनी बहन से जिसे कभी चोटी पकड़-पकड़ सताते थे ! एक ही परिवार, एक ही खेत की मिट्टी में कितना फर्क ! कितनी अलग-अलग ताब ! एक पराऐपन की गंध आ समाई थी। एक ही मिट्टी से बने पात्र हालात के भरोसे, अलग-अलग स्वरुप, क्षमता अलग-अलग स्वभाव के हो रहे थे-कोई सहनशीलता की नाँद, कोई व्यावहारिकता-सांसारिकता से लबालब मर्तबान ....... ऊपर से अपनी-अपनी पहचान के प्रति अनभिज्ञ या पहचान छिपाने की कोशिश करते हुए से। पापाजी बीमार थे तो क्यों भाई लोग उसके पास आ खुल कर बतियाने से बचते फिर रहे, उसकी आँखों में आँखें नहीं डाल रहे ?
इसमें किसी की कोई गलती थोड़े ही है कि पापाजी कोमा में है ! उम्र का असर है, भगवान से मुलाकात का समय हो चला है, तो उससे क्यों आँखं चुराई जा रही हैं !
‘कैसे..........? कैसे, बिट्टो रानी ? कैसे हुए पापाजी बीमार ! पूछो तो तनिक !’
‘कैसे भला !..........’ उसने धड़क-धड़क कर बाहर ही निकल पड़ने को बेताब ह्दय को न जाने कैसे काबू में कर पूछा था। शुक्ला चाची घर को राई-रत्ती जानती थी। घर का चलता-फिरता इन्साइक्लोपीडिया थी।
‘तुम काॅफी खतम करो लाड़ो। हम तनिक दरवाजा उढ़काए दें ।’
’उसीयत-फसीयत सब्बै तैयार थी। कजाने कौन-कौन कागद-पत्तर तैयार थे, बस् पापाजी से सैन ( साइन) भर ना करा पाए भैयाजन !’
पर, ऐसी क्या बात थी जो चाची को चटकनी लगाना जरुरी लगा था ?
बात ऐसी ही थी। पापाजी ओर दोनों भाइयों के बीच बात बढ़ती गई, बात बढ़ती गई कि ‘रत्ना एस्टेट’ के पूर्वी ईशान क्षेत्र की खाली जमीन जो कि अभी भी गगन चुम्बी इमारतों के बीच हरियाले समंदर की तरह पसरी हुई थी, की विशाल ह्दयस्थली पर एक और विशाल हाॅस्पीटल बना दिया जाए। या फिर,
पापाजी बड़े भैया की देश वापसी की जो उमीद लगाए बैठे हैं वह तभी पूरी हो सकती थी जब उस जमीन पर एक अच्छा कम से कम थ्री स्टार होटल बनाने की मंजूरी पापाजी दे दें क्योंकि कमलिनी भाभी के लेखे घर का होटल-शोटल होने से खाना बनाने आदि के सारे जंजाल ही खत्म ! वे तभी इंडिया वापस आने की हांँ करेंगी ! भैया के बिजनेस में वे बराबर की पार्टनर थीें, इसकी पूरी ठसक उनकी रग-रग, रेशे-रेशे से टपकती थी ! और इतना ही नहीं उस जमीन में पानी का जो अथाह भंडार है उसे ले कर मिनरल वाॅटर की फैक्ट्री डालने की भी तीनों भाइयों की हांँ थी।
पापाजी, जाहिर है कि इसमें से किसीके भी पक्ष में नहीं थे। प्रेम भैया से बात की गई, तो बहुत पहले ही अपने हिस्से की काफी संपत्ति ले कर वहीं जर्मनी के फ्रेंकफर्ट में सेटल हो गए प्रेम भैया ने भी बाकी भाइयों का ही साथ देते हुए पापाजी की एक न चलने दी। हताश पापाजी आक्रोशित भी थे। फोन परे पटक कर अपना ह्दय सहलाते रहे। बैचेनी में इधर-उधर होते रहे। एसी में भी पसीने से लथपथ होते रहे। यह नौकरों की समझ में नहीं आया, भाभियों को न दिखा यहाँं तक तो ठीक ! लेकिन दोनों समझदार भैया लोगों की भी समझ में क्यों न आया ?..........किसीको कहीं कोई परवाह न थी। और,
बैचेनी भरे जागरण में बीती रात के बाद, अगली सुबह वाॅकिंग से लौट, नहा-धो कर, पूजा-पाठ निबटा कर आदतन न्यूज पेपर देख ही रहे थे पापाजी कि ‘साइलेंट अटैक’ ने उन्हें कोमा की स्थिति में ला दिया।
‘वो तो सच्ची बीबीजी, जो प्रीतो भाभी न आई होतीं तो सब्बै का सब्ब तब्भी के तबी खतम था, उन्होंने चीख-पुकार मचाई और भैयाजन नाइटडरेस में थे। वैसे ही भागे उन्हें अस्पताल ले गए ?’
अस्पताल खुद मंझले व छोटे भैया मिलकर ही चलाते थे। कभी जिसे पापाजी के किसी एक पार्टनर ने बैंक व पापाजी के आर्थिक सहयोग से एक छोटे से अस्पताल के रूप में शुरू किया था, वह इस प्रकार घाटे की बलि चढ़ा कि पापाजी व बैंक द्वारा दिया हुआ लोन न चुका पाने की स्थिति में वह अस्पताल स्वयँ पापाजी व प्रेम भैया को ही तब आनन-फानन खरीदना पड़ा था। तब तक बाकी दोनों भैया लोग अपनी-अपनी पढ़ाई-लिखाई से तौबा कर चुके थे। लेकिन उनके सधे हुए बिजनेस नेटवर्क के चलते वही घाटे में जाता अस्पताल मानो चुटकियों में, अस्पताल तो क्या अच्छा खासा फाइव स्टाॅर होटल ही सा हीे रहा था। जो दवाओं की गंध, बीमार व बीमारियों की उपस्थिति न दिखे तो सर्वसुविधायुक्त होटल ही था आलीशान। इसी आलीशान अस्पताल में कि जिसका उद्घाटन कभी स्वयँ पापाजी ने ही किया था आज वे खुद बेसुध हुए पड़े थे !
उसे याद है कि पापाजी बड़े निराश हुए थे जब मंझले भैया का मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनकी इच्छा थी कि एक बेटा उनका बिजनेस संभाले, घर में एक डाॅक्टर भी हो और एक हो बेहतरीन वकील। निहायत अपने सब। मगर काफी कोशिशों के बाद छोटे भैया भी जब पढ़ाई-लिखाई की रेस से बाहर ही हो लिये थे, एलएलबी की अनिवार्य योग्यता यानि ग्रेज्यूएशन में भी जब वे बार-बार लुढ़क रहे थे, तोे भी खासी जमा पूंजी लगाकर दादाजी के नाम पर अस्पताल खोलने के अपने इरादे से राई-रत्ती न डिगते हुए पापाजी ने, साथ ही विदेश में बसने के इच्छुक प्रेम भैया को देश में ही रोक रखने की गरज में प्रेम भैया की पार्टनरशिप में उस घाटे में जाते-डूबते अस्पताल को खरीदा था इस इच्छा शक्ति के साथ कि उसमें एक ओपीडी सदा धर्माथ इलाज के लिये होगी, और कहीं न कहीं उन्हें उमीद थी कि उनका बेटा अपने देश में ही अपने काम-काज में रम जाएगा।
आज, धर्माथ का तो पता नहीं, मगर वह हाॅस्पीटल उनकी आशाओं से कुछ क्या बल्कि कहीं अधिक ही बेहतरीन रूप में चाँदी काट रहा था। प्रेम भैया को यद्यपि पापाजी अपने देश में न रोक पाए। उनके पीछे, दोनों भैया काफी अच्छे से पापाजी के मेडिकल इक्विपमेंट्स के बिजनेस के धुरंधर माने जाते थे। उधर, उस नामी हो चले हाॅस्पीटल में अनेक नामी-गरामी स्पेशलिस्ट बुलाए जाते थे। कुल मिला कर मरीज के बेहतर से बेहतर इलाज की पूरी व्यवस्था थी बशर्ते कि वह गाँठ का पूरा पक्का हो !
मंझले भैया शुरु से पूरा संसारीपन दिखलाते थे। उसका पाॅकेटमनी उससे छीन-झपट लिया करते- ‘तू तो घर में रहती है, तुझे क्या जरुरत पड़ती है इत्ते पैसों की ?’
छोटू भैया रही-सही कसर पूरी कर देते थे-
’और सुन री बहना आगे जब कभी बीमार पड़ेगी तो अपने अस्पताल में फ्री इलाज करके सब हिसाब-किताब बराबर कर दिया करेंगे समझी !’
‘मम्मी इन्हें डाॅक्टर मत बनाना। देखना ये बिना फीस लिये इलाज नहीं करेंगे !’
’हट री ! मेरे हीरे जैसे बेटे को ऐसा कहती है ! और फिर फीस ना लेगें तो कैसे डाॅक्टर कहाऐंगे ? जित्ता बड़ा डाॅक्टर उत्ती ज्यादा फीस !’ मम्मी गर्व से चहकतीं। भैया तुरुप छोड़ते ‘वाह् मम्मी ! पर मम्मी डाॅक्टर अपने परिवार वालों का इलाज नहीं करता .......!’
’हाँं हाँ मम्मी भैया ठीक कह रहे हैं। अपना परिवार तो फीस देगा नहीं और बिना फीस के.....’ भैया नकली गुस्से से उसे मारते-धकियाते। यही शुक्ला चाची तब खी-खी कर हँसती थी, कहती थी,
‘मैं तो मंझले बाबू सेई इलाज कराऊँगी।’
‘तो एडवांस में ही मुझे खूब सारा भुट्टे का भरता और मेरी मनपसंद सब चीजें खिलाया करो चाची।’
‘ऐल्लो पेहले सेई फीस लेंगे।’
बेटों के डाॅक्टर न बन पाने के मम्मी के गम को अस्पताल चला कर रफूचक्कर कर दिया था भाई लोगों ने। स्थितियों से बड़ी जल्दी समायोजन कर डालती थीं मम्मी। कहती न थकती थीं वे-
’अरे गेर परे डाॅक्टरी-फाक्टरी को, अब देख लो पचास डाॅक्टर आगे-पीछे घूमें हैं !’
लड़कपन की बातें थीं। लड़कपन अपने साथ ही ले जाता तो क्या ही अच्छा होता ! अब वही चाची जो कभी अपना इलाज भैया से ही कराने की चाह रखती थी आज कह रही थी-
’इत्ते बड़े अस्पताल में जाने में भी डर लगे हैं बीबीजी। मेरे जैसे की तो उसे देखते ही जान निकल जाए हे। मंझले भैया, छोटे भैया चाहे हैं कि एक और बरांच उसी खाली पड़ी जमीन में डाल दें। परेम भैया भी पानी की बोतल की फैक्टरी और होटल डाल अपनी वापसी का रस्ता खोलना चाहें हैं।’
सब समझ में आ गया था, कुछ समझना बाकी न रहा था। भाई लोग अपनी अलग-अलग मिल्कियत चाह रहे थे ! और इसके लिये ऊँची-ऊँची आसमान छूती इमारतों में रहने वालों के इस व्यस्त इलाके में उस खाली पड़ी जमीन से बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता था।
भैयाओं की व्यापार बुद्धि ने बिल्कुल सही जगह का चुनाव किया था। मगर पापाजी उस हरियाले टुकड़े को बचाने की जुगत में थे ! इसीलिये जरुर उनके तर्क कुछ ऐसे ही रहे होंगे कि ’किनके लिये एक और हाॅस्पीटल ? किनके लिये एक और होटल ? रईसों-रसूख वालों के ही
लिये न ?’
भले ही पापाजी स्वयं खासे रईस, रसूख वाले थे। लेकिन उसे पता है कि दबे-कुचले, शोषित, गरीब के लिये उनके दिल से दया के भाव वैसे ही नहीं मिटाए जा सकते थे जैसे चंद्रमा से धब्बे ! भाई लोग उनकी इस नरमी, कोमलता को हमेशा उनकी रईसी के लिये दाग-धब्बेदार मानते थे मगर उन्हें अपने दाग-धब्बे मंजूर थे, कोई शर्म न थी उनसे, इसीलिये कितनी ही निर्धन कन्याओं के कन्यादान, कितनों की फीसें, दवाओं आदि के बिल वे चुपचाप सहज रुप से अपने पर्स के हवाले किये रहते थे। उनकी पीठ पीछे भाई भाभियों द्वारा उन्हें कोसा जाता था कि नाहक ही ऐसे गैरजिम्मेदार लोगों पर खर्चते, रुपया उड़ाते हैं।
अब
कि जब शेर बूढ़ा हो चुका है उसे सहज ही पिंजरे में डाला जा सका होगा। मल्टी स्टोरी हाॅस्पीटल, प्लस होटल, प्लस पता नहीं क्या-क्या के रास्ते का एकमात्र रोड़ा पापाजी हीे तो थे। वे टले कि सब कुछ आसान।
अपनी-अपनी व्यावहारिक-व्यावसायिक सुविधाके चलते भाइयों को क्या पापाजी की भावनाएं नहीं दिखती ? अरे इतनी भी क्या जल्दी थी ! और
कितना जीवित रहते पापाजी ? कोई सौ साल का खत्ता तो लिखवा लाए नहीं होंगे ! शादी उनकी, बताते थे बीस-इक्कीस वर्ष की उमर में हुई थी। फिर दादी व बुआ ने मिल कर मम्मी को कम दहेज व चेचक के दागों के कारण वापस लौटा दिया था। पहले भी यह सब आसान था, अभी भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मम्मी अपने मायके में यही कोई सात-आठ साल तक रहीं। जैसे-तैसे भी रख ही लिया गया था उन्हें ! आज अगर इन भाइयों को सात दिन भी बहन रखनी पड़ जाए तो ?
खैर ! पापाजी के किसी नए बने दोस्त ने उन्हें कुंवारा समझ कर उनके लिये जब लड़कियाँ खोजनी शुरु कीं तब पापाजी ने अपना पूरा किस्सा बयाँं किया !
दोस्त को तैश आ गया दोस्ती भरा। मगर अड़चन ये थी कि, तब तक मम्मी के भाई और गाँव के जिम्मेदार लोग अपनी बेकसूर बिटिया लौटाने वाले अपराधियों की जान के ग्राहक बने बैठे थे। पापाजी को तो बरसों पहले ही सुना दिया गया था कि-
‘पाहुन इधर आ मत जइयो भूल के भी कभी। नाए तो चीर के सुखा देंगे !’
दादी के सामने पीपल के पत्ते की तरह डर से थर-थर काँपने वाले पापाजी पर दोहरी मार ! वे अपनी पत्नी की निर्दोषता और अपनी माँ के दोष मन ही मन स्वीकारने के बावजूद भी पत्नी को उसका हक दे पाने में अक्षम थे। उनके उन सहृदय दोस्त ने अपने बलबूते पर मम्मी के गाँव जा कर अपनी ‘बहन’ का दर्जा दे कर उनको विदा कराया, इस बिना पर कि उन्हें दोष लगा कर वापस फेरने वाली उनकी सास का तो तब तक लकवा मारने से निधन हो चुका था। उनके कर्म की सजा वे भुगत गईं ! बाकी को क्यों भुगताना ?
ये वो दौर था जब बात की, मर्द की जुबान की कीमत हुआ करती थी। ऐसे जुमले तब खूब चलन में रहा करते थे। उन दोस्त ने मम्मी को भाभी नहीं वरन् बहन बनाया। स्वयं पापाजी के दोस्त हो कर वे देवर के स्थान पर मम्मी के भाई बन गए, और इस प्रकार एक उजड़ी गृहस्थी बसी तो मानो पापाजी के गुलशन में बहार ही बहार आ गई। वे ही वकील दोस्त आने वाले सालों में तीन अदद भानजों व एक खूबसूरत सी प्यारी सी भानजी के वकील मामा बन इस घर के गाइड, गार्जियन, फिलाॅसफर वगैरह सब हो रहे थे। कंपनी और बिजनेस के सारे कानूनी जाल-जंजाल वे ही संभाला करते। उन्हीं से मम्मी-पापा अपने सारे दुख-दर्द बाँटा करते थे। जिनमें एक दर्द यह भी था कि परंपरा कहती थी कि तीन बेटियों के बाद का बेटा या तीन बेटों के बाद की बेटी अशुभ होते हैं। पापाजी इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। अलबत्ता मम्मी की फिक्रों में वे अवश्य शामिल रहते कि कहीं उनकी तैत्तरी बिटिया का कुछ अनिष्ट न हो जाए ! उसकी पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस ओर से हमेशा सजगता बरती गई कि उसका ध्यान, दिमाग सब ठीक-ठाक है या नहीं ! क्योंकि मम्मी के लेखे यह कहा जाता था कि ऐसी संतान या तो स्वयं के लिये अशुभ लाती है या फिर परिवार के लिये !
मगर खुशी व तसल्ली की बात थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ उल्टे तैत्तरी बिटिया के आगमन के बाद पापाजी का बिजनेस खूब बढ़ा और उसी तर्ज पर वकील मामा को भी आए दिन कानूनी पचड़े ज्यादा सुलझाने पड़ते रहे। वे इसे खुशी की बात मानते थे।
’आखिर जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी इधर-उधर लगी रहती है न !’
तो प्रेम भैया का जब जन्म हुआ तब पापाजी करीब उनतीस-तीस वर्ष के रहे होगें। आज वे प्रेम भैया ही पैंतालीस-छियालीस के हो रहे हैं। तो, पापाजी की कुल उम्र पचहत्तर-छिहत्तर के आस-पास तो होगी ही। हालांकि जिसके दो-दो बेटे शहर के नामी बिजनेसमेन हों, एक बेटा बाहर खासा बिजनेस जमाए बैठा हो, जिसका खासा-चोखा हाॅस्पीटल चलता हो, जिसकी पल-पल पूरी देखरेख होनी संभव हो, उसके लिये यह उमर कोई ज्यादा नहीं, मगर............पूरी देख-रेख व इंतजाम के बाद भी एक वो आदमी जिसके ह्दय पर टनों-मनों भार हो वो आखिर कितनी उमर खींचेगा ?
क्या थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे भाई लोग ?
एकदम ही नर्सिंगहोम व होटल बनवाने जरूरी थे क्या ? क्यों उन्हें इतना चोट पहुँचाई ? और एकाध साल रूक जाते। मरने के बाद कौन बैठा रहता है देखने कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं ?
‘तुम तनिक आँखें झपक लो बिटिया। हम भी यहीं पड़ रहते हैं। अब सुबह आठ से पहले तो कोई नीचे आनी नहीं !’ शुक्ला चाची नीचे ही कारपेट पर ढेर हो रही थी। नींद उसकी आँखों में किसी तरह संभाले न संभल रही थी। दिन भर की थकान। मिनट भर को आराम कहाँ मिला होगा उसे ? भीतर-बाहर के सारे नौकरों को वापस भेज-भाज कर, घर के सब ताले बंद कर चाबी सिरहाने रखती कहती थी-
’बस् जो जल्दी जग जाओ तो तुम हमें सुबहो जगते ही उठा देना बिट्टो। बड़ी किरपा होगी, लो हम तो सोते हैं । ऐसी-फेसी में तो हमें ठंड चढ़ जाती है।’
चाची ने अपनी शाल ओढ़ ली थी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी शाॅल भर में पड़ जाती थी। मुट्ठी भर चीजें और पूरा का पूरा जीवन जी लेते हैं कुछ लोग, और फिर भी कोई शिकायत नहीं किसी से, और कुछ वे जो मुट्ठी भर सा जीवन जीने के लिये जमाने भर के सरंजाम जुटा कर भी लालच में दोहरे हुए रहते हैं। भूल ही जाते हैं कि सुविधाएं जीवन के लिये हैं न कि जीवन सुविधाओं के लिये।
थोड़ी ही देर में चाची गहरी नींद के आगोश में थी। रत्ना ने पंखा थोड़ा तेज कर एसी बंद कर दिया। अविजित को ठंड सहन नहीं होती। वे तो एसी कोच से सफर करने पर ही चार दिनों तक छींकते रहते हैं। पहले की आदतें उसकी भी कभी की छूट-छुटा गईं। अब तो वह स्वयं भी एसी में नहीं सोती। गनीमत है भाभियों कोे इस बाबत् कुछ नहीं पता वरना वे खूब हँसने-हँसाने के बहाने ढूंढ लेतीं। शायद, शायद क्या निःसंदेह उसे उन दोनों के नौकरी में होने पर हल्की टिप्पणियाँ सुननी पड़तीं। यद्यपि भाभियों के मायके उसके मायके से बेहद कमतर ही थे। फिर भी भाभियाँ अपने मायके के बखान करती न थकती थीं। जबकि अपनी ननद का मूल्याकंन वे उसके ससुराल से करती थीं ! अजीब दोहरे मानदंड थे।
रत्ना को झुंझलाहट सी होनी स्वाभाविक थी मगर उसके समस्त संस्कार उसे यही दिलासा देते थे कि ‘उन पर चिढ़ो-कुढ़ो मत, तरस खाओ। गुस्से के लायक नहीं वरन् तरस खाने लायक ही हैं वे लोग।‘ उसे फिर भी बड़ा ही आश्चर्य व अफसोस होता था कि कैसे अपेक्षया कम हैसियत व कम पैसे वाले परिवारों से भरपूर हैसियत वाले परिवार में आ कर वे औसत लड़कियाँ अपने को आदतन रईस सिद्ध करने के फितूर में, पैसे वालों की खूबियाँ अपनाने की जल्दबाजी व उथलेपन में, केवल भौतिकवादिता और निर्मोंहीपन ही को भौथरे रूप में अपना कर अधिक कू्रर व साथ ही साथ हास्यास्पद भी हो चली थीं ! वे मानवीय सहज संबंधों-रिश्तों के प्रति, जमीन से जुड़ाव के प्रति सहज आत्मीयता जैसे भावों को अपने परिवेश के लिये विजातीय मानने में बेहद आगे-आगे चल रही थीं।
शरीर उसका पूरी तरह थक चुका था। निढाल था मन, हताश था। दोनों ही अपने-अपने मानसिक-जैविक स्तरों पर निढाल हो सुस्ताना चाहते थे। घड़ी की टिक-टिक, पंखे की सर्-सर् और शुक्ला चाची की बजती नाक के खर-खर वादन के बीच न जाने कब बेआहट, दबे पाँव आ नींद ने उसे आगोश में ले लिया।
कितना ही निर्दय दर्द हो, कितना ही भयावह समां हो, नींद की कलछौंही चादर तले वह निर्दयता, वह भयावहता कुछ तो बेअसर हो ही जाते हंै। रात के अंधेरे में, नींद के दामन में उसके तमाम दुख, तमाम अवसाद रात भर के लिये ही सही कहीं छुप गए थे सुबह फिर प्रकट होने के इंतजार में।
अतल अंधेरा अपनी कालिमा में क्या-क्या नहीं समा लेता है ! जीवित बचे होने के अहसास के लिये नींद शायद सबसे ज्यादा जरुरी थी। एक आदिम सी थकन उसके पोर-पोर पर यूँ छाई हुई थी कि उफनती नींद में उसका तन-मन सब निश्चेष्टता से बिला गया था . .
4-
रात जरुर अपनी-निहायत अपनी कही जा सकती है लेकिन सुबह तो ‘काॅमन’ होती है। किस्मत से सुनने को मिली चिड़ियों कीचहचहाहट हो या सिर पर जबरदस्ती चौतरफा लदा सांसारिक शोर हो। सुबह तो सांझी ही होती है ! सांझी रौशनचेहरा सुबह चिड़ियों के चिर परिचित चहचहाहट भरे उद्घोष के साथ रात का निराकरण करती मंद गति से जब पलकों को थपथपाने लगी तब तलक तो शुक्ला चाची के पूजापाठ निबट चुके थे।
‘उठो बिटिया, भोइ भई। जाओ सुबह घूम आओ पापाजी की मनपसंद जगह’
कभी दीदीरानी, कभी बीबीजी तो कभी बिटिया कहती-पुकारती चाची रात को हाथ में काॅफी का प्याला लिये आई थी। सुबह उसके हाथ में चाय का प्याला था। रात का काॅफी पीना भी उसने कभी का छोड़ दिया और सुबह की चाय की जगह नीबू पानी ने ले ली है।
क्या करेगी शुक्ला चाची को बता कर ?
ये उसका अपना घर है। लेकिन रुटीन अपना नहीं। जो जैसा यहाँ चले वैसा चलाना ही ठीक है। ऐसे परिवर्तनों से उसे कोई उलझन नहीं होती। भले ही भाभियांँ एडजस्टमेंट को अपनी हेठी समझ अकड़ फों-फों दिखाने का कोई मौका न चूकती थीं मगर वह तो मम्मी के हाथ तले पाली ही ऐसे गई थी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर ! बड़े घर की बेटी को यह नहीं शोभा देता, वह नहीं शोभा देता। नखरे नहीं दिखाना, बकर-बकर नहीं करना, जो सामने आ जाए खा लेना।
वैसे भी आए दिन सेमिनारांे वगैरह में जाने से रुटीन गड़बड़ाता ही था। मानो यह भी एक ऐसा ही वाकया हो, कुछ यही भाव लेकर वह कुछदेर बाद माॅनिंग वाॅक पर थी।
जो पौधे तब छोटे थे अब वृक्ष हो चुके थे। कई तो काटे भी जा चुके थे। कोठी की पुरानी छटा निहायत भव्य बंगले के रुप में ढल चुकी थी। वैसे ही आस-पास फैला गार्डन भी अपना बिल्कुल नया रुप पा चुका था। गुलाबों की क्यारियाँ अलग हो चुकी थीं। मम्मी की पसंद रहा कैक्टस गार्डन भी खासा ‘रिच’ हो चुका था। जोड़े की संख्या में पंक्ति बद्ध खड़े नारियल के पौधों को बालू रेत की आधार भूमि देकर, रेतीला टच देकर माकूल माहौल देने के पूरे प्रयास किये गए दिखते थे। मह-मह करते मोहक फूलों की तरतीबवार रंगबिरंगी क्यारियाँ, कुछ गज के फासले पर-हाँ हाँ वहीं, रंगीन शेड तले जहाँ तुलसी चैरा था, वहाँं अब भी सब वैसा का वैसा ही था। किचन गार्डन वैसे ही लहलहा रहा था। अभी किचन की ओर का दरवाजा शुक्ला चाची ने खोला नहीं था। मम्मी तो अब तक तुलसी जी को जल चढ़ा चुकी होती थीं !
जो हो बड़ी तसल्ली मिली उसे। इस गार्डनिंग की परीक्षा में तो मम्मी आप की बहुओं को पूरे-पूरे माक्र्स देने ही पडे़ंगे ! हालांकि इसमें, मालियों के किये कराऐ में उनका तिल भर भी कोई क्या योगदान रहा होगा ?
सूरज अभी धरा की ओट से बस् झाँक ही रहा था। जैसे कोई शर्मीला बच्चा घर आए अजनबी से कतराता उसे छुप-छुप कर देखता हो ! ......... मैं तो यहीं की हूँ सूरज महाराज ! मुझसे कैसा परदा और कब तक परदा करोगे जी ?
......... अभी धीरे-धीरे करवट लेती तुम्हारी मस्त किरणें इस धरती के संग मिली-भगत कर तुम्हारे सारे रंग-ढंग उजागर करके रख देगीं ! धीरे-धीरे पौधों-पुष्पों पर स्नेहिल कुनकुना प्यार लुटा उन्हें जीवनदायी ऊष्मा से भर देते हो, फिर तेजी दिखलाते हो, और अंततः पस्त पड़ जाते हो, वैसे ही जैसे
पापाजी ........
कोई भी विचार पापाजी के बिना पूरा न होता था। कहीं से भी चले विचार प्रक्रिया, गतंव्य मानो एक ही था। फूल पौधों से बतियाती, चिड़ियों के करलव को बूझती-गहती वह निरुद्देश्य सी चली जाती थी। रुकते-ठिठकते से, अनमने कदमों से ........ जाना कहाँ था ? वहीं ही तो पहुँचती जा रही थी जहाँ एक और भव्य बहुमंजिले अस्पताल और शायद उसीके कहीं आस-पास में बाॅटलिंग प्लांट की नीवं रखी जानी थी। नवपत्तियाँ-कलियां फूलों की खुशगवार पैरहन पहने डाल-डाल पुलकित हो वसंत के आगमन की मुनादी करती उसकी प्रतीक्षा में बड़े जोर-शोर से बौराई जाती थीं। खिलखिलाती, इठलाती उषा पूरे नाजो-नखरे,
साजो-श्रृंगार किये उमंगती, पौधे-पौधे को, टहनी-टहनी को जगाती फिर रही थी।
कल दिन भर के अवसाद ने उसे कमरे में ही बंद रखा था। वह थोड़ा भी निकलती तो जान पाती कि वही पुराना खजाना चौतरफा बिखरा पड़ा है। रात के अंधेरे में खिड़की से जो छायाएं भुतहा सी हिलती-डुलती लग रही थीं, वे ही आकाश निहारते दरख्त उषा की लालिमा में पर्यावरण के सिपहसालार, संरक्षक और न जाने क्या-क्या के रुप में अपनी सतर तैनाती बड़े गर्व से दिखलाते,यूँ ही डटे रहने का अपना फैसला बड़ी बुलंदी से बयंाँ कर रहे थे।
बस् - - -
उनसे कुछेक गज के फासले से शुरु हो रहा था वही टुकड़ा जमीन का। अपने पोर-पोर में इलाके भर की तमाम हरीतिमा छिपाए न जाने कैसे, कितने जतनों से, सारे जमाने की खुफिया नजरों से स्वयँं को न जाने कैसे बचाए रख सका होगा गरीब ! ऐसे घने काँक्रीट के जंगल में उसका बचा रहना एक अचंभा सा ही तो लगता था ! कि जब सारे आस-पास के परिवेश ने सीमेंट-क्राँकीट, लोहे-स्टील की चादर ओढ़ लेने की मजबूरी पाल ली थी;
तब, कैसे वह जमीन का टुकड़ा निरीह अपनी सबसे अनमोल धरोहर के रुप में हरियाला आँंचल संभाले सह सका होगा ? यह तो चाची वाली द्रोपदी सा ही हो रहा !
इस हरियाले आँचल की गरिमा भरी मौजूदगी के पीछे पापाजी का आग्रह और भाई लोगों का ‘संयम’ भी अवश्य रहा होगा। पर्यावरण के प्रति पापाजी वैसे ही उतावले रहते थे जैसे कोई शिशु माँ की गोद के लिये रहे। इसी माँ की गोद के से भाव को, इसके अस्तित्व को वे अकेले आखिर कहाँ तक मिटने से रोक पाते ?
भैयाओं का संयम टूटता गया होगा और .......और...
ऐसा लगता था रत्ना को कि पीछे कोई आए जाता है। हल्के-हल्के एक दूरी से उठते कदमों की आहट वह एक दो मिनट से महसूस कर रही थी। अब तो देख ही लेना होगा कौन आ रहा है ? पंद्रह-सोलह बरस का अरसा बहुत होता है कुछ पहचानों को बिसराने के लिये, लेकिन मुड़ कर देखने के साथ ही हैरत मिश्रित खुशी सी हुई उसे कि वही माली दादा अभी भी यहीं काम कर रहे थे।
‘कैसे माली दादा चुपचाप आ रहे हो ? मैं तो डर गई थी थोड़ा !’
’कसो डर बिटिया ? हुं देख्यो के आप एकली-एकली सगरा (सारा) बाग-बगीचा छानो हो, ते डिश्टप नी करियो !’
उमर की पूरी छाप दिखती थी, कमर कुछ झुक-झुका कर बीत गए युग को रेखांकित कर रही थी लेकिन माली दादा की बात सुन कर उसे खिल-खिल हँसी आ गई ! साथ ही कुछेक पुरानी यादें भी आ डटीं । वह घर में सबसे छोटी थी, सबकी लाडली, मुंहलगी ! स्कूल से आने पर वह मम्मी की नजरें बचा कर खानसामे शेखर से अपना हिंदी का होमवर्क कराया करती थी ताकि उसकी खराब हैंडराइटिंग के कारण टीचर को लगे कि खुद बच्चे ने ही होमवर्क किया है। होमवर्क से मुक्ति पा कर कई नौकरों को अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। अंग्रेजी के वाक्य अपनी जुबान में दुहरा-दुहरा कर वे सब खूब खुश होते, हँसते थे ! माली दादा अभी भी उसी लेन पर थे।
’कतरो टेम वई ग्यो बिटिया ? कजने क्यां चाली दिया आप तो ! कदी मुंडा देखवा के बी तरसी ग्यो जीव ! (कितना समय हो गया बिटिया,न जाने कहां चली गईं आप तो ! कभी मुंह देखने को भी तरस गया मन !) अहसास गहराते थे उसके मनस में अचानक कि कैसे और क्यों उसके लिये उसका अपना आंगन पहाड़ सा तो मायका विदेश की तरह हो गया था ?
कुछ भी तो अपना न रहा हो जैसे ! आखिर ये सब क्यों हुआ ?
किससे पूछे ? कौन बताऐ उसे ?
एक लंबी उसाँंस के साथ वह अपने सोच में गडमड हुई जाती थी। कहाँ, कौन, किसी दूसरी ही दुनिया में जा बसी थी वह ? विदेश में बसे हुओं को भी इतना नहीं बिसराया जाता। तो फिर, परिवार की बेटी के लिये अपने घर से, अपने ही एक घर की दूरी इतनी असीमित क्यों बन गई थी ? बन गई या सप्रयास बना दी गई थी ? थे तो सभी अपने ही ! एक ही माँ-बाप के साए में, एक ही छत तले पले-बढ़े, फिर क्यूं सब अलग-अलग अपने मनमाने टापुओं पर जा बैठे ....?
अपने-अपने हितों और मान्यताओं के फेर में आखिर क्यूं वे अपने बीच इतना खारा का खारा समुद्र ले आए थे कि एक दूसरे तक आने के लिये उन्हें किसी दुख की घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी !
’चालो नी म्हारा साथे। हूँ आपने वोई जगा पे लई ने चालूं, जाँ बड़ा साब रोजाने के रोजाने रेस्ट करवा वास्ते जाताईज जाता था ........।’ (चलो मेरे साथ। मैं आपको उसी जगह पर ले चलता हूं जहां बड़े साहब रोज के रोज आराम करने के लिये जाते ही थे।)
अपनी हिंदी-मालवी, राजस्थानी घुली-मिली भाषा के कारण माली दादा उसे पहले भी बड़े अपने से लगते थे। उत्साह की संजीवनी से पगे वे अपनी झुकती कमर को भरसक सीधी करते फुर्ती से उसके आगे-आगे चल पड़े। आकाश अभी भी अपने उसी अनंत दुशाले में लिपटा था, सूरज जिसे थोड़े ही अंतराल से खींच डालेगा। पूरे के पूरे दिन आकाश, सूरज रुपी जिद्दी, अख्खड़ बच्चे की इस शरारत पर कुड़कुड़ाता बादलों को सूरज के पीछे लगाए-लगाए पूरे दिन हाथ मलेगा, लेकिन जिद्दी बच्चा साँझ को जब थक-थका कर शिथिल हो जाएगा तभी, चंदा मामा के हाथांे वह दुशाला फिर से आकाश को मिल सकेगा, जो दिन भर की धका-पेल में काला पड़ चुका होगा, धूल धुसरित हो चुका होगा।
फिर ............
’फिर चाँदनी मामी आएंगी और उस अंधेरी काली चादर में सितारे टाँक देंगी ताकि देखने वाले को जिद्दी बच्चे की शरारत चंगी लगने लगे।’
फिर ?........
’फिर आकाश भी शौक से वह सितारों भरी दुशाला ओढ़ इठलाएगा। अगली सुबह फिर जिद्दी बच्चा धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल वो सितारों जड़ी दुशाला छीनने की कोशिश करेगा।’
फिर क्या पापाजी ?
’क्या फिर, फिर लगा रखी है पुत्तर? बस् ऐसे ही होते जाएगा।’........
कैसे रोज-रोज चाँदनी मामी सितारे टाँके जाती हैं ? कहाँ से लाती हैं इत्ते सारे सितारे ? क्या वो रोज-रोज थकती नहीं, बोर नहीं होतीं ? और आखिर आकाश का दुशाला फट नहीं जाता ?
’हाँ बिट्टो दुशाला अब फटने लगा है !’
आज से इतने बरस पहले कि जब पापाजी उसे कहानियाँ सुना-सुना कर सुलाते थे, तब उन्होंने बताया था कि वो दुशाला सचमुच फटने लगा है। उसमें छेद पर छेद हो रहे हैं। जब वो कुछ बड़ी हुई तभी पापाजी की चिंताओं से कुछ रुबरु हो पाई थी। पर्यावरण संबंधी विचार उनके खून में दौड़ते थे। खेती-किसानी वाले घर के पढ़े-लिखे, समझदार बेटे थे। पढ़ाई के दौरान ही अपने दादाजी के साथ-साथ खेतों की देखभाल करते-करते उन्होंने माटी के सौंधेपन से अपना नाता जोड़ा, माटी से उपजे कण-कण का मोल जाना। पेड़-पौधों से नेह उनका यूं हुआ कि अपने खेतों-बागों के एक-एक पौधे को पालते-दुलराते वे धरा व आकाश के बीच संपूर्ण प्रकृति जगत् के अणु-अणु से यूं गुंथ गए, घुल मिल गए थे कि किस पौधे में कब कली चटकेगी, कब फसल का कौन सा हिस्सा पकेगा, कब कौन सा आम सबसे पहले बौराएगा वे जो-जो अनुमान लगाते राई-रत्ती गलत न निकल पाते !
इस पेड़ की उमर कितनी है ? कौन-कौन सी चिड़ियाएं इस पर अपना बसेरा बनाती हैं ? यहाँ तक कि चूहों, साँपांे, गिलहरियों, केकड़ों, टिड्डों व मकोड़ों-चींटियों की अनेक किस्मों के भी किसी जानकार तक को भी शरमा देने वाले विवरण उनके महापिटारे में ठसाठस भरे होते थे। घाघ और भड्डरी के मौसम संबंधी अनुमानों के दोहे अक्सर उनकी जुबान पर रहते थे। कभी बादलों को देख कहते-
’ये बादल बरसेंगे नहीं ....... ये तो जलचोर हैं जलचोर !
‘ये बादल आँधी के साथ उड़ लेंगे कमजोर। ये पानी क्या देंगे, ये तो घुमक्कड़ी को निकले हैं, देखती नहीं, चिड़िया धूल में नहा रही है, ये पानी के बादल ना हैं।’ उनके अनुमान के अनुसार बादल बिन पानी बरसाए लौट जाते थे।
चींटियाँ अंडे ले लेकर कहीं ऊपर को जा रही हैं, जैसे छोटे से छोटे प्राणियों के क्रिया-कलाप उनकी पारखी नजरों से बच न पाते थे। इन ही जैसे किन्हींे आधारों पर वे वातावरण को भांप कर मौसम की सही-सटीक भविष्यवाणी करते कह देते थे कभी -
‘लाली वे, ये भरपूर बारिश के आसार हैं।’ और, उनके कहेनुसार बादल झूम-झूम के बरस जाते थे।
वसंत के खुलते दरवाजों-खिड़कियों से महमह करता मौसम जब अबोली भाषा में गीत गाता तो पापाजी पत्ते-पत्ते, फूल-फूल पर से उस गीत के बोल उठा लेते।
जब मौसम शीत में ठिठुरने का थरथराता संदेश देता तब भी वे उस संदेश को डाल-डाल से गह लेते।
भीषण बारिश के गमकते और गर्मी के उबलते सारे संदेश हों कि हों पतझर के झड़ते पत्तों की सिसकारियाँ, पापाजी के दिल रुपी आंगन मेंहमेशा छोटे से छोटा संदेश, छोटी सी छोटी सिसकी भी अपनी आहट छोड़ जाती ...
इसी हरियाले टुकड़े के पास बसे अनाथ आश्रम में कोई मौसम ऐसा न जाता था जब मौसमी फल, मिठाइयों से भरे टोकरे न भेजे जाते हों ! बीते बरसों की तो नहीं पता पर पापाजी की जब तक चलती रही वे ऐसे ही चलाते रहे ! अभी भी पुराने पत्रों के कबड में ऐसे कई पत्र पड़े होंगे, इनमें से अपने देश से तो अनेक अमेरिका, सिंगापुर, कैनेडा और न जाने कहाँ-कहाँ से आए होंगे। थैंक्स गिविंग डे पर या अन्य अवसरों पर पापाजी को उन कई अनाथ बच्चों द्वारा भेजे जाते थे जो पापाजी के रहते ‘अनाथ’ न थे। जिनकी पढ़ाई-लिखाई पापाजी के आश्रय में हुई थी। नदी सी फैली उनकी बाहों में मानो समुद्र को समो देने के प्रयास करते वे पत्र उन फूलों की खुश्बू जैसे थे जो घर के बाहर लगी रातरानी में से आती रहे। . . .
रत्ना के सामने ये आ गई थी वो हरियाली चादर, वो हरा आंचल जिसे ओढ़ने का पूरा अधिकार धरा को था, किंतु उसके इस आँचल को नोंच, खींच लेने के पूरे प्रयास मूरख मानव किये ही जाता था ! सृष्टि के दो ही तो रंग हैं जो दिन के उजाले में सबसे अधिक सूझ पड़ते हैं। माटी की भूरी-रंगत पे हरी रंगत का आंचल उसे एक मूत्र्त गरिमा देता है। इधर आकाश रुपी मस्तक की नीलिमा इस मूत्र्त अस्तित्व को अमूत्र्त से मिला सारी सीमितताओं से उबार देती है। क्षितिज के साथ-साथ धरा के हरे आँचल पर काँंक्रीट का कोढ़ पसरे जा रहा था, उधर इस हरे आँचल के चैड़े नीली किनारी वाले भाग में भी झीनापन आने लगा था। एक तरफ धरती का आँचल फटा जाता था तो दूसरी तरफ सृष्टि के माथे का नीलांचल ! किसे परवाह थी ?
‘क्या होगा लाली जो यूं खेत-खलिहान खतम होते जाएंगे ? क्या खाने की जगह विटामिनों की गोलियां खा के जिंदा रहेगा इनसान ? एक महीने तक, एक सप्ताह तक भूख ना लगे ऐसी गोलियां बने करेंगी ........?’ पहाड़ घूमने जाते तो पहाड़ों की बिगड़ी दशा को लेकर परेशान होते रहते ! उन्हें जरा न भाते वृक्ष विहीन होते जा रहे नंग-धड़ंग पहाड़। गाँवों में जहाँं कहीं भी जाते तो गाँवों में छाया निठल्लापन, चैपालबाजी, समय की बरबादी, मुर्दनी उन्हें हलाकान
रखती ! ओह् !
वह जहाँं खड़ी थी उससे दस कदम दूर था वह पंप जो धरती के सीने को चीर पाताल तक जाकर पानी ले आया था ! इतना पानी कि बिना उफ्कि ये आधे शहर की प्यास बुझा दे ! जब गर्मी में पानी के लिये आस-पास की निचली
बस्तियों में हाहाकार मचता था तो बिना किसी के आग्रह के पापाजी वह पंप घंटांे चलवा देते थे ........उस अमृत से मीठे पानी ने कभी अपना या मुहल्ले-कालोनी का भेद-भाव न किया। सबको पापाजी की छत्रछाया में समान मीठापन दिया। अब वही पानी परीक्षण के लिये भेजा हुआ है मिनरल वाॅटर बनाने के लिये !
’यांज ( यहीं) लगे फेक्टरी बिटिया ! कागज पत्तर चाली दिया फाइल मा..........’
माली काका कुशलता से जहाँ जरुरत होती जानकारी का टुकड़ा जोड़ देते थे। इतनी जानकारी कुछ-कुछ उसे हाँसिल हो गई थी कि इसी टुकड़े का पूरा मालिकी हक पाने को उसके कुछेक हस्ताक्षरों की जरुरत थी उसके अपनों को ! उसे अपने भीतर कहीं कुछ भारी-भारी, डूबता-डूबता सा तो लगने लगा था। इससे तो यही ठीक था कि पापाजी के सीरियस होने की खबर देते भैयाओं के आग्रह पर यहाँ नहीं ही आती। मालूम तो था ही कि इतनी उमर में सीरियस होने का मतलब इलाज से फिर नार्मल हो जाना प्रायः नहीं ही होता। क्या थोड़ी दुनियादार हो कर नहीं सोच सकती थी वह ? अविजित ने तो कहा भी था कि ‘अगली सूचना आ जाने देते हैं’ तब तक उनके ऑफिस में ऑडिट इंस्पैक्शन भी पूरा हो जाता। उनके साथ आकर एक-दो रोज में लौट जाती वह, तो इतनी भीतरघात, तोड़-जोड़, आदि से तो पाला नहीं पड़ता !
तब उसे अविजित पर भी गुस्सा आया था कि बड़े आए चल कर ‘अगली सूचना’ की बात करने वाले ! यदि उनके पूज्य पिता के ऐसे हाल होते तो भी क्या वे यही दृष्टिकोण अपनाते ? मगर वहाँ से भी हाँसिल क्या था ? प्रेम-मुहब्बत का ज्वार तो समय के रेतीले विस्तार में उतर, सूख गई नदी सा कब का सूख चुका था। अब तो एक जिम्मेदारी, एक निबाह बचा था, जिसे औसत जोड़े की तरह वे दोनों भी निबाहे जाते थे। अविजित धनी-ससुराल के घमंड के आगे झुकना नहीं चाहते थे और वह बस, किसी भी तरह पापाजी से दो शब्द उनके आशीष के रुप में हाँसिल कर लेना चाहती थी।
इसीलिये अपने मायके का पिछला सब किया-धरा भूल खबर मिलते ही, भैयाओं का एक ही बार किया गया आग्रह मान मुंह उठाए चली आई थी टक्-टक् करती।
यह मानने को न जाने क्यों मन तैयार न होता था कि पापाजी अपनी बेटी से यूंँ रुठे ही रहेंगे। उनकी क्षीण-जर्जर हो चुकी काया में कोई स्पदंन अब तक न जागा था ! कैसी निष्ठुरता ओढ़ ली थी उन्होंने उसके प्रति ? एक बार तो कह देते ‘पुत्तर जा माफ किया तुझे ! मगर शायद अब कुछ भी उनके हाथ में न रहा था। रहा होता तो उसे अपने सामने पा कर कभी इतने पत्थर न होते वे।
पापाजी की प्रिय बेंच पर बैठने के समय जो धूप उसे कुनकुने अहसास से सहला रही थी वही जब तीव्र हो अपनी ताप की क्षमता दिखलाने लगी तभी उसे ध्यान आया कि वह बड़ी देर तलक वहाँ बैठ ली थी। माली काका को नजरों ने ढूंढा
तो उन्हें पूरे बगीचे को बड़ी तन्मयता से सींचते पाया। माली काका उस बगिया को सींच रहे थे जो थोड़े अंतराल के बाद काँक्रीट का लबादा ओढ़ लेने वाली है। क्या उन्होंने गीता पढ़ी है ? निःसंदेह उन जैसों को गीता पढ़ने की जरुरत थी भी नहीं। कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात उनके लिये प्रस्तुत की है जो उसे नहीं जानते। माली काका के तो हर भाव में निष्कामता के ही दर्शन हो रहे थे उसे। उनके कार्य में बिना हस्तक्षेप किये उठ चली वह किंतु अपनी पूरी कर्म तन्मयता में भी वे उसकी उपस्थिति से अनजान कहाँ थे ? उनका ध्यान उससे हटा तो न था........
‘जाओ बिटिया। अपणो काम काज करो। काँई नी रख्यो यां तो अब्बे !’
जी हुआ पलट कर पूंछे कि -’फिर क्यों ये ’कांई नी’ के सींचे जाओ हो ?’
मगर दर्द जब तन-मन पर गाज बन कर गिरता है तो एक दौर ऐसा आता है कि लगता है कि न किसी से कुछ पूछा जाए, न कोई हमसे ही कुछ पूछे। न कोई कुछ पूछे, न हम कोई जवाब ही दें। न कोई हमसे हमारा कुछ जानना चाहे, न ही किसी को कुछ बताने की हमारी कोई मजबूरी हो ! काश !
इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता था कि ना ही हमारे पास छिपाने को कुछ होता ना ही अगला जानने का इच्छुक होता ? क्या यह संभव नहीं था कि आप उसके मन की हर बात जानते होते ? वह भी आपके मन की सब जानता। तब, न वो कुछ और जानना चाहता, न आप कुछ छिपा पाते ! मानव का मन जो अथाह गहरा हुआ उसमें चीजें छिप गईं, दुख-दर्द छिप गए, कालिख छिप गई, स्वार्थ, कमीनापन, नीचता सब छिप गए।
ऊपर से मनुष्य का लबादा ओढ़ मनुष्य अपने भीतर के पशु को मन में लिये घूमता है। दर्द छिपा रखे हैं ताकि पड़ौसी जल-जल कर मरे कि ये इत्ता सुखी कैसे ? कालिख छिपा रखी है ताकि दूसरे के मुख पे मल कर यह बताया जा सके कि हम तो इतने उजले और अगला इतना काला।
स्वार्थ का ये हाल है कि पहले लोग स्वार्थ के लिये गधांे को बाप कहने में नहीं चूकते थे तो अब बाप को गधा साबित करने में देर नहीं करते। बाप तो गधा था संपत्ति कमा ली, उसका क्या, कैसे उपयोग करना है ये उसे क्या पता, ये तो हम तय करेंगे ! कमीनेपन और नीचता का आलम ये कि अगर वे आपसे ऊँचे न उठ जाएं तो आपको नीचे धकेल आपके कंधे पर पैर धर कर जताएंगे कि वे आपसे ऊँचे हैं।
पुरखों की धरोहर के कण-कण के, बूँद-बूँद के व्यावसायिक उपयोग के लिये व्यग्र भाई वृद्ध असहाय पापाजी के खून पसीने से कमाए किंतु जतन से संजोए कोमल स्वप्न पर कैसे अपनी व्यावसायिक पथराई बुद्धि का कलुषित हथौड़ा चला पाए होंगे ? थोड़ी भी माया-ममता न रही होगी क्या उनमें अपने उस आकाश सम बाप के प्रति ?
थोड़ा उसके हिलने-खिरने का इंतजार ही कर लेते ! और आखिर कोई कमी तो थी नहीं किसी तरह की। तीनों भाई खासे दौलतमंद तो थे ही ........ पारसमणि भी लोहे को ही सोना बना सकती बताई जाती है। भाई लोग तो कहें कि
राजा मिडास से थे जिसे, जिसे छू लेते थे सोना बन जाता था। और कितना धन चाहिये था उन्हें ? धन ही तो सब कुछ नहीं होता। अकेला धन क्या देगा उन्हें ? जब कि पापाजी ने बच्चों को संस्कार देने में कोई कोताही नहीं की थी, तब उनकी संतान उन्हें इतनी अवहेलना दिये दे रही है ! आपके पास तो बस् धन ही धन होगा, तब आपकी संतान से आपको क्या मिल पाएगा ?
बार-बार यही विचार उसे मथते थे ! यदि यहाँ न आती तो अपनों के काले मनस की कालिमा से यूं दो-चार हो पाती ?
थके कदमों को वह खींचे ला रही थी या निर्जीव से वे उसे खींचे ला रहे थे, कहना मुश्किल था। वही थे सब मगर अब वे उसके अपने न रहे थे, वही दरो-दीवार थे, मगर अब कोई चाहत न रही थी वहाँ रहने की। जी होता था चुपचाप टैक्सी कर लौट चले वापस कि ओ मां बस् हो गया ! अब ये अंगने का पहाड़ और नहीं चढ़ सकती, इस देहरी बिदेसवा में अब और नहीं रह सकती !
मगर कहाँ ?
उसकी सांस चढ़ आई थी। अस्थमा का हल्का दौरा पहचान रही थी वह। फूलते दम को साधने का प्रयास करती उसकी दुबली काया किसी तरह उसके कहे में चलती लाॅन, लाॅन से सटी खूबसूरत मौसमी फूलों से ढंकी, जर्रा-जर्रा लदी पड़ी क्यारी और उससे सटे बरामदे तक तो आ लगी थी किंतु वहीं पड़े मूढ़े पर निढाल हो कर पड़ जाने में
ही उसे अपनी खैर दिख रही थी ! प्यास से उसका गला अकाल की मारी, दरकी-फटी जमीन सा सूखा हो आया था। काश !
उचटती नजरों से उसने देख डाला था सब ओर, कहीं कोई मानुस जात न था इतने बड़े बंगले में जो उसकी जरुरत का एक ग्लास गर्म पानी उसे ला देता। चाची ! कहाँ होगी बेचारी। सजी-धजी किचन में खट रही होगी, मशीन सी !
शांति पुत्तर शांति ! शांति रखे करे हैं ! पापाजी वहाँ नहीं थे, ये तो उनके शब्द उसके मानस-प्रागण में गूंज रहे थे। वो ऐसे ही तो दिलासा देती, संभालती आई है खुद को ! आस्था का आगार साक्षात उपस्थित नहीं है तो क्या हुआ ?
मन में, अंतस में उसकी मौजूदगी के विचार को कौन रोक सकता है ? उसके तो जीवन के रेशे-रेशे में वह प्यार, वह देख-रेख घुली-मिली है। सीपी में मुक्ता की तरह, फूल में सुगंध की तरह का वह अनुराग उसके ह्दय में रचा-बसा
है। क्यों दुख पाती हो रत्ने, क्यों ???
‘’सभना मरण आइआ, वेछोड़ा सभनाह।
पुछहू जाइ सियाणिया, आगै मिलशु कि नाह !’’
( सबको एक दिन मरना है, सभी को एक दिन बिछड़ना है,
जा कर सुधीजनों, समझदारों से पूछो के फिर मिलना
होगा के नहीं ?)
उसने आंखें मूंद कर लंबी सांस लेने की कोशिश की, लंबी सांस ले ही ली ........एक सघन तनाव था जो सांसों की डोरी से रह-रह खेलता उसके अंतरतम को एंठने लगता था....
’पुछहुँ जाइ सियाणिया........‘
तनाव को परे करती उसके कानों में गुरुबानी गूंजने लगी थी। मम्मी को सुबह-सुबह हल्का भजन-संगीत पसंद था। शुक्ला चाची पर भी उनका यह शौक चढ़ गया था। वह तो भजन गाते-गुनगुनाते फिरकनी सी काम किया करती थी।
सामने रखी बेंत की टेबल को हौले से उसके सामने खींच कर किसी ने बड़े अदब से ट्रे रख दी थी। पानी से भरा ग्लास, दूसरे ग्लास में थी गर्म-गर्म भाप छोड़ती चाय और साथ में एक छोटा पैकेट मारी बिस्किट ! उसने आंखें कुछ-कुछ खोल कर देखा, अरे ये तो वही हरनामा था।
‘कैसे ? तू क्यों आया ?’
‘वो अम्मा ने आपको देखा तो मेरे ही हाथ भिजा दी। मैं इधर ही तो आता था जी मेम साब जी !’
फीकी सी हँसी आ गई उसे। पानी की उसे बेहद जरुरत थी। धन्यवाद हरनामे। मन ही मन उसने कहा और पूछा -
’क्यों रे ? तू ये मेम साब, मेम साब क्या कर रहा है ? भूल गया मुझे क्या कह कर बुलाता था तू ?’
जुबान से निकला प्रश्न उतना पैना न था जितनी पैनी धार उसकी सतर प्रश्नवाचक दृष्टि में थी-हरनामा बेचारा ! सिटपिटा सा गया। भाभियों को मेमसाब्, मेमसाब् कहने की आदी हो चुकी जुबान से और वह कहता भी क्या ? रट्टू तोते सा
बेचारा !........
‘बोल क्या कहा करता था मुझे ? बिल्कुल भूल गया ?’
’ज, जी ........ नई दीदी रानी ..... हम कैसे भूलेंगे !’
’हाँ अब आई न तुझे याद !’
’आप अच्छे तो हो न दीदी रानी ? बच्चे कित्ते बड़े हो गए ? जीजाजी साब् कैसे हैं ?’ अगली पंक्ति में खड़े शांत, सीधे से दिख रहे बच्चों को जैसे कोई शरारती बच्चा अचानक पीछे से धकिया दे, कुछ ऐसे ही हरनामे के प्रश्न पर प्रश्न आ गिरे उसके सामने।
‘सब अच्छे हैं। तेरे बारे में जा कर बताऊँगी तो सब तुझे भी खूब याद किया करेंगे ! आना तू कभी लखनऊ मिलने सबसे।’
’कहाँ दीदी रानी ! हम कहाँ आ सकेंगे ! हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आपसे अब कभी मिल भी पाएंगे ........!’
‘‘पुछहू जाइ सियाणिया आगे मिलशु कि नाह ?‘‘
उसके कानों में फिर सबद प्रतिध्वनित होने लगे थे। किंतु डर सा हो चला कि कहीं कोई देख न ले कि घर के नौकर से वह ऐसी घुल-मिल कर बतिया रही थी। अभी चर्चा हो रहेगी कि उधर तो पापाजी खाट से लगे हैं इधर बिट्टो बतरस में डूबी हैं, और वो भी नौकरों-शोफरों से भई !
‘चल रहने भी दे। ये चाय तू पी ले मुझे तो बस् पानी ही चाहिये था’ ...... कहती उठ खड़ी हुई थी वह यह जानते बूझते भी कि हरनाम को और बातचीत की आस थी। पर किस-किस की आस पूरी करे वह ? फिर भी पूछ ही बैठी
‘तू इतनी सुबह से ड्यूटी करता है ? ’
‘नई दीदी रानी, हमारी तो कल नाइट शिफ्ट रही थी। हम तो वापस हो रहे हैं अब ........’
‘अच्छा तू जा आराम कर अब ........’
कल रात ही शुक्ला चाची बता चुकी थी लड़के का शादी-ब्याह निबटा दिया है। माली काका के बाजू वाले कमरे में रहता है वह। उसकी पत्नी बड़ी मस्त ! सुबह आठ बजे सो कर उठती है। किचन गार्डन की देख-रेख कर बाहर ही
बाहर लौट जाती है। घरैलू नौकरानी के काम नहीं करना मांगती। तब उसे ख्याल आया था कि क्या होगा विश्वासपात्र नौकरानी न मिलने की हालत में शुक्ला चाची के बाद बेचारी भाभियों का ? जो होटल न बने तो रह भी कहाँ लेंगी ? क्या होगा इनके चाय-काॅफी, लंच, डिनर, किटी-शिटी का ?
‘भई ऽ ऽ ! आप तो अच्छी ठहरीं बीबी जी ! सुभे-सुभे जमाना नापर्आइं ! हें ! मैं बैठी इधर मर रही हूँ के आपके साथ चाय-शाय पी लंू, पर भैया आप को हमसे इत्ती मोहब्बत कहाँ ? आपका जी तो ड्रायवर, माली, नौकर-चाकरों पर ही मेहरबान दिख रा है !’
वह चुप्प ! अपनी जगह, अपने विषय की एक काबिल प्रोफेसर- वह क्यों ऐसे मौकों पर गूंगी सी हो जाती है ? पीछे पचास जवाब सूझेंगे मगर ऐन मौके पर वह इस प्रकार के उलाहनों से बिंध कर ही रह जाती है। क्या जवाब दे अभी वह प्रीतो भाभी को कि जिनकी जुबान की धार देख कर वकील मामा ने कभी उन्हें कोडनेम दिया था कतरनी !
सांसों में फिर खिंचता-उलझता सा था कुछ। आज बिना इनहेल किये गुजारा न होता लगता था।
‘अब चलिये भी बीबी जी, इकलौती होने का इतना लुत्फ न उठाइये। अपने को तो भइया यहाँ कोई नहीं मनाता !’ यह तीर पुनीता भाभी की ओर से आया था।
‘अरे-यहाँ कोई क्यों अपन लोगों को मनाएगा ? यहाँ तो तीन-तीन भाइयों की इकलौती बहन की चर्चा है।’ बस् कमी कमलिनी भाभी की ही रह गई थी, सो वह भी उन्होंने अपने नश्तर से पूरी कर ही दी। महँगा डिजाइनर गाउन शरीर के प्रत्येक हिस्से पर चढ़ आए माँस की बेतरह चुगली करने को मजबूर था। उसे समझ में नहीं आया कि वह उनके कटाक्ष सुने या उन्हें देखे ?
मगर चाय तो उसे पीनी ही पड़ी।
भाई लोग अस्पताल चले तो वह भी साथ चलने को तैयार थी।
‘मैं यहाँ क्या करुंगी दिन भर ? ’
‘तू वहाँ भी क्या करेगी रत्नो ? तू आखिर डाॅक्टर तो है नहीं !’
प्रेम भैया ने ऐसे भाव से कहा था मानो पापाजी के पास केवल डाॅक्टर ही जा सकता हो। कोई अपना, किसी का जी चाहे, और वह जो डाॅक्टर न ठहरा तो क्यों पापाजी के पास नहीं जा सकता ? उसका गला रुंध आया, आंसू बह चले।
‘तू पगलू रो मत। हम लोग हैं न वहाँ। हमारी फिक्रें मत बढ़ा तू।’
’समझदार, इत्ती पढ़ी-लिखी हो कर ऐसा व्यवहार करती है।’
मंझले भैया का रौबदार स्वर सुन एक तरफ जहाँ उसे तसल्ली सी हुई, वहीं काठ सा भी मार गया। उससे कुछ बोला न गया फिर।
‘अब बीबीजी ऐस्सा तो है नहीं कि हमें दुक्ख नहीं है- अब जिसका जित्ता भोगना लिखा है वह तो भोगना ही पड़ेगा। आप हम तो उसकी जगह भोग नहीं लेंगें।’
पुनीता भाभी कुछ असहज हो आई थीं। बाकी ने भी यही सुर मिलाया और तो और शुक्ला चाची भी उधर की ही बजा रही थी।
‘बिट्टो कौन सदा को बैठे रहा है ? पिंजर में प्रान अटके हैं, जित्ती जल्दी कैद छूटे सो भली ! आप कर बी क्या लोगे वाँ ?’
फिर वही प्रश्न ! मैं कुछ कर नहीं लूंगी मगर मैं वहाँ रहना चाहूं तो क्यों नहीं रह सकती ? अब किससे जिद करे वह ? कौन मान रखे उसका ? उस तीन-तीन भाइयों की इकलौती बहन का ? भाइयों के जाते ही भाभियाँ भी इधर-उधर हो ली थीं।
‘ऐ ल्लो बिटिया। जी कड़ा करके रक्खो। समय बड़ा महाजन ठहरा। अपना हिसाब-किताब किसी पे ना छोड़े है। काहे जी दुखाओ हो अपना ? जित्ता कोई मान रखे उत्ता लीजो। वो कही है ना किसी ने- ‘माँ बिना मायका, पति बिना ससुराल ........’
शुक्ला चाची मम्मी की तरह बात-बात पे मुहावरे, कहावतें कहती थी। ठीक ही तो कह रही थी ..........। शुक्ला चाची भी दर्शन बघार कर चल पड़ी थी। उसे बाकी पड़े कामों का अंबार बुलाता था। अब रत्ना अकेली थी।
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
5-
‘बुआजी आप हमारे साथ खेलिये न ........‘
’देखिये ना ये कित्ती रोन्टई खाता है !’ नन्ही अपर्णा उसके निपट एकाकी पड़ गए मनस को मोहासिक्त करती अपने बड़े भाई की शिकायत लिये खड़ी थी,
ओह !
उसे अब कुछ और नहीं चाहिये था ! धन्य होले रत्नो धन्य हो ले।
बुआजी खेलेंगी साथ में, इस उल्लास में वह छुट-पुट जनता उसके चारों ओर आ जुटी थी जिनकी माँओं को आज फेशियल, हेयर कलरिंग, नेल पाॅलिश तमाम तरह की सेटिंग आदि से फुरसत न थी क्योंकि वैसे भी उनके वीआईपी क्लब की महिला शाखा ने आज दोपहर को लंच के साथ एक मींटिग रखी थी जिसका मुख्य आकर्षण थीं फ्रेंकफर्ट से कई सालों के बाद लौटी कमलिनी भाभी। सो रोजाना के ताम-झाम से कहीं बढ़ कर आज ब्यूटी केयरिंग मोर्चे पर डट जाना था उन्हें। उनके लिये तो ब्यूटिशियन आ भी डटी थी। भाड़ में जाऐं सब ! रत्ना का ध्यान अब कहीं और ही आ ठहरा था।
तनावहीन करने की क्षमता से भरी उस नन्हीं पब्लिक में वे कुल छह थे जिनमें सबसे छोटी और उन पांच भाईयों में इकलौती थी अपर्णा कुल नौ वर्ष की, बाकी सब उसे मनमाने नचाना चाहते दीख रहे थे, मगर वह नाचे तब ना ?
’रोन्टाई मैं नहीं तू खेलती है, हर चांस पर चीटिंग करती है !’
वे आपस में लड़-झगड़ कर कितना सुकून भरा, बचपन का सा माहौल दे रहे थे रत्ना को।
‘देख लीजियेगा बुआ जी ये आपसे भी चीटिंग करेगी।’
‘बहुत बड़ी चीट है ये!‘
वे पाँचों समर्थन करते हँसने लगे थे।
’हाँ हाँ बुआजी ये है ही ऐसी।’
’कोई बात नहीं ! हम तो खेलेंगे अपनी अपु के साथ।’
’आप भी मुझे अपु कहोगे ?’ नन्हीं अपु ने पूछा था निरे-निरे भोलेपन से।
’हाँ ! तुम्हें अपु नाम नहीं पसंद ?’
’है है। खूब पसंद है। दादा जी भी हमें अप्पू ही कहते थे ! पर मम्मी कहती हैं कि नाम नहीं बिगाड़ना चाहिये। पता है, पता है बुआजी हमारा नाम तो दादी जी ने ही रखा था। पता है स्कूल में टीचर हमें कहती है एपेराना एपेरेना .........
पता है आपको हमारे नाम का क्या मतलब होता है ?’
वो सब हँसने लगे थे उसकी पटर-पटर सुन कर।
’ये खुद नहीं जानती बुआजी। ऐसे ही सबको बताती रहती है कुछ-कुछ। ये ऐसी ही है ........‘
’कुछ कुछ क्या ?’
’यही कि इसके नाम का मतलब पार्वती होता है। पत्ते तक त्याग के पार्वती जी ने व्रत किया था, ये उसी वाले दिन पैदा हुई थी न, इसीलिये दादीजी ने इसका नाम अपर्णा रखा था।’
’हे हे एक और मीनिंग होता है मेरे नाम का . . . . . . .’
’जा-जा वो तू बिल्कुल नहीं बता सकती। तेरे पास इत्ता भेजा ई नईं है , ’
’हाँ-हाँ याद है मुझे- मैं है ना बुआजी ! सबको लोन से फ्री कर दूँगी’ . . . .
’ही-ही, खी-खी करते वे सब हँस-हँस कर दुहरे हुए जा रहे थे। रुआंसी होती अपु बुआ की गोद में छुप गई थी। बुआ को भी बड़ी खुल कर हँसी आ रही थी।
’जरुर हमारी अपु सबको लोन से फ्री कर देगी !‘ अपर्णा नाम का एक अन्य अर्थ उसकी भोली बाल बुद्धि इसी प्रकार लगा पाई थी। अपर्णा - ? रत्ना को ध्यान आया पापाजी कहा करते थे कि एक बेटी को पाल-पोसने में इंसान अपने सब अभौतिक कर्जों से मुक्त हो जाता है। भले ही उसके शादी-ब्याह में वह आधा हो जाए। सच् ही, बच्ची ने उसे निष्कलुष
रुप से अपने गु्रप में शामिल करके ऋण मुक्त सा, भार मुक्त सा कर दिया था।
पुनीता भाभी आपको किस तरह धन्यवाद दूं अपु के लिये ? ईश्वर की कृपा ही तो थे वे सब के सब जो अभी तक तो अपने अपने माता-पिता के बैर भावों से, कलुषों से खुद को बिल्कुल अछूते रखे हुए थे। आगे की कौन जाने। उनकी इस सरलता-सहजता को कभी काल की क्रूर नजर न लगे ! इस नन्ही जनता के निमित्त भैया-भाभियों के सौ सौ खून माफ न कर दे तो क्या करे रत्ना ?
नन्ही-नन्हीं कोंपलों के सामीप्य के उल्लास ने पापा जी की देह पर ठहरे असाध्य मौन को बिसरा दिया था। काश ! ऐसे ही दिन गुजरते रहें। पर कब तक ? एक कहर जो बरपा होना ही है कब तक थमा रहेगा।
शाम होते न होते यह बात साफ हो गई थी कि पापाजी को अब यूं ही पड़े रहना है जब तक भी जियें तब तक ! इतनी उमर में ऐसे मरीज फिर नाॅर्मल होते नहीं देखे गए। तो फिर अब कैसे क्या होगा ? गमगीन माहौल में गम का एक और
पहाड़ टूट पड़ने से सब बौरा से गए थे।
क्लब से लौटी भाभियों पर कहर कुछ ज्यादा ही बरपा होता दिखता था ? किसी बहुप्रतीक्षित परिणाम दिलाने वाली घटना के परिणाम के लंबित हो जाने से उपजे असमंजस, झल्लाहट उनके हाव-भावों में साफ पढ़े जा सकते थे ? कमलिनी भाभी की व्यग्रता तो छिपाए न छिपती थी कि आखिर वे कब तक यहाँ इंडिया में पड़ी रहेंगी ? जो कुछ होना हवाना है हो हुवा जाए तो अपना फर्ज निबाह, बाकी बचा हिस्सा पाती ले उड़ चलें। उन्हें तो इंडिया का मौसम रास न आ रहा था। घर में एसी, कार में एसी, भैया लोगों के आॅफिस में एसी, हाॅस्पीटल में, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स में, रेस्टारेंट
में कहां तो नहीं एसी ? कहां तो, कहो क्या और कितना तो छुआ होगा उन्हें मौसम ने ? फिर भी, घर से निकल कर कार में बैठने तक में उन्हें तो एक्सपोजर हो-हो जाता था। दूसरे, सब ओर नाक पर रूमाल धरे-धरे घूमती थीं।
’बाब्बा जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे कि अजीब, दुर्गंध आनी शुरू ! कोई दोनों आँंख बंद किये हुए हो तो भी बता दे कि इंडिया में हैं इंडिया में !’
राम जाने कैसे रहेंगी वे अब दुबारा इंडिया में, जो रहना पड़ा तो . . . . . !
‘रत्नों तू ठहर कुछ बातें करनी हैं ........
डिनर के बाद उसे रोक लिया गया था। बच्चों को अपने-अपने कमरों में भेज, भैया-भाभी सब उससे मुखातिब थे।
तो फैसले की घड़ी आ ही पहुँची थी ! मन में उसके सब तरफ शून्य ही शून्य भर गया था। कोई आशंका-कुशंका, चिंता रुपी पाखी भी न था वहाँ पंख फड़फड़ाने को। कैसी वीरानी पसर गई थी मन-प्राण पर !
पड़ाव छोड़ आगे बढ़ गए यात्रियों के ठंडे पड़ चुके अलाव में कोई रंच मात्र सुलगन न बची थी जैसे, फिर भी रत्ना क्यों उसमें किसी अपनत्व भरी गर्माहट की आस लगाऐ बैठी थी ? अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ चुके उस काफिले से कोई यात्री अब इधर वापस नहीं आने का। आगे जाना भले ही बेहद जरूरी हो, लेकिन वे यह जानना ही नहीं चाहते थे कि लौट कर आने का भी अपना अलग ही महत्व होता है। उन्हें भावनाओं में बह कर पीछे आना मंजूर नहीं और रत्ना को भावनाओं को खूंद कर आगे जाना मंजूर नहीं ! दोनों के अपने-अपने मानदंड, दोनों अपने-अपने अनुसार सही।
तो, एकदम खाली सा मन था रत्ना का, वो इतने खालीपन में भी भला क्यों निपट बैरागी होने को मचलता था तब, कि जब आसन्न कुशंकाओं-आशंकाओं के प्रहार झेलने के पल उस पर भरपूर बीतने थे ?
तो,
उस धन के स्त्रोत की चर्चा होनी थी अब जिसके कारण पापाजी को ये दिन देखने पड़े थे ! कोई उनका अपना न रहा था ........।
शुक्ला चाची स्वादिष्ट खीर के महकते प्याले सजा लाई थी। उसे देख कर लगता था वह आज की बहस के मुद्दों की पूरी जानकारी रखती है। तभी न कैसी खाली-खाली दृष्टि से देखा था उसने उसे . . . . .।
’बस, अब कुछ नहीं चाहिये।’ बड़े भैया ने इस प्रकार कहा था शुक्ला चाची को, जिसका आशय यही था कि अब वह दुबारा आ कर उन लोगों को डिस्टर्ब न करे !
‘हाँ तो रत्ना . . . . . . . . . ’
उसे विष बेलें कसे ले रही थीं हर ओर से। क्षत-विक्षत किये दे रही थीं पोर-पोर से। टूटते मोह, छूटते अपनत्व के हालाहल के सैलाब में कोई उसे बस् एक गोली भर दे दे नींद की ! ह्दय कभी आग-आग हो आता था, कभी बर्फ सा ठंडा पड़ जाता था। सुबह भी इनहेल करना पड़ा था, अब फिर जरुरी हो आया था।
चंदन के पेड़ों पर कैसे भुंजग पल गए थे ! ऋतुओं के निष्ठुर प्रहारों को सहकर-सहकर जिन पक्षी वृंद को पलकों की छाया तले पल-पल संभाला था पापाजी ने, वे ही उन पलकों के मुंदने के इंतजार में अकुलाए जाते थे। वह सरपट भाग जाना चाहती थी वहाँ से कि- कहीं नमक की खदान में नमक न बन जाए !
‘पापाजी अब चंगे नहीं होने के . . . . . . ’
’और हम सब भी कितने दिन अपना-अपना काम छोड़ कर बैठे रहेंगे ?’
मंझले भैया की बात को सहारा दिया था बड़े भैया ने जिन्हें फ्रेंकफर्ट से आ कर यहाँ बैठे रहने में अनेक नुकसान थे। हालांकि वे अपनी वापसी का मार्ग पक्का करने में लगे थे।......सब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी, क्योंकि सबके अपने-अपने नुकसान थे। वो भी तब कि जब वे सब बराबर अपने काम किये जाते थे। कोई काम छोड़ कर न बैठा था सिवाय रत्ना के। मगर उसका नुकसान किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि उसकी प्रोफेसरी में उनके लिये कुछ न रखा था, वहाँँ किसी को कोई नुकसान न दिखता था। उसका डी. लिट् का वाइवा होना है। तीन विश्वविद्यालयों की पेपर सेटिंग बाकी है। दो पीएच.डी. छात्रों का थीसिस सबमिशन उसके यहाँ होने के कारण रुका हुआ है।
क्या ये महत्वपूर्ण काम नहीं हैं उसके ?
‘मुझे तो बाब्बा रे ! कभी ऐसा कुछ हो-हुवा जाए तो तुम मर्सिकिलिंग से सुला देना !’ कमलिनी भाभी के शब्द अस्त हो चुके सूरज की बची-खुची लालिमा को लीलते प्रतीत होते थे।
‘बात तुम्हारी नहीं है। बात पापाजी की है। अभी और उससे भी पहले तो रत्ना, बात उस जमीन की है जो पापाजी तेरे नाम . . . . . . .’
कंधे से कंधा मिला कर जो शोक कम हो जाता, वो साथ बैठ कर महाशोक में तब्दील हो गया था। साथ बैठकर जो पीड़ा बांट ली जाती, वह पीड़ा और गहरी खाई खोद गई थी। न जाने कैसा साथ दिया था भैया लोगों ने। न जाने क्यों पापाजी की चिरनिद्रा-यात्रा यूं लंबी हुई जाती थी कि उन्हें उस निद्रा पर भेजने के लिये उनके अपने चिंतित होने लग पड़े थे !
रत्ना को और करना भी क्या था ? बस् सुने गई उनकी, सुने गई, सुनती ही गई, न जाने कब तक।
‘कुल मिलाकर इतने दिन की ’छुट्टी’ के बाद अब, इस दरमियान लौट नहीं गया तो करोड़ों का असाइनमेंट हाथ से निकल जाएगा वो अलग . . .आखिर बिजनेस कोई खेल है ?’
‘और क्या ! हम तो लुट ही जाएंगे।’ कमलिनी भाभी को ऐसे मौके बहुत सुहाते थे !
’अगर और देर हुई तो प्राॅडक्शन चार्जेस ही इतने बढ़ जाएंगे कि अगले छह महीनों तक घाटा ही झेलते रहेंगे हम।’
’बैंक लोन की किश्तों में ही सारा खून-पसीना एक हो जाएगा। आपको तो यूरो बचा लेगा, हमें तो डूबना ही डूबना है।’ मंझले भैया व छोटे भैया के दर्द एक से थे। बातें शुरु हुईं इकतरफा, बातें खतम कर दी गईं इकतरफा, अगर ये बातें थी; फरमान नहीं थे भाईयों की तरफ के . . . . . ।
‘जा, तू सो जा अब। रात बहुत हो गई है। हम लोगांे को तो अभी नींद की गोली से भी नींद नहीं आएगी. . . . . . ’
आश्वस्त भाई लोग उसे सोने भेज रहे थे। वे उसे मशीन सी क्यों पाते थे ? उन्होंने कहा, उसने सुन लिया, उन्होंने जैसे चाहा वैसे मान लिया, उन्होंने कहा बैठ तुझसे बातें करनी है और साथ बिठा कर अपनी ही अपनी थोप दी उस पर . . . . .
उन्होंने कहा जा अब रात हो गई है सो जा ........रोबोट सी वह जा कर सो गई ?
क्यों ऐसा वे संभव मान रहे थे ?
वे उसे बचपन से ही ऐसी देखते आ रहे हैं !
‘रत्नों ! ले केले खा, चल दूध पी !’ मम्मी का आदेश होता। भाई लोग सब उल्टी की एक्टिंग कर-कर के दिखलाते, केले खाने से कई बार बच जाते।
मगर रत्नों को तो केले खाने ही पड़ते ! ऊपर से दूध भी पीना ही पड़ता ! उसे मेथी, पालक, कद्दू , परवल, टमाटर का सूप, ककड़ी का रायता सब चुपचाप उदरस्थ करना पड़ता, क्योंकि दुबली-पतली बीमार सी रहती थी, बीमार ही दिखती थी। खाऐगी तो शरीर निखरेगा, रंग भी भाईयों से दबा हुआ था -
‘रत्नों मेथी खाने से गोरे हो जाते हैं ! पता है जब आदमी बीमार पड़ा तो बाहर से सब्जी की आवाज आई मैथी, मैथी। मैं थी तब यह क्यों पड़ा बीमार ? क्योंकि इसने मैथी ना खाई।’ पापाजी उसे फुसलाते।
‘मैथी ना खाई इसीसे यह काला हो गया, इसीसे बीमार हो गया, चंगा हुआ कि रंग निखरा।’ मम्मी भी उसे पटातीं।
‘और पालक ? पालक तो पालता है।’
उसे वही करना पड़ता जो कहा जाता ! किसी न किसी तरह उससे करवा लिया जाता। एक हरे-भरे परिवार में इकलौती नाजुक बिटिया को यूं प्यार-दुलार दिया गया कि उसकी अपनी कोई पहचान, कोई अपना व्यक्तित्व इस सौम्य, प्यारी-दुलारी, चाबी भरी गुड़िया से परे बन ही न पाया !
किंतु इसी सौम्य-दुलारी गुड़िया ने इक रोज वह चाबी निकाल कर फेंक ही तो दी थी ! अविजित के साथ ने यह क्षमता उसमें उंडेल दी थी तब ! क्या भाई लोगों को यह नहीं पता कि वही अविजित अब भी उसके साथ हैं, और वे यह क्यों माने बैठे हैं कि अविजित भी ठेठ उन्हीं की तरह पैसों के लिये बावले नहीं हुए जा रहे होंगे ?
यह बात तो वही, केवल वही जानती है कि दिखाने भर की आजादी देते हुए अविजित ने भी उसे अपने ही अनुसार एक अन्य प्रकार से चाबी वाली गुड़िया बनाने के ही तो प्रयास किये हैं सदा !
आज भाई लोग यह क्या जानें कि फिर कोई चाबी अपने अस्तित्व में न लगने देने की जद्दो-जहद में ही उसकी उमर कटी जाती थी ! वह स्नेह, वह देख-रेख तो किसी चाबी में था भी नहीं कि जिसके ऐवज में वह अपनी स्वतंत्रता स्वयं
ही आगे हो कर गिरवी रख देती ! एक बार जो उस स्नेह पगी चाबी से विरत हुई तो फिर तो वह उसके लिये तरसकर रह गई। फिर न मिला उसे कहीं वो स्नेहिल-संरक्षण !
वैसे, समाज में स्त्री तो वही भली लगती है जो आपकी बात माने, आपके संरक्षण व अधिकार में रहे, चाहे आप उसके पिता हों, भाई हों, पति हों, बेटे ही क्यों न हों ! मानो स्नेह प्राप्त करने की शर्त ही हो अपनी स्वतंत्रता या निजता को पूरी तरह से गिरवी रख देना ! यदि आपको स्नेह की दरकार है तो अपनी सोचने, समझने की शक्ति का त्याग करना होगा। बच्चा जब तक माँ-बाप के इशारों पर नाचता है उन्हें भाता है। जैसे-जैसे बच्चा अपनी स्वतंत्रता को जीने लगता है तब माता-पिता स्नेह कम व ’बिगड़ गया है’ कह-कह कर उसे कोसने अधिक लगते हैं। यही हाल पति-पत्नी के बीच का भी है। जब तक स्त्री अपनी स्वतंत्रता को भूली रहती है, तभी तक वह अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी भाभी कहलाती है।
अपनी खुद की स्वतंत्रता का ख्याल मात्र उसे बिगाड़ने के लिये काफी है।
प्रेमी प्रेमिका को तभी तक दिलो-जान से चाहता है जब तक प्रेमिका बेचारी उसके कदमों में बिछी रहती है अपना सारा अहं भूल कर ! ज्योंहि वह स्वतंत्र हुई त्यों ही प्रेमी के मन से उतरी। यही स्थिति दूसरी तरफ भी होती है।
यानि प्रेम हम किसके लिये करते हैं ? अपने ही लिये न ?
लेकिन होता उल्टा ही है। अपने आप को पूरा खतम कर दो, मार दो तब ही प्रेम प्रेम कहलाता है। अपने अहं को पूरा
समाप्त करके ही प्रेम की असल अदायगी होती है। इसी से राधा, राधा न रहकर कृष्ण की दीवानी हो रही थी, मीरा
पगला गई थी, शिव अर्धनारीश्वर हो रहे थे, कबीर भी कह गए हैं प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाए ! यानि अपने अहं को बलि दे कर ही इस गली में चला जा सकता है !
पर सवाल यह है कि अपने अहं की बलि दे कौन ? जो प्रेम करे ! जो प्रेम का दिखावा करे उसे तो बस् अहं की संतुष्टी ही चाहिये ! प्रेम प्रायः ऐसे ही दो पक्षों के बीच हो जाया करता है- एक पक्ष प्रेम करता है, दूसरा पक्ष प्रेम दिखाता है। प्रथम पक्ष अपनी अस्मिता, अपनी स्वतंत्रता को प्रेम के नाम पर गिरवी रख देता है, दूसरा पक्ष अपनी स्वतंत्रता व चालाकी के आधार पर अपने प्रेम के दिखावे को हर लम्हा भुनाता है, भुनाता ही चला जाता है, तब तक कि जब तक पहले के पैर जमीं पर न आ टिकें ! अब कहाँ रहा दोनों पक्षों का वास्तविक प्रेम ? ऐसा न रहा होता तो आज भी लैला मजनू, हीर-रांझा की कथा में कुछ नए नाम और न जुडे होते ?
या कि न जाने किन कारणों से कहानीकारों ने कोई ऐसा अप्रतिम किस्सा न गढ़ा ! जो हो,
वो अब ये मानने को मजबूर सी, अभिशप्त सी ही थी
कि-
प्रेम चाहे माता-पिता व बच्चों के बीच हो, भाई-बहन के बीच हो, भाई-भाई के बीच हो, या प्रेमी-प्रेमिका के बीच ही क्यों न हो, दोनों पक्ष एक दूजे से समान रुप से प्रेम नहीं कर सकते। एक पक्ष प्रेम करता है तो, एक पक्ष शासन। ऐसा ही शासन उसे प्रेम के बदले मिलता आया था।
एक शून्य से दूसरे शून्य की अनंत यात्रा करती हुई वह अपने जीवन को शून्य की आरती में जल रही ठंडी सी ज्योत की तरह ही पाती थी जिसमें उजास तो था, किंतु मटियाला-मटियाला सा था वह उजास, जिसमें रिश्ते दिखलाई तो पड़ते थे किंतु रिश्तों की गर्माहट न थी ! कुछ रिश्ते जन्म के थे। कुछ धर्म के थे जिनको प्यार की, अपनेपन की लेखनी से लिखने की बहुतेरी कोशिशें की मानव ने; पर समय का न जाने कैसा, कौन चितेरा, किसी धूत्र्त योगी सा सारी लिखत को स्वार्थ के भीगे रुमाल से रह-रह कर पोंछ-पोंछ डालता था ! दुष्ट !
मानव से मानवता को अपदस्थ करने को तत्पर कोई निरंकुश तानाशाह सा कुटिल बुद्धिधारी, ह्दय के धनी को
ठगता, छलता, मजाक का पात्र बनाता बिना एक क्षण को भी ठिठके बेरोक-टोक अपना कार्य किये जाता था, ठिठकी थी तो केवल मानवता ही !
भीतर ही भीतर लहुलुहान होती जीजिविषा इस मानवता की ठिठकन का अर्थ समझ तो जाएगी न ? यह साथ तो न छोड़ देगी उसका ? कहीं उसका साहस भीतर ही भीतर उसका साथ तो न छोड़ जाएगा ?
मुझमें छिपे ओ जीर्ण मानव, मत मरण की ओर तक -
कुछ और जी, कुछ और जी, कुछ और सह।
मत बहा अब और अश्रु, महासमर में हार मत सब,
कुछ जीत भी, कुछ जीत भी, कुछ और गह !!!
क्या जीतेगी वह ? क्या गहेगी भला ? अनथक चलते विचार-क्रम की हर परिक्रमा पहले पापाजी के बिगड़े हाल पर जा कर पूरी होती थी, अब उनके छोड़े माल पर, भाइयों के बवाल पर जा-जाकर सिर पटक पटक कर पुनः उसी के पास लौट आती थी !
अब क्या करेगी वह ? भाइयों को जमीन चाहिये वही। बदले में तू मम्मी के जेवर ले ले ! उसने अपने आप से नजरें चुरा लीं। वह सदा की ऐसी ही थी कमजोर सी, संरक्षित सी, ताकतवर भाईयों की ताकतहीन, निशक्त सी बहन !
अपने पैरों पर खड़े हो कर कभी-कभी ना कहने की रंचमात्र सी क्षमता जो धीरे-धीरे इतने बरसों में विकसित कर ली थी जो उसने, आश्चर्य कि वह भाइयों में पुनः लौट कर न जाने कहाँ बिला गई। इसीसे वे उसे पूर्ववत पाकर बड़े आश्वस्त थे ! वह उन्हें वैसी ही लगती थी पहले जैसी, मंत्रबिद्ध-अभिमंत्रित सी। शरणार्थी सी !
इतने बरस मायके न आ पाने का जो मलाल रहा था वह कब का धुल-पुंछ गया था। अतीत तो मूलधन ही था जो किसी खून चूसने वाले साहूकार के रेहन रह गया था। अब लौट कर नहीं आ सकता--- बस् उसकी याद में अपना सुख-चैन भी साहूकार को अर्पित करते जाना था चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। क्यों वह कातर सी हुई जाती थी ?
भाइयों ने रिश्तों की कोमल-स्नेहसिक्त चादर उतार फेंकी तो वही क्यों उस उनकी उतरन को लादे-लादे, संभाले-संभाले बावली हुई जाती थी ? पर किसी न किसी को तो उठाना ही होगा इसे ? हजार स्याणों के बीच में एक बावला भी चाहिये ही।
उसे याद है कि खेती-किसानी-बागवानी से पल-पल रूबरू रहने वाली मम्मी एक दिन दस-बारह गुलाब के पौधे
खरीद कर बड़ी खुश थीं। उनकी खुशी पे हंसते थे शाम को उस रोज पापाजी, कि -
‘ये एक ही रंग के इतने सारे पौधे गुलाब के ही क्यों खरीदे ?‘
ना ना, एक लाल गुलाब है, एक पीला, एक गुलाबी, एक हरा, एक काला और वगैरह वगैरह बता कर बेच गया था बेचने वाला तो।
मगर पापाजी ने उसी दिन उन सब पौधों की पत्तियों, डंडियों की बनावट पर एक ही नजर डाल कर उस ठगी को परख लिया था। बता दिया था अपनी खरीद पर बड़ी आश्वस्त मम्मी को कि कोई एक ही रंग के गुलाब खिलेंगे। और वास्तव में,
जब पौधों पर फूल आने लगे तो लाइन से वे सब लाल के लाल गुलाब थे ! अपने बच्चों को न पहचान पाए वे। यदि
पहचान भी पाते तो क्या कर लेते ? जान पाते कि सारे के सारे उनकी हर सीख, हर शिक्षा के विपरीत निकलेंगे तो कर क्या लेते ?
‘सौ दिन ठगाएंगे, एक दिन खुद ठाकुरजी आएंगे !’ मम्मी जब-तब कहा करती थीं। कब ?
मगर कब आएंगे
ठाकुरजी ? वह तो बस् ठगी ही जाती है ! मम्मी का ध्यान लोरी के जैसा था, उसे थपकता, लड़ियाता, सुलाता था।
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
6-
न जाने कितना सो चुकी थी वह कि किसीकी आवाजाही से जब नींद खुली तो इतने तनाव के बाद भी फे्रश थी ! सामने शुक्ला चाची टेª
लिये खड़ी थी ।
‘अच्छी नींद आई दीदी ?’
अपने इस कथन में वह आश्वस्त दीख रही थी कि शायद भाइयों ने अपनी बहन से कोई अप्रिय चर्चा नहीं ही की होगी। उसे क्या पता ! अप्रिय प्रसंग तो घट चुका था। वह तो घटित होना ही था कभी भी, किसी भी समय !
आज सुबह कछ ज्यादा ही मैच्योर हो गई थी। फिर भी सुनाई पड़ी थी बुलबुल की चहक, साथ ही फुदकी, फूलसूंघनी, दंहगल, बया, पतेना सब न जाने कितना शोर मचा कर अपनी-अपनी डालियों-डेरों पर जगार फैलाती फिरती थीं। इसीसे सुबह एकदम आबाद सी लगती थी, मगर फिर भी न जाने कैसी तो कुछ सपाट सी। बस, कभी-कभी कौए की काँय-काँय अवश्य ही इस सपाटपन को तोड़ती थी, मगर भली ही लगती थी।
सुबह-शाम अनेक पक्षियों की, बुलबुलों की मधुर मोहक बोली के मनमाफिक अर्थ निकाले हों पापाजी ने ऐसा नहीं था। वे कहते ‘ध्यान से सुन क्या कह रही है ये बुलबुल !‘ तो सच ही उसकी बोली में रत्ना को सुन पड़ता था -
‘बी क्विक्‘ ‘बी क्विक्‘ !
'अरे बुलबुल तो इंग्लिश बोलती है !‘
‘हां, जल्दी उठ, अपने काम कर। खाली-ठाली बैठने से अच्छा है अपना काम निबटाओ और खुश रहो।‘ बच्चों को सिखाने का कोई मौका पापाजी ने कब छोड़ा ? उन्हींसे सीख लिया था उसने, जब खाने का मन न होता तो वह कहती थी-
‘पापाजी बुलबुल को तो मालवी भाषा भी आती है, कह रही है
‘पेट भरी ग्यिो, पेट भरी गियो !‘
‘पेट फटी ग्यो, पेट फटी ग्यो‘ भाई लोग को जो सुन पड़ता वे वही अर्थ कहते। पापाजी हंसते, मम्मी नाराजी दिखातीं और ऐसे ही चिड़ियाओं को दाने बिखेरते, पेड़-पौधों से बतकही करते जीवन के अनेक नए व सार्थक अर्थ गहते जीवन महकता-गमकता रहता था अविराम।
‘मैं दो तीन बेर आ के देख डाली, आप सोई थीं चित्त !’
’हाँ चाची जम के आँख लगी !’
’फिर भी इत्ते सबेरे उठ ही जाओ हो बीबी जी आप। यहाँ तो नौ बजे भी बहू लोग उठने को जल्दी ही कहे हैं।’
उसका मन न था चाची की चुगल चूं चूं में साथ देने का। इस सबसे तो अच्छा है कि वह अपना वाॅकिंग का काम ही निबटा आए।
‘चाय अभी नहीं लूंगी चाची, बस् एक ग्लास कुनकुना पानी ही दे दो।’
‘हे राम ! मैं तो चाय लिये खड़ी हूँ, आप तनिक मुंह पखारो मैं अभी कुनकुना पानी ले के आई।’ मशीन की सी गति से चाची ट्रे लिये मुड़ ली थी।
खिड़की के भारी परदे सुबह की हवा से हिल-हिल जाते थे। इनके पीछे बिखरा पड़ा था एक अवर्णनीय प्राकृतिक सौंदर्य का शहर में बच गया एक ऐसा पिटारा जो अब कुछ ही दिनों का मेहमान था। काले-हरे अंगूर की बेलों से भरा, आम, चीकू, बादाम, सेमल, नीम, आंवला, अनार, कटहल, सहजन और न जाने क्या-क्या वृक्षों की धरोहरें अपने में समेटे यह पिटारा जल्द ही भाईयों की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ने वाला था। जल्द ही सब कुछ भाईयों के हवाले करके,
शायद मम्मी का कुछ सोना-गहना ले-लिवा कर या शायद उसे भी छोड़-छाड़ कर वह अपने छोटे से बसेरे की ओर चल देगी, फिर माली काका के खुरपे-खुरपी के स्थान पर कुल्हाड़ी, आरी, जेसीबी और न जाने क्या-क्या चलेंगे यहां सनन-सनन। तब,
ये सब कुदकते-फुदकते, कूकते-सीटी बजाते चिड़ियाएं, कौव्वे, तोते, ये टोपी सी पहने उड़ती-गाती बुलबुल जिसे पापाजी इनकी लता मंगेशकर कहते थे, कभी-कभी दिखाई पड़ जाने वाले ये कल्लू कोतवाल, ये नीलकंठ पटवारी महोदय कहाँ जाएंगे सब के सब ? हँस पड़ी वह अपनी इस छोटी सी चिंता पर ? गनीमत है कि भाई-भाभी लोग उसकी इस चिंता से वाकिफ न थे, वरना वे बिलाशक उसे पागलखाने भेज कर ही दम लेते !
’कैसे दीदी, आप ही आप हंसो हो ? मम्मी जी कहे करें हीं के दुख-दरद की बात भले ही खुद सहो, पर हंसी-खुशी में सबको शामिल करो। हमें भी बताओ काहे अकेले-अकेले हंसे ले रहीं थीं ?’
चाची कुनकुना पानी ले कर लौट आई थी। वह जब मम्मी का हवाला देती थी तो उसे टालना मुश्किल हो आता था, सो उसने चाची को बता ही दी थी अपने हँसने की वजह ! जिसे सुन कर पहले तो चाची भी अच्छी हँसी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। फिर कुछ उसके समझ में आया तो बोली ........
’धन्न दीदी, धन्न ! इत्ता बड़ा दिल, इत्ते छोटे-छोटे पाखी-पाखुरों की इत्ती चिंता आपको ? पर दीदी, इनका क्या है ? ये तो जहाँं आधा गज हरियाली पाएंगे वहीं जा चहकने लगेंगे !’ उसके लिए तो कितना आसान था चिड़ियों के निमित्त हरियाली की समस्या का उत्तर देना ! बस् ! सारी चिड़ियाऐं यहां से उड़ कर फुर्र से वहां जा बसेंगी जहां हरियाली होगी। ना उन्हें सामान बांधना, ना उन्हें कोई टिकट कटाना !
हाँं सो तो है।
वे सब के सब तमाम पक्षी अपनी-अपनी बोलियों में अपनी अविराम चहचहाहट से वातावरण की सारी उदासी दूर करने का प्रण सा लिये हुए थे जैसे। वे आपस में एक-दूजे से न जाने क्या-क्या कहते-कूकते, बावले से इधर-उधर डोल
रहे थे कल की फिक्र से अनजान। हरियाली मानो वरदान थी उनके लिये, उन्हें और क्या चाहिये था ?
मनुष्य को ही न जाने क्या-क्या चाहिये जिसे वो हरियाली की कीमत पर हांसिल करने से नहीं चूकता, और कहने को कहेगा के हरियाली भी होनी चाहिये क्योंकि खून में लालिमा तो हरियाली की ही देन ठहरी !
मगर हरियाली खत्म करता जाता मानव अपने घरों में हरियाली के चित्र लगा-लगा कर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री किये लेता है। कौन है जिससे वह पूछे, और कौन है कि जो उसे जवाब दे कि हरियाली के विस्तार समेटे सुंदर से सुंदर, महँगे से महँगे, जीवंत से जीवंत चित्रों में बयाँ हरियाली किसी नन्हें से एकमात्र पक्षी को भी आश्रय दे सकती है ? नदी- तालाबों के चित्रों से क्या किसी प्यासे का सूखा गला तर हो सकता है ? भारी बारिश- झरनों के चित्रों से क्या किसी खेत की माटी से सौंधी गंध आ सकती है ? और तो सब छोड़ो !
’गलत जगह पर हो तुम।’ अविजित उसके प्रकृति-प्रेम से खीजते थे अक्सर ही। कितना विचित्र सोच रखते थे कि प्रकृति से जुड़ने के लिये गाँव-खेड़े में रहना जरूरी था।
’तुम्हें तो प्रकृति विज्ञानी होना चाहिये था ! या सबसे बढ़कर तुम्हें तो ठेठ प्रकृति की गोद में, कहीं गाँव-खेड़े में पड़े होना चाहिये था, जहां गोबर-कँंडा, लकड़ी-चूल्हा, खेत-खलिहान, दिशा-मैदान में प्रकृति से बतकही करते-करते तुम्हारे सारे प्रकृति प्रेम की हवा निकल न जाती तो मैं अपनी मूछें मुंडवा देता !’
बेचारे !
जब-जब वे प्लान बनाते, जहाँ-कहीं के भी वे प्लान बनाते, जहाँ-कहीं भी वे लोग छुट्टियां मनाने जाते, उनकी साथिन हर कहीं प्रकृति पर ही रीझी मिलती। शहरों के फैलते जाते शरीर और जंगलों-नदियों की प्रतिपल दुबलाती-सूखती जा रही देह पर वो घंटों बिना रुके बक-बक (अविजित के शब्दों में) करने को तत्पर रहती। अल्लसुबह उठ कर वह प्रोफेसर काॅलोनी के अपने अति पुराने से बंगले का गार्डन खुद संभालती थी। उसके कर्मठ हाथ, कुशल अंगुलियाँ केवल चाॅक-डस्टर ही नहीं बल्कि खुरपी-सब्बल थामने के भी खासे आदी थे। पेड़-पौधों के बारे में, बाग बगीचों के
बारे में राई-रत्ती जानने वाली वह कई-कई आलसी, अलाल, नाकारा मालियों को भाग जाने पर मजबूर कर चुकी थी। उसके बागवानी के शौक और ज्ञान पर उसके बड़कू बेटे ने कभी ताज्जुब करते हुए हँसी-हँसी में कहा भी था-
‘मम्मी जरुर पिछले जन्म की कोई मालिन अलबेली रही होंगी !'
‘इस जन्म में भी किसी मालिन से कुछ कम हंै क्या ?’ अविजित ऐसे ही मौकों पर बच्चों का भरपूर साथ देते थे।
उसे यह प्रकृति से अविरल बतियाने की लत पापाजी से लगी थी। एक मुहब्बत दूसरी मुहब्बत के करीब लाई थी, किंतु पापाजी ने, भाइयों ने, किसीने दामाद को नहीं अपनाया तो नहीं ही अपनाया था। सो, अविजित के लिये संबंधों का यह ठंडापन दूसरे ठंडेपन को न्यौत गया था। शादी के बाद वह प्रायः पापाजी-मम्मीजी के राग अलापा करती थी।
अविजित भी दिलचस्पी से सुनते थे। धीरे-धीरे ठंडेपन ने दिलचस्पी की गर्माहट पर काबू पा लिया। कुछ छिपी हुई अपेक्षाऐं पूरी न हो पाने का ठंडापन मुहब्बत के खड़े खेत को हौले हौले बर्फ की परत से ढंक गया, पाला सा आ पड़ा हो जैसे तैयार फसल पर।
अविजित एक साइंटिस्ट थे, जो करना चाहते थे सुविधाओं के अभाव में कर नहीं पाए थे। उसके करोडों में खेलते मायके से उन्होंने खुल्लम-खुल्ला कोई अपेक्षा लगा रखी हो ऐसा तो न दीखता था। किंतु जो दिखाई नहीं देता जरुरी तो नहीं कि वैसा ही होता भी हो ! सो एक अनकही सी बौखलाहट, झुंझलाहट अक्सर मखौल के रुप में उस पर आ गिरती थी ! धीरे-धीरे उसे आदत पड़ चुकी थी इस सबकी। पहले-पहले बड़ा टीसता था यह सब, फिर धीरे-धीरे बच्चों के मुंह देख-देख कर अपने टीसते भीतरीे जख्मों को भरना खुद-ब-खुद सीखते गई वह।
किसने सिखाया उसे यह सब ?
उसी ने, जिसके साए में उगते सूरज, चढ़ती धूप, उतरती शाम, चांद-तारों की चादर ओढ़े आती रात से अपनापा जोड़ वह बाहर से मिलने वाली हर चोट को अपने लिये जीने की कला सीखने का एक अवसर मानती थी; ऐसे ही अवसर वह चिड़ियों के चहचहाने में, कबूतरों के दाना चुगने में, नन्हे से बीज के अंकुर के रुप में, अंकुर से पौधा बन कर फूटने में ढूंढ लेती -
अक्सर वह अंदाज लगाती कि यह फूल ‘इस’ कलर का निकलेगा लेकिन निकलता वह किसी और रंग का . . .।
इतना सा पिद्दा और इतना बड़ा फ्लर्ट ! इस तरह के अनेक फ्लर्ट उसे सिखाते कि जिंदगी में कोई भी, कहीं भी फ्लर्ट कर सकता है ! वह मानती कि कभी भी, कहीं भी, कुछ भी हो सकता है। जीवन की कोई निश्चित बंधी बंधाई लकीर
नहीं, कि जिसका फकीर हो कर खुशहाल जीवन जिया जा सके। उसके लेखे तो वास्तव में खुशहाल जीवन का कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं कि जिसे पढ़ डालो, रट डालो और खुशहाल जीवन हाजिर ! खुशहाल जीवन जीने के लिये क्षण-क्षण अपने को खुशहाली की तलाश में डुबोना पड़ता है। पहले-पहल सब अजब-गजब सा लगता है, पर धीरे-धीरे प्रकृति अपने शिष्य को अपने भीतर का अनमोल खजाना जर्रे-जर्रे से सौंपने लगती है। जिसने इसे पहचान लिया समझो उसीने इसे पा लिया।
पापाजी कहते थे ‘लाली वे, ये तो हरा खजाना है, हरा खजाना !’ एक रोज वो बच्चों से कभी उनके नानाजी के किस्से बताती कहती थी कि जिसे सुन, किसी काम से उधर आए अविजित ने हँंसते हुए तत्काल उसमें अपने शब्द जोड़ दिये थे-
‘जरुर। अगर यह दहेज में मिल जाए तो !’
अविजित का एक ओैर तल्खी भरा प्रसंग न चाहते हुए भी याद आए जाता था उसे बैठे-ठाले ! उसका तो प्रेम विवाह था। सो दहेज का प्रश्न क्यों ? मन में कभी प्रश्न उठता था कि प्रेम किससे था ? उससे, उसके खानदान से, उसके पिता के पैसे से ?
आखिर किससे ?
क्यों विवाह के समय का प्रेम समय की सच्चाईयों से रुबरु होते ही शेर की गंध मात्र से कुलांँचे लगा कर गायब होते हिरण सा फुर्र हो गया ?
क्या हर प्रेम की यही गति होती है ? उसने जो प्यार किया था वह भी तो शायद अपनी एक दमघोटू कैद से मोक्ष की चाह का ही दूसरा रूप रहा था ! ओफ ! एक कैद से मुक्ति दूसरी उम्रकैद का ही रास्ता खोल गई थी। वह तो दिल पर
ठुंकी एक कील सी, एक नश्तर सी ही हो चली थी। चाहे अनचाहे अविजित उस पर चोट दे देते थे। पर वह इसे ढोए जाती थी। अब इस कील से, इस नश्तर से कैसा छुटकारा ? साँप छछूंदर सी हालत हो चुकी थी उसकी। इस कील, इस नश्तर को निकाल फेंके तो गुजर नहीं, और इसके साथ भी गुजर नहीं ! एक धूप से बचने को निकली वह एक दूसरी ही कड़ी धूप के लंबे से सफर पर चलने को मजबूर थी।
अब जब अविजित जानेंगे कि वह हरा खजाना लुटा आई तो ? उस शीत युद्ध का विचार मात्र उसे अवसाद से भर-भर देता था। फिर भी, मम्मी के गहने भी उसे नहीं चाहिये। नहीं चाहिये उसे कुछ भी। वह कह देगी अविजित को नहीं था यहाँ कुछ भी उसका। जो था वह पहले ही अविजित के साथ हो लिया था उसका सर्वस्व, उसका तन-मन-प्राण। अब
उसका क्या है यहाँ ?
उसे भूलते न थे वे पल जब वह अविजित की दुल्हन के रुप में अविजित के माता-पिता के सामने आर्शीवाद लेने पहुँची थी। तो सिवाय खाली शब्दों के वे उसे कुछ न दे पाए थे क्योंकि वो उनकी मनपसंद न थी। जब आस-पास में कानाफूसी हुई कि बहू को क्या खाली हाथ ही अपना लिया, कुछ मुँह दिखाई तो दी होती ! तो उसकी सास का टका सा जवाब था-
’वह तो ’प्रोफेसर है। प्रोफेसर कहाँं गहना-जेवर डाले फिरेगी ? दोनों कमाते हैं अपनी पसंद से खरीद लेगी खुद। वैसे भी,अब क्या बाकी है देने को ? अपना हीरे सा बेटा तो दे ही दिया उसे ?’
आखिर उसके अपनों ने ही सारे द्वार बंद कर लिये थे तो परायों पर क्या अंगुली उठाई जाए ? और फिर, उसने तो ऐसी कोई सोने-चाँदी की उमीद न की थी। न वह अधकचरी, अपढ़-देहातिनों के जैसे सोना चांँदी लटकाए फिरना पसंद ही
करती थी। अपने मायके में सोना-चांँदी देखती पली थी, यदि खाया जाने योग्य होता तो भरसक उसे सोना ही खिलाया-पिलाया जाता। मगर अविजित के परिवार ने अभाव की धारणा देखी-परखी-भोगी थी। सो, इकलौते बेटे के ब्याह में दहेज से घर भर देने वाली बहू की आस लगाए बैठी माँ के कलेजे पर लौटने वाले साँप एक दो नहीं, कई-कई रहे थे। दुबली-पतली कीकर सी है, बीमार-शीमार है, विजातीय है, बड़े घर के घमंड से चूर है-बहू क्या थी कहो कि नापसंदगियों का अंबार ही तो थी ! तब से ले कर उसके साथ कोई शगुन, कोई नेग की परंपरा निभानी किसी ने जरुरी नहीं समझी। उसे ऐसी कोई तमन्ना थी भी नहीं।
प्रेम का ज्वार जब ठंडा पड़ने लगा तब तक बच्चों ने आ कर उसे बांध लिया था। ठीक ही तो कहा करते थे पापाजी कि एक मुहब्बत दूसरी मुहब्बत को जिंदा रखती है ! बच्चों की मुहब्बत ने पति व ससुराल की मुहब्बत को जिंदा रखा ही था। इसके अलावा, उसके संस्कारों से उसे जो जीवट मिला था उसने उसे एक मिशन की गुलाम नहीं रहने दिया। अतः यदि उसके जीवन का एक मिशन खत्म होता तो उसके खत्म होने के पहले ही वह कई अनेक मिशन, कई मोर्चे अपने सामने खुले पाती। जीवन की प्रेरणा किसी एक रस्ते से नहीं आती थी उसके लिये। अतः वह एक खो कर किसी अगले उद्देश्य को पूरी ईमानदारी से जीने की प्रेरणा के रुप में पाती गई।
उसे कतई मलाल नहीं है कि अविजित ठीक उसके मैच के नहीं निकले। वह भी तो उनके लेखे ऐसी ही रही होगी ! उनके मलाल भी तो बहुत कुछ वैसे ही रहे होंगे !
तो, उसने अपने सामने अवसरों के अनंत विस्तार खोल रखे थे। पति, नौकरी, बच्चे, बागवानी, लेखन। अगर बच्चे भी कल को बड़े हो कर किन्हीं कारणों से उसे महत्व नहीं देंगे तो वह उपेक्षित हो कर नहीं पड़ जाएगी, बल्कि वह अपने को अपने योग्य किसी कार्य में खपा देगी।
उसका यह निस्पृह भाव अविजित को फूटी आँख न सुहाता था। शायद वे उसे घटनाओं से आहत होते देखना चाहते थे ताकि उसे दुलार-संभाल की आवश्यकता महसूस हो जिसे पूरा करने के लिए उसे अविजित का मुंह जोहना पड़े,
जिसके बदले में वे उससे अपनी बेहिसाब मांगें मनवा सकें। उन्हें यह उसकी उद्दंडता लगती थी कि वह स्त्री हो कर उनसे मदद नहीं मांगती, उनके चरणों में गिरकर नहीं रोती, उनके आगे हाथ नहीं पसारती ! उसका यह स्वाभिमान उन्हें अभिमान लगता था कि ‘दुनिया को अनावश्यक रूप से बताने से अपनी समस्या हल नहीं हो जातीं, बल्कि कई समस्याएं तो इससे और खतरनाक हो जाती हैं। बताओ उसे जो सुनने-समझने लायक हो।’
क्या अविजित इस सबके लायक नहीं थे ? ? ?
उसका मन जुबान पर ताला ठोंक देता है !
क्या वजह थी जो उसने चुपचाप अपना बतियाने का संबंध पेड़-पौधों, फूलों से, कलियों से, चिड़ियों से जोड़ लिया था ?
अपने लिखने-पढ़ने के कामों आदि में अपने आप को धंसा डाला था।
आखिर. . . . . . खिसियाए, खीजे इंसान से क्या बतियाना ?
निम्न मध्यमवर्गीय जीवन की अनेक त्रासदियों को जी चुके शापग्रस्त से उस इंसान के पास वह नैतिक साहस भी तो नहीं था कि अपनी अभावग्रस्तता की आत्म-स्वीकृति ही कर सके ! वह तो झूठे दंभ में, अभिमान में चूर अपनी मिथ्या धारणाओं के साथ जिये जाता था। ऐसे में आत्म-संतोष क्यों कर प्राप्त होगा ? वह आज ये तो कल वो डाॅक्टर बदलता था। उसके नाश्ते, लंच, डिनर मंे खाने की सामग्रियां कम तथा दवा-गोलियों की मात्रा बढती जाती थी। उसे भी नींद लाने के लिये, प्रतिस्र्पधा में बावले हुए जाते उच्च वर्ग की तरह नींद की गोलियों की दरकार होती ही थी !
अपने तनाव से मुक्ति पाने की आस में कभी फलाने तो कभी ढिमाके बाबाओं, ढोंगी गुरूओं की शरण में जा पड़ने वाला वह निरीह जान ही नहीं पाता था कि उसके सारे तनाव को छू-मंतर करने की दवा तो उसके अपनों से पुख्ता-पुरजोश संबंधों की गहराई में, मासूमों की मुस्कुराहटों में थी, एक बसे हुए घर की तसल्ली में थी जिसे यदि वह समझ लेता तो कभी किसी बाबा की कोई आवश्यकता ही कहांँ रह जाती थी ?
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
7-
धुले उजले प्रकाश में नहा कर अपने पूर्ण कांतिमान रूप में सूर्यदेव के धरती पर प्रवेश करने के साथ ही उनकी शर्मीली प्रियतमा उषा शनैः शनैः दिन की आड़ में जा छिपी थी। जिसे ढंूढते हुए ही शायद सूर्यदेव का माथा गरम हुआ जाता था। यह तो रोज का ही धंधा हुआ। पहले पहल तो शांत ढूंढते हुए धरती को उपकृत करते हो। सोचते हो कि अब मिली कि तब मिली, पर फिर बाद में, प्रियतमा को न रिझा पाने का गुस्सा धरती के कण-कण पर उतारते हो। यह कहाँ का न्याय हुआ ? मगर क्या करेगी ये धरा जो ये वृक्ष, ये टहनियों के साए न होंगे ? अभी तो ये सब मिलकर बचा लेते हैं सूर्य देव के प्रकोप से।
फिर ?
टहलते-विचरते न जाने किन-किन ख्यालों के गली-कूचों में भटक आई थी वह। खासा दिन निकल आया था यह तो ! कितनी देर से चहल-कदमी किये जा रही थी वह ? उसे क्या हुआ जाता है ? इतने सोच-विचार क्यों ? क्यों नहीं वह भी
औरों की तरह अपने दिमाग से विचारों को झटक कर जी लेना सीख जाती ? क्यों वह सोचती ही रहती है ? अलबत्ता
इससे कोई नुकसान नहीं मगर इतना सोच क्यों उस पर हमेशा ही हावी रहता है ? क्यों विचारों की नदी अहरह बहती ही रहती है लहर-बहर उसके उचाट मानस-विस्तार पर ?
‘सोच-विचार ही तो आदमी के जिंदा होने की पहचान है लाली। जो सोचे ना करे हैं वे तो मुरदे या फिर पत्थर ही होवे हैं।’
पापाजी के शब्द उसे अक्सर याद आते। वे उसे दिखलाते थे कि कैसे उनके मुताबिक जर्रा-जर्रा प्रकृति का, सोचता है-फूल, कली, डाल, पत्ती उन्हें कोई भी सोच से परे न लगता था।
‘ये फूल सोच रहा होगा कहाँ इन्होंने इत्ते से गमले में लगा दिया मैं !’
’ये पत्ती कैसी इठलाई पड़ रही है जरा देख, मजबूत डाली का सहारा जो मिला हुआ है !’ और तो और, कांटे भी उन्हें तो फूल की रक्षा में अदब-ओ-कायदे से तैनात दिखते थे। अदब और कायदा आखिर बिना सोच-विचार के तो नहीं आता !
‘बिटिया अब कैसे हैं तुम्हारे पापाजी ?’
निद्रा से जागी सी, वह आँखें विस्फारित करके देखती थी। सामने था वही हरा समंदर जिसे बाहरी रास्ते से अलग करती कांटों की बाड़ के उस छोर पर निर्बाध आने वाली लहरों की तरह के थे वे सब पापाजी के माॅर्निंग वाॅक के
साथी जो उससे पूछ रहे थे -
’कैसे हैं तुम्हारे पापाजी ? कोई सुधार आया हालत में ? ? ?’
उन्हें उसने जो था जैसा था जवाब दे दिया। लेकिन घर वापस लौट कर जब यही प्रश्न उसने भाइयों से किया तो वे ‘‘जो था जैसा था’’ वैसा जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उनके जवाब गोलमोल थे !
‘कैसी है तबीयत पापाजी की ?’
’कैसी और क्या होनी है अब उनकी तबीयत ? खुद जितना नहीं झेल रहे उससे चौगुना हमें झिलवा रहे हैं।’ माथा पीटने जैसा स्वर था बड़े भैया का-
‘पता है तुझे ? इस एक महीने ही मैं अपने साथ वालों से कितना पीछे हो जाऊँगा ! क्या-क्या नहीं निकल जाएगा मेरे हाथ से !’
‘न जाने किन जनमों का बदला ले रहे हैं पापाजी हमसे ! आज-कल में भी कुछ हो-हुआ जाए तो अभी भी इत्ता टाइम है के हम अपनी फ्रेंकफर्ट की डील निपटा सकते हैं।’ वे होंठों ही होंठों में बुड़बुड़ाए थे। भाभी के साथ रह कर बेहतर
होता कि वे भाभी को कुछ अपने जैसी बना देते, उल्टे वे ही भाभी जैसे हो लिये लगते थे।
’मैं देख आऊँ पापाजी को !’ वह क्या कहती सिवाय इसके ?
‘हाँ हाँ आप देख ही आओ। क्या पता आपमें ही प्राण अटके हों ! डाॅक्टर्स तो जैसे देख ही नहीं रहे उन्हें ?’
बड़ी कुढ़न व ढीठता के साथ कमलिनी भाभी दांत किटकिटा उठी थीं। अब तो उन्हें भैया की उपस्थिति आदि की भी चिंता-फिक्र न रह गई थी जैसे। रत्ना भी न जाने कैसी तो, पत्थर सी निर्लज्ज हो आई। उसने अपने ऊपर कोई असर न महसूस किया।
‘देख ही आती हूँ।’ बस् यही कहना काफी लगा था उसे। शुक्ला चाची भी जब उसके साथ नत्थी हो गई तो भाभी ने फिर दो टूक सुना दी थी-
’तुम कहाँ चली देवी जी ? तुममें भी प्राण तो नहीं ही अटके होंगे परम पूज्य ससुर जी के ! तिवारी कल तक की छुट्टी ले गया है पता तो है तुम्हें। कौन चाय-पानी देखेगा यहाँ आने-जाने वालों का ?’
शुक्ला चाची बेचारी एकदम से ही ठिठक कर जड़ हो आई थी एक पल के लिये तो, मगर ऐसे प्रतिदिन के ओछेपन की तो वह आदी हो चुकी थी भाभियों के राज में।
सुनने की देर थी कि उधर हरनामा जल्दी से कार ले आया था। कुढ़ती, दाँत पीसती भाभी पीछे रह र्गइं। कार उन्हें ले उड़ चली थी हाॅस्पिटल की ओर। कार में अकेलापन पाते ही उसके आँसू बह निकले रेलम-पेल। वह ढह गई शुक्ला चाची की गोद में। रोना था कि थमने का नाम न लेता था।
’मत रोओ दीदी, मत रोओ इत्ता। सब भली करेंगे भगवान। बीबीजी !’
मगर आँसू थे कि किसी की गोद, किसी के कंधे का सहारा चाहते थे। वे यह कहां देखते थे कि कंधा किसका है ? गोद किसकी है ? गनीमत थी कि यह सीन देख पाने को भैया-भाभी लोग वहाँं नहीं थे !
विजिटिंग आवर्स में हाॅस्पिटल रोगियों के परिजनों की आवाजाही से भरा पड़ा था। लंबे-लंबे वृक्षों ने अपने साऐ अभी अपने जिस्म में ही समेट रखे थे। चढ़ता सूरज धीरे-धीरे उन सायों की पीठ थपथपा रहा था। सहमे दुबके, माँ के पीछे खड़े से ये साऐ सूरज के आश्वासन से थोड़ा-थोड़ा बाहर झांक पड़ने को आतुर थे, होते-होते शाम तलक ये निडर हो वृक्ष से भी लंबे हो कर आसपास की दुनिया देख पुनः जैसे माँं के आँचल में छिप सो जाएंगे।
हरनामे ने ऐसे ही पेड़ों की कतारों से सजे रास्ते से गुजार कर कार को ठीक पोर्च में बीचों-बीच ला खड़ा किया था वहां से कुछेक गज के फासले पर कि जहाँ भैया लोगों के लिये पार्किंग रिर्जव्ड थी।
‘उतरो दीदी।’
कहती हुई शुक्ला चाची ने उसे सहारा दे कर कार से उतारा। हरनामा कार का डोर लाॅक कर उनके पीछे-पीछे चल दिया। शुक्ला चाची का दिल घटनाओं से बिना व्यथित हुए कार्य करते रहने का आदी हो चुका था। उसने अपने पीछे आते हरनामे को डपटा था-
‘ओ जा ओय, कार स्टैंड पे तो खड़ी कर, बीचमबीच लगा के आरा हे. . . . ’
व्हिसिल की तेज आवाज के साथ सिक्योरिटी गार्ड वीआईपी स्टैंड पर कार लगवाने वहाँ तब तक पहुँच ही गया था। मालिकों की गाड़ी से कौन उतरा है यह जानने की उसे उत्सुकता थी।
‘दीदी रानी हैं ये, साब भैयाओं की इकलौती बेहेन ! ’नखलऊ’ से आई हैं। वहाँ ’इनवरसीटी’ में पढ़ाती हैं।’ शुक्ला चाची ने अपनी बोली में परिचय कराया था।
‘भोत सालों में आए दीदीजी आप ! आप को हमने कब्भी नी देखा।’
‘हाँ, मैं बहुत सालों मंे आ पाई।’ उसने कहा और कहने के साथ ही उसे ख्याल आया कि कितनी दूरी थी लखनऊ और दिल्ली के बीच ? मगर दिलों के बीच पसरी दूरी का कोई क्या करे ?. . . .अब यह सब कोई मायने नहीं रखता। सिक्यूरिटी गार्ड आर्शीवाद लेने उसके पैरों मे झुक गया था। कोई पैर छुए उसे पसंद नहीं, पर जब कोई छू ही चुका तो आर्शीवाद तो देना ही होता है। वह उसके सिर पर हाथ रखती थी निशब्द।
’दीदी रानी, पापाजी जल्दी चंगे हो जाएं हमारी तो यही प्रार्थना है। आपनिराश मत होइये। रब सब भली करेगा।’
उसके बहते आंँंसू संभालना उसके वश की बात नहीं थी। उसने पाया कि वह बच्चों की तरह रो रही थी। कितनी लाचार थी वह। कितनी मूर्ख भी ! कहाँ तो प्रकृति और दर्शन की बड़ी-बड़ी भारी भरकम बातों से दिमाग को भरे
रखना, और कहाँ जज्बाती हो कर यूं आँसुओं में छल-छल बहना, वह खुद सोचती आई है कि यह सब मैच्योरिटी के लक्षण नहीं हैं । उसे समझना होगा कि वह कोई बच्ची नहीं रही अब -
‘ऐसे रोओगे दीदी, तो कैसे चलता है ? अभी तो खूब मंजर आने हैं रोने-धोने के। संभालना तो होगा ही अपने आप को।’ शुक्ला चाची अपने अनुभवों में पूर्ण परिपक्व सी, वह उसे कंधे से थामे ले चली थी, हरनामें से कार की चाबी सिक्योरिटी को संभलवाती . . .
‘चलो जी, अब जाओ तुम भी, फटाफट हमको वापस भी होना है फिर। गाड़ी सही स्टैंड पे लगा देना।’
हरनामा उनसे आगे-आगे, लम्बे-लम्बे डग भरता दौड़ा जाता था राह बताता सा, जरूर पापाजी से जुड़ी कोई-कुछ यादें होंगी उसके पास भी तभी नवह भी एक नजर उन्हें देख भर लेने को उत्सुक था। मालिकों के सामने तो वह यहांँ आने
से रहा।
वार्ड में रत्ना की विशेष उपस्थिति को तरजीह देते हुए भी डाॅक्टर निस्पंद से थे। मशीन के जैसे, बेचारे करें भी क्या ? क्या सचमुच कुछ नहीं था
उनके हाथ में अब ? बस् एक बार ! एक बार बस् पापाजी आंँंखें खोल कर उसे देख भर लें !
’नहीं, नहीं ! कोई चमत्कार ही हो तो और बात है !’ डाॅ मिन्हास का सिर ना में हिल ही गया था। पापाजी की निस्पृह देह में कहीं कोई स्पंदन न था। माॅनीटर पर आ रहे ग्राफ में ही उनका जीवन सिमटा था। प्राणवायु सिर्फ जीवन रक्षक नलियों के ही रास्ते सफर कर रही थी लड़खडाती-डगमगाती।
‘आपको सर ने बताया नहीं ? अब कोई चाँस नहीं है ? केवल मशीनों के सहारे जिंदा हैं। . . . अगर इसे जिंदा रहना कहें तो !’ डाॅक्टर ने तो कह दिया जो कहना था।
जानती तो थी वह भी कुछ-कुछ, मगर क्यों मानने को तैयार न होता था जिद्दी मन ? इस मन को कैसे, कहां पकड़े ? जो हाथ आ जाए तो क्या करे इसका ?
बीस थप्पड़ जडे़ इसे, और एक गिने !
खूब दबाते-रोकते भी रूलाई थी कि हिलक-हिलक कर उसे अपनी ही नजरों में बौनी बनाए जाती थी। भला ऐसा भी क्या मोह आ जुड़ा था अब अंतिम बेला में ? नजरें न हटती थीं उसकी, कैसा कोमल भाव छाया था पापाजी के चेहरे पर आज भी ! कैसा असीम शांति का विराट भाव मृत्यु तुल्य कष्ट भोग कर भी वे अपने दामन में समेटे हुए थे !
कभी उन्हें गुस्सा होते उसने नहीं देखा था। गुस्से होते तो बस्, वे बात नहीं करते थे। इसी से बच्चों को लग जाता था कि पापाजी उनसे नाराज हैं। कभी डाँटा फटकारा नही। थप्पड़ नहीं जमाए। बस् बातचीत बंद कर दी !
इसीसे वे सब अकुला जाते थे। उनका अबोलापन किसी को न सुहाता था। अब ?
अब कब से अबोल व्रत लिये पड़े हैं, अब भी तो सब अकुला रहे हैं। सबकी इस अकुलाहट का रंग अब जुदा है। अब सबको पंछी के पिंजरा छोड़ उड़ जाने की व्याकुलता भरी प्रतीक्षा है। अपने-अपने कारणों से सब चाह रहे हैं कि प्राण
पखेरु तज दे पिंजरा। अपने आराम-सुविधाएं छोड़ पूरा कुनबा हलाकान है।
कहाँ, क्यों और किसमें तथा किसलिये अटक हो ऐ विरागी ? इतने दिनों में देख तो लिया सबका आंतरिक स्नेह ? काहे चिपटे बैठे हो इस पराई माया से ? अब और क्या देखना बचा है पापाजी ?
मन में उथल-पुथल मची थी। उसके दोनों हाथ पापाजी की ठंडी सी कलाई थामे थे। फिल्मों में, किस्से-कहानियों में चमत्कार हो जाते हैं, असली जिंदगी में नहीं। जीवन भर खूब-खूब काम निबटा चुके पापाजी खासे आराम की मुद्रा में थे। उसे रह-रह कर लग रहा था कि अब उन्हें और बेआराम क्यों और क्योंकर होना है ? जो ठान लिया सो ठान लिया पापाजी ने तो ! वे तो अब जगते नहीं दीखते।
नर्स ने सावधानी से पापाजी के शरीर में लगी किन्हीं नलियों की देख-रेख की और उसके पास यूँ आ खड़ी हुई कि मानो जताना चाह रही थी कि अब बस् भी करिये, बहुत हुआ ! शुक्ला चाची ने उसे सहारा दे कर ठीक से बिठा
दिया, नर्स ने तत्काल मौका देख कर उसके हाथों से पापाजी की कलाई छुड़ा दी ...
‘धैर्य रखिये मेम, अब धैर्य ही से काम लेना है।’
मम्मी कहा करती थीं कि अपने देश में तो डाॅक्टर और फिलाॅस्फर एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जरा छींक एक आई नहीं, कि बिना फीस के डाॅक्टरों की सलाहें शुरु-तुलसी अदरक का काढ़ा पिला दो ! सिर दुखा नहीं कि दूध-जलेबी खिलाओ। किसी के यहाँ हारी-बीमारी हुई नहीं कि बीमार का हाल-चाल पूछने आने वालों में डाॅक्टरों के साथ-साथ दार्शनिकों की संख्या ज्यादा होती है। किसी घर में गमी हो गई तो अपढ़ से अपढ़ भी दोहराता मिलेगा कि ‘अब कित्तना रोना है ? जो आया है उसे तो एक दिन जाना ही है ! दुनिया आनी-जानी है !’
’दुनिया आनी-जानी है ! खुद पापाजी कहते थे कि जन्म के साथ ही मृत्यु का भी समय लिख दिया करे हे विधाता ! काल तो शाश्वत है ! बड़ा ही कठोर है ! काल की पकड़ से कोई नहीं बच सकता लाली ।’
’मैं बच जाऊँगी ! काल आएगा तो मैं आपके पीछे छुप जाऊँगी, वो इधर-उधर ढूंढ के चला जाएगा।’ वो हँसती, पापाजी भी हँसते, मगर उनकी वह हँसी एक दार्शनिक की हंसी होती। वह तब इन सब चीजों के अर्थ कहाँ समझती थी ! धीरे-धीरे विधाता, काल, प्रकृति आदि उसके मनो-मस्तिष्क पर गाढ़ी मेंहदी से रचते चले गए। पापाजी ही उसके ठिठके हुए दर्शन में फेर-बदल भी किया करते थे -
’विधाता कोई अपना नौकर नहीं है जो अपने हर काम को बनाने दौड़ा चला आएगा। अपना हाथ ही जगन्नाथ है। हाथ हिलाऐंगे तो विधाता भी हाथ का सहारा देगा।’ उनके सूखे-सट्ट से हाथ पर अपने सिर को रखा तो जीजुड़ सा गया। साथ ही न जाने कहाँ-कहाँ की और यादें दौड़ी चली आती थीं। पापाजी कहते थे -
’काल की मार से बिट्टो, वो ही बच सकता है जो मनुष्य के दुख-दर्द समझता है। जिसने मानवता के लिये जीवन जिया वही कालजयी होगा। अपने हाथों अगर एक का भी भला हो गया तो जीवन सार्थक हो गया।’
भैया लोग पीठ पीछे उनकी हँसी उड़ाते। उसका सारा पाॅकेट मनी हड़प लेते और मजाक बनाते कि-
’जा तेरे हाथों हमारा भला हुआ है। अब तेरा जीवन सार्थक हो गया ! तू कालजयी हो गई !’
वह हँसी-ठिठोली की ही उम्र थी। पापाजी की बातों को बहुत ज्यादा न समझ पाने की उम्र थी। किंतु पूरी कोशिश करती कि ध्यान से सुनती दिखे ! वैसे भी बेटों से अधिक बेटियाँ संस्कारों, विचारों की विरासतें संभालती आई हैं। उन्हीं को नाजुक-कोमल माना गया, उन्हीं को संरक्षण में रखे जाने के निर्देश, आदेश दिये गए, और ताज्जुब कि उन्हीं के
कोमल कंधों पर परिवार-समाज की सारी, भारी-भरकम इज्जत आबरु के वजनी से वजनी जुए रख दिये गए ! परिवार-खानदान की इज्जत ढोती हुई बेटी शेषनाग सी हो रही, जरा हिली नहीं कि खानदान की इज्जत का फालूदा बना ! इसलिये सारे लेक्चर लड़कियों को पिलाने जरुरी समझे गए ! लड़कों के लिये इस सब के कोई मायने नहीं ?
’यहाँ भी दीदी सोचते बैठ गए ! भोत सोचते हो दीदी आप। पापाजी को देखना था। देख लिया। चलंे अब।’ शुक्ला चाची को अब घर में अधूरे पड़े अपने काम और उनसे भी अधिक भाभियों की झिड़कियों के ख्याल सता रहे थे। नर्स ने भी जुमला जोड़ा ‘अब विजिटर्स आवर्स भी खतम होने वाले हैं।’
एक बार भर नजर पापाजी पर डाल उठ ही खड़ी हुई वह मगर कदम थे कि आगे बढ़ने को तैयार नहीं, जैसे जमीन में धंस से गए थे। उसे वहीं निढाल किये जाते थे ! सच ही कहते थे भाई लोग ‘तू क्या करेगी देखकर ?’
’आप भी दीदीजी, अब बस् करो ! जाने दो जाने वाले को !’
शुक्ला चाची कहे कि रत्ना को फिर से रोना ना आए तो कैसे न आए ? क्या उसके रोके रूके हुए थे पापाजी ?
’सब लिखतें लिखी जा चुकी, अब कैसी तकरार ?
तज के चोला मैं चला, रख अपना प्यार-दुलार !’
कौन था जो उसे हिला-डुला, चला रहा था ? कौन था जो लंबे-लंबे काॅरीडोर्स से पार कराता, लिफ्ट से चढ़ाता-उतराता उसे लिये जाता था यहाँ से वहाँ ?
जैसे वह स्वयं यह सब नहीं कर रही हो। जैसे ये शरीर भी उसका न था। पता नहीं किस तत्व से वह वंचित सी हुई जाती थी। इस पोर्च से घर के उस पोर्च तक की यात्रा में उसे लगा मानो जो कुछ साथ ले कर चली थी वह सब कुछ छूट सा गया था, जैसे राह में ठग कोई, रेशा-रेशा लूट गया था।
’हें, बिट्टो बावरी ! यूं कहें हैं कि होई है वही जो राम रच राखा !’
अथाह हताशा की बर्फ से ढंके उसके दिल के कोने-कोने में कोई पापाजी की वाणी में गुनगुनाता सा था जैसे। या. . . . .
कि उसीका अंदरूनी डिफेंस मेकेनिज्म उसे हाथों-हाथ संभालता था ? पापाजी यदि देख रहे होंगे उसे तो मन ही मन यही तो सोच रहे होंगे कि न जाने कौन-कौन दर्शन की घुट्टी पिला-पिला कर इत्ता संभाल कर पाला, फिर भी रोती-पगलाती फिरे है निरी बौड़म सी ! क्या सीखा तूने लाड़ो मुझसे री ? यँूं रो-रो के बिखरना कौन सिखा गया मेरी लाड़ो को ? रोता कलपता हिया जार-जार रोए और रो-रो कर पुनः बस में न आए तो क्या करे ? माता-पिता के पालन-पोषण पर समझदारी की अंतिम मुहर जो लगानी थी जिसे भाई लोग न जाने कब से लगाए घूमते थे ! ना ना ! वह उतनी समझदार कब होनी थी !
ना चाहते हुए भी जाने कैसा-कैसा तो कुछ अजीब उखड़ा-उखड़ा सा आए जाता था मन में। निपट एकाकीपन भरी मगर एक ढीठ ठंड सी धीरे-धीरे आ पसर रही थी उसके मन पर, बेचैनी व छटपटाहट भरा कोलाहल मगर थमता जाता था। जब सब तरफ से अकेलापन हो जाए तो अजब साहस की तरह का कुछ समाने लगता था उसके भीतर। कुछ वैसा ही आ ठहरा दीखता था। जिन चीजों को, जिन बातों को आप अपने तरीके से न निपटा सको तो फिर
प्रकृति को ही उसका काम करने दो !
अरे, आप क्या करने दोगे वह तो खुद-ब-खुद कर ही लेगी न ? लाओ, लाओ इतना शीत भाव ले आओ अपने में कि सब दुख-दर्द केअणु-जीवाणु निस्तेज हो रहें ! आखिर जीवित होने का, जीवित कहलाने का फर्ज भी तो निभाना होगा !
’ये बड़ी भली हुई दीदी के आपने भरपूर समय बिता लिया पापाजी के संग। अब लगा चंगा आपको।’
शुक्ला चाची को तसल्ली हो गई लगती थी। क्यों न हो बेचारी न जाने कब से इस परिवार के साथ रहते-रहते न जाने कब परिजन सी ही तो हो रही थी। कोई इसे माने या न माने, कोई जाने या न जाने ! और फिर ये किसने कह दिया कि
परिजन बड़ा स्नेहभाव ही रखते हैं ? उनके दिये जख्मों की पीड़ा तो सहने वाला ही जानता है। शून्य में खोई वह कब घर पहुंची उसे जैसे कोई भान न था।
‘तुम्हारे इंडिया में एक बात खूब देखी ! अरे रसाला कोई एक बंदा बीमार हुआ है और सारी जमात हाजिर रिश्तेदारों की ! हा हा हा’ कमलिनी भाभी प्रीती भाभी से यूं बतिया रही थीं मानों वे जन्मी, पली ही इंडिया के बाहर हों।
‘हाँ दीदी ये तो है, सब रिश्तेदार चुटकियों में आ जुटते हैं चाहे उनकी जरुरत हो कि न हो !’ प्रीतो भाभी के अंदाज भी जुदा न थे।
‘अब भई यहीं देख लो ! पापाजी ने बिस्तर पकड़ा नहीं कि इसको-उसको, फलाने-ढिमाके सबको खबर मिलने की
देर थी और सब अपने काम-धाम छोड़ के यही स्टिकर बन लिये। कित्ते दिन से हो रहा है इंतजार-इंतजार और इंतजार बाब्बा !’
’कित्ता टाइम है भैया इंडिया में सबके पास ! कित्ता इंतजार कर लेते हैं लोग यहाँं ! किस्सी को कोई और काम-धाम नहीं ....... ’
प्रीतो भाभी सुर से सुर मिला रही थीं।
रत्ना के कानों में जैसे पिघला सीसा कोई डाले दे रहा हो। कहीं ये सब उसी के लिये तो नहीं कहा जा रहा ? न जाने इन दिनों वह क्यों आत्मविश्वास खो चुकी सी महसूस करती थी ! जो भी वार्तालाप होता उसे लगता उस वार्तालाप में मजाक का, अवांछितता का मुख्य बिंदु वही भरहै। उसका इतने दिनों से यहाँ टिके रहना शायद भाभियों को पसंद नहीं आ रहा इसीलिये वे वक्त बेवक्त कुरेदने में लगी रहती है। उनमें आपस में कोई प्रेम भाव हो, आत्मीयता हो यह तो दूर-दूर तक सोचा भी नहीं जा सकता था किंतु पापाजी के प्रति, उस अपनी इकलौती ननद के प्रति तल्खी भरा विरोध प्रदर्शित करने में वे तीनों एक सूत्र में बंधी नजर आती थीं। तब वे एक-दूजे की सगी दिखाई देतीं थीं। जाहिर है तीनों के स्वार्थ एक से थे। उन स्वार्थों की पूर्ति में संभावित बाधा यदि कोई थी तो वह लखनऊ से आई अदना सी प्रोफेसर ननद ही तो थी।
‘भई अपन से तो इत्ते दिन अपना घर-परिवार छोड़ के कहीं नहीं रहा जात्ता। सारी दुनिया एक तरफ अपना घर एक तरफ। अब तो बड़ी याद आ रही है घर की। न जाने कब तक पड़े रहना है यहाँ। भई उन्हें जाना है तो टलें , जीना हो तो जगें । जाने कब तक झेलना है बाब्बा !’ कमलिनी भाभी बड़ी हताश और उकताई हुई कहे जाती थीं जैसे अपना
टलना या जीना पापाजी के हाथ की बात हो !
भाभियों ने देख लिया था कि वह उनकी कहा-सुनी को स्वयँ तक ही सीमित रखती है, भाइयों तक नहीं पहुँचाती है इसलिये वे अब खुल्लम-खुल्ला उसके सामने अपने मन की सारी दबी-घुटी भड़ास निकाल दिया करती थीं ! गमगीन माहौल में रहते-रहते, गमगीन बने रहने का ढोंग करते-करते वे सब बौरा सी गईं थीं। अविजित अलग फोन पर
झुंझला गए थे-
‘पापाजी का सब ऐसे ही चलना है तो वहाँ आखिर कब तक पड़ी रहोगी ? आ जाओ वापस। संभालो अपने बच्चों को। एक्जाम्स सिर पर हैं, और बिल्कुल पढ़ कर नहीं देते हैं !’
वहाँं बच्चों की पढ़ाई का सीजन और माँ यहाँ बैठी है ! पिता को सब रेडीमेड चाहिये ! कुछ अच्छा कर देते हैं बच्चे, तो बच्चे उनके हैं। कुछ गड़बड़ की आशंका होती है तो फौरन बच्चे माँ के मान लिये जाते हैं !
एक बड़े संत्रास के अंदर अनेक छोटे-छोटे संत्रास थे। उसका यहाँ रुके रहना भाभियों और अविजित को रास नहीं आ रहा था। उसका यहाँ से चल देना शायद....... शायद भाइयों केमनमाफिक न हो। वे भी तो भाभियों की ही तरह यही कुछ चाहते थे कि वह तो बस् अपना हिस्सा रफा-दफा करे और चलती बने। लेकिन सब कहीं न कहीं फंसे हुए थे, संत्रस्त थे। जब तक पापाजी का महाप्रयाण नहीं होता तब तक उनकी वसीयत को खोला नहीं जा सकता था जो कि
वकील मामा तथा उनके ग्रुप के हाथों में सुरक्षित थी और पापाजी ? वे तो बस् चुप्प साधे थे। न जाने उनके माध्यम से वक्त उनके बच्चों के क्या-क्या न इम्तहान ले रहा था ! सब अपने-अपने तरीके से इस इम्तहान को झेल रहे थे। सबकी अपने-अपने स्तर की अकुलाहट थी !
उसाँस और रह-रह कर बस् उसाँस थी लेती वह और करती भी क्या ? उसके आसपास सब शून्य, शून्य लगता था
उसे। सब शून्य शून्य, सब थमा-थमा सा !
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
8-
अगली सुबह और सुबहों से भिन्न न थी। वही चिड़ियों का अविराम कलरव, वही मंद-मंद निर्लिप्त योगिनी सी,
साध्वियों सी शांत चलती पवन, उनके बीच कोई निरा लुच्चा-लफंगा सा एकाध पवन झकोरा सबको ठेलता-धकियाता,
छेड़खानी सी करता,पूरी ढिठाई से कुछ-कुछ अंतराल से गुजर जाता था। वही मुंह अंधेरे जागती दनादन अपने काम-काज निबटाती शुक्ला चाची, वही नींबू पानी। वही अस्थमा के अटैक का हल्का-फुलका सा डर।
अलग क्या था ? कुछ भी नहीं। बच्चे-कच्चे सब वैसे ही सोए पड़े होंगेे अपने-अपने ठिकानों में, जिनके स्कूल रहे होंगे वे न जाने कब अपने स्कूल निकल लिये होंगे सर्र से। बाहर पोर्च में कोई कार आती थी तो कोई जाती थी। सब कुछ वैसा ही गुम-गुम, गुम-सुम सा। वैसी ही बोझिलता भरा हृदय लिये वह टहलती रही एक-एक कदम गिनती, कभी सारी गिनती भूल-भूल जाती सी। लौट कर अपने निर्धारित कमरे में राॅकर पर आ ढही थी चुपचाप।
आजकल सांँसें धौंकनी की तरह चलने लगती थीं रह-रह कर। इधर की वैचारिक उठाई-धराई में बीपी नाॅर्मल तो नहीं ही रह गया था। और भी अनेक मानसिक-आंतरिक ज्वार-भाटे आते-जाते रहते थे, अभी जिनसे दूर-दूर तक कहीं कोई छुटकारा न दीखता था। आंँंखें बंद किये यूं ही पड़ी रहती चुपचाप न जाने कब तक। आँखें मूंदे हुए भी किसी की पगध्वनि व किसी साए की मौजूदगी का एहसास होने पर उसने आँखें भरसक खोल कर न देखा था, क्योंकि, शुक्ला चाची ही तो होगी। लेकिन ये तो बड़े भैया थे-
’रत्नो चल। बाॅडी ले आए हैं !’ भैया के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था। वह जैसे आसमान से जमीन पर गिर पड़ी थी।
क्या सुना था उसके सुन्न से पड़े जाते कानों ने ? क्या सच् ही उसके सामने प्रेम भैया खड़े थे या कि उसे उनकी उस उपस्थिति का कोई निरीह सा, नालायक सा भ्रम ही हो रहा था ? और यदि भ्रम ही हो रहा था तो क्यूं हो रहा था ? आँॅंखें झपकाती स्तंभित सी वह देख रही थी उस साए को एकटक जो निःसंदेह भैया ही थे। हाँ ! यह भ्रम न था। अभी वह इतनी स्मृति-विध्वंस की हालत में नहीं आ पहुंची थी। पर काश !
भैया सामने खड़े उसे कुछ कह रहे थे और उसे लग रहा था कि बर्बर शीत उस पर आ पसरा है। वह कैसे निपटे उस जानलेवा से शीत से ?
क्या सुना था उसने ? क्या कहा था भैया ने ? होना यही था, किंतु कैसे हो गया सब इस प्रकार से कि घर पर बाॅडी भी आ गई और उसे कुछ भनक तक न हुई ? वह टहलती-राॅकर पर पड़ी झूलती रह गई ! वह कहाँॅं कैसे पड़ी सोती थी बेसुध ? कौन से चिंता-फिक्रों के अनगिनत घोड़े बेच पड़ रही थी कि उधर सब हो हवा गया और लो इधर बाॅडी भी आ गई !
क्यों, क्यों ऐसा होता है कि कोई इतना करीबी आपके पास से यूं चला जाए सदा के लिये, और आपके दिल पे, दिल के भीतरी किसी कोने-कोठरे पे उस के जाने की कोई आहट तक न हो !
कैसे यूं बेआवाज, बिना पद्चाप चले गए आप ?
कभी तो आपने किसी को ठगा नहीं पापाजी, अब अंत समय अपनी ही बेटी को यूं ठगना जरूरी था क्या ? अब मैं क्या जवाब दूं अपनी इस भीतर बैठी बंजारन को कि क्या तुझे भी उन्होंने औरों के जैसा ही समझा ! पल के पल में न जाने क्या-क्या दूरियां नापे लेते थे विचार के निर्बाध पंछी। ठगी सी, लुटी सी हो रही थी वह।
जाते हुए पापाजी उसके सिर पर एक बार आर्शीवाद का हाथ फेरने भी न आए होंगे क्या ? या अपनी मर्जी से ब्याह रचाने की सजा में कमी न करते हुए, कहीं दूर से ही उसे सोती निहार, मौन चले गए होंगे निष्ठुर, निर्लिप्त अपनी महायात्रा पर ! या कहें कि अस्पताल में उसक प्रतीक्षा में ही ठहरे-ठिठके हुए थे ? उसे देख लिया और चल दिये महाप्रयाण पथ पर।
क्या सच् ही उसीमें प्राण अटके थे उनके ? जो उसे पता होता तो वो कभी उन्हें देखने न जाती ! उसकी रूलाई फूट पड़ी थी। वह भैया के आगोश में बंध रोने को उतावली हो आई मगर अब उन्हें उसे अपने आगोश में लेने से भी जरूरी अन्य अनेकों काम निबटाने थे जो एक के बाद एक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर भी, वे हिलकती-सुबकती उसे, अपनी बांह का सहारा दे हाॅल की ओर ले चले थे पूरी व्यवहार कुशलता से. . . . . .
’देख, जो होना था अब हो ही गया है। अब हंगामा मत कर। शाँंति रख शाँंति ! हें, देख शाँंति रखे करे हैं।’ जलती-दहकती भूमि पर जैसे बारिश की बौछार बन कर आते थे भैया के शब्द। क्या उनमें पापाजी उतर आए थे ? ठीक उन्हीं की शैली में बोलते थे वे।
ठीक भी तो था। रो-धो कर क्या हंगामा किया जाए अब ? पापाजी तो जा ही चुके। उनके पीछे की जिम्मेदारियों को उठाना ही अब अहम् था। सो, जिम्मेदारियाँ निभती रहीं। सब यंत्रवत होता रहा। एक-एक कर भाभी-भाई लोग आ-आ कर उसके गले लग-लग कर रोते-कलपते रहे, पगलाते से . . . . .
’रत्नों हम अनाथ हो गए,- - -
' बीबीजी मम्मी के बाद अब पापाजी ने भी अपन छत्तर छाया उठा ली हमारे सिर से !’ पत्थर का भी कलेजा टूक-टूक हो जाए ऐसा रूदन ! ऐसा हाहाकार !
भाभियाँ रोते-रोते भी लगातार हर नाते-रिश्तेदार के आगमन को लक्ष्य करके सबको सुना-सुना कर, दिखा-दिखा कर सप्रयास रो रही थीं !
ओह् ! रत्ना या तो रो ले, या फिर बोल ही ले। उस
निरी, निपट
मूरख से एक समय में ये दो काम नहीं सधते तो नहीं ही सधते थे। सो, वो बेचारी चुपचाप रोए जाती थी, निशब्द की निशब्द ! नाते-रिश्तेदार सब धीरज बंधाते थे कि कितने सुख से बिदा हुए हैं। भरी पूरी उमर जी कर गए हैं। बड़े भाग्यशाली थे। सबको कहाँ मिलती है ऐसी अंतिम घड़ी ?
घर के पुराने नौकर-चाकर रोते-सुबकते, हाथ के काम निबटाते रहे। शुक्ला चाची अपने बढ़ गए पचास कामों के बीच भी उसके चाय-पानी का इंतजाम न भूली। एक समय तक रो-धो कर भाभियाँं दुख की मूर्ति बन सिर पे पल्ला संभाले हाथ-पैर हिलाती रहीं। जुबानें उनकी, मौत की सजा पाए कैदी सी मौन हो गईं थीं। उनके अंतरतम का थम गया उत्पात उनके चेहरों पर शाँत भाव से पसरा हुआ था। मगर उन्हें देख कर यह लगता था कहीं न कहीं कि भीतर ही भीतर एक दूसरा ही लावा उधर उनमें कुलबुला अवश्य रहा होगा। कौन सा लावा ? बंटवारे का। विवादित जमीन के हरे टुकड़े की चिंता में वे सब अवश्य घुली जाती थीं।
उसी की चिंता में कि जिसे पापाजी रत्ना के नाम लिख गए ? कुछ ऐसी सुगबुगाहट सी उसके कानों में न पड़ती तो कैसे न भला ? शांत भाव से आते जा रहे लोगों के समंदर में ही तो ऐसी कोई बातें डगमगाती, थरथराती कश्तियों की तरह रत्ना से आ-आ टकरा जाती थीं। गमी में भी लोग यूं सज-धज कर, बन-ठनकर तशरीफ लाए थे कि जैसे ब्याह-शादी में आए हों, यही लोग फुसफुसाते, कुछ कहते, सजे-धजे और फिर उसकी तरफ यूं देखते कि उनकी बातों की वह कश्ती गरीब सीधी उससे आ कर पनाह मांगती।
महाअग्नि की विराट लपटों के हवाले हुआ पार्थिव शरीर अपने पीछे एक के बाद एक चिरंतन धधकते कई प्रश्न छोड़ गया था उसके अंतस में।
क्यों, आखिर क्यों मानव संपत्ति बनाता है ? अपने, अपनी संतान के भविष्य की सुरक्षा के ही लिये तो ना ? उस संपत्ति से यदि भविष्य सुरक्षित होने के स्थान पर असुरक्षित ही हो जाने लगे तो क्या लाभ उस संपत्ति के अर्जन से ? मानव अपनी, अपने परिवार के सुख-सुविधा के लिये ही तो संपत्ति बनाता है। उस संपत्ति से यदि उसका, उसके परिवार का सुख ही खतरे में पड़ जाए तो कुछ लाभ उस संपत्ति से ? अपने पीछे अपने नाम, यश, कीर्ति की ही कामनावश ही मानव संपत्ति गढ़ता है। उस संपत्ति से यदि उसका नाम, यश, कीर्ति ही विवाद में पड़ जाए तो क्या हाँसिल उस संपत्ति से ?
पापाजी की बनाई हुई संपत्ति भाइयों को विवादों की खाई में धकेल रही थी। उन्होंने तो कभी रंचमात्र भी, कभी सपने में भी न सोचा होगा कि जो संपत्ति वे अपने बच्चों के सुख-सुविधा, संपन्नता, भविष्य की सुरक्षा के लिये बड़े मनोयोग से, बड़े जतन से खड़ी कर जा रहे हैं वही कभी उन्हीं बच्चों के बीच मनमुटाव, दुराव का खासा कारण बनेगी। या फिर, यही क्यों न मान लिया जाए रत्नारानी कि आज की जरूरत के हिसाब से ही उस संपत्ति का बंटवारा हो रहा था तो ठीक ही ता था ? काहे अतीत में पड़े-पड़े कुलबुलाना ? पापाजी की पसंद-नापसंद उनके जीते जी मायने रखती थी, अगली पीढ़ी को अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के साथ जीना है। है कि नहीं ? कहां से मिले जवाब ? कौन दे जवाब ?
महानिद्रा में लीन हो पापाजी तो अब इस सारे नाटक से परे जा चुके थे। नाटक के बाकी बचे पात्र अपनी-अपनी आपाधापी में लगे, न जाने किसकी लिखी स्क्रिप्ट पर कठपुतलियों की तरह, या न जाने खुद अपनी ही रची स्क्रिप्ट पर भाग्य का, समय का, परिस्थितियों का, या विधाता का ही झूठा नाम चस्पा कर किसी भी तरह अपने-अपने पक्ष में इस विवाद को सुलझाने की जी तोड़ कोशिशों में उलझ पड़े थे। रत्ना की रूलाई रह-रह कर गले में आ फँसती थी। बड़े
प्रयास से वह उसे घुटक लेती थी। घर वापसी की तैयारी कर ली थी उसने।
घर ? कौन सा घर ?
वही कि जहाँ उसके हिस्से की जायदाद को ले कर बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा की जा रही होगी ! क्या करे वह ऐसे घर जा कर ?
बच्चों की माया-ममता न होती तो क्या रत्ना उस अपना कहे जाने वाले उस घर से यूं बंधी होती ?
उसके लिये तो किसी होस्टल का कोई एक साधारण सा कमरा ही काफी होता। अरसा बीत गया कि हृदय का कण-कण जानता था ! क्या ? यही कि पाई-पाई के जोड़, गुणा-भाग में माहिर अविजित उसके व्यक्तिगत दुखों-सुखों से कोई सरोकार न रखने वाले, एक निरी दैहिक उपस्थिति मात्र में ही तब्दील हो चुके थे। कोई है बस् ! वे कोई उसके लगते थे बस् ! इतना ही अर्थ था उस उपस्थिति का। कोई अपना है ? न न् ! नहीं। कोई अपना न था वहांँ उस घर में उसका, उसके अपने मासूम बच्चों के सिवाय।
उसके पिता ने अंतिम विदा ली थी यह घटना अविजित और उनके परिवार के लिये कोई मायने नहीं रखती थी सिवाय इसके कि इस घटना के ऐवज में रत्ना के माध्यम से वे क्या प्राप्त करने वाले थे। ऐसी संपत्ति का क्या-क्या किया जाएगा, सब तय किया जा चुका होगा। जैसे उसके वेतन के आने के पूर्व ही उसे कैसे, कहाँ, खर्च किया जाएगा, कहाँ इनवेस्ट किया जाएगा सब आना-फानन तय हो चुका होता था।
उसे खूब पता था कि वह इन्हीं सब कारणों से किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की बहू या फिर किसी की पत्नी कहलाती थी। पत्नी बने रहना है तो पैसा दो, किसी की भाभी, ताई, चाची, बहू कहलवाना है तो पैसा
दो। ये आपकी अपनी सुख-सुरक्षा के वाहक संबंध हैं जिनकी कीमत आपको चुकानी ही होगी। यहाँ तक कि माँ कहलाने के गौरव के लिये भी यदि आप कमाती हैं तो अपने बच्चों की सुख-सुविधा के लिये आपको ही खर्च करना होगा। आपके बच्चों की स्कूल फीस, उनकी ट्यूशन, उनकी यूनिफाॅर्म, उनका बर्थ डे, उनकी चाॅकलेट, उनकी पिकनिक, उनकी दवाईयों का खर्च कौन देगा ? आप ही तो !
यदि वह न कमाती होती तो ? तो उसके मायके से वसूला जाता ! या बच्चों को काफी कुछ से वंचित किया जाता। सो, वह यही मान कर तसल्ली कर लेती थी कि अपने बच्चों के साथ रहना है तो उस आदमी को इसकी कीमत तो देनी ही होगी कि जो बच्चों का बायोलाॅजिकल पिता था। आखिर वह कोई अपने आप से तो बच्चों को पा नहीं सकती थी ! अतः
’जाओ अपनी मम्मी से ले लो।’ यह उस घर का इतना एक सुना-सुनाया, रटा-रटाया जुमला था कि बच्चे धीरे-धीरे अपनी सारी आवश्यकताऐं, हर बात उसीसे बताना सीख गऐ थे। आखिर बताने लायक को ही तो बताया जाएगा न ! थोड़ा सा कुछ यदि वह अपनी सेफमनी रख लेती थी तो अविजित किसी न किसी प्रकार उसकी सारी बचत खाली करवा के ही दम लेते थे। वहाँ हर संबंध की शर्त पैसा था, लेकिन ये वह नहीं समझ पाती थी कि यदि वह भी पैसे के
आधार पर ही उनसे संबंध रखे तो ? तब वह खराब कही जाएगी क्योंकि कमाऊ बीवी पैसा देती ही भली लगती है। वह ससुराली परिजनों पर पैसा लुटाती ही जंँॅंचती है। वह पति को पैसा न दे या अपने पर खर्च करे तब तो हो लिया !
उसे याद नहीं कि आखिरी बार कब उसने खुद अपने लिये अपनी पसंद से साड़ी खरीदी थी। कहीं वह अपने हिसाब-किताब से कोई महँंगी साड़ी न खरीद ले इस करके अविजित प्रेम प्रदर्शन करते हुए स्वयं ही की पसंद के धूसर,
मटमैले रंगों की मैलखोरी कही जाने वाली, मीडियम रेंज की साड़ियांँ उसके लिये खरीद कर एक तीर से दो शिकार कर लिया करते थे। उसे खुलते हुए रंग पसंद थे। मगर अविजित का मानना था कि धूसर या मटमैले रंगों में मैल या गंदगी दिखती नहीं। वो छुप जाती है। यानि भले ही मैलापन रहे मगर वह दिखना नहीं चाहिये ! मनोविज्ञान तो इसे आपके चरित्र पर भी लागू करता है। ओह् !
रत्ना के सोच की डुगडुग गाड़ी तो थमने से रही ! मगर अब, यह भी तो देखो कि आखिर उन्हीं साड़ियों में वह अपनी बड़ी सोबर इमेज बनी पाती थी कि नहीं ?
और फिर, यह भी तो सोचने की ही बात ठहरी कि अविजित की पसंद का मान वह न रखे तो कौन रखे ? उसकी पसंद-नापसंद के क्या मायने थे ? वो तो अब माँ थी। और माँ का क्या श्रृंगार-पटार ? वह तो या फिल्मों में होता है या
देवी माँं का। कभी उसे उन्हीं की पसंद की घड़ी दिला दी जाती तो कभी इसी तरह का कुछ। स्वयँं की अपनी कमाई में से उसे किसी कमीशन ऐजेंट को दिया जाने जितना मिल तो जाता था। यही क्या कम था ? उसे याद ही नहीं कि आखिरी बार कब ब्यूटी पाॅर्लर गई थी, कब आखिरी बार उसने आईब्रोज बनवाई थीं।
’भाभी को तो भगवान ने मेकअप कर-कराके ही भेजा है !’
ऐंडी-बेंडी सी दिखने वाली ननदों में चलो कुछ तो ठसक थी उसकी। चाहे सच्ची हों कि झूठी ही सही, अपने सौंदर्य की तारीफें सुन वह ननदों की बलाऐं लेती न थकती थी।
’मेरी रत्नो, जो थोड़ा ठीक से दूध-घी खाए तो खरे सोने सा है इसका रंग।’ कभी उसे घी-दूध खिलाने के सौ-सौ तरीके ढूंढती मम्मी कहा करती थीं। वही मम्मी जब फैशन के मारे रत्ना अपनी आईब्रो धनुष जैसी बनवाना चाह रही थी तो कैसे उसे बेवकूफ बना डालती थीं . . . . . .
’मेरी लाड़ो, अरे, अभी पतली भवों का फैशन है पर जब मोटी भवों का आएगा तो ये मरी धनुष जैसी भवों वालियां सब क्या करेंगी भला ?’
वो खूब जानती रही होती थी कि मम्मी को नुची-धजी भवें नहीं पसंद थीं इस करके ही वे उसे किसी न किसी बहाने से रोक लिया करती थीं। बस् उनका जी रखने को ही उसने कभी आईब्रोज नहीं बनवाईं। इधर, अविजित को यह पसंद ही न था कि वे स्वयं या कोई अन्य उनकी पत्नी की किसी भी रूप में तारीफ करे। तो काहे की और कैसी कोई फैशनपरस्ती ? उनके लिये तो वैसे भी उनका प्रिय मुहावरा था कि अंधेरे में काली हो या सफेद, सब एक बराबर ही
होती हैं। यही बात यदि पति के बारे में एक महिला कह दे तो ? तो वह कुलटा ! और लो, ऐसे दुखद पलों में भी
कहंँा-कहंाँ की न सैर किये जाता था मन हिरन सा कुलाँॅंचें भरता !
जो मन में क्या चल रहा है यह जानने की कोई विधि होती, भाभी लोग जानतीं कि वह क्या-क्या ने सोचे जाती है तो ? यह तय था कि तब वे अवश्य उसके मन की जान लेतीं, मगर इतना तय था कि खुद के मन की छिपाने की कला वे अवश्य ढूंढ चुकी होतीं !
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
9-
शुक्ला चाची ने बार-बार बजे जाता मोबाइल उसे ला थमाया था। कुछ मिस्ड काॅल थे बच्चों के, कुछ थे परिचितों के कुछ थे अन्य रिश्तेदारों के और न जाने कितने मिस्ड काॅल थे अविजित के जिन्हें देख कर ही उसने मोबाइल स्विच आॅफ करना तो चाहा था मगर आदत से लाचार ! क्या उनके फोन काॅल की यूं अवहेलना कर सकती थी ? उनके सौ उलाहने अलग वहां उसके इंतजार में थे। उलाहनों के साथ-साथ हिदायतें भी थीं अब तो। वे समझ रहे थे कि धनवान ससुराल से पंगा तो ले नहीं पाएंगे वे। तो जो भी मिले वही ले लेने में ही उन्हें अब अपनी भलाई दिखती थी। आखिर कहा भी तो है बड़े-बूढ़ों ने कि भागते भूत का लंगोट ही सही ! सोना भी कुछ कम नहीं उछला हुआ है इन दिनों। काॅल बैक करने पर अविजित उसे सारी दुनियादारी मानो एक ही सांस में सिखा दिये देते थे। कहीं ऐसा न हो कि बेवकूफ भावुक बीवी सब छोड़-छाड़ कर खाली हाथ वापस वापस चली आए। उनकी कुछ नाराजी भी वह भांपे ले रही थी। अब वह क्या करे जो भाई-भाभी लोग अविजित को नहीं बुला रहे ? यह कोई ऐसा आमंत्रित करने का मौका तो था भी नहीं, और कोई अपनी इच्छा से आ जाए तो बुरा समझा जाए-ऐसा मौका भी नहीं ही था। आ जाते वे, उसे लिवा ले जाते तो अच्छा ही लगता उसे। मगर उनका दंभ अपनी जगह, रत्ना को अच्छा लगना अपनी जगह।
उनकी उत्सुकता धनवान ससुर से मिलने वाली संपत्ति को लेकर थी और उनकी खूबी यह कि वे अपनी इस उत्सुकता को सरेआम करने को भी कतई तैयार नहीं। ’भई, अब क्या करें आखिर, उन्हांेने जाते-जाते दे डाला तो उनकी अंतिम इच्छा का मान तो रखना ही होगा’ वाला साधु-संत का भाव हर कड़ी हिदायत में अभी भी बरकरार था !
बिना अस्थमा के लम्बी सांस लेने की रह-रह इच्छा होती थी रत्ना की। वे तो खैर दूर के लोग थे- - - रत्ना को फिर ढेरों
सोच घेरे लेते थे।
कोई आखिर सोचे नहीं तो करे क्या ?
कोई और न सोचे तो कुछ और कर भी ले, मगर रत्ना न सोचे तो कैसे न सोचे ? वह चुपचाप बैठी सोचती थी-कि उसके ससुराल वालों का क्या ? वे सब तो थे ही पराया खून।
उसके अपने, उसके सगे ही कौन बेहतर सोच-संस्कार लिये बैठे थे ? चल तो रहा था गुणा-भाग, सब अंदर-अंदर गणित ही गणित। पापाजी के उठते ही सब अपना-अपना हिस्सा लेने, बहन को उसका हिस्सा न देने की कवायद में पुरजोर लगे हुऐ थे।
इस प्रकार की कवायदें भाभियां कर रही होतीं तो ठीक ही लगतीं एक बार, कि चलो परजाई, पराई ही ठहरीं ! मगर ये कवायदें तो पापाजी के सुपुत्रों में जारी थीं। ओह्-
’रे बनपाखी चुपके उड़ जईयो,
उड़ जो जईयो ते, फिर न अईयो।’
’फिर के न अईयो !’ . . . . . .
रत्ना को न जाने कैसी ठंडी सी, अजीब सी, विरक्ति की सी स्थिति ने आ घेरा था। एकबारगी सोचती थी कि अच्छा ही हुआ कि अपने कभी के, पुराने समय के चले आ रहे दंभ की वजह से अविजित यहाँं नही आए। अगर वे यहां होते, यहाँ का सारा मंजर देखते-जानते तो उसेे जीवन भर किस-किस कदर न कोंचते-टोंचते ?
अब तो जो हो रहा है होता रहे।
बूझो तो कि कहाँ-कहाँ की फिक्रें पालती रहे एक मरी रत्नारानी ही ? पापाजी ने कितनी नहीं फिक्रें पालीं अपनी तमाम उमर सबकी ?
और क्या मिला उन्हें ? मगर-
क्या नहीं मिला ? बताओ तो ? सब तो मिला ! ऐसे फिक्रमंद बच्चे मिले उन्हें आखिरकार, जो कितना-कितना तो बिसूर रहे हैं उनके पीछे उनकी याद में ! कोई देखे तो कि कैसे-कैसे आदर व स्नेह पगे इश्तेहार दिये गऐ हैं चुनिंदा
अखबारों के गमी-मातम के काॅलमों में, कि पढ़ने वाले का दिल भर न आए तो कैसे न भर आए ! कोई पत्थर ही का कलेजा रखता हो उसकी बात फिर छोड़ो। आने-जाने वालों को भरपूर दिखलाया जा रहा है कि पापाजी क्या गऐ मानो हम तो अनाथ ही हो गए ! जो परलोक चला जाने वाला उनके इस रूदन को ऊपरी तौर पर देखने में समर्थ हो तो वापस ही लौट आने को तुल जाए भोला-भाला !
अपने सारे काम-धंधे छोड़ कर भाई लोग पापाजी के मोक्षपर्व को निबटाने में पूरे मनोयोग से लगे हुऐ हैं। वैसे, ठीक ही तो लगे हुए हैं। कौन पापाजी अब दुबारा मरने हैं रत्ना आपा ? क्यों आखिर आप भी एक-एक चीज के पीछे मैग्नीफाइंग ग्लास लिये पड़ी हो ? क्यों, आखिर क्यों चैन से नहीं जिया जाता आपसे ? क्यों कुट-कुट किये जाती हो मन ही मन ? क्यों मन में इन बंजारे सोचों को प्रवेश की अनुमति देती हो जो तुम्हें तुम्हारे ही एरिया से हड़काने लगते हैं ससुरे ? ना गाली नहीं देते ! फिर,
आखिर . . . . . .
क्यों इन आवारा सोचों के समुंदर में अपने सोच की सारी धाराऐं बिला डालती हो चाहे जब ?
अब यही लो. . . तुम्हें क्या करना ये सोच-सोच कर कि भाई लोग क्यूं ऐसा कर रहे हैं ? वैसा क्यूं नहीं कर रहे जैसा तुम
चाहती हो ?
क्यूं सोच के हैरान-हैरान, बावरी-बावरी हुई जाती हो कि रईसी ठाठ का आलम तो देखो कि मौत को भी एक त्यौहार सा ही बना दिया गया है, या
शायद ऐसे आलम में मौत भी स्वयँं एक त्यौहार सा बन ही जाती है ! इन सबको कितनी प्रतीक्षा थी इन सब पलों की, क्या तुम नहीं जानतीं ? तब ? चुपचाप देखो तमाशा !
शाँत-क्लाँत दिखता एक त्यौहार बड़ी गरिमा के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, बड़े नियम-धर्म, बड़ी श्रद्धा बड़े विधि-विधान के साथ मनाया गया। तो---
आखिर, उबाऊ थकान, दमघोंटू प्रतीक्षा से सबका पिंड छूटने के क्षण आ ही गए थे। भाई-भाभी सब निश्चिंत होने को आतुर थे। मगर निश्चिंतता अभी कहाँ ? अभी तो वह कोसों दूर थी ! अभी तो वसीयत खुलनी थी !!! जिसे ठेठ पापाजी की ही तरह बुढ़ा चुके वकील मामा अपनी-बगल में दाबे थे। भाभियों के लेखे वे भी अपने प्रकार के किसी पुराने चिड़ियाघर के एक अलग ही, अनोखे ही जीव थे। हुंह !
’रत्नों को मम्मीजी के सोने में से थोड़ा दे दिवा दो, उसे जमीन-शमीन क्या करनी है ?’
तो ?. . . . . .
उसे तो सोना भी क्या करना है ? लाॅकर में ही तो पड़ा रहना है। कौन वह कभी सोना पहनती है ? वह तो प्रोफेसर थी। इतनी पढ़ी-लिखी प्रोफेसर क्या सोना लटकाती अच्छी लगेगी ? सच् ही तो था। उसे सच् ही तो पसंद न था सोना लटकाए घूमना। यह भी क्या मजबूरी कि मन मिले न मिले, प्यार मिले न मिले, मगर लोक दिखावे के लिये मांग में
सिंदूर खींचे, कलाइयों में चूड़ियां-कंगन भरे, मंगलसूत्र लटकाए घूमती फिरो !
’हाँ तो भला ! क्या करेगी वो मायके की जमीन का ?’
’ना ना ना, रत्नो तो कभी जमीन लेगी ही नहीं ! मायका भला क्यों बिगाड़ेगी हमारी रत्नो !’
’लखनऊ में मकान बन गया है उसका। और क्या चाहिये नौकरी-शौकरी वालों को ?’
’जमीन-शमीन संभालना वैसे भी कोई आसान काम नहीं है आज !’
’और ,लड़की जात के पास मायके की जमीन गई तो पराऐ ही ऐश करेंगे न ?’
’ले-दे के हद से हद उसे पापाजी की बीएमडब्ल्यू भी दे देंगे .
. . . . . ’
प्रस्ताव भाभियों की तरफ से धड़धडाते हुए आए जाते थे जिन पर भैयाओं के सभी के सिर सहमति में हिलते न थकते थे। घर का पत्ता-पत्ता तक तो जानता था कि भाइयों की मुश्किलें बढ़ाए ऐसी बहन न थी वह।
और यह वह खूब जानती थी कि बीएमडब्ल्यू के पुराने हो चुके माॅडल से पिंड छुड़ाने की गरज में भाभियों का एक तीर से दो शिकार का यह एक पैंतरा ही तो था। क्या वे सब नहीं जानती थीं कि वह बीएमडब्ल्यू उसके पोर्च में कहाँ समाएगी ? वहाँ तो उसकी जनता क्लास कही जाती कार ही सोहती थी जिसे शहर की पुरानी से पुरानी तंग गलियां भी आसानी से अपना लेती थीं।
रत्ना में वैसे, पहले भी कहाँ थी पैसे की ऐसी कोई भूख ? रही-सही जो कहीं दबी-छिपी थी भी, तो पैसे वालों का यह हाल देख कर जाती ही तो रही थी।
रही बात अविजित की तो वह उन्हें खुश करने को और कितना पैसा न्यौछावर करे ? वह निपट लेगी सबसे। सो, पापाजी यदि कुछ नाम उसके कर भी गए होंगे तो वह सब भाइयों का ठहरा। वह लिख देगी कि उसे अपना हिस्सा नहीं चाहिये।
अविजित को दे लेगी जवाब जैसे अब तक देती आई है ! उन्हें उसके साथ रहना है तो रहें, न रहना है तो छोड़ दें उसका साथ। दहेज न मिला तो क्या हुआ, दहेज बन कर उसके वेतन की इतनी मोटी रकम किश्तों के रूप मिलती तो है हर माह। यही क्या कम है ? वह बड़े आराम से उसमें अपना व अपने बच्चों का गुजारा कर सकती है। आखिर कोई रूपए-पैसे के बल पर कब तक व कितना साथ ले किसीका ?
और आखिर ऐसा उनमें है क्या, क्या है उनमें जो वह अपने मायके के जमीन-जायदाद के बल पर अपने लिये उनके जैसा पति खरीदे ? क्या फायदा ऐसे खरीदे हुऐ पति का ? उस पर भी उसके, उसके परिजनों के घमंड भरे नखरे हजार !
’कोई फायदा नहीं होगा रत्नों को मामाजी इस जमीन का।’
’अपना मायका अलग खो देगी !’
’उसे तो कोई उसका असली खैर-ख्वाब हो तो यही समझाए कि बहना, बेटी, जेवर-शेवर ले ले, और भाइयों को
समृद्धि का आशीर्वाद दे कर राजी-खुशी अपने घर जा।’
’इतने समय बाद तो उसका मायके का रास्ता खुला है। अब उसे फिर से बंद करेगी भला ?’
’कौन बहन भाइयों से जमीन लेगी ?’
’हें ?’ वकील मामा की बोलती न बंद हो जाए तो क्या हो ?
ठीक !
जमीन का वही सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा भाइयों की सबसे बड़ी दरकार था। छाती में भरपूर पानी लिये वह मिनरल वाॅटर उगलता हुआ अपने उस पानी को सोने में, अकूत संपदा में बदल देने वाला था। बेचारी रत्ना ! अदना सी
प्रोफेसर ! अपनी टके सी नौकरी से अपना व अपने परिवार का गुजारा चलाने वाली। वह कैसे व क्यों कर ऐसी बेशकीमती जमीन की मालिकिन बने ? वह आखिर करेगी क्या उसका ?
बेच-बाच ही तो देगी न् ! तो ले, मम्मीजी के अनमोल सोने में से अपने लायक थोड़ा सा, ले, संभाल इस पारिवारिक विरासत को और जमीन को भूल ! जा बिट्टो घर जा अपने !
रत्ना का मुंह सिला का सिला था।
’लिखवा लो रत्ना से स्टांप . . . . . . ’
वकील मामा बुत बने बैठे रह ही जाने थे।
उनके इशारे, उनकी अर्थपूर्ण दृष्टि से जब रत्ना अनजानी हो रही तो फिर तो करा लो जहाँ कराने हों, जब कराने हों रत्ना से हस्ताक्षर !
वह तो तैयार ही थी।
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
10-
’अच्छा हुआ बाब्बा ! अच्छा हुआ जो इन लोगों ने सही वक्त पर इत्ता जरूरी फैसला ले डाला !’ किसी निहायत अपने से फोन पर बतिया रहीं थीं कमलिनी भाभी।
. . . . . .
’नहीं तो हम तो बहुत बड़ा असाइनमैंट खो देत्ते बाब्बा ! अब वक्त पर पहुंच जाऐंगे तो सब हाथ आ जाएगा !’ वे फुसफुसा कर बात कर लेने वालों में से न थीं, फिर भी बेहद फुसफुसाती ही सी आवाज थी उनकी।
’बैंक लोन की इंस्टाॅलमेंट में ही करोड़ों में धंसे जा रहे हैं सब के सब, बाब्बा।’
हुश !
कमलिनी भाभी आदत से लाचार ! उनका अपनी जुबान पर कब नियंत्रण रहा ?
सो, वसीयत खुलते न खुलते ही वह असलियत भी बहुत कुछ खुल ही गई थी कि बड़े भैया के फ्रेंकफर्ट वापसी के केवल-कुल जमा नपे-तुले, कुछ इने-गिने ही दिन बचे थे। मंझले भैया के प्रोजेक्ट की लागत हर घंटे बढ़ी जाती थी। छोटे भैया के नाम लिये जा चुका भारी बैंक लोन . . . . और क्या-क्या तो !
और इधर पापाजी थे कि अविचल विश्राम किये जाते थे ! अभी भी यदि वे चल दें , . . . . . . तो सारा का सारा इधर व उधर का साम्राज्य सुविधाजनक रूप से संभाला जा सकता था !
तो. . . . . . ?
तो ?. . . . . . तीनों भाइयों की सलाह पर पापाजी की यथास्थिति को अनिश्चितता की कैद से आजादी दिलवा दी गई ?
. . . . . .
रत्ना के काटो तो खून नहीं।
फोन पर शायद भाभी की बहन ही थीं जिनसे अपनी पूरी भड़ास बेखौफ निकाल रही थीं भाभी।
’इत्ते दिनों से कोमा में था डोकरा। अब इस उमर में कहीं रिकवरी होती है बाब्बा ? हें ?‘
. .. . . . .
‘तो जाओ ना बाब्बा जाओ अब, भोत देख लिया पोता-पोतियों का सुख !‘
ठक् ठक् ठक् ! पापाजी के लिये सपाट, मगर अपनी जहालत से छुटकारे के चलते भाभी की कुछ चहकती सी आवाज हथौड़े की चोट सी बजे जाती थी रत्ना के दिल में।
कौन कहता है इस देश में मर्सिकिलिंग नहीं होता ?
’भैया ! जो सहता है वो ही जानता है ऐसे कोमा के मरीज कित्ता झिलवाते हैं बाब्बा रे !’ वो तो थैंक गाॅड कि - - -
. . . . . .
तो क्या सचमुच् पापाजी गए नहीं ?.
. . . . .
बल्कि भेज दिये गऐ चुपचाप ?
???
आखिर उनके जाने के इंतजार में कैसे और कब तक सब लटके रहते ?
और - - - आखिर,
आखिर कैसे, किस ताकत से डरपोक सी कही-समझी जाने वाली रत्ना की आंखें फैल गईं थीं और भवों पर बल पड़ गए थे ? और वो भी अपने ताकतवर भाई लोगों के सामने ?
’पापाजी के हाथ में रहा होता तो वो भी यही करते कि बच्चों को परेशानी दिये बिना चुटकियों में चले जाते !’ प्रेम भैया कहते थे।
’रत्ना तू बेवजह बात का बतंगड़ तो बना मत ! हम पापाजी को तुझसे ज्यादे जानते हैं। हाँं।’
’तू तो इत्ते दिनों से बाहर थी। तुझे क्या पता कि पापाजी क्या चाहते थे ? उन्होंने तो हमें कहा भी था के कभी ऐसा कुछ हो जाए तो उन्हें मुक्ति दिला देना !’
‘जा तू सोई नहीं है ठीक से। जा के आराम कर अपने कमरे में।‘ कहते थे, मानो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह उसे फुसलाते थे प्रेम भैया -
जंगल में नाचे मोर को किसने देखा था ? ?
अब, तुम भी रत्नाबाई ! मान क्यों नहीं लेतीं कि पापाजी की भी यही मंजूरी थी !
हाँ हाँं हाँ !
यही मंजूर करते वो भी ! यही यही मंजूर करते ! यही, यही और बिल्कुल यही मंजूर करते वो भी !!!
मुनिया एक जीवन दूसरे जीवन को चलाए रखता है पर बावरी, एक मशीन भला जीवन को कितना चलाएगी ? एक मशीन तो ठीक, मगर भैया लोग उससे भी ज्यादा मशीनें हो गए लगते थे !
रत्ना के हृदय के अंश-अंश पर निपट असह्य सी वीरानी आ पसरी थी। कभी-कभी ऐसा क्यूं होता है कि इस गरीब दिल से कभी कोई छोटी सी भी, रूई के फाहे जितनी भी चोट सही नहीं जाती। और कभी ? कभी ये लगता है कि पत्थर का बना है जैसे ! कितना-कितना कुछ चुपचाप सह लेता है मरदूद !
उसके आस-पास, भीतर-बाहर सब वीरान ही वीरान सा ही कुछ घनघनाता था। उस वीरानी में, मरे-मरे मन में हताश-हताश से शब्द तिरते थे, हाँ !
हाँं हाँं पापाजी भी निःसंदेह, पापाजी भी यही चाहते कि बच्चों को कोई परेशानी उनकी तरफ से न हो, और . . . . . .
उस रात . . . . . .
नर्स जब पापाजी के वार्ड में आई तब तक तो पंछी मुक्त हो चुका था, कहो कि मुक्त किया जा चुका था। नर्स के सामने थीं चलती मशीनें, मगर ठप्प जीवन। नर्स की हाय-तौबा पर सब दौड़े। और. . . . . .योग्य व काबिल डाॅक्टरों की उस टीम ने डिक्लेयर कर फोन कर दिया. . . . .फिनिश्ड !
कमलिनी भाभी सहित भाभियों के अंतःपुर तक यदि किसीकी पहुंच थी तो वह थी शुक्ला चाची की। कमलिनी भाभी मुंह बंद रख नहीं सकती थीं चाहे सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए। शुक्ला चाची के कानों में और भी जो-जो उनके अंर्तवचन पड़ते गऐ वे सब एक के बाद एक रत्ना के कानों में पिघले सीसे की मानिंद जाते रहे।
दुख की, सौम्यता की मूर्ति बने भैया लोगों को देख कर रत्ना को सहसा यकीन नहीं होता था कि दान-पुण्य सब निपटाते इन्हीं हाथों ने पापाजी की बची-खुची सांसों का भी निबटारा किया है !
’तू बहन है कि दुश्मन ? तू हम पर इल्जाम लगा रही है ! अपने भाइयों पर !’
’तुझे कुछ पता भी है प्रोफेसर महारानी, किस दुनिया में रहती है तू ? ऐसे मरीजों के परिजन तो आज खुद होकर कह देते हैं कि हमें पेशेंट को घर ले जाना है। इसका मतलब यही होता है कि सब जीवनरक्षक हटा लिये जाएं।’ भाई लोग किसके किये-धरे की लीपापोती करते न थकते थे ? उसके बिना मांगे सफाई दे रहे थे।
कुछ कहने-सुनने की ताकत उसमें न थी। बस् रह-रह कर चुपचाप सिसक-सिसक कर रह जाती थी।
’आहो बीबीजी। दुख तो बस् एक आपको ही हुआ है। हमें कोई दुख नहीं क्या पापाजी के जाने का ? हमें देख कर ही धीरज धरिये तो भला।’
पुनीता भाभी प्रीतो भाभी के साथ उसे लिवाने आई थीं। डाइनिंग हाॅल में वकील मामा और भाइयों की बैठक जमी थी। भाइयों की ओर से एक-दो और वकील बुला लिये गए थे। वकील मामा हालातों के आगे नत थे। स्टांप पेपर तैयार थे। रत्ना अपनी तरफ से बिना किसी दबाव के, अपने पूरे होशोहवास में अपना पुश्तैनी जायदाद का सारा हिस्सा तीनों भाइयों के हक में छोड़ रही थी। पूरे होशो - हवास में, स्वेच्छा से।
स्टांप पेपर तो यही कहता था।
अब कि जब रत्ना सिग्नेचर कर देगी तो उस जमीन पर मल्टीस्टोरी नर्सिंगहोम या होटल, या फिर न जाने क्या-क्या तो मल्टीस्टोरी बन सकेगा।
और- -और मिनरल वाॅटर की फैक्ट्री डाली जा सकेगी। घर की संपत्ति घर ही में रहेगी। लड़की जात उसे बाहर ले जाती। यह संभावना खत्म कर भाई-भाभी लोग निश्चिंतता से उसके सिग्नेचर के महापर्व केे इंतजार में थे।
और. . . .
सब कुछ वह घटित हो गया जो रत्ना की सोच में, भाई-भाभियों के सोच में, वकील मामा की सोच में कहीं दूर-दूर तक, कतई-कतई भी संभव न था !
बचपन की उस छुई-मुई, दबी-घिरी, परम संतोषी सी, उस आज्ञाकारी गूंगी गुड़िया के जुबान कैसे उग आई ?
उसने आज्ञा मानने से साफ-साफ इंकार कर दिया !!!
किसने रत्ना ने ??? तो और किसने भला !!!
रत्ना में इतना बल कहाँ से आ गया ???
कहाँ से आ गई इतनी हिम्मत ???
’मैं तो पहले ही कहती थी ये घुन्नी है, घुन्नी !’
’पूरी घुन्नी है, नहीं तो !’
’आस्तीन का सांप निकली सांप !’
’लालच भारी पड़ गया भाइयों के प्यार पर !’
’अजी किस ससुरी मरी को चाहिये भाई का प्यार ? जमीन-जायदाद मिल जाए तो सौ-सौ भाई न्यौछावर !’
’तुम स्सालियों बंद भी करोगी अपनी कटर-कटर ! कुछ सोचने तो दो !’
दांँत पीसते, आगे की रणनीति सोचते अकुलाते-व्याकुल भाई, माथा पीटती, भर-भर मुंह गरियाती न थकतीं भाभियाँं
उसके संकल्प को डिगा न सके।
उसे नहीं करने सिग्नेचर। कोई जोर-जबरदस्ती है क्या ?
वह लेगी अपना वह हिस्सा जो पापाजी उसे दे गऐ हैं। उन्होंने अवश्य उस पर भरोसा करके ही उसे वह जमीन दी होगी। वह कैसे उनके उस भरोसे की डोर को तोड़ दे ?
कैसे ठुकरा दे स्वर्ग सिधार चुके जनक का वह विश्वास भरा पुश्तैनी उपहार ?
कद्दावर भाइयों के सामने एक चींटी के बराबर, बौना सा अस्तित्व था उसका, यह जानते हुए भी पापाजी उस पर यकीन कर गए थे। उसे अपने अस्तित्व को सिद्ध करना होगा। उसे पापाजी के उस विश्वास की डोर कस कर, मजबूती से थामनी होगी।
कर सकेगी वह ऐसा ? एक तरफ लालच में गाढ़े रंगे-पुते भाई, दूसरी तरफ ऐसे ही रंगों से भरपूर सराबोर अविजित। उसके एक तरफ खाई तो दूजी तरफ कुअंा था। नागनाथ और सांपनाथ के बीच वह कब तक अपना अस्तित्व संभाले रख पाएगी ?
मगर नहीं। वह नहीं टूटेगी, अब और ना टूटेगी। बहुत टूटन सहती आई है, टूट-टूट कर, बिखर-बिखर कर, मर-मर कर जीती आई है। क्यों ? क्यों इस प्रकार जीती रहे ? एक परिवार की बेटी बन सारी परंपराओं को सहेजा है उसने, एक परिवार की बहू बन उस के वंशजों को उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम बनाने का ही तो कार्य कर रही है वह ? इन दोनों में से कौन सा उसका कार्य गलत है ? क्या अपराध है उसका ?
बेटी हो कर वह क्यों पुश्तैनी जायदाद से बहिष्कृत की जाने लायक ? और बेटे होकर ही भाई लोग क्यों उस जायदाद के लायक थे ?
वह क्यों अपने सारे अधिकार छोड़ दे ?
और भाई ही क्यों सारे स्वयंँ के व उसके भी अधिकार एंजाय करते रहें ? आज तक वे यही तो करते आए हैं।
अपनी सुविधा के अनुसार जीते रहने के अलावा उन्होंने क्या योगदान दिया है परिवार को, समाज को ? अपनी सुविधा के लिये अंततः उन्होंने पापाजी की आसन्न मौत को भी जल्दी बुला भेजा। अब क्या उसे भी रास्ते से हटाऐंगे ?
इतने सुविधापरस्तों की थोड़ी सी सुविधाऐं कम हो रहेंगी उस जमीन के टुकड़े के न मिलने से। बस् और क्या होगा ! एक और आलीशान नर्सिंगहोम, एक और आलीशान होटल उपलब्ध नहीं हो पाएगा इलाके के रईसों को, एक और मिनरल वाॅटर फैक्ट्री न डलने से क्या हो जाना है हद से हद ? शहर के, परिवार के केप में फेदर लगने से रह जाएगा क्या ?
कोई आसमान थोड़े ही ना टूट पड़ेगा ?.
. . . . .
वह सोचे जाती थी या विचार खुद-ब-खुद उसमें घुसे पड़ते थे। सिलसिला थमता न था विचारों का। एक जाता था कि दूसरा आ जाता था। रेलम-पेल मची थी उसके मनस में। महासंग्राम के जैसा निरंतर कुछ चलता था।
हृदय में लहराते विचारों के विराट समंदर पर आशा से भरा, अपराजित सी आस की किसी मजबूत मगर लचीली डाली से एक परिंदा नादान उड़ तो चला था मगर हैरान-परेशान सा भटकता था क्योंकि उसे अभी अपने परों की हैसियत पता न थी।
रत्ना ने सब तरफ से नजरें हटा लीं अपनी।
भाइयों से, भाभियों से, वकील मामा तक से, किसीसे नहीं मिलानी उसे अपनी नजरें, कहीं वे उसे नजरों से कमजोर न कर दें ! कहीं घुटे-दबे संस्कारों की थरथराहट उसे निश्चय से न डिगा दे। कहीं किसी के नापाक इरादों के पथरीले वार उसके उस मनपाखी को घायल न कर दें। उसने अपनी आँखें कस कर बंद कर लीं कि कहीं ये परिंदा निरीह, अपनों के खोल में छिपे किसी चतुर शिकारी का निशाना न बन जाए !
आँखें भरसक बंद की हुईं थी मगर कान तो बंद न थे उसके। उन्हीं भरपूर खुले, चैकन्ने कानों में पड़ रही थी उसके मोबाइल की बेसब्री से बजे जाती, निरंतर नजदीक आती ध्वनि। बड़ी फुर्ती से शुक्ला चाची ने अविराम बजे जाता मोबाइल उसे ला थमाया था। उसने मोबाइल के स्क्रीन पर नजरें गड़ा कर देखे बगैर जान लिया कि अविजित के काॅल पर काॅल थे। और आखिर किसके हो सकते थे। जब से वह यहाँ आई है उनके प्राण गले में फंसे हुए थे।
उसने न कुछ इधर सोचा, न कुछ उधर, मोबाइल को स्विच आॅफ कर के उसे पास की टेबल से चाय-नाश्ते आदि के बरतन समेटती शुक्ला चाची को उतनी ही फुर्ती से वापस थमा दिया था।