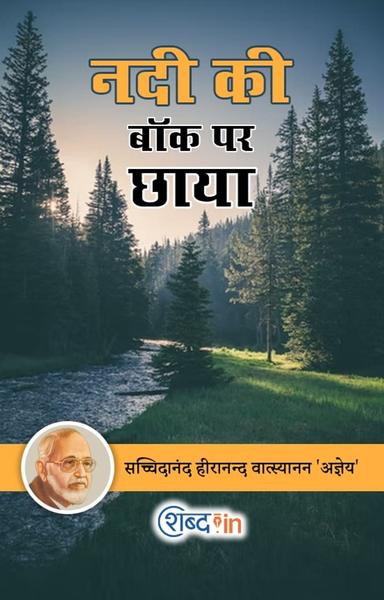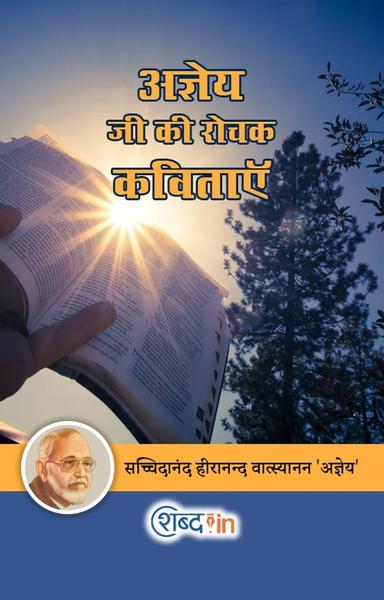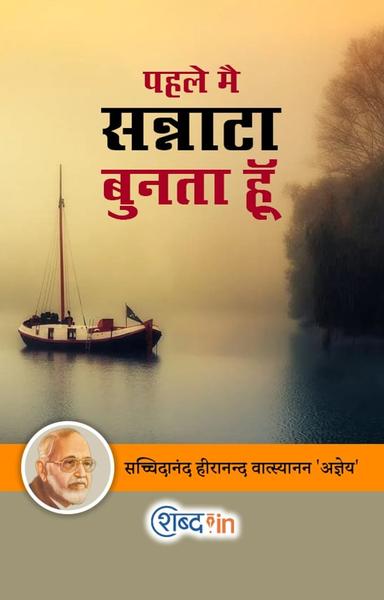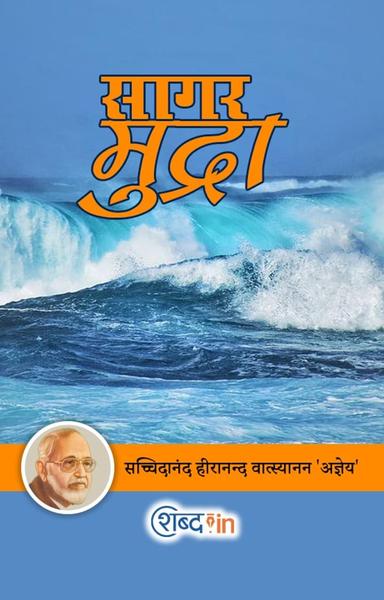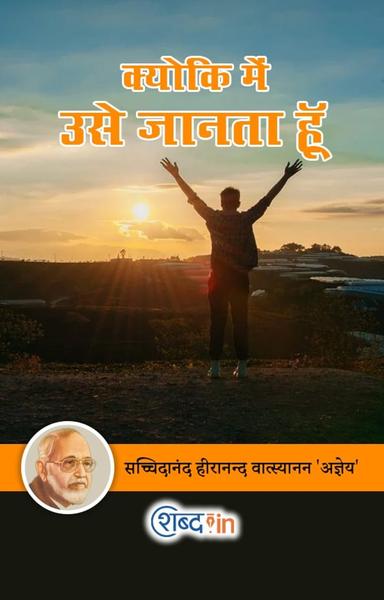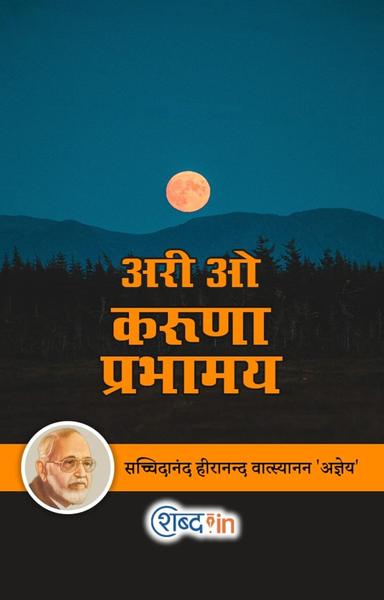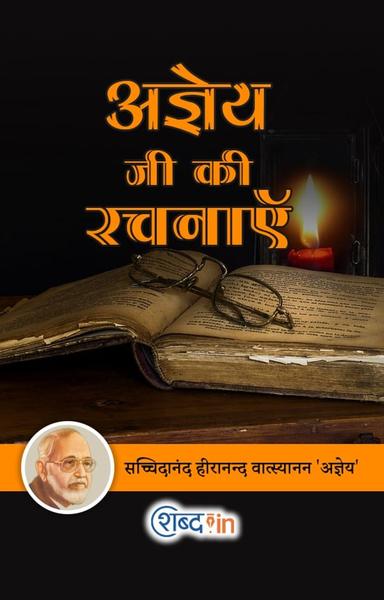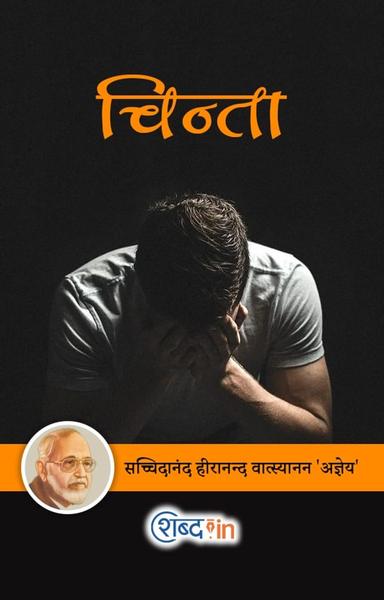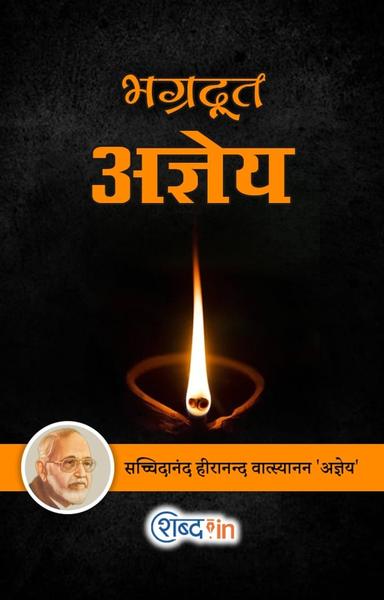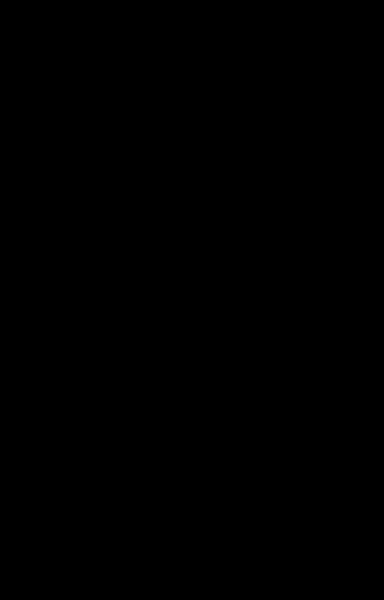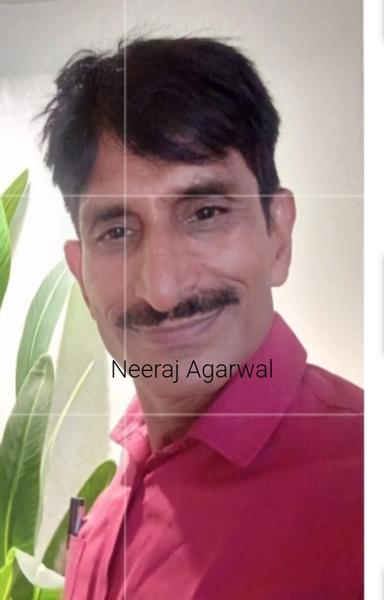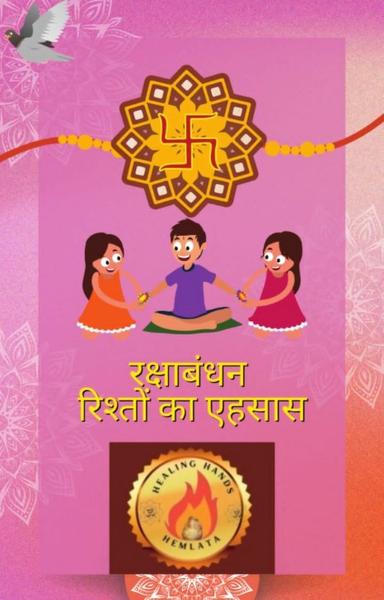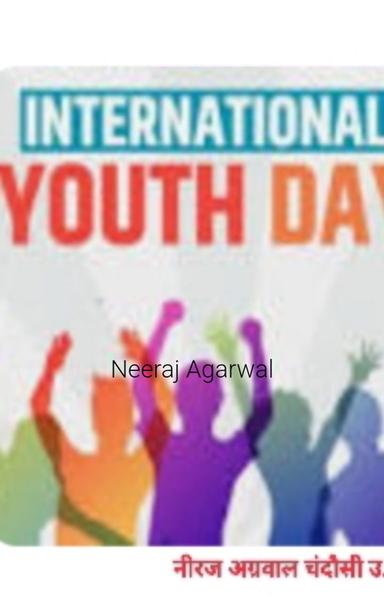एक का अनकहा संकल्प था
कि मुझे मार-मार कर दुम्बा बना देगा
दूसरे की ऐलानिया डींग थी कि मुझे बना लेगा
मार-मार कर हकीम
पर मैं हूँ कि कुछ न बना
न हकीम, न दुम्बा,
मार खाते-खाते-करूँ तसलीम
बन गया एक अजूबा
जिसे और नामों की कमी में
कहते हैं इनसान।
इनसान नाक, मुँह, आँख, कान,
कलेजा, और सब से अजब बात
यह कि खोपड़ी के भीतर
भेजा। अब मैं चाहूँ
(हाँ, एक तो यह कि अब मैं सिर्फ़ कराह नहीं, चाह भी सकता हूँ)
तो बैठ कर अपनी देह के ददोरे सहला सकता हूँ
या कुढ़, या किसी को कोस, या धर कर
झँझोड़ भी सकता हूँ
या नारे लगा सकता हूँ
या सिनेमाई प्रणय-गीत गा सकता हूँ
या सोच सकता हूँ
कि जो हुआ वह क्यों हुआ या जो होना चाहिए वह कैसे हो;
मैं चाहूँ तो कुछ कर सकता हूँ
चाहूँ तो इसी आनन्द में मगन हो जा सकता हूँ
कि मेरे आगे एकाएक कितने रास्ते खुल गये हैं
(मार से क्या मेरे बखिये-टाँके खुल गये हैं या कि मेरे पुराने पाप धुल गये हैं?)
चाहूँ तो बिना कुछ किये
खुशी से मर सकता हूँ।
सब से पहले तो यह बात
कि मैं अवध्य नहीं हूँ।
कोई भी हवा मुझे उखाड़ सकती है
कोई भी दाँव मुझे पछाड़ सकता है,
किसी भी खाई में मैं गिर सकता हूँ
किसी भी जाल में फँस, दलदल में धँस,
कुंज मे रम या गली-कूचे में बिलम सकता हूँ,
किसी भी ठोकर से औंधे मुँह गिर सकता हूँ।
अवध्य नहीं हूँ : एक दिन गच्चा खाऊँगा
और मारा जाऊँगा
(नहीं, होगा वह फिर भी बेमौत : शहादत का रुतबा नहीं पाऊँगा)
न मेला जुड़वाऊँगा, न ही बनूँगा किसी स्मारक-समिति के
लिए चन्दा-उगाही का वसीला,
या नगरपालिका के लिए नयी चुंगी का हीला।
तो क्यों न यहीं से हो शुरुआत?
दूसरे यह कि मुझ में
जीतने की कामना और संकल्प तो है
पर जीतने का गुर मुझे अभी नहीं मिला।
जीतना कैसे होता है यह मैं नहीं जानता।
और हारना मैं कभी नहीं चाहता, बिलकुल नहीं चाहता,
पर हारना चाहिए कैसे यह मैं जानता हूँ,
हारने का शील तो मुझे बपौती-ददौती में मिला है।
तो हार मानी नहीं जाती
और जीत पानी नहीं आती
क्यों न थोड़ी देर जम कर
हो जाय इसी की बात?
लेकिन क्या बात?
यही कि रोज़ मार खाता हूँ, पर मार से कुछ बनता नहीं,
क्यों कि मुझे मार खानी नहीं आती?
आता क्या है?
और मुझे कुछ आता नहीं तो किसी का जाता क्या है?
मैं जहाँ जो हूँ, उस स्थिति के लिए यह सब ‘दिया हुआ’ है।
जो करना होगा, उस की यह प्रतिज्ञा है।
और जो दिया हुआ है, उस पर जमना क्या,
थमना क्या?
जिस चट्टान से कूद पड़े वह चट्टान भी हुई तो अब
उस का सहारा क्या?
(हालाँकि वह चट्टान थी नहीं, धारा में डोलता हुआ
एक थम्भ-भर था)
‘दिया हुआ है’ इसी से तो छूट गया
चट्टान से नाता टूट गया।
सौ बात की बात यह कि किसी अनजाने सागर के ऊपर
अधर में हूँ :
और यह बात भी रूपक है
और मुझे झक है कि
कहूँगा खरी, रूखी, सब की पहचान में
आने वाली बेलाग बात;
सौटंच खरी, भले ही कच्ची धात।
यानी तीसरी यह बात
कि न मेरे पैरों के नीचे कोई पक्की भीत है
न मेरे साथ खड़ा कोई पक्का मीत है;
कि मैं एक दिन मरूँगा या मारा जाऊँगा
कि नन्ही-सी जान हूँ;
कि मैं बहुत कम जानता हूँ और बहुत कुछ
बेवजह मानता हूँ,
सिवा इसके कि यही नहीं मान पाता
कि मुझे कुछ नहीं आता,
कि ईश्वर-पुत्र हूँ, पर बड़े बाप का बेटा होने का
न लोभ करता हूँ, न लाभ उठा सकता हूँ
कि मानव-पुत्र हूँ, पर प्रजातन्त्र में इस दावे पर
हर दूसरा मानव-पुत्र हँसेगा कि क्या बकता हूँ!
उफ़्! कितने हैं कि सब समझते हैं
इस लिए किसी को कुछ समझते नहीं।
मैं वध्य हूँ, अकेला हूँ, बेसहारा हूँ
इनसान हूँ।
यानी जहाँ से चलोगे वहीं आ अटकोगे।
जो चक्कर खींचोगे उसी के भीतर खुद भटकोगे।
बचाव के लिए जो-जो दीवार उठाओगे उसी पर
सिर पटकोगे।
मैं, तुम, यह, वह, हम सब, सारा जहान
थेली का हर चट्टा, हर बट्टा-हर इनसान।
लेकिन यह सभी कुछ तो ‘दिया हुआ’ है
पहले से तय किया हुआ है
इसे दुहराना क्या, और इसी का रोना है
तो गाना क्या?
भाई मेरे, हमदम, मेरे हकीम, या निहायत हलीम मेरे गधे-
ईश्वर-पुत्र, मानव-पुत्र,
आओ, अगर यह तुम से सधे
तो इस ‘दिये हुए’ के सिर पर चढ़ कर ही
अपना नारा वरेंगे
जो अभी ‘पाया हुआ’ नहीं है
कि हम करेंगे या नहीं
करेंगे और मरेंगे
जाते-जाते भी मार खाते-खाते भी
कर गुज़रेंगे
करेंगे क्यों कि मरेंगे।