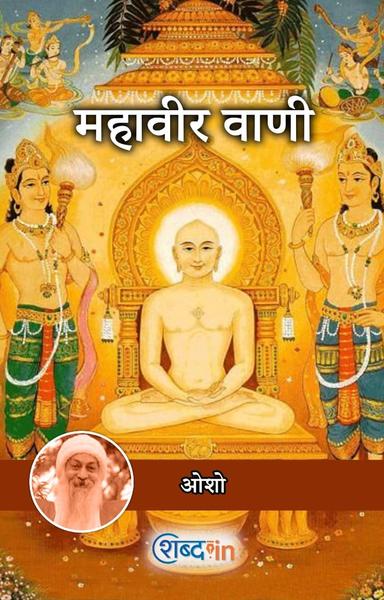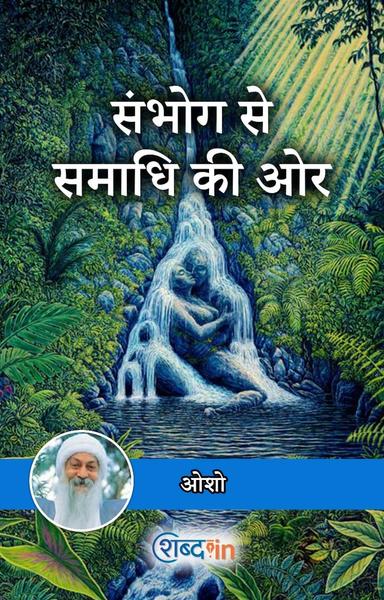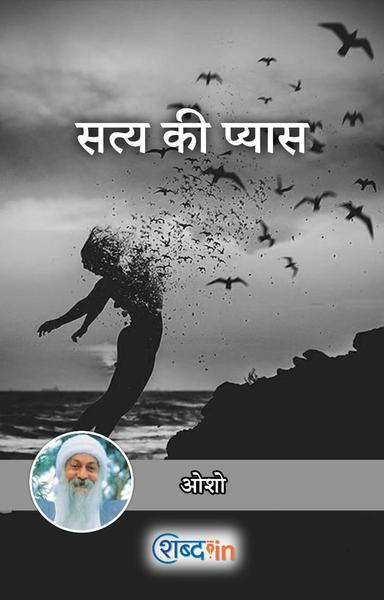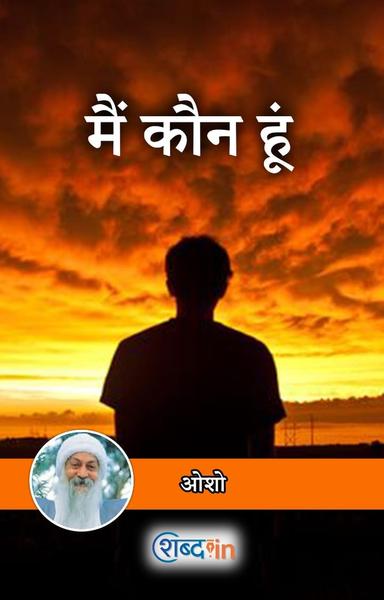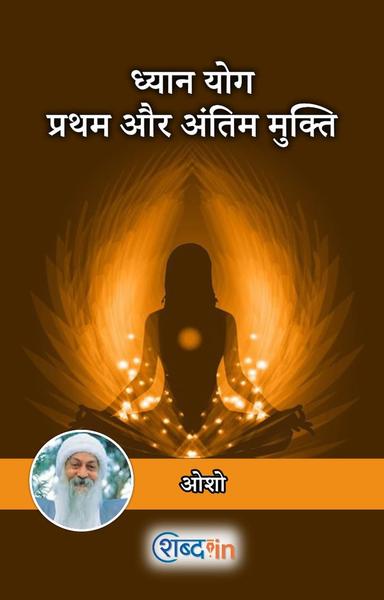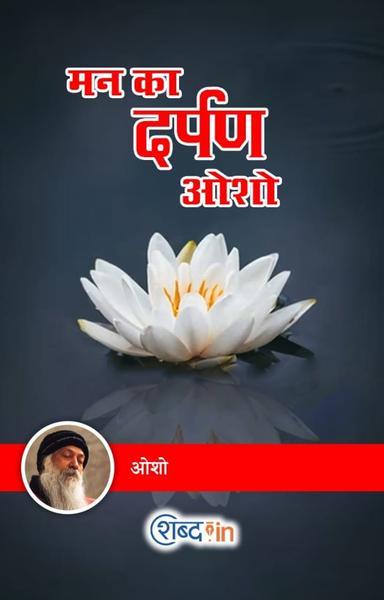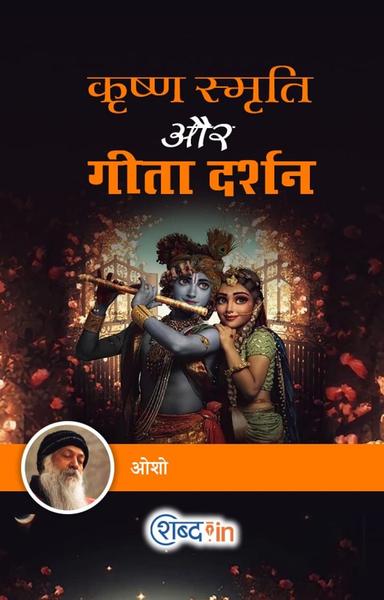प्रश्न-सार:
1—परमात्मा शब्द ही मेरी समझ में नहीं आता है। परमात्मा यानी क्या?
2—वैसे गत पंद्रह वर्षों से आप निरंतर प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, परंतु यहां आपके ऊर्जा-क्षेत्र में रहते हुए कुछ माह में ही कुछ-कुछ आश्चर्यचकित घटित होने लगा है। हमें इतने दिनों तक दूर क्यों रहना पड़ा, जब कि पहली ही पहचान में आपकी भगवत्ता स्पष्ट हो गई थी?
3—संत विरहावस्था की चर्चा बहुत करते हैं। यह विरह क्या बला है?
कभी ध्यान में मुझे लगता है कि मंजिल बहुत निकट है, सुबह होने को है।
कभी भीतर गहन अंधकार अनुभव होता है, तब बहुत पीड़ा होती है।
कभी आनंद, कभी पीड़ा; यह आंखमिचौनी प्रभु कब तक चलेगी?
पहला प्रश्न: परमात्मा शब्द ही मेरी समझ में नहीं आता है। परमात्मा यानी क्या?
स्वरूप! जो समझ में नहीं आता है, उसी का नाम परमात्मा है। जो समझ में आ जाता है, उसका नाम संसार। जो समझ में नहीं आता, वह भी है। समझ पर ही अस्तित्व की परिसमाप्ति नहीं है, समझ के पार भी अस्तित्व फैला हुआ है, इस बात की उदघोषणा ही परमात्मा है।
परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए जो परमात्मा को व्यक्ति मान कर खोजने चलेंगे, व्यर्थ ही भटकेंगे, कहीं न पहुंचेंगे। परमात्मा तो अज्ञात का नाम है। अज्ञात का ही नहीं वरन अज्ञेय का। जिसे जानो तो जान न पाओगे। जिसे जितना जानने की चेष्टा करोगे, उतना ही पाओगे कि अनजाना हो गया।
लेकिन फिर भी, एक और द्वार से परमात्मा में प्रवेश होता है–उस द्वार का नाम ही प्रेम है। जानने से नहीं जाना जाता, लेकिन प्रीति से जाना जाता है, प्रेम से जाना जाता है। जानना ही अगर जानने का एकमात्र ढंग होता, तो परमात्मा से संबंधित होने का कोई उपाय न था। लेकिन एक और ढंग भी है। बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे भीतर सब कुछ, हृदय का भी स्मरण करो। सोच-विचार ही सब कुछ नहीं है तुम्हारे भीतर, भाव की आर्द्रता को भी थोड़ा अनुभव करो। आंखें सिर्फ कंकड़-पत्थर ही नहीं देखती हैं, उनसे प्रीति के आंसू भी झरते हैं। अगर विचार पर ही ठहरे रहे तो परमात्मा नहीं है। इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं है, बल्कि इसलिए कि विचार की क्षमता नहीं है परमात्मा को जानना।
यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई आदमी आंख से संगीत सुनना चाहे। और फिर संगीत सुनाई न पड़े। और वह कहे कि आंख से जब तक सुनाई न पड़ेगा संगीत, मैं मानूंगा नहीं। तो क्या करेंगे हम? आंख से संगीत सुना नहीं जा सकता। उसकी जिद्द है कि आंख से सुनेगा। कान से सुना जा सकता है, उसकी जिद्द है कि कान खोलेगा नहीं।
प्रत्येक उपकरण की सीमा है। बुद्धि पदार्थ को जान सकती है, परमात्मा को नहीं। हृदय परमात्मा को जान सकता है, पदार्थ को नहीं। कान संगीत सुन सकते हैं, रोशनी नहीं देख सकते। आंखें रोशनी देख सकती हैं, संगीत नहीं सुन सकतीं। हाथ छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गंध का अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए तो नासापुटों की जरूरत होगी। प्रत्येक अनुभूति का अपना द्वार है। और प्रत्येक अनुभूति केवल अपने ही द्वार से उपलब्ध होती है।
तुम पूछते हो, स्वरूप: “परमात्मा शब्द मेरी समझ में नहीं आता।’
किसकी समझ में कब आया? किसी की समझ में कभी आया है? समझ से नाता ही नहीं है। यह तो नासमझों के लिए संभावना है। यह तो दीवानों का रास्ता है। यह तो मस्तों का मार्ग है। इसीलिए तो इतना कठिन है प्रेम का पंथ। प्रेम-पंथ ऐसो कठिन!
क्या कठिनाई है?
कठिनाई यही है कि इस जीवन का सब कुछ तो हम विचार से सुलझा लेते हैं। और इसलिए एक भ्रांति पैदा होती है कि जब विचार से सब सुलझ जाता है–गणित सुलझ जाता है, भाषा सुलझ जाती है, तर्क सुलझ जाता है, दर्शन सुलझ जाता है; भूगोल, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, सब बुद्धि से सुलझ जाता है–तो एक आशा बंधती है कि इसी बुद्धि से हम परमात्मा को भी सुलझा लें। और इसी आशा में उपद्रव हो जाता है। इसी आशा में हमारी निराशा के बीज हैं। इसी आशा में हमारी विफलता है। और स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक तुम्हें बुद्धि की ही शिक्षा दी जाती है। इस जगत में कहीं भी तो कोई स्थान नहीं है जहां हृदय का प्रशिक्षण होता हो। इसलिए मैं कहता हूं, यह जगत मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों से भरा है, फिर भी मंदिर इस जगत से समाप्त हो गए हैं। क्योंकि मंदिर है वह जगह, जहां हृदय का प्रशिक्षण मिलता हो।
तुम्हारे मंदिर भी बुद्धि से भर गए हैं। वे भी पाठशालाएं हैं। वहां धर्मशास्त्र समझाया जा रहा है। तुम्हारे मंदिर भी मस्तिष्क के ही आवास हो गए हैं। अब वहां हृदय नहीं नाचता, अब वहां प्रेम की बांसुरी नहीं बजती, अब तो वहां भी तर्क के जाल फैलाए जा रहे हैं। हिंदू है, वह मुसलमान के खंडन में लगा है; मुसलमान है, वह हिंदू के खंडन में लगा है। आर्यसमाजी सनातनी का खंडन कर रहा है, सनातनी आर्यसमाजी का खंडन कर रहा है। मंदिरों में भी खंडन-मंडन हो रहा है। प्रीति का फूल खिले तो खिले कहां? मस्जिदों में भी प्रेम की शराब नहीं ढाली जा रही है; वहां भी तर्क और तर्क के सहारे ही जितनी दूर तक जाया जा सकता है, उतनी दूर तक जाने की कोशिश की जा रही है।
तर्क तो ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में लकड़ी। थोड़ा टटोल लेता है। और अंधे के हाथ में लकड़ी थोड़े काम भी आती है। एकदम व्यर्थ है, ऐसा मैंने कहा भी नहीं, ऐसा मैं कहूंगा भी नहीं। उसकी अपनी सार्थकता है। अंधा आदमी है तो लकड़ी से टटोल कर अपने घर आ जाता है, दरवाजा खोज लेता है, अपने जूते तलाश कर लेता है, टकराता नहीं। मगर अंधे की लकड़ी उसकी आंख नहीं बनती; न आंख बन सकती है। और आंख अगर मिल जाए तो लकड़ी को तत्क्षण छोड़ देना होगा। फिर कौन चिंता करता है लकड़ी की?
इसलिए जिन्होंने हृदय को थोड़ा खुलने का अवसर दिया, हृदय की कली को फूल बनने दिया, उन्होंने फिर तर्क की बकवास छोड़ दी। फिर वे परमात्मा में जीने लगे। वे परमात्मा के लिए प्रमाण नहीं देते फिर, वे स्वयं परमात्मा के प्रमाण हो जाते हैं। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका न बोलना–सब परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है। उनका सारा जीवन परमात्मा का एक गीत हो जाता है। उनके जीवन से एक सुवास उठती है।
तुम्हारे जीवन से भी वैसी सुवास उठ सकती है। हकदार तुम भी हो। उतने ही मालिक हो तुम, जितना कोई बुद्ध, जितना कोई कृष्ण, जितना कोई क्राइस्ट। उतने ही मालिक हो तुम, जितने महावीर, जितने मोहम्मद, जितनी मीरा। तुम्हारी मालकियत जरा भी कम नहीं है। मगर अगर तुम दीवाल से निकलने की चेष्टा करोगे और न निकल पाओ, तो अपने भाग्य को कसूर मत देना। दरवाजा है तो दीवाल से निकलने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? क्यों दीवाल से सिर मार रहे हो? और सिर से जितने भी काम होते हैं, बस वे दीवाल से सिर मारने जैसे हैं।
तुम्हारे भीतर एक और भी अंतरंग जगत है। तुम्हारे भीतर भाव का भी एक लोक है। बहुत कोमल, बहुत नाजुक। और चूंकि कोमल है, नाजुक है, इसलिए बहुत छिपा कर रखा गया है। जितनी बहुमूल्य चीज होती है, उतना ही तो गहरा हम खोद कर जमीन में उसे गड़ा देते हैं कि चोरी न हो जाए। बुद्धि तो ऊपर-ऊपर है, क्योंकि कचरा है। हृदय बहुत गहरे में है, क्योंकि वही तुम्हारी संपदा है। वहीं तुम्हारी समाधि छिपी है। और वहीं तुम्हारे समाधान हैं। बुद्धि कामचलाऊ है; बाजारू है, सस्ती है। हृदय तुम्हारा जीवन का मूल आधार है।
समझा तो कोई भी नहीं परमात्मा को कभी; और न कोई कभी समझ सकेगा। जिस दिन परमात्मा समझ में आ जाएगा, उस दिन धर्म का अंत हो जाएगा। उस दिन धर्म की मृत्यु समझ लेना। उस दिन जल जाएंगी होलियां कुरानों की, गीताओं की, वेदों की। उस दिन कुछ नहीं सार रह जाएगा फिर धर्म में, जिस दिन परमात्मा समझ में आ जाएगा।
कार्ल माक्र्स कहता था कि मैं तब मानूंगा परमात्मा को, जब प्रयोगशाला में वह पकड़ा जाएगा। जब परखनली में प्रयोगशाला की परमात्मा को पकड़ कर और जांच-परख लेंगे। जब उसका विश्लेषण कर लेंगे। जब उसके भीतर झांक कर यंत्रों से देख लेंगे। जब सूक्ष्म यंत्रों की पकड़ और नापत्तौल में आ जाएगा। जिस दिन मापा जा सकेगा, तौला जा सकेगा; जिस दिन उसकी थाह ली जा सकेगी, गणित से, तर्क से, विज्ञान से, उस दिन मैं मानूंगा।
लेकिन अगर किसी दिन परमात्मा को तुमने पकड़ लिया प्रयोगशाला में और जांच-परख कर ली, उस दिन के बाद क्या परमात्मा बचेगा? फिर पूजा किसकी करोगे? परखनलियों में पकड़े गए परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती। प्रार्थना किसकी करोगे? प्रयोगशाला में सिद्ध हो गए परमात्मा से प्रार्थना निवेदन नहीं की जा सकती। वह तो तुम्हारा गुलाम हो गया, चाकर हो गया। जैसे बिजली बंधी है आज तुम्हारी गुलाम होकर और बत्ती जलाती है–बटन दबाओ, बत्ती जली; बटन दबाओ, बत्ती बुझी–ऐसा परमात्मा भी तुम्हारे हाथों में होगा। जब आज्ञा दो, तो कहेगा: जी हुजूर! हुकुम! जहां ले जाओ, जाएगा; जो करवाओ, करेगा। फिर तो परमात्मा से तुम बड़े हो जाओगे, जिस दिन तुम समझ लोगे उसे।
नहीं, परमात्मा विराट है, हमारी समझ बड़ी छोटी है। हमारी समझ है चम्मच जैसी और परमात्मा है सागर जैसा। और चम्मच से सागर को नापने बैठे हैं। छोटी सी बुद्धि है, विराट को समझने की चेष्टा चल रही है। देखते हो मूढ़ता? बुद्धि की मूढ़ता है यह। इतने छोटे से चम्मच से इतना बड़ा सागर तुम न नाप सकोगे। कोई नहीं नाप सका।
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सागर नहीं है, क्योंकि तुम नाप नहीं पाते। नापने की जरूरत नहीं है, सागर में डुबकी लो! नहाओ! सागर की लहरों पर तिरो! नौका छोड़ो सागर में! सागर की पुकार है अज्ञात की पुकार। और जितना-जितना तुम समझने लगोगे…और जब मैं समझने शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा अर्थ है: जितना-जितना तुम्हारा हृदय भावित होने लगेगा; जैसे-जैसे तुम्हारी भावना गहन होने लगेगी, भक्ति सघन होने लगेगी, वैसे-वैसे तुम पाओगे–और भी समझने को शेष है। जितना समझोगे, उतना ही ज्यादा समझने को शेष है। और जो पराकाष्ठा है ज्ञान की, वह जानते हो क्या है? पराकाष्ठा है ज्ञान की इस बात की उदघोषणा कि मैं अज्ञानी हूं और परमात्मा के समक्ष सदा अज्ञानी रहूंगा। क्योंकि परमात्मा अज्ञेय है।
इसलिए समझ तो तुम न पाओगे। लेकिन जी सकते हो।
मैं तुम्हें परमात्मा को जीने का रास्ता बता रहा हूं–समझने का रास्ता नहीं। मैं कोई पंडित नहीं हूं, कोई उपदेशक नहीं हूं, कोई दार्शनिक नहीं हूं। शास्त्रों से मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। शास्त्रों का मुझे कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं, वह निज की भावना का निवेदन कर रहा हूं। बुद्धि से मैंने भी परमात्मा को पाना चाहा था, नहीं पा सका। बहुत बुद्धि लगाई! जितनी बुद्धि लगाई उतना मैं नास्तिक होता गया। फिर एक दिन यह व्यर्थता दिखाई पड़ी कि बुद्धि जितनी सघनता से प्रयोग करो, उतनी ही नास्तिकता गहन होती जा रही है। तो जरूर मैं कुछ गलत रास्ते पर चल रहा हूं।
अगर सूरज की तरफ चलेंगे तो आंखों में रोशनी बढ़नी चाहिए। अगर सूरज की तरफ पीठ करके चलेंगे तो अंधेरा बढ़ता जाएगा। अगर बगीचे की तरफ चलेंगे तो हवाएं सुगंधित होने लगेंगी, शीतल होने लगेंगी। अगर पीठ करके चलेंगे तो हवाओं में जो सुगंध थी वह भी खो जाएगी, जो शीतलता थी वह भी खो जाएगी।
जल्दी ही यह बात मुझे समझ में आनी शुरू हो गई कि जितना ही मैंने विचारा है, जितना ही सोचा है, उतना ही परमात्मा मुश्किल हो गया–मानना ही मुश्किल हो गया; जानना तो दूर, स्वीकार करना मुश्किल हो गया।
और मैंने परिपूर्णता से चेष्टा की थी!
विश्वविद्यालय से मुझे निकाल दिया गया था, क्योंकि कोई अध्यापक मुझे अपनी कक्षा में लेने को तैयार नहीं था। अध्यापक कहने लगे कि इतना ज्यादा तर्क, इतना ज्यादा विवाद, कि पढ़ना-लिखना तो कुछ हो ही नहीं पाता। हर चीज पर विवाद है। और उनकी भी तकलीफ मैं समझता हूं। और हर चीज पर विवाद किया जा सकता है। और विवाद से ही मैं खोजने चला था सत्य को।
जितना-जितना मैंने विचार और तर्क से सोचना चाहा, उतना ही पाया कि कोई उपाय नहीं है। एक नकारात्मकता गहन होती चली गई। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, लोग रास्ता काट जाते थे। क्योंकि मुझसे बात करने का अर्थ था कि उनकी सारी मान्यताएं, उनकी सारी धारणाएं गलत हैं। लेकिन एक बात मुझे जल्दी ही समझ में आने लगी कि ईश्वर हो या न हो, लेकिन ईश्वर को इनकार करके मैं अपने जीवन को पंगु किए ले रहा हूं। मेरा जीवन संकुचित होता जा रहा है।
नकार से कोई जी नहीं सकता। इनकार में कैसे जीओगे? “नहीं’ में जगह ही नहीं है जीने लायक। जीवन तो “हां’ में होता है, स्वीकार में होता है। हर चीज को “नहीं’ करते जाओगे तो सिकुड़ते जाओगे। परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, तो फिर बचेगा क्या? जो सबको इनकार करेगा, उसको अंततः अपने को भी इनकार करना पड़ेगा–तर्क की वह पराकाष्ठा है। जो तर्क की तलवार से खेलेगा, एक न एक दिन उसे अपनी गर्दन भी काट ही लेनी होगी। उसके संदेह बढ़ते चले जाएंगे। और जितने संदेह होंगे, उतना ही जीवन मुश्किल हो जाएगा। एक-एक कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा।
जीने के लिए तो श्रद्धा चाहिए। अश्रद्धा से कोई भी नहीं जी सकता। जिसको तुम नास्तिक कहते हो, वह भी जीता है श्रद्धा से। सिर्फ उसकी श्रद्धा उलटी है, शीर्षासन करती हुई है। वह भी असली नास्तिक नहीं है। उसकी श्रद्धा है कि ईश्वर नहीं है। इसी श्रद्धा से वह जीता है। नास्तिकता उसका धर्म है। क्रेमलिन उसका काबा है। दास कैपिटल उसकी कुरान, बाइबिल, वेद है। कार्ल माक्र्स, लेनिन, स्टैलिन, माओ, ये उसके ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। नास्तिकता नास्तिकता नहीं है उसकी।
कम्युनिस्ट अपने कम्युनिज्म के लिए मरने को तैयार है उतना ही जितना मुसलमान इस्लाम के लिए मरने को तैयार है। भेद कहां है? दास कैपिटल के लिए वह अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। किताब के लिए! न कोई ईश्वर है, न कोई आत्मा है; अकेली किताब के लिए, सिद्धांत के लिए! उसने नास्तिकता में से धर्म निकाल लिया। नास्तिकता उसकी आस्तिकता बन गई है। कहता है, “नहीं’, लेकिन भीतर “हां’ छिपा है।
मेरा “नहीं’ पूरा-पूरा “नहीं’ था। उसमें कहीं कोई “हां’ नहीं था।
और इसलिए मैं कहता हूं, जो अगर हिम्मत रखते हो परम नास्तिक होने की तो घबड़ाना मत। लेकिन परम नास्तिकता का अर्थ है कि नास्तिकता में भी सहारा मत खोजना। सब सहारे ही गिरा देना। इतने बेसहारे हो जाओगे कि उसी बेसहारे में तुम्हें पहली दफा याद आएगी कि यह मैंने क्या किया? यह तो मैंने अपने ही हाथ से अपने जीवन की नौका में छेद कर डाले! अब यह नौका डूबने लगी। उसी असहाय अवस्था में तुम्हारे भीतर क्रांति की घटना घट सकती है–कि मस्तिष्क से हृदय की याद आए! कि मेरे पास एक और भी उपाय है: प्रीति का, प्रेम का, भाव का। चलूं उससे भी तलाश लूं! मरता क्या न करता! तिनके का सहारा भी खोज लेता है, खयाल रखना।
तो जब तुम्हारी बुद्धि बिलकुल असफल हो जाए और तुम्हें गहन अमावस में डाल जाए और सब तरफ गहन अंधकार हो कि एक रात में तारा भी न चमके। सुबह की तो बात ही नहीं। सूरज तो है ही नहीं तो ऊगेगा कैसे! प्रभात तो होने वाली नहीं है। जब ऐसी गहन अंधेरी रात हो, तारा भी न चमकता हो, सूरज का भी भरोसा न हो, रोशनी होती है यह भी श्रद्धा न रह गई हो, उस गहन अंधेरी रात में तिनके का सहारा शुरू होगा। उस गहन अंधेरी रात में तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि एक अंग मेरा अनजीया रहा है। विचार तो मैंने खूब किया, भाव मैंने बिलकुल नहीं किया। तो थोड़ा भाव भी करके देख लूं! मरता क्या न करता! इस दरवाजे से कभी नहीं निकला, इससे भी निकल कर देख लूं। कौन जाने, शायद यही द्वार हो!
और जिस दिन मैं उस दरवाजे से निकला, मैंने देखा कि परमात्मा ही परमात्मा है। पहले मैं पूछता था, परमात्मा कहां है? फिर पूछने लगा कि परमात्मा कहां नहीं है?
स्वरूप, तुम पूछते हो: “परमात्मा यानी क्या?’
परमात्मा यानी हृदय। परमात्मा यानी भाव। परमात्मा यानी प्रीति।
तुमको समझ न पाया!
प्यासा अंतर जग के विस्तृत
मरु में भटक-भटक कर हारा,
तुम्हें समझने के प्रयत्न में
बिता दिया निज जीवन सारा!
पर तुम बने रहे जीवन भर मृगतृष्णा की छाया!
तुमको समझ न पाया!
तुम हो मन के मीत, कहा
व्याकुल विह्वल मानस ने मेरे,
तुम्हें प्राप्त करने के हित
पूजे मानव-पत्थर बहुतेरे!
तुमने किस पर्दे के पीछे निज संसार बसाया!
तुमको समझ न पाया!
या तो तुम मुझमें अपने में
भेद-भाव-आभास मिटा दो,
या मेरे मन का अपने प्रति
तुम समूल विश्वास मिटा दो।
मैं जीवन भर जग की भूल-भुलैया में भरमाया!
तुमको समझ न पाया!
समझ उपाय नहीं। दीवानगी! कहो नासमझी! ज्ञान मार्ग नहीं, कहो अज्ञान, निर्दोष भाव! छोटे बच्चे की भांति आश्चर्य-विमुग्ध होकर देखोगे, तो परमात्मा है। तर्क-विक्षुब्ध होकर देखोगे, परमात्मा नहीं है। तर्क का चश्मा चढ़ाया कि परमात्मा एकदम विदा हो जाता है संसार से। तर्क का चश्मा उतारो, प्रीति की जरा आंख खोलो और तुम पाओगे: चारों तरफ वही-वही!
रवींद्रनाथ ने गीतांजलि लिखी। उस अदभुत गीत-संग्रह पर उन्हें नोबल प्राइज मिली। बड़ा सम्मान हुआ। पहले जो लोग गाली देते थे, उन्होंने भी सम्मान किया। रवींद्रनाथ के बड़े विरोधी थे बंगाल में। कुछ आदमी अजीब ही है! रवींद्रनाथ ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, मगर बड़े विरोधी थे!र् ईष्या, जलन, हजार उपद्रव खड़े होते। लेकिन नोबल प्राइज मिलते ही बड़े सम्मान होने लगे। जगह-जगह समारोह, आयोजन, फूलमालाएं।
लेकिन एक आदमी रवींद्रनाथ के पड़ोस में रहता था, एक बूढ़ा आदमी। उसने नहीं किया सम्मान। वह तो एक दिन आया–उससे रवींद्रनाथ थोड़े डरते भी थे; उसकी आंखों में कुछ ऐसा था; वह ऐसे देखता था जैसे कि आंख कटार हो, कि भीतर तक भेद जाए; उस आदमी में कुछ बात थी–उसने आकर फिर रवींद्रनाथ की आंखों में देखा और कहा, कुछ नहीं, सब बकवास है! तुमने ईश्वर देखा है? चले ईश्वर की बात करने! मिल गई नोबल प्राइज!…क्योंकि गीतांजलि तो ईश्वर के गीत हैं, और बड़े प्यारे गीत हैं!…तुमने देखा है ईश्वर?
रवींद्रनाथ ऐसे व्यक्ति भी न थे कि झूठ बोलें। इसलिए यह भी नहीं कह सकते थे–देखा है। और उस आदमी की आंखों को धोखा देना था भी मुश्किल। वह यह कह कर चला गया कि पहले देखो, फिर लिखना ये गीत! जब देखोगे, तब मैं स्वीकार करूंगा। गीत-वीत लिखने से कुछ भी नहीं होता। यह तो कोई भी लिख लेता है। हां, तुम अच्छे कवि हो, मगर अभी ऋषि नहीं हो। भूल मत जाना! ये सम्मान, समारोह, ये फूलमालाएं, यह जगह-जगह आदर-सत्कार…भूल मत जाना! याद दिलाने आता रहूंगा।
और वह याद दिलाने आता था। वह याद कोई अच्छी नहीं दिलाता था, रवींद्रनाथ को बुरा लगता था। रास्ते पर मिल जाता तो हाथ पकड़ कर बीच रास्ते पर याद दिला देता था–भूल मत जाना! फूलमालाओं में बहुत भूल गए हैं। देख कर ही रहना! देखो, तब मानूंगा।
उससे रवींद्रनाथ बचने लगे। कहीं जाना होता तो दूसरे रास्ते से जाते, ताकि उसका घर न पड़े। वह आता घर तो इनकार करवा देते कि घर पर नहीं हैं।
फिर एक दिन सुबह एक घटना घटी। रात वर्षा हुई थी। और जगह-जगह रास्ते के किनारे पानी के डबरे भर गए थे। और सुबह-सुबह रवींद्रनाथ सागर की तरफ घूमने गए। सागर में सूरज को ऊगते देखा। बड़ा सुंदर प्रभात था। सुबह का सन्नाटा, सागर की नमकीन हवा, रात भर की नींद की ताजगी, पक्षियों का उड़ना, सूरज का ऊगना–एक क्षण को रवींद्रनाथ स्तब्ध बंधे रह गए। उस घड़ी में विचार सरक गए, बुद्धि सरक गई। उस घड़ी में हृदय से कुछ नाता बना। उस घड?ी में सूरज ने जैसे हृदय को छू लिया। जैसे सूरज की किरणों ने हृदय के साथ छेड़खान कर दी। थोड़ा रंग भीतर छिटक गया। आनंदमग्न लौटते थे, कि वही सूरज रास्ते के किनारे भरे डबरों में भी दिखाई पड़ा; और जब-जब जहां-जहां डबरों में सूरज दिखाई पड़ा, फिर-फिर वही भनक, फिर-फिर वही मस्ती आ गई, बार-बार आती रही।
और तभी अचानक वह आदमी रास्ते पर मिल गया। आज उस आदमी को देख कर मन में कोई विरोध नहीं उठा, तिरस्कार नहीं उठा, बचने का भाव नहीं उठा। खुद पर भरोसा न आया! भाव उठा उसे आलिंगन में लगा लेने का। और जाकर उस आदमी को गले लगा लिया। और वह बूढ़ा मुस्कुराया, रवींद्रनाथ की आंखों में देखा और कहा कि अब मुझे स्वीकार है। आज कुछ हुआ। आज तुम्हारे भाव आंदोलित हुए हैं। आज तुम्हारी हृदयतंत्री बजी है। स्वागत! धन्यवाद! मैं इस दिन की प्रतीक्षा में था। वह जो तुमने गीतांजलि लिखी है, सब बुद्धि का ही विलास है। मगर आज कुछ हुआ। आज तुम्हारा रंग और, ढंग और। आज तुम्हारी गंध और। आज तुम्हारी तरंग और।
और रवींद्रनाथ ने कहा है कि नोबल प्राइज पाकर मुझे जो आनंद न मिला था, उस दिन उस आदमी की इस बात से मुझे आनंद मिला। उसकी आंखों ने मेरे ऊपर अमृत की वर्षा कर दी।
बुद्धि से ही जीओगे, तो प्रश्न उठता रहेगा–परमात्मा यानी क्या? और उत्तर कभी न पाओगे। बुद्धि के पास कोई उत्तर नहीं है। स्मरण रहे, बुद्धि केवल प्रश्न उठाने में कुशल है, उत्तर देने में बिलकुल नपुंसक है। प्रश्नों में बड़ी निष्णात। और अगर किसी प्रश्न का उत्तर दो, तो उस उत्तर में से भी दस प्रश्न निकाल लेने में कुशल है। बुद्धि की सारी कुशलता प्रश्नों को बढ़ाने की है, उलझाने की है, सुलझाने की उसकी क्षमता नहीं है। हृदय की क्षमता बिलकुल और है। प्रश्न जानता ही नहीं हृदय, उत्तर ही जानता है।
यह बड़े मजे की बात है! बुद्धि में प्रश्न ही प्रश्न और हृदय में उत्तर ही उत्तर। अगर उत्तर चाहते हो, हृदय में डुबकी मारो। अगर प्रश्नों में ही मजा है, तो बुद्धि में अटके रहो, उलझे रहो। अगर दर्शनशास्त्र में तुम्हारी रुचि हो, तो पूछते रहो बुद्धि में ही; दर्शनशास्त्र बढ़ता रहेगा। पुच्छल तारे की तरह उसकी पूंछ है। बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए, समाधि चाहिए, तो बुद्धि से थोड़े हटो, थोड़ी छलांग लो, भाव के जगत में प्रवेश करो। नाचो, गाओ, गुनगुनाओ। इतना प्यारा जगत है, इसके साथ थोड़ा तारतम्य बनाओ। इतना अपूर्व सौंदर्य बरस रहा है चारों तरफ, इस सौंदर्य में नहाओ! चांदत्तारों से गुफ्तगू करो। शास्त्रों में मत तलाशो। वहां क्या मिलेगा? कागज हैं, स्याही के धब्बे हैं कागजों पर। आकाश ज्योतिर्मय तारों से भरा है, तुम अपनी किताबों में खोजने में लगे हो? परमात्मा जगह-जगह सघन होकर मौजूद है–वृक्ष में वृक्ष होकर, चट्टान में चट्टान होकर, मनुष्य में मनुष्य होकर। ये सब उसके ही रूप हैं। मगर बुद्धि नहीं इनको पहचान पाएगी। चलो, थोड़ा प्रीति में खोजें। चलो, थोड़ा दूसरा द्वार टटोलें।
यही भेद है दर्शनशास्त्र और धर्म का।
दर्शनशास्त्र बुद्धि का ऊहापोह है और धर्म हृदय में डुबकी है। मिलेगा, मन का मीत जरूर मिलेगा। तुम्हारे भीतर छिपा है, मिलेगा क्यों नहीं? चूकते कैसे हो, यही चमत्कार है! चूकते कैसे हो? जिस दिन जानोगे, उस दिन भरोसा भी न आएगा कि कैसे इतने दिन चूका–कैसे?
लेकिन चट्टान की तरह तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे हृदय में एक दीवाल उठ गई है। मैं तुमसे कहूंगा: शास्त्र की जगह संगीत; ताकि चट्टान टूटे। गद्य की जगह पद्य; ताकि चट्टान टूटे। तर्क की जगह प्रीति; ताकि चट्टान टूटे।
होशियारी छोड़ो! परमात्मा के सामने होशियार होकर जाना चाहते हो? होशियारी परदा है। नादान बनो। नादान बनने का अपना मजा है। उसके पास ऐसे चलो जैसे छोटा सा बच्चा अपनी मां को पुकार उठता है। ऐसे उसे पुकारो। और अगर तुम्हारी पुकार में तुम्हारी प्यास होगी, और तुम्हारी पुकार में तुम्हारे आंसू होंगे, और तुम्हारी पुकार में तुम्हारी अभीप्सा होगी, तो तत्क्षण पुकार पूरी होती है।
दूसरा प्रश्न: वैसे गत पंद्रह वर्षों से आप निरंतर प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, परंतु यहां आपके ऊर्जा-क्षेत्र में रहते हुए कुछ माह में ही कुछ-कुछ आश्चर्यचकित घटित होने लगा है। मेरी गति तो बहुत ही धीमी है, परंतु कृष्णा को जो नित नये चमत्कार घट रहे हैं, उन पर हर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें इतने दिनों तक दूर क्यों रहना पड़ा, जब कि पहली ही पहचान में आपकी भगवत्ता स्पष्ट हो गई थी?
अद्वैत बोधिसत्व! वसंत का पहला फूल खिलता है तो यह मत समझ लेना कि वसंत आ गया। वसंत का पहला फूल सिर्फ खबर लाता है कि वसंत आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है…। अब आया, अब आया, अब आया…। वसंत का पहला फूल तो केवल उदघोषणा है। फिर आते-आते वसंत आएगा। वर्षा के पहले मेघ घिरे, इससे वर्षा नहीं आ गई। लेकिन अषाढ़ के पहले मेघ खबर ले आए कि अब देर नहीं। अब जल्दी ही आते होंगे वर्षा के मेघ। अब जल्दी ही आकाश मेघों से भर जाएगा और खूब वर्षा होगी और पृथ्वी के उत्तप्त प्राण, प्यासे प्राण तृप्त होंगे। कि फिर वृक्ष हरे होंगे। कि फिर पहाड़ों पर नदियों के जल-स्रोत जीवंत हो उठेंगे। कि फिर झरने बहेंगे।
पंद्रह वर्ष कोई लंबा समय नहीं है। पंद्रह वर्ष पहले तुम मिले थे। और तुम कहते हो कि आपकी भगवत्ता का तभी स्पष्टीकरण हो गया था।
पहला फूल खिला था। आज तुम्हें लगता है कि तभी स्पष्टीकरण हो गया था। तब स्पष्टीकरण नहीं हुआ था। पहला फूल खिला था। भनक पड़ी थी। कान में पहली आवाज आई थी। और बड़ी दूर की आवाज थी। और ऐसी अपरिचित थी, अनजानी थी कि तब पहचानना संभव भी नहीं था। जिसके जीवन में वसंत आया ही न हो, वह पहले फूल को देख कर भी, वसंत आ रहा है, इसका भरोसा न कर सकेगा। हां, जब वसंत आ जाएगा, तब लौट कर देखेगा तो उसे याद आएगा कि अरे, जब पहला फूल आया था, तभी क्यों न मैं झुक गया! तभी तो वसंत आ चुका था! मैंने इतनी देर क्यों लगाई? तब तड़फेगा।
ऐसा ही, बोधिसत्व, तुम्हारे साथ भी हुआ। मुझे तुम्हारी आंखों का पता है, कि पहला फूल तुम्हें दिखाई पड़ा था। तुम पंद्रह वर्षों से निरंतर मुझसे जुड़ते ही गए हो। रोज-रोज जुड़ते गए हो। रोज-रोज और-और फूल खिलते गए हैं। लेकिन ये बातें गहरी हैं, और पंद्रह वर्ष कुछ भी नहीं–पंद्रह जन्म भी कुछ नहीं। जल्दी ही तुम आ गए! तुमसे पहले भी जिन्होंने फूल देखा था, वे भी अभी नहीं आ पाए हैं। कई तो जिन्होंने फूल देख लिया था, फूल देख कर भी और दूर चले गए हैं। तुम सौभाग्यशाली हो! तुम दूर नहीं गए, तुम निरंतर पास ही आते गए हो।
और तुमने साहस किया है। बोधिसत्व राजस्थान में न्यायाधीश के बड़े पद पर हैं। छोड़-छाड़ दिया सब। छोड़ने में जरा भी झिझक नहीं ली है। तुम्हें तो घूंट लग गया शराब का! और तब चमत्कार होंगे। इतनी तैयारी हो, तो चमत्कार क्यों न होंगे?
तुम कहते हो कि कुछ-कुछ आश्चर्यचकित घटित हो रहा है।
बहुत कुछ होगा। अभी तो शुरुआत है, आगे-आगे देखिए…। भरोसा नहीं आएगा। क्योंकि भरोसा जिस बुद्धि को आता है, यह अब उस बुद्धि के बस के बाहर की बात है जो होना शुरू हो रही है। अब यह हृदय अपनी मालकियत की घोषणा कर रहा है। अब ये तरंगें, यह आनंदभाव, ये चमत्कृत कर देने वाली अनुभूतियां हृदय से उठ रही हैं। बुद्धि तो भौंचक्की रह जाएगी। और अगर तुम किसी से कहोगे, तो स्वभावतः लोग समझेंगे पागल हो गए हो। कहना भी मत!
ये तो पागलों की बातें हैं, बस पागलों से कहना। हां, चार दीवाने मिल जाएं तो जरूर इनकी चर्चा करना। जरूर इनकी चर्चा का लाभ है। लेकिन हर किसी से मत कहना। हर किसी से कहोगे, तो भीड़ तो समझदारों की है, वे समझदार सब कहेंगे–तुम पागल हो गए हो। और तुम्हारी बुद्धि अभी भी मर नहीं गई है, जिंदा है। हृदय उठना शुरू हुआ है, मगर बुद्धि मर नहीं गई है। जन्मों-जन्मों की बुद्धि ऐसी आसानी से मर नहीं जाती। और वे जो सैकड़ों लोग हैं, समझदार, वे तुम्हारी बुद्धि को अभी भी राजी कर सकते हैं, तुममें भी शक पैदा कर सकते हैं कि पता नहीं, कहीं मैं ही तो भूल में नहीं हूं!
इसलिए एक बात खयाल रहे। संन्यासियों को जब कुछ चमत्कृत करने वाली बातें घटने लगें, कुछ ऐसे अनुभव आने लगें जो बुद्धि की क्षमता के बाहर हैं, तो उनकी बात जहां तक बने करना मत। लेकिन मैं जानता हूं कि बड़ी आकांक्षा उत्पन्न होती है कि किसी से कहें, हलके हो लें। जैसे फूल जब गंध से भर जाता है तो गंध को लुटाता है। ऐसे ही जब तुम्हारे प्राणों में कुछ भाव उठेंगे तो तुम भी चाहोगे। इसीलिए तो संन्यास को जन्म दिया है।
लोग मुझसे पूछते हैं, संन्यास की क्या जरूरत?
उसकी जरूरत बहुत है। बड़ी से बड़ी जरूरत तो यह है कि जब एक के भीतर कुछ भाव घटने लगे, तो उसे कुछ लोग तो मिल जाएं कहीं जो उसके भाव को समझेंगे, समादर करेंगे, श्रद्धा करेंगे। जो उसके भाव को बढ़ाएंगे, सींचेंगे, सहारा देंगे। जो कहेंगे, ठीक हो रहा है। ऐसा ही तो हमें भी हुआ है। ऐसा ही तो हमें भी हो रहा है। जो कहेंगे कि तुम धन्यभागी हो! इसी की तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही फूल तो हम भी चाहते हैं कि खिलें। यही रोशनी तो हम भी तलाश रहे हैं। तुम आगे निकल गए, हमें भी हाथ का सहारा दो। हमें भी खींच लो। ऐसे लोगों की जमात पैदा करने के लिए ही संन्यास है।
और तुम कहते हो, बोधिसत्व, कि मेरी गति तो बहुत धीमी है, परंतु मेरी पत्नी कृष्णा को नित नये चमत्कार घट रहे हैं।
तुम्हारी गति थोड़ी धीमी होगी–न्यायाधीश रहे हो! एकदम से इतनी बड़ी छलांग तुमने ली है। बड़ा साहस किया है। दुस्साहस किया है। लेकिन एकदम न्यायाधीश चला नहीं जाएगा। वह छिपा कोने में बैठा देख रहा होगा कि क्या ठीक है, क्या गलत है। कौन सा अनुभव मानने योग्य है, कौन सा अनुभव केवल सपना है। कौन सा अनुभव सम्मोहन है, कौन सा अनुभव मन की कल्पना है, कौन सा अनुभव वास्तविक है। वह न्यायाधीश बैठा है अपनी कसौटी लिए। जैसे सुनार अपनी कसौटी लिए बैठा रहता है, सोना कसता रहता है। मगर सोना कसना तो ठीक है, फूल मत कसने लगना सोने की कसौटी पर। जरा अपने भीतर बैठे सुनार से सावधान रहना!
कृष्णा इससे लाभ में है। तुम्हारी पत्नी न्यायाधीश नहीं है। और न्यायाधीश की पत्नी है, इसलिए न्यायाधीश होने से तो वह बिलकुल ऊब ही गई होगी। उतना उसका लाभ है।
फिर कृष्णा स्त्री है, तुम पुरुष हो। पुरुष का सहज झुकाव बुद्धि की ओर होता है। स्त्री का सहज झुकाव भाव की ओर होता है। कृष्णा दीवानी है, आती भी है मीरा के जगत से। सच तो यह है कि कृष्णा ही धीरे-धीरे करके तुम्हें यहां खींच लाई है। हालांकि उसने सीधा-सीधा तुमसे कभी कुछ कहा नहीं है। यहां बहुत से पुरुष हैं, जिनको उनकी पत्नियां धीरे-धीरे करके खींच लाई हैं, फुसला लाई हैं। उसने कभी प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें यहां लाने की चेष्टा नहीं की है। लेकिन उसमें जो रूपांतरण होते रहे हैं, उसकी जो मस्ती बढ़ती चली गई है, उसके जो अनुभव गहरे होते चले गए हैं, वे तुम्हारे लिए प्रमाण बनते चले गए हैं। तुम्हें कृष्णा के प्रति आभारी भी होना चाहिए। ऐसी पत्नी पाना धन्यभाग है। वह तुम्हें ठीक मंदिर में ले आई है। शायद अपने से तुम आ भी न सकते। शायद अपने से तुम्हें आने में हजार झंझटें आतीं। लेकिन तुम्हारा प्रेम उसके प्रति इतना है कि तुम उसके प्रेम में बंधे चले आए हो। और उसका प्रेम मेरे प्रति इतना है कि उसे आना ही था।
तुम्हारे प्रेम में भी मेरे प्रति कोई कमी नहीं है। तुम्हारा प्रेम भी गहन है। लेकिन पुरुष के प्रेम में विचार की छाया पड़ती ही रहती है। वह सोच-विचार करता ही रहता है।
इसलिए चैतन्य भी नाचे–और खूब नाचे–मगर फिर भी कुछ बात है जो मीरा की है और चैतन्य में नहीं है। चैतन्य नाचते हैं तो कुछ अजीब सा लगता है। मृदंग भी बजाते हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है। मीरा के लिए नाचना बिलकुल स्वाभाविक मालूम होता है। नाचती न तो और क्या करती! महावीर नाचते तो जरा अड़चन तो मालूम होती। वैसी ही चैतन्य के साथ मालूम होती है। महावीर तो वह जो मौन खड़े हो गए, उसमें ही बिलकुल स्वाभाविक मालूम होते हैं।
फिर, बोधिसत्व, जैन परिवार से आते हो तुम। पुरुष, न्यायाधीश, जैन परिवार! न मालूम कितनी चट्टानें थीं, जिनको तोड़ कर तुम मेरे पास तक आ गए हो। क्योंकि जैन-विचार में भाव की कोई ज्यादा जगह नहीं है। प्रार्थना का कोई उपाय नहीं है। भक्ति की कोई संभावना नहीं है। जैन-विचार तो शुष्क, तार्किक, गणित है।
मुझसे अनेक बार लोग कहते हैं कि आप जैन-शास्त्रों पर क्यों नहीं बोलते?
अदभुत शास्त्र हैं! मगर बोलने योग्य नहीं। उनमें रसधार नहीं है। सूखे-साखे हैं। अब मरुस्थलों पर बोलो भी तो क्या बोलो? अपूर्व शास्त्र हैं! जैसे कुंदकुंद का समयसार है। कई बार न मालूम कितने जैन मुझसे आकर कहे हैं: कुंदकुंद पर बोलें। उनकी बात मान कर मैं कभी-कभी कुंदकुंद की किताब उठा कर उलटता-पलटता भी हूं। फिर बंद करके रख देता हूं। क्योंकि गणित ही गणित है, तर्क ही तर्क है, विचार ही विचार है। भाव का कहीं कोई दूर का भी नाता नहीं है। हृदय से बहुत संबंध नहीं है।
इसलिए जैन-विचार इस देश में पनप नहीं सका। सिकुड़ गया। और जो जैन हैं भी, वे भी नाममात्र को ही जैन हैं। क्योंकि गणित से धर्म का कोई संबंध जुड़ नहीं सकता। कभी एकाध का जुड़ जाए–कोई अलबर्ट आइंस्टीन जैसा आदमी गणित के द्वारा भी धार्मिक हो सकता है। और महावीर अलबर्ट आइंस्टीन जैसे आदमी ही रहे होंगे। अलबर्ट आइंस्टीन और महावीर के विचार में तारतम्य भी बहुत है।
तुम यह जान कर हैरान होओगे, महावीर पहले प्रस्तोता थे सापेक्षवाद के। और उसी सापेक्षवाद का अंतिम प्रस्तोता था आइंस्टीन। थियरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको आइंस्टीन ने कहा है, सापेक्षवाद का सिद्धांत, उसी को महावीर ने स्यातवाद कहा है, सप्तभंगि न्याय कहा है। वह महावीर के समय की भाषा है। बस भाषा का भेद है। मगर दोनों कुछ एक जैसे हैं। अलबर्ट आइंस्टीन गणित के ही माध्यम से धीरे-धीरे जीवन के रहस्य की तरफ उन्मुख हो रहा था।
लेकिन यह कभी एकाध को हो सकता है कि जिसके लिए गणित ही उसका काव्य हो! गणित से ऐसा प्रेम हो जैसा काव्य से होता है। और गणित में ही जिसे संगीत सुनाई पड़ता हो। ऐसा कभी-कभी हो सकता है। ऐसे ही कुछ जैनाचार्य हुए हैं। कुंदकुंद ऐसे ही अदभुत व्यक्ति रहे होंगे। उमास्वाति ऐसे ही अदभुत व्यक्ति रहे होंगे। मगर उन पर बोलने जैसा कुछ भी नहीं है।
उपनिषदों पर बोलना हो तो बोले चले जाओ। घने जंगल हैं। और न मालूम कितने फूल खिलते हैं। एक-एक फूल का वर्णन करो, अंत नहीं आए। संतों पर बोलना हो, बोलते चले जाओ। एक-एक शब्द में इतने दीये जलते हैं। और एक-एक शब्द में ऐसी रस की बूंदें टपकती हैं। और एक-एक शब्द में ऐसे मोतियों के भंडार पड़े हैं। मगर शुष्क गणित हो तो क्या करो!
बोधिसत्व का यहां आ जाना जरूर मेरे प्रति गहन प्रेम का परिणाम है। नहीं तो आना संभव नहीं था। चमत्कार है आ जाना! सब छोड़-छाड़ कर आ जाना! बड़ा पद, बड़ी नौकरी, प्रतिष्ठा, सब छोड़-छाड़ कर चले आना। लेकिन कृष्णा को जरूर कुछ ज्यादा हो रहा है। सीखो उससे। भाव सीखो। भाव में डूबो। विचार को भी त्याग दो। जैसे न्यायाधीश होने को त्याग दिया, अब विचार को भी त्याग दो। थोड़े और भी ज्यादा स्त्रैण हो जाओ। क्योंकि जितना ही तुम भावपूर्ण होने लगो, जितनी ही तुम्हारे भीतर स्त्रैण कोमलता आने लगे, ग्राहकता आने लगे, उतने ही चमत्कार तुम्हें भी घटित होने शुरू हो जाएंगे। अभी कृष्णा को जो हो रहा है, कल तुम्हें भी होगा। और होना निश्चित है; क्योंकि तुम्हें कृष्णा पर कोई संदेह नहीं है। यद्यपि चकित तुम होते हो।
और किसी से कहोगे तो कोई उन पर विश्वास भी नहीं करेगा। ये बातें अनुभव से ही जानी जाती हैं। किसी दूसरे पर कोई कभी विश्वास नहीं करता। अंधा आदमी कैसे विश्वास करे कि आकाश में इंद्रधनुष निकला है सात रंगों वाला? अंधा आदमी कैसे विश्वास करे कि आकाश अरबों-खरबों तारों के सौंदर्य से भरा है? अंधा आदमी कैसे विश्वास करे कि जगत में प्रकाश है, रंग है, रूप है, सौंदर्य है? आंख खुले तो ही!
इसलिए कृष्णा और तुम्हारे बीच जो घटे, यहां इतने दीवाने हैं उनसे बात कर लेना, मगर यहां-वहां किसी से मत कहना। एक बहुत बात महत्वपूर्ण स्मरण रखने जैसी है: जीवन के जो सूक्ष्म अनुभव हैं, बड़े नाजुक होते हैं। उन्हें बनाने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन उन्हें तोड़ने में बहुत आसानी है, कोई भी तोड़ सकता है। कोई भी बुद्धू, जिसे कुछ अनुभव नहीं है, इतना ही कह दे–अरे, यह सब बकवास है! इस कहने में क्या लगता है–कि यह सब अंधविश्वास है। कि तुम सम्मोहित हो गए हो। कि तुम कल्पना के जाल में पड़ गए हो। यह कोई भी कह देगा। और बहुत कहेंगे ही। क्योंकि आखिर उन्हें अपनी आत्मरक्षा भी करनी है न!
तुर्गनेव की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक गांव में एक महामूर्ख था। वह बड़ा पीड़ित था, क्योंकि कहीं भी कुछ कहे, लोग उस पर हंसें। उसकी मूर्खता इतनी प्रसिद्ध थी कि वह बोले ही नहीं। न बोले तो लोग हंसें कि वह मूर्ख है, बोलेगा क्या? अगर बोले तो कुछ गलती निकाल लें। गांव में एक फकीर आया। उस महामूर्ख ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे बचाओ! मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही जाएगी? बोलता हूं तो लोग समझते हैं मूर्ख हूं। जो भी बोलूं वह गलत। सही भी बोलूं तो लोगों को शक होता है कि गलती होनी ही चाहिए, जब महामूर्ख कह रहा है तो गलत होगा ही। वही बात दूसरे कहते हैं तो कोई नहीं हंसता। वही बात मैं कहता हूं तो लोग हंसते हैं। अगर चुप रहूं तो लोग कहते हैं, चुप न रहेगा तो और क्या करेगा? बोला कि फंसा! तो मेरी बड़ी मौत हो गई, मेरी फांसी लगी है। मुझे बचा लो।
उस फकीर ने कहा, तू घबड़ा मत। यह ले तरकीब! सात दिन बाद आकर मुझे बता जाना। तरकीब सीधी-सादी है। कोई कुछ भी कह रहा हो, तू खंडन कर। मंडन किसी बात का करना ही मत। क्योंकि मंडन में खतरा है। वह बड़े बलशालियों की बात है। खंडन में कोई खतरा नहीं है।
उसने पूछा, मतलब?
फकीर ने कहा, मतलब, जैसे कोई कहे कि देखो, कितना सुंदर चांद निकला है! तू एकदम कहना: इसमें क्या सौंदर्य है? अरे चांद सदा निकलता रहा है, इसमें कौन सी नई बात है! और मुझे तो कोई सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता। सिद्ध करो कि सौंदर्य कहां है?
कौन सिद्ध कर पाएगा?
कोई कहे कि देखो, पक्षी पंख मार रहा है आकाश में, कितना प्यारा लग रहा है! फौरन खंडन करना: इसमें क्या प्यारा है? पक्षी सदियों से पंख मारते रहे–फड़फड़-फड़फड़। इसमें क्या कोई सौंदर्य है? सिद्ध करो! कोई कहे कि देखो, शेक्सपियर की कविताएं कितनी प्यारी! बस पकड़ लेना वहीं कि सिद्ध करो! कौन सा काव्य है इनमें? कौन सा सौंदर्य है इनमें? और कोई सिद्ध न कर पाएगा। कोई कहे, ईश्वर है। कहना, नहीं है। प्रमाण लाओ! और सात दिन बाद आकर मुझे बताना।
सात दिन बाद जब वह आदमी आया, उसके साथ दोत्तीन सौ आदमी आए। वह फकीर के चरणों पर गिर पड़ा और उसने कहा, खूब कुंजी दी! गांव भर मानता है कि मुझसे बड़ा प्रतिभाशाली कोई नहीं है। अब ये सब मेरे भक्त हो गए हैं। ये जो आप आदमी देख रहे हैं मेरे पीछे खड़े, ये सब मेरे शिष्य हैं। ये कहते हैं, ऐसी प्रतिभा तो हमारे गांव में कभी पैदा हुई ही नहीं। तुम तो लाखों में एक हो! तुम तो हीरों में हीरे हो! क्योंकि मैंने सबकी जबानें बंद कर दीं। जो बोला, उसी की जबान बंद कर दी। गजब की तरकीब दी आपने!
उस फकीर ने कहा, बस तू खंडन पर ही रहना, मंडन पर मत जाना कभी, तो ही चलेगी यह बात।
क्योंकि खंडन के लिए कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, न प्रतिभा की आवश्यकता होती है। कोई भी मूढ़ कह सकता है: सब बकवास है। कोई भी मूढ़ कह सकता है: न कोई परमात्मा है, न कोई आत्मा है। कोई भी मूढ़ कह सकता है: न कोई सौंदर्य है, न कोई सत्य है। कोई भी मूढ़ कह सकता है: यह सब सपना है, कल्पना है, भ्रमजाल है। और तुम सिद्ध न कर पाओगे। क्योंकि ये बातें भीतर की हैं; बाहर लाओगे कैसे? तुम्हारे भीतर जो हो रहा है, उसे तश्तरी में रख कर लोगों को दिखा तो न सकोगे।
इसलिए खयाल रहे, भीतर के अनुभव बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होते हैं। और कोई भी मूढ़ एक जरा सी चोट करके उन्हें तोड़ दे सकता है। इसलिए उनसे ही कहना जो सहारा दें। पुराने समय से यह रिवाज रहा, अपने सदगुरु को जाकर कहना कि वह आशीर्वाद दे; कि वह तुम्हारे ऊपर अमृत की वर्षा कर दे; कि तुम्हारे भीतर जो नई-नई कोंपलें निकल रही हैं, नये-नये अंकुर प्रकट हो रहे हैं, वे मजबूत हो जाएं।
तुमने पूछा है, बोधिसत्व: “हमें इतने दिनों तक दूर क्यों रहना पड़ा’ जब कि पहली ही पहचान में आपकी भगवत्ता स्पष्ट हो गई थी?’
दूरी भी सहयोगी है। जैसे निकटता सहयोगी है। दूरी पकाती है, प्रेम को उमगाती है। दूरी प्यास को जगाती है। दूरी तड़फाती है। तुम आते रहे, तुम जाते रहे–इन पंद्रह वर्षों में न मालूम कितनी बार तुम आए, न मालूम कितनी बार तुम गए–हर बार तुम नया रस लेकर जाते रहे, हर बार नई प्यास लेकर जाते रहे। प्यास घनी होती रही, घनी होती रही, घनी होती रही। जैसे सौ डिग्री पर पानी भाप बनता है न! गरम होते-होते, होते-होते…अट्ठानबे डिग्री पर भाप नहीं बनता, निन्यानबे डिग्री पर भाप नहीं बनता, ठीक सौ डिग्री पर भाप बनता है। ये पंद्रह वर्ष लगे कि तुम्हारी प्यास सौ डिग्री पर पहुंच जाए। उससे पहले नहीं हो सकता था। उससे पहले होता तो कच्चा होता।
और कभी-कभी कुछ कच्चे लोग आ जाते हैं। मैं उन्हें मना नहीं करता। क्योंकि कच्चे हों भला, आखिर उनकी प्यास तो है ही! मना नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं वे कच्चे लोग हैं, टिक न पाएंगे। पच्चीस कारण खोज लेंगे और वापस लौट जाएंगे। कोई ऐसा क्षुद्र कारण खोज लेंगे और वापस लौट जाएंगे, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी छोटी-मोटी अड़चन उनको पर्याप्त हो जाएगी और वे लौट जाएंगे। कभी-कभी जिद्द से आ जाते हैं। मैं मना भी करता रहता हूं कि अभी आने का समय नहीं है, थोड़ी देर और रुको, मगर नहीं मानते। मैं जितना रोकता हूं, उनकी जिद्द बढ़ती है। वे चले ही आते हैं। लेकिन बस महीने, पंद्रह दिन में टूट जाता है मामला। फिर लौटना पड़ता है। और वह लौटना महंगा हो जाता है। क्योंकि फिर और लंबा अंतराल हो गया मेरे और उनके बीच। इससे अच्छा था, वे न आते। दूर थे, याद तो करते थे। दूर थे, आना तो चाहते थे।
हर चीज का समय है। हर चीज के पकने का नियत समय है।
इसलिए तुमने कई बार, बोधिसत्व, मुझसे आने को कहा। मैंने कहा कि ठीक है, और थोड़ी देर रुको, और थोड़ी देर रुको। अभी जल्दी क्या है, यह साल गुजार दो, फिर। नया कम्यून बनेगा तब आ जाना, और गुजारो, और गुजारो। मैं टालता ही रहा हूं। तुम आते गए, तुम पूछते गए, मैं टालता गया। अब टालने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम पक गए हो। अब तुम बेशर्त आने को राजी हो। पकने का अर्थ होता है: बेशर्त।
कुछ लोग शर्तें लेकर आते हैं। जो शर्त लेकर आता है वह चूक जाएगा। उसकी शर्त ही मेरे और उसके बीच बाधा रहेगी। जो बेशर्त आता है वही केवल मुझसे जुड़ पाता है।
और तुम धन्यभागी हो इसलिए कि तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी–सब मुझसे जुड़े हैं। एक से भाव से जुड़े हैं। जरा भी कोई बाधा नहीं है।
जीत मेरी, तुम न मानो हार अपनी,
मैं तुम्हारी हार पर प्रिय! जीत अपनी वारती हूं।
कर रही चित्रित तुम्हीं को आज मैं कंपित करों से।
गीत जिसमें गूंज हो तव, प्यार है उसके स्वरों से।
तुम न अपनाओ अकिंचन गीत मेरा,
किंतु मैं हर गीत में तव रूप सहज संवारती हूं।
मैं तुम्हारी हार पर प्रिय! जीत अपनी वारती हूं!
कब चकोरी चांद से मधु प्रीति का वरदान पाती!
पर कभी क्या स्वप्न में भी लक्ष्य को अपने भुलाती!
तुम अपरिचित लक्ष्य ही बन कर रहो पर,
मैं तुम्हारी राह के ध्रुव चिह्न सतत निहारती हूं!
मैं तुम्हारी हार पर प्रिय! जीत अपनी वारती हूं!
चाहने से हो सकी कब कामना पूरी किसी की,
नापने से कम हुई क्या राह की दूरी किसी की!
प्रीति मेरी छू न पाए तव चरण पर,
मैं उसी लघु प्रीति पर शत जन्म अपने वारती हूं!
मैं तुम्हारी हार पर प्रिय! जीत अपनी वारती हूं!
कौन बाती को संजोए! कौन पूजा दीप बाले!
कौन चरणों में तुम्हारे नीर लेकर अर्घ्य ढाले!
कौन जाने पहुंच पाती या न तुम तक,
किंतु मैं हर श्वास में गाती तुम्हारी आरती हूं!
मैं तुम्हारी हार पर प्रिय! जीत अपनी वारती हूं!
मैं तुम तीनों की आरती सुन रहा हूं। मैं तुम तीनों का गीत समवेत उठ रहा मेरी ओर, उसे अनुभव कर रहा हूं।
यह मुश्किल से होता है कि पूरा परिवार एक साथ मुझसे जुड़ जाए। पत्नी जुड़ जाती है तो पति बाधा डालता है; पति जुड़ जाता है तो पत्नी बाधा डालती है। बच्चे आना चाहते हैं तो मां-बाप नहीं आने देना चाहते; मां-बाप आना चाहते हैं तो बच्चे उपद्रव खड़ा करते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा पूरा परिवार एक से रस में डूब गया है। इसलिए सुबह ज्यादा दूर नहीं है। डूबो!
और वे जो चमत्कृत करने वाली घटनाएं घट रही हैं, उन पर सोच-विचार न करना, उनका विश्लेषण न करना। उनका अनुभव करो, मगर विश्लेषण नहीं। क्यों, ऐसा प्रश्न ही मत उठाओ। जो हो, उसे स्वीकार कर लो, आनंदभाव से, प्रभु का प्रसाद मान कर। तो और-और, और-और घटता जाएगा। नये-नये शिखर चढ़ने हैं अभी, और नये-नये प्रकाश अनुभव करने हैं अभी। नई-नई समाधि के द्वार खुलने हैं अभी। “क्यों’ में मत अटक जाना। और “क्यों’ उठता है। कोई भी बात नई भीतर घटती है, तो “क्यों’ उठता है। कि ऐसा क्यों हो रहा है? मगर अगर तुम “क्यों’ में उलझ गए, तो जो ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाती वह “क्यों’ के चक्कर में पड़ जाती है। और “क्यों’ का चक्कर बड़ा है। उससे गुत्थी सुलझती नहीं, उलझती है। “क्यों’ को तो विदा कर दो। जो है, है। जैसा है, है। ऐसे सर्व-स्वीकार में जीने का नाम आस्तिकता है।
और मैं आस्तिकता सिखाता हूं। हिंदू नहीं बनाता तुम्हें, मुसलमान नहीं बनाता तुम्हें, ईसाई नहीं बनाता तुम्हें, तुम्हें सिर्फ आस्तिक बनाता हूं। “हां’ कहने की अपूर्व क्षमता का नाम आस्तिक है। और “हां’ जब कहना आता है, तो कौन फिक्र करता है “क्यों’ की!
तुम फर्क समझो।
गुलाब का फूल खिला। तुम पूछो कि क्यों, यह लाल क्यों है? यह आज ही क्यों खिला? यह इतना ही बड़ा क्यों है? तुम हजार “क्यों’ पूछ सकते हो। मगर इस सब “क्यों’ की उलझन में तुम भूल ही जाओगे कि गुलाब का फूल खिला है। और उसके सौंदर्य का आनंदमग्न होकर जो रसपान हो सकता था, वह नहीं हो पा रहा है। इस “क्यों’ की उलझन में तुम नाच न पाओगे गुलाब के फूल के पास। और तुम क्यों ही क्यों करते रहोगे और गुलाब का फूल कुम्हला भी जाएगा, उसकी पंखुड़ियां भी झर जाएंगी और तुम क्यों ही क्यों करते रहोगे। ज्यादा से ज्यादा तुम यह करोगे कि गुलाब के फूल को तोड़ कर, किताब में दबा कर, सुखा कर, सम्हाल कर रख लोगे नाम लिख कर कि किस जाति का गुलाब का फुल है, कब खिला था, कितना बड़ा था।
मगर वे सूखे गुलाब के फूल तुम्हारी किताबों में किसी काम के नहीं हैं। तुम्हारी किताबें सूखे गुलाब के फूलों से ही तो भरी हैं। जब फूल जिंदा है, तब नाच लो, मगन हो लो। जब फूल जिंदा है, तब गीत गा लो। जब फूल जिंदा है, तब तुम भी फूल हो लो।
गोरी-धन धरैं चौमुखी बाती
नेह भरैं सजना
दिपै दूधिया जोति
प्रकासैं घर देहरी अंगना
नवेली बारि धरैं दिअनां
पहलो दिया धरयो मैया तैं
जागी जोति दिवारी
याके चरन-कमल सब पूजैं
राजा रंक भिखारी
दाता लेय धरम की खातिर
लगी सूम के रतना
दूजो दिया गयो मंदिर पै
तीजो देविन खेरा
चौथो जरै नगर पनघट पै
पचओं तुलसिन चौरा
पांच दिया पूजा के बारे
चढ़ो जोति पै जुबना
तनिक देर मैं सब चिनि डारे
सूने अटा अटरियां
आंगन तै पुरि गए पौर लौं
जागी द्वार दुअरियां
गांव गुजरियां पहने घूमै
बरन-बरन के वसना
लौ पै दीठि दिया आंचर तै
कढ़यो लाज को घुंघटा
हौले-हौले चलैं कामिनी
आंगनवा तैं कुअटा
पांव तरत खुनकत पायलिया
हाथ उठत कंगना
मैया बांटै दिआ कुचुरुआ
भरि-भरि खील बताशे
भैया मांगे लाल अमिरती
सब दिन रहे उपासे
आवै दौज पेट भरि खइयो
कहै बिरन सौं बहिना
एक जोति सौं जरैं प्रकासैं
कोटि दिया लख बाती
जिनके हिया नेह बिनु सूखे
तिनकी सुलगैं छाती
बुद्धि को सुअना मरम न जानै
कथे प्रीति की मैना
एक जोति सौं जरैं प्रकासैं
कोटि दिया लख बाती
ज्योति एक है, लाखों दीयों में जलती है। ध्यान एक है, लाखों अनुभूतियों में प्रकट होता है। समाधि की प्रतीति एक है, लेकिन लाखों चमत्कार बन जाती है।
एक जोति सौं जरैं प्रकासैं
कोटि दिया लख बाती
जिनके हिया नेह बिनु सूखे
तिनकी सुलगैं छाती
और अभागे हैं वे लोग, जिनके हृदय नेह से सूखे हैं। क्योंकि उनके हृदय में सिवाय चिता के और कुछ भी नहीं जल रहा है। वहां जीवन नहीं है। जीवन तो वहीं है जहां प्रेम है।
जिनके हिया नेह बिनु सूखे
तिनकी सुलगैं छाती
बुद्धि को सुअना मरम न जानै
कथे प्रीति की मैना
वह जो बुद्धि का तोता है, उसे प्रेम का कोई राज पता नहीं है। प्रेम का राज पूछना हो तो प्रीति की मैना से पूछना।
इसलिए मैंने कहा, हो जाओ जितने स्त्रैण हो सको, जितने कोमल हो सको। परमात्मा ही एकमात्र पुरुष है। वही एक कृष्ण, बाकी सब गोपी–ऐसा भाव सघन करो। और चमत्कारों पर चमत्कारों की कतारें लग जाएंगी। दीये पर दीये जल जाएंगे। पूरी दीपावली तुम्हारे भीतर उतर आने को तैयार है। द्वार खोलो! प्रीति के द्वार खोलो!
तीसरा प्रश्न: संत विरहावस्था की चर्चा बहुत करते हैं। यह विरह क्या बला है?
संतोष! बला ही है! बड़ी बला है। तुमने जितनी बलाएं जानी हैं, सब बहुत छोटी हैं। किसी को धन नहीं मिला, तो तड़प रहा है। यह तड़पन कुछ भी नहीं। किसी को पद नहीं मिला, जार-जार रो रहा है। ये आंसू कुछ भी नहीं। इनकी उतनी ही कीमत है जितनी धन की और पद की हो सकती है। धन मिल भी जाता तो क्या मिलता? धन नहीं भी मिला तो क्या खोया? पद पाकर भी कौन से पद मिल गए हैं? पद खोने से भी क्या पद खो जाता है? न मिलने से कुछ होता, न खोने से कुछ होता। इस जगत की और सब बलाएं तो बड़ी छोटी हैं। यहां सफलता ही छोटी है तो असफलता तो छोटी होगी ही। यहां जीत भी हार जैसी है तो हार का तो कहना ही क्या! लेकिन विरह की अवस्था निश्चित ही बड़ी बला है। प्रेम-पंथ ऐसो कठिन!
विरह का अर्थ है: बूंद सागर होने की आकांक्षा से भरी। असंभव की आकांक्षा, जो नहीं होता मालूम पड़ता, जो तर्क से लगता है कि हो ही नहीं सकता, सब विचार जिसके विपरीत हैं, सारा जीवन-अनुभव जिसको सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसे असीम, असंभव, अरूप को पाने की आकांक्षा विरह है।
भक्त ही रोता है। भक्त ही जानता है कि रोना क्या है। उसके आंसू साधारण आंसू नहीं हैं। उसके आंसुओं की परीक्षा तुम जाकर किसी वैज्ञानिक से मत करवा लेना। क्योंकि वैज्ञानिक उसके आंसुओं में भी वही पाएगा जो तुम्हारे आंसुओं में पाता है। यही तो विज्ञान की सीमा है। एक आदमी का दस रुपये का नोट खो गया है और वह रो रहा है। और एक आदमी परमात्मा के लिए रो रहा है। दोनों के आंसुओं को ले जाओ वैज्ञानिक के पास, वह कोई फर्क न कर पाएगा। वह दोनों की आंखों के आंसुओं का विश्लेषण करके बता देगा कि दोनों में इतना नमक है–बराबर-बराबर। और इतना पानी है, और इतना यह है, इतना यह है। लेकिन वह यह न बता सकेगा कि कौन आदमी दस रुपये के लिए रो रहा है और कौन आदमी परमात्मा के लिए रो रहा है। यह नहीं बता सकेगा। दोनों के आंसुओं में कोई भेद न होगा। यह विज्ञान की सीमा है कि वह क्षुद्र को ही पकड़ पाता है। विराट चूक जाता है।
लेकिन तुम जानते हो। क्योंकि तुम भी बहुत तरह से रोए हो। तुम्हारी मां चल बसी और तुम रोए थे। वह भी एक रोना था। तुम असफल हो गए थे किसी दौड़ में और रोए थे। वह भी एक रोना था। लेकिन दोनों रोनों में बहुत फर्क–बहुत-बहुत फर्क, जमीन-आसमान का फर्क।
भक्त इस जगत में सबसे बड़े रोने को जानता है–सबसे गहरे रोने को जानता है। उसके आंसू आंख से नहीं आते, उसके आंसू आत्मा से आते हैं। उसके आंसू उसके प्राणों का निचोड़ हैं। और चूंकि भक्त के आंसू सबसे बड़े हैं, इसलिए भक्त का आनंद भी सबसे बड़ा है। इन्हीं आंसुओं की सीढ़ियों पर चढ़ कर तो वह उस परम आनंद तक पहुंचता है। ये आंसू कीमत हैं जो वह चुकाता है।
विरह-अवस्था का अर्थ है कि अहसास होने लगा कि परमात्मा है। पास ही है। तड़प पैदा होने लगी। झंकार उठने लगी। तलाश शुरू हो गई–और मिलता नहीं! पास है और मिलता नहीं!
तुमने कभी खयाल किया? किसी आदमी को रास्ते पर देखा, याद आ गया, चेहरा याद आ गया, सब याद आ गया, पहचाना है, जानते रहे, नाम जबान पर रखा है। तुम कहते हो: नाम जबान पर रखा है। मगर आ नहीं रहा। तब तुमने तकलीफ देखी, कैसी बेचैनी होती है! कैसी उमड़-घुमड़ होती है! कैसे भीतर ही भीतर तुम परेशान होते हो! जबान पर रखा है और आ नहीं रहा है। जानते हो कि जानता हूं और फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा है।
ऐसी ही दशा हो जाती है भक्त की, इतने पास और इतने दूर! यह रहा, और छूट-छूट जाता है। जैसे कोई पारे पर मुट्ठी बांधे और पारा छितर-छितर जाए। और जितनी मुट्ठी बांधे उतना छितर-छितर जाए। ऐसी भक्त की दशा है–रोए न तो क्या करे!
खूब रोता है। मगर उसका रोना रासायनिक रूपांतरण करता है। जितना रोता है, उतना ही हलका होता है। जितना हलका होता है, उतना परमात्मा के करीब जाने के लिए पंख मिलते हैं। जितना रोता है, उतना निखरता है। जितना निखरता है, उतनी परमात्मा की छवि स्पष्ट बनने लगती है। जितना रोता है, उतनी धूल झड़ जाती है आंखों से।
तुम जाकर आंख के डाक्टर से पूछना कि आंसुओं का असली प्रयोजन क्या है? तो वह तुम्हें आंसुओं का असली प्रयोजन बताएगा–ताकि आंख पर धूल न जम पाए। आंख पर धूल न जमे, इसीलिए आंसू आते हैं। इसलिए जरा सी कंकड़ी आंख में चली गई कि फौरन आंसू आते हैं। क्यों? ताकि कंकड़ी बह जाए आंसुओं में। और तुम दिन भर पलक झपकते हो, पता है क्यों? सिर्फ इसीलिए कि पलक गीली है भीतर आंसू से, बार-बार झपक कर तुम्हारी आंख को पोंछती रहती है, तुम्हारी आंख को गीला करती रहती है, आर्द्र करती रहती है, ताकि धूल न जम पाए।
यह तो डाक्टर कह देगा तुमसे। यह बाहर की आंख की बात हुई। मगर भीतर की आंख के संबंध में भी यही सच है।
भक्त जैसे ही रोता है, वैसे ही उसकी आत्मा की धूल भी झड़ती है, धूल भी पुंछती है। और जैसे-जैसे उसका रुदन गहरा होता जाता है, उसकी प्रार्थना में प्राण आने लगते हैं। उसकी प्रार्थना सांस लेने लगती है। और जितनी तुम्हारी प्रार्थना श्वासपूर्ण हो जाएगी, उतना ही तुम पाओगे: परमात्मा निकट, और निकट, और निकट। एक ऐसी भी घड़ी आती है, जब भक्त अलग नहीं होता रोने से, रोना ही होता है। विरह की अवस्था नहीं होती, भक्त विरह की अग्नि हो जाता है। बस विरह ही रह जाता है, विरही नहीं बचता। उसी घड़ी मिलन। उसी घड़ी प्राप्ति। उसी घड़ी उपलब्धि।
तुम पूछते हो: “संत विरहावस्था की बहुत चर्चा करते हैं। यह विरह क्या बला है?’
तुमने कोई छोटा-मोटा विरह जीवन में जाना या नहीं? किसी से कभी प्रेम किया, संतोष? कि संतोष ही करते रहे?
यह शरद की पूर्णिमा की प्यास मेरे पास,
चांदनी का लिपटता अहसास मेरे पास,
याद की यह गंध मेरे साथ सोएगी,
आज तो बस रात भर यह रात रोएगी,
दूर हो तुम!
लो, उधर ढोलक बजी, उमड़े सुरीले गीत,
बांह में ले बांह नाचे, मस्तियों में मीत,
रात भर गाने-नचाने के हुए वादे,
और मेरे गीत सारे रह गए आधे,
दूर हो तुम!
यह जुन्हाई खिड़कियों से झांकती आती,
और बैठा लिख रहा हूं मैं तुम्हें पाती,
क्या तुम्हारे द्वार पूनम ने न दी थपकी?
सच बताना, एक पल भी आंख क्या झपकी?
पास होतीं, पूछ लेता, लग रहा कैसा?
दूर हो तुम!
किसी को प्रेम किया? किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी मित्र को, किसी प्रियजन को प्रेम किया? अगर प्रेम किया है, तो थोड़ा सा विरह अनुभव किया होगा–छोटा विरह, संसार का विरह। मगर उसी विरह के आधार से परम विरह को समझा जा सकता है। जिन्होंने परमात्मा को प्रेम किया है, उनके विरह को जानने की तुम्हारे पास और तो कोई सुविधा नहीं है, सिवाय इसके कि तुमने किसी को कभी प्रेम किया हो। तुम्हारा प्रेम बूंद जैसा, उनका प्रेम सागर जैसा। तुम्हारा प्रेम बहुत क्षुद्र, क्षणभंगुर, उनका शाश्वत, सनातन। पर प्रेम तो प्रेम है।
लो, उधर ढोलक बजी, उमड़े सुरीले गीत,
बांह में ले बांह नाचे, मस्तियों में मीत,
रात भर गाने-नचाने के हुए वादे,
और मेरे गीत सारे रह गए आधे,
दूर हो तुम!
कभी किसी की दूरी अनुभव हुई है? नहीं हुई हो तो प्रेम करो! तो प्रेम से डरो मत! भयभीत न होओ! क्योंकि वही प्रेम तुम्हें और बड़े प्रेम की तरफ इशारे करेगा। प्रेम में जलो! क्योंकि वही जलन तुम्हें परम विरह-अग्नि की ओर ले चलेगी।
रामानुज से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं?
रामानुज ने उस आदमी की तरफ देखा। रामानुज जैसे लोग जब किसी की तरफ देखते हैं तो आर-पार देख लेते हैं। दिख गया वह आदमी कि किस तरह का आदमी है। रामानुज ने पूछा कि मेरे भाई, पहले एक जवाब दे। तूने कभी किसी को प्रेम किया है?
उस आदमी ने कहा, प्रेम-व्रेम की झंझट में मैं पड़ा ही नहीं। मुझे तो ईश्वर चाहिए!
रामानुज ने कहा, मैं फिर पूछता हूं, किसी को तो किया होगा प्रेम? किसी मित्र को, मां को, पिता को, भाई को, बहन को, किसी को तो प्रेम किया होगा?
लेकिन वह आदमी भी एक ही; पक्का त्यागी था। उसने कहा, प्रेम? प्रेम बंधन है। प्रेम मोह है, आसक्ति है। मैंने किसी को प्रेम नहीं किया। और बार-बार यही सवाल क्यों पूछते हैं? मैं तो सिर्फ ईश्वर को पाना चाहता हूं।
कहते हैं, रामानुज की आंखों से आंसू टपके और उन्होंने कहा, फिर मैं असमर्थ हूं। मैं तेरे किसी काम न आ सकूंगा। मैं तुझे कोई सहायता न पहुंचा सकूंगा। तूने प्रेम ही नहीं जाना, तो परमात्मा से तेरा प्रेम कैसे जुड़वा दूं? तूने घूंट भर भी चखा होता, तो सागर भी समझाया जा सकता था। मगर तू घूंट से भी वंचित है।
और तुम्हारे साधु-संत तुम्हें यही समझाते रहे हैं। प्रेम के दुश्मन हैं वे। हर जगह तुम्हें घबड़ा दिया है–मोह, आसक्ति, यह, वह! तुम्हें ऐसा डरा दिया है कि तुम्हारे प्रेम को जगने की संभावना नहीं छोड़ी है। और इस सब से ऊपर मजाक यह है कि वे तुमसे कहते हैं: परमात्मा को प्रेम करो। अब तुम फंसे मुश्किल में। लगी फांसी! प्रेम करने नहीं देते, क्योंकि सब प्रेम आसक्ति, बंधन, संसार। शुद्ध प्रेम करो परमात्मा का! कीचड़ तो सब छीन ली, कहते हैं, कमल खिलाओ!
मगर बिना कीचड़ के कमल खिलता नहीं। कमल तो कीचड़ में खिलता है। कमल तो कीचड़ का ही शुद्धतम रूप है। कमल तो कीचड़ में छिपा है। अप्रकट पड़ा है। जिसे सांसारिक प्रेम तुम कहते हो, उसमें ही तुम्हारी भक्ति छिपी है, भक्ति का कमल छिपा है। कीचड़ सही संसार, मगर मैं उस कीचड़ को भी सम्मान देता हूं। क्योंकि उसमें से कमल प्रकट होते हैं। इसी संसार में बुद्ध प्रकट होते हैं। इसी संसार में मीरा, इसी संसार में दरिया, इसी संसार में कबीर, नानक। इतने कमल इस संसार में पैदा होते हैं और फिर भी तुम संसार को गाली दिए जाते हो? कुछ तो संकोच करो। कुछ तो बेशर्मी अनुभव करो।
संसार को गाली मत दो! अगर इस संसार ने एक भी बुद्ध पैदा कर दिया है तो इस संसार ने अपने होने की पर्याप्त प्रामाणिकता दे दी है। अगर इस संसार ने इतने बुद्ध पैदा किए हैं, बुद्धों का सिलसिला पैदा किया है, तो काफी प्रमाण दे दिए हैं कि कीचड़ कीचड़ ही नहीं है, कीचड़ में कमल छिपे हैं। अब यह बात तुम्हारी है कि तुम कीचड़ से कमल खोज पाओगे कि न खोज पाओगे। अपनी अकुशलता को, अपनी बुद्धिहीनता को संसार के लिए गालियां देने में मत लगाओ।
संतोष, प्रेम करो! कैसा भी प्रेम हो, शुभ है। क्योंकि कैसा भी प्रेम हो, उसको निखारा जा सकता है। अगर व्यक्तियों से डरते हो, तो चलो, संगीत से प्रेम करो। प्रकृति से प्रेम करो। चांदत्तारों से प्रेम करो। कुछ तो करो! किसी सृजनात्मक आयाम में अपने प्रेम को उंडेल दो। मूर्तियां बनाओ, कि गीत रचो, कि नाचो। मगर किसी दिशा में तुम्हारे प्रेम को प्रवाहित तो होने दो, ताकि थोड़ा प्रेम का अनुभव हो। प्रेम का अनुभव हो, तो उसी के पीछे-पीछे विरह का अनुभव होगा। विरह प्रेम की छाया है।
मलयज रथ के स्वर डोल चले
गुंजार भ्रमर पुट खोल चले
पलकों में क्यों प्लावन मचले
मन में उठती कोई कराह,
रोके न रुके जिसका प्रवाह।
मकरंद मधुर मुख मौन लीन
रह-रह बजती चेतना बीन
स्मृति कादंबिनी अनुराग पीन
छाई ले किसकी छिपी छांह;
लय भाग रही खोजती राह।
रे प्रणय पयोनिधि की लहरी!
क्यों आज बनी इतनी गहरी;
तू मर्मवती केवल सह री
वेदना बाड़वी कलित दाह;
सिर पीट लगा पाई न थाह।
संसृति रचती निज सृष्टि पिए
फणियों-सी मणि के दीप लिए
मर-मर कर शत-शत बार जिए
प्राणों में जिसकी पली चाह;
निष्ठुर वह इतना हुआ आह।
प्रेम करोगे तो विरह झेलोगे। क्योंकि जिसे चाहोगे, जब चाहोगे तभी न मिल जाएगा। और जितना चाहोगे, उतना निष्ठुर मालूम होगा। क्योंकि जितना मांगोगे, उतना ही पाओगे कि दूरी अभी और शेष है। प्रेम दूरी बर्दाश्त नहीं करता, इंच भर दूरी बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम द्वैत बर्दाश्त नहीं करता। और जब तक द्वैत रहता है, तब तक विरह रहता है। प्रेम तो अद्वैत चाहता है। प्रेम तो चाहता है, एक हो जाऊं, बिलकुल एक हो जाऊं।
इस संसार के प्रेम की अगर कोई भूल है तो बस इतनी ही है कि इस संसार का कोई भी प्रेम अद्वैत का अनुभव नहीं देता। और देता भी है तो क्षणभंगुर को, जरा सी देर को, एक झलक। और झलक आई और गई। और झलक जाने के बाद और भी अंधेरा रह जाता है, और भी गङ्ढे में गिर जाते हो, और भी विषाद घना हो जाता है। क्योंकि जान ली झलक एकता की, तो अब दुई और खलती है, और अखरती है।
मैं तो तुमसे कहता हूं: इस जगत के प्रेम को जानो। ताकि दुई खले, अखरे। द्वैत छाती में चुभ जाए कटार की भांति। तभी तो तुम अद्वैत की तरफ चलोगे। तभी तो तुम उस परम प्यारे को खोजोगे, जिसके साथ मिलन एक बार हुआ तो हुआ। हुआ तो हुआ। जिसके साथ मिलन होने के बाद फिर कोई बिछुड़न नहीं होती। जिसमें डूबे तो डूबे, फिर निकलना नहीं होता। जहां से वापस आने का कोई उपाय नहीं। उस परम अवस्था को ही हम मोक्ष कहते हैं, जहां से वापस लौटने का कोई उपाय नहीं।
लेकिन प्रेम के थोड़े अनुभव करने होंगे। और तुम्हारी सड़ी-सड़ाई धारणाओं को छोड़ो! तुम्हारी सदियों-सदियों तक पीटी गई, पुनरुक्त की गई अंधी धारणाओं को त्यागो! उनके कारण ही तुम प्रेम से वंचित हो और विरह का अनुभव भी नहीं हो रहा है। उनके कारण ही तुम सूखे-सूखे हो गए हो। रसधार बहती ही नहीं। और ऐसा भी मत समझना कि तुम किसी प्रेम में होओ, तो अनुभव हो जाएगा। तुम्हारा मन इतना विषाक्त हो गया है प्रेम के विपरीत कि जो लोग प्रेम में भी हैं, वे भी अपराधी की तरह प्रेम में हैं। भीतर अपराध-भाव रहता है, कि मैं भी यह क्या गलती कर रहा हूं!
मेरे पास युवक आ जाते हैं, वे कहते हैं कि क्या करें, मन में बड़े बुरे विचार उठते हैं।
बुरे विचार? मैं पूछता हूं, कौन से बुरे विचार?
वे कहते हैं, एक स्त्री से प्रेम हो गया है। बड़े बुरे विचार उठते हैं। आप हमें छुड़ाओ।
स्त्री से प्रेम हो गया है, इसको वे बड़े बुरे विचार कह रहे हैं। प्रेम और बुरा विचार! लेकिन यह समझाया गया है, यह सिखाया जा रहा है। पंडित-पुरोहितों की जमातें इस जहर को फैला रही हैं।
यह बिलकुल स्वाभाविक है। इसमें कुछ बुरा नहीं है। इसमें कुछ पाप नहीं है, अपराध नहीं है। हां, यह बात जरूर सच है, इतने पर ही रुक मत जाना। कीचड़ को ही समेट कर बैठ मत जाना। कीचड़ में ही बैठे मत रह जाना। कमल भी जन्माने हैं। कमल की याद रहे, कमल की तलाश रहे। मगर कीचड़ में ही पड़े हैं कमल। करो प्रेम! निर्भय होकर प्रेम करो! प्रेम करो जागरूक होकर। सब अपराध-भाव छोड़ कर प्रेम करो।
तो तुम प्रेम भी जानोगे, विरह भी जानोगे और संसार के प्रेम की क्षणभंगुरता भी जानोगे, और संसार के प्रेम की व्यर्थता भी जानोगे, और संसार के प्रेम का विषाद भी जानोगे। और संसार के प्रेम की आशाएं भी जानोगे, निराशाएं भी जानोगे। और उन सारी आशाओं-निराशाओं का जो परिपक्व निचोड़ मनुष्य के हाथ में लगता है, वही उसे परमात्मा की तरफ आंख उठाने के लिए मजबूर करता है। जब इस जगत के सारे प्रेमी असफल हो जाते हैं, जब यहां का सारा प्रेम असफल हो जाता है, तभी आंखें आकाश की तरफ उठती हैं परम-प्रेमी की तलाश में। फिर तुम्हें पता चलेगा विरह क्या है!
संत यूं ही विरह की बात नहीं करते। उनके हृदय में छुरी लगी है, तीर बिंधा है, वे बड़ी पीड़ा में हैं। यद्यपि वह पीड़ा मधुर है। बड़ी मीठी। क्योंकि परमात्मा के लिए पीड़ित भी होना सौभाग्य है। उसे बला मत कहो। वह धन्यभाग है! बड़भागी हैं वे जिनके जीवन में परमात्मा को पाने की आकांक्षा उठी है, विरह जगा है, विरह की अग्नि भभकी है, क्योंकि वे ही एक दिन उसे पाने के अधिकारी भी होंगे। वे उसे पाने के अधिकारी हो ही गए हैं।
आखिरी प्रश्न: कभी ध्यान में मुझे लगता है कि मंजिल बहुत निकट है, सुबह होने को है। तब मन बहुत आनंदित होता है। कभी भीतर गहन अंधकार अनुभव होता है, तब बहुत पीड़ा होती है। कभी आनंद, कभी पीड़ा; यह आंखमिचौनी प्रभु कब तक चलेगी?
राजपाल! यह तुम पर निर्भर है कि आंखमिचौनी कब तक चलेगी। मुझ पर निर्भर नहीं है, न परमात्मा पर निर्भर है, बस तुम पर निर्भर है। एक छोटी सी कुंजी खयाल में रखो, आंखमिचौनी आज ही बंद हो सकती है। कुंजी सीधी-सरल है, यद्यपि याद रखना कठिन है।
कुंजी क्या है?
तुम कहते हो: कभी लगता है मंजिल बहुत निकट है, सुबह होने को है। तब मन बहुत आनंदित होता है।
उस समय तुम आनंद के साथ तादात्म्य मत करना। ऐसा मत सोचना कि मैं आनंद हो गया। जागरूक रह कर साक्षी रहना। देखना कि आनंद चारों तरफ घेरे है, मैं पृथक, मैं अलग। मैं देखने वाला, मैं साक्षी, मैं द्रष्टा। आनंद दृश्य है, मैं द्रष्टा। बस यह कुंजी है।
फिर कभी गहन अंधकार का अनुभव होता है, तब बहुत पीड़ा होती है।
तब भी वही कुंजी। कुंजी वही है। जानना: अंधकार है, गहन पीड़ा है, मैं द्रष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। न तो मैं आनंद, न मैं दुख। न तो मैं प्रकाश, न मैं अंधकार। न मैं यह, न मैं वह–नेति-नेति।
तुम इस नेति-नेति की छोटी सी कुंजी को पकड़ लो। तब सुबह होगी। नहीं तो बस सुबह होती लगेगी हमेशा और रात बनी रहेगी। अब आई, अब आई सुबह, और रात बनी रहेगी। आते-आते चूकती रहेगी। क्योंकि तुम तादात्म्य कर लेते हो चित्त की दशाओं से।
दुख से तो अपने को अलग मानना आसान है, सुख से अलग मानना बहुत कठिन है। और वही असली बात है। इसलिए मैं कहता हूं: शुरू करो आनंद से। जब तुम्हें लगे आनंदित हो रहे हो, प्रफुल्लित हो रहे हो, तब भी जानते रहना कि ठीक है, मैं द्रष्टा हूं। अभी आनंद ने मुझे घेरा; जैसे कल पीड़ा ने घेरा था, आज आनंद ने घेरा, कल फिर पीड़ा घेरेगी; अभी सुबह थी, अब सांझ हो गई; मगर मैं अलग हूं, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं।
तुम द्रष्टा में ठहरते जाओ, ठहरते जाओ, ठहरते जाओ। इसको दरिया ने कहा है: जागे में जागना। ऐसे तुम जागे हुए हो, मगर यह कोई असली जागना नहीं है। जागे में जागना! और फिर तुम चकित हो जाओगे। तब न तो आनंद रह जाता है और न दुख। वही दशा असली आनंद की है। तब न तो दिन रह जाता है, न रात। वही दशा असली दिन की है। तब दो नहीं रह जाते। और जब दो नहीं रह जाते, तो आंखमिचौनी समाप्त हो जाती है।
तुम्हारे हाथ में है। मेरे किए कुछ भी न होगा। परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। यही तो मनुष्य की गरिमा है, गौरव है, कि उसे पूरी स्वतंत्रता दी है–कि दुख भोगना हो, दुख भोगो; सुख भोगना हो, सुख भोगो; आंखमिचौनी खेलनी हो, आंखमिचौनी खेलो; खेल के बाहर हो जाना हो, खेल के बाहर हो जाओ।
द्रष्टा है खेल के बाहर हो जाने की कला। और वही परम कला है।