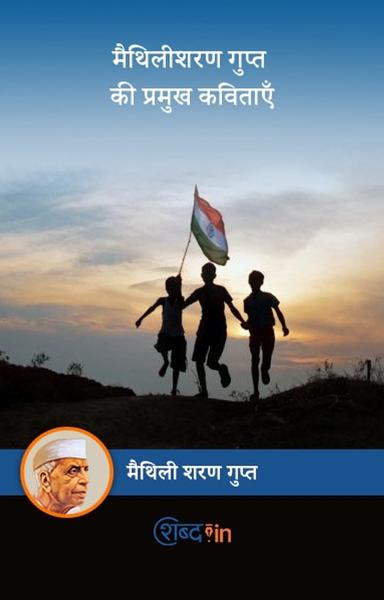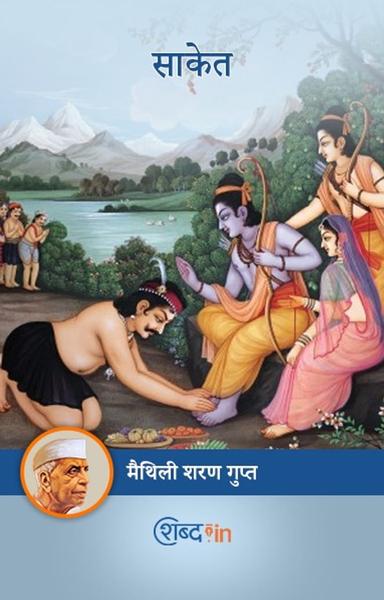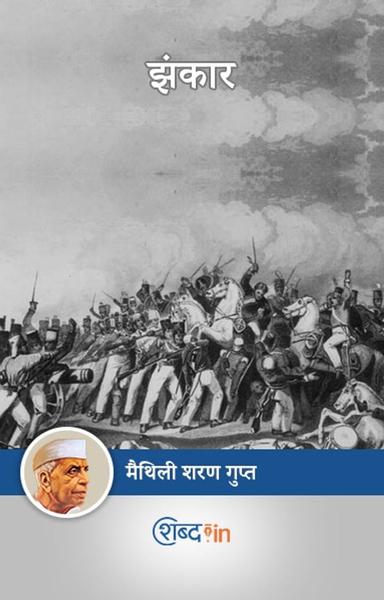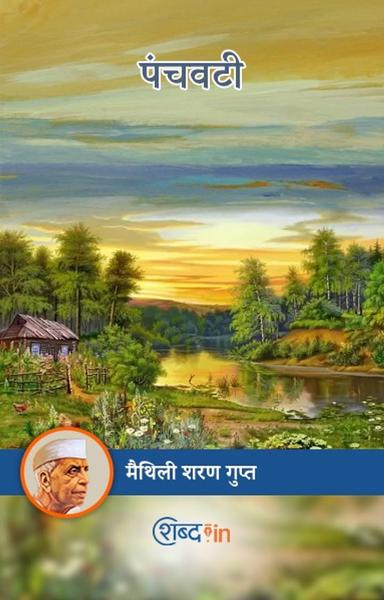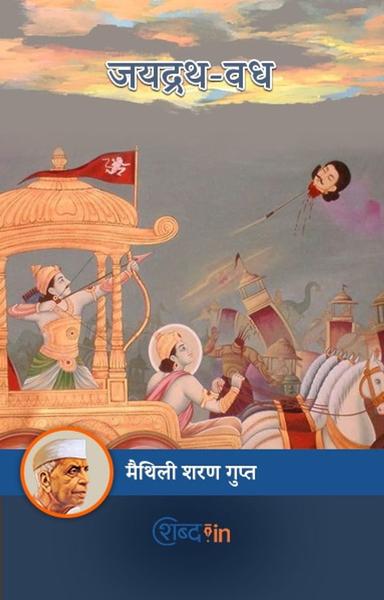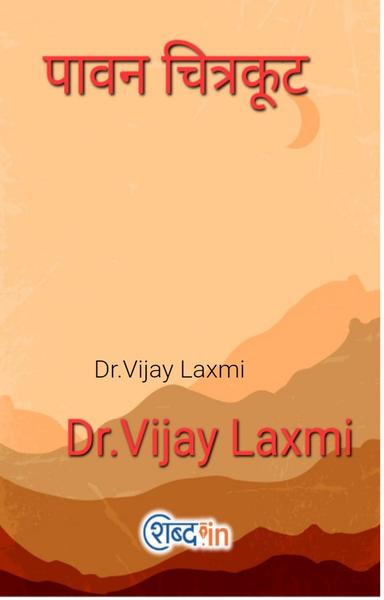लेखनी, अब किस लिए विलम्ब?
बोल,--जय भारति, जय जगदम्ब।
प्रकट जिसका यों हुआ प्रभात,
देख अब तू उस दिन की रात।
धरा पर धर्मादर्श-निकेत,
धन्य है स्वर्ग-सदृश साकेत।
बढ़े क्यों आज न हर्षोद्रेक?
राम का कल होगा अभिषेक।
दशों दिक्पालों के गुणकेन्द्र,
धन्य हैं दशरथ मही-महेन्द्र।
त्रिवेणी-तुल्य रानियाँ तीन,
बहाती सुखप्रवाह नवीन।
मोद का आज न ओर न छोर;
आम्र-वन-सा फूला सब ओर।
किन्तु हा! फला न सुमनक्षेत्र,
कीट बन गये मन्थरा-नेत्र।
देख कर कैकेयी यह हाल,
आप उससे बोली तत्काल
"अरी, तू क्यों उदास है आज,
वत्स जब कल होगा युवराज?"
मन्थरा बोली निस्संकोच--
"आपको भी तो है कुछ सोच?"
हँसी रानी सुन कर वह बात,
उठी अनुपम आभा अवदात।
"सोच है मुझको निस्सन्देह,
भरत जो है मामा के गेह।
सफल करके निज निर्मल-दृष्टि,
देख वह सका न यह सुख-सृष्टि!"
ठोक कर अपना क्रूर-कपाल,
जता कर यही कि फूटा भाल,
किंकरी ने तब कहा तुरन्त--
"हो गया भोलेपन का अन्त!"
न समझी कैकेयी यह बात;
कहा उसने--"यह क्या उत्पात?
वचन क्यों कहती है तू वाम?
नहीं क्या मेरा बेटा राम?"
"और वे औरस भरत कुमार?"
कुदासी बोली कर फटकार।
कहा रानी ने पाकर खेद--
"भला दोनों में है क्या भेद?"
"भेद?"-दासी ने कहा सतर्क--
"सबेरे दिखला देगा अर्क।
राजमाता होंगी जब एक,
दूसरी देखेंगी अभिषेक!"
रोक कर कैकेयी ने रोष,
कहा--"देती है किसको दोष?
राम की माँ क्या कल या आज
कहेगा मुझे न लोक-समाज?"
कहा दासी ने धीरज त्याग--
"लगे इस मेरे मुहँ में आग।
मुझे क्या, मैं होती हूँ कौन?
नहीं रहती हूँ फिर क्यों मौन?
देख कर किन्तु स्वामि-हित-घात,
निकल ही जाती है कुछ बात।
इधर भोली हैं जैसी आप,
समझती सब को वैसी आप!
नहीं तो यह सीधा षड्यन्त्र,
रचा क्यों जाता यहाँ स्वतन्त्र?
महारानी कौसल्या आज,
सहज सज लेतीं क्या सब साज?"
कहा रानी ने--"क्या षड्यन्त्र?
वचन हैं तेरे मायिक मन्त्र।
हुई जाती हूँ मैं उद्भ्रान्त;
खोल कर कह तू सब वृत्तान्त।"
मन्थरा ने फिर ठोका भाल--
"शेष है अब भी क्या कुछ हाल?
सरलता भी ऐसी है व्यर्थ,
समझ जो सके न अर्थानर्थ।
भरत को करके घर से त्याज्य,
राम को देते हैं नृप राज्य।
भरत-से सुत पर भी सन्देह,
बुलाया तक न उन्हें जो गेह!"
कहा कैकेयी ने सक्रोध--
"दूर हो दूर अभी निर्बोध!
सामने से हट, अधिक न बोल,
द्विजिह्वे, रस में विष मत घोल।
उड़ाती है तू घर में कीच;
नीच ही होते हैं बस नीच।
हमारे आपस के व्यवहार,
कहाँ से समझे तू अनुदार?"
हुआ भ्रू-कुंजित भाल विशाल,
कपोलों पर हिलते थे बाल।
प्रकट थी मानों शासन-नीति;
मन्थरा सहमी देखि सभीति।
तीक्ष्ण थे लोचन अटल अडोल;
लाल थे लाली भरे कपोल।
न दासी देख सकी उस ओर;
जला दे कहीं न कोप कठोर!
किन्तु वह हटी न अपने आप,
खड़ी ही रही नम्र चुपचाप।
अन्त में बोली स्वर-सा साध
"क्षमा हो मेरा यह अपराध।
स्वामि-सम्मुख सेवक या भृत्य,
आप ही अपराधी हैं नित्य।
दण्ड दें कुछ भी आप समर्थ;
कहा क्या मैंने अपने अर्थ?
समझ में आया जो कुछ मर्म,
उसे कहना था मेरा धर्म।
न था यह मेरा अपना कृत्य;
भर्तृ हैं भर्तृ, भृत्य हैं भृत्य।"
मही पर अपना माथा टेक,
भरा था जिसमें अति अविवेक,
किया दासी ने उसे प्रणाम,
और वह चली गई अविराम।
गई दासी, पर उसकी बात
दे गई मानों कुछ आघात