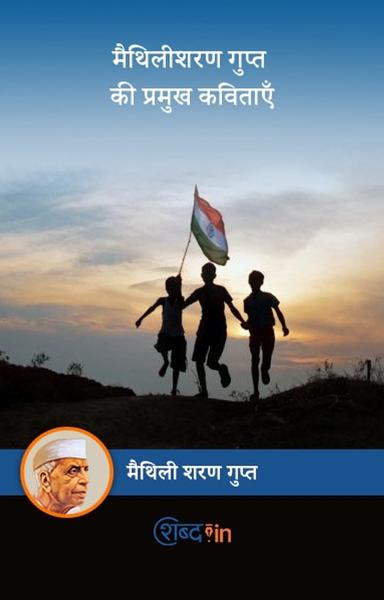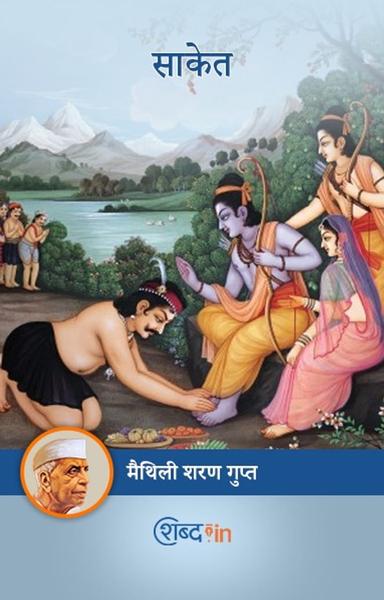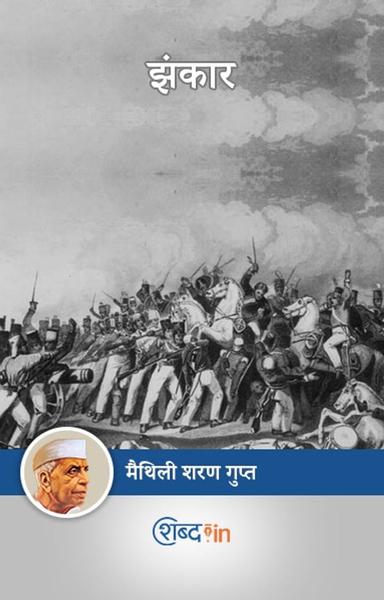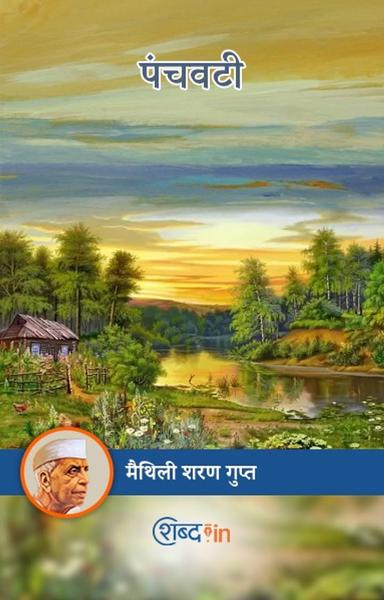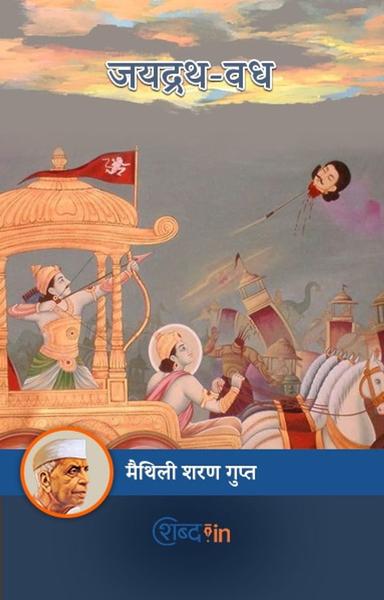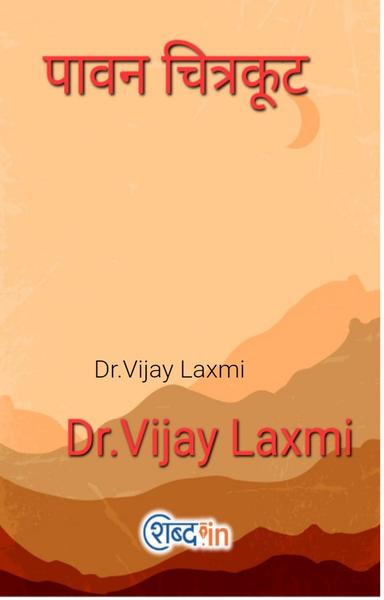"जय गंगे, आनंद-तरंगे, कलरवे,
अमल अंचले, पुण्यजले, दिवसम्भवे!
सरस रहे यह भरत-भूमि तुमसे सदा;
हम सबकी तुम एक चलाचल सम्पदा।
दरस-परस की सुकृत-सिद्धि ही जब मिली,
माँगे तुमसे आज और क्या मैथिली?
बस, यह वन की अवधि यथाविधि तर सकूँ,
समुचित पूजा-भेट लौट कर कर सकूँ।"
उद्भासित थी जह्नुनन्दिनी मोद में,
किरण-मूर्तियाँ खेल रही थीं गोद में।
वैदेही थीं झलक झलक पर झूमती,
त्रिविधपवनगति अलक-पलक थी चूमती।
बोले तब प्रभु, परम पुण्य पथ के पथी
"निज कुल की हो कीर्ति प्रिये, भागीरथी।"
"तुम्हीं पार कर रहे आज किसको अहो!"-
सीता ने हँस कहा--"क्यों न देवर, कहो?"
"है अनुगामीमात्र देवि, यह दास तो!"
गुह बोला--"परिहास बना वन-वास तो!"
वहाँ हर्ष के साथ कूतुहल छा गया,
नाव चली या स्वयं पार ही आ गया!
"मिलन-स्मृति-सी रहे यहाँ यह क्षुद्रिका,"
सीता देने लगीं स्वर्णमणि-मुद्रिका।
गुह बोला कर जोड़ कि-"यह कैसी कृपा?
न हो दास पर देवि, कभी ऐसी कृपा।
क्षमा करो, इस भाँति न तुम तज दो मुझे;
स्वर्ण नहीं, हे राम, चरण-रज दो मुझे।
जड़ भी चेतन मूर्ति हुई पाकर जिसे,
उसे छोड़ पाषाण भला भावे किसे?"
उसे हृदय से लगा लिया श्रीराम ने,
ज्यों-त्यों करके बिदा किया धी-धाम ने।
पथ में सब के प्रीति-हर्ष-विस्मय बनें,
तीर्थराज की ओर चले तीनों जनें।
कहीं खड़े थे खेत, कहीं प्रान्तर पड़े;
शून्य सिन्धु के द्वीप गाँव छोटे-बड़े।
पथ के प्रहरी वृक्ष झूमते थे कहीं,
खग-मृग चरते हुए घूमते थे कहीं।
छोटी-मोटी कहीं कहीं थी झाड़ियाँ,
बनी शशादिक हेतु प्राकृतिक बाड़ियाँ।
पगडंडी थी गई मार्ग से ठीक यों--
शास्त्र छोड़ बन जाय लोक की लीक ज्यों।
टीले दीखे कहीं और भरके कहीं,
दृश्य बावड़ी, कूप और सर के कहीं।
पथ-पार्श्वों में मिले पथिक-चत्वर उन्हें,
कौतूहल ने हरा किया सत्वर उन्हें।
चरणों पर कर और मुखों पर बिन्दु थे,
रजःपूर्ण थे पद्म, अमृतयुत इन्दु थे।
देख घटा-सी पड़ी एक छाया घनी,
ठहर गये कुछ काल वहाँ कोसलधनी।
"तुम दोनों क्या नहीं थके? मैं ही थकी?"
सीता कुछ भी और न आगे कह सकी।
हँसते हँसते सती अचानक रो पड़ी,
तप्त हेम की मूर्ति द्रवित-सी हो पड़ी।
"मुझको अपने लिए नहीं कुछ सोच है।
तुम्हें असुविधा न हो, यही संकोच है।"
"प्रिये, हमारे लिये न तुम चिन्ता करो,
अभी नया अभ्यास, तनिक धीरज धरो।"
जुड़ आई थीं वहाँ नारियाँ ग्राम की,
वे साधक ही सिद्ध हुईं विश्राम की।
सीता सब से प्रेम-भावपूर्वक मिलीं,
लतिकाओं में कुसुमकली-सी वे खिलीं।
"शुभे, तुम्हारे कौन उभय ये श्रेष्ठ हैं?"
"गोरे देवर, श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं।"
वैदेही यह सरल भाव से कह गईं,
तब भी वे कुछ तरल हँसी हँस रह गईं।
यों स्वच्छन्द विराम लाभ करते हुए,
मार्ग-जनों में भूरिभाव भरते हुए,
पर दिन तीनों तीर्थराज में आ गये,
द्विगुण पर्व-सा भरद्वाज मुनि पा गये।
स्वयं त्रिवेणी धन्य हुईं उन तीन से,
बोल उठे सौमित्रि अमृत में लीन-से
"देखो भाभी, तीर्थराज की यह छटा,
वर्षा से आ मिली शरद् की-सी घटा।"
हँस कर बोलीं जनकसुता सस्नेह यों
"श्याम-गौर तुम एक प्राण, दो देह ज्यों!"
रामानुज ने कहा कि "भाभी, क्यों नहीं,
सरस्वती-सी प्रकट जहाँ तुम हो रहीं!"
"देवर, मेरी सरस्वती अब है कहाँ?
संगम-शोभा निरख निमग्न हुई यहाँ!
धूप-छाँह का वस्त्र मात्र उसका बड़ा,
मन्द पवन से लहर रहा है यह पड़ा!"
प्रभु बोले--"यह गीत-काव्य-चित्रावली!
तुम माई के लाल! जनक की वे लली!
अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला,
किन्तु आप अनुभूति यहाँ है निश्चला!
तुम ये दो दो कलाकार जीते रहो,
मुझे प्रशंसा कठिन एक की भी अहो!
सुनों, मिलन ही महातीर्थ संसार में,
पृथ्वी परिणत यहीं एक परिवार में;
एक तीसरे हुए मिले जब दो जहाँ,
गंगा-जमुना बनीं त्रिवेणी ज्यों यहाँ।
त्याग और अनुराग चाहिए बस, यही।"
भरद्वाज ने कहा--"भरा तुम में वही।