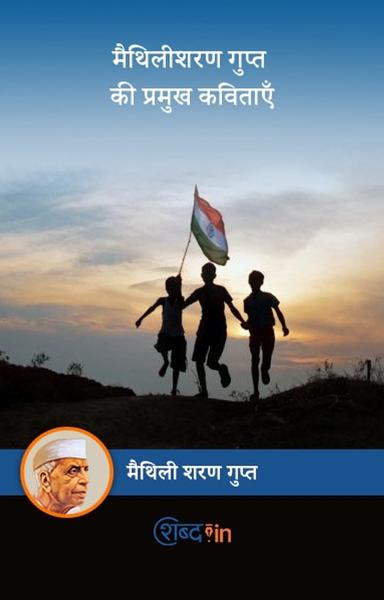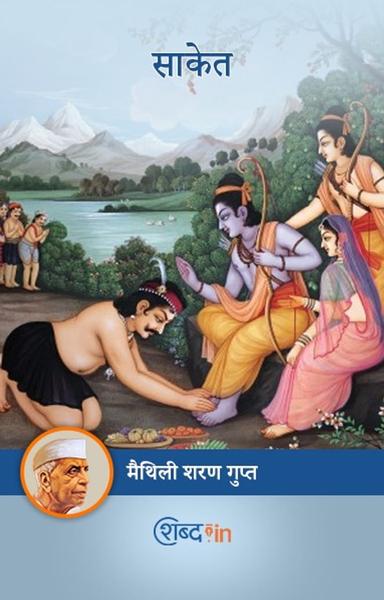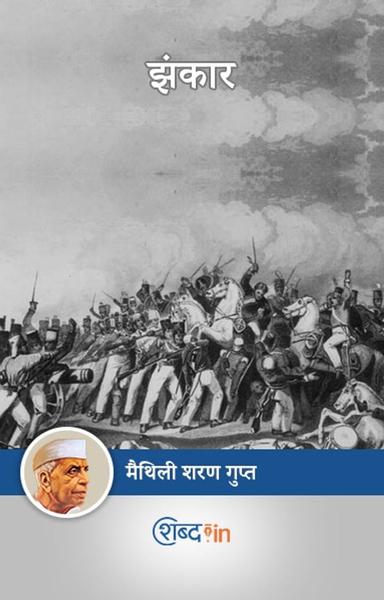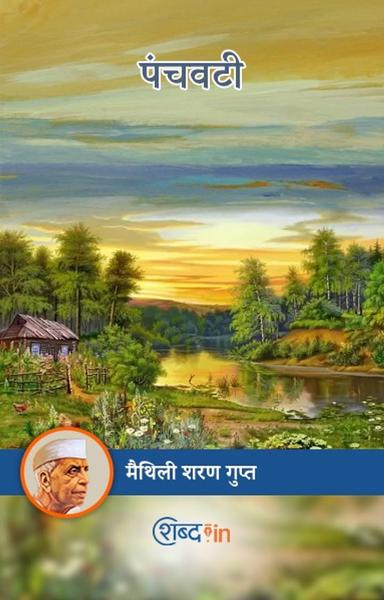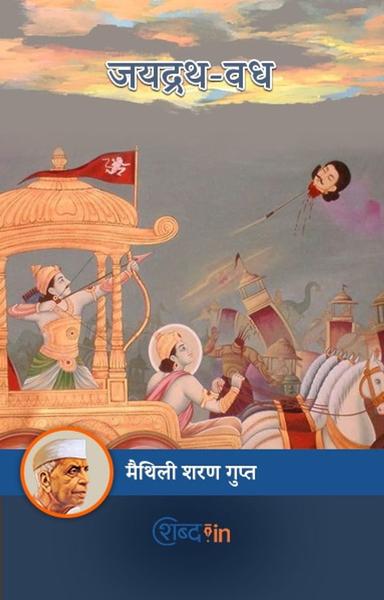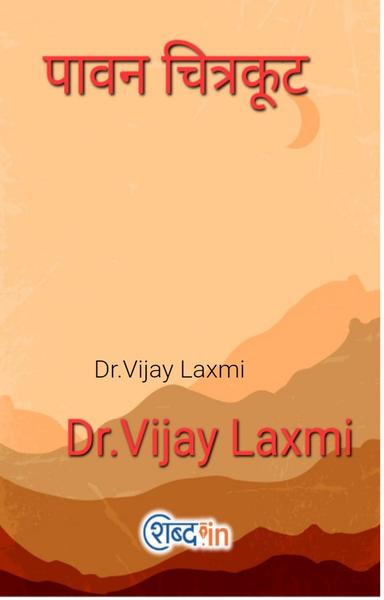वनदेवीगण, आज कौन सा पर्व है,
जिस पर इतना हर्ष और यह गर्व है?
जाना, जाना, आज राम वन आ रहे;
इसी लिए सुख-साज सजाये जा रहे।
तपस्वियों के योग्य वस्तुओं से सजा,
फहराये निज भानु-मूर्तिवाली ध्वजा,
मुख्य राजरथ देख समागत सामने,
गुरु को पुनः प्रणाम किया श्रीराम ने।
प्रभु-मस्तक से गये जहाँ गुरु-पद छुए,
चोटी तक वे हृष्टरोम गद्गद हुए।
बोल उठे,-"हम आज सु-गौरव-युत हुए,
सुत, तुम वल्कल पहन, शिष्य से सुत हुए!"
प्रभु बोले--"बस, यही राम को इष्ट है,
क्योंकि पिता के लिए प्रतीत अरिष्ट है।
त्रिकालज्ञ हैं आप, आपकी बात से,
हुए भविष्यच्चिन्ह मुझे भी ज्ञात-से।
जो हो, व्याकुल आज प्रजा-परिवार है,
उन सबका अब सभी आप पर भार है।
माँ मुझको फिर देख सकें, जैसे सही,
पितः, पुत्र की प्रथम याचना है यही।"
भाव देख उन एक महा व्रतनिष्ठ के,
भर आये युग नेत्र वरिष्ठ वसिष्ठ के।
कहा उन्होंने-"वत्स, चाहता हूँ, अभी
किन्तु नहीं, कल्याण इसीमें हैं सभी।
देवकार्य हो और उदित आदर्श हो;
उचित नहीं फिर मुझे कि क्षोभ-स्पर्श हो।
मुनि-रक्षक-सम करो विपिन में वास तुम;
मेटो तप के विघ्न और सब त्रास तुम।
हरो भूमि का भार भाग्य से लभ्य तुम,
करो आर्य-सम वन्यचरों को सभ्य तुम।"
"जो-आज्ञा" कह रामचन्द्र आगे बढ़े,
उदयाचल पर सूर्य-तुल्य रथ पर चढ़े।
रुदित जनों को छोड़ बैठ उसमें भले,
सीता-लक्ष्मण-सहित राम वन को चले।
प्रजा वर्ग के नेत्र-नीर से पथ सिंचा,
रुकता रुकता महा भीड़ में रथ खिंचा।
सूर्योद्भासित कनक-कलश पर केतु था,
वह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था?
कहता-सा था दिखा दिखाकर कर-कला,
यह जंगम-साकेत-देव-मन्दिर चला!
सुन कैकेयी-कर्म, जिसे लज्जा हुई,
पाकर मानों ताप गलित मज्जा हुई,
वैदेही को देख बधू-गण बच गया।
कोलाहल युग भावपूर्ण तब मच गया।
उभय ओर थीं खड़ीं नगर-नर-नारियाँ,
बरसाती थीं साश्रु सुमन सुकुमारियाँ।
करके जय जयकार राम का, धर्म का,
करती थीं अपवाद केकयी-कर्म का।
"जहाँ हमारे राम, वहीं हम जायँगे।
वन में ही नव-नगर-निवास बनायँगे।
ईंटों पर अब करें भरत शासन यहाँ!"
जन-समूह ने किया महा कलकल वहाँ।
"हर कर प्रभु का राज्य कठोरा केकयी,
प्रजा-प्रीति भी हरण करे अब यह नई।"
भाभी को यह भाव जताने के लिए,
लक्ष्मण ने निज नेत्र उधर प्रेरित किये।
वैदेही में पुलक भाव था भर रहा,
प्रियगुणानुभव रोम रोम था कर रहा।
कैकेयी का स्वार्थ, राम का त्याग था,
परम खेद था और चरम अनुराग था।
राम-भाव अभिषेक-समय जैसा रहा,
वन जाते भी सहज सौम्य वैसा रहा।
वर्षा हो या ग्रीष्म, सिन्धु रहता वही,
मर्यादा की सदा साक्षिणी है मही।
सत्य-धर्म का श्रेष्ठ भाव भरते हुए,
जन-समूह को स्वयं शान्त करते हुए,
विपिनातुर वे किसी भाँति आगे बढ़े,
पहुँचे रथ से प्रथम, मनोरथ पर चढ़े।
रखकर उनके वचन, लौटते लोग थे;
पाते तत्क्षण किन्तु विशेष वियोग थे।
जाते थे फिर वहीं टोल के टोल यों
आते-जाते हुए जलधि-कल्लोल ज्यों।
सम्बोधन कर पौरजनों को प्रीति से,
बोले हँस कर राम यथोचित रीति से
"रोकर ही क्या बिदा करोगे सब हमें?
आना होगा नहीं यहाँ क्या अब हमें?
लौटो तुम सब, यथा समय हम आयँगें;
भाव तुम्हारे साथ हमारे जायँगें!
पहुँचाते हैं दूर उसी को शोक में
जिससे मिलना हो न सके फिर लोक में।"
बोल उठे जन--"भद्र, न ऐसा तुम कहो,
देते हैं हम तुम्हें बिदा ही कब अहो!
राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना;
करो न तुम यों हाय! लोकमत अनसुना।
जाओ, यदि जा सको रौंद हमको यहाँ!"
यों कह पथ में लेट गये बहु जन वहाँ।
अश्व अड़े-से खड़े उठाये पैर थे,
क्योंकि समझते प्रेम और वे वैर थे।
ऊँचा कर कुछ वक्ष कन्धरा-संग में,
शंखालोड़न यथा उदग्र तरंग में
करता है गम्भीर अन्बुनिधि नाद ज्यों,
बोले श्रीमद्रामचन्द्र सविषाद यों
"उठो प्रजा-जन, उठो, तजो यह मोह तुम;
करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम?
तुम से प्यारा कौन मुझे? कातर न हो;
मैं अपना भी त्याग करूँ तुम पर कहो?
सोचो तुम सम्बन्ध हमारा नित्य का,
जब से भव में उदय आदि आदित्य का।
प्रजा नहीं, तुम प्रकृति हमारी बन गये;
दोनों के सुख-दुःख एक में सन गये।
मैं स्वधर्म से विमुख नहीं हूँगा कभी,
इसी लिए तुम मुझे चाहते हो सभी।