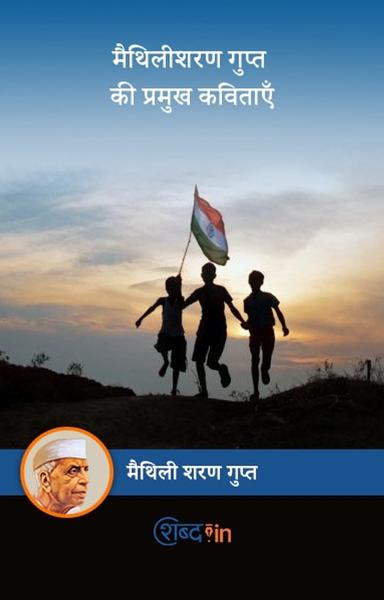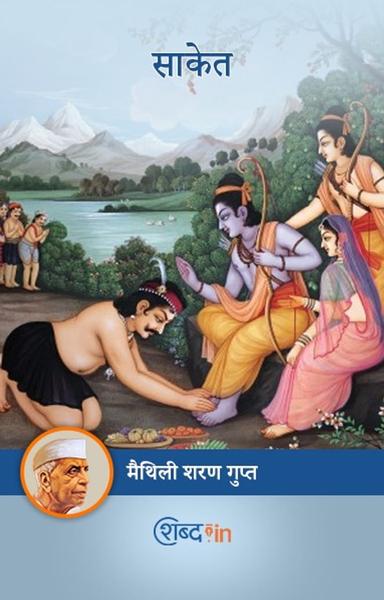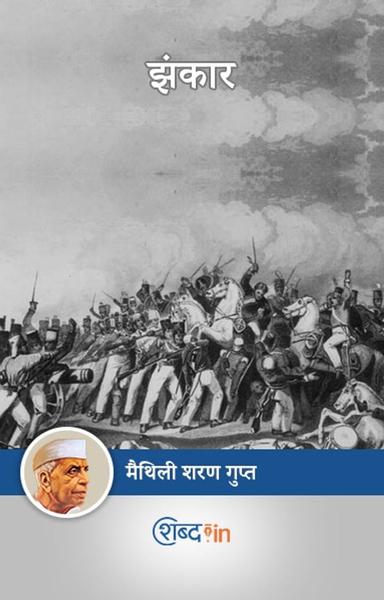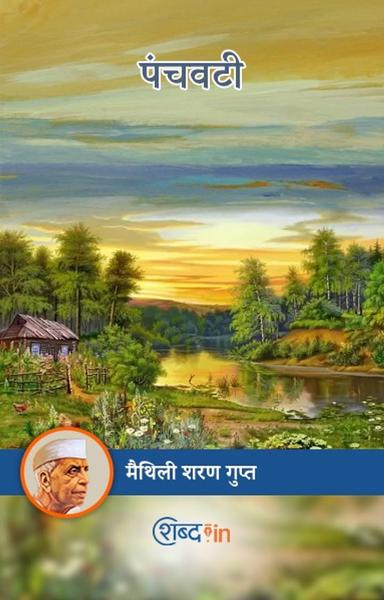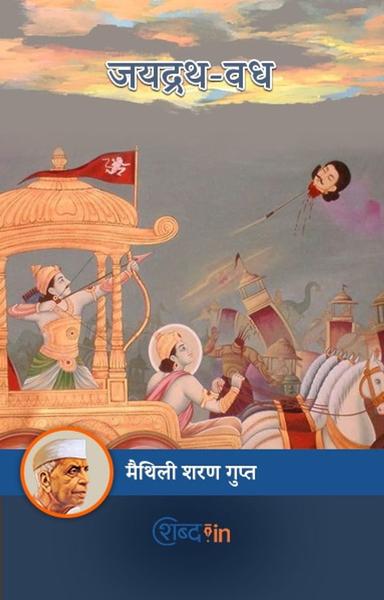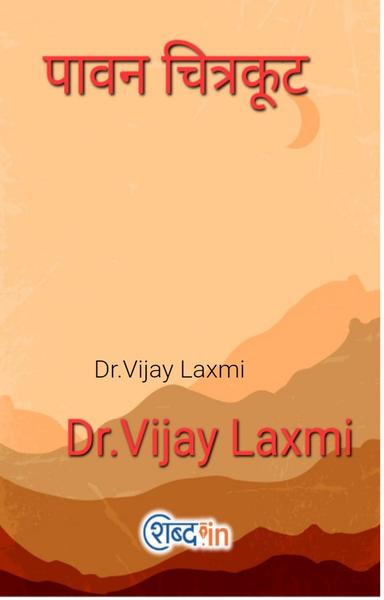’अपनी जगती अधीन-सी
चरणों में चुपचाप लीन-सी!’
निकली उनकी उसाँस-सी,
उसने दी यह एक आँस-सी
’उनकी पद-धूलि जो धरूँ,
न अहल्या-अपकीर्ति से ड़रूँ!’
मुझको कुछ आत्म-गर्व था;
क्षण में ही अब सर्व खर्व था।
नत थी यह देह सर्वथा,
सरयू, सिन्धु-समीप तू यथा।
झषकेतन-केतु नम्र थे,
(तब ये लोचन मीन-कम्र थे!)
विजयी वर थे विनीत क्या,
हम हारीं, पर तुच्छ जीत क्या?
वर आकर धीर-वीर-से,
सहसा लौट गये गभीर-से।
सुनस्फुट हाथ में गये,
मन पैरों पड़ साथ में गये।
कुछ मर्मर-पूर्ण मर्म था,
श्रम क्या था, पर हाय! धर्म था।
यह कण्टक-पूर्ण चर्म था,
गद-सा गद्गद प्रेम धर्म था!
वह अल्हड़ बाल्य क्या हुआ?
नयनों में कुछ नीर-सा चुआ।
इस यौवन ने मुझे धरा,
नव संकोच भरा, भरा, भरा!
दिखला कर दृश्य ही नया
यह संसार समक्ष आ गया।
करता रव दूर द्रोण था,
मुझको इच्छित एक कोण था।
तिरछी यह दृष्टि हो उठी,
तकती-सी सब सृष्टि हो उठी।
मन मोहित-सा विमूढ़ था,
प्रकटा कौन रहस्य गूढ़ था?
घर था भरपूर पूर्व-सा,
पर विश्राम सुदूर पूर्व-सा।
मन में कुछ क्या अभाव था?
तन में भी अब कौन हाव था?
यह देह-लता छुई-मुई,
निशि आई, पर नींद क्या हुई?
जिसका यह भूरि भोग था,
वह था जो पहला वियोग था!
चुपचाप गवाक्ष खोल के,
अपने आप नवाक्ष खोल के,
निशि का शशि देखने लगी,
सब सोये, पर मैं जगी-जगी!
जब थे सब जागने लगे,
दब रात्रिचर भागने लगे,
निशि हार उतारने लगी,
तब मैं स्वप्न निहारने लगी।
फट पौ उर थी दिखा रही,
कलि, यों फूट, यही सिखा रही!
बढ़ दीपक की शिखा रही;
अलि-लेखा नलिनी लिखा रही।
कलिकावलि फूटने लगी;
अलि-आली उड़ टूटने लगी।
नभ की मसि छूटने लगी;
हरियाली हिम लूटने लगी।
विहगावलि बोलने लगी;
यह प्राची पट खोलने लगी;
अटवी हिल डोलने लगी;
सरसी सौरभ घोलने लगी।
मिलती यह थी स्वकोक थे
हत कोकी बच दुःख-शोक से।
वह सूर्य्यमुखी प्रसन्न थी;
फिर भी चेतन सृष्टि सन्न थी।
अविलोड़ित था जमा दही,
तिमिराम्भोधि-समुद्घृता मही।
मृदु वायु विहारने लगी,
तब मैं स्वप्न निहारने लगी।
वह स्वप्न कि सत्य, क्या कहूँ?
सरयू, तू बह और मैं बहूँ।
प्रकटी प्रिय-मूर्त्ति मोदिता,
कब सोई यह दृष्टि रोदिता!
यह मानस लास्य-पूर्ण था,
वह पद्मानन हास्य-पूर्ण था,
झड़ता उड़ अंशु-चूर्ण था,
सरिते, सम्मुख स्वर्ग-घूर्ण था।
अब भी यह देह की लता
कितनी कण्टकिता-नता-हता!
कँपते बस अंध्रि-वेत्र थे,
नत भी हो सकते न नेत्र थे।
अयि चेतन-वृत्ति निष्क्रिये!
हँस बोले प्रिय प्रेम से-’प्रिये!’
प्रति रोम स्वतन्त्र तन्त्र-था,
बजता जो सुन सिद्धि-मन्त्र था।
तटिनी, यह तुच्छ किंकरी
सुख से क्यों न, बता, वहीं मरी?
वह जीवन का निमेष था,
पर आगे यह काल शेष था!
कितनी उस इन्दु में सुधा,
सरयू, मैं कहती नहीं मुधा।
वह रूप-पयोधि पी सकी,
तब तो मैं यह आज जी सकी।