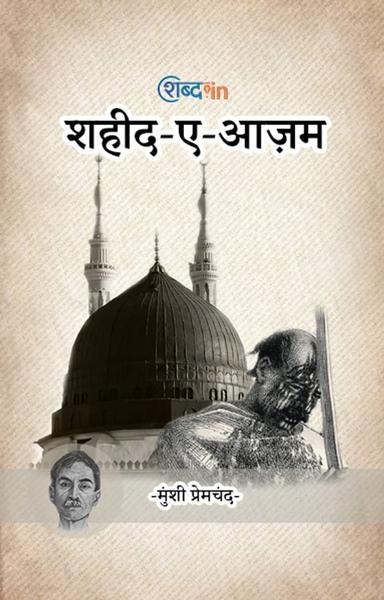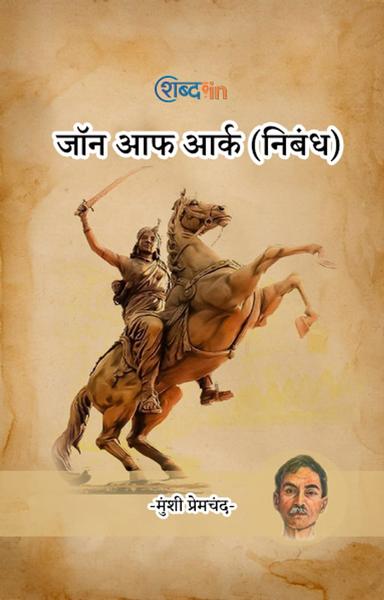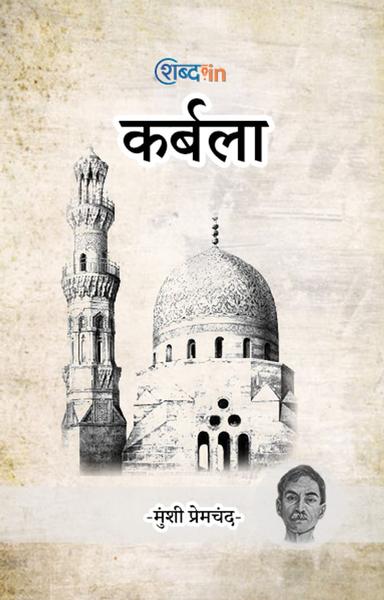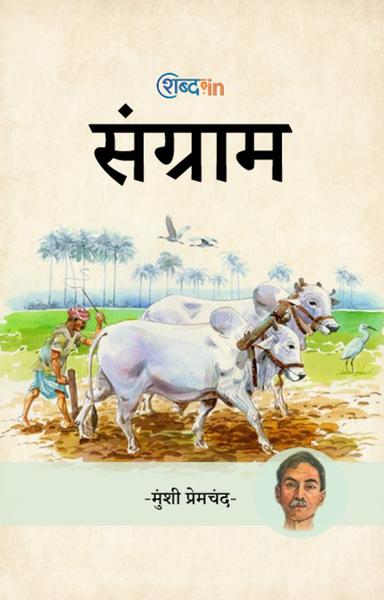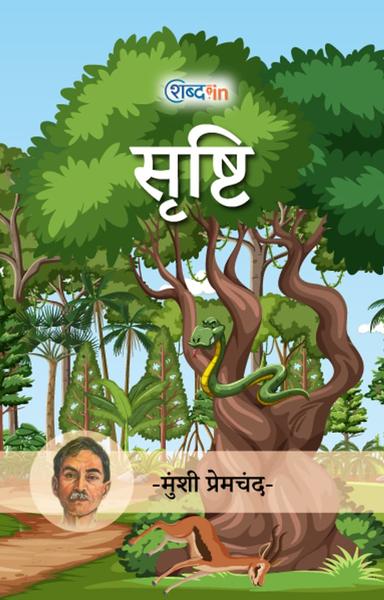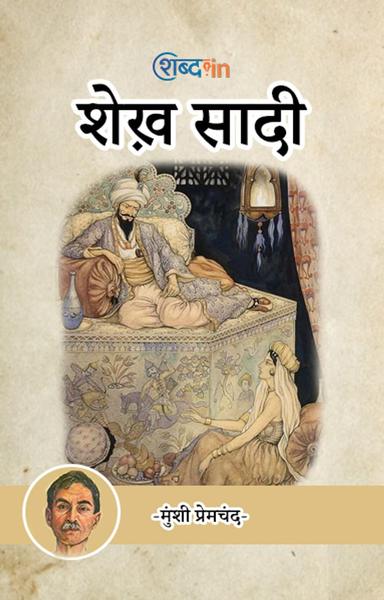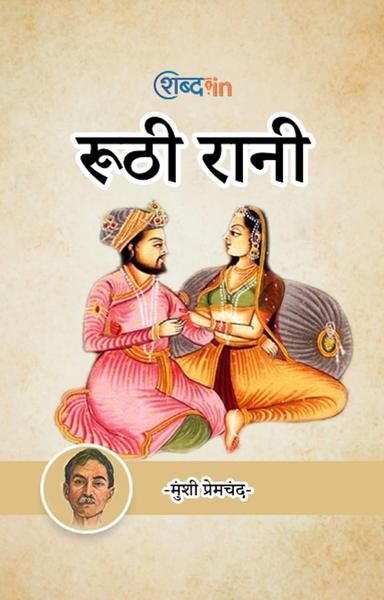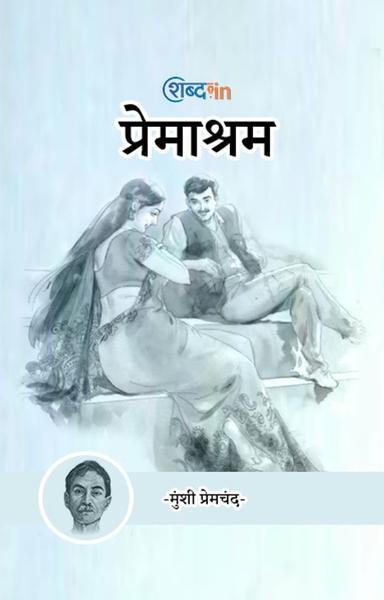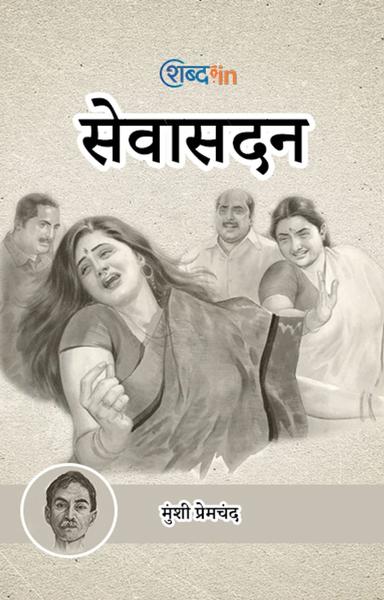संतकुमार यहाँ से चले तो उनका हृदय आकाश में था। इतनी जल्दी देवी से उन्हें वरदान मिलेगा इसकी उन्होंने आशा न की थी। कुछ तकदीर ने ही जोर मारा, नहीं तो जो युवती अच्छे-अच्छों को उँगलियों पर नचाती है, उन पर क्यों इतनी भक्ति करती। अब उन्हें विलंब न करना चाहिए। कौन जाने कब तिब्बी विरुद्ध हो जाए और यह दो ही चार मुलाकातों में होनेवाला है। तिब्बी उन्हें कार्य-क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा करेगी और वह पीछे हटेंगे। वहीं मतभेद हो जाएगा। यहाँ से वह सीधे मि. सिन्हा के घर पहुँचे। शाम हो गई थी। कुहरा पड़ना शुरू हो गया था। मि. सिन्हा सजे-सजाए कहीं जाने को तैयार खड़े थे। इन्हें देखते ही पूछा -
– किधर से?
– वहीं से। आज तो रंग जम गया।
– सच।
– हाँ जी। उस पर तो जैसे मैंने जादू की लकड़ी फेर दी हो।
– फिर क्या, बाजी मार ली है। अपने फादर से आज ही जिक्र छेड़ो।
– आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा।
– हाँ, हाँ मैं तो चलूँगा ही मगर तुम तो बड़े खुशनसीब निकले – यह मिस कामत तो मुझसे सचमुच आशिकी कराना चाहती है। मैं तो स्वाँग रचता हूँ। और वह समझती है, मैं उसका सच्चा प्रेमी हूँ। जरा आजकल उसे देखो, मारे गरूर के जमीन पर पाँव ही नहीं रखती। मगर एक बात है, औरत समझदार है। उसे बराबर यह चिंता रहती है मैं उसके हाथ से निकल न जाऊँ, इसलिए मेरी बड़ी खातिरदारी करती है, और बनाव-सिंगार से कुदरत की कमी जितनी पूरी हो सकती है उतनी करती है। और अगर कोई अच्छी रकम मिल जाए तो शादी कर लेने ही में क्या हरज है।
संतकुमार को आश्चर्य हुआ – तुम तो उसकी सूरत से बेजार थे।
– हाँ, अब भी हूँ, लेकिन रुपए की जो शर्त है। डॉक्टर साहब बीस-पच्चीस हजार मेरी नजर कर दें, शादी कर लूँ। शादी कर लेने से में उसके हाथ में बिका तो नहीं जाता।
दूसरे दिन दोनों मित्रों ने देवकुमार के सामने सारे मंसूबे रख दिए। देवकुमार को एक क्षण तक तो अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उन्होंने स्वच्छंद, निर्भीक, निष्कपट जिंदगी व्यतीत की थी। कलाकारों में एक तरह का जो आत्माभिमान होता है, उसने सदैव उनको ढाढ़स दिया था। उन्होंने तकलीफें उठाई थीं, फाके भी किए थे, अपमान सहे थे, लेकिन कभी अपनी आत्मा को कलुषित न किया था। जिंदगी में कभी अदालत के द्वार तक ही नहीं गए। बोले – मुझे खेद होता है कि तुम मुझसे यह प्रस्ताव कैसे कर सके और इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि ऐसी कुटिल चाल तुम्हारे मन में आई क्योंकर।
संत कुमार ने निस्संकोच भाव से कहा – जरूरत सब कुछ सिखा देती है। स्वरक्षा प्रकृति का पहला नियम है। वह जायदाद जो आपने बीस हजार में दे दी, आज दो लाख से कम की नहीं है।
– वह दो लाख की नहीं, दस लाख की हो, मेरे लिए वह आत्मा को बेचने का प्रश्न है। मैं थोड़े-से रुपयों के लिए अपनी आत्मा नहीं बेच सकता।
दोनों मित्रों ने एक-दूसरे की ओर देखा और मुस्कराए। कितनी पुरानी दलील है। और कितनी लचर। आत्मा जैसी चीज है कहाँ? और जब सारा संसार धोखेधड़ी पर चल रहा है तो आत्मा कहाँ रही? अगर सौ रुपए कर्ज दे कर एक हजार वसूल करना अधर्म नहीं है, अगर एक लाख नीमजान, फाकेकश मजदूरों की कमाई पर एक सेठ का चैन करना अधर्म नहीं है तो एक पुरानी कागजी कार्रवाई को रद्द कराने का प्रयत्न क्यों अधर्म हो?
संतकुमार ने तीखे स्वर में कहा – अगर आप इसे आत्मा का बेचना कहते हैं तो बेचना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। और आप इस दृष्टि से इस मामले को देखते ही क्यों है? धर्म वह है जिससे समाज का हित हो। अधर्म वह है जिससे समाज का अहित हो। इससे समाज का कौन-सा अहित हो जाएगा, यह आप बता सकते हैं?
देवकुमार ने सतर्क हो कर कहा – समाज अपनी मर्यादाओं पर टिका हुआ है। उन मर्यादाओं को तोड़ दो और समाज का अंत हो जाएगा।
दोनों तरफ से शास्त्रार्थ होने लगे। देवकुमार मर्यादाओं और सिद्धांतों और धर्म-बंधनों की आड़ ले रहे थे,, पर इन दोनों नौजवानों की दलीलों के सामने उनकी एक न चलती थी। वह अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर-फेर कर और खल्वाट सिर खुजा-खुजा कर जो प्रमाण देते थे, उसको यह दोनों युवक चुटकी बजाते धुन डालते थे, धुनक कर उड़ा देते थे।
सिन्हा ने निर्दयता के साथ कहा – बाबूजी, आप न जाने किस जमाने की बातें कर रहे हैं। कानून से हम जितना फायदा उठा सकें, हमें उठाना चाहिए। उन दफों का मंशा ही यह है कि उनसे फायदा उठाया जाए। अभी आपने देखा जमींदारों की जान महाजनों से बचाने के लिए सरकार ने कानून बना दिया है। और कितनी मिल्कियतें जमींदारों को वापस मिल गईं। क्या आप इसे अधर्म कहेंगे? व्यावहारिकता का अर्थ यही है कि हम इन कानूनी साधनों से अपना काम निकालें। मुझे कुछ लेना-देना नहीं, न मेरा कोई स्वार्थ है। संत कुमार मेरे मित्र हैं और इसी वास्ते मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ। मानें या न मानें, आपको अख्तियार है।
देवकुमार ने लाचार हो कर कहा – तो आखिर तुम लोग मुझे क्या करने को कहते हो?
– कुछ नहीं, केवल इतना ही कि हम जो कुछ करें आप उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई न करें।
- मैं सत्य की हत्या होते नहीं देख सकता।
संतकुमार ने आँखें निकाल कर उत्तेजित स्वर में कहा – तो फिर आपको मेरी हत्या देखनी पड़ेगी।
सिन्हा ने संतकुमार को डाँटा – क्या फजूल की बातें करते हो, संत कुमार! बाबू जी को दो-चार दिन सोचने का मौका दो। तुम अभी किसी बच्चे के बाप नहीं हो। तुम क्या जानो बाप को बेटा कितना प्यारा होता है। वह अभी कितना ही विरोध करें, लेकिन जब नालिश दायर हो जाएगी तो देखना वह क्या करते हैं। हमारा दावा यही होगा कि जिस वक्त आपने यह बैनामा लिखा, आपके होश-हवास ठीक न थे, और अब भी आपको कभी-कभी जुनून का दौरा हो जाता है। हिंदुस्तान जैसे गर्म मुल्क में यह मरज बहुतों को होता है, और आपको भी हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं। हम सिविल सर्जन से इसकी तसदीक करा देंगे।
देवकुमार ने हिकारत के साथ कहा – मेरे जीते-जी यह धाँधली नहीं हो सकती। हरगिज नहीं। मैंने जो कुछ किया सोच-समझ कर और परिस्थितियों के दबाव से किया। मुझे उसका बिलकुल अफसोस नहीं है। अगर तुमने इस तरह का कोई दावा किया तो उसका सबसे बड़ा विरोध मेरी ओर से होगा, मैं कहे देता हूँ।
और वह आवेश में आ कर कमरे में टहलने लगे।
संतकुमार ने भी खड़े हो कर धमकाते हुए कहा – तो मेरा भी आपको चैलेंज है - या तो आप अपने धर्म ही की रक्षा करेंगे या मेरी। आप फिर मेरी सूरत न देखेंगे।
– मुझे अपना धर्म, पत्नी और पुत्र सबसे प्यारा है।
सिन्हा ने संत कुमार को आदेश किया – तुम आज दर्खास्त दे दो कि आपके होश-हवास में फर्क आ गया और मालूम नहीं आप क्या कर बैठें। आपको हिरासत में ले लिया जाए।
देवकुमार ने मुट्ठी तान कर क्रोध के आवेश में पूछा – मैं पागल हूँ?
– जी हाँ, आप पागल हैं। आपके होश बजा नहीं हैं। ऐसी बातें पागल ही किया करते हैं। पागल वही नहीं है जो किसी को काटने दौड़े। आम आदमी जो व्यवहार करते हों उसके विरुद्ध व्यवहार करना भी पागलपन है।
– तुम दोनों खुद पागल हो।
– इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा।
– मैंने बीसों पुस्तकें लिख डालीं, हजारों व्याख्यान दे डाले, यह पागलों का काम है?
– जी हाँ, यह पक्के सिरफिरों का काम है। कल ही आप इस घर में रस्सियों से बाँध लिए जाएँगे।
– तुम मेरे घर से निकल जाओ नहीं तो मैं गोली मार दूँगा।
– बिलकुल पागलों की-सी धमकी। संतकुमार, उस दर्खास्त में यह भी लिख देना कि आपकी बंदूक छीन ली जाए, वरना जान का खतरा है।
और दोनों मित्र उठ खड़े हुए। देवकुमार कभी कानून के जाल में न फँसे थे। प्रकाशकों और बुकसेलरों ने उन्हें बारहा धोखे दिए, मगर उन्होंने कभी कानून की शरण न ली। उनके जीवन की नीति थी – आप भला तो जग भला, और उन्होंने हमेशा इस नीति का पालन किया था, मगर वह दब्बू या डरपोक न थे। खासकर सिद्धांत के मुआमले में तो वह समझौता करना जानते ही न थे। वह इस षडयंत्र में कभी शरीक न होंगे, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मगर क्या यह सब सचमुच उन्हें पागल साबित कर देंगें? जिस दृढ़ता से सिन्हा ने धमकी दी थी वह उपेक्षा के योग्य न थी। उसकी ध्वनि से तो ऐसा मालूम होता था कि वह इस तरह के दाँव-पेंच में अभ्यस्त है, और शायद डॉक्टरों को मिला कर सचमुच उन्हें सनकी साबित कर दे। उनका आत्माभिमान गरज उठा – नहीं, वह असत्य की शरण न लेंगे चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी सहना पड़े। डॉक्टर भी क्या अंधा है? उनसे कुछ पूछेगा, कुछ बातचीत करेगा या यों ही कलम उठा कर उन्हें पागल लिख देगा। मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके होश-हवास में फितूर पड़ गया हो। हुश। वह भी इन छोकरों की बातों में आए जाते हैं। उन्हें अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उनकी बुद्धि सूर्य के प्रकाश की भाँति निर्मल है। कभी नहीं। वह इन लौंडों के धौंस में न आएँगे।
लेकिन यह विचार उनके हृदय को मथ रहा था कि संतकुमार की यह मनोवृत्ति कैसे हो गई। उन्हें अपने पिता की याद आती थी। वह कितने सौम्य, कितने सत्यनिष्ठ थे। उनके ससुर वकील जरूर थे, पर कितने धर्मात्मा पुरुष थे। अकेले कमाते थे, और सारी गृहस्थी का पालन करते थे। पाँच भाइयों और उनके बाल-बच्चों का बोझा खुद सँभाले हुए थे। क्या मजाल कि अपने बेटे-बेटियों के साथ उन्होंने किसी तरह का पक्षपात किया हो। जब तक बड़े भाई को भोजन न करा लें खुद न खाते थे। ऐसे खानदान में संतकुमार जैसा दगाबाज कहाँ से धँस पड़ा? उन्हें कभी ऐसी कोई बात याद न आती थी जब उन्होंने अपनी नीयत बिगाड़ी हो।
लेकिन यह बदनामी कैसे सही जाएगी। वह अपने ही घर में जब जागृति न ला सके तो एक प्रकार से उनका सारा जीवन नष्ट हो गया। जो लोग उनके निकटतम संसर्ग में थे, जब उन्हें वह आदमी न बना सके तो जीवन-पर्यंत की साहित्य-सेवा से किसका कल्याण हुआ? और जब यह मुकदमा दायर होगा उस वक्त वह किसे मुँह दिखा सकेंगे? उन्होंने धन न कमाया, पर यश तो संचय किया ही। क्या वह भी उनके हाथ से छिन जाएगा? उनको अपने संतोष के लिए इतना भी न मिलेगा? ऐसी आत्मवेदना उन्हें कभी न हुई थी।
शैव्या से कह कर वह उसे भी क्यों दुखी करें? उसके कोमल हृदय को क्यों चोट पहुँचाएँ? वह सब कुछ खुद झेल लेंगे। और दुखी होने की बात भी क्यों हो? जीवन तो अनुभूतियों का नाम है। यह भी एक अनुभव होगा। जरा इसकी भी सैर कर लें।
यह भाव आते ही उनका मन हलका हो गया। घर में जा कर पंकजा से चाय बनाने को कहा।
शैव्या ने पूछा – संतकुमार क्या कहता था?
उन्होंने सहज मुस्कान के साथ कहा – कुछ नहीं, वही पुराना खब्त।
– तुमने तो हामी नहीं भरी न?
देवकुमार स्त्री से एकात्मता का अनुभव करके बोले – कभी नहीं।
– न जाने इसके सिर यह भूत कैसे सवार हो गया।
– सामाजिक संस्कार हैं और क्या?
– इसके यह संस्कार क्यों ऐसे हो गए? साधु भी तो है, पंकजा भी तो है, दुनिया में क्या धर्म ही नहीं?
– मगर कसरत ऐसे ही आदमियों की है, यह समझ लो।
उस दिन से देवकुमार ने सैर करने जाना छोड़ दिया। दिन-रात घर में मुँह छिपाए बैठे रहते। जैसे सारा कलंक उनके माथे पर लगा हो। नगर और प्रांत के सभी प्रतिष्ठित, विचारवान आदमियों से उनका दोस्ताना था, सब उनकी सज्जनता का आदर करते थे। मानो वह मुकदमा दायर होने पर भी शायद कुछ न कहेंगे। लेकिन उनके अंतर में जैसे चोर-सा बैठा हुआ था। वह अपने अहंकार में अपने को आत्मीयों की भलाई-बुराई का जिम्मेदार समझते थे। पिछले दिनों जब सूर्यग्रहण के अवसर पर साधुकुमार ने बढ़ी हुई नदी में कूद कर एक डूबते हुए आदमी की जान बचाई थी, उस वक्त उन्हें उससे कहीं ज्यादा खुशी हुई थी जितनी खुद सारा यश पाने से होती। उनकी आँखों में आँसू भर आए थे, ऐसा लगा था मानो उनका मस्तक कुछ ऊँचा हो गया है, मानो मुख पर तेज आ गया है। वही लोग जब संत कुमार की चितकबरी आलोचना करेंगे तो वह कैसे सुनेंगे?
इस तरह एक महीना गुजर गया और संतकुमार ने मुकदमा दायर न किया।
उधर सिविल सर्जन को गाँठना था, इधर मि. मलिक को। शहादतें भी तैयार करनी थीं। इन्हीं तैयारियों में सारा दिन गुजर जाता था। और रुपए का इंतजाम भी करना ही था। देवकुमार सहयोग करते तो यह सबसे बड़ी बाधा हट जाती पर उनके विरोध ने समस्या को और जटिल कर दिया था। संतकुमार कभी-कभी निराश हो जाता। कुछ समझ में न आता क्या करे। दोनों मित्र देवकुमार पर दाँत पीस-पीस कर रह जाते।
संतकुमार कहता – जी चाहता है इन्हें गोली मार दूँ। मैं इन्हें अपना बाप नहीं, शत्रु समझता हूँ।
सिन्हा समझाता – मेरे दिल में तो भई, उनकी इज्जत होती है। अपने स्वार्थ के लिए आदमी नीचे से नीचा काम कर बैठता है, पर त्यागियों और सत्यवादियों का आदर तो दिल में होता ही है। न जाने तुम्हें उन पर कैसे गुस्सा आता है। जो व्यक्ति सत्य के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने को तैयार हो वह पूजने के लायक है।
– ऐसी बातों से मेरा जी न जलाओ, सिन्हा। तुम चाहते तो वह हजरत अब तक पागलखाने में होते। मैं न जानता था तुम इतने भावुक हो।
– उन्हें पागलखाने भेजना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। और इसकी कोई जरूरत भी तो नहीं। हम यह साबित करना चाहते हैं कि जिस वक्त बैनामा हुआ वह अपने होश-हवास में न थे। इसके लिए शहादतों की जरूरत है। वह अब भी उसी दशा में हैं। इसे साबित करने के लिए डॉक्टर चाहिए और मि. कामत भी यह लिखने का साहस नहीं रखते।
पं देवकुमार को धमकियों से झुकाना तो असंभव था, मगर तर्क के सामने उनकी गर्दन आप-ही-आप झुक जाती थी। इन दिनों वह यही सोचते रहते थे कि संसार की कुव्यवस्था क्यों हैं? कर्म और संस्कार का आश्रय ले कर वह कहीं न पहुँच पाते थे। सर्वात्मवाद से भी उनकी गुत्थी न सुलझती थी। अगर सारा विश्व एकात्म है तो फिर यह भेद क्यों है? क्यों एक आदमी जिंदगी-भर बड़ी-से-बड़ी मेहनत करके भी भूखों मरता है, और दूसरा आदमी हाथ-पाँव न हिलाने पर भी फूलों की सेज पर सोता है। यह सर्वात्म है या घोर अनात्म? बुद्धि जवाब देती – यहाँ सभी स्वाधीन हैं, सभी को अपनी शक्ति और साधना के हिसाब से उन्नति करने का अवसर है मगर शंका पूछती – सबको समान अवसर कहाँ है? बाजार लगा हुआ है। जो चाहे वहाँ से अपनी इच्छा की चीज खरीद सकता है। मगर खरीदेगा तो वही जिसके पास पैसे हैं। और जब सबके पास पैसे नहीं हैं तो सबका बराबर का अधिकार कैसे माना जाए? इस तरह का आत्ममंथन उनके जीवन में कभी न हुआ था। उनकी साहित्यिक बुद्धि ऐसी व्यवस्था से संतुष्ट तो हो ही न सकती थी, पर उनके सामने ऐसी कोई गुत्थी न पड़ी थी। जो इस प्रश्न को वैयक्तिक अंत तक ले जाती। इस वक्त उनकी दशा उस आदमी की-सी थी जो रोज मार्ग में ईटें पड़े देखता है और बच कर निकल जाता है। रात को कितने लोगों को ठोकर लगती होगी, कितनों के हाथ-पैर टूटते होंगे, इसका ध्यान उसे नहीं आता। मगर एक दिन जब वह खुद रात को ठोकर खा कर अपने घुटने फोड़ लेता है तो उसकी निवारण-शक्ति हठ करने लगती है। और वह उस सारे ढेर को मार्ग से हटाने पर तैयार हो जाता है। देवकुमार को वही ठोकर लगी थी। कहाँ है न्याय? कहाँ है? एक गरीब आदमी किसी खेत से बालें नोच कर खा लेता है, कानून उसे सजा देता है। दूसरा अमीर आदमी दिन-दहाड़े दूसरों को लूटता है और उसे पदवी मिलती है, सम्मान मिलता है। कुछ आदमी तरह-तरह के हथियार बाँध कर आते हैं और निरीह, दुर्बल मजदूरों पर आतंक जमा कर अपना गुलाम बना लेते हैं। लगान और टैक्स और महसूल और कितने ही नामों से उसे लूटना शुरू करते हैं, और आप लंबा-लंबा वेतन उड़ाते हैं, शिकार खेलते हैं, नाचते हैं, रंग-रेलियाँ मनाते हैं। यही है ईश्वर का रचा हुआ संसार? यही न्याय है?
हाँ, देवता हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे हैं। उन्हें अब भी संसार धर्म और नीति पर चलता हुआ नजर आता है। वे अपने जीवन की आहुति दे कर संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन्हें देवता क्यों कहो? कायर कहो, स्वार्थी कहो, आत्मसेवी कहो। देवता वह है जो न्याय की रक्षा करे और उसके लिए प्राण दे दे। अगर वह जान कर अनजान बनता है तो धर्म से फिरता है, अगर उसकी आँखों में यह कुव्यवस्था खटकती ही नहीं तो वह अंधा भी है और मूर्ख भी, देवता किसी तरह नहीं। और यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं। देवताओं ने ही भाग्य और ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएँ फैला कर इस अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य ने अब तक इसका अंत कर दिया होता या समाज का ही अंत कर दिया होता जो इस दशा में जिंदा रहने से कहीं अच्छा होता। नहीं, मनुष्यों में मनुष्य बनना पड़ेगा। दरिंदों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बाँधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं, जड़ता है। आज जो इतने ताल्लुकेदार और राजे हैं वह अपने पूर्वजों की लूट का ही आनंद तो उठा रहे हैं। और क्या उन्होंने वह जायदाद बेच कर पागलपन नहीं किया? पितरों को पिंडा देने के लिए गया जा कर पिंडा देना और यहाँ आ कर हजारों रुपए खर्च करना क्या जरूरी था? और रातों को मित्रों के साथ मुजरे सुनना, और नाटक-मंडली खोल कर हजारों रुपए उसमें डुबाना अनिवार्य था? वह अवश्य पागलपन था। उन्हें क्यों अपने बाल-बच्चों की चिंता नहीं हुई? अगर उन्हें मुफ्त की संपत्ति मिली और उन्होंने उड़ाया तो उनके लड़के क्यों न मुफ्त की संपत्ति भोगें? अगर वह जवानी की उमंगों को नहीं रोक सके तो उनके लड़के क्यों तपस्या करें?
और अंत में उनकी शंकाओं को इस धारणा से तस्कीन हुई कि इस अनीति भरे संसार में धर्म-अधर्म का विचार गलत है, आत्मघात है और जुआ खेल कर या दूसरों के लोभ और आसक्ति से फायदा उठा कर संपत्ति खड़ी करना उतना ही बुरा या अच्छा है जितना कानूनी दाँव-पेंच से। बेशक वह महाजन के बीस हजार के कर्जदार हैं। नीति कहती है कि उस जायदाद को बेच कर उसके बीस हजार दे दिए जाएँ, बाकी उन्हें मिल जाए। अगर कानून कर्जदारों के साथ इतना न्याय भी नहीं करता तो कर्जदार भी कानून में जितनी खींचतान हो सके करके महाजन से अपनी जायदाद वापस लेने की चेष्टा करने में किसी अधर्म का दोषी नहीं ठहर सकता। इस निष्कर्ष पर उन्होंने शास्त्र और नीति के हरेक पहलू से विचार किया और वह उनके मन में जम गया। अब किसी तरह नहीं हिल सकता और यद्यपि इससे उनके चिर-संचित संस्कारों को आघात लगता था, पर वह ऐसे प्रसन्न और फूले हुए थे, मानो उन्हें कोई नया जीवन मंत्र मिल गया हो ।
एक दिन उन्होंने सेठ गिरधर दास के पास जा कर साफ-साफ कह दिया – अगर आप मेरी जायदाद वापस न करेंगे तो मेरे लड़के आपके ऊपर दावा करेंगे।
गिरधर दास नए जमाने के आदमी थे, अंग्रेजी में कुशल, कानून में चतुर, राजनीति में भाग लेनेवाले, कंपनियों में हिस्से लेते थे, और बाजार अच्छा देख कर बेच देते थे। एक शक्कर का मिल खुद चलाते थे। सारा कारोबर अंग्रेजी ढंग से करते थे। उनके पिता सेठ मक्कूलाल भी यही सब करते थे, पर पूजा-पाठ, दान-दक्षिणा से प्रायश्चित करते रहते थे। गिरधर दास पक्के जड़वादी थे, हरेक काम व्यापार के कायदे से करते थे। कर्मचारियों का वेतन पहली तारीख को देते थे, मगर बीच में किसी को जरूरत पड़े तो सूद पर रुपए देते थे। मक्कूलाल जी साल-साल भर वेतन न देते थे, पर कर्मचारियों को बराबर पेशगी देते रहते थे।
हिसाब होने पर उनको कुछ देने के बदले कुछ मिल जाता था। मक्कूलाल साल में दो-चार बार अफसरों को सलाम करने जाते थे, डालियाँ देते थे, जूते उतार कर कमरे में जाते थे, और हाथ बाँधे खड़े रहते थे। चलते वक्त आदमियों को दो-चार रुपए इनाम दे आते थे। गिरधर दास म्युनिसिपल कमिश्नर थे, सूट-बूट पहन कर अफसरों के पास जाते थे, और बराबरी का व्यवहार करते थे, और आदमियों के साथ केवल इतनी रियायत करते थे, कि त्योहारों में त्योहारी दे देते थे, वह भी खूब खुशामद कराके। अपने हकों के लिए लड़ना और आंदोलन करना जानते थे, मगर उन्हें ठगना असंभव था।
देवकुमार का यह कथन सुन कर चकरा गए। उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उनकी कई पुस्तकें पढ़ी थीं, और उनकी रचनाओं का पूरा सेट उनके पुस्तकालय में था। हिंदी भाषा के प्रेमी थे, और नागरी-प्रचार सभा को कई बार अच्छी रकमें दान दे चुके थे। पंडा-पुजारियों के नाम से चिढ़ते थे, दूषित दान प्रथा पर एक पैंफलेट भी छपवाया था। लिबरल विचारों के लिए नगर में उनकी ख्याति थी। मक्कूलाल मारे मोटापे के जगह से हिल न सकते थे, गिरधर दास गठीले आदमी थे, और नगर-व्यायामशाला के प्रधान ही न थे, अच्छे शहसवार और निशानेबाज थे।
एक क्षण तो वह देवकुमार के मुँह की ओर देखते रहे। उनका आशय क्या है, यह समझ में ही न आया। फिर खयाल आया बेचारे आर्थिक संकट में होंगे, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बेतुकी बातें कर रहे हैं। देवकुमार के मुख पर विजय का गर्व देख कर उनका यह खयाल और मजबूत हो गया।
सुनहरी ऐनक उतार कर मेज पर रख कर विनोद भाव से बोले – कहिए, घर में सब कुशल तो है।
देवकुमार ने विद्रोह के भाव से कहा – जी हाँ, सब आपकी कृपा है।
- बड़ा लड़का तो वकालत कर रहा है न?
- जी हाँ।
- मगर चलती न होगी और आप की पुस्तकें भी आजकल कम बिकती होंगी। यह देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे सरस्वती के पुत्रों का यह अनादर। आप यूरोप में होते तो आज लाखों के स्वामी होते।
- आप जानते हैं, मैं लक्ष्मी के उपासकों में नहीं हूँ।
- धन-संकट में तो होंगे ही। मुझ से जो कुछ सेवा आप कहें, उसके लिए तैयार हूँ। मुझे तो गर्व है कि आप जैसे प्रतिभाशाली पुरुष से मेरा परिचय है। आप की कुछ सेवा करना मेरे लिए गौरव की बात होगी।
देवकुमार ऐसे अवसरों पर नम्रता के पुतले बन जाते थे। भक्ति और प्रशंसा दे कर कोई उनका सर्वस्व ले सकता था। एक लखपती आदमी और वह भी साहित्य का प्रेमी जब उनका इतना सम्मान करता है तो उससे जायदाद या लेन-देन की बात करना उन्हें लज्जाजनक मालूम हुआ। बोले – आप की उदारता है जो मुझे इस योग्य समझते हैं।
- मैंने समझा नहीं आप किस जायदाद की बात कह रहे थे।
देवकुमार सकुचाते हुए बोले – अजी वही, जो सेठ मक्कूलाल ने मुझसे लिखाई थी।
– अच्छा तो उसके विषय में कोई नई बात है?
– उसी मामले में लड़के आपके उपर कोई दावा करनेवाले हैं। मैंने बहुत समझाया, मगर मानते नहीं। आपके पास इसीलिए आया था कि कुछ ले-दे कर समझौता कर लीजिए, मामला अदालत में क्यों जाए? नाहक दोनों जेरबार होंगे।
गिरधर दास का जहीन, मुरौवतदार चेहरा कठोर हो गया। जिन महाजनी नखों को उन्होंने भद्रता की नर्म गद्दी में छिपा रखा था, वह यह खटका पाते ही पैने और उग्र हो कर बाहर निकल आए।
क्रोध को दबाते हुए बोले – आपको मुझे समझाने के लिए यहाँ आने की तकलीफ उठाने की कोई जरूरत न थी। उन लड़कों ही को समझाना चाहिए था।
- उन्हें तो मैं समझा चुका।
- तो जा कर शांत बैठिए, मैं अपने हकों के लिए लड़ना जानता हूँ। अगर उन लोगों के दिमाग में कानून की गर्मी का असर हो गया है तो उसकी दवा मेरे पास है।
अब देवकुमार की साहित्यिक नम्रता भी अविचलित न रह सकी। जैसे लड़ाई का पैगाम स्वीकार करते हुए बोले – मगर आपको मालूम होना चाहिए वह मिल्कियत आज दो लाख से कम की नहीं है।
- दो लाख नहीं, दस लाख की हो, आपसे सरोकार नहीं।
- आपने मुझे बीस हजार ही तो दिए थे।
– आपको इतना कानून तो मालूम ही होगा, हालाँकि कभी आप अदालत में नहीं गए, कि जो चीज बिक जाती है वह कानूनन किसी दाम पर भी वापस नहीं की जाती। अगर इस नए कायदे को मान लिया जाए तो इस शहर में महाजन न नजर आएँ।
कुछ देर तक सवाल-जवाब होता रहा और लड़नेवाले कुत्तों की तरह दोनों भले आदमी गुर्राते, दाँत निकालते, खौंखियाते रहे। आखिर दोनों लड़ ही गए।
गिरधर दास ने प्रचंड हो कर कहा – मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी।
देवकुमार ने भी छड़ी उठा कर कहा – मुझे भी न मालूम था कि आपके स्वार्थ का पेट इतना गहरा है।
– आप अपना सर्वनाश करने जा रहे हैं।
– कुछ परवाह नहीं।
देवकुमार वहाँ से चले तो माघ की उस अँधेरी रात की निर्दय ठंड में भी उन्हें पसीना हो रहा था। विजय का ऐसा गर्व अपने जीवन में उन्हें कभी न हुआ था। उन्होंने तर्क में तो बहुतों पर विजय पाई थी। यह विजय थी। जीवन में एक नई प्रेरणा, एक नई शक्ति का उदय।
उसी रात को सिन्हा और संतकुमार ने एक बार फिर देवकुमार पर जोर डालने का निश्चय किया। दोनों आ कर खड़े ही थे, कि देवकुमार ने प्रोत्साहन भरे हुए भाव से कहा – तुम लोगों ने अभी तक मुकदमा दायर नहीं किया। नाहक क्यों देर कर रहे हो?
संतकुमार के सूखे हुए निराश मन में उल्लास की आँधी-सी आ गई। क्या सचमुच कहीं ईश्वर है जिस पर उसे कभी विश्वास नहीं हुआ? जरूर कोई दैवी शक्ति है। भीख माँगने आए थे, वरदान मिल गया।
बोला – आप ही की अनुमति का इंतजार था।
– मैं बड़ी खुशी से अनुमति देता हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं।
उन्होंने गिरधर दास से जो बातें हुई वह कह सुनाई।
सिन्हा ने नाक फुला कर कहा – जब आपकी दुआ है तो हमारी फतह है। उन्हें अपने धन का घमंड होगा, मगर यहाँ भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं।
संतकुमार ऐसा खुश था गोया आधी मंजिल तय हो गई। बोला – आपने खूब उचित जवाब दिया।
सिन्हा ने तनी हुई ढोल की-सी आवाज में चोट मारी – ऐसे-ऐसे सेठों को उँगलियों पर नचाते हैं यहाँ।
संतकुमार स्वप्न देखने लगे – यहीं हम दोनो के बँगले बनेंगे, दोस्त।
– यहाँ क्यों, सिविल लाइन्स में बनवाएँगे।
– अंदाज से कितने दिन में फैसला हो जाएगा?
– छह महीने के अंदर।
– बाबू जी के नाम से सरस्वती मंदिर बनवाएँगे।
मगर समस्या थी, रुपए कहाँ से आएँ। देवकुमार निस्पृह आदमी थे। धन की कभी उपासना नहीं की। कभी इतना ज्यादा मिला ही नहीं कि संचय करते। किसी महीने में पचास जमा होते तो दूसरे महीने में खर्च हो जाते। अपनी सारी पुस्तकों का कॉपीराइट बेच कर उन्हें पाँच हजार मिले थे। वह उन्होंने पंकजा के विवाह के लिए रख दिए थे। अब ऐसी कोई सूरत नहीं थी जहाँ से कोई बड़ी रकम मिलती। उन्होंने समझा था संतकुमार घर का खर्च उठा लेगा। और वह कुछ दिन आराम से बैठेंगे या घूमेंगे। लेकिन इतना बड़ा मंसूबा बाँध कर वह अब शांत कैसे बैठ सकते हैं? उनके भक्तों की काफी तादाद थी। दो-चार राजे भी उनके भक्तों में थे जिनकी यह पुरानी लालसा थी कि देवकुमार जी उनके घर को अपने चरणों से पवित्र करें और वह अपनी श्रद्धा उनके चरणों में अर्पण करें। मगर देवकुमार थे कि कभी किसी दरबार में कदम नहीं रखा, अब अपने प्रेमियों और भक्तों से आर्थिक संकट का रोना रो रहे थे, और खुले शब्दों में सहायता की याचना कर रहे थे। वह आत्मगौरव जैसे किसी कब्र में सो गया हो।
और शीघ्र ही इसका परिणाम निकला। एक भक्त ने प्रस्ताव किया कि देवकुमार जी की साठवीं सालगिरह धूमधाम से मनाई जाए और उन्हें साहित्य-प्रेमियों की ओर से एक थैली भेंट की जाए। क्या यह लज्जा और दुख की बात नहीं है कि जिस महारथी ने अपने जीवन के चालीस वर्ष साहित्य-सेवा पर अर्पण कर दिए, वह इस वृद्धावस्था में भी आर्थिक चिंताओं से मुक्त न हो? साहित्य यों नहीं फल-फूल सकता। जब तक हम अपने साहित्य-सेवियों का ठोस सत्कार करना न सीखेंगे, साहित्य कभी उन्नति न करेगा और दूसरे समाचारपत्रों ने मुक्त कंठ से इसका समर्थन किया। अचरज की बात यह थी कि वह महानुभाव भी जिनका देवकुमार से पुराना साहित्यिक वैमनस्य था, वे भी इस अवसर पर उदारता का परिचय देने लगे। बात चल पड़ी। एक कमेटी बन गई। एक राजा साहब उसके प्रधान बन गए। मि. सिन्हा ने कभी देवकुमार की कोई पुस्तक न पढ़ी थी, पर वह इस आंदोलन में प्रमुख भाग लेते थे। मिस कामत और मिस मलिक की ओर से भी समर्थन हो गया। महिलाओं को पुरुषों से पीछे न रहना चाहिए। जेठ में तिथि निश्चित हुई। नगर के इंटरमीडिएट कॉलेज में इस उत्सव की तैयारियाँ होने लगीं।
आखिर वह तिथि आ गई। आज शाम को वह उत्सव होगा। दूर-दूर से साहित्य-प्रेमी आए हैं। सोराँव के कुँवर साहब वह थैली भेंट करेंगे। आशा से ज्यादा सज्जन जमा हो गए हैं। व्याख्यान होंगे, गाना होगा, ड्रामा खेला जाएगा, प्रीति-भोज होगा, कवि-सम्मेलन होगा। शहर में दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं। सभ्य-समाज में अच्छी हलचल है। राजा साहब सभापति हैं।
देवकुमार को तमाशा बनने से नफरत थी। पब्लिक जलसों में भी कम आते-जाते थे। लेकिन आज तो बरात का दूल्हा बनना ही पड़ा। ज्यों-ज्यों सभा में जाने का समय समीप आता था उनके मन पर एक तरह का अवसाद छाया जाता था। जिस वक्त थैली उनको भेंट की जाएगी और वह हाथ बढ़ा कर लेंगे वह दृश्य कैसा लज्जाजनक होगा। जिसने कभी धन के लिए हाथ नहीं फैलाया वह इस आखिरी वक्त में दूसरों का दान ले? यह दान ही है, और कुछ नहीं। एक क्षण के लिए उनका आत्मसम्मान विद्रोही बन गया। इस अवसर पर उनके लिए शोभा यही देता है कि वह थैली पाते ही उसी जगह किसी सार्वजनिक संस्था को दे दें। उनके जीवन के आदर्श के लिए यही अनुकूल होगा, लोग उनसे यही आशा रखते हैं, इसी में उनका गौरव है। वह पंडाल में पहुँचे तो उनके मुख पर उल्लास की झलक न थी। वह कुछ खिसियाए-से लगते थे। नेकनामी की लालसा एक ओर खींचती थी, लोभ दूसरी ओर। मन को कैसे समझाएँ कि यह दान दान नहीं, उनका हक है। लोग हँसेंगे, आखिर पैसे पर टूट पड़ा। उनका जीवन बौद्धिक था, और बुद्धि जो कुछ करती है नीति पर कस कर करती है। नीति का सहारा मिल जाए तो फिर वह दुनिया की परवाह नहीं करती। वह पहुँचे तो स्वागत हुआ, मंगल-गान हुआ, व्याख्यान होने लगे जिनमें उनकी कीर्ति गाई गई। मगर उनकी दशा उस आदमी की-सी हो रही थी जिसके सिर में दर्द हो रहा हो। उन्हें इस वक्त इस दर्द की दवा चाहिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सभी विद्वान हैं, मगर उनकी आलोचना कितनी उथली, ऊपरी है जैसे कोई उनके संदेशों को समझा ही नहीं, जैसे यह सारी वाह-वाह और सारा यशगान अंध-भक्ति के सिवा और कुछ न था। कोई भी उन्हें नहीं समझा, किस प्रेरणा ने चालीस साल तक उन्हें सँभाले रखा, वह कौन-सा प्रकाश था जिसकी ज्योति कभी मंद नहीं हुई।
सहसा उन्हें एक आश्रय मिल गया और उनके विचारशील, पीले मुख पर हलकी-सी सुर्खी दौड़ गई। यह दान नहीं, प्राविडेंट फंड है जो आज तक उनकी आमदनी से कटता रहा है। क्या वह दान है? उन्होंने जनता की सेवा की है, तन-मन से की है, इस धुन से की है, जो बड़े-से-बड़े वेतन से भी न आ सकती थी। पेंशन लेने में क्या लाज आए?
राजा साहब ने जब थैली भेंट की तो देवकुमार के मुँह पर गर्व था, हर्ष था, विजय थी।
(प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास, जिसे वे पूरा न कर सके)
4
8 फरवरी 2022

मुंशी प्रेमचंद
133 फ़ॉलोअर्स
प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले (उत्तर प्रदेश) के लमही गाँव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनन्दी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायबराय था जो लमही में डाकमुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरम्भिक शिक्षा का आरंभ उर्दू, फारसी से हुआ और जीवनयापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म-ए-होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ 'शरसार', मिर्ज़ा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया । १८९८ में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी।१९१० में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और १९१९ में बी.ए. पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। प्रेमचंद आधुनिक हिन्दी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यों तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ १९०१ से हो चुका था पर उनकी पहली हिन्दी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसम्बर अंक में १९१५ में सौत नाम से प्रकाशित हुई और १९३६ में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। बीस वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। प्रेमचन्द की रचना-दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, सम्पादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे ‘उपन्यास सम्राट’ की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल १५ उपन्यास, ३०० से कुछ अधिक कहानियाँ, ३ नाटक, १० अनुवाद, ७ बाल-पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, सम्पादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिन्दी और उर्दू भाषा दोनों में समान रूप से दिखायी देती है। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं सेवासदन ,प्रेमाश्रम , रंगभूमि , निर्मला , कायाकल्प, गबन , कर्मभूमि , गोदान, D
प्रतिक्रिया दे
किताब पढ़िए
- हॉरर - भूतप्रेत
- सस्पेंस - थ्रिलर
- स्त्री विमर्श
- प्रेम - रोमांस
- हास्य व्यंग्य
- कॉमिक्स - मीम्स
- जीवनी – संस्मरण
- समीक्षा
- यात्रा वृतांत
- सेल्फ हेल्प
- बाल साहित्य
- स्वास्थ्य - फिटनेस
- इतिहास
- कानून - व्यवस्था
- प्रौद्योगिकी - विज्ञान
- पाक-कला
- व्यापार - धन
- शिक्षा
- खेल – खिलाड़ी
- डायरी
- अन्य
- अनुवाद
- विज्ञान गल्प्
- सामाजिक
- इरोटिक
- पारिवारिक
- धर्म - आध्यात्म
- शिल्प - शौक
- अपराध - जासूसी
- फैशन - लाइफस्टाइल
- ग़ज़ल
- हिंदी नाटक
- हिंदी पत्रिका
- हिंदी क्लासिक
- साहित्य और कथा
- नयी किताबें
- प्रसिद्ध किताबें
- लिस्टेड किताबें
- प्रिंटेड किताबें
- ऑडियो बुक्स
- समीक्षित पुस्तकें
- उपन्यास
- कहानी / कहानी संग्रह
- काव्य / कविता संग्रह
- पत्रिका
- जनरल बुक्स
- पुस्तक प्रतियोगिता
- सभी किताबें...
लेख पढ़िए
- अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस
- विश्व हास्य दिवस
- विश्व प्रेस आज़ादी दिवस
- कोविशील्ड वैक्सीन विवाद
- पेरिस ओलंपिक 2024
- दिल्ली शराब घोटाला
- हनुमान जयंती
- लोकसभा चुनाव 2024
- रामनवमी 2024
- ईद-उल-फ़ितर
- हिन्दू नववर्ष
- PMLA अधिनियम
- मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल
- मुख़्तार अंसारी
- शहीद दिवस
- नागरिकता संशोधन कानून
- ऑस्कर अवार्ड्स
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
- सन्देशखाली घटना
- किसान आंदोलन 2.0
- दीपकनीलपदम्
- दीपक श्रीवास्तव नीलपदम
- दीपक नील पदम्
- दीपक नीलपदम्
- अनुभव
- व्यवहारिक
- आधुनिक
- फ्रेंडशिप डे
- आध्यात्मिक
- नैतिक
- मानसिक स्वास्थ्य
- दीपक नीलपदम
- महापुरुष
- करवाचौथ
- मंत्र
- आत्मकथा
- धार्मिक
- नील पदम्
- परिवारिक
- चीरहरण
- ईश्वर
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन
- विश्व पर्यावरण दिवस
- दैनिक प्रतियोगिता
- ग्लोबल वार्मिंग
- सभी लेख...