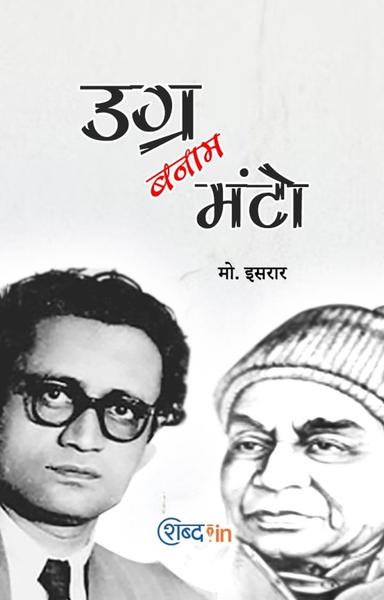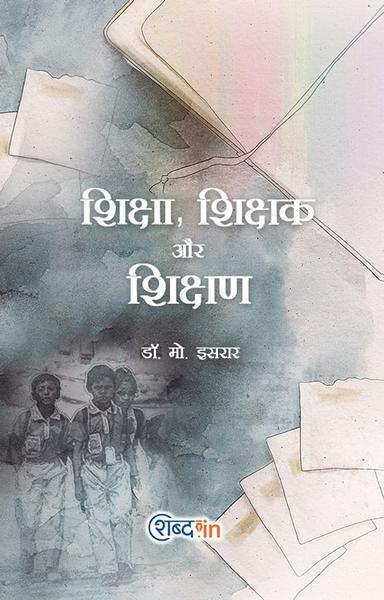पिछले अध्यायों में हमने ‘उग्र’ और मंटो के व्यक्तित्व और कृतित्त्व को अलग-अलग रूपों और सन्दर्भों में जानने-समझने का प्रयास किया है। अब हम दोनों साहित्यकारों की एक साथ तुलना करके देखते हैं कि वे कहाँ एक-दूसरे से समानता रखते हैं और कहाँ अलग हैं। सामीप्य और भिन्नता में जीवन चरित्र और रचना वैविध्य दोनों को आधार बनाया जाएगा। वैसे जब उनकी जीवन संघर्ष गाथा और रचनाधर्मिता के विविध पक्षों का अवलोकन करते हैं तो उनमें गजब की समानता दिखाई देती है। वे जीवनपर्यन्त अपने विरुद्ध ऐसे संकुचित सोच वाले लोगों की कारगुजारियों से टकराते और आहत होते रहे, जो उनके काम का आकलन करने के योग्य कभी थे ही नहीं। आज के सन्दर्भों और बदली हुई परिस्थितियों में भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की अलग पहचान है।
प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र की दो विशेषताएं होती हैं- अच्छा और बुरा। कोई भी व्यक्ति सबके लिए अच्छा नहीं होता और सबके लिए ख़राब भी नहीं होता। ‘उग्र’ और मंटो भी कुछ इसी तरह के इन्सान थे। न सबके लिए अच्छे थे और न सबके लिए ख़राब। उन दोनों का व्यक्तित्व ऐसा था जो दूसरों पर प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः अवश्य प्रभाव डालता था। कोई उनसे दिल से मुहब्बत करता था, तो कोई हद दर्जे की नफ़रत। जो उनसे मिला प्रभावित हुए बिन न रहा। दोनों बेख़ौफ, बेफिक्र इनसान थे। साहित्य में उन्हें बहुत बुरा-भला कहा गया, पर उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। जब कभी कोई उनसे भिड़ा, उन्होंने साफ-साफ लताड़कर सुना भी दिया। उनका मिजाज बेबाक था। जो कुछ कहते, बिन किसी की शर्म-लिहाज किए मुँह पर ही कह देते। कोई बुरा माने या भला माने। वे साहित्य में सबसे अधिक बदनाम हुए, पर उनके व्यक्तित्व की अलग पहचान भी रही। उनकी जो लोकप्रियता और प्रसिद्धि रही वह केवल प्रयत्न करने से नहीं प्राप्त की जा सकती। उसके लिए कलाकार में असली जौहर होना चाहिए। उनका साहित्य कुछ अलग ढर्रे का है। जिसने लोगों को सोचने-विचारने और नई परिभाषा गढ़ने पर मजबूर किया। उनके साहित्य में हिन्दुस्तान के मध्यम वर्ग के अन्तःकरण की पुकार सुनाई देती है। अपनी सामाजिक परिस्थितियों का सही विश्लेषण करते हुए वे जीवन भर बागी लेखक बने रहे।
पांडेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ का नाम जितना विचित्र है, उनका व्यक्तित्व भी उतना ही विचित्र है। उनके नाम के पीछे अपनी ही तरह की अनूठी कहानी है, तो व्यक्तित्व के पीछे और भी अधिक किस्से छिपे हैं। वे स्वभाव से अक्कखड़ और तबीयत से फक्खड़ थे। इसलिए उनका चरित्र प्रायः विवादों से घिरा रहा। उनके विरूद्ध ‘घासलेटी आन्दोलन’ क्या चला कि वे हिन्दी साहित्य में प्रायः अस्पृश्य और त्याज्य रचनाकार मान लिए गए। लेकिन जब से ‘उग्र’ की जन्मशताब्दी मनायी गई है, तब से उनको नए दृष्टिकोणों से परखने की परम्परा चल पड़ी और उनके विषय में नए-नए किस्से-कहानियाँ सामने आने लगे हैं। गठीले कद-काठी के इस साहित्यकार का व्यक्तित्व ऐसा था जो दूसरों प्रभावित करता था। उन्होंने अपने अभिन्न मित्र पं. विनोद शंकर व्यास को जो पत्र लिखे उनमें उनका व्यक्तित्व प्रकट हुआ है। इन पत्रों को सुधाकर पांडेय ने संग्रहीत करके वाणी प्रकाशन दिल्ली से सन् 1996 में प्रकाशित कराया था। इन पत्रों से ‘उग्र’ का ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होता है जो घोर संघर्षशील और न टूटने वाला है। वे भूखों रह सकते थे लेकिन अपनी इज्ज़त या अहंकार से समझौता नहीं कर सकते थे। मान रक्षा के लिए मुँह नहीं खोल सकते थे। यदि माँगना ही पड़ा तो मित्रों से माँगा नहीं तो बिन खाए चुपचाप पड़े रहे।
किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान में उसके पत्र अत्यधिक सहयोगी हो सकते हैं। व्यक्तित्व की व्याख्या में वे भाष्यकार का काम करते हैं। ‘उग्र’ के पत्र भी उनके व्यक्तित्व के दस्तावेज़ हैं। कहा जाता है कि वे पत्रों के जवाब देने में बहुत माहिर थे।
बचपन में वे गोल मटोल और सुन्दर थे। चाचा-चाची ने उन्हें रीझकर गोद ले लिया था। ग्यारह-बारह वर्ष की अवस्था में उन्हें रामलीला मंडलियों में सीता-लक्ष्मण-भरत आदि की भूमिकाएं अदा करते हुए, तत्कालीन पंजाब में ‘हसीन-तरीन’ की उपाधि मिली थी। उस समय रामलीला मंडलियों में सीता-भरत-लक्ष्मण आदि का अभिनय करने वाले कुमारों को ‘स्वरूप या सरूप’ कहा जाता था। मंडली वाले उनकी सुन्दरता पर मुग्ध होकर, उनका यौन-शोषण भी किया करते थे। सुन्दर होने और अभिनय में पारंगत हो जाने के कारण ‘उग्र’ ने भी चौदह वर्ष की अवस्था तक ‘सरूप’ बनकर सीता-भरत आदि का अभिनय किया। परन्तु वे रामलीला मंडली वालों की बुरी नज़र से इसलिए बच गए क्योंकि उनके दो बड़े भाई उनके साथ ही रहते थे, जो तगड़े जवान थे।
पांडये बेचन शर्मा ‘उग्र’ का नाम ही बड़ा विचित्र है। इस नाम के पीछे भी एक आकर्षक और रोचक सी कहानी है। पैदा होते ही बेच दिए जाने के कारण वे ‘बेचन’ थे। ब्राह्मण घर में जन्मे होने के कारण वे ‘बेचन पांडेय’ हो गए। सन् 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित साप्ताहिक स्वदेश में जब उनकी ‘आह्वान’ कविता छपी तो सम्पादक ने लेखक का नाम दिया ‘श्रीयुत पांडेय बेचन शर्मा ‘उग्र’। यह नाम उन्हें पसंद आया। और उन्होंने यह नाम जीवन भर के लिए अपना लिया।
‘उग्र’ ने सन् 1930 से 1938 तक अर्थात् पूरे आठ वर्ष फिल्मी जगत में व्यतीत किए। उन्होंने पहले अवाक् फिल्मों में बाद में सवाक फिल्मों में काम किया। वे फिल्मों की कहानी, संवाद, गाने आदि सभी कुछ लिखते रहे और मस्तियाँ लेते रहे। वहीं पर ‘उग्र’ से प्रभावित होकर गृहस्थ बनी हुई एक वेश्या उन पर आसक्त थी और एक अर्धवेश्या पारसीक परम सुन्दरी पर वे स्वयं बुरी तरह मोहित थे।
गोरखपुर में ‘स्वदेश’ के अंक का संपादन करने के जुर्म में केस चलने पर वे इसलिए बच गए थे क्योंकि वे देखने में भोले-भाले और सीधे लगते थे। लोअर कोर्ट ने माना था, ‘‘यह नन्हा सा, दाढ़ी न मूँछ वाला इक्कीस साल का लल्ला है।”
प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन स्वयं ‘उग्र’ पर मोहित हो गए थे। इस विषय में एक रोचक-सा प्रसंग उन्होंने अपनी आत्मकथा के चौथे व अन्तिम भाग ‘दशद्वार से सोपान तक’ में लिखा है। वे ‘जनगीता’ (बच्चन द्वारा सन् 1958 में रचित प्रसिद्ध ग्रन्थ) प्रकाशित होने पर पहली बार ‘उग्र’ से मिलने गए। ‘उग्र’ उस समय दिल्ली के कृष्णा नगर में रहते थे। जैसे ही ‘जनगीता’ की प्रति लेकर वे ‘उग्र’ के पास पहुँचे तो ‘उग्र’ सहसा बोल उठे ‘यह तो अच्छा हुआ कि तुम अपनी कम उमरी में मुझे न मिले, मैं तुम्हें छोड़ता नहीं।’ तभी बच्चन जी भी बोल उठे ‘मैं छोड़वाता भी नहीं।’
विनोद शंकर व्यास को लिखे ‘उग्र’ के पत्रों से ज्ञात होता है कि वे चार्वाक दर्शन के अनुयायी थे। सदा यही मानते रहे कि जो कुछ है, वह यहीं है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं। भोगने लायक प्रत्येक वस्तु का उन्होंने भोग किया, पान-तम्बाकू, भंग-शराब आदि खूब खाते-पीते थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, पर वे रूप-सौन्दर्य के पारखी थे। उसका भरपूर आनन्द भी उन्होंने लिया था। मंहगा कपड़ा, विशेषत: खादी खरीदकर पहनते थे। सुगन्धित गजरा लगाकर घूमने का उन्हें शौंक था। हिन्दी के मनीषी विद्वान सुधाकर पांडेय ने उनके व्यक्तित्व के विषय में लिखा है, ‘‘उनकी शादी नहीं हुई, कुछ तो ग़रीबी के कारण और कुछ उनके अक्खड़ रमतापानी जीवन के करण। पर वे ब्रह्मचारी नहीं थे। रूप बाजार के ग्राहक भी थे। कभी भी उन्होंने न तो किसी का घर खराब किया, न कभी किसी के गृहस्थी में टांग अड़ायी। वे हिन्दी के आधुनिक साहित्यकारों में परशुराम थे। माँ, भाई, दोस्त, लेखक, प्रकाशक, गुरू, नेता आदि सभी पर उन्होंने बाण चलाए। ‘उग्र’ का जीवन यदि आदर्श में बंधा होता और साधु संतो की पंक्ति में होते तो वे आधुनिक हिन्दी के कबीर कहलाते।’’
सआदत हसन मंटो भी अपनी ही तरह के इंसान थे। यदि मंटो के व्यक्तित्व का सही और सच्चा खाका जानना हो तो, उसके पत्रों और कहानियों से उपयुक्त माध्यम नहीं हो सकता। मंटो के पत्रों का ऐतिहासिक महत्व है। वे उसके चरित्र का आईना हैं। अपने दोस्तों को लिखे पत्रों में मंटो के आचार-व्यवहार, स्वभाव, क्रिया कलाप आदि का ज्ञान होता है। पाकिस्तान की तत्कालीन स्थिति से अवगत कराते हुए ‘चाचा साम के नाम’ से उसने जो काल्पनिक पत्र लिखे, उनसे ज्ञात होता है कि अपने अन्तिम दिनों में मंटो किस सीमा तक टूट चुका था। वह बोलचाल में बेबाक था। उसके लिखे में कोई दोष निकाले या नुक्ता-चीनी करे यह उसे बिलकुल बर्दाश्त नहीं था। यदि कोई ऐसा करता वह उससे सीधे भिड़ जाता था। उपेन्द्रनाथ ‘अश्क’ ने जब उसकी कहानी ‘खुशिया’ को ‘दो कोड़ी की कहानी’ कहा तो, वह कई महीनों तक इसी ताक में रहा कि कब ‘अश्क’ से इस विषय पर बात हो। और जब प्रत्यक्ष वार्तालाप हुआ तो ‘अश्क’ ने वही बात दोहराते हुए कहा, ‘‘कहानी तुम्हारी कल्पना की देन है। तुम्हें विचार सूझा और तुमने कहानी लिख डाली। तुम कहानियों में जैसे दलाल बनाते हो वैसे होते नहीं। इतना सुनते ही मंटो झल्लाकर बोला, हाँ, हाँ, मैं हूँ वह दल्लाल, मंटो वह दल्लाल है।’’
मंटो विरोधी स्वभाव वाला व्यक्ति था। जब उसे कड़ा होना होता वह नरम हो जाता और जब नरम होना होता वह ज़िद्दी या हठी बन बैठता या मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता। उसका व्यक्तित्व असाधारण था। वह दूसरों पर जब तक हावी रहता, तब तक मैदान में डटा रहता, पर जब दूसरे उस पर हावी होने लगते वह वहाँ से खिसक लेता। जब ‘आल इंडिया रेडियो दिल्ली’ में अश्क उसके प्रतिद्वन्द्वी के रूप में आए तो, जब तक वह उन्हें मात देता रहा वहाँ डटा रहा, पर जब मात खानी पड़ी, वह अपनी नौकरी की कुर्बानी देकर मुम्बई चला गया। बॉम्बे टाकीज, मुंबई में मुसलमानों की नियुक्ति को लेकर विवाद उठा तो वह पाकिस्तान चला गया। क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार वे नियुक्तियां मंटो के कारण हुई थी।
मंटो, जिस भी स्थान पर रहता, अपनी अलग पहचान बना लेता। ‘आल इंडिया रेडियो दिल्ली’ में वह केवल उन्नीस महीने रहा, पर इतने समय उसकी तूती बोली। अश्क के अनुसार, ‘‘रेडियो स्टेशन में हर समय ‘मंटो साहब, मंटो साहब’ होती रहती और हर मामले में मंटो की राय आखिरी समझी जाती और मंटो चापलूसों या मित्रों से घिरा रहता था।’’ मुंबई फिल्मिस्तान में भी उसका अलग मक़ाम था। फिल्मी हस्तियों के साथ जब मंटो अन्य लोगों से मिलता, तब फिल्मी सितारे नहीं, लोग मंटो की ओर अधिक आकर्षित होते, क्योंकि ऐक्टरों, डायरेक्टरों में वह अपनी योग्यता, हास्य और विनोद के कारण सुनने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचे रहता था। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा ख़ास था कि लोग उससे नफरत करते हुए भी मुहब्बत करते थे।
अपने लड़कपन में ही मंटो पीने का आदी हो चुका था। वेश्या बाज़ार की भी उसे अच्छी-खासी जानकारी हो चुकी थी। लोग घूमने के लिए हिल स्टेशनों, टूरिस्ट प्लेसों पर जाते हैं, पर उसके घूमने के लिए वेश्या बाज़ार ही सबसे उपयुक्त स्थान थे। यहाँ से उसे अपनी कहानियों के लिए कच्चा माल मिलता था। मंटो हर मनुष्य से इस आशा के साथ मिलता था कि उसके अस्तित्व में अवश्य कोई न कोई अर्थ छिपा होगा जो एक न एक दिन प्रकट हो जाएगा। वह ऐसे-ऐसे लोगों के साथ हफ्तों घूमता था जिन्हें आम इंसान भी एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मंटो अपने दोस्त-दुश्मनों से कसकर झगड़ा करता और सबके ऊपर व्यंग्य करता। कारदार, सितारा देवी, के. आसिफ जैसी फिल्मी हस्तियों पर उसने अनेक व्यंग्यात्मक लेख लिखे, लेकिन किसी ने भी उसके विरूद्ध मानहानि का मुकदमा नहीं किया। अपनी किसी भी रचना से पहले 786 लिखकर आरम्भ करना उसका विशेष अंदाज था। पर यह उसके धार्मिक या आस्तिक होने का प्रतीक नहीं। न वह रोज़े रखता था और न नमाज़ पढ़ता था। रोटी के बिन रह सकता था पर शराब के बिन नहीं। उसका मिज़ाज़ बेबाक था, जो कुछ कहता बिन किसी की शर्म लिहाज किए मुँह पर ही कह देता था। मंटो दंभ से बहुत चिढ़ता था। इसी कारण उसकी बोलचाल में हमेशा निरन्तरता रहती थी।
एक बार मंटो ने देवेन्द्र सत्यार्थी को फोन पर खूब गालियाँ दी। उसके मन में देवेन्द्र के लिए जो छाप थी, उसने उसे ज़ाहिर कर दिया। जब उसकी पत्नी सफिया ने यह सब देखा तो मंटो को बुरा भला कहा। मंटो बोला, ‘‘मैं हृदय में घृणा रख मुँह से प्रेम भरे शब्द नहीं कह सकता।’’ मंटो के अहं और खुद्दारी ने उसे सदा दोषी सिद्ध किया। जबकि वह उतना देाषी नहीं था। कहानियों पर चले मुकदमों ने उसकी इज्ज़त पर बट्टा लगाया। उसे न केवल साहित्य में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत गालियाँ खाने को मिली। पर बदनाम होकर भी वह उर्दू साहित्य में ऐसा चिरस्थायी स्थान बना गया, जिसके अस्तित्व को आज तक बड़े से बड़ा कथाकार भी हिला नहीं पाया है। उसके पात्रों का सीध प्रभाव पाठकों के मन-मष्तिष्क पर पड़ता है। पाठक उसकी कहानियाँ पढ़कर उसके पात्रों के विषय में कई-कई दिन तक सोचता रहता है।
उपरोक्त विवरण से लगता है कि दोनों साहित्यकारों का व्यक्तित्व कुछ अलग ही तरह का रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ने बेहतरीन साहित्य लिखा, लेकिन जहाँ तक उनकी चारित्रिक विशेषताओं और व्यवहार का सवाल है वह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तनिक सी बात पर चिढ़ जाना, दूसरों पर कटाक्ष करना, दंभ और अहं से भरे रहना, लड़ने-झगड़ने को तैयार रहना आदि कुछ उनके व्यतित्व की ऐसी विशेषताएं थी जिन्होंने उन्हें उबरने नहीं दिया। अपने असभ्य व्यवहार और भद्दी गालियों के कारण ‘उग्र’ को तो लक्ष्मी फिल्म कंपनी से भी निकाल दिया गया था। सब लोग उनसे इतने तंग थे कि निकाले जाते समय किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। इसी प्रकार मंटो का व्यवहार भी दूसरों के साथ बहुत अच्छा नहीं था। साहित्य में अक्सर यह प्रथा प्रचलित है कि किसी साहित्यकार के मरने के बाद उसकी अच्छाईयाँ ही अच्छाईयाँ उजागर की जाने लगती हैं, उसके सभी ऐब छिप जाते हैं। लेकिन नर्तकी सितारा देवी ने मंटो की मौत की ख़बर सुनकर कहा था, “बड़ा बत्तमीज़, बेवकूफ आदमी था। मेरा चैन हराम कर दिया था उसने।”
कहानीकार के रूप में ‘उग्र’ और मंटो की तुलना करके देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ‘उग्र’ एक बड़े कहानीकार हैं। उन्होंने बेहतरीन कहानियाँ लिखी। लेकिन इस सन्दर्भ में मंटों उनसे कहीं अधिक महान और श्रेष्ठ कहानीकार हैं। मंटों की प्रसिद्धि उसकी कहानियों के कारण ही है। ये कहानियाँ उसे विश्व के महान कहानीकारों चेखव, मोपासा, ओ हेनरी आदि की श्रेणी में ला बैठा देती है। ‘उग्र’ ने केवल कहानियाँ ही लिखीं लेकिन मंटो ने कहानियों के अतिरिक्त अनेक लघुकथाएं, छोटी-छोटी घटनाएँ (हाशिए) भी लिखी। ‘उग्र’ और मंटो ने दंगो, फसाद, साम्प्रदायिकता आदि पर बेहतरीन कहानियाँ लिखी हैं। लेकिन ‘उग्र’ की उक्त विषयवस्तु पर लिखी कहानियों जैसे- दोजख की आग, दोजख नरक, आँखों में आँसू, ईश्वरद्रोही, खुदा के सामने, खूंखार मौला, दिल्ली की बात, हिन्दू, मुसलमान, शाप आदि और कुछ उपन्यासों को पढ़ने से लगता है कि उनकी दृष्टि कहीं-कहीं हिन्दूवादी भी हो उठी है। मंटो की इस प्रकार की कहानियों को पढ़ने से उसके साम्प्रदायिक या कट्टर होने का कोई संकेत नहीं मिलता है। उसने ‘दो कौमें’ कहानी में हिन्दू और इस्लाम दोनों धर्मों की अवहेलना ही है। उसकी कई कहानियाँ धार्मिक रूढ़ियों पर सीधा कटाक्ष करती हैं। लेकिन इस संबंध में एक बड़ा सवाल यह उठ सकता है कि यदि मंटो सांप्रदायिक नहीं था तो पाकिस्तान क्यों चला गया? इसके बारे में कई आलोचकों ने उसके पारिवारिक कारण बताए हैं।
उपन्यासकार के रूप में ‘उग्र’ काफी सिद्धहस्त कलाकार दिखाई देते हैं। उनके एक दर्जन उपन्यास प्रकाशित हुए, जिनमें से कई ने तो बिक्री के रिकॉर्ड तक तोड़े। अपने उपन्यासों में उन्होंने उन विषयों की समीक्षा की जो उस समय के अन्य लेखकों से छूट रहा था। मंटो ने अपने जीवन में केवल एक उपन्यास ही लिखा, जिसे कोई खास प्रसिद्धि नहीं मिली। इस प्रकार देखा जाए तो इस क्षेत्र में ‘उग्र’, मंटो से काफी आगे हैं।
‘उग्र’ और मंटों ने नियमित लेखन की शुरुआत पत्रकारिता जगत में कदम रखने के बाद की थी। साहित्य के अतिरिक्त हिन्दी-उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हिन्दी-उर्दू पत्रकारिता के विकासात्मक इतिहास में जिन महान विभूतियों के नाम लिए जा सकते हैं, उनमें इन दोनों का नाम अग्रपंक्ति में गिना जा सकता है। साहित्यकार होने के साथ ही उनका व्यक्तित्व संपादकीय कौशल से भी व्याप्त था। उन्होंने जीवन में कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया।
‘उग्र’ में पत्रकारिता के संस्कार उस युग में विकसित हुए थे, जिसमें पत्रकारिता एक ‘मिशन’ हुआ करती थी। पत्रकारिता उनकी नस-नस में बसी थी इसीलिए उनके साहित्य में अनेक पात्र पत्रकार और संपादक भी हैं। वे संपादक-पत्रकार उसे नहीं मानते थे जो सालभर में पन्द्रह बार जूतों से नहीं पिटा हो, चार-पाँच बार जिसकी खोपड़ी न फूटी हो और आठ-दस मुकदमें दीवानी और फौजदारी के उस पर न चले हों। वे स्वयं इसी आदर्श के जुझारू, प्रखर और जोजस्वी पत्रकार संपादक थे। वे आजीवन एक दर्जन से भी अधिक पत्र-पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे, पर खेद का विषय है कि उनके द्वारा संपादित कोई भी पत्र-पत्रिका दीर्घजीवी न हो सका। उन्होंने सदैव जन-समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया इसलिए उनके विचार सामाजिक जीवन में छाए रहे। उनके क्रान्तिकारी व्यक्तित्व की झलक उनकी पत्रकारिता में भी दिखाई देती है। इसलिए उनके द्वारा संपादित पत्र जब्त हुए या फिर राजनीति का शिकार बने। उन्होंने संपादक के रूप में निर्भीक होकर जनसेवा और समाजसेवा की, परिणाम भले ही कुछ भी निकला हो। उनमें एक सफल संपादक के सभी गुण विद्यमान थे। पत्रकारिता के विषय में वे अपने विचार व्यक्त करते रहे, जो आज भी उनके साहित्य में बिखरे पड़े हैं। वे विचार आज भी नवीन और खोजी पत्रकारिता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। शोषण को तार-तार कर देने वाले ‘उग्र’ ने अपने लक्ष्य से कभी कोई समझौता नहीं किया। उनकी पत्रकारिता के दो पक्ष सामने आते हैं- प्रथम स्वतन्त्रता पूर्व का और दूसरा स्वतन्त्रता के बाद। स्वतन्त्रता पूर्व वे सेठ-धनाढ्य या मित्रों के आग्रह पर संपादक रहे। देश की स्वतन्त्रता के बाद सारे पत्र उन्होंने अपने बूते और अपने आदर्शों के अनुरूप निकालने का प्रयास किया।
‘उग्र’ ने सर्वप्रथम सन् 1921 में दैनिक पत्र ‘आज’ में ‘अष्टावक्र’ उपनाम से ‘ऊटपटाँग’ शीषर्क के अन्तर्गत व्यंग्यात्मक लेख लिखने आरम्भ किए थे। वे लेख तत्कालीन समस्याओं पर आधारित होते थे। इसी वर्ष उन्होंने वाराणसी से ‘उग्र’ नामक हस्तलिखित मासिक पत्र निकालना आरम्भ किया। तीन अंक निकलने के पश्चात वह काल के गर्त में समा गया। सन् 1924 में ‘भूत’ नामक हास्य पत्र प्रकाशित करने की योजना बनाई और उसे कार्यान्वित किया। इस पत्र ने जन्म लेते ही काशी की आनंदवादी परम्परा और मस्ती को बनारसी शैली में व्यक्त करना प्रारंभ किया और भारतेंदु की परंपरा को पुन: जीवित करने का प्रयास किया। ऐसा माना जाता है कि ‘भूत’ के विभिन्न स्तम्भों के अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री हिन्दी साहित्य में अपने ढंग की अकेली है। यह पत्र कुछ अंक निकलकर बंद हो गया। इसी वर्ष उन्होंने गोरखपुर से निकलने वाले साप्ताहिक ‘स्वदेश’ के दशहरा अंक का संपादन किया। सम्पूर्ण अंक देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण था। उनके विरूद्ध सरकारी वारंट निकला और वे कलकत्ता भागकर ‘साप्ताहिक मतवाला’ के संपादन मंडल में सम्मिलित हो गए। लगभग छह वर्षों तक वे इस पत्र से जुड़े रहे जो उनके लिए ऐतिहासिक महत्व के वर्ष सिद्ध हुए। उनकी अधिकाशं प्रसिद्ध रचनाएं जैसे- चाकलेट, चन्द हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी आदि ‘मतवाला’ में धारावाहिक रूपों में प्रकाशित हुई। ‘मतवाला’ मंडल में उनकी निराला के साथ भावों की भिडंत भी खूब हुई। क्योंकि निराला की अपेक्षा उनकी रचनाओं की माँग जानता में अधिक रहती थी।
सन् 30 तक आते-आते मतवाला की स्थिति बिगड़ने लगी तो ‘उग्र’ मतवाला छोड़कर मुंबई फिल्मी दुनिया में सम्मिलित हो गए। सन् 1934-35 में उन्होंने ‘हिंदिया’ और ‘गधा’ नामक दो पत्र निकालने की योजनाएं बनाई पर योजनाएं फलीफूत न हो सकी। पूर्व में मासिक रूप में निकाले गए ‘उग्र’ नामक पत्र को सन् 1938 में उन्होंने साप्ताहिक रूप में काशी से फिर से प्रकाशित करने की योजना बनाई। लेकिन उसके सात अंक ही प्रकाशित हो सके। ‘उग्र’ साप्ताहिक के प्रथम अंक में ‘मेरा जर्नलिज्म’ शीर्षक आलेख में उन्होंने लिखा था, ‘‘एक पत्र की मुझे सख्त जरूरत है और रहेगी सारी जिन्दगी।’’ 1938 में वाराणसी से प्रकाशित ‘खुदा की राह पर’ के होली अंक के संपादन में भी ‘उग्र’ ने अपना योग दिया। इसके पश्चात वे ‘मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति’ इंदौर की मासिक पत्रिका ‘वीणा’ से सहायक संपादक के रूप में जुड़े। पर समिति से जुड़े लोगों के विरूद्ध ‘स्वराज्य’ नामक पत्र में खुली चिट्ठी प्रकाशित करवाने लगे। जिसके कारण उनको सहायक संपादक के पद से हटना पड़ा। ‘वीणा’ से हटने के पश्चात वे 1942 में पं. सूर्यनारायण व्यास द्वारा संचालित ‘विक्रम मासिक पत्र’ उज्जैन का संपदन करने लगे। पर इसके पाँच अंक निकलने के पश्चात वे संपादन कार्य छोड़कर मुंबई चले गए। ‘विक्रम’ के प्रत्येक अंक में आधे से अधिक सामग्री स्वयं ‘उग्र’ की लेखनी से निःसृत होती थी। मुंबई आने पर उन्होंने सन् 1942 और 1945 में क्रमशः ‘संग्राम’ साप्ताहिक तथा ‘विक्रम’ मासिक पत्रों का संपादन किया। सन् 1948 में ‘मतवाला’ के संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ के पुत्र हरगोविंद सेठ के आग्रह पर गऊ घाट, मिरजापुर आ गए और हरगोविंद सेठ द्वारा उपलब्ध सुविधाओं से प्रसन्न होकर उन्होंने ‘मतवाला’ का पुनः प्रकाशन प्रारम्भ किया।
अस्थिर और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ‘उग्र’ को एक स्थान पर टिके रहना सम्भवतः अखरता था। सन् 1953 के अन्त में वे दिल्ली आ गए और ‘उग्र साप्ताहिक’ का पुनः संपादन करने लगे, पर सफलता नहीं मिली। सन् 1956 में ‘हिंदी पंच’ पाक्षिक पत्र का संपादन करने लगे। लेकिन इस पत्र के केवल चार अंक ही प्रकाशित हो सके। कुछ समय के लिए वे ‘गणराज्य’ दैनिक के संपादन से भी जुड़े। सन् 1963 में अपने 63वें जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ‘उग्र’ नामक पत्र, दैनिक के रूप में तीसरी बार पुनः प्रकाशित किया। चार पृष्ठों का यह पत्र सायंकालीन विचार दैनिक के रूप में था। लेकिन इस पत्र के कुल दस अंक ही प्रकाशित हो सके।
उन्होंने अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए साहित्य के साथ ही पत्रकारिता को भी हथियार माना था। उनकी लेखनी में दुराग्रह कम और बेबाकी अधिक रहती थी। सम्भवतः इसी कारण उनके द्वारा संपादित कोई भी पत्र दीर्घजीवी न हो सका। फिर भी हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में उनका पत्रकार और संपादक की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यदि उनका ध्येय केवल साहित्य सृजन होता तो हिन्दी साहित्य में उनका और भी श्रेष्ठ स्थान होता लेकिन उनकी प्रतिभा का अधिकांश उपयोग दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में होता रहा।
अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाते हुए, सआदत हसन मंटो ने जो व्यंग्यात्मक लेख लिखे वे वर्तमान सन्दर्भ की दृष्टि से पीली पत्रकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण माने जा सकते हैं। मंटो ने लेखन की शुरूआत पत्रकारिता से ही की थी, परन्तु पत्रकार के रूप में उनकी जीवन-यात्रा अधिक लम्बी नहीं रही। जब मंटो के गुरु पत्रकार बारी साहब अमृतसर से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र ‘मसावात’ के संपादक नियुक्त होकर, लाहौर से अमृतसर आए, तो उनकी मंटो के साथ भेंट हो गई। परिणामस्वरूप मंटो की आवारागर्दी समाप्त हो गई और जो समय पहले फ़्लश खेलने में कटता था अब ‘मसावात’ के दफ्तर में कटने लगा। कभी-कभी बारी साहब एक-आध समाचार अनुवाद के लिए मंटो को भी दे देते थे, जो वह टूटी-फूटी उर्दू में कर दिया करता था। धीरे-धीरे मंटो ने फिल्मी समाचारों का कालम (स्तम्भ) संभाल लिया। मंटो के अन्दर छिपी लेखन प्रतिभा देखकर, बारी साहब ने उसे समसामयिक लेख लिखने की सलाह दी। मंटों ने उसे गुरू की आज्ञा समझकर, उसका पालन किया। और यह सिलसिला आजीवन चलता रहा।
मंटो सन् 1936 में मुंबई से प्रकाशित होने वाले ‘साप्ताहिक मुसव्विर’ का संपादक नियुक्त हो गया। ‘मुसव्विर’ के संस्थापक नजीर ने संपादन भार संभालने के लिए मंटो को स्वयं पत्र लिखा था। ‘मुसव्विर’ एक फिल्मी पत्र था, जिसका कार्यालय मुंबई के क्लीयर रोड़ सत्रह नम्बर फ्लेट में था। इस पत्र में फिल्मी हस्तियों के परदे के पीछे वाले रोचक किस्से छपते थे। ‘मुसव्विर’ का संपादन करते हुए मंटो ने फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखना भी आरम्भ किया। ‘इम्पीरियल फिल्म कम्पनी’ के लिए मंटो ने संवाद लिखे तो ‘मुसव्विर’ के मालिक नजीर ने उसके संपादन की तनख्वाह आधी कर दी। क्योंकि नजीर ने ही उसे चालीस रूपये मेहनताने पर ‘फिल्म कंपनी’ में रखवाया था। इससे रूष्ट होकर मंटो ने ‘मुसव्विर’ का संपादन छोड़कर ‘समाज मासिक पत्रिका’ का संपादन आरम्भ कर दिया। परन्तु शीघ्र ही ‘मुसव्विर’ के मालिकों ने उसे वापस बुला लिया। और अनेक प्रलोभन देते हुए, पुरानी तनख्वाह चालीस से बढ़ाकर अस्सी कर दी। ऊपर से फिल्म की कहानी लिखने का मेहनताना अलग से देने का वादा किया।
क्योंकि मंटो, विरोधी स्वाभाव वाला व्यक्ति था। पत्र के मालिक जैसा कहते, वह ठीक उनके विपरीत किया करता। इसलिए ‘मुसव्विर’ छोड़कर वह ‘फिल्म इंडिया’ के संपादक बाबूराव पटेल से मिला, जो ‘कारवाँ’ नामक साप्ताहिक उर्दू पत्र निकालते थे। बाबूराव पटेल ने 150 रूपये महीना की तनख्वाह पर मंटो से ‘कारवाँ’ का संपादन करने की पेशकश की। लेकिन उसने सशर्त 60 रूपये महीना पर इसका संपादन किया। मुसव्विर, समाज और कारवाँ जैसे पत्रों का संपादन करते हुए मंटो धीरे-धीरे फिल्म-पटकथा, कहानी और रेडियो ड्रामें लेखन की ओर मुड़ गया। फिर उसने पत्रकारिता की ओर मुड़कर नहीं देखा। तथापि वह व्यंग्यात्मक लेख लिखता रहा, जिनकी पत्र-पत्रिकाओं में जबरदस्त माँग रहती। बाल की खाल, नितनई और चश्म-ए-रोज स्तम्भों के अन्तर्गत उसने बेखौफ और बेबाक होकर लिखा। अवसर मिलते ही वह बड़ी हस्तियों तक पर कटाक्ष करने से नहीं चूकता था। प्रसिद्ध नृत्यांगना और फिल्म अभिनेत्री सितारादेवी तथा फिल्म निर्देशक कारदार के साथ मंटो का सदैव छत्तीस का आँकड़ा रहा। क्योंकि मंटो निडर था इसलिए उसने समाज या बड़ी हस्तियों की कभी कोई परवाह नहीं की। इतना ही नहीं उसने पाकिस्तान में अमेरिकी नीतियों का भी खुलकर विरोध किया।
‘उग्र’ और मंटो ऐसे संपादक-पत्रकार थे जिन्होंने अभिव्यक्ति के समस्त खतरे उठाए। उन्होंने सत्य को सत्य कहने में कभी आनाकानी नहीं की, परिणाम भले ही कुछ भी निकला हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो ‘उग्र’ और मंटो की पत्रकारिता, पीत-पत्रकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण है। ‘उग्र’ यदि आजीवन उग्र बने रहे तो मंटो ने भी अपने भीतर छिपे क्रान्तिकारी व्यक्तित्व को प्रकट किया। दोनों कभी किसी से डरे नहीं, दबे नहीं, झुके नहीं। वे संपादक और पत्रकार की शक्ति भली-भाँति जानते थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा डंके की चोट पर कहा। साहित्य के साथ ही पत्रकारिता जगत में भी ‘उग्र’ और मंटो सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे।
पटकथा लेखक के रूप में भी ‘उग्र’ और मंटों ने काफी लेखन कार्य किया। वे दोनों साहित्य से सिनेमा की ओर मुड़े अवश्य लेकिन वापस साहित्य में ही आ गए। सफलता दोनों में से किसी को नहीं मिली। इस मामले में दोनों को समान स्तर का समझा जा सकता है।
‘उग्र’ पहली बार सन् 1924 में सिनेमा से जुड़े थे। ‘साप्ताहिक स्वदेश’ के विजयांक का संपादन करने के कारण जब उनके विरूद्ध वारंट निकला वे पुलिस से बचने के लिए मुंबई भागकर फिल्मी दुनिया में सम्मिलित हो गए। अपने मित्र भगवती प्रसाद मिश्र के साथ मिलकर मूक फिल्मों में अभिनय और लेखन कार्य करने लगे। लेकिन इस समय वे केवल पाँच महीने ही फिल्मी दुनिया में रहे। दूसरी बार ‘चाकलेट’ के कारण ‘घासलेटी आन्दोलन’ से चिढ़कर सन् 1930 में वे फिल्मी जगत से जुड़े। इस बार वे पूरे आठ वर्ष अर्थात् 1938 तक वहाँ जमे रहे। वे फिल्मों में संवाद, पटकथा और गीत आदि लिखते रहे और मजे लेते रहे। उन्होंने अपने फिल्मी जीवन को ‘सिनेमा संसार और मैं’ नामक आलेख में अभिव्यक्ति दी है। यह आलेख ‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ के फिल्म गोष्ठी’ विशेषांक में 27 फरवरी 1955 को प्रकाशित हुआ था। जब दूसरी बार ‘उग्र’ फिल्मी दुनिया में पहुँचे तब बोलते चलचित्रों का उदय हो रहा था और मूक चलचित्रों की आभा फीकी पड़ती जा रही थी। सन् 1931-32 तक भारत में इनी-गिनी ध्वनि ग्रहिणी मशीने ही आई थी। भारतीय फिल्मों का पहला बोलचित्र ‘आलमआरा’ जब मुंबई की ‘इंपीरियल फिल्म कंपनी’ में बनकर तैयार हो रहा था उन्ही दिनों ‘शारदा फिल्म कंपनी’ में जर्मन रेकार्डिंग मशीन पर ‘उग्र’ का लिखा हुआ चित्र भी उतारा जा रहा था। वह फिल्म ‘शशि-पुन्नू’ सिंधी प्रेमियों की लोककथा पर आधारित थी। लेकिन जर्मन मशीन की गड़बड़ी के कारण ध्वनि अंकन बहुत खराब हुआ। जिसके कारण ‘शशि-पुन्नू’ चलचित्र असफल हो गया। कंपनी के स्वामी भोगीलाल को लाखों की हानि हुई। ‘शशि-पुन्नू’ की असफलता के बाद भी ‘उग्र’ अपनी सिद्धहस्त लेखनी के कारण फिल्मी दुनिया के लिए प्रासंगिक बने रहे। एक सफल फिल्म में किस चीज का क्या महत्व होता है वे भली-भाँति जानते थे। फिल्म कहानी के विषय में उन्होंने लिखा है, ‘‘कहानी अच्छी न होने से सर्वांग सुंदर फिल्म भी असफल हो जाता है और शरतबाबू जैसी कहानी होने से अन्य गुणों के अभाव में भी तस्वीरें सफलता का सोना बरसा जाती हैं। तत्वतः फिल्म के धंधे में कहानी की जगह सर्वोच्च है।’’
‘उग्र’ आदर्शवादी या मार्यादावादी लेखक तो थे नहीं, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो मार्ग चुना था, फिल्म लेखन के क्षेत्र में भी उसी को अपनाया था। उनकी लिखी फिल्मी कहानियाँ अश्लील होती थी, पर उनकी माँग सदैव बनी रहती। दर्शकों को क्या चाहिए ‘उग्र’ अच्छी तरह जानते थे। तभी तो उनकी मिरजापुरी अक्खड़ता और भोजपुरी गालियों के कारण जब वे महालक्ष्मी फिल्म कपनी से निकाले गए और उनके स्थान पर प्रेमचंद आए तो, प्रेमचंद फिल्मों में कहानियाँ लिखते हुए आहत होने लगे। फिल्मकारों के लिए नग्न यथार्थ सुपाच्य अश्लीलता और रोमांचक दृश्य जरूरी थे। इसलिए उन्होंने 7 फरवरी 1935 को जैनेन्द्र से अपनी असफलता का जिक्र करते हुए लिखा था, ‘मैं जो प्लाट सोचता हूँ उसमें आदर्शवाद घुस जाता है और कहा जाता है कि उसमें ‘एन्टरटेनमेंट वैल्यू (मनोरंजननात्मक क्षमता) नहीं है।’
‘उग्र’ जब ‘सागर फिल्म कंपनी’ के लिए कहानियाँ लिख रहे थे, उस समय उनकी भेट आचार्य चतुरसेन शास्त्री से हुई। एक रात चतुरसेन जी, ‘उग्र’ के साथ शूटिंग देखने चले गए। ‘उग्र’ द्वारा लिखी फिल्म-कहानी के अश्लील दृश्य देखकर वे हतप्रभ रह गए। वापस घर लौटकर उन्होंने ‘उग्र’ के विरूद्ध ‘विशाल भारत’ को एक लेख लिखा। जिसने पहले से ही ‘उग्र’ के विरूद्ध ‘घासलेटी आन्दोलन’ छेड़ रखा था। ‘उग्र’ बाजार भाव पहचानते थे, इसलिए वे अपने दर्शकों के अनुरूप लिखते थे। अपने द्वारा लिखी कुछ प्रमुख फिल्मों के विषय में बताते हुए उन्होंने लिखा है, ‘‘शशि-पुन्नू’ की असफलता के बाद ही मैंने फिल्म जगत का त्याग किया हो सो बात नहीं। अपनी लिखी चार और फिल्मों के नाम मुझे याद आ रहे हैं- रामविलास (शारदा फिल्म), पतित पावन (प्रतिभा पिक्चर्स फोटोफोन), राधामोहन नंदलाल (महालक्ष्मी फिल्म कंपनी) और ‘छोटी बहू’ उन दिनों की सफलता की कसौटी पर सफल चित्र थे। ‘छोटी बहू’ की कहानी ‘गुजराती’ लेखक शैदा जी की थी, केवल संवाद मेरे थे।’’ फिल्म ‘छोटी बहू’ संवादों के बाँकपन के कारण ही बाक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिल्म के कलाकार ‘उग्र’ के सांवादिक कौशल पर मुग्ध थे। और ‘उग्र’ की तूती पूरे फिल्मिस्तान मे बोलने लगी थी। पूर्व की फिल्मों में से ‘रामविलास’ और ‘पतित पावन’ दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। जबकि ‘राधामोहन नंदलाल’ फिल्म दर्शकों द्वारा पंसद की गई। ‘उग्र’ के द्वारा लिखी फिल्मों में उस समय के श्रेष्ठ कलाकारों ने अभिनय किया था। अपने फिल्मी जीवन को स्मरण करते हुए वे लिखते हैं, ‘‘पृथ्वीराज कपूर युग के मुंबई फिल्म कलाकार, डायरेक्टर, केमरामैन, साउंडरेकार्डिस्ट और फिल्म कंपनियों के मालिक मुझे मजे में जानते थे- परिचित और अपरिचित दोनों।’’ पृथ्वीराज कपूर उनके विशेष मित्रों में से थे। हिन्दी फिल्मों के प्रथम गीत गायक के.एल. सहगल से भी उनका परिचय था। मुंबई में विशेष प्रकार की अंग्रेजी शराब पीने, रेस खेलने तथा अपनी बुरी आदतों के कारण जब ‘उग्र’ कर्ज से लद गए, तो वे कर्जदारों से भागकर मालवा इंदौर चले गए।
तीसरी बार सन् 1945 में वे फिर मुंबई आए। परन्तु इस बार माया नगरी मुंबई ने न उन्हें मस्तियाँ लेने दी और न ढाई वर्ष से अधिक ठहरने दिया। फिल्मी दुनियाँ के विभिन्न रंग-रूप उन्होंने अपनी आँखों से देखे थे, जिनका ‘फागुन के दिन चार’ नामक उपन्यास में उन्होंने दृश्यांकन भी किया है।
‘उग्र’ के समान ‘सआदत हसन मंटो भी ऐसा कथाकार है जो सिनेमा जगत की चमक-दमक से आकर्षित होकर अधिक रूपये कमाने के लालच में साहित्य से सिनेमा की ओर मुड़ा पर सफलता न मिलने पर पुनः साहित्य की ओर लौट गया। ‘मुसव्विर’ नामक पत्र का संपादन करते हुए, मंटो को फिल्मी दुनिया में प्रवेश मिल गया था। क्योंकि ‘मुसव्विर’ एक फिल्मी पत्र था, इसलिए मंटो के लिए फिल्म कंपनियों के मालिकों, निर्देशकों और नायक-नायिकाओं आदि से मिलने का टिकट सिद्ध हुआ। फिल्मी खबरों की खोज के लिए वह संबंधित व्यक्तियों से मिलता था। इस सिलसिले में वह ‘इंपीरियल फिल्म कंपनी’ के मालिक सेठ आरडेशर ईरानी से मिला तो जान-पहचान बढ़ गई। अतः मंटो को कंपनी में अस्सी रूपये महीने पर संवाद लेखक की नौकरी मिल गई। इस कंपनी के लिए मंटो ने अपनी पहली फिल्म कहानी लिखी। लेकिन कंपनी के मालिक आरडेशर को यह पंसद नहीं आया कि कोई पत्रकार फिल्म की कहानी लिखे। उनकी दृष्टि में पत्रकार की हैसियत बाबू से अधिक नहीं थी। अतः वही कहानी किसी अन्य के नाम से स्वीकार की गई। मंटो अहंवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने इसे अपना अपमान समझा और कंपनी छोडकर ‘सरोज फिल्म कंपनी’ में चला गया। सरोज मूवी टोन या सरोज फिल्म कंपनी में मंटो को सौ रूपये महीना की नौकरी मिल गई लेकिन दो महीने बाद ही कंपनी का दिवालिया निकल गया। इसके लिए मंटो ने एक कहानी लिखी जो तीन चौथाई फिल्माई भी गई।
‘सरोज फिल्म कंपनी’ बन्द हो जाने पर उसके मालिक नानू भाई देसाई ने उसके स्थान पर ‘हिन्दुस्तान सिने टोन’ नाम से दूसरी नई फिल्म कंपनी खड़ी कर दी। उसमें मंटो सौ रूपये महीना पर नियुक्त हो गया। इंपीरियल और सरोज फिल्म कंपनियों में मंटो की हैसियत एक बाबू से अधिक की नहीं रही थी। उसे अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला ‘हिंदुस्तान सिनेटोन में’। यहीं उसने अपनी पहली फिल्म अपने नाम से लिखी। इस विषय में मंटो ने लिखा है, ‘‘मैं, अब फिल्मी दुनिया में दाखिल हो चुका था। कुछ देर मुंशी की हैसियत से इंपीरियल फिल्म कंपनी में काम किया अर्थात् डायरेक्टरों की आज्ञा के अनुसार उल्टी-सीधी भाषा में फिल्मों के संवाद लिखता रहा, साठ रूपये महीना पर। तरक्की की तो ‘हिंदुस्तान सिने टोन’ में सेठ नानू भाई देसाई के यहाँ सौ रूपये महीना पर नौकर होकर। यहाँ मैंने अपनी पहली फिल्मी कहानी ‘मड’ के नाम से लिखी जिसका उर्फ ‘अपनी नगरिया’ था।’’
फिल्म ‘मड’ (कीचड़) अर्थात् ‘अपनी नगरिया’ की पटकथा साम्यवादी विचारों पर आधारित थी। मंटो को डर था कि अंग्रेज सरकार के डर से कोई भी प्रोडयूसर ‘मड’ को फिल्माने का साहस नहीं करेगा। लेकिन नानू भाई देसाई दिलेर आदमी थे उन्होंने यह जुर्रत कर ही डाली। फिल्म डायरेक्ट की दादा गुंजाल ने। परिणामतः दंगे भड़कने के डर से सिनेमा हॉल में दर्शकों से अधिक पुलिस पहुँची। फिल्म बुरी तरह पिट गई। नानू भाई देसाई को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी।
आरम्भ में फिल्मिस्तान में मंटो की स्थिति अपरिचितों जैसी थी, पर धीरे-धीरे उसने अपनी योग्यता, हास्य और विनोद के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब कभी वह फिल्म कंपनियों के मालिकों, निर्देशकों और अन्य कलाकारों से मिलता, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता। शीघ्र ही उसे उक्त लोगों में अच्छी जान पहचान मिल गई। संबंध बढ़ने से एक कंपनी में काम छूटता तो तुरन्त दूसरी में मिल जाता। ‘हिंदुस्तान फिल्म कंपनी’ पर मंटो की उधारी के लगभग दो हजार रूपये बकाया थे। मंटो ने रूपये मांगे तो कंपनी मालिक के साथ अनबन हो गई। क्योंकि उस समय कंपनी की स्थिति बड़ी गंभीर थी। मामले ने तूल पकड़ा तो मंटो कंपनी छोड़कर ‘ताजमहल पिक्चर्स’ फिल्म कंपनी में चला गया। कंपनी के मालिक अहसान के साथ उसके अच्छे संबंध थे। ‘ताजमहल पिक्चर्स’ के लिए मंटो ने उजाला फिल्म लिखी। प्रोडक्शन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एस.मुखर्जी (फिल्म अभिनेता जॉय मुखर्जी के पिता) को सौंपी गई और हिरोईन के रूप में उस समय की प्रसिद्ध अदाकारा नसीम बानो (फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो की माँ) को लिया गया। परन्तु ‘उजाला’ एस. मुखर्जी के अतिरिक्त किसी के भी जीवन में उजाला नहीं कर पाई, क्योंकि वे नसीम बानों पर आसक्त हो गए थे, बाकी सभी को उसने अंधकार के गर्त में गिरा दिया।
इसके बाद मंटो को ‘बेगम’ फिल्म की कहानी लिखने की सलाह दी। बेगम की पटकथा लिखते समय मंटो को नसीम को समीप से देखने का अवसर मिला। क्योंकि मंटो और मुखर्जी दोपहर का भोजन नसीम बानो के घर खाते थे और प्रतिदिन रात को देर तक कहानी को परिष्कृत व संशोधित करते थे। ‘उजाला’ और ‘बेगम’ में से कोई भी फिल्म नहीं चल पाई अतः निराश होकर निर्माता-निर्देशक एस. मुखर्जी ने अभिनेत्री नसीम बानों के साथ भाग कर विवाह कर लिया और दिल्ली आ गया। लेकिन मंटो मुंबई में ही जमा रहा। इस समय तक मुंबई और मंटो एक दूसरे को रास आने लगे थे। मुंबई के साथ उसका दिल जुड़ गया था।
मंटो जब तक मुंबई में रहा, फिल्मों की पटकथा लिखने में अत्यधिक व्यस्त रहा। पर दुर्भाग्य से उसके द्वारा लिखी फिल्मों में से अधिकांश नहीं चल सकी। और जो सफल रही उनका श्रेय दूसरों को चला गया। रफीक गजनवी के लिए लिखी ‘नौकर’ कोई कमाल नहीं दिखा सकी। निर्देशक मिर्ज़ा साहब की लड़की के लिए फिल्म ‘बेली’ की कहानी लिखी तो वह भी बुरी तरह असफल रही। राजेन्द्र सिंह बेदी के संवादों के साथ उसने ‘मिर्ज़ा ग़ालिब’ लिखी। ये फिल्म समीक्षकों की नज़र में तो आई परन्तु प्रेक्षकों की दृष्टि से उतनी सफल नहीं रही। फिल्म को जो कुछ सफलता मिली, उसका सारा श्रेय सोहराब मोदी और सुरैया को मिल गया।
फिल्म कलाकार अशोक कुमार और मंटो बड़े अच्छे मित्र थे। दोनों ने मुंबई में काफी समय एक साथ व्यतीत किया था। मंटो ने अशोक कुमार के लिए अनेक फिल्मों की पटकथाएं लिखी, जिनमें से प्रमुख हैं- आगोश, जिद्दी, आठ-दिन, चल-चल रे नौजवान आदि। पर पूर्व की भाँति कोई भी सफलता के शिखर पर नहीं पहुँच सकी। जबकि सभी का निर्देशन अशोक कुमार ने किया था। फिल्म आगोश कमजोर अभिनय और प्रदर्शन के कारण पिटी। इस्मत चुगताई की कहानी ‘जिद्दी’ को लेकर मंटो ने पटकथा का रूप दिया तो वह अशोक कुमार को जँची नहीं और उन्होंने निर्देशन करने से मना कर दिया। फिल्म ‘आठ दिन’ में मंटो ने पागल फ्लाईट लेफ्टिनेंट कृपाराम का रोल किया, जो फुटबाल फेंककर कहा करता था कि उसने बम फेंका है। ‘आठ दिन’ ने भी पुराने दिनों को दोहराया। दर्शक मंटो को परदे पर देखकर प्रसन्न नहीं हुए। इसके नायक अशोक कुमार और नायिका नसीम बानो थे। फिल्म के निर्माण में पूरे दो वर्ष का समय लगा था। लेकिन फिल्म को अपेक्षित सफलता नहीं मिली।
सन् 1948 के आस-पास मुंबई में साम्प्रदायिक दंगे भड़के। ‘बांबे टाकीज’ में मुसलमानों की नियुक्तियों को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि वे नियुक्तियाँ मंटो के कारण हुई थी। कुछ आलोचकों के अनुसार इसी कारण मंटो पाकिस्तान चला गया। मंटो की अनुपस्थिति में उसकी लिखी कहानी पर ‘घमंड’ फिल्म बनी। लेकिन यह फिल्म भी सिनेमाघरों मे अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी। पाकिस्तानी फिल्मी जगत में उसे कोई अवसर नहीं मिला। क्योंकि उसकी असफलता की सूचना वहाँ उससे पहले पहुँच चुकी थी।
भारतीय सिनेमा के इतिहास में यदि मंटो के योगदान की बात की जाए तो उसके कारण ‘प्राण’ जैसा सशक्त कलाकार हिन्दी फिल्मों को मिला। फ़िल्मी हस्तियों के उसने जो संस्मरण-रेखाचित्र लिखे हैं उनमें प्राण का कई बार वर्णन किया है। उसने सन् 1937 में फिल्म ‘किसान कन्या’ को रंगीन बनाने का आंशिक प्रसास भी किया था। जिस मंटो ने अनेक फिल्मों की कहानियाँ लिखी उस पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में दो बेहतरीन फ़िल्में बनी। लेकिन वे फ़िल्में तब तक ठीक से समझ में नहीं आएंगी और न उनमें आनंद आएगा, जब तक आप मंटों के जीवन और उसके साहित्य से परिचित न हों। अन्यथा उन फिल्मों को देखकर मंटो से खीज और नफरत होगी।
‘उग्र’ और मंटो ऐसे पटकथा लेखक थे, जो विषम परिस्थितियों से जूझकर सिनेमा जगत की ओर मुड़े थे। वे साहित्यकार थे, अतः अपेक्षित सफलता न मिलने पर पुनः साहित्य की ओर प्रस्थान कर गए। फिर भी उन्होंने हिन्दी सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए जब भी हिन्दी सिनेमा का विकासात्मक इतिहास लिखा जाएगा तो ‘उग्र’ और मंटो अवश्य स्मरण किए जाएंगे।