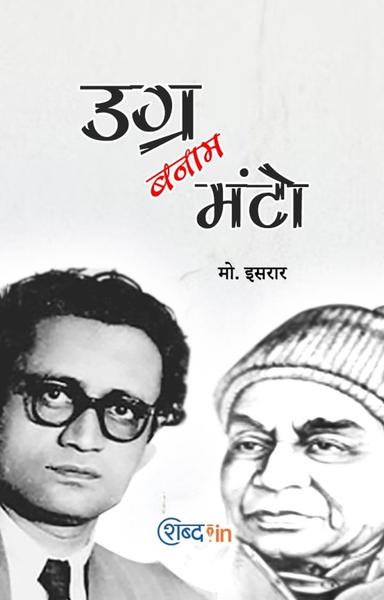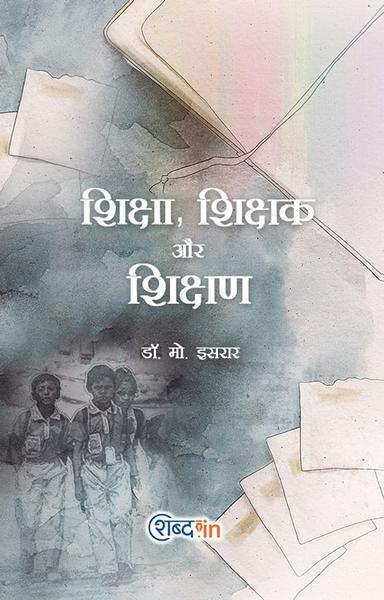हिन्दी साहित्य में ‘उग्र’ अपनी ही तरह के साहित्यकार माने जाते हैं। जिस तरह उनका नाम थोड़ा विचित्र सा है उसी प्रकार उनका साहित्य भी अपने ही ढंग का है। नाम ही देखिए आगे-पीछे जाति सूचक विशेषण और उससे जुड़ी विचित्र कहानी। ऊपर से विवादों के साथ चोली-दामन का रिश्ता। उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘अपनी खबर’ में स्वयं का परिचय देते हुआ कुछ इस प्रकार लिखा है, ‘‘मनिक बेचन पाँडे, वल्द बैजनाथ पाँडे, उम्र साठ साल, क़ौम बरहमन, पेशा अखबार नवीसी और अफसाना नवीसी, साक़िन मुहल्ला सद्दूपुर चुनार, जिला मिर्जापुर (यू0पी0) में विक्रमीय संवत् के 1957 (सन् 1900) वर्ष के पौष शुक्ल अष्टमी की रात आठ बजे कौशिक गोत्रोत्पन्न सरयूपारीण ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ।’’ यह ज्ञातव्य है कि ‘उग्र’ ने अपनी आत्मकथा, आचार्य शिवपूजन सहाय के कहने पर साठ वर्ष की आयु में लिखी थी। यह आत्मकथा उनके जीवनकाल में आए व्यक्तियों का स्मरण के आधार पर संस्मरण है। इसकी तिथियों में कुछ हेर-फेर हो सकता है क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, ‘‘डायरी रखने की आदत मैंने नहीं पाली है।’’ उनकी माता का नाम, ‘जयकली’ था, जिसे लोग बिगाड़कर ‘जयकल्ली’ कहते थे। माँ के स्वभाव के विषय में पता चलता है कि वह तेजस्वी, वैष्णव-हृदय होने के बावजूद भी परम उग्र, कराल-क्षत्राणी स्वभाव की, किन्तु भोली थी। बड़े बेटे के हाथों पिटने और परेशान किए जाने पर भी कभी प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन सोलह साल के ‘उग्र’ को मारने तक दौड़ती थी। माँ के अच्छे-बुरे स्वभाव का ‘उग्र’ पर सीधा प्रभाव पड़ा। क्योंकि वे विपत्तियों के समय प्रतिरोध या सामना करने के स्थान पर डर कर भाग खड़े हुए और सुख सुविधाओं के समय नैतिकता को भूलकर मजे लेने में व्यस्त हो गए।
बचपन में ‘उग्र’ अपनी माँ को ‘आई’ कहकर बुलाते थे। जिसका उन्हें उस समय अर्थ ज्ञात नहीं था। पर बड़े होने पर ज्ञात हुआ कि मराठी भाषा में माँ को ‘आई’ कहते हैं। ‘उग्र’ सहित उनके एक दर्जन भाई-बहन उत्पन्न हुए, लेकिन उनमें से उमाचरण पाँडे और श्रीचरण पाँडे ही जीवित बचे। ‘उग्र’ सबसे छोटे थे। उनके जन्म पर किसी को कोई उत्साह नहीं हुआ। कारण था परिवार की ग़रीबी। परिवार इतना निर्धन था कि लोग उन्हें ग़रीब और ब्राह्मण समझकर स्वयं ही उनके घर भीख पहुँचाते थे।
कहीं ‘उग्र’ भी अपने अग्रजों के समान दिवंगत न हो जाए, इस अंधविश्वास के कारण न उनकी कुंडली बनाई गई और न सगुन मनाया गया। साथ ही उन्हें ‘एक टके’ में एक दलित महिला को बेच दिया गया। इसलिए जन्मजात बिके जाने के कारण उनका नाम पड़ा- ‘बेचन’। ‘पाँडे’ उनकी पैतृक उपाधि थी। इसलिए वे हो गए ‘बेचन पाँडे’। यह नाम उन्हें जीवन भर नापसन्द रहा। फिर भी इस नाम का शुद्धिकरण ‘पांडेय बेचन शर्मा’ के रूप में करते हुए उन्होंने ‘उग्र’ उपनाम बाद में रखा।
जब वे केवल दो वर्ष के थे, उनके पिता का क्षय रोग से पीड़ित होकर देहान्त हो गया। पिता, सत्यवादी सज्जन और सिद्धान्तवादी ब्राह्मण थे। सत्यवादी हरिश्चन्द के समान, पिता की सत्य के पक्ष में गवाही देने के कारण ‘उग्र’ के परिवार को अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। पिता के देहान्त के पश्चात, घर की समस्त जिम्मेदारी उनके बड़े भाई उमाचरण पर आ गई, जो विवाहित थे। ‘उग्र’ के अनुसार उन्होंने विधिपूर्वक कुछ भी पढ़ा नहीं था, फिर भी हिन्दी, संस्कृत और बंगला अच्छी खासी जानते थे। समस्या-पूर्ति की कविताएं और गद्य लेखन भी किया करते थे। वैद्यक और ज्योतिष में भी टांग अड़ाने की क्षमता रखते थे।
सद्दूपुर की जिस गली में बेचन का जन्म हुआ था, उसमें सभी ब्राह्मण परिवारों की हालत बेचन के परिवार जैसी ही थी अर्थात् निर्धन, ग़रीब, दान-दक्षिणा पर जीवन यापन करने वाले। उस मुहल्ले में प्रायः जुआ खिला करता था। और जिसके घर जुआ खिलता उसे एक-दो रूपये नाल के रूप में मिलते। ग़रीबी की इस दुरावस्था में ‘उग्र’ के बड़े भाई ने भी घर में जुआ खिलाना और स्वयं भी खेलना आरंभ किया। नाल के रूप में जो रूपये मिलते उनसे घर की रोजी-रोटी चलती। जुएं के वक़्त माँ और भाभी को मकान के पिछले खंड में कैद कर दिया जाता और बेचन दरवाजे पर बैठकर पुलिसवालों से रखवाली करता। जिसके बदले में उसे भी पैसा दो पैसा मिलता।
जुएं की जबरदस्त लत पड़ जाने पर उमाचरण ने माँ और पत्नी, दोनों के गहने तक बेच ड़ाले। घर के बर्तन तक गिरवी रख दिए गए। खेत-खलिहानों की रक़म चरस-गाँजों में उड़ा दी गई। ऐसी स्थिति में कर्ज बढ़ता चला गया। रोज़ी-रोटी तक के लाले पड़ गए। जिसने विरोध किया उसकी बुरी तरह पिटाई हुई। माँ-पत्नी के साथ निरपराध बेचन भी पिटता था। एक दिन छापा मारकर पुलिस ने सभी जुंआरियों को पकड़ लिया, जिनमें उमाचरण पाँडे भी था। काफी दिन केस चलने पर सज़ा तो हुई, पर पचास रूपये जुर्माने पर रिहाई हो गई।
अत्यधिक कर्ज बढ़ने पर जब कर्ज़दाता बेइज्जत करने लगे तो, उमाचरण पहले काशी में और बाद में अयोध्या की रामलीला मंडली में अभिनय करने के लिए घर से चला आया। मुफ़्त भोजन और तीस रूपये मासिक पर मंडली में शामिल हो गया। अभिनय का शौंक उसे बचपन से ही था। दस रूपये घर भेजता, जिनसे परिवार का खर्च चलता। सात वर्ष की अवस्था में बेचन को भी अपने साथ मिलाकर ‘सीता’ के अभिनय का अभ्यास कराने लगा। जब बेचन आठ वर्ष का हुआ तो भाई ने उसे बनारस की एक रामलीला मंडली में बुला लिया, जिसमें उनके बड़े भाई उमाचरण स्वयं कार्यरत थे। बेचन को साथ रखने के उमाचरण को अनेक लाभ दिखाई दिये थे- एक, घर में कोई शरारती नहीं रहेगा। दूसरे उसकी निगरानी में रामलीलावालों की बुरी नज़र से बेचन बचा रहेगा। तीसरे, बिन तनख़्वाह के चैबीस घंटे ‘ब्वाय सरवेंट’ उपलब्ध होगा और चौथे लक्ष्मण या सीता का अभिनय करके आठ-दस रूपये महीना कमाकर भी देगा।
वहीं बेचन ने थोड़ा बहुत नाच-गाना और कुछ आरम्भिक शिक्षा ग्रहण की। उमाचरण अत्यधिक सख़्त स्वभाव का था। वह तनिक-सी गलती पर बेचन को खूब पीटता। अतः जब बेचन अपने भाई और पढ़ाई दोनों से तंग था, उसे ज्ञात हुआ कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर सब दुःख मिट जाते हैं। अत: उसने अपने एक सहपाठी, छोटी जाति के लड़के का हनुमान चालीसा चुरा लिया। चाव से पढ़ने पर कुछ सुफल दिखाई दिया। क्योंकि बेचन को स्कूली शिक्षा से हटाकर रामलीला मंडली में डटाया गया, जहाँ उसे ‘श्रीरामचरितमानस’ का पाठ करने का अवसर मिला। एक बार भरत का अभिनय करने वाला लड़का बीमार पड़ गया तो बेचन को पार्ट करने का मौका मिला। जिसे उसने, भाई और महन्त की मार के डर से इतनी सुन्दरता से निभाया कि सभी प्रसन्न हो गए। उसे दस रूपये ईनाम मिले और तनख़्वाह में एक रूपये की बढ़ोतरी हो गयी।
सन् 1910 में जब बेचन की अवस्था केवल दस वर्ष की थी, वह अपने बड़े भाई के साथ, नागा भागवतदास की रामलीला मंडली में शामिल हो गया। भागवतदास की मंडली उस समय पंजाब और सीमान्त प्रदेश की यात्रा पर थी। भागवतदास एक आँख से काने थे, जिन्हें लोग ‘भागवतदास कानियाँ’ कहकर पुकारते थे। उन पर ‘अंधे, काने और लंगड़े में एक ऐब फालतू होता है’ वाली कहावत पूर्णतः चरितार्थ होती थी। क्योंकि वे त्यागी और वैरागी होकर भी लंगोट के कच्चे और पैसे के अत्यधिक लोभी थे। उनकी मंडली में बेचन लक्षमण, भरत और सीता का अभिनय करने और ‘रामचरितमानस’ का पाठ करने में शीघ्र ही अभयस्त हो गया। क्योंकि तनिक सी भूल-चूक होने पर बड़े भाई द्वारा खूब पिटाई जो होती थी। ऊपर से महन्तजी के कठोर शासन में उनकी चाँवरी चलने का डर था। फिर भी बेचन के बड़े भाई उमाचरण पर भागवतदास की विशेष कृपा थी। क्योंकि वह उनके पत्र अच्छी हिन्दी में लिखा करता था।
एक बार भागवतदास की मंडली से बेचन और उनके बड़े भाई घर आए तो उमाचरण फिर से जुआ खेलने में जुट गया। कर्जदारो ने तंग करना आरंभ किया तो सन् 1911-12 में उमाचरण, बेचन के साथ मंझले भाई श्रीचरण पाँडे के आग्रह पर राममनोहरदास की रामलीला मंडली में सम्मिलित हो गया। बेचन जब चार वर्ष का था और श्रीचरण सोलह का, तब वह भाई-भाभी से लड़कर अयोध्या में राममनोहरदास की मंडली में शामिल हो गया था। राममनोहरदास, महन्त भागवतदास कानियाँ से अधिक धनवान और उदार थे। वैरागी होने पर भी वे गृहस्थों के समान बन-ठन कर रहते थे। उनकी मंडली संगठित और उत्तम थी।
रामलीला मंडलियों में फैले अनैतिक व्यभिचार का बेचन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी से प्रभावित होकर आगे चलकर उसने ‘चाकलेट’ नामक पुस्तक लिखी, जिसकी कहानियों का विषय ‘समलैंगिकता’ था। इसके पक्ष-विपक्ष में बहुत विवाद उठा। यहीं बेचन को सत्रह वर्षीय एक अभिरामा श्यामा से प्रेम हुआ, जो उसका पहला और अन्तिम प्रेम था। लेकिन उस ताकझाँक वाली आली को मंडली वालों ने बहला-फुसला कर पहले महन्त से उसका संयोग कराया, फिर स्वयं उसे बरबाद किया। फलतः वह यौन-रोग-ग्रस्त हो गई। भेद प्रकट हो जाने पर उसके पति ने उसे जलाकर मार डाला। बेचन ने जीवन भर उसकी याद को सीने से लगाए रखा। राममनोहरदास की मंडली के साथ बेचन ने दो-तीन वर्ष तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का खूब भ्रमण किया।
चौदह वर्ष की अवस्था में जब बेचन अपने भाई के साथ रामलीला मंडली से छुट्टियाँ मनाने चुनार आए तो राममनोहरदास से झगड़ा करके आए। फलतः उन्होंने मंडली में काम करने से मना कर दिया। बेचन के चाचा-चाची, जो पुत्रहीन थे और जिनकी केवल एक कन्या थी, ने उन्हें गोद ले लिया। चाची उनके प्रति बचपन से ही स्नेहमयी रही थी। चाचा ने चौदह वर्ष की अवस्था में चुनार के ‘चर्च मिशन स्कूल’ में तीसरी कक्षा में उनका नाम लिखाया। जब बेचन छठी कक्षा में पहुँचा तो उनकी चाची को सुन्दर सा पुत्र उत्पन्न हो गया। इसलिए शीघ्र ही उनका बेचन से मोह भंग हो गया और वे उसे भाई के जिम्मे छोड़कर बनारस चले गए। फीस, कपड़े और राशन की कमी के कारण बेचन की पढ़ाई वहीं की वहीं रूक गई। इसी बीच बेचन बनारस में चाचा की लड़की के गोने में गए तो वे उनके समक्ष गिड़गिड़ाए, ‘कि उनकी पढ़ाई का प्रबंध करें।’ उस समय बनारस में उनका साला और दामाद उन्हीं के व्यय से पढ़ते थे। दयावश चाचा ने बनारस के प्रसिद्ध ‘हिन्दू स्कूल’ में बेचन का प्रवेश करा दिया। वह छठी और सातवीं कक्षा चाचा की कृपा से उत्तीण हो गया। लेकिन आठवीं में आते ही चाचा उससे फिर विमुख हो गए। क्योंकि उन्होंने काशी के भदैनी मुहल्ले का मकान बेचकर खोजवाँ मे नया खरीद लिया था। तब निराश्रय बेचन को, बाबू शिवप्रसाद गुप्त की कृपा से ‘सेवा उपवन’ का सहारा मिल गया, जहाँ से उसे आटा, दाल, चावल और कुछ नकद पैसे मिल जाते थे।
हिन्दू स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ़ अपमानजनक तुकबंदी करने से उनकी नाराजगी के कारण बेचन कक्षा आठ में अनुत्तीर्ण हो गया। अतः ‘सेवा उपवन’ से मिलने वाली सेवा भी समाप्त हो गई। इसलिए निराधार बेचन ने बनारस में ठोकरे खाने से, घर में भाई की लात खाना अच्छा समझा। जब वह घर पहुँचा तो संयोग से भाई घर पर नहीं था। तभी किसी अहीरन ने उसे उधारी के दस रूपये भाभी को देने के लिए दिए। अतः भाई के डर से वह कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) भाग गया, जहाँ उनके पड़ौसी भाई विश्वनाथ त्रिपाठी रहते थे। लेकिन वहाँ पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि वे चुनार चले गए हैं। एक सप्ताह के पश्चात विश्वनाथ जी लौटे तो उन्होंने बेचन को एक रूपया रोज पर एक कम्पनी के दफ्तर में ग्राहकों के छपे फर्मो पर पता लिखने का काम दिला दिया। लेकिन एक महीने पश्चात ही बेचन, भाई के बुलावे पर कलकत्ता से काशी लौटकर लाला भगवानदीन के सम्पर्क में आकर काव्याभ्यास करने लगे।
कविताएं लिखने का चस्का बेचन को स्कूली जीवन से ही लग गया था। हिन्दू स्कूल में जब वे कक्षा आठ के छात्र थे, तब महात्मा गाँधी के जन्म दिवस पर पढ़ी जाने वाली उनकी कविता को दूसरा स्थान मिला था, पहला सुमित्रा नन्दन पंत की कविता को। इस प्रकार बेचन ने अपने लेखन की शुरूआत काव्य से की। लेकिन धीरे-धीरे अख़बारों के दफ्तरों में नौकरी करते हुए, यायावारी का जीवन व्यतीत करते हुए, कब और कैसे ‘उग्र’ जैसा कथाकार उभर आया, यह भी किसी रोचक कहानी से कम नहीं। वे जीवन भर अपने आपको कथाकार मानते रहे। ‘आज’ पत्र में उनकी पहली कविता, बाबू शिवप्रसाद गुप्त की कृपा से छपी थी। वह कविता राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण थी। परन्तु उनकी पहली कहानी ‘गाँधी आश्रम’ को संपादक महोदय ने अस्वीकृत कर दिया था। बाबू विष्णु पराड़कर जी ने उसमें आवश्यक सुधार किए तो वह बेचन के एक अन्य नाम ‘शशिमोहन शर्मा’ के नाम से छप गई। इस प्रकार धीरे-धीरे बेचन का साहित्य जगत में प्रवेश होने लगा।
11 अगस्त 1919 को गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले ‘साप्ताहिक स्वेदश’ के अंक में बेचन की ‘आह्वान’ कविता छपी। जिस पर संपादक ने लेखक का नाम दिया ‘श्रीयुत पांडेय बेचन शर्मा ‘उग्र’। अपने नाम का परिवर्तित रूप ‘पांडेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ उन्हे पसंद आया और उन्होंने यही नाम अपना लिया। लेकिन यह भी सत्य है कि व्यवस्थित जीवन न जी पाने के कारण भी बेचन को परिस्थितियों ने उग्र बनाया था। इस विषय में कई कहानियाँ प्रचलित हैं।
इसी समय उन्हें राष्ट्रीयगान-द्वन्द्व में सम्मिलित होना था, उन्होंने सोचा यह नाम राष्ट्र भक्त लेखकों को पंसद आएगा। क्योंकि उस समय राष्ट्रभक्त लेखक ऐसे कर्कश उपनाम, जैसे त्रिशूल, धूमकेतू, भीम, भयंकर, प्रलयंकर आदि इसलिए चुना करते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के नृशंस शासक नाम से ही दहल जाएँ। और यह सभी जानते हैं कि ‘उग्र’ की लेखनी में आरम्भ से ही अंग्रेजी राज के प्रति घोर घृणा थी और क्रान्तिकारियों के लिए प्रेम। ‘उग्र’ पर लाला भगवानदीन की विशेष कृपा रही, उन्हें ‘उग्र’ ने गुरूवत माना। उनके पुस्तकालय से वे एक हस्तलिखित सचित्र मासिक पत्र ‘उग्र’ भी प्रकाशित करते थे। ‘उग्र’ ने जब अपना प्रथम खण्ड काव्य ‘ध्रुव धारणा’ रचा तो लाला जी ने ही कई दिन तक परिश्रम करके उसकी त्रुटियों को दूर करते हुए उसे प्रकाशन के योग्य बनाया था। इसके पश्चात ‘उग्र’ ने ‘महात्मा ईसा’ नामक नाटक लिखा। इसका सम्यक संशोधन भी लाला भगवानदीन ने ही किया।
सन् 1920 के आस-पास देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन जोरों पर था। साहित्यकारों से आशा की जा रही थी कि वे भी नवजागरण के लिए, आजादी के लिए लिखें। इस प्रकार का साहित्य रचने के कारण ‘उग्र’ को कई बार ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा था। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया और वे जेल चले गए। 1921 में जेल से आने के पश्चात उनकी मुलाकात ‘आज’ मंडल के यशशवी संपादकों बाबूराव विष्णु पराड़कर, श्री प्रकाश गुप्त, सम्पूर्णानन्द, शिवप्रसाद गुप्त आदि से हुई। इनसे प्रेरित होकर ‘उग्र’ ने राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण अनेक कविताएं, प्रचारात्मक कहानियाँ, गद्यकाव्य, एकांकी, व्यंग्य-विनोद आदि लिखे। आज पत्र में ‘उग्र’ ने अष्टावक्र उपनाम से ऊटपटाँग शीषर्कों से हास्य-व्यंग्य के खूब लेख लिखे। इस समय तक वे धुँआधार लिखने लगे थे और उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी थी।
‘उग्र’ को आज में लिखने की मज़दूरी दस आने कालम के हिसाब से मिलती थी। साथ ही यह शर्त भी थी कि वे तीन रूपये मासिक से अधिक कालम नहीं लिखेंगे। आज के कारण ‘उग्र’ को खूब प्रसिद्धि मिली। इसी समय उनकी मुलाकात शचीन्द्रनाथ सान्याल और राजेन्द्र सिंह लोहड़ी जैसे क्रान्तिकारियों से हुई। इन दोनों ने ‘उग्र’ के क्रान्तिकारियों को नवीन ऊर्जा देने वाले, देशभक्ति-भावना से परिपूर्ण साहित्य का संग्रह किया। ‘उग्र’ की लेखनी में जो आग थी, उसके शचीन्द्रनाथ कायल थे। यही कारण था कि ‘उग्र’ क्रान्तिकारी कहानियों के जनक भी माने गए।
सन् 1924 आते-आते ‘उग्र’ हिन्दी साहित्य में काफी चर्चित और प्रसिद्ध हो चुके थे। लेकिन उन्हें आभास हो चला था कि काशी का वातावरण उनके अनुकूल नहीं रहा है। अतः जब वे, कुछ दिन ‘काकनाडा क्रांग्रेस’ में शामिल होने के पश्चात एक मित्र के साथ कलकत्ता ‘मतवाला मंडल’ देखने आए, तो उसी में शामिल हो गए। ‘मतवाला’ (साप्ताहिक-पत्र) में उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी। साथ ही पत्र के संस्थापक सेठ महादेव प्रसाद जी से, मिरजापुर में ‘उग्र’ का परिचय भी हो चुका था। मतवाला में उनका परिचय आचार्य शिवपूजन सहाय और निराला जैसे साहित्यकारों से हुआ। यहीं से उनके हंगामाखेज साहित्यिक जीवन की शुरूआत हुई।
अप्राकृतिक दुराचार की कलई खोलने वाली ‘चाकलेट’ की कहानियाँ किस्तवार जैसे ही मतवाला में प्रकाशित होने लगी, हिन्दी साहित्य में भूचाल-सा आ गया। ‘विशाल भारत’ के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी जी हाथ-धोकर ‘उग्र’ के पीछे पड़ गए और उनके साहित्य को ‘घासलेटी साहित्य’ की संज्ञा दे डाली। इसी बीच अक्टूबर 1924 में ‘उग्र’ दशरथ द्विवेदी द्वारा संपादित ‘स्वदेश’ के विजयांक’ का संपादन करने अतिथि के रूप में गोरखपुर आए। पत्र छपा प्रेमचंद जी के सरस्वती प्रेस में। पत्र छपते ही ब्रिटिश सरकार उनके विरूद्ध हो गई। क्योंकि सारा अंक देशभक्ति की भावना से प्रेरित था। ‘उग्र’ की ‘लाल क्रांति के पंजे में’ विस्फोटक एकांकी अधिक खटकी थी। फलत: सरस्वती प्रेस रौंद डाली गयी। प्रेमचंद के भाई महताब राय पकड़े गए। ‘उग्र’ के विरूद्ध सरकारी वारंट निकला तो वे कतकत्ता भाग गए। गोरखपुर का वारंट जब कलकत्ता आया तो वे मुंबई भाग गए। अपने एक साथी के संग साइलेन्ट फिल्म कंपनी में काम करने लगे। मुंबई की फिल्मी दुनियाँ में शराब, कबाब और भोग-क्रीड़ा का आनन्द उठाते हुए जब उन्हें छह महीने बीत गए तभी एक सी.आई.डी. वाले ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तीन महीने तक केस चलने के पश्चात नौ माह की सख्त जेल हुई। जेल में भी वे साहित्य साधना में रत रहे और अपने नाम अथवा छद्म नाम से ‘मतवाला’ में अपनी रचनाएं भेजते रहे। जेल से छूटकर मतवाला कार्यालय में आए तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। सन् 1927 में उग्र ने ‘बुढ़ापा और रूपया’ (जिन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने कथात्मक शैली के निबंध कहा है) नामक कहानियाँ, ‘आज’ पत्र के लिए लिखी। इनके कारण सरकार ने उन्हें फिर से कैद कर लिया।
सन् 1927 से 1929 का समय ‘उग्र’ के जीवन का सबसे अधिक कोलाहलकारी रहा। उनके सभी महत्वपूर्ण उपन्यास जैसे ‘चन्द हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, आदि ‘मतवाला’ में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुए। इन उपन्यासों ने पाठकीय बाजार-भाव के सभी कीर्तिमान तोड़ दिए। सन् 1929 आते-आते ‘मतवाला’ की स्थिति बिगड़ने लगी। मंडल के सदस्यों में आन्तरिक कलह रहने लगा। ‘उग्र’ की निराला के साथ भावों की भिडंत हो उठी। ‘मतवाला’ के संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ के एक मात्र पुत्र हरगोविंद सेठ, जो मिरजापुर में रहते थे, वे ‘मतवाला’ को भी मिरजापुर में ही लाना चाहते थे। मंडल का कोई भी सदस्य इससे सहमत नहीं था। यहाँ तक कि निराला और ‘उग्र’ ने भी इसका विरोध किया। हरगोविंद जी ने किसी की परवाह नहीं की और सन् 1929 में ‘मतवाला’ मिरजापुर से प्रकाशित होने लगा। ‘उग्र’ जी ‘चाकलेट’ के कारण मिरजापुर में अत्यधिक बदनाम होने के कारण, वहाँ नहीं आना चाहते थे। इसलिए वे ‘मतवाला-मंडल’ और हिन्दी साहित्य से अलग हो गए और मुंबई जाकर फिल्मी दुनियाँ में शामिल हो गए।
सन् 1930 में जब दूसरी बार वे फिल्मी दुनिया में आए तो उस समय बोलती फिल्मों का दौर आरंभ हो चुका था। नई-नई तक़निकियाँ फिल्मों में प्रयुक्त होने लगी थी। अच्छी फिल्म कम्पनियों ने साउंड रिकार्डिंग मशीने खरीद ली थी। उस समय ‘इम्पीरियल फिल्म कंपनी’ पूरे मुंबई में सबसे आगे थी। पर उसमें उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। अतः वे ‘शारदा फिल्म कंपनी’ से जुड़ गए। इस कंपनी के लिए जब उन्होंने सिन्धी प्रेमियों की लोक कथा पर कहानी लिखी, तो फिल्म बुरी तरह असफल हो गई। फिल्म कंपनी तो डूबी ही उसके मालिक भोगीलाल भाव जी क्षति को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दुनिया से ही उठ गए।
अपने फिल्मी जीवन को ‘उग्र’ ने ‘सिनेमा संसार और मैं’ आलेख में विस्तार से वर्णित किया है। यह आलेख 27 फरवरी 1955 को साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ था। शारदा फिल्म कंपनी का दिवाला निकलने के पश्चात वे ‘सागर फिल्म कंपनी’ के लिए फिल्म लेखन करने लगे। उनकी लिखी फिल्मी कहानियाँ अत्यधिक अश्लील होती थी। इसी समय जब उनकी मुलाकात आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी से हुई तो एक रात वे ‘उग्र’ के साथ सागर कंपनी का शूटिंग-दृश्य देखने चले गए। वे ‘उग्र’ के अश्लील दृश्य-परिदृश्य देखकर क्षुब्ध रह गए और उनके विरूद्ध ‘विशाल भारत’ में एक लेख लिखा। विशाल भारत पत्र के संपादक पं0 बनारसीदस चतुर्वेदी, जो प्रेमचंद जी के समक्ष प्रतिज्ञा कर चुके थे कि ‘उग्र’ के घासलेटी साहित्य के विरूद्ध कोई लेख नहीं लिखेंगे। शास्त्री जी का लेख मिलते ही अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। ‘विशाल भारत’ तो ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा करता ही रहा था। इसलिए ‘उग्र’ के विरुद्ध फिर से आन्दोलन आरम्भ हो गया।
अपनी अश्लीलता के कारण ‘उग्र’ न केवल साहित्य जगत बल्कि फिल्मी दुनिया में भी काफी बदनाम हो चुके थे। जब वे ‘महालक्ष्मी फिल्म कंपनी’ के लिए फिल्म लेखन कर रहे थे, तो अपने असभ्य व्यवहार और भद्दी भोजपुरी गालियों के कारण कंपनी से बाहर निकाल दिए गए थे। हालांकि इस कंपनी में बनी फिल्म ‘छोटी-बहू’ बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही थी। फिल्म की कहानी ‘शैदा’ ने और संवाद ‘उग्र’ ने लिखे थे। पूरी फिल्मी दुनिया में ‘उग्र’ की तूती बोलने लगी थी। फिल्म के कलाकार दुर्गा खोटे, जुबैदा, मामा गोरे आदि सभी ‘उग्र’ के सांवादिक कौशल पर मुग्ध थे। जबकि डायरेक्टर, कैमरामैन, साज-सज्जा करने वाले आदि उनके असामान्य बर्ताव से तंग थे। कंपनी से निकाले जाते समय किसी ने उनका पक्ष नहीं लिया। ‘उग्र’ सन् 1930 से 1938 तक यानि पूरे आठ वर्ष फिल्मी दुनिया में लिखते रहे और मजे लेते रहे।
फिल्म लेखन के क्षेत्र में उन्हें सफलता और विफलता दोनों ही मिली। उन्होंने केवल एक विषय (अश्लीलता) अपनाए रखा जबकि फिल्मी दुनिया में बहुमुखी प्रतिभा की आवश्यकता थी। यही कारण था कि उनसे फिल्मी दुनिया का एक विशेष वर्ग ही जुड़ा था। उनकी कहानियों और संवादों के आधार पर निर्मित रामविलास, पतितपावन और राधामोहन नन्दलाल नामक फ़िल्में परदे पर प्रदर्शित हुई। इनमें से रामविलास और पतितपावन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली परन्तु राधामोहन नन्दलाल फिल्म दर्शकों द्वारा सराही गयी।
पान की गिलौरियों पर सोने के वर्क़ चढ़े पान खाते हुए, शराब, कबाब और भोग का मजा लेते हुए जब ‘उग्र’ मुंबई में काफी कर्जदार हो गए तो वे मुंबई से भागकर मालवा आ गए। यहाँ कुछ महीने व्यतीत करने के पश्चात इंदौर चले गए। इंदौर में ‘मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति’ की मासिक पत्रिका ‘वीणा’ में सहायक संपादक का पद मिल गया। वहीं पर समिति की ओर से हिन्दी की प्रगति का आन्दोलन भी चलाने लगे। लेकिन ‘उग्र’ तो उग्र थे, शायद चैन से बैठना उन्हें अखरता था। इसलिए इंदौर में थोड़े से पैर जमते ही, यहीं से प्रकाशित ‘स्वराज्य’ नामक पत्र में मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति से जुड़े कुछ गणमान्य व्यक्तियों के विरूद्ध खुली चिट्ठी प्रकाशित करवाने लगे। उन चिट्ठियों में मध्य प्रदेश के राजशाही घराने से संबद्ध व्यक्तियों में भी छिद्रान्वेषण किया गया था। इंदौर की जनता को संबोधित करते हुए, ‘उग्र’ ने आरोप लगाया था कि समिति की उन्नति न हो पाने का कारण, इसके कर्ता-धरता समिति के तवे पर अपने मतलब की रोटियाँ सेकना चाहते हैं और जनता को ठग रहे हैं।
हिन्दी की उन्नति और प्रगति के लिए ‘उग्र’ ने समिति को अनेक सुझाव दिए। इसके लिए वे राज्य के प्रधानमंत्री तक मिले। परन्तु ‘स्वराज्य’ में दिए गए उग्र ब्यानों के कारण इंदौर के कई लोगों को सामाजिक बदनामियाँ भी झेलनी पड़ी थी। इसलिए उनके विरूद्ध साजिश रची जाने लगी। अतः जब वे सन् 1941 में एक महीने के लिए ‘विक्रम’ नामक पत्र का संपादन करने उज्जैन गए, तभी ‘वीणा’ के प्रबंध मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर ‘उग्र’ को वीणा से अलग कर दिया। साथ ही वीणा में उनकी कोई भी रचना प्रकाशित न करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनकी जो रचनाएं प्रकाशन के लिए स्वीकृत थी वे भी जब्त कर ली गई। सभी रचनाएं व्यंग्यात्मक थी जो इंदौर के सम्मानित व्यक्तियों और मध्यप्रदेश के राजशाही घराने से संबंधित थी।
सन् 1945 तक आते-आते इंदौर की फिजा ‘उग्र’ के लिए और उग्र हो गयी। शायद वे अपनी सीमा से आगे बढ़कर लोगों पर आक्षेप करने लगे थे। जब उन्हें कोई सहारा, कोई संस्थान और संरक्षण न दिखाई दिया, उन्होंने विवश होकर इंदौर छोड़ दिया। वे तीसरी बार मुंबई चले गए। लेकिन समय से दो क़दम आगे चलने वाले मुंबई शहर की फिजा भी अब बदल चुकी थी। अतः इस बार मुंबई ने उन्हें मस्तियाँ लेने का कोई माहौल नहीं दिया। यहाँ उन्होंने सन् 1945 में ‘साप्ताहिक संग्राम’ और सन् 1947 में ‘विक्रम मासिक’ का संपादन किया। पर इनके प्रकाशन में उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। किसी प्रकार ढ़ाई वर्ष मुंबई में व्यतीत किए। सन् 1948 में महादेव प्रसाद सेठ के पुत्र हरगोविंद सेठ के आग्रह पर मिरजापुर आ गए और हरगोविंद सेठ द्वारा उपलब्ध सुविधाओं से प्रसन्न होकर उन्होंने ‘मतवाला’ का पुनः प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया।
‘उग्र’ अक्खड़-फक्कड़ और घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। एक स्थान पर टिके रहना उनके स्वभाव के अनुकूल न था अथवा वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती कि ‘उग्र’ को मैदान छोड़कर भागना पड़ता। वे जीवन भर यायावारी का जीवन व्यतीत करते रहे। शहरी जीवन के आदि हो चुके ‘उग्र’ सन् 1950 में मिरजापुर से कलकत्ता आ गए। सन् 1952 तक का समय बुरी तरह काटा। भाग्य प्रतिकूल बना रहा। सन् 1953 में दिल्ली आए और हास्य-व्यंग्य से परिपूर्ण ‘उग्र’ नामक पत्र का संपादन करने लगे। चार अंक निकलने के पश्चात ही पत्र बंद हो गया। कुछ समय के लिए जयपुर चले गए, पर वहाँ मन नहीं लगा तो पुनः दिल्ली लौट आए। दिल्ली सब्जी मंडी और पंजाबी बाग में सात-आठ महीने रहने के पश्चात लोधी बस्ती में चले गए। वहाँ तीन वर्ष व्यतीत करने के पश्चात, यमुनापार कृष्णानगर में रहने लगे। दिल्ली में निवास करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। जिनमें से जी जी जी, फागुन के दिन चार और गंगामाता महत्वपूर्ण है। गंगामाता अधूरा था जिसे हंसराज रहबर ने ‘उग्र’ की मृत्यु के बाद अपने ठंग से पूरा किया। फागुन के दिन चार आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास है, जिससे ‘उग्र’ के जीवन और रचना- सिद्धान्त को गहराई से समझने में बहुत सहायता मिलती है।
‘उग्र’ ऐसे लेखक थे जिन्होंने जीवन को जिया नहीं बल्कि झेला। उन्होंने सामाजिक विसंगतियों पर खूब प्रहार किए, भले ही परिणाम कुछ भी निकलता हो। वे किसी से डरे नहीं, दबे नहीं, झुके नहीं पर टूट अवश्य गए थे। विंडबनाओं को झेलते हुए 23 मार्च 1967 को दिल्ली में इस दुनिया को अलविदा कह गए। सन् 1924 से 1967 तक वे विकृत-संस्कारी लेखक बने रहे। हिन्दी साहित्य में उनके बहिष्कार का जो आन्दोलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने 1925 में आरम्भ किया था वह उनकी मृत्यु तक जारी रहा। फिर भी उन्हें अन्तिम समय में थोड़ा संतोष था, क्योंकि उनके जीवनकाल में ही उन पर शोध कार्य होने लगा था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है- ‘‘सागर विश्वविद्यालय आजकल ‘उग्र’ पर रिसर्च करा रहा है। उसी हनुमान चालीसा चुराने वाले पर।’’