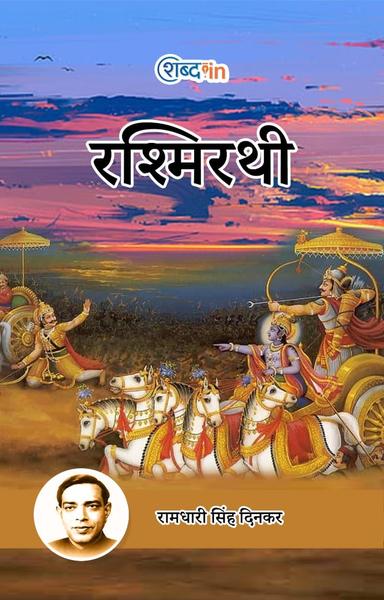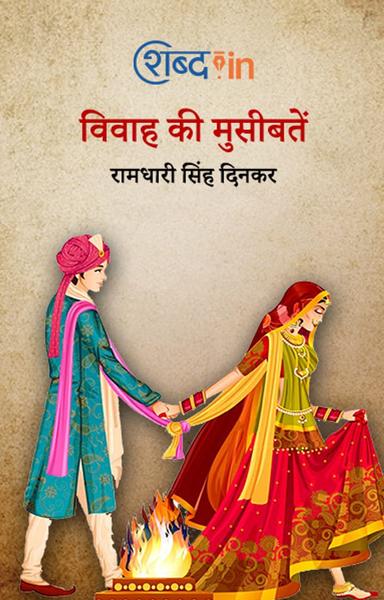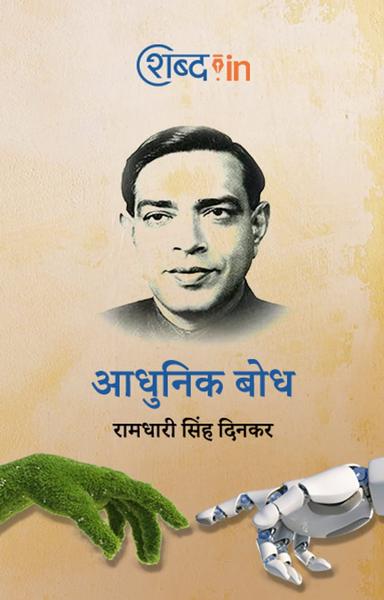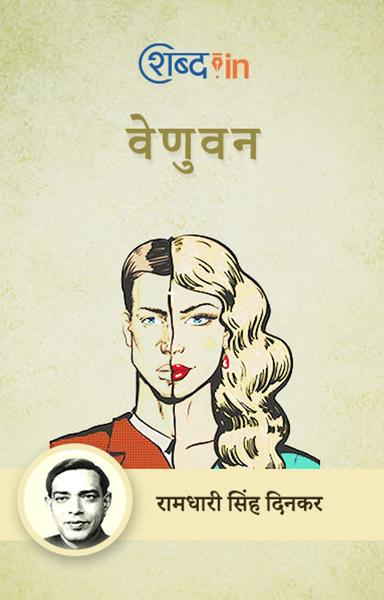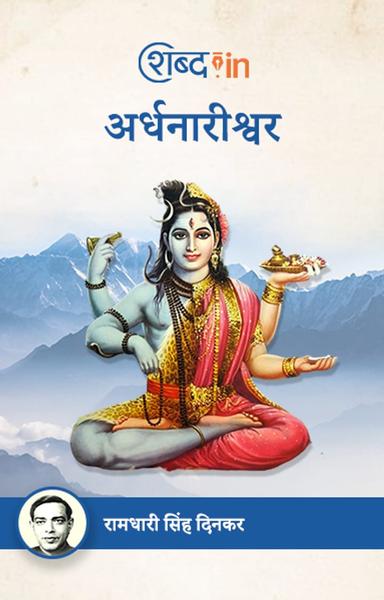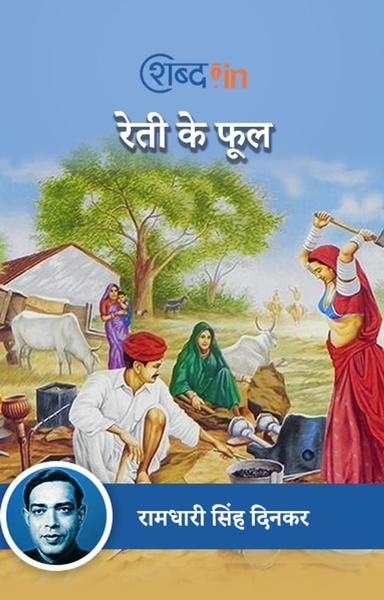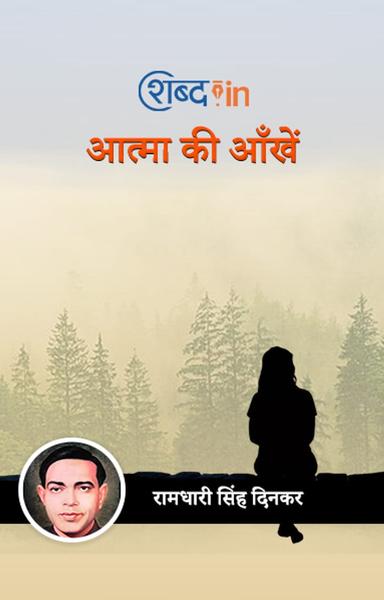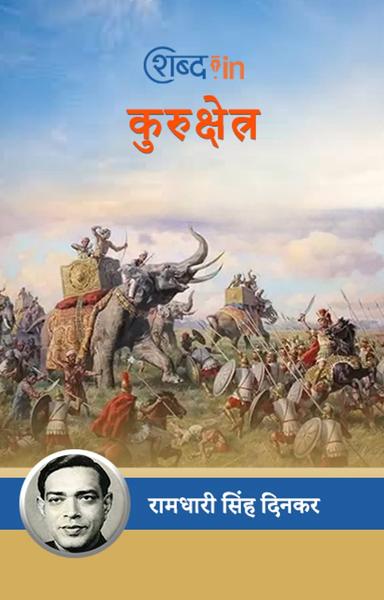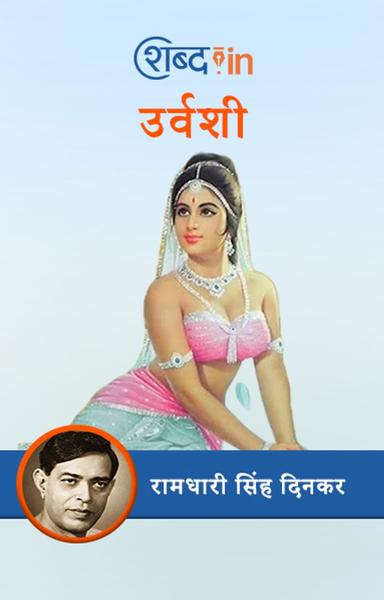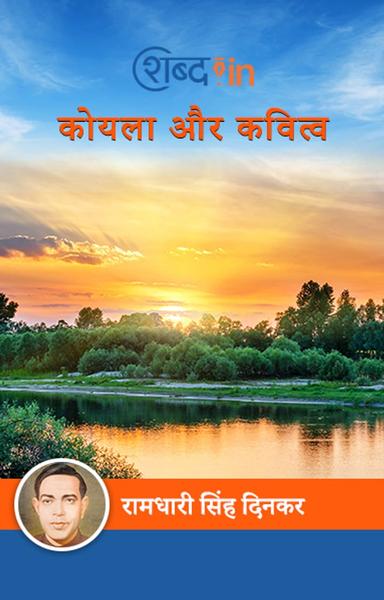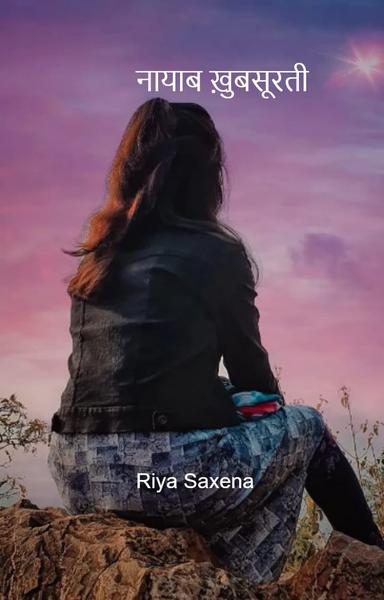पंचम अंक आरम्भ
अहमपि तव सूनावद्य विन्यस्य राज्यम्
विचरित्मृग्यूथान्याश्रयिष्ये वनानि
-विक्रमोर्वशीयम्
क्रन्दंस देशदेशेषु बभ्राम नृपति: स्वयं।
-देवीभागवत
अवेत्य शापदोषं तं सोअथ गत्वा पुरुरवा
हरेराराधनं चक्रे ततो बदरिकाश्रमे
-कथासरित्सागर
स्थान-पुरुरवा का राजप्रसाद
[पुरुरवा, उर्वशी, महामात्य, राज-पंडित, राज-ज्योतिषी,
अन्य सभासद, परिचायक और परिचारिकाएँ यथास्थान
बैठे या खड़े । राजा की मुद्रा अत्यंत चिंताग्रस्त। आरम्भ
में, कई क्षणों तक, कोई कुछ नहीं बोलता]
महामात्य देव क्षमा हो कुतुक, महामय के विशाल नयनों में,
देख रहा हूँ, आज नई चिंता कुछ घुमड़ रही है ।
महाराज जब से आए हैं, मूक, विषण्ण, अचल हैं
सुखदायक कल रोर रोक, निस्पन्द किए लहरों को
महासिन्धु क्यों, इस प्रकार, अपने में डूब गया है?
सभा सन्न है, कौन विपद हम पर आने वाली है?
पुरुरवा
कुशल करें अर्यमा, मरुद्गण उतर व्योम-मन्डल से
अभिषुत सोम ग्रहण करने को आते रहें भुवन में ।
वरुण रखें प्रज्वलित निरंतर आहवनीय अनल को,
रहे दृष्टि हम पर अभीष्ट-वर्षी अमोघ मघवा की
सभासदो! कल रात स्वप्न मैने विचित्र देखा है ।
सभी सभासद
स्वप्न! पुरुरवा
स्वप्न ही कहो, यद्यपि मेरे मन की आंखों के
आगे, अब भी, सभी दृश्य वैसे ही घूम रहे हैं,
जैसे, सुप्ति और जागृति के धूमिल, द्वाभ क्षितिज पर
मैने उन्हें सत्य, चेतना, सुस्पष्ट, स्वच्छ देखा था ।
कितनी अद्भुत कथा! दृश्य वह मानव की छलना थी?
या जो मुद्रित पृष्ठ अभी आगे खुलने वाले हैं,
देख गया हूँ उन्हें रात निद्रित भविष्य में जा कर?
कौन कहे, जिसको देखा, वह सारहीन सपना था
या कि स्वप्न है वह जिसको अब जग कर देख रहा हूँ?
क्या जानें, जागरण स्वप्न है या कि स्वप्न जागृति है?
महामात्य
बड़ी विलक्षण बात! देव ने ऐसा क्या देखा है,
जिससे जागृति और स्वप्न की दूरी बिला रही है,
परछाईं पड़ रही अनागत की आगत के मुख पर,
मुँदी हुई पोथी भविष्य की उन्मीलित लगती है?
देव दया कर कहें स्पष्ट, दुश्चिंत्य स्वप्न वह क्या था?
अश्विद्वय की कृपा, विघ्न जो भी हों, टल जाएँगे ।
पुरुरवा
कौन विघ्न किसका? जो है, जो अब होने वाला है,
सब है बद्ध निगूढ, एक ऋत के शाश्वत धागे में;
कहो उसे प्रारब्ध, नियति या लीला सौम्य प्रकृति की ।
बीज गिरा जो यहाँ, वृक्ष बनकर अवश्य निकलेगा ।
किंतु, भीत मैं नहीं; गर्त के अतल, गहन गह्वर में
जाना हो तो उसी वीरता से प्रदीप्त जाऊँगा
जैसे ऊपर विविध व्योम-लोगों में घूम चुका हूँ ।
भीति नहीं यह मौन; मूकता में यह सोच रहा हूँ,
अबकी बार भविष्य कौन-सा वेष लिए आता है ।
महामात्य
महाराज का मन बलिष्ठ; संकल्प-शुद्ध अंतर है ।
जिसकी बाँहों के प्रसाद से सुर अचिंत रहते हैं,
उस अजेय के लिए कहाँ है भय द्यावा-पृथ्वी पर?
प्रभु अभीक ही रहें; किंतु, हे देव! स्वप्न वह क्या था,
जिसकी स्मृति अब तक निषण्ण है स्वामी के प्राणों में?
मन के अलस लेख सपने निद्रा की चित्र-पटी पर
जल की रेखा के समान बनते-बुझते रहते हैं ।
पुरुरवा देखा, सारे प्रतिष्ठानपुर में कलकल छाया है,
लोग कहीं से एक नव्य वट-पादप ले आए हैं ।
और रोप कर उसे सामने, वहाँ बाह्य प्रांगण में
सीच रहे हैं बड़ी, प्रीति, चिंताकुल आतुरता से ।
मैं भी लिए क्षीरघट, देखा, उत्कंठित आया हूँ;
और खड़ा हूँ सींच दूध से उस नवीन बिरवे को ।
मेरी ओर, परंतु, किसी नागर की दृष्टि नहीं है,
मानो, मैं हूँ जीव नवागत अपर सौर मंडल का,
नगरवासियों की जिससे कोई पहचान नहीं हो ।
तब देखा, मैं चढ़ा हुआ मदकल, वरिष्ठ कुंजर पर
प्रतिष्ठानपुर से बाहर कानन में पहुंच गया हूँ ।
किंतु, उतर कर वहाँ देखता हूँ तो सब सूना है,
मुझे छोड़, चोरी से, मेरा गज भी निकल गया है ।
एकाकी, नि:संग भटकता हुआ विपिन निर्जन में
जा पहुँचा मैं वहाँ जहाँ पर वधूसरा बहती है,
च्यवनाश्रम के पास, पुलोमा की दृगम्बु-धारा-सी ।
उर्वशी
च्यवनाश्रम! हा! हंत! अपाले, मुझे घूँट भर जल दे ।
[अपाला घबरा कर पानी देती है।उर्वशी पानी पीती है।]
पुरुरवा देवि! आप क्यों सहम उठीं? वह, सचमुच, च्यवनाश्रम था ।
ऋषि तरु पर से अपने सूखे वसन समेट रहे थे ।
घूम रहे थे कृष्णसार मृग अभय वीथि-कुंजों में;
श्रवण कर रहे थे मयूर तट पर से कान लगा कर
मेघमन्द्र डुग-डुग-ध्वनि जलधारा में घट भरने की ।
और, पास ही, एक दिव्य बालक प्रशांत बैठा था
प्रत्यंचा माँजते वीर-कर-शोभी किसी धनुष की
हाय, कहूँ क्या, वह कुमार कितना सुभव्य लगता था!
उर्वशी
दुर्विपाक! दुर्भाग्य! अपाले! तनिक और पानी दे ।
उमड़ प्राण से, कहीं कंठ में, ज्वाला अटक गई है ।
लगता है, आज ही प्रलय अम्बर से फूट पड़ेगा
[पानी पीती है]
पुरुरवा
देवि! स्वप्न से आप अकारण भीत हुए जाती हैं ।
मैं हूँ जहाँ, वहाँ कैसे विध्वंश पहुंच सकता है?
भूल गईं, स्यन्दन मेरा नभ में अबाध उड़ता है?
मैं तो केवल ऋषि-कुमार का तेज बखान रहा था ।
उरु-दंड परिपुष्ट, मध्य कृश, पृथुल, प्रलम्ब भुजाएँ,
व्क्षस्थल उन्नत, प्रशस्त कितना सुभव्य लगता था!
ऊषा विभासित उदय शैल की, मानो, स्वर्ण-शिला हो ।
उफ री, पय:शुभ्रता उन आयत, अलक्श्म नयनों की!
प्राण विकल हो उठे दौड़ कर उसे भेंट लेने को
पर, तत्क्षण सब बिला गया, जानें, किस शून्य तिमिर में!
न तो वहाँ अब ऋषि-कुमार था, न तो कुटीर च्यवन का ।
देखा जिधर, उधर डालों, टहनियों, पुष्पवृंतों पर
देवि! आपका यही कुसुम-आनन जगमगा रहा था
हँसता हुआ, प्रहृष्ट, सत्य ही, सद्य:स्फुटित कमल-सा ।
किंतु, हाय! दुर्भाग्य! जिधर भी बढ़ा स्पर्श करने को
डूब गया वह छली पुष्प पत्तों की हरियाली में ।
चकित, भीत, विस्मित, अधीर तब मैं निरस्त माया से,
अकस्मात उड़ गया छोड-अवनीतल ऊर्ध्व गगन में,
और तैरता रहा, न जानें, कब तक खंड-जलद-सा ।
जगा, अंत को, जब विभावरी पूरी बीत चुकी थी ।
वह बालक था कौन? कौन मुझको छलने आई थी ।
दिखा उर्वशी का प्रसन्न आनन डाली-डाली में।
महामात्य
महाश्चर्य!
एक सभासद
विस्मय अपार!
दूसरा सभासद
यह स्वप्न या कि कविता है
उज्जवलता
में रमें, रूप-ध्यायी, रस-मग्न हृदय की?
और उड्डयन तो नैतिक उन्नति की ही महिमा है ।
जो हो, मैं मंगल की शुभ सूचना इसे कहता हूँ
तीसरा सभासद
शांति! ज्योतिषी विश्वमना गणना में लगे हुए हैं ।
सुनें, सिद्ध दैवज्ञ स्वप्न का फल क्या बतलाते हैं ।
विश्वमना
हाय, इसी दिन के निमित्त मैं जीवित बचा हुआ था?
महाराज! यदि कहूँ सत्य तो गिरा व्यर्थ होती है ।
मृषा कहूँ तो क्यों अब तक आदर पाता आया हूँ?
मुझ विमूढ़ को अत: देव मौन ही आज रहने दें;
क्योंकि दीखता है जो कुछ, उसका आधार नहीं है ।
पुरुरवा
किसका है आधार लुप्त? क्या है परिणाम गणित का?
यह प्रहेलिका और अधिक उत्कंठा उपजाती है ।
कहें आप संकोच छोड़ कर, जो कुछ भी कहना हो,
गणित मृषा हो भले, आपको मिथ्या कौन कहेगा?
विश्वमना
वरुण करें कल्याण! देव! तब सुनें, सत्य कहता हूँ ।
अमिट प्रवज्या-योग केन्द्र-गृह में जो पड़ा हुआ है,
वह आज ही सफल होगा, इसलिए की प्राण-दशा में
शनि ने किया प्रवेश, सूक्ष्म में मंगल पड़े हुए हैं ।
अन्य योग जो हैं, उनके अनुसार, आज सन्ध्या तक
आप प्रव्रजित हो जाएंगे अपने वीर तनय को
राज-पाट, धन-धाम सौंप, अपना किरीट पहना कर ।
पर विस्मय की बात! पुत्र वह अभी कहाँ जनमा है?
अच्छा है, पुत जाए कालिमा ही मेरे आनन पर;
लोग कहें, मर गई जीर्ण हो विद्या विश्वमना की ।
इस अनभ्र आपद् से तो अपकीर्ति कहीं सुखकर है ।
उर्वशी
आह! क्रूर अभिशाप! तुम्हारी ज्वाला बड़ी प्रबल है ।
अरी! जली, मैं जली, अपाले! और तनिक पानी दे ।
महाराज! मुझ हतभागी का कोई दोष नहीं है ।
(पानी पीती है। दाह अनुभूत होने का भाव)
पुरुरवा
किसका शाप? कहाँ की ज्वाला? कौन दोष? कल्याणी!
आप खिन्न हो निज को हतभागी क्यों कहती हैं?
कितना था आनन्द गन्धमादन के विजन विपिन में
छूट गई यदि पुरी, संग होकर हम वहीं चलेंगे ।
आप, न जानें, किस चिंता से चूर हुई जाती हैं!
कभी आपको छोड़ देह यह जीवित रह सकती है?
[प्रतीहारी का प्रवेश]
प्रतीहारी
जय हो महाराज! वन से तापसी एक आई हैं;
कहती हैं, स्वामिनी उर्वशी से उनको मिलना है!
नाम सुकन्या; एक ब्रह्मचारी भी साथ लगा है ।
पुरुरवा
सती सुकन्या! कीर्तिमयी भामिनी महर्षि च्यवन की?
सादर लाओ उन्हें; स्वप्न अब फलित हुआ लगता है ।
पुण्योदय के बिना संत कब मिलते हैं राजा को?
[सुकन्या और आयु का प्रवेश]
पुरुरवा
इलापुत्र मैं पुरु पदों में नमस्कार करता हूँ ।
देवि! तपस्या तो महर्षिसत्तम की वर्धमती है?
आश्रम-वास अविघ्न, कुशल तो है अरण्य-गुरुकुल में?
सुकन्या
जय हो, सब है कुशल ।
उर्वशी! आज अचानक ऋषि ने
कहा, “आयु को पितृ-गेह आज ही गमन करना है!
अत:, आज ही, दिन रहते-रहते, पहुंचाना होगा,
जैसे भी हो, इस कुमार को निकट पिता-माता के” ।
सो, ले आई, अकस्मात ही, इसे; सुयोग नहीं था
पूर्व-सूचना का या इसको और रोक रखने का ।
सोलह वर्ष पूर्व तुमने जो न्यास मुझे सौंपा था,
उसे आज सक्षेम सखी! तुम को मैं लौटाती हूँ ।
बेटा! करो प्रणाम, यही हैं माँ, वे देव पिता हैं ।
[आयु पहले उर्वशी को, फिर पुरुरवा को प्रणाम
करता है। पुरुरवा उसे छाती से लगा लेता है।]
पुरुरवा
महाश्चर्य! अघट घटना! अद्भुत अपूर्व लीला है!
यह सब सत्य-यथार्थ या कि फिर सपना देख रहा हूँ?
पुत्र! देवि! मैं पुत्रवान हूँ? यह अपत्य मेरा है?
जनम चुका है मेरा भी त्राता पुं नाम नरक से?
अकस्मात हो उथा उदित यह संचित पुण्य कहाँ का?
अमृत-अभ्र कैसे अनभ्र ही मुझ पर बरस पड़ा है?
पुत्र! अरे मैं पुत्रवान हूँ, घोषित करो नगर में,
जो हो जहाँ, वहीं से मेरे निकट उसे आने दो ।
द्वार खोल दो कोष-भवन का, कह दो पौर जनों से
जितना भी चाहें, सुवर्ण आकर ले जा सकते हैं
ऐल वंश के महामंच पर नया सूर्य निकला है;
पुत्र-प्राप्ति का लग्न, आज अनुपम, अबाध उत्सव है ।
पुत्र! अरे कोई संभाल रखो मेरी संज्ञा को,
न तो हर्ष से अभी विकल-विक्षिप्त हुआ जाता हूँ ।
पुत्र! अरे, ओ अमृत-स्पर्श! आनन्द-कन्द नयनों के!
प्राणों के आलोक! हाय! तुम अब तक छिपे कहाँ थे?
ऐल वंश का दीप, देवि! यह कब उत्पन्न हुआ था?
और आपने छिपा रखा इसको क्यों निष्ठुरता से?
हाय! भोगने से मेरा कितना सुख छूट गया है!
उर्वशी
अब से सोलह वर्ष पूर्व, पुत्रेष्टि-यज्ञ पावन में
देव! आप यज्ञिय विशिष्ट जीवन जब बिता रहे थे,
च्यवनाश्रम की तपोभूमि में तभी आयु जनमा था
मुझमें स्थापित महाराज के तेजपुंज पावक से
किंतु, छिपा क्यों रखा पुत्र का मुख पुत्रेच्छु पिता से,
आह! समय अब नहीं देव! वह सब रहस्य कहने का ।
लगता है, कोई प्राणों को बेध लौह अंकुश से,
बरबस मुझे खींच इस जग से दूर लिए जाता है ।
पुरुरवा
अच्छा, जो है गुप्त, गुप्त ही उसे अभी रहने दें ।
आतुरता क्या हो रहस्य के उद्घाटित करने की,
जब रहस्य वपुमान सामने ही साकार खड़ा हो?
सभासदो! कल रात स्वप्न में इसी वीर-पुंगव को
प्रत्यंचा माँजते हुए मैने वन में देखा था ।
और बढ़ा ज्यों ही उदग्र मैं इसे अंक भरने को,
यही दुष्ट छल मुझे कहीं कुंजों मे समा गया था ।
किंतु, लाल! अब आलिंगन से कैसे भाग सकोगे?
यह प्रसुप्त का नहीं, जगे का सुदृढ़ बाहु-बन्धन है?
आयु
आयु तक रहा वियुक्त अंक से, यही क्लेश क्या कम है?
तात! आपकी छन्ह छोड़ मैं किस निमित्त भागूँगा?
जब से पाया जन्म, उपोषण रहा धर्म प्राणों का;
हृदय भूख से विकल, पिता! मैं बहुत-बहुत प्यासा हूँ,
यद्यपि सारी आयु तापसी माँ का प्यार पिया है।
पुरुरवा
रुला दिया तुमने तो मेरे चन्द्र! व्यथा यह कह कर ।
सुना देवि! यह लाल हमारा कितना तृषित रहा है
माँ के उर का क्षीर, पिता का स्नेह नहीं पाने से?
[उर्वशी अदृश्य हो चुकी है।]
महामात्य
महाराज! आश्चर्य! उर्वशी देवि यहाँ नहीं हैं?
कहाँ गई? थीं खड़ी अभी तो यहीं निकट स्वामी के?
पुरुरवा
क्यों, जाएँगी कहाँ विमुख हो इस आनन्द सघन से?
किंतु, अभी वे श्रांत-चित्त, कुछ थकी-थकी लगती थीं;
जाकर देखो, स्यात् प्रमद-उपवन में चली गई हों
शीतल, स्वच्छ, प्रसन्न वायु में तनिक घूम आने को ।
सुकन्या
वृथा यत्न; इस राज-भवन में अब उर्वशी नहीं है ।
चली गई वह वहाँ, जहाँ से भूतल पर आई थी
खिंची आपके महाप्रेम के आकुल आकर्षण में ।
भू वंचित हो गई आज उस चिर-नवीन सुषमा से ।
महाराज! उर्वशी मानवी नहीं, देव-बाला थी;
चक्षुराग जब हुआ आपसे , उस विलोल-हृदया ने,
किसी भाँति, कर दिया एक दिन कुपित महर्षि भरत को ।
और भरत ने ही उसको यह दारुण शाप दिया था,
“भूल गई निज कर्म, लीन जिसके स्वरूप-चिंतन में,
जा, तू बन प्रेयसी भूमि पर उसी मर्त्य मानव की ।
किंतु, न होंगे तुझे सुलभ सब सुख गृहस्थ नारी के,
पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाएगी;
सो भी तब तक ही जिस क्षण तक नहीं देख पाएगा
अहंकारिणी! तेरा पति तुझसे उत्पन्न तनय को।”
वही शाप फल गया, उर्वशी चली गई सुरपुर को ।
महाराज! मैं तो इसके हित उद्यत ही आई थी!
क्योंकि ज्ञात था मुझे, आयु को जभी आप देखेंगे,
गरज उठेगा शाप, उर्वशी भू पर नहीं रहेगी ।
किंतु, आयु को कब तक हम वंचित कर रख सकते थे
जाति, गोत्र, सौभाग्य, वंश से, परिजन और पिता से?
हुआ वही, जो कुछ होना था, पश्चाताप वृथा है ।
अब दीजिए आयु को वह, जो कुछ वह माँग रहा है ।
महाराज! सत्य ही आयु का हृदय बहुत प्यासा है ।
[पुरुरवा आयु से अलग हो जाता है]
पुरुरवा
चली गई? सब शून्य हो गया? मैं वियुक्त, विरही हूँ?
देवों को मेरे निमित्त, बस, इतनी ही ममता थी!
लाओ मेरा धनुष, सजाओ गगन-जयी स्यन्दन को,
सखा नहीं, बन शत्रु स्वर्ग-पुर मुझे आज जाना है ।
और दिखाना है, दाहकता किसकी अधिक प्रबल है,
भरत-शाप की या पुरुरवा के प्रचंड बाणों की ।
कहाँ छिपा रखेंगे सुर मेरी प्रेयसी प्रिया को?
रत्नसानु की कनक-कन्दरा में? तो उस पर्वत को
स्वर्ण-धूलि बन वसुन्धरा पर आज बरस जाना है ।
छिन्न-भिन्न होकर मनुष्य के प्रलय-दीप्त बाणों से ।
दिव के वियल्लोक में छाए विपुल स्वर्ण-मेघों में?
तो मेघों के अंतराल होकर अरुद्ध शम्पा-सा
दौड़ेगा मेरा विमान कम्पित कर प्राण सुरों के;
और उलट कर एक-एक मायामय मेघ-पटल को
खोजूँगा, उर्वशी व्योम के भीतर कहाँ छिपी है ।
लाओ मेरा धनुष, यहीं से बाण साध अम्बर में
अभी देवताओं के वन में आग लगा देता हूँ ।
फेंक प्रखर, प्रज्वलित, वह्निमय विशिख दृप्त मघवा को
देता हूँ नैवेद्य मनुजता के विरुद्ध संगर का ।
और सिन्धु में कहीं उर्वशी को फिर छिपा दिया हो,
तो साजो विकराल सैन्य, हम आज महासागर को
मथ कर देंगे हिला, सिन्धु फिर पराभूत उगलेगा
वे सारे मणि-रत्न, बने होंगे जो भी उस दिन से,
जब देवों-असुरों ने इसको पहले-पहल मथा था ।
और उसी मंथन क्रम में बैठी तरंग-आसन पर
एक बार फिर पुन: उर्वशी निकलेगी सागर से
बिखराती मोहिनी उषा की प्रभा समस्त भुवन में,
जैसे वह पहले समुद्र के भीतर से निकली थी!
भूल गए देवता, झेल शत्रुता अमित असुरों की
कितनी बार उन्हें मैने रण में जय दिलवाई है ।
पर, इस बार ध्वंस बनकर जब मैं उन पर टूटूँगा,
आशा है,आप्रलय दाह विशिखों का स्मरण रहेगा;
और मान लेंगे यह भी, उर्वशी कहीं जनमी हो,
देवों की अप्सरा नहीं, वह मेरी प्राणप्रिया है ।
उठो, बजाओ पटह युद्ध के, कह दो पौर जनों से,
उनका प्रिय सम्राट स्वर्ग से वैर ठान निकला है;
साथ चलें, जिसको किंचित भी प्राण नहीं प्यारे हों ।
महामात्य्
महाराज हों शांत; कोप यह अनुचित नहीं, उचित है ।
तारा को लेकर पहले भी भीषण समर हुआ था
दो पक्षों मे बँटे, परस्पर कुपित सुरों-असुरों में ।
और सुरों के, उस रण में भी छक्के छूट गए थे ।
वह सब होगा पुन:, यही यदि रहा इष्ट स्वामी का ।
पर, यद्यपि, यह समर खड़ा होगा मानवों-सुरों में,
किंतु दनुज क्या इस अपूर्व अवसर से अलग रहेंगे?
मिल जाएँगे वे अवश्य आकर मनुष्य सेना में ।
सुरता के ध्वंसन से बढ़्कर उन्हें और क्या प्रिय है
और टिकेंगे किस बूते पर चरण देवताओं के
वहाँ, जहाँ नर-असुर साथ मिलकर उनसे जूझ रहे हों?
इस संगर में महाराज! जय तो अपनी निश्चित है;
मात्र सोचना है, देवों से वैर ठान लेने पर
पड़ न जाएँ हम कहीं दानवों की अपूत संगति में ।
नर का भूषण विजय नहीं, केवल चरित्र उज्जवल है
कहती हैं नीतियाँ, जिसे भी विजयी समझ रहे हो,
नापो उसे प्रथम उन सारे प्रकट, गुप्त यत्नों से,
विजय-प्राप्ति-क्रम में उसने जिनका उपयोग किया है ।
डाल न दे शत्रुता सुरों से हमें दनुज-बाँहों में,
महाराज! मैं, इसीलिए, देवों से घबराता हूँ ।
पुरुरवा
कायरता की बात ! तुम्हारे मन को सता रही है
भीति इन्द्र के निथुर वज्र की, देवों की माया की;
किंतु, उसे तुम छिपा रहे हो सचिव! ओढ़ ऊपर से
मिथ्या वसन दनुज-संगति-कल्पना-जन्य दूषण का ।
जब मनुष्य चीखता व्योम का हृदय दरक जाता है
सहम-सहम उठते सुरेन्द्र उसके तप की ज्वाला से ।
और कहीं हो क्रुद्ध मनुज कर दे आह्वान प्रलय का,
स्वर्ग, सत्य ही टूट गगन से भू पर आ जाएगा ।
क्यों लेंगे साहाय्य दनुज का? हम मनुष्य क्या कम हैं?
बजे युद्ध का पटह, सिद्ध हो द्रुत योजना समर की
यह अपमान असह्य, इसे सहने से श्रेष्ठ मरण है ।
[नेपथ्य से आवाज आती है]
“पीना होगा गरल, वेदना यह सहनी ही होगी ।
सावधान! देवों से लड़ने में कल्याण नहीं है ।
देव कौन हैं? शुद्ध, दग्धमल, श्रेष्ठ रूप मानव के;
तो अपने ही श्रेष्ठ रूप से मानव युद्ध करेगा
या उससे जो रूप अभी दानवी, दुष्ट, मलिन है?”
पुरुरवा
यह किसका स्वर? कौन यवनिकाओं में छिपा हुआ है?
जो भी होती घटित आज, अचरज की ही घटना है ।
बड़ी अनोखी बात! कौन हो तुम जो बोल रहे हो
इतने सूक्ष्म विचार? छिपे हो कहाँ, भूमि या नभ में/
[नेपथ्य से आवाज]
मैं प्रारब्ध चन्द्रकुल का, संचित प्रताप तेरा हूँ
बोल रहा हूँ तेरे ही प्राणों के अगम,अतल से ।
अनुचित नहीं गर्व क्षणभंगुर वर्तमान की जय का
पर, अपने में डूब कभी यह भी तूने सोचा है,
तेरे वर्तमान मन पर जिनका भविष्य निर्भर है,
अनुत्पन्न उन शत-सहस्र मनुजों के मुखमंडल पर
कौन बिम्ब, क्या प्रभा, कौन छाया पड़ती जाती है?
जैसे तूने प्रणय-तूलिका और लौह-विशिखों से
ओजस्वी आख्यान आत्मजीवन का आज लिखा है,
वैसे ही कल चन्द्र-वंश वालों के विपुल-हृदय में
लौह और वासना समंवित होकर नृत्य करेंगे
अतुल पराक्रम के प्रकाश में भी यह नहीं छिपेगा
ताराहर विधु के विलास से ये मनुष्य जनमें हैं
चिंतन कर यह जान कि तेरे क्षण-क्षण की चिंता से
दूर-दूर तक के भविष्य का मनुज जन्म लेता है
उठा चरण यह सोच कि तेरे पद के निक्षेपों की
आगामी युग के कानों में ध्वनियाँ पहुंच रही हैं ।
और प्रेम! वह बना नहीं क्यों अश्रुधार करुणा की,
आराधन उन दिव्य देवता का, जो छिपे हुए हैं
रमणी के लावण्य, रमा-मुख के प्रकाश मंडल में?
बना नहीं क्यों वह अखंड आलोक-पुंज जीवन का,
जिसे लिए तू और व्योम में ऊपर उठ सकता था?
अरुण अधर, रक्तिम कपोल, कुसुमाघव घूर्ण दृगों में;
आमंत्रण कितना असह्य माया-मनोज्ञ प्रतिमा का!
ग्रीवा से आकटि समंत उद्वेलित शिखा मदन की,
आलोड़ित उज्जवल असीमता-सी सम्पूर्ण त्वचा में;
वक्ष प्रतीप कमल, जिन पर दो मूँगे जड़े हुए हैं;
त्रिवली किसी स्वर्ण-सरसी में उठती हुई लहर-सी
किंतु, नहीं श्लथ हुईं भुजाएँ किन विक्रमी नरों की
आलिंगन में इस मरीचिका को समेट रखने में?
पृथुल, निमंत्रण-मधुर, स्निग्ध, परिणत, विविक्त जघनों पर
आकर हुआ न ध्वस्त कौन हतविक्रम असृक-स्रवण से?
जिसने भी की प्रीति, वही अपने विदीर्ण प्राणों में
लिए चल रहा व्रण, शोणितमय तिलक प्रेम के कर का;
और चोट जिसकी जितनी ही अधिक, घाव गहरा है,
वह उतना ही कम अधीर है व्यथा-मुक्ति पाने को ।
नारी के भीतर असीम जो एक और नारी है,
सोचा है उसकी रक्षा पुरुषों में कौन करेगा?
वह, जो केवल पुरुष नहीं, है किंचित अधिक पुरुष से;
उर में जिसके सलिल-धार, निश्चल महीद्र प्राणों में,
कलियों की उँगलियाँ, मुट्ठियाँ हैं जिसकी पत्थर की ।
कह सकता है पुरू! कि तू पुरुषाधिक यही पुरुष है?
तो फिर भीतर देख, शिलोच्चय शिखर-शैल मानस का
अचल खड़ा है या प्रवाल-ताडन से डोल रहा है?
यह भी देख, भुजा कुसुमों का दाम कि वज्र-शिला है?
हाथों में फूल ही फूल हैं या कुछ चिंगारी भी?
विपद्व्याधिनी भी जीवन में तुझको कहीं मिली थी?
पूछा जब तूने भविष्य, उसने क्या बतलाया था?
त्रिया! हाय छलना मनोज्ञ वह! पुरुष मग्न हँसता है,
जब चाहिये उसे रो उठना कंठ फाड़, चिल्ला कर ।
पूछ रहा क्या भाग्य ज्योतिषी से, अंकविद, गणक से?
हृदय चीर कर देख प्राण की कुंजी वही पड़ी है ।
अंतर्मन को जगा पूछ, वह जो संकेत करेगा,
तुझे मिलेगी मन:शांति उपवेशित उसी दिशा में ।
बिना चुकाए मूल्य जगत में किसने सुख भोगा है?
तुझ पर भी है पुरू! शेष जो ऋण अपार जीवन का
भाग नहीं सकता तू उसको किसी प्रकार पचाकर ।
नहीं देखता, कौन तेरे नयन समक्ष खड़ा है?
पुरुरवा! यह और नहीं कोई, तेरा जीवन है ।
जो कुछ तूने किया प्राप्त अब तक इसके हाथों से,
देना होगा मूल्य आज गिन-गिन उन सभी क्षणों का ।
पर, कैसे? जा स्वर्ग उर्वशी को फिर ले आएगा?
अथवा अपने महाप्रेम के बलशाली पंखों पर
चढ़ असीम उड्डयन भरेगा मन के महागगन में,
जहाँ त्रिया कामिनी नहीं, छाया है परम विभा की,
जहाँ प्रेम कामना नहीं, प्रार्थना निदिध्यासन है?
खोज रहा अवलम्ब? किंतु, बाहर इस ज्वलित द्विधा का
कोई उत्तर नहीं। पुन: मैं वही बात कहता हूँ,
हृदय चीर कर देख, वहीं पर कुंजी कहीं पड़ी है।
पुरुरवा
देख क्रिया। मंत्रियो! एक क्षण का भी समय नहीं है;
पुरोहित करें स्वस्ति-वाचन शुभ राज-तिलक का ।
विश्वमना का फलादेश चरितार्थ हुआ जाता है ।
मृषा बन्ध विक्रम-विलास का, मृषा मोह-माया का;
इन दैहिक सिद्धियों, कीर्तियों के कंचनावरण में,
भीतर ही भीतर विषण्ण मैं कितना रिक्त रहा हूँ!
अंतर्तम के रूदन, अभावों की अव्यक्त गिरा को
कितनी बार श्रवण करके भी मैने नहीं सुना है!
पर, अब और नहीं, अवहेला अधिक नहीं इस स्वर की,
ठहरो आवाहन अनंत के, मूक निनद प्राणों के!
पंख खोल कर अभी तुम्हारे साथ हुआ जाता हूँ
दिन-भर लुटा प्रकाश, विभावसु भी प्रदोष आने पर
सारी रश्मि समेट शैल के पार उतर जाते हैं
बैठ किसी एकांत, प्रांत, निर्जन कन्दरा, दरी में
अपना अंतर्गगन रात में उद्भासित करने को
तो मैं ही क्यों रहूँ सदा ततता मध्याह्न गगन में?
नए सूर्य को क्षितिज छोड़ ऊपर नभ में आने दो ।
पहुँच गया मेरा मुहुर्त, किरणें समेट अम्बर से
चक्रवाल के पार विजन में कहीं उतर जाने का ।
यह लो अपने घूर्णिमान सिर पर से इसे हटाकर
ऐल-वंश का मुकुट आयु के मस्तक पर धरता हूँ ।
लो, पूरा हो गया राज्य-अभिषेक! कृपा पूषण की ।
ऐल-वंश-अवतंस नए सम्राट आयु की जय हो
महाराज! मैं भार-मुक्त अब कानन को जाता हूँ ।
भाग्य-दोष सध सका नहीं मुझसे कर्त्तव्य पिता का;
अब तो केवल प्रजा-धर्म् है, सो, उसको पालूँगा,
जहाँ रहूँगा, वहीं महाभृत का अभ्युदय मनाकर ।
यती नि:स्व क्या दे सकता है सिवा एक आशिष के?
सभासदो! कालज्ञ आप, सब के सब कर्म-निपुण हैं,
क्या करना पटु को निदेश समयोचित कर्त्तव्यों का?
प्रजा-जनों से मात्र हमारा आशीर्वाद कहेंगे ।
जय हो, चन्द्र-वंश अब तक जितना सुरम्य, सुखकर था,
उसी भाँति वह सुखद रहे आगे भी प्रजा-जनों को ।
[एक ओर से पुरुरवा का निष्क्रमण: दूसरी ओर से
महारानी औशीनरी का प्रवेश]
औशीनरी
चले गए?
सभी सभासद
जय हो अनुकम्पामयी राजमाता की ।
औशीनरी
हाँ, मैं अभी राज महिषी थी, चाहे जहाँ कहीं भी
इस प्रकाश से दूर भाग्य ने मुझे फेंक रखा था ।
किंतु, नियति की बात! सत्य ही, अभी राजमाता हूँ ।
आ बेटा! लूँ जुड़ा प्राण छाती से तुझे लगाकर ।
[आयु को हृदय से लगाती है]
कितना भव्य स्वरूप! नयन, नासिका, ललाट, चिबुक में
महाराज की आकृतियों का पूरा बिम्ब पड़ा है ।
हाय, पालती कितने सुख, कितनी उमंग, आशा से,
मिला मुझे होता यदि मेरा तनय कहीं बचपन में ।
पर, तब भी क्या बात? मनस्वी जिन महान पुरुषों को
नई कीर्ति की ध्वजा गाड़नी है उत्तुंग शिखर पर,
बहुधा उन्हें भाग्य गढ़ता है तपा-तपा पावक में,
पाषाणों पर सुला, सिंह-जननी का क्षीर पिला कर
सो तू पला गोद में जिनकी सीमंतिनी-शिखा वे,
और नहीं कोई जाया हैं तपोनिधान च्यवन की;
तप:सिंह की प्रिया, सत्य ही, केहरिणी सतियो में
पुत्र! अकारण नहीं भाग्य ने तुझे वहाँ भेजा था ।
हाय, हमारा लाल चकित कितना निस्तब्ध खड़ा है!
और कौन है, जो विस्मित, निस्तब्ध न रह जाएगा
इस अकांड राज्याभिषेक, उस वट के विस्थापन से
जिसकी छाया हेतु दूर से वह चल कर आया हो?
कितना विषम शोक! पहले तो जनमा वन-कानन में;
जब महार्घ थी, मिली नहीं तब शीतल गोद पिता की ।
और स्वयं आया समीप, तब सहसा चले गए वे
राजपाट, सर्वस्व सौंप, केवल वात्सल्य चुराकर ।
नीरवता रवपूर्न, मौन तेरा, सब भाँति, मुखर है;
बेटा! तेरी मनोव्यथा यह किस पर प्रकट नहीं है?
पर, अब कौन विकल्प? सामने शेष एक ही पथ है
मस्तकस्थ इस राजमुकुट का भार वहन करने का ।
उदित हुआ सौभाग्य आयु! तेरा अपार संकट में
किंतु, छोड़ कर तुझे, विपद में हमें कौन तारेगा?
मलिन रहा यदि तू, किसके मुख पर मुस्कान खिलेगी?
तू उबरा यदि नहीं, महाप्लावन से कौन बचेगा?
पिता गए वन, किंतु, अरे, माता तो यहीं खड़ी है
बेटा! अब भी तो अनाथ नरनाथ नहीं ऐलों का ।
तुझे प्यास वात्सल्य-सुधा की, मैं भी उसी अमृत से
बिना लुटाए कोष हाय! आजीवन भरी रही हूँ ।
फला न कोई शस्य, प्रकृति से जो भी अमृत मिला था,
लहर मारता रहा टहनियो में, सूनी डालों में ।
किंतु, प्राप्त कर तुझे आज, बस, यही भान होता है,
शस्य-भार से मेरी सब डालियाँ झुकी जाती हों ।
हाय पुत्र! मैं भी जीवन भर बहुत-बहुत प्यासी थी
शीतल जल का पात्र अधर से पहले पहल लगा है ।
तप्त बना मत इसे वीरमणिअ! द्विधा, ग्लानि,चिंता से ।
नहीं देखता, मैं विपन्नता में किस भाँति खड़ी हूँ,
गँवा शतऋतु-सम प्रतापशाली, महान भर्त्ता को,
अंतर से उच्छलित वेदना का विस्फोट दबाकर?
और हाय, तब भी, मैं केवल त्रिया, भीरु नारी हूँ;
रुदन छोड़ विधि ने सिरजा क्या और भाग्य नारी का?
पर, किशोर होने पर भी बेटा! तू वीर नृपति है ।
नृपति नहीं टूटते कभी भी निजी विपत्ति-व्यथा से;
अपनी पीड़ा भूल यंत्रणा औरों की हरते हैं ।
हँसते हैं, जब किरण हास्य की हो सबके अधरों पर,
रोते हैं, जब प्रजा-जनों के नयन सिक्त होते हैं
अपनी पीड़ा कहाँ,उसे अपना आनन्द कहाँ है,
जिस पर चढ़ा किरीट, भार दुर्वह् समाज-शासन का?
किंतु, हाय, हो गया यहाँ यह सब क्या एक निमिष में?
महामात्य
घटित हुआ सब, इस प्रकार्, मानो, अदृश्य के कर में
नाच रही हो पराधीन यह सभा दारु-पुतली-सी
सब की बुद्धि समेट, सभी को अपना पाठ सिखा कर
यह नाटक दुखांत भाग्य ने स्वयं यहाँ खेला है ।
कौन जानता था, अनभ्र ही अशनि आज टूटेगी?
मिला कहाँ आभास देवि! हमको आसन्न विपद का?
कुछ तो भाग्य-अधीन और कुछ महाराज के भय से
हम स्तम्भित रह गए; गिरा खोलें-खोलें, तब तक तो
राज-मुकुट नृप से कुमार के सिर पर पहुंच चुका था ।
सब कुछ हुआ, मरुत जैसे अम्बर में दौड़ रहे हों,
जैसे कोई आग शुष्क कानन को जला रही हो;
सब कुछ हुआ, देवि! जैसे हम मनुज नहीं, पत्थर हों,
जैसे स्वयं अभाग्य हमें आगे को हाँक रहा हो
चले गए सम्राट छोड़ हमको अपार विस्मय में,
कह पाए हम कहाँ देवि! जो कुछ हमको कहना था?
औशीनरी
कौन सका कह व्यथा? नहीं देखा, समग्र जीवन में
जो कुछ हुआ देख उसको मैं कितनी मौन रही हूँ
कोलाहल के बीच मूकता की अकम्प रेखा-सी?
वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु, मौन कंचन है ।
पर, क्या मिला, अंत में जाकर, मुझको इस कंचन से?
उतरा सब इतिहास, जहाँ निर्घोष, निनद, कलकल था;
चले गए उस मूक नीड़ की छाया सभी बचाकर
घटनाओं से दूर जहाँ मैं अचल, शांत बैठी थी ।
महाराज कितने उदार, कितने मृदु, भाव-प्रवण थे!
मुझ अभागिनी को उनने कितना सम्मान दिया था!
पर, चलने के समय कृपा अपनी क्यों भूल गए वे?
रहा नहीं क्यों ध्यान, दानवाक्र्ति इस बड़े भवन में
कहीं उपेक्षित शांत एक वह भी धूमिल कोना है,
कभी भूल कर भी जातीं घटनाएं नहीं जहाँ पर,
न तो जहाँ इतिहासों की पदचाप सुनी जाती है;
जहाँ प्रनय नीरव, अकम्प, कामना, स्निग्ध, शीतल है,
अभिलाषाएँ नहीं व्यग्र अपनी ही ज्वालाओं से;
जहाँ नहीं चरणों के नीचे अरुण सेज मूँगों की,
न तो तरंगों में ऊपर नागिनियाँ लहराती हैं;
जहाँ नहीं बसती कृशानु सुशमा कपोल, अधरों की,
न तो छिटकती हैं रह-रह कर चिंगारियाँ त्वचा से;
स्थापित जहाँ शुभेच्छु, समर्पित हृदय विनम्र त्रिया का,
उद्वेगों से अधिक स्वाद है जहाँ शांति, संयम में;
एक पात्र में जहाँ क्शीर, मधुरस दोनों संचित हैं,
छिपे हुए हैं जहाँ सूर्य-शशधर एक ही हृदय में;
जहाँ भामिनी नहीं मात्र प्रेयसी विमुग्ध पुरुष की,
अमृत-दायिनी, बल-विधायिनी माता भी होती है ।
भूल गए क्यों दयित, हाय, उस नीरव, निभृत निलय में
बैठी है कोई अखंड व्रतमयी समाराधन में,
अश्रुमुखी माँगती एक ही भीख त्रिलोक-भरन से,
कण्-भर भी मत अकल्याण् हो प्रभो! कभी स्वामी का ।
जो भी हो आपदा, मुझे दो,। मैं प्रसन्न सह लूँगी,
देव! किंतु मत चुभे तुच्छतम कंटक भी प्रियतम को
किंतु, हाय, हो गई मृषा साधना सकल जीवन की;
मैं बैठी ही रही ध्यान में जोड़े हुए करों को;
चले गए देवता बिना ही कहे बात इतनी भी,
हतभागी! उठ, जाग, देख, मैं मन्दिर से जाता हूँ ।
याग-यज्ञ, व्रत-अनुष्ठान में, किसी धर्म-साधन में
मुझे बुलाए बिना नहीं प्रियतम प्रवृत होते थे ।
तो यह अंतिम व्रत कठोर कैसे सन्यास सधेगा
किए शून्य वामांक, त्याग मुझ सन्यासिनी प्रिया को?
और त्यागना ही था तो जाते-जाते प्रियतम ने
ले लेने दी नहीं धूलि क्यों अंतिम बार पदों की?
मुझे बुलाए बिना अचानक कैसे चले गए वे?
अकस्मात ही मैं कैसे मर गई कांत के मन में?
शुभे! गाँस यह सदा हृदय-तल में सालती रहेगी,
मेरा ही सर्वस्व हाय, मुझसे यों बिछुड गया है,
मानो, उस पर मुझ अभागिनी का अधिकार नहीं हो।
सुकन्या
देवि! यही है नियम;पाश जो क्षणिक, क्षाम, दुर्बल हैं,
वैराग्योन्मुख पुरुष नहीं उन बन्धों से डरता है ।
जन्म-जन्म की जहाँ, किंतु, श्रृखला अभंग पड़ी है,
यती निकल भागता उधर से आंखें सदा चुराकर ।
परामर्श क्यों करे मुक्तिकामी अपने बन्धन से?
गृहिणी की यदि सुने, गेह से कौन निकल सकता है?
विस्मय की क्या बात? यहाँ जो हुआ, वही होना था ।
अचरज नहीं, आपसे मिलकर नृप यदि नहीं गए हैं ।
औशीनरी
पतिव्रते! पर, हाय,चोट यह कितनी तिग्म, विषम है/
कैसी अवमानना1 प्रतारण कितना तीव्र गरल-सा
मैं अवध्य, निर्दोष, विचारा यह क्यों नहीं दयित ने?
छला किसी ने और वज्र आ गिरा किसी के सिर पर
गँवा दिया सर्वस्व हाय, मैने छिप कर छाया में,
अस्वीकृत कर खुली धूप में आंख खोल चलने से ।
देवि! प्रेम के जिस तट पर अप्सरा स्नान करती है,
गई नहीं क्यों मैं तरंग-आकुल उस रसित पुलिन पर?
पछताती हूँ हाय, रक्त आवरण फाड़ व्रीड़ा का
व्यंजित होने दिया नहीं क्यों मैने उस प्रमदा को
जो केवल अप्सरा नहीं, मुझमें भी छिपी हुई थी?
बसी नहीं क्यों कुसुम-दान बन उन विशाल बाँहों में?
लगी फिरी क्यों नहीं पुष्प-सज्र बन उदग्र ग्रीवा से?
बेध रहे थे उठा शरासन जब से वक्ष तिमिर का,
बनी न क्यों शिंजिनी, हाय, तब मैं उस महाधनुष की?
गई नहीं क्यों संग-संग मैं धरणी और गगन में
जहाँ-जहाँ प्रिय को महान घटनाएं बुला रही थीं?
अंकित थे कर रहे प्राणपति जब आख्यान विजय का
पर्ण-पर्ण पर, लहर-लहर् में, उन्नत शिखर-शिखर पर,
समा गई क्यों नहीं, हाय, तब मैं जीवंत प्रभा-सी
बाणों के फलकों, कृशानु की लोहित रेखाओं में?
जीत गई वे जो लहरों पर मचल-मचल चलती थीं,
उड़ सकती थीं खुली धूप में, मेघों भरे गगन में
हारी मैं इसलिए कि मेरे व्रीड़ा-विकल दृगों में
खुली धूप की प्रभा,किरण कोलाहल की गड़ती थी ।
देखा ही कुछ नहीं, कहाँ, क्या महिमा बरस रही है
अंतर की छाया-निवास से बाहर कभी निकल कर
हाय, भाग्य ने मुझे खींच इस त्रपा-त्रस्त छाया से
फेंक दिया क्यों नहीं धूप में, उस उन्मुक्त भुवन में ।
जहाँ तरंगाकुल समुद्र जीवन का लहराता है
और पुरुष हो रणारूढ, विशिखों के निक्षेपन से-
पूर्व, पास में खड़ी प्रिया का मुख निहार लेता है?
हाय, सती मैं ही कदर्य, दोषी, अनुदार, कृपण हूँ,
केवल शुभकामना, मंगलैषा से क्या होता है?
मैं ही दे न पाई भावमय वह आहार पुरुष को
जिसकी उन्हें अपार क्षुधा, उतनी आवश्यकता थी ।
मुझे भ्रांति थी, जो कुछ था मेरा, सब चढ़ा चुकी हूँ;
शेष नहीं अब कोई भी पूजा-प्रसून डाली में;
किंतु, हाय, प्रियतम को जिसकी सबसे अधिक तृषा थी,
अब लगता है चूक गई मैं वही सुरभि देने से ।
रही समेटे अलंकार क्यों लज्जामयी विधु-सी?
बिखर पड़ी क्यों नहीं कुट्टमित, चकित, ललित,लीला में?
बरस गई क्यों नहीं घेर सारा अस्तित्व दयित का
मैं प्रसन्न,उद्दाम, तरंगित, मदिर मेघ-माला-सी?
हार गई मैं हाय! अनुत्तम, अपर ऋद्धि जीवन की
प्राणों के प्रार्थना-भवन में बैठी ध्यान लगाकर ।
सुकन्या
देवि! आपकी व्यथा, सत्य ही, अति दुरंत, दुस्सह है;
आजीवन यह गाँस हृदय से, सचमुच नहीं कढ़ेगी ।
पर, इस ग्लानि,प्रदाह, आत्म-पीड़न से अब क्या होगा?
उन्मूलित वाटिका नहीं फिर से बसने वाली है ।
उसे देख कर जिएँ, नया पादप जो आन मिला है ।
जितना भी सिर धुनें शोक से प्रियतम की विच्युति पर,
किंतु, सुचरिते! यह अचिंत्य विस्मय की बात नहीं है ।
पुरुष नहीं विक्रांत, भीम, दुर्जय, कराल होता है,
जहाँ सामने तथ्य खड़े हों, अरि हों, चट्टानें हों ।
पर, जब कभी युद्ध ठन जाता इसी अजेय पुरुष का
अपने ही मन की तरंग, अपनी ही किसी तृषा से
उससे बढ़कर और कौन कायर जग में होता है?
कर लेता है आत्म-घात, क्या कथा यतीत्व-ग्रहण की?
पर के फेंके हुए पाश से पुरुष नहीं डरता है,
वह, अवश्य ही, काट फेंकता उसे बाहु के बल से ।
पर, फँस जाता जभी वीर अपनी निर्मित उलझन में,
निकल भागने की उसको तब राह नहीं मिलती है ।
इसीलिए दायित्व गहन,दुस्तर गृहस्थ नारी का ।
क्षण-क्षण सजग, अनिन्द्र-दृष्टि देखना उसे होता है,
अभी कहाँ है व्यथा, समर में लौटे हुए पुरुष को
कहाँ लगी है प्यास, पाँव में काँटे कहाँ चुभे हैं?
बुरा किया यदि शुभे! आपने देखा नहीं नृपति के
कहाँ घाव थे, कहाँ जलन थी, कहाँ मर्म-पीड़ा थी?
यह भी नियम विचित्र प्रकृति का, जो समर्थ, उद्भट है,
दौड़ रहा ऊपर पयोधि के खुले हुए प्रांगण में;
और त्रिया जो अबल, मात्र आंसू, केवल करुणा है,
वही बैठ सम्पूर्ण सृष्टि के महा मूल निस्तल में
छिगुनी पर धारे समुद्र को ऊंचा किए हुए है ।
इसीलिए इतिहास, तुच्छ अनुचर प्रकाश, हलचल का,
किसी त्रिया की कथा नहीं तब तक अंकित करता है,
छाँह छोड़ जब तक आकर वह वरवर्णिनी प्रभा में
बैठ नहीं जाती नरत्व ले नर के सिंहासन पर
या जब तक मोहिनी फेंक मदनायित नयन-शरों की
किसी पुरुष को ले जग में विक्षोभ नहीं भरती है ।
देवि! ग्लानि क्या। हम इतिहासों में यदि प्रथित नहीं हैं
अपनी सहज भूमि नारी की धूप नहीं, छाया है
इतिहासों की सकल दृष्टि केन्द्रित, बस एक क्रिया पर ।
किंतु, नारियाँ क्रिया नहीं, प्रेरणा, पीति, करुणा हैं;
उद्गम-स्थली अदृश्य ,जहाँ से सभी कर्म उठते हैं ।
लिखता है इतिहास कथा उस जनाकीर्ण जीवन की;
जहाँ सूर्य का प्रखर ताप है, भीषण कोलाहल है
पर, फैला है जहाँ चान्द्र साम्राज्य मूक नारी का;
वह प्रदेश एकांत, बोलता केवल संकेतों में ।
अंवेषी इतिहास शूरता का, संघर्ष-सुयश का;
किंतु, हाय, शूरता नारियों की नीरव होती है;
वह सशब्द आघात नहीं, ममता है, कष्ट-सहन है ।
सदा दौड़ता ही रहता इतिहास व्यग्र इस भय से,
छूट न जाए कहीं संग भागते हुए अवसर का;
किंतु, अचंचल त्रिया बैठ अपने गम्भीर प्राणों में
अनुद्विग्न, अनधीर काल का पथ देखा करती है ।
पर, तब भी हम छिन्न नहीं इतिहासों की धारा से
कौन नहीं जानता पुरुष जब थकता कभी समर में,
किस मुख का कर ध्यान, याद कर किसके स्निग्ध-दृगों को
क्लांति छोड़ वह पुन: नए पुलकों से भर जाता है?
और कौन प्रति प्रात हाँक नर को बाहर करती है
नई उर्मि, नूतन उमंग-आशा से उसे सजा कर
लड़ने को जा वहाँ, जहाँ जीवन-रण छिड़ा हुआ है,
करने को निज अंशदान इतिहासों के प्रणयन में?
और सांझ के समय पुरुष जब आता लौट समर से,
दिन भर का इतिहास कौन उसके मुख से सुनती है
कभी मन्द स्मिति-सहित, कभी आंखों से अश्रु बहाकर?
नारी क्रिया नहीं, वह केवल क्षमा, शांति, करुणा है ।
इसीलिए, इतिहास पहुंचता जभी निकट नारी के,
हो रहता वह अचल या कि फिर कविता बन जाता है ।
हाय, स्वप्न! जानें, भविष्य भू का वह कब आयेगा,
जब धरती पर निनद नहीं, नीरवता राज करेगी;
दिन भर कर संघर्ष पुरुष जो भी इतिहास रचेगा,
बन जाएगा काव्य, सांझ होते ही, भवन-भवन में!
अभी चंड मध्याह्न, सूर्य की ज्वाला बहुत प्रखर है;
दिवस लग्न अनुकूल वह्नि के,पौरुष-पूर्ण गुणों के ।
जब आएगी रात, स्यात, तब शांत, अशब्द क्षणों में
मही सिक्त होगी नरेश्वरी की शीतल महिमा से ।
और देवि! जिन दिव्य गुणों को मानवता कहते हैं
उस्के भी अत्यधिक निकट नर नहीं, मात्र नारी है ।
जितना अधिक प्रभुत्व-तृषा से पीड़ित पुरुष-हृदय है,
उतने पीड़ित कभी नहीं रहते हैं प्राण त्रिया के ।
कहते हैं, जिसने सिरजा था हमें, प्रकांड पुरुष था;
इसीलिए, उसने प्रवृत्ति नर में दी स्वत्व-हरण की ।
और नारियों को विरचा उसने कुछ इस कौशल से,
हम हो जाती हैं कृतार्थ अपने अधिकार गँवा कर ।
किंतु, कभी यदि हमें मिला निर्बाध सुयोग सृजन का,
हम होकर निष्पक्ष सुकोमल ऐसा पुरुष रचेंगी,
कोलाहल, कर्कश, निनाद में भी जो श्रवण करेगा
कातर, मौन पुकार दूर पर खड़ी हुई करुणा की;
और बिना ही कहे समझ लेगा, आँखों-आँखों में,
मूक व्यथा की कसक, आँसुओं की निस्तब्ध गिरा को ।
औशीनरी
कितना मधुर स्वप्न! कैसी कल्पना चान्द्र महिमा की!
नारी का स्वर्णिम भविष्य! जानें, वह अभी कहाँ है!
हम तो चलीं भोग उसको, जो सुख-दुख हमें बदा था,
मिलें अधिक उज्जवल, उदार युग आगे की ललना को
आयु
माँ! हताश मत हो, भविष्य वह चाहे कहीं छिपा हो,
मैं आया हूँ अग्रदूत बन उसी स्वर्ण-जीवन का ।
पिया दूध ही नहीं, जननि! मैं करुणामयी त्रिया के
क्षीरोज्जवल कल्पनालोक में पल कर बड़ा हुआ हूँ ।
जो कुछ मिला मातृ-ममता से, माँके सजल हृदय से,
पिता नहीं, मैने जीवन में माताएं देखी हैं ।
दिया एक ने जन्म, दूसरी माँ ने लगा हृदय से
पाल-पोस कर बड़ा किया आँखों का अमृत पिलाकर;
अब मैं होकर युवा खोजते हुए यहाँ आया हूँ
राज-मुकुट को नहीं, तीसरी माँ के ही चरणों को ।
माँ! मैं पीछे नृप किशोर, पहले तेरा बेटा हूँ ।
[आयु औशीनरी के चरणों पर गिरता है। औशीनरी
उसे उठाकर हृदय से लगाती है और अपने आसूँ पोंछती है।]
सुकन्या
बरस गया पीयूष; देवि! यह भी है धर्म त्रिया का
अटक गई हो तरी मनुज की किसी घाट-अवघट में,
तो छिगुनी की शक्ति लगा नारी फिर उसे चला दे;
और लुप्त हो जाए पुन: आतप,प्रकाश, हलचल से ।
सो वह चलने लगी;
आइए, वापस लौट चलें हम,
मैं अपने घर, देवि! आप अपने प्रार्थना-भवन में ।
त्यागमयी हम कभी नहीं रुकती हैं अधिक समय तक ।
इतिहासों की आग बुझाकर भी उनके पृष्ठों में।
पंचम अंक समाप्त