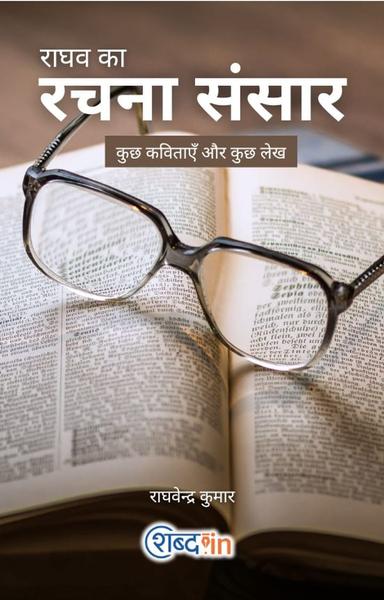जिस देश में 50 फ़ीसदी लोग अशिक्षित हैं । जहाँ के 35 प्रतिशत लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है । जिस देश में विकास
की ढोलक तो बजती है लेकिन यह भुला दिया जाता है कि ढोलक के आवरण के साथ ही दोनों
छोर एक विशाल रिक्तता में जीते हैं । जहाँ प्रत्येक तीसरे दिन किसी न किसी के भूख
से तड़प कर मर जाने की ख़बर आम है । ऐसे में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता
का रोना व्यर्थ ही जान पड़ता है । संविधान निर्माताओँ ने संविधान में मूल अधिकारों
को स्थान देकर हमें मुक्त आकाश में विचरण करने वाला पक्षी तो बना दिया है, लेकिन पंखों को काट दिया है । यह सही भी है क्योंकि अधिकारों का महत्व और
अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक यह एक परिसीमा में रहें । जब अधिकारों का कोई
नाज़ायज़ उपयोग करता है तब यही अधिकार धारदार हथियार बनकर किसी और की ज़िन्दगी
तबाद करने लगते हैं । दूसरों के अधिकारों पर चोट कर स्वअधिकार की बात पाप है ।
भारतीय संस्कृति के आधार पर समाज एवं समुदाय का हित व्यक्ति के हित से बड़ा होता
है । ए. के. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ इसी तरह का निर्णय दिया था ।
किसी एक इंसान के लाभ के लिए पूरे समाज के हितों को कुचलना अमानवीय और न्याय
विरुद्ध है । लोकव्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, अपराध उद्दीपन औरो साधारण जनता का हित यह पाँच ऐसे क्षेत्र हैं जिनका व्यक्ति
की स्वतन्त्रता से सीधा सरोकार है और आए दिन इनसे सामना भी होता रहता है । जब भी
कभी साम्प्रदायिक वैमनस्यता की स्थिति बनती है, इन्हीं कारकों में से किसी कारक का योगदान होता है । एक बात और सामाजिक
नियन्त्रण के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जानलेवा बीमारी के अतिरिक्त और
कुछ नहीं । सामाजिक नियन्त्रण के तत्वों में नैतिक मूल्य, धर्म, साहित्य, शिक्षा, क़ानून और लोक प्रथाओँ आदि को शामिल कर सकते हैं । समाज विज्ञानी रॉबर्ट के
मर्टन कहते हैं कि - अगर समाज के नियमों पर वैयक्तिक इच्छाएं हावी हो जाएँ तो
सामाजिक व्यवहार में अनेक विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी । ये विसंगतियाँ समाज में
अनुशासनहीनता,
अपराध व विद्रोह पैदा करती हैं ।
दादरी में बीफ खाने की अफवाह के बाद एक
शख्स की हत्या और सामाजिक कार्यकर्ताओं, साहित्यकारों की हत्या
होने के विरोध में कई साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया है ।
जाने-माने साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने अपने फैसले के बारे में कहा कि एक व्यक्ति
की सिर्फ इस अफवाह पर हत्या कर दी गई कि उसने गोमांस खाया था ? प्रधानमंत्री को ऐसा अपराध करने वालों को रोकना होगा । जिन लोगों को कुचला और
रौंदा जा रहा है उन्हें बचाने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना होगा । अख़लाक के
क़त्ल के बाद एक नयी साम्प्रदायिक सियासत आकार लेती दिखायी दे रही है । गोमांस के
प्रयोग की अफवाह पर दादरी के बिसाहड़ा गांव में अखलाक नामक व्यक्ति को भीड़ ने
पीट-पीट कर मार डाला था । इस घटना की चौतरफा निंदा हुई और इस पर खूब राजनीति भी ।
काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नेता संगीत सोम, सांसद महेश शर्मा और एआईएमआईएम
नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेता गांव पहुंचे थे । गांव में कवरेज के लिए गई
मीडिया का भी स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया था । बाद में यूपी पुलिस ने इस
मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया । यहां तक की राष्ट्र पति प्रणब मुखर्जी
ने भी इस घटना की निंदा की थी । इस घटना से अपराध उद्दीपन की स्थिति उत्पन्न हुई ।
परिणामतः साम्प्रदायिक टकराव की गम्भीर स्थिति का सूत्रपात हुआ । इसलिए
स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ ही युक्तियुक्त प्रतिबन्ध की भी महती आवश्यकता
प्रतीत होती है । जब बात अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की हो तब प्रतिबन्ध अपरिहार्य
हो जाते हैं । माना कि मूक रहना दासता की निशानी है और मुँह का खुलना आज़ादी का
सूचक । किन्तु मुँह का ज्यादा खुलना भी तो बीमारी का सूचक ही है । कहा जाता है कि
"हमारी आज़ादी वहीं पर खत्म होती है जहाँ पर दूसरे की नाक शुरु होती है ।
प्रसिद्ध भारतीय समाज शास्त्री डॉ. राधाकमल मुखर्जी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहते
हैं कि – “यदि समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्तित्व के परम या सर्वोच्च मूल्यों की
नियमित रूप से पूर्ति करता रहे । व्यक्तित्व की सर्वोत्तम खोज सुन्दरता, अच्छाई तथा प्रेम के आधार पर सामाजिक सम्बन्धों व संस्थाओं की सृष्टि और पुनः
सृष्टि होती है । सम्पूर्ण मानव समाज व मानव कल्याण के लिए इन मूल्यों का संरक्षण
आवश्यक है ।” इस स्थिति में जहाँ गाय को भारत में माँ का दर्जा हासिल है, उसके प्रति किसी भी तरह की क्रूरता सामाजिक असन्तुलन और क्षोभ का कारण बनती है
तथा साथ ही अपराध उद्दीपन एवं विद्रोह को भी आमन्त्रित करती है ।
जहाँ तक बात बीफ़ खाने के समर्थन की है
तो उसके बारे में यह जान लेना ज़रूरी है कि बीफ़ शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए
अहितकर है । बीफ़ खाने को लेकर देश भर में बेचैनी है और सभी तरह के फ़सली नेता
सियासत के अखाड़े में अपना-अपना दाँव खेल रहे हैं । धार्मिक मत तो एक पक्ष है, लेकिन बीफ़ न खाने को लेकर बहुत मजबूत पर्यावरणीय वजहें भी हैं । संयुक्त
राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम ने बीफ़ को 'जलवायु के लिए नुक़सानदेह गोश्त' बताया है । विज्ञान के
क्षेत्र के जाने माने लेखक पल्लव बागला ने समाचार एजेंसी पीटीआई के लिए लिखे गए एक
लेख में कहा है कि रोम में संयुक्त राष्ट्र इकाई फ़ूड एंड एग्रीकल्चर संगठन
(एफ़एओ) की रिपोर्ट के मुताबिक़ गोश्त खाने वाले और ख़ासकर बीफ़ खाने वाले दुनिया
के पर्यावरण के प्रति सबसे कम दोस्ताना हैं । यह अचरज की बात लग सकती है लेकिन
दुनिया में बीफ़ उत्पादन जलवायु परिवर्तन की एक मुख्य वजह है । कुछ तो यह भी कहते
हैं कि बीफ़ गोश्त उत्पादन उद्योग का 'शैतान' है ।
लेकिन बीफ़ खाने के संदेह में एक आदमी
की पीट-पीटकर हत्या को किसी भी समाज में सही नहीं ठहराया जा सकता । विशेषज्ञों का
कहना है कि बीफ़ छोड़ देने से दुनिया का कार्बन उत्सर्जन, कारों के इस्तेमाल के मुक़ाबले कई गुना कम हो जाएगा । एक स्वीडिश अध्ययन के
आंकड़ों के आधार पर यूएनईपी ने कहा, "ग्रीनहाउस गैसों के
उत्सर्जन के संदर्भ में एक घर में एक किलो गोश्त खाए जाने का अर्थ है 160 किलोमीटर तक गाड़ी चलाना ।" इसका अर्थ यह हुआ कि नई दिल्ली से आगरा तक
कार से यात्रा करने से ग्लोबल वॉर्मिंग पर जो असर पड़ेगा वह एक किलो बीफ़ खाने के
बराबर होगा ! इसलिए अचरज की बात नहीं कि बीफ़ को पर्यावरण के लिए बेहद अहितकारी
माना जाता है । बीफ़ खाना चाहिए या नहीं इस पर नैतिक पक्ष तो रखा तो सकता है लेकिन
कानूनन किसी को बलपूर्वक बीफ़ के सेवन से रोकना भी नाज़ाय़ज़ है । खाने की
स्वतंत्रता को जीने के अधिकार में हम देख सकते हैं । कोई व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, और क्या पहनता है ? इसमें दूसरे व्यक्ति की
दखल-अंदाज़ी सही नहीं कही जा सकती है ।
साम्प्रदायिकता के आधार पर भी देश
के इस बदलते माहौल में भोजन की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध
किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त नहीं ठहराया जा सकता है । आज जब विश्व भूमण्डलीकरण
की अवधारणा के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर है और विदेशी संस्कृतियों के साथ
सांमञ्जस्य बिठाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में बीफ़ के
मुद्दे पर भारतीय समाज राजनीति के हाथ का खिलौना बन अपनी बहुलतावादी संस्कृति का
ही उपहास कर रहा है । भारत में अनेकों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं । इनमें
से हजारों लोग विदेशी दूतावासों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य
प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले भी हैं । क्या सभी को हम अपनी भावनाओं के आधार
पर ही भारत में जीने और रहने देंगे ? नहीं न ! तब फिर इस
तरह की सामाजिक बहस का तात्पर्य क्या है ? भारत में इस तरह के मुद्दे तभी उठाए जाते हैं जब मौसम चुमावी रंग में रंगा
होता है । सनातन संस्कृति तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, की बात करती है । यहाँ किसी भी निरपराध को मारना या सताना पाप है । आज जब
व्यवसायिकता की अंधी दौड़ में सरकारें ही माँस का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय
(आयात और निर्यात) कर रहीं हैं तब इस तरह के कृत्य बेहूदा जान पड़ते हैं ।
सफ़ल लोकतन्त्र एवं राजनीतिक
स्वतन्त्रता के लिए नैसर्गिक अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता आवश्यक है (यहाँ नैसर्गिक
शब्द अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को एक सन्तुलित रूप देकर तार्किक बन्धन देता है )
। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए भी नितान्त ज़रूरी है ।
जिस समाज में स्वतन्त्रतापूर्वक विचारों की अभिव्यक्ति न हो सके, उस समाज पर अनैतिकता का शासन हो जाता है । वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता
के आधार पर एक समाज स्वतन्त्र रूप से बस सकता है । प्रत्येक समाज के अपने कुछ नियम
होते हैं जो समाज की निरंकुशता पर अंकुश लगाकर उसे सुरक्षित भविष्य देते हैं ।
साहित्य सृजन भी इसी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का एक सशक्त पहलू है ।
साहित्य समाज का दर्पण होता है । यदि दर्पण गन्दा हो तो देखने वाले का चेहरा भी
गन्दा ही दीखता है । इसीलिए साहित्य का स्वच्छ रहना अत्यावश्यक है । शायद इसी साहित्यिक
व सामाजिक शुचिता को बरकरार रखने के लिए वर्तमान समय के श्रेष्ठ साहित्यकार, इतिहासकार,
फ़िल्मकार, कलाकार और वैज्ञानिक गण अपने
सरकारी साहित्यालंकरण सरकार को वापस करने को विवश हुए हैं ।
सरकारी पुरस्कार एक तरह से प्रबुद्ध
वर्ग और साहित्यकार का स्वातन्त्र्य बन्धक बनाने का कार्य करते हैं । भारतीय
परिदृश्य में स्पष्ट है कि पुरस्कार और पद बिना किसी राजनीतिक दखल के नहीं मिलते
हैं । ऐसे में साहित्यकार व अन्य पदारूढ़ होते या पुरस्कृत होते ही राज्य की
बौद्धिक स्वतन्त्रता गिरवी रखकर राज्याश्रय प्राप्त करते हैं और क़लम और कला को
सियासी रंग में रंग डालते हैं । वास्तविक सृजन की जगह पर वह राज्य के लिए
चापलूसीपरक सृजन में लग जाते हैं । साहित्यकार का एकमात्र उद्देश्य स्वामिभक्ति बन
जाता है । आज जब साहित्यकारों व अन्य के द्वारा सरकारी सम्मान वापस किए जाने का
मामला तूल पकड़ रहा है, तब समझना होगा कि सामाजिक नुमाइंदे
और साहित्यकार बौद्धिक स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर है । अब सामाजिक उत्थान के लिए
अभिव्यक्ति के सारे ख़तरे उठाने ही होंगे । तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब ।
साहित्यकारों व अन्य गणमान्यों द्वारा
पुरस्कार वापसी का मामला सामाजिक परिवर्तन की जगह राजनैतिक पैंतरेबाजी का हिस्सा
नज़र आता है । इसी कारण विरोध के स्वर भी उभर कर सामने आए हैं । प्रगतिशील आलोचक
नामवर, वरिष्ठ पत्रकार कवि विष्णु खरे और मशहूर चरित्र कलाकार अनुपम खेर ने सरकारी
सम्मान वापस करने वाले साहित्यकारों व अन्य बुद्धजीवियों को खरी-खरी सुनाई है ।
गोपालदास 'नीरज' ने कहा कि पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार झूठ बोल रहे हैं । ये सब
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा
कि साहित्य की उपासना करना सत्य की उपासना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । साहित्यकारों को चाहिए कि यदि उन्हें किसी मामले
का विरोध करना है तो कविताएं और कहानियां लिखें । उन्होंने कहा कि अप्रिय सत्य
नहीं बोलना चाहिए । गोपाल दास 'नीरज' ने सवाल उठाया और कहा, आखिर सांप्रदायिकता कहाँ है ? मोदी ने अपने मुँह से सांप्रदायिक बातें तो नहीं की हैं । मैंने भी इमरजेंसी
के दौरान विरोध किया था, लेकिन उस वक्त मैंने कविताएं और
गीत लिखे थे । इससे समाज को एक सन्देश दिया था । उन्होंने कहा कि गोमांस पर विवाद
नहीं होना चाहिए । भारतीय संस्कृति में गाय को माता माना गया है । भगवान कृष्ण गाय
चराते थे । मां के दूध के अलावा गाय ही है जिसका दूध बच्चे से बड़ों तक को फायदा
पहुंचाता है । नीरज ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए । सारे
विवाद समाप्त हो जाएंगे । लेखकों का अवॉर्ड लौटाना सही है या नहीं विषय पर बोलते
हुए मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने कहा कि यह बात और सम्मानजनक होगी अगर एक
साहित्यकार अपनी रचना के ज़रिए खुद को ज़ाहिर करता है । कलाकार अपने काम के लिए
जाने जाते हैं,
न कि अवॉर्ड लौटाने के लिए ।
अन्धविश्वास के विरुद्ध सामाजिक मुहिम
छेड़ने वाले व्हिसिल ब्लोअर नरेन्द्र अच्युत दाभोलकर की जब 20 अगस्त 2013 को हत्या कर दी गयी तब यह बुद्धिजीवी गण क्या कुम्भकर्णी नींद में थे या फिर
आकाओं का आदेश प्राप्त नहीं हुआ था । जब
जून-2015 में मस्जिद के पास बस का हॉर्न बजाने पर धर्म विशेष के लोग बस ड्राइवर रमेश
की पीट-पीटकर हत्या कर देते हैं । अगस्त में मेरठ के पास हरदेवनगर में ऐसी ही
उन्मादी भीड़ लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर सेना के जवान वेदमित्र चौधरी की
हत्या कर देती है । इसी वर्ष मार्च में मुस्लिम लड़की से विवाद करने पर बिहार के
हाजीपुर में एक हिन्दू युवक की हत्या कर दी जाती है । इरूल (आंध्र),पश्चिमी भांडुप (मुम्बई), मुजफ्फरनगर और कोसीकलां
(उत्तरप्रदेश) में भी इसी तरह विशेष समुदाय के लोगों के समूह ने हिन्दू युवकों की
पीट-पीटकर हत्या कर दी थी । तब 'साहित्यकारों' ने सम्मान नहीं लौटाए, क्यों ? आज साहित्यकार इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं ? आम आदमी भी साफतौर पर देख पा रहा है कि यह साहित्यकारों की राजनीति है । कुछ
खास किस्म के साहित्यकारों का 'पॉलिटिकल स्टैंड' । साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने साहित्यकारों से आग्रह
किया है कि सम्मान या पुरस्कार लौटाना, विरोध प्रदर्शन का सही
तरीका नहीं है । भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है । लिखकर, बोलकर सरकार पर दबाव बनाइए, विरोध कीजिए । अगर आपकी क़लम की
ताक़त चुक गयी है या फिर एम. एम. कलबर्गी की हत्या से आपकी कलम डर गई है, तब ज़रूर आप विरोध के आसान तरीके अपना सकते हो । आप तो सरस्वती पुत्र हो ।
तर्क के आधार पर सरकार को कठघरे में खड़ा कीजिए, अन्यथा समाज तो यही कहेगा कि आप साहित्य को राजनीति में घसीट रहे हो । सरकार
की आलोचना के लिए आपके पास तर्क नहीं हैं, इसलिए आप भी ओछी राजनीति कर रहे हो । आम और ख़ास लोग बातें बना रहे हैं कि आप
सम्मान के बूते खूब प्रतिष्ठा तो हासिल कर ही चुके हो, अब उसे लौटाकर मीडिया में सुर्खियां भी बटोर रहे हो ।
फ़ेसबुक पर विश्व हिंदी संस्थान, कनाडा नाम के पेज की एक पोस्ट में सरन घई लिखते हैं कि “आजकल एक चर्चा प्रमुखता से मीडिया पर छायी हुई है, सम्मान लौटाने की । मेरा यह मानना है कि केवल कागज का टुकड़ा लौटा देने से
इतिश्री नहीं हो जाती । उन लेखकों को सम्मान पत्र के साथ मिला पैसा (ब्याज़ सहित), वो मान सम्मान और वो तालियाँ भी वापस करनी चाहिए जो उन्हें सम्मान प्राप्त
करते समय मिली थीं । साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से उन्हें इस बात को प्रमाणत:
सत्यापित करना चाहिए कि क्यों वे वह सम्मान लौटा रहे हैं ? मेरा यह मानना है कि सम्मान को लौटाना उस सम्मान को असम्मानित करने के समान है
। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत से लोग मेरी इस बेबाक राय के लिये मुझे बहुत कुछ
भला-बुरा कहेंगे लेकिन मेरे लिये यह प्रश्न अहम बन गया है क्यों कि मैं भी अपनी
संस्था - विश्व हिंदी संस्थान, कनाडा के प्लैटफ़ार्म से बहुत सी
साहित्यिक विभूतियों को सम्मानित करता रहता हूँ
।”
जो साहित्यकार “दादरी काण्ड” को आतंकी हमला बताकर अपना सम्मान वापस
कर रहे हैं क्या उन्हें पहली बार राष्ट्र-भक्त होने का अहसास हुआ है ? वो साहित्यकार कैसा जो सम्मान का सम्मान न कर सके ? यह जो सम्मान लौटने का फैशन चल गया है केवल एक दिखावा है स्टंट है और कुछ नहीं
। सच्चा साहित्यकार कला और सच्चाई के पथ पर निरंतर अग्रसर रहता है और अपने विचार
विरोध व प्रतिरोध के साथ कलम के माध्यम से व्यक्त करता है न कि सम्मान का तिरस्कार
करके । हम बहुधा एक बात भूल जाते हैं कि साहित्यकार भी एक इंसान है । समाज देश, काल और परिस्थितियों से प्रभावित और विचलित होता है । इसका सीधा असर
साहित्यकार की लेखनी पर पड़ता है । उसकी भी कुछ प्रतिबद्धताएं और विचारधारा होती
है । मैं यहाँ कोई नई बहस शुरु नहीं करना चाहता । लेकिन हर युग हर काल में साहित्य
सम्मानित किया जाता रहा है । साहित्यकार विचारों का वाहक भर होता है । साहित्य
कालजयी होता है जबकि साहित्यकार की विचारधारा समय के सापेक्ष परिवर्तनशील होती है
। यदि कोई साहित्यकार सम्मानित हुआ है तो समकालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में अपने
उद्दात्त विचारों और हितकारी निरपेक्ष नज़रिये के प्रकटीकरण के लिए सम्मानित हुआ
है । व्यक्ति नहीँ विचार सम्मानित होते हैं । चाटुकार व्यक्ति समाज को ग्राह्य है
लेकिन चाटुकारिक सृजन कभी भी दीर्घजीवी नहीं रहा । व्यक्तिगत चाटुकारिता के दम पर
पाये सम्मान जन के मन में स्थान नहीं दिला पाते । अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धता के
चलते व्यक्ति अपनी निष्ठा तो बदल लेता है पर उसका सृजन मुँह चिढ़ाता रहता है ।
सम्मान लौटाने वाले कितने साहित्यकार जनमानस से स्वीकृति पा सके हैं । कभी वे अपने
गिरेबां में झांकें तो पायेंगे कि इस सम्मान के लिए उन्हें सामाजिक स्वाकृति
कभी मिली ही नहीं थी । वह ओहदा तो केवल
रसूख और शासकीय सुविधा पाने का ज़रिया भर था । वक़्त के साथ यदि माहौल बदला है तो
अपनी कलम से वे कहर बरपा दें । किन्तु आज वे अपने ही सृजन को कलंकित कर रहे हैं ।
सम्मान की गरिमा घटाने से किसका भला होगा । सार्थक साहित्य का सृजन संघर्ष की कोख़
से जन्मता है । सुविधा की गोद में तो केवल चाटुकारिता ही पनप सकती है । अधिकांश
साहित्यकार अच्छे सृजन से नाम कमा लेने के बाद जब लगभग लिखना छोड़ चुके होते हैं
तब सम्मान पाते हैं और उसके दम पर तिकड़मों से सुविधाएं । अच्छा होता यदि व्यक्ति
के बजाए उसका सृजन सम्मानित किया जाता क्योंकि व्यक्ति से साहित्य की पहचान नहीं
अपितु साहित्य से व्यक्ति ख्यातनाम होता है ।
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर जब भी
कहीं कुठाराघात होता है, उसके पीछे सदैव बौद्धिक वर्ग की
भूमिका पायी जाती है । अनेकानेक मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन
राजनैतिक पैंतरेबाजी के परिणाम के रूप में सामने आता है । मक़बूल फ़िदा हुसैन ने
भारतीय देवाड़्गनाओं के नग्न चित्र बनाकर स्वतन्त्रता के अधिकार का चीर हरण तो
किया ही साथ ही भारतीय संविधान की आत्मा को भी आहत करने का काम किया । अश्लील
फ़िल्में, भोंडे साहित्य, अश्लील विज्ञापन और अराजक राजनैतिक
बयानबाजी के ज़रिए कथित स्ययम्भू बौद्धिक वर्ग अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का मान
मर्दन करने के सिवा और कुछ नहीं कर रहा । बिना नैसर्गिक स्वतन्त्रता अर्थात
सत्तात्मक स्वतन्त्रता के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है । स्वतन्त्रता
पर प्रतिबन्ध लगाने में एक धारणा यह भी काम करती है कि यदि किसी बुराई को रोकने के
लिए कोई निरपराध फाँसी पर चढ़ता है तो उपयुक्त है । यह वह चिन्तन विधि है जिससे
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का नाश हो जाता है और साहित्यकार तथा राज्य का पारस्परिक
संघर्ष शुरू हो जाता है । लेकिन भारतीय परिदृष्य में किसी भी निरपराध को बचाने के
लिए अपराधी को भी सन्देह का लाभ मिलते जा सकता है । दमन कभी भी बुराई के विनाश का
आदर्श तरीका नहीं हो सकता । दमन की नीति दो अनैतिक विचारधाराओं में से एक का चयन
है । यह दो अनैतिक विचार हिंसा और स्वविचारों का पोषण हैं । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
ही वह आयुध है जिसके बूते इंसान बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेता
है । इसी सन्दर्भ में विद्वान जे. बी. बरी कहते हैं कि “भौतिक और नैतिक उन्नति की एक श्रेष्ठ अवस्था वह है जिसकी प्राप्ति सम्पूर्ण
तौर पर मनुष्य की शक्ति में है और वह है चिन्तन और विवाद की पूर्ण स्वतन्त्रता ।
ज्ञान की उन्नति और त्रुटियों के सुधार के लिए निरंकुश स्वतन्त्रता अनिवार्य है ।
जब चिन्तन स्वातन्त्र्य के सिद्धान्त को सामाजिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ अवस्था
स्वीकार कर लिया जाता है, तब यह साधारण उपयोगिता की परिधि से
निकल कर श्रेष्ठ उपयोगिता की परिधि में प्रवेश कर लेता है, जिसे हम न्याय कहते हैं ।” चिन्तन और विवाद की पूर्ण
स्वतन्त्रता का तात्पर्य स्वतन्त्रता की उस स्थिति से है जिसमें वह सामाजिक रूप से
मज़बूत होकर समाज के हित में भी सोचता और कार्य करता है । स्वतन्त्रता केवल
व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती वरन् समाज के प्रत्येक घटक को प्राप्त होती है ।
अभिव्यक्ति की असीमित स्वतन्त्रता की सार्थकता का दर्शन वाल्टेयर के इन शब्दों में
किया जा सकता है “तुम जो कुछ भी कहते हो, मैं उसे अस्वीकार करता हूँ, परन्तु उक्त कथन को कहने के
तुम्हारे अधिकार की रक्षा मैं अन्तिम श्वास तक करूँगा ।”
वैसे तो कोई भी व्यक्ति वाह्य या आन्तरिक
तौर पर सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं हो सकता । वह वंश, परिवार के पालन और पोषण, वातावरण और मनः स्थिति से विवश
होता है और इनमें परिवर्तन लाने की शक्ति और स्वतन्त्रता पर उसका बहुत कम अधिकार
होता है । मनुष्य कुछ मानसिक विवशताओं और अवचेतन की कुण्ठाओं के अन्तर्गत जीवन
व्यतीत करता है किन्तु फिर भी स्वतन्त्रता की अनुभूति पैदा हो सकती है ।
साहित्यकार के लिए इस अनुभूति को व्यक्त करना अनिवार्य है । स्वतन्त्रता के दो
पक्ष हैं- एक आन्तरिक और दूसरा वाह्य और इसी कारण स्वतन्त्रता की व्याख्या आन्तरिक
और वाह्य पक्ष से ही हो सकती है । आन्तरिक तौर पर स्वतन्त्रता की अनुभूति तब पैदा
होती है जब हमें अपनी वृत्तियों, आकांक्षाओं और मन की मौज़ में बिना
किसी बाधा और विवशता के बह जाने का अवसर प्राप्त होता है, जब हम अपनी त्रुटियों में से किसी एक को दूर करने की क्षमता रखते हैं और प्रतिबन्ध
में परिवर्तन महसूस करते हैं । अर्थात बिना किसी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रतिबन्ध के अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता साहित्य के लिए
अनिवार्य है ।
मिल्टन कहते हैं कि “मुझे समस्त स्वतन्त्रताओं से अधिक अपने विवेक के अनुकूल ज्ञान, वाणी और विवाद की स्वतन्त्रता दो ।” चिन्तन स्वातन्त्र्य
और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य एक दूसरे से जुड़े हैं । शताब्दियों के संघर्ष के बाद
यह स्वीकार किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का
अविच्छिन्न अंग है । इसका एक तार्किक, नैतिक या सामाजिक पक्ष
यह भी है कि जो लोग राजनीतिक, धार्मिक सुरक्षा के लिए इस सुरक्षा
को नष्ट करना चाहते हैं, वे अपने आप में पूर्ण रूप से
विश्वास कर लेते हैं कि साहित्यकार का विचार ग़लत है अर्थात वह मानसिक दासता के
अधीन है । स्वतन्त्रता का नाश करने वाले लोग सही भी हो सकते हैं और ग़लत भी हो
सकते हैं । किन्तु सही और ग़लत का निर्णय वे स्वयं नहीं कर सकते । यदि वह सही भी
हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह दूसरों की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण करें ।
अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य के सन्दर्भ में जे. एस. मिल कहते हैं कि- एक मत को सत्य
स्वीकारने, क्योंकि उसको असत्य सिद्ध करने के प्रत्येक अवसर के बावज़ूद भी रद्द नहीं किया
जा सकता और उसे रद्द करने की आज्ञा न देने के उद्देश्य से इसे सत्य स्वीकार करने
में बड़ा अन्तर है । किसी विचार को रद्द करने और असत्य सिद्ध करने की पहली शर्त ही
सम्पूर्ण स्वतन्त्रता है, जिसे हम क्रिया के उद्देश्य के लिए
उसको सत्य समझने में न्यायसंगत हैं और दूसरी किसी शर्त पर मानव प्रवृत्ति के साथ
कोई व्यक्ति बौद्धिक तौर पर अपने आप को सत्य समझने का विश्वास नहीं कर सकता ।
अभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध से अभिव्यक्ति
और तीव्र हो जाती है । जब-जब अभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगा है, विचारों की तीक्ष्णता से आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ है । अभिव्यक्ति की
स्वतन्त्रता पर लगने वाले पहरे के आलोक में नयी विचारधाराओँ का जन्म हुआ है ।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य का मनुष्य होना । अभिव्यक्ति पर
प्रतिबन्ध का अर्थ है मानव को दासता की बेड़ियों में जकड़ कर उसे जानवरों सरीखा
जीवन जीने के लिए विवश करना । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर श्री
राजेंद्र यादव जी द्वारा हंस पत्रिका के माध्यम से मुशी प्रेमचंद के जन्म दिवस पर “अभिव्यक्ति और प्रतिबन्ध” विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया
गया, जिसमें अशोक वाजपेयी, गोविन्दाचार्य, अरुंधती रॉय और नक्सली विचारधारा के कवि वरवर राव को आमंत्रित किया गया । वरवर
राव दिल्ली आये भी लेकिन उसके बाद गायब हो गए और कार्यक्रम में भी नहीं आये ।
अरुंधती रॉय ने भी गोष्ठी में अनुपस्थित रहकर अपना विरोध दर्शाया । विरोध इस बात
का था कि कभी पूंजीवाद का विरोध न करने वाले और कॉर्पोरेट जगत के चहेते अशोक
वाजपेयी और खांटी हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े रहने वाले गोविन्दाचार्य को क्यों
बुलाया गया ? चर्चा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हो और उसमें किसी विशेष विचारधारा के ही
लोगों को बुलाने का दुराग्रह फ़ासिज्म नहीं तो क्या है ? क्या केवल वामपंथी विचारधारा के लोगों को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी
चाहिए ? क्या लोकतंत्र में अन्य विचारधाराओं को अपने विचार व्यक्त करने से रोका जाना
उचित है ? क्या इसी वैचारिक जड़ता के कारण ही आज दुनिया से वामपंथ की दुकान बंद नहीं हो
रही है ? क्या ये मानसिकता भारतीय चिंतन “आ नो भद्र कृत्वो
यन्तु विश्वतः”
(सभी दिशाओं से नए विचारों को आने दो) अथवा माओत्से
तुंग के “हजार फूल खिलने दो” के विपरीत नहीं है ?
भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु और उदार समाज का पोषक है । संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को
व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है । अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता मनुष्य का एक सार्वभौमिक और प्राकृतिक अधिकार है । लोकतंत्र एवं
सहिष्णुता में विश्वास रखने वालों का कहना है कि कोई भी राज्य और धर्म इस अधिकार
को छीन नहीं सकता । लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान किया जाना चाहिए
। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है । उसे समाज में सम्मान से जीने का
अधिकार है । अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की आड़ में कोई भी किसी दूसरे के सम्मान को
ठेस नहीं पहुँचा सकता । इसलिए भारतीय संविधान के अनुछेद १९ च में मान हानि का
प्रतिषेध किया गया है । भारतीय दण्ड
संहिता की धारा 499 और 500 में मान हानि को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यह व्यवस्था दी गयी है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण तथा दैहिक
स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार वंचित न किया
जाएगा । अर्थात क़ानून के दायरे में वह पूर्ण स्वतन्त्रता पाता है । स्वतन्त्रता
चाहें जीवनशैली की हो या फिर अभिव्यक्ति (रचनात्मक या सम्भाषणात्मक) की । लेकिन
क्या इसकी कोई सीमा भी बांधी जानी चाहिए और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से की
जाने वाली आलोचना और अपमान के बीच कोई लकीर होनी चाहिए ? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर भारत में भी समय समय पर विवाद होता
रहा है और कई पुस्तकों को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है । भारत में दो बड़े
धर्मों हिन्दू और इस्लाम के अनुयायी धर्मों और धार्मिक पात्रों पर लिखी जाने वाली
पुस्तकों, फ़िल्मों और कलाकृतियों को प्रतिबंधित करने के लिए
अनुच्छेद २९५ क का इस्तेमाल करते रहे
हैं । पिछले कुछ वर्षों में असहिष्णुता में अधिक तेज़ी आई है और हिन्दुओं
और मुसलमानों के समूहों ने कई बार हिंसक प्रदर्शन के माध्यम से किताबों, फ़िल्मों और नुमाइशों पर पाबंदी लगवाने में सफलता हासिल की है । प्रसिद्ध
भारतीय ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी की किताब 'सैटेनिक वर्सेज़' पर मुसलमानों के विरोध और धमकियों के
कारण भारत में 1988 में प्रतिबंध लगाया गया था । अभी हाल के वर्षों में कुछ मुस्लिम संगठनों की
धमकी के मद्देनज़र सलमान रश्दी जयपुर के साहित्यिक समारोह में शामिल नहीं हो सके ।
भारत में दर्जनों पुस्तकों पर तथाकथित 'धार्मिक भावनाओं को
ठेस पहुँचाने'
के नाम पर प्रतिबंध लगा हुआ है । डी. एन. झा की पुस्तक 'द मिथ ऑफ़ द होली काउ', वेंडी डोनिगर की 'द हिन्दूज़'
और डेसमंड स्ट्वार्ट की 'अर्ली इस्लाम' आदि इन दर्जनों प्रतिबन्धित पुस्तकों
में शामिल हैं । बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन कुछ साल पहले कोलकाता में रहती
थीं । वहाँ मुस्लिम अतिवादियों ने शहर की सड़कों पर उनके ख़िलाफ़ दंगा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें शहर छोड़ना पड़ा और वह कोलकाता वापस न जा सकीं ।
हैदराबाद में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान वहाँ के एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन के
कार्यकर्ताओं ने तसलीमा पर हमला किया था । देश के अग्रणी पेंटर मक़बूल फ़िदा हुसैन
की बनाई गई हिंदू देवी और देवताओं की कुछ कला कृतियों को कथित कट्टरपंथी हिंदू
संगठनों ने हिन्दू देवताओं का अपमान क़रार दिया । मक़बूल फ़िदा हुसैन की पेंटिंग
प्रदर्शनियों पर हमले किए गए और वह चरमपंथियों के हमले के अन्देशे से अपनी धरती पर
वापस न आ सके और विदेश में अंतिम सांस ली । अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सबसे बड़ा
हमला फ्रांस में व्यंग्य और हास्य की अग्रणी पत्रिका 'शार्ली एब्डो' पर हुआ । 'शार्ली एब्डो' के पत्रकारों की हत्या की भारत में हर तरफ़ निंदा की गई । ऐसे में शार्ली
एब्डो पर हमले के बाद यह सवाल और मौजू हो गया है । पेरिस में 'शार्ली एब्डो' के पत्रकारों की नृशंस हत्या के बाद
भारत में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि किसी लोकतान्त्रिक समाज में अन्य
सभी संस्थानों की तरह क्या धर्मों और धार्मिक पात्रों को भी आलोचना और किसी के
अपमान के दायरे में नहीं लाना चाहिए ? पत्रिका 'शार्ली एब्डो' पर हमले के विषय में मुसलमानों के संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत ने
कहा, "हम पेरिस पत्रिका कार्यालय पर हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में निंदा
करते हैं जिसमें 12 मासूम इंसानों की जान चली गई
।" "इस्लाम और मुसलमान किसी भी
राष्ट्रीयता और धर्म से सम्बन्धित मासूम इंसानों की हत्या को ख़ारिज करते हैं ।
सिर्फ़ अदालतें ही किसी को सज़ा देने के लिए अधिकृत हैं और केवल एक मुस्लिम राज्य
ही ज़िहाद की घोषणा कर सकता है ।" मजलिस ए मुशावरत के इसी बयान में यह भी कहा
गया है कि सभी सभ्य समाज में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन यह स्वतन्त्रता 'रचनात्मक आलोचना' तक सीमित होनी चाहिए और विभिन्न धार्मिक पुस्तकों और पैग़म्बरों आदि के अपमान के
लिए उपयोग नहीं की जानी चाहिए ।
भारत में पेरिस जैसे मामले का सामना
पहली बार 1920 के दशक में उस समय हुआ जब अविभाजित भारत के शहर लाहौर में एक आर्य समाजी
हिन्दू प्रकाशक ने मुसलमानों के पैग़ंबर हज़रत मोहम्मद के निजी जीवन के बारे में
एक विवादास्पद किताब (रंगीला रसूल ) प्रकाशित की । पैग़म्बर मोहम्मद पर लिखी जाने
वाली क़िताब के प्रकाशक राजपाल को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा
चला । तब धर्म के अपमान का कोई क़ानून
नहीं था । कई साल की सुनवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया । लेकिन एक मुस्लिम युवक ने पुस्तक के प्रकाशक
राजपाल की 1929 में हत्या कर दी । हत्यारे को उसी साल फांसी की सज़ा हुई । इस घटना के परिणाम
स्वरूप भारतीय दंड संहिता में धर्म के अपमान के लिए धारा 295-ए को शामिल किया गया । यह संघर्ष और तनाव आज का नहीं है । अभिव्यक्ति की
स्वतन्त्रता के लिए सुकरात को विषपान करना पड़ा था । गैलिलियो को सिर्फ इसीलिए चुप
करा दिया गया था क्योंकि उसके विज्ञान सम्बन्धी निष्कर्ष धर्माधिकारियों के खिलाफ
थे । यदि वह अपने विचारों और वक्तव्यों के लिए खेद प्रकट न करते तो उनका जीवन
समाप्त हो जाता और मानव जाति उनकी महान खगोलीय खोजों से वंचित रह जाती ।
आज विश्व पर साम्राज्यवाद की नयी शाखा का असर
सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । भारत जैसे विकासशील और बहुलतावादी सांस्कृतिक
विरासत के धनी देश में सदैव ही नवीन विचारों (ख़ासतौर पर पश्चिमी देशों द्वारा
प्रवर्तित) का स्वागत किया गया है । आज विश्व सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की चपेट में
है । भारत सहित विश्व के कई देश सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से संक्रमित हैं । विदेशी
भाषा-शैली, रहन-सहन, खान-पान और दूषित मानसिकता से देशी मान्यताओं को ख़तरा पैदा हो गया है ।
व्यक्तिवादी विचारधारा में सारी मनुष्य जाति डूबने को आमादा नज़र आती है । आलोचक
सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को सांस्कृतिक प्रभुत्व की संज्ञा देते हैं । सांस्कृतिक
साम्राज्यवाद सदैव ही पूँजीवाद के कन्धे पर चढ़कर आता है । धन लोलुपता ने सदैव ही
व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करने का काम किया है । धन की चमक में पाप और
पुण्य का भेद मिटने लगता है । सद् और असद् की धारणा क्षीण हो जाती है । समाज
धनोपार्जन के लिए अपनी मान्यताओं और धारणाओं में आमूलचूल परिवर्तनों को अन्ज़ाम
देता है । यही परिवर्तन संस्कृति का रूप विद्रूप कर डालते हैं और एक अपसंस्कृति को
जन्म देते हैं । यह अपसंस्कृति आगे चलकर धार्मिक और साम्प्रदायिक टकराव का कारण
बनती है । अब यदि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का विहंगावलोकन किया जाए तो हमें
स्वतन्त्रता के अधिकार का बिना अतिक्रमण किए एक अपसंस्कृति परिणामरूप में प्राप्त
होती है । यदि हमारी स्वतन्त्रता कुछ बन्धनों के साथ आगे बढ़ती तो शायद सांस्कृतिक
साम्राज्यवाद की जगह सौम्य सनातन संस्कृति का जीवन्त रूप कुलांचे भरता दीखता ।
विचारणीय है कि क्या धर्म के नाम पर
किसी के विचारों का गला घोंटा जा सकता है ? क्या धर्म इतना असहिष्णु हो गया है, जो ज़रा-ज़रा सी बात
पर उसे तक़लीफ़ हो जाती है ? दिल्ली की सड़कों सहित भारत के
ज़र्रे - ज़र्रे में हुए पैशाचिक कृत्यों पर न किसी को शर्म आयी और न ही किसी
धर्मावलम्बी या मूर्धन्य साहित्यकार ने कोई ठोस क़दम उठाया । निर्भया काण्ड भी इन
कथित धर्मावलम्बियों को धर्म पर प्रहार प्रतीत नहीं हुआ । धर्म भी तो अभिव्यक्ति
की स्वतंत्रता का एक रूप है । किन्तु क्या धर्म केवल राजनीति का विषय भर रह गया है
? धर्म के विषय में इतना जान लेना आवश्यक है कि- ''जो धारण करने योग्य हो '' वही धर्म है । धर्म देश, काल और परिस्थिति के आधार पर परिवर्तित होता रहता है । मनुष्य तो परिस्थितियों
का दास है और परिस्थितियाँ कभी-कभी इंसान को उस कृत्य के लिए प्रेरित करती हैं जो
आदर्श स्थिति में अधर्म होता है; किन्तु ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति
को वह अधर्म करना ही होता है जो समय की आवश्यकता है । लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में
धर्म आडम्बर से ज्यादा कुछ नहीं । हम किसी भी धर्म की आलोचना , अच्छाई या बुराई में नहीं पड़ना चाहते । लेकिन इतना ज़रुर है कि जब कोई धर्म के
नाम पर इंसानों का बंटवारा करता है; धर्म के सीने में खंजर घोपने का
काम करता है । धर्म में निष्ठा छिपी है, यही निष्ठा धर्म को
मानने न मानने का आधार है । श्रीमद्भगवदगीता में भगवान् कहते हैं -
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः
स्मृतिर्ग्यानमपोहनम् च ।
वेदैश्च सर्वेरहमेव
वेद्योवेदांतकृद्वेदविदेव
चाहम् ।।
अर्थात मैं ही सब प्राणियों के हृदय में
अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन (विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम 'अपोहन' है) होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य (सर्व वेदों का
तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा ''जानने के योग्य '' एक परमेश्वर ही है) हूँ तथा वेदांत का
कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ ।
लेकिन अफ़सोस हमारे पाखंडी धर्मवेत्ताओं
ने श्लोकों की अनुचित व्याख्या कर हम मनुष्य रुपी प्राणियों को आपस में लड़ने का
मंच तैयार कर दिया । इसके पीछे इनकी मंशा यही रही होगी जो हमें गुलाम बनाने वाले
अंग्रेजों की थी । हम धर्म के नाम पर लड़कर दिन-प्रतिदिन पीछे ही खिसक रहे है । ऐसे
में जरुरत है धर्म के सही ज्ञान की, जिससे हम आपसी मतभेदों को भुलाकर
प्रगति की ओर बढ़ सके । धर्म विघटन का नहीं अपितु सामञ्जस्य का स्थापक है । इसे
विनाश का नहीं विकास
का साधन बनाना प्राणिमात्र के लिए
श्रेयस्कर होगा । धर्म की स्वतन्त्रता का यह अर्थ कतई नहीं कि किसी की भावनाओं से
खिलवाड़ किया जाए । धर्म देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता
है । हो सकता है कि जो हमारे लिए धर्म हो वही अन्यत्र अधर्म हो । अनेकों देशों और
सम्प्रदायों के आचरण जो उनके लिए ईश वाक्य हैं सनातन धर्म की दृष्टि में अधर्म ।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर धर्म को मानने का अधिकार सिर्फ इन्सान को है
। मुक्तिबोध और फैज जैसे कवियों ने जब ‘अभिव्यक्ति के खतरे
उठाने’ और ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे’ का आह्वान किया था, वे राज्यसत्ता के चरित्र और उसके द्वारा समय-समय पर लगायी गयी पाबंदियों से
भली भाँति परिचित थे ।
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और प्रतिबन्ध
की बात की जाए और 1975
का काला अध्याय छोड़ दिया जाए तो यह अभिव्यक्ति की
स्वतन्त्रता पर न लिखने जैसा ही होगा । आज़ाद हिन्दुस्तान में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गयी । इसी के साथ पत्र-पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लगा
दी गई । 1975 में 25 जून की रात जब सभी सोए थे तो लोकतन्त्र कुलांचे भरता नज़र आया था । लेकिन न
जाने क्यों आज यह रात बहुत ही बड़ी हो गयी थी । जगने को तो पूरा हिन्दुस्तान ही
जगा था । किन्तु आज के सूरज में लालिमा की जगह कालिमा थी । आज़ादी की सुबह की जगह
एक बार पुनः ग़ुलामी की रात मुँह बाए खड़ी थी । अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कठोर
प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गयी । अखबारों की रात में
ही बिजली काट दी गयी जिससे कोई समाचारपत्र न छप सके । जो कुछ छपे थे सभी ने
आपातकाल का विरोध किया था । जब सुबह अख़बार लोगों के हाथों में पहुँचा, अखबार के मुख्य पृष्ठ काले रंग से सराबोर थे या फिर प्रश्नचिन्ह लगाकर छोड़ दे
गए थे और सम्पादकीय स्तम्भ भी या तो रिक्त थे या प्रश्नचिन्ह लगाकर छोड़ दिये गये
थे । कोई न कोई आपातकाल विरोधी प्रयत्न सभी के द्वारा किया गया था । सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को बन्दी
बनाते हुए सारे समाचार पत्र जब्त करा लिये, उनके सम्पादकों को उनके इस दु:साहस के लिए जेल में ठूंस दिया । किंतु तमाम
प्रतिबंधों के बावजूद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह ग्रहण नहीं लगा ।
पत्र-पत्रिकाओं पर सेंसर लगा तो भूमिगत बुलेटिनों ने कुछ हद तक इसकी क्षतिपूर्ति
की । कुछ संपादकों ने संपादकीय का स्थान खाली छोड़कर तो कुछ ने अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता के पक्ष में महापुरूषों की उक्तियों को छापकर सरकार का विरोध किया ।
आपात काल के दिनों में हिन्दी के दो सम्पादक शीर्ष पर थे- 'नवभारत टाइम्स' के अक्षयकुमार जैन और 'हिन्दुस्तान' के रतन लाल जोशी । जहाँ अक्षय कुमार जैन
ने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध को स्वीकार करते हुए इन्दिरा गांधी के
जयकारे लगाए और उन्हें बधाई देने गये, वहीं क़लमकार रतनलाल
जोशी ने अपने सम्पादकीय में लिखा, कितना सुखद आश्चर्य है कि उच्चतम
न्यायालय के तीन माननीय न्यायमूर्त्तियों ने अलग - अलग निर्णय दिये; परन्तु तीनों निर्णय एक समान हैं । अक्षय जैन पत्रकारिता के शिखर पर होते हुए
भी अपकीर्ति के गर्त में गिर गए । लेकिन रतनलाल जोशी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर
लगे प्रतिबन्ध को लेकर पत्रकार के धर्म का निर्वाह कर हम पत्रकारों के आदर्श बन गए
। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कुछ एक छोटे-मोटे हमलों और प्रतिबन्धों को झेलते
भारतीय लोकतन्त्र इक्कीसवीं सदी में आ पहुँचा ।
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का असली
स्वरूप नव मीडिया अर्थात वेब मीडिया ने इक्कीसवीं सदी में प्रस्तुत किया । नव
मीडिया सूचना क्रान्ति का संवाहक बनकर उभरा है । जन जागरण से लेकर राजनैतिक
आन्दोलनों तक में इण्टरनेट मीडिया ने अल्प समय में ही महती भूमिका का निर्वाह कर
अपना अलग और विशिष्ट स्थान बना लिया है । सन् 2008 में भारत सरकार द्वारा सन् 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
में धारा 66-ए जोड़ी गयी (जिसे अभी मार्च, 2015 में सर्वोच्च
न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया गया अनुचित अंकुश मानकर निरस्त
किया है) । इस धारा के अनुसार पुलिस को यह अधिकार था कि वह चाहे जिस अभिव्यक्ति को
अपराधी मानकर दमनात्मक कार्रवाई कर सके । उदाहरण के लिए, इस धारा के खिलाफ 21 याचिकाएं दायर की गयीं, जिनमें पहली याचिका कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी । बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई बंद के
विरोध में फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखने वाली लड़की शाहीन ढाडा को ही नहीं, उस टिप्पणी को ‘लाइक’ करने वाली एक दूसरी लड़की रीनू श्रीनिवासन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ।
श्रेया सिंघल ने इस धारा को चुनौती दी थी । गत 24 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और आरएफ नरीमन की पीठ ने इससे संबंधित सभी जनहित
याचिकाओं पर दिये फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत मूल्य घोषित करते
हुए इस धारा को निरस्त कर दिया । सुप्रीम कोर्ट की दलील है कि स्वतंत्रता और
स्वच्छंदता के बीच संतुलन कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है । सरकारें खुद तय करें
कि यह काम कैसे किया जाए । लेकिन कानून का भय दिखाकर बोलने की आजादी पर प्रतिबंध
लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त वैचारिक
अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है । इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि अदालत का फैसला
अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकारों की दलीलों के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा
लेकिन सरहद और समाज की सुरक्षा एवं सामाजिक सरोकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी
सरकार की है और इसके बोझ तले दबी सरकारों के लिए यह फैसला बेशक चुनौती को बढ़ाने
वाला साबित होगा । इस ऐतिहासिक फैसले के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं की हकीकत
से इंकार नहीं किया जा सकता है । इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में साइबर स्पेस की स्वच्छंदता
को काबू में करने की चुनौती सरकार के लिए एक तरफ परेशानी का सबब बन सकती है वहीं
सोशल मीडिया पर सक्रिय तबके लिए खुद को काबू में करने की चुनौती होगी । असली
दुनिया की ही तरह वर्चुअल दुनिया भी कानून से वंचित दुनिया नहीं है । इस सच्चाई से
मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि साइबर स्पेस में अधिकतर युवा वर्ग सक्रिय है । यह
वर्ग अपनी भावनाओं के ज्वार में बहकर मर्यादा की हदों को लांघने के नैसर्गिक खतरे
से जूझता रहा है । उसे कानून और मर्यादा की हदें पहचाननी होंगी । इस फैसले का
सकारात्मक पहलू यह है कि सूचना क्रांति के दौर में जानने, समझने और अपने विचारों को व्यापकतम आयाम देने की आजादी मिलेगी । आज़ादी का यह
स्वाद तभी सार्थक कहा जा सकता है जबकि सोशल मीडिया या साइबर जगत में अपनी मौजूदगी
दर्ज करा चुके लोग इस माध्यम की संवेदनशीलता को समझें । साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल
का कहना है कि अदालत का यह फैसला बेहद संतुलित है लेकिन सरकारों के प्रति सजगता और
दायित्वबोध की सीमा को बढ़ा देगा । खासकर भारत की विशेष परिस्थितियों में जहां
शिक्षा के पर्याप्त प्रसार की कमी के बावजूद समाज के सभी तबकों में साइबर जगत की
पहुंच अब आसान हो गई है । शिक्षा, रोजगार, आर्थिक हालात जैसे सामाजिक सरोकारों से इतर हर वर्ग के लोग किसी न किसी रुप
में इंटरनेट की पहुंच में हैं । इस फैसले के माध्यम से अदालत का सन्देश साफ है कि
सरकारें कानून की तलवार से सोशल मीडिया पर नियंत्रण का चाबुक नहीं चला सकती हैं ।
यह सर्वमान्य सत्य है कि देश में हर फैसला राजनीति से प्रेरित होता है । धारा 66 ए का अब तक का इस्तेमाल यह बताता है कि पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया पर
सक्रिय युवाओं की सियासी जमात के खिलाफ उभरती आवाज को दबाने के लिए ही किया है ।
मुंबई में बाल ठाकरे से लेकर उत्तर प्रदेश में आजम खान तक के खिलाफ उठी आवाज को
कानून के बल पर दबा दिया गया ।
आज जब अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा उस
पर लगने वाले राजनैतिक और साम्प्रदायिक प्रतिबन्धों को केन्द्र में रखकर
बुद्धजीवियों के मध्य एक बड़ी बहस चल ही पड़ी है तब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह
लड़ाई अब कहाँ तक जाती है ? आज जब भारतीय लोकतन्त्र विवशता के
गर्त की ओर अग्रसर है, रुढ़िवादी बन्धनों में फंसा तिलमिला रहा
है । वर्तमान युग में लोकतन्त्र अपनी अस्मिता बचाने को एकटक दृष्टि से मीडिया
(टी.वी., रेडियो, समाचार पत्र और वेब मीडिया) की ओर ताक रहा है । ब्रजभूषण बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली
मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रेस की स्वतन्त्रता वाक् एवं
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का ही एक अंग है, जिसे इस प्रकार (सेन्सर करके) प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता । अभिव्यक्ति की
स्वतन्त्रता के लिए आज जब लेखक और साहित्यकार आगे आए हैं मीडिया को भी जीवट दिखाना
होगा । आज बहुतेरे मीडिया माध्यमों पर पेड न्यूज़ का आरोप लग रहा है । किसी न किसी
राजनैतिक विचारधारा के पोषण का भी आरोप न्यूज़ चैनलों और समाचार पत्रों पर लगता
रहता है । ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि निष्पक्षता के साथ फत्रकारिता के बूते
मीडिया अपनी छवि सुधारने का प्रयास करे । यदि अभिव्यक्ति स्वातन्य्र्छ की इस लड़ाई
में साहित्यकार वर्ग अकेला पड़ा तो आने वाली कई सदियों को अभिव्यक्ति को गिरवीं रख
जीने के लिए विवश होना होगा । आज के समय में लेखक को समाज और सरकार दोनों का
कोपभाजन होना पड़ता है । लेखक को सरकार और दरबार दोनों ही अपना ग़ुलाम समझते हैं ।
आख़िर लेखक की भी अपनी भावनाएं हैं । यदि वह सभी की इच्छा के अनुरूप लिखने लगेगा
तो फिर वह लेखक कहाँ रह जाता, तब तो वह चारण और भांड़ बनकर रह
जाएगा । लेखक का भी तो अपना अस्त्तित्व है । सरकारों को लेखन नाग़वार गुज़रा तो वह
लेखक को जेल में डालती है और यदि सम्प्रदायों को धार्मिक बदबू आयी तो साहित्यकारों
के प्राणों पर बन आती है । प्रत्येक ओर से एक ही कोशिश कि साहित्यकार भयभीत होकर
अभिव्यक्ति की दासता स्वीकार कर ले ।
प्रो. सैयद एहतेशाम हुसैन ज़ौके-अदब और
शऊर में एक जगह कहते हैं कि यह विवेक के अनुसार जीवन को समझने की बात है, मूल्यों को अपनाने और पूरे कलात्मक विवेक के साथ अभिव्यक्ति की सारी शक्ति और
कोमलता के साथ उसे प्रस्तुत करने की बात है । इस प्रकार हर साहित्यकार इस प्रश्न
का उत्तर अपने विवेक के अनुसार देगा और यदि वह दुनियाँ को शान्ति, सन्तुष्टि और सौन्दर्य से मालामाल देखना चाहता है, तो उसका यह उत्तर नहीं हो सकता कि वह अपने लिए लिखता है या उनके लिए लिखता है
जो इन मूल्यों के विरोधी हैं ।
मार्क्स कहते हैं कि “समाज में अस्तित्व के लिए जो निरन्तर संघर्ष चल रहा है वही हमारे समाज को
परिवर्तित करता रहता है ।” भारतीय परिदृष्य से समाजवादी
बौद्धिक आन्दोलन की विदाई होती दीख रही है । इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के
नाम पर यही बौद्धिक वर्ग अपनी साख बचाने का प्रयास कर रहा है । आज जब विश्व नव
विचारों व स्वसंस्कृति के आधार पर प्रगति के मार्ग पर अग्रसारित है, भारत भी स्वसंस्कृति के आलम्बन पर ही प्रगति की ओर निहार रहा है । भारत में
पश्चिमी मानसिकता और संस्कृति के विरोधी किसी भी कीमत पर ऐसा होने देना नहीं चाहते
हैं । इसलिए बौद्धिक सामाजिक आन्दोलन का नाम देकर संस्कृति विरोधी दल भारत सरकार
पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं । कोई इतिहास बदलने का विरोध कर रहा है तो
किसी को सनातनी संस्कृति का उभार रास नहीं आ रहा है । पंथनिरपेक्षता के नाम पर
साहित्यकारों का एक समूह राष्ट्रवादी विचार धारा का परोक्षतः खण्डन करता नज़र आ
रहा है । भारत में मानवाधिकार संवैधानिक भी हैं और नैसर्गिक भी । वर्तमान में
लोकतन्त्रात्मक सत्ताएँ जिन अधिकारों को मानव समाज के विकास का अभिन्न अंग मानती
हैं वे तो भारतवर्ष के न्यायिक दर्शन का प्रमुख अंग हैं । मनु, गौतम, याज्ञवल्क्य सहित आचार्य चाणक्य तक सभी भारतीय मनीषी स्वतन्त्रता के अधिकार की
वकालत करते हैं । अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का प्रयास करने वाली शक्तियाँ
सदैव ही शक्ति शून्य और श्रीहीन हुई हैं । कारावासों और प्रतिबन्धों ने सदैव ही
कलात्मकता को नए युग के सूत्रपात का आधार दिया है । प्राचीन भारत में अभिव्यक्ति
की स्वतन्त्रता पर कठोर प्रतिबन्ध के कोई ठोस प्रमाण दृष्टिगत नहीं होते अपितु
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को पुष्ट करने वाला उदाहरण श्रीराम और सीता मइया का
वियोग सामने आता है । अभिव्यक्ति स्वातन्य्र्र के लिए राजागण जनता दरबार का आयोजन
करते थे । सामाजिक असन्तुलन को रोकने के लिए असामाजिक तत्वों पर अवश्य ही ऐसे
प्रतिबन्धों की बात सामने आती है । वाक् एवं अभिव्यक्ति की मर्यादित स्वतन्त्रता
भारतीय दर्शन का आधार रही है । भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के सौ अपराध क्षमा
करने का दृष्टान्त भी मर्यादित स्वतन्त्रता को पुष्ट करता है । अभिव्यक्ति की
अमर्यादित स्वतन्त्रता ने महाभारत जैसे युद्ध की बुनियाद रखी । यदि द्रुपदसुता ने
दुर्योधन का उपहास न उड़ाया होता तो शायद यह विनाशकारी महाभारत का युद्ध ही न होता
। समाज को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होनी चाहिए जिसके सहारे समाज चहुँमुखी विकास
कर सके । लेकिन साथ ही ऐसे प्रतिबन्ध भी लगाए जाने चाहिए जो विकास को विनाश के पथ
पर जाने से पहले ही रोक सकें ।