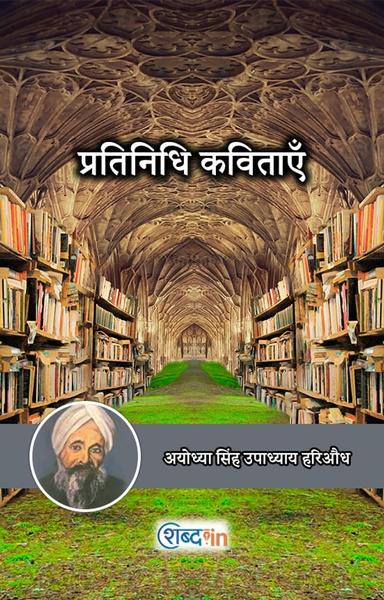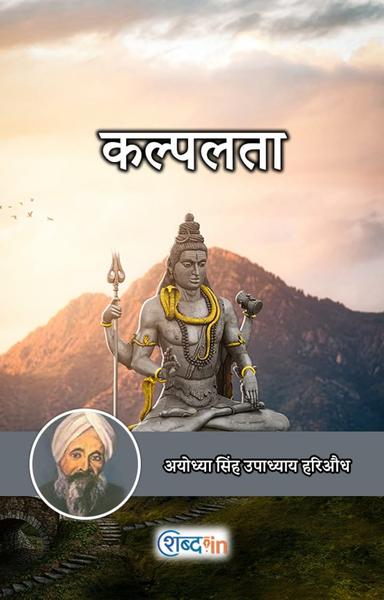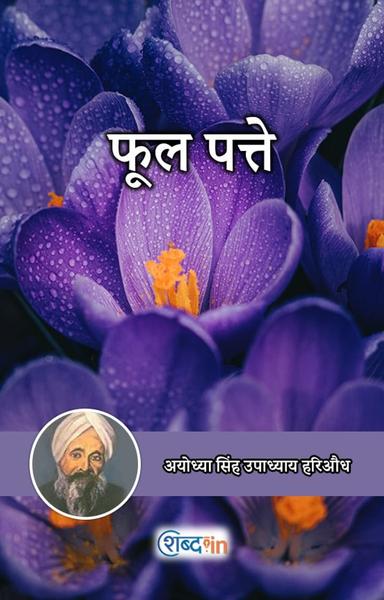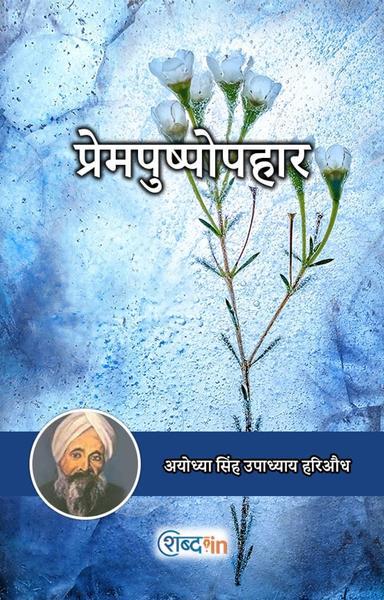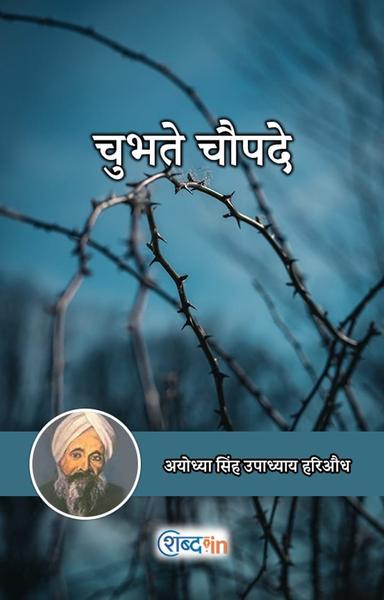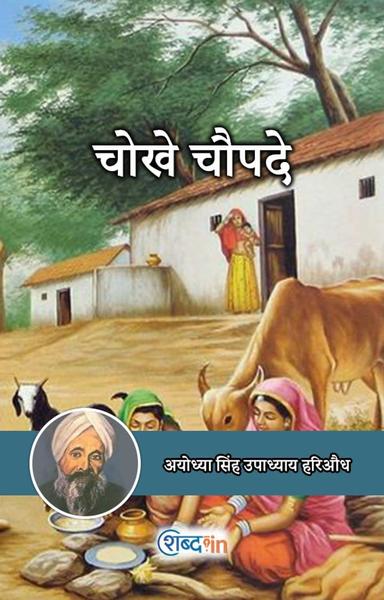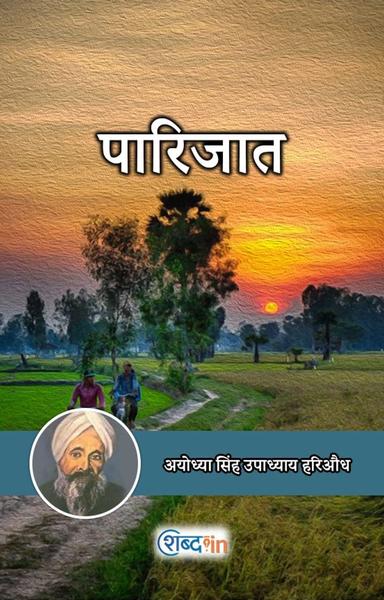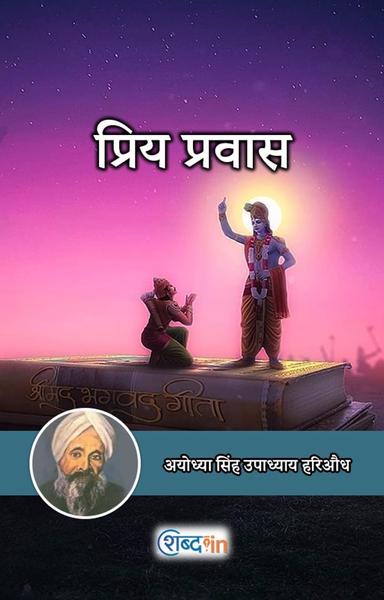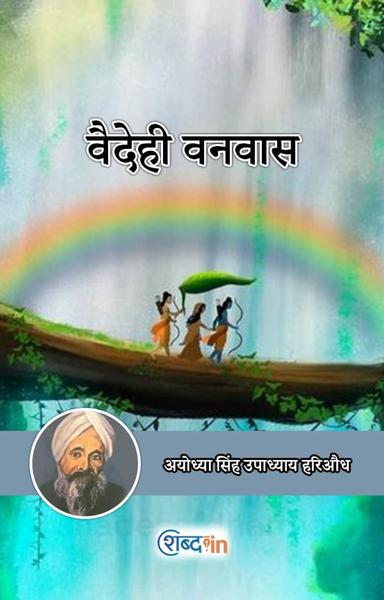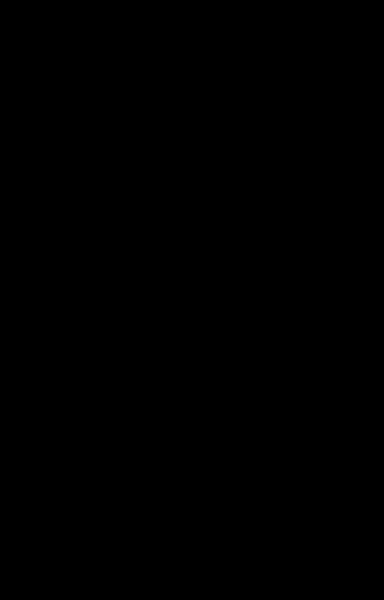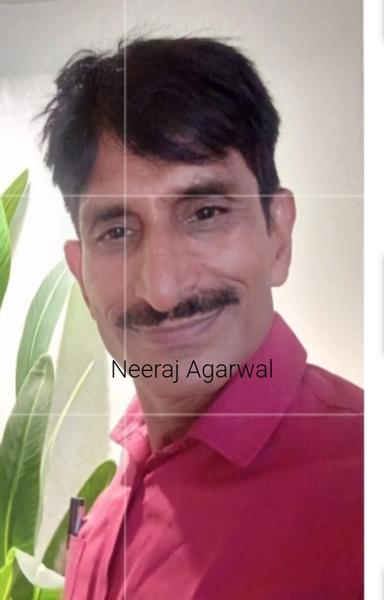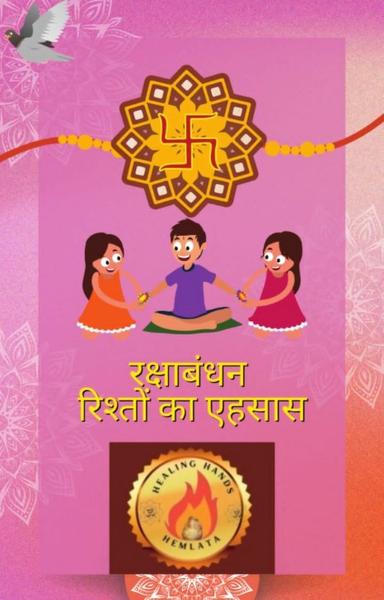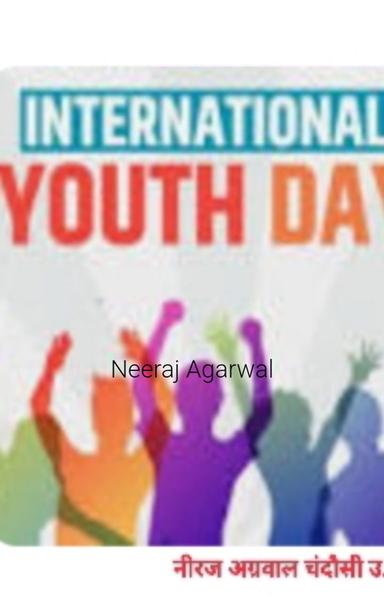महर्षिकल्प, महामना, परमपूज्य कुलपति
श्रीमान् पंडित मदनमोहन मालवीय
के पवित्र करकमलों में सादर समर्पित
वक्तव्य
करुणरस
करुणरस द्रवीभूत हृदय का वह सरस-प्रवाह है, जिससे सहृदयता क्यारी सिंचित, मानवता फुलवारी विकसित और लोकहित का हरा-भरा उद्यान सुसज्जित होता है। उसमें दयालुता प्रतिफलित दृष्टिगत होती है, और भावुकता-विभूति-भरित। इसीलिए भावुक-प्रवर-भवभूति की भावमयी लेखनी यह लिख जाती है-
एको रस: करुण एव निमित्त भेदाद्।
भिन्न: पृथक् पृथिगिवाश्रयते विवर्तान्॥
आवर्तबुद्बुदतरंग मयान् विकारान्।
अम्भो यथा सलिलमेवहि तत् समस्तम्॥
एक करुणरस ही निमित्त भेद से शृंगारादि रसों के रूप में पृथक्-पृथक् प्रतीत होता है। शृंगारादि रस करुणरस के ही विवर्त्त हैं, जैसे भँवर, बुलबुले और तरंग जल के ही विकार हैं। वास्तव में ए सब जल ही हैं, केवल नाम मात्र की भिन्नता है। ऐसा ही सम्बन्ध करुणरस और शृंगारादि रसों का है।
सम्भव है यह विचार सर्व-सम्मत न हो, उक्त उक्ति में अत्युक्ति दिखलाई पड़े, किन्तु करुणरस की सत्ता की व्यापकता और महत्ता निर्विवाद है। रसों में श्रृंगाररस और वीररस को प्रधानता दी गयी है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। उसके दो अंश हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार अथवा विप्रलम्भ श्रृंगार/वियोग श्रृंगार में रति की ही प्रधानता है, अतएव प्राधन्य उसी को दिया गया है। दूसरी बात यह कि आचार्य भरत का यह कथन है-
यत्किझिल्लोके शुचि मेधयमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तत्सर्वं शृंगारेणोपमीयते (उपयुज्यते च)।
लोक में जो कुछ मेध्य, उज्ज्वल और दर्शनीय है, उन सबका वर्णन श्रृंगाररस के अन्तर्गत है।
श्रीमान् विद्या वाचस्पति पण्डित शालिग्राम शास्त्री इसकी यह व्याख्या करते हैं-
छओ ऋतुओं का वर्णन, सूर्य और चन्द्रमा का वर्णन, उदय और अस्त, जलविहार, वन-विहार, प्रभात, रात्रि-क्रीड़ा, चन्दनादि लेपन, भूषण धारण तथा जो कुछ स्वच्छ, उज्ज्वल वस्तु हैं, उन सबका वर्णन श्रृंगार रस में होता है।
ऐसी अवस्था में श्रृंगार रस की रसराजता अप्रकट नहीं, परन्तु साथ ही यह भी कहा गया है-
'न बिना विप्रलम्भेन संभोग: पुष्टिमश्नुते'।
'बिना वियोग के सम्भोग श्रृंगार परिपुष्ट नहीं हो पाता'।
'यत्र तु रति: प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ'।
'जहाँ अनुराग तो अति उत्कट है, परन्तु प्रिय समागम नहीं होता उसे विप्रलम्भ कहते हैं।'
'स च पूर्वराग मान प्रवास करुणात्मकश्नतुर्धा स्यात्'।
'वह विप्रलम्भ 1. पूर्वराग, 2. मान, 3. प्रवास और 4. करुण-इन भेदों से चार प्रकार का होता है'।
इन पंक्तियों के पढ़ने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रृंगार रस पर करुण रस का कितना अधिकार है और वह उसमें कितना व्याप्त है। यह कहना कि बिना विप्रलम्भ के संभोग की पुष्टि नहीं होती, यथार्थ है और अक्षरश: सत्य है। प्रज्ञाचक्षु श्रृंगार साहित्य के प्रधान आचार्य श्रीयुत् सूरदासजी की लेखनी ने श्रृंगार रस लिखने में जो कमाल दिखलाया है, जो रस की सरिता बहाई है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, थोड़ी है। किन्तु संभोग श्रृंगार से विप्रलम्भ श्रृंगार लिखने में ही उनकी प्रतिभा ने अपनी हृदय-ग्राहिणी-शक्ति का विशेष परिचय दिया है। उध्दव सन्देश सम्बन्धिनी कविताएँ, श्रीमती राधिका और गोपबालाओं के कथनोपकथन से सम्पर्क रखनेवाली मार्मिक रचनाएँ, कितनी प्रभावमयी और सरस हैं, कितनी भावुकतामयी और मर्मस्पर्शिनी हैं। उनमें कितनी मिठास, कितना रस, कैसी अलौकिक व्यंजना और कैसा सुधास्रवण है, इसको सहृदय पाठक ही समझ सकता है। वास्तव बात यह है कि सूरसागर के अनूठे रत्न इन्हीं पंक्तियों में भरे पड़े हैं। नवरस सिध्द महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के कोटिश: जन-पूजित रामचरितमानस में जहाँ-जहाँ उनकी हृत्तांत्री के तार विप्रलम्भ कर से झङ्कृत हुए हैं, वहाँ-वहाँ की अवधी भाषा का हृदय-द्रावक राग कितना रस-वर्षणकारी और विमुग्धकर है, कितना रोचक, तल्लीनतामय और भावुकजन विमोहक है, उसको बतलाने में जड़ लेखनी असमर्थ है। रामचरितमानस के वे अंश जो अन्तस्तल में रस की धरा बहा देते हैं, जिनमें उच्च कोटि का कवि-कर्म पाया जाता है, जिनकी व्यंजना में भाव-व्यंजना की पराकाष्ठा होती है, उसके विप्रलम्भ श्रृंगार सम्बन्धी अंश भी वैसे ही हैं। मलिक मुहम्मद जायसी का 'पद्मावत' भी हिन्दी-साहित्य का एक उल्लेखनीय ग्रन्थ है, उसमें भी पद्मावती का पूर्वानुराग और नागमती का विरह-वर्णन ही अधिकतर हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी है। प्रज्ञाचक्षु सूरदास और महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जैसे महाकवि हिन्दी-संसार में अब तक उत्पन्न नहीं हुए। इन महानुभावों की लेखनी में अलौकिक और असाधारण क्षमता थी। इन लोगों की लेखन-कला से विप्रलम्भ श्रृंगार को जो गौरव प्राप्त हुआ है, उससे सिध्द है कि श्रृंगार रस पर विप्रलम्भ श्रृंगार का कितना अधिकार है। श्रृंगार रस के बाद वीर रस को ही प्रधानता दी जाती है, किन्तु इस रस में भी करुण रस की विभूतियाँ दृष्टिगत होती हैं। वीर रस की इतिश्री युध्द-वीर और धर्म-वीर में ही नहीं हो जाती, उसके अंग दया-वीर और दान-वीर भी हैं, जो अधिकतर करुणार्द-हृदय द्वारा संचालित होते रहते हैं। श्मशान का कारुणिक-दृश्य निर्वेद का ही सृजन नहीं करता है, भयानक और बीभत्स रस का प्रभाव भी हृदय पर डालता है। वसुंधरा के पाप-भार से पीड़ित होने पर किसी विभूतिमत् सत्तव का धरा में अवतीर्ण होना क्या करुण रस का आह्वान नहीं है? क्या ग्राह से गज-मोक्ष सम्बन्धिनी क्रिया में कारुणिकता नहीं पाई जाती और क्या यह अद्भुत रस के कार्य-कलाप का निदर्शन नहीं है? कान्त-कवितावली के आचार्य जयदेवजी ने जिन बुध्ददेव को 'कारुण्यमातन्वते' वाक्य द्वारा स्मरण किया है, उनका वसुंधरा की एक तृतीयांश जनता के हृदय पर केवल करुणा के बल से अधिकार कर लेना क्या अतीव-अद्भुत कार्य नहीं है? एक बहुत बड़ा सम्राट भी आज तक इतनी बड़ी जनता पर अस्त्र शस्त्र अथवा पराक्रम बल से अधिकार नहीं कर सका। अतएव बुध्ददेव के कारुणिक-कार्य-कलाप में अद्भुत रस का कैसा समावेश है, इसको प्रत्येक सहृदय व्यक्ति समझ सकता है। रही रौद्र रस की बात, उसके विषय में यह कहना है कि क्या उपहास-मूलक हास्य उस रौद्र-भाव का सृजनकर्त्ता नहीं है, जिसकी संचालिका कारुणिक खिन्नता होती है। आतताइयों, अत्याचारियों, देश जाति के द्रोहियों, लोकहित-कंटकों की विपन्न दशा क्या मानवता के अनुरागियों, संसार के शान्ति सुख के कामुकों और लोकोपकार निरतों को हर्षित नहीं करती, और क्या उनके उत्फुल्ल आननों पर स्मित की रेखा नहीं खींचती, और क्या यह करुण रस का विकास हास्य-रस में नहीं है? अब तक जो कुछ कहा गया उससे भवभूति प्रतिभा प्रसूत श्लोक की वास्तवता मान्य और करुण रस की महनीय महत्ता पूर्णतया स्वीकृत हो जाती है।
यह विचार-परम्परा भी करुण रस को विशेष गौरवित बनाती है, कि कविता का आरम्भ पहले पहल इसी रस के द्वारा हुआ है। कवि-कुल-गुरु कालिदास लिखते हैं-
'निषादविध्दाण्डजदर्शनोत्थ: श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोक:।
निषाद के बाण से बिध्द पक्षी के दर्शन से जिसका (महर्षि वाल्मीक का) शोक श्लोक में परिणत हो गया। वह श्लोक यह है-
मा निषाद प्रतिष्ठात्वमगम: शाश्वती: समा।
यत्क्रौंच मिथुनादेकमबधी: काममोहितम्॥
हे निषाद! तू किसी काल में प्रतिष्ठा न पा सकेगा। तू ने व्यर्थ काममोहित दो क्रौंचों में से एक को मार डाला।
वाल्मीकि-रामायण में लिखा है कि यही पहला आदिम पद्य है, जिसके आधार से उसकी रचना हुई। वाल्मीकि रामायण ही संस्कृत का पहला पद्य-ग्रंथ है। और उसका आधार करुण रस का उक्त श्लोक ही है। अतएव यह माना जाता है कि कविता का आरम्भ करुण रस से ही हुआ है। आश्चर्य यह है कि फारसी के एक पद्य से भी इस विचार का प्रतिपादन होता है। वह पद्य यह है-
आंकि अव्वल शेरगुफ्त आदम शफीअल्ला बुवद।
तबा मौजूं हुज्जतेफरजंदिए आदम बुवद॥
जिसने पहले पहल शेर कहा वह परमेश्वर का प्यारा आदम था। इसलिए 'आदमी, का मौजतबा (कवि) होना 'आदम' की संतान होने की दलील है।
बाबा आदम के एक लड़के का नाम 'हाबील' था और दूसरे का नाम 'काबील'। दूसरे ने पहले को जान से मार डाला। इस दुर्घटना पर बाबा आदम के शोक संतप्त हृदय से अनायास जो उद्गार निकला, वही करुण वाक्य कविता का आदि प्रवर्तक बना। उक्त शेर का यही मर्म है। हमारे मनु ही मुसलमान और ईसाइयों के 'आदम', हैं। 'मनुज' और 'आदमी' पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे हम लोग मनु भगवान को आदिम पुरुष मानते हैं, वैसे ही वे लोग 'बाबा आदम' को आदिम पुरुष कहते हैं। आदिम शब्द और आदम शब्द में नाम मात्र का अन्तर है। फारसी ईरान की भाषा है। ईरानी एरियन वंश के ही हैं। ईरानियों के पवित्र ग्रंथ जिन्दावस्ता में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। इसलिए इस प्रकार का विचार-साम्य असम्भव नहीं है। भाषा के साथ भाव-ग्रहण अस्वाभाविक व्यापार नहीं है।
पद्य-प्रणाली का जो जनक है, वाल्मीकि-रामायण जैसे लोकोत्तर महाकाव्य की रचना का जो आधार है, उस करुण रस की महत्ता की इयत्ता अविदित नहीं। तो भी संस्कृत श्लोक के भाव का प्रतिपादन एक अन्यदेशीय प्राचीन भाषा द्वारा हो जाने से इस विचार की पुष्टि पूर्णतया हो जाती है कि करुण रस द्वारा ही पहले पहल कविता देवी का आविर्भाव मानव-हृदय में हुआ है। और यह एक सत्य का अद्भुत विकास है।
करुण रस की विशेषताओं और उसकी मर्मस्पर्शिता की ओर मेरा चित्त सदा आकर्षित रहा, इसका ही परिणाम 'प्रिय-प्रवास' का आविर्भाव है। 'प्रिय-प्रवास' की रचना के उपरान्त मेरी इच्छा 'वैदेही-वनवास' प्रणयन की हुई। उसकी भूमिका में मैंने यह बात लिख भी दी थी। परन्तु चौबीस वर्ष तक मैं हिन्दी-देवी की यह सेवा न कर सका। कामना-कलिका इतने दिनों के बाद ही विकसित हुई। कारण यह था कि उन दिनों कुछ ऐसे विचार सामने आए, जिनसे मेरी प्रवृत्ति दूसरे विषयों में ही लग गई। उन दिनों आजमगढ़ में मुशायरों की धूम थी। बन्दोबस्त वहाँ हो रहा था। अहलकारों की भरमार थी। उनका अधिकांश उर्दू-प्रेमी था। प्राय: हिन्दी भाषा पर आवाज कसा जाता, उसकी खिल्ली उड़ाई जाती, कहा जाता हिन्दी-वालों को बोलचाल की फड़कती भाषा लिखना ही नहीं आता। वे मुहावरे लिख ही नहीं सकते। इन बातों से मेरा हृदय चोट खाता था, कभी-कभी मैं तिलमिला उठता था। उर्दू-संसार के एक प्रतिष्ठित मौलवी साहब जो मेरे मित्र थे और आजमगढ़ के ही रहने वाले थे, जब मिलते, इस विषय में हिन्दी की कुत्सा करते, व्यंग्य बोलते। अतएव मेरी सहिष्णुता की भी हद हो गई। मैंने बोलचाल की मुहावरेदार भाषा में हिन्दी-कविता करने के लिए कमर कसी। इसमें पाँच-सात बरस लग गये और 'बोल-चाल' एवं 'चुभते चौपदे' और 'चोखे चौपदे' नामक ग्रंथों की रचना मैंने की। जब इधर से छुट्टी हुई, मेरा जी फिर 'वैहेदी-वनवास' की ओर गया। परन्तु इस समय एक दूसरी धुन सिर पर सवार हो गई। इन दिनों मैं काशी विश्वविद्यालय में पहुँचा गया था। शिक्षा के समय योग्य विद्यार्थी-'समुदाय' ईश्वर अथच संसार-सम्बन्धी अनेक विषय उपस्थित करता रहता था। उनमें कितने श्रध्दालु होते, कितने सामयिकता के रंग में रँगे शास्त्रीय और पौराणिक विषयों पर तरह-तरह के तर्क-वितर्क करते। मैं कक्षा में तो यथाशक्ति जो उत्तर उचित समझता, दे देता। परन्तु इस संघर्ष से मेरे हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इन विषयों पर कोई पद्य-ग्रंथ क्यों न लिख दिया जाए। निदान इस विचार को मैंने कार्य में परिणत किया और सामयिकता पर दृष्टि रखकर मैंने एक विशाल-ग्रंथ लिखा। परन्तु इस ग्रंथ के लिखने में एक युग से भी अधिक समय लग गया। मैंने इस ग्रंथ का नाम 'पारिजात' रखा। इसके उपरान्त 'वैहेदी-वनवास' की ओर फिर दृष्टि फिरी। परमात्मा के अनुग्रह से इस कार्य की भी पूर्ति हुई। आज 'वैदेही-वनवास' लिखा जाकर सहृदय विद्वज्जनों और हिन्दी-संसार के सामने उपस्थित है। (महाराज रामचन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम, लोकोत्तर-चरित और आदर्श नरेन्द्र अथच महिपाल हैं, श्रीमती जनक-नन्दिनी सती-शिरोमणि और लोक-पूज्या आर्य-बाला हैं। इनका आदर्श, आर्य-संस्कृति का सर्वस्व है, मानवता की महनीय विभूति है, और है स्वर्गीय-सम्पत्ति-सम्पन्न।) इसलिए इस ग्रंथ में इसी रूप में इसका निरूपण हुआ है। सामयिकता पर दृष्टि रखकर इस ग्रंथ की रचना हुई है, अतएव इसे बोधगम्य और बुध्दिसंगत बनाने की चेष्टा की गयी है। इसमें असम्भव घटनाओं और व्यापारों का वर्णन नहीं मिलेगा। मनुष्य अल्पज्ञ है, उसकी बुध्दि और प्रतिभा ही क्या? उसका विवेक ही क्या? उसकी सूझ ही कितनी, फिर मुझ ऐसे विद्या-विहीन और अल्पमति की। अतएव प्रार्थना है कि मेरी भ्रान्तियों और दोषों पर दृष्टिपात न कर विद्वज्जन अथच महज्जन गुण-ग्रहण की ही चेष्टा करेंगे। यदि कोई उचित सम्मति दी जाएगी तो वह शिरसाधार्य होगी।
कवि-कर्म
कवि-कर्म कठिन है, उसमें पग-पग पर जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। पहले तो छन्द की गति स्वच्छन्द बनने नहीं देती, दूसरे मात्रओं और वर्णों की समस्या भी दुरूहता-रहित नहीं होती। यदि कोमल-पद-विन्यास की कामना चिन्तित करती रहती है, तो प्रसाद-गुण की विभूति भी अल्प वांछित नहीं होती। अनुप्रास का कामुक कौन नहीं, अन्त्यानुप्रास के झमेले तो कितने शब्दों का अंग भंग तक कर देते हैं या उनके पीछे एक पूँछ लगा देते हैं। सुन्दर और उपयुक्त शब्द-योजना कविता की विशेष विभूति है, इसके लिए कवि को अधिक सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि कविता को वास्तविक कविता वही बनाती है। कभी-कभी तो एक उपयुक्त और सुन्दर शब्द के लिए कविता का प्रवाह घण्टों रुक जाता है। फारसी का एक शायर कहता है-
बराय पाकिले लफजे शबे बरोज आरन्द।
कि मुर्ग माहीओ बाशन्द ख़ुफता ऊ बेदार॥
'एक सुन्दर शब्द बैठाने की खोज में कवि उस रात को जागकर दिन में परिणत कर देता है, जिसमें पक्षी से मछली तब बेखबर पड़े सोते रहते हैं'-
इस कथन में बड़ी मार्मिकता है। उपयुक्त और सुन्दर शब्द कविता के भावों की व्यंजना के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एक उपयुक्त शब्द कविता को सजीव कर देता है और अनुपयुक्त शब्द मयंक का कलंक बन जाता है। शब्द का कविता में वास्तविक रूप में आना ही उत्तम समझा जाता है। उसका तोड़ना-मरोड़ना ठीक नहीं माना जाता। यह दोष कहा गया है, किन्तु देखा जाता है कि इस दोष से बड़े-बड़े कवि भी नहीं बच पाते। इसीलिए यह कहा जाता है, 'निरंकुशा: कवय:' कौन कवि निरंकुश कहलाना चाहेगा, परन्तु कवि-कर्म की दुरूहता ही उसको ऐसा कहलाने के लिए बाध्य करती है। आजकल हिन्दी-संसार में निरंकुशता का राज्य है। ब्रज-भाषा की कविता में शब्द-विन्यास की स्वच्छन्दता देखकर खड़ी बोली के सत्कवियों ने इस विषय में बड़ी सतर्कता ग्रहण की थी, किन्तु आजकल उसका प्राय: अभाव देखा जाता है। इसका कारण कवि-कर्म की दुरूहता अवश्य है। किन्तु कठिन अवसरों और जटिल स्थलों पर ही तो सावधानता और कार्य-दक्षता की आवश्यकता होती है। हीरा जी तोड़ परिश्रम करके ही खनि से निकाला जाता है। और चोटी का पसीना एड़ी तक पहुँचा कर ही ऊसरों में भी सुस्वादु तोय पाया जा सकता है।
खड़ी बोली की विशेषतायें
इस समय खड़ी बोली की कविता में शब्द-विन्यास का जो स्वातन्त्रय फैला हुआ है, उसके विषय में विशेष लिखने के लिए मेरे पास स्थान का संकोच है। मैं केवल 'वैदेही-वनवास' के प्रयोगों पर ही अर्थात् उसके कुछ शब्द-विन्यास की प्रणाली पर ही प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसलिए कि हिन्दी-भाषा के गण्यमान्य विद्वानों की उचित सम्मति सुनने का अवसर मुझको मिल सके। मैं यह जानता हूँ कि कितने प्रयोग वाद-ग्रस्त हैं, मुझे यह भी ज्ञान है कि मत-भिन्नता स्वाभाविक है, किन्तु यह भी विदित है 'वादे' 'वादे' जायते तत्तव बोध:।
हिन्दी भाषा की कुछ विशेषतायें हैं, वह तद्भव शब्दों से बनी है, अतएव सरल और सीधी है। अधिक संयुक्ताक्षरों का प्रयोग उसमें वांछनीय नहीं, वह उनको भी अपने 'ढंग में ढालती रहती है। वह राष्ट्र-भाषा-पद पर आरूढ़ होने की अधिकारिणी है, इसलिए ठेठ प्रान्तीय-शब्दों का अथवा ग्राम्य-शब्दों का प्रयोग उसमें अच्छा नहीं समझा जाता। ब्रज-भाषा अथवा अवधी शब्दों का व्यवहार गद्य में कदापि नहीं किया जाता। परन्तु पद्य में कवि-कर्म की दुरूहताओं के कारण यदि कभी कोई उपयुक्त शब्द खड़ी बोलचाल की कविता में ग्रहण कर लिया जाता है, तो वह उतना आपत्तिजनक नहीं माना जाता, किन्तु क्रियाएँ उनकी कभी पसन्द नहीं की जातीं। कुछ सम्मति उपयुक्त शब्द-ग्रहण की भी विरोधिनी है, परन्तु यह अविवेक है। यदि अत्यन्त प्रचलित विदेशी शब्द ग्राह्य हैं, तो उपयुक्त सुन्दर ब्रज-भाषा और अवधी के शब्द आग्राह्य क्यों? वह भी पद्य में, और माधुर्य उत्पादन के लिए। बहुत से प्रचलित विदेशी शब्द हिन्दी-भाषा के अंग बन गये हैं, इसलिए उसमें उनका प्रयोग निस्संकोच होता है। वह अवसर पर अब भी प्रत्येक विदेशीय भाषा के उन शब्दों को ग्रहण करती रहती है, जिन्हें उपयोगी और आवश्यक समझती है, इसी प्रकार प्रान्त-विशेष के शब्दों को भी। किन्तु व्यापक संस्कृत-शब्दावली ही उसका सर्वस्व है और इसी से उसका समुन्नति-पथ भी विस्तृत होता जा रहा है।
हिन्दी-भाषा की विशेषताओं का ध्यान रखकर ही उसके गद्य-पद्य का निर्माण होना चाहिए। जब तद्भव शब्द ही उसके जनक हैं, तो उसमें उसका आधिक्य स्वाभाविक है। अतएव जब तक हम ऑंख, कान, नाक, मुँह लिख सकते हैं, तब तक हमें अक्ष, कर्ण, नासिका, और मुख लिखने का अनुरक्त न होना चाहिए, विशेषकर मुहावरों में। मुहावरे तद्भव शब्दों से ही बने हैं। अतएव उनमें परिवर्तन करना भाषा पर अत्याचार करना होगा। ऑंख चुराना, कान भरना, नाक फुलाना और मुँह चिढ़ाना के स्थान पर अक्ष चुराना, कर्ण भरना, नासिका फुलाना और मुख चिढ़ाना हम लिख सकते हैं, किन्तु यह भाषाभिज्ञता की न्यूनता होगी। कुछ लोगों का विचार है कि खड़ी बोली के गद्य और पद्य दोनों में शुध्द संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, जिससे उसमें नियम-बध्दता रहे। वे कहते हैं, चित के स्थान पर चित्त, सिर के स्थान पर शिर और दुख के स्थान पर दु:ख ही लिखा जाना चाहिए। किन्तु वे नहीं समझते कि इससे तो हिन्दी के मूल पर ही कुठाराघात होगा। तद्भव शब्द जो उसके आधार हैं, निकल जावेंगे और संस्कृत-शब्द ही अर्थात् तत्सम शब्द ही उसमें भर जाएँगे, जो दुरूहता और असुविधा के जनक होंगे और मुहावरों को मटियामेट कर देंगे। तद्भव शब्दों को तो सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, हाँ अर्ध्द तत्सम शब्दों के स्थान पर अवश्य तत्सम शब्द ही रखना समुचित होगा। तद्भव शब्द चिरकालिक परिवर्तन के परिणाम और बोलचाल के शब्दों के आधार हैं, इसलिए उनका त्याग तो हो ही नहीं सकता। 'कर्म' शब्द बोलचाल के प्रवाह में पड़कर पहले कम्म बना (पंजाब में अब भी 'कम्म' बोला जाता है)। यही 'कम्म' इस प्रान्त में अब काम बोला जाता है। उसको हटाकर उसकी जगह पर फिर कर्म को स्थान देना वास्तवता का निराकरण करना होगा, हाँ गद्य-पद्य लिखने में यथावसर आवश्यकतानुसार दोनों का व्यवहार किया जा सकता है, यही प्रणाली प्रचलित भी है। यही बात सब तद्भव शब्दों के लिए कही जा सकती है। रही अर्ध्द तत्सम की बात। प्राय: ऐसे शब्द ब्रज-भाषा और अवधी-भाषा के कवियों के गढ़े हुए हैं, वे बोलचाल में कभी नहीं आये, कविता ही में उनके व्यवहार उन भाषाओं के नियमानुसार उस रूप में होते आये हैं, अतएव उनको तत्सम रूप में व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। कत्तर्र, हृदय, निर्दय का प्रयोग आज भी सर्वसाधारण में नहीं है, पहले भी नहीं था, परन्तु उन भाषाओं की कविताओं में इनका प्रयोग करतार, हिरदय, निरदय के रूप में पाया जाता है, इसलिए इनका प्रयोग खड़ी बोली की कविता में शुध्द रूप में होना ही चाहिए, ऐसा ही होता भी है।
संयुक्ताक्षरों की दुरूहता निवारण और उनकी लिपि-प्रणाली को सुगम बनाने के लिए धर्म्म, मर्म, कर्म्म को धर्म, मर्म, कर्म लिखा जाने लगा है। इसी प्रकार गर्त, आवर्त, कैवर्त आदि को गर्त, आवर्त, कैवर्त। बात यह है कि जब वर्ण के द्वित्व का उपयोग नहीं होता, एक वर्ण के समान ही वह काम देता है तब उसको दो क्यों लिखा जाए। उत्पत्ति में 'त्ति' के द्वित्व का उच्चारण होता है, इसी प्रकार सम्मति में म्म का, इसलिए उनमें उनका उस रूप में लिखा जाना आवश्यक है, अन्यथा शब्द का उच्चारण ही ठीक न होगा। किन्तु उक्त शब्दों में यह बात नहीं है, अतएव उनमें द्वित्व की आवश्यकता नहीं ज्ञात होती। इसलिए प्राय: हिन्दी में अब उनको उस रूप में लिखा जाने भी लगा है। संस्कृत के नियमानुसार भी ऐसा लिखना स-दोष नहीं है। मुनिवर पाणिनि का यह सूत्र इसका प्रमाण है। 'अचोरहाभ्यां द्वे' इसी प्रकार पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार से काम लेना भी आरम्भ हो गया है। कल(, कद्बचन, मण्डन, बन्धन और दम्पती को प्राय: लोग कलंक, कंचन, मंडन, बंधन और दंपती लिखते हैं। बहुत लोग इस प्रणाली को पसन्द नहीं करते, संस्कृत रूप में ही उक्त शब्दों का लिखना अच्छा समझते हैं। यह अपनी-अपनी रुचि और सुविधा की बात है। कथन तो यह है कि उक्त द्वित्व वर्ण और पंचम वर्ण के प्रयोग में जो परिवर्तन हो रहा है, वह आपत्ति-मूलक नहीं माना जा रहा है। इसलिए जो चाहे जिस रूप में उन शब्दों को लिख सकता है। खड़ी बोली के गद्य-पद्य दोनों में यह प्रणाली गृहीत है, अधिकतर पद्य में। श्रुतबोधकार लिखते हैं-
संयुक्ताद्यं दीर्घ सानुस्वारं विसर्ग संमिश्रं।
विज्ञेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन॥
संयुक्त अक्षर के पहले का दीर्घ, सानुस्वार, विसर्ग संयुक्त अक्षर गुरु माना जाएगा, विकल्प से पादान्तस्थ अक्षर भी गुरु कहलाता है।
इस नियम से संयुक्त अक्षर के पहले का अक्षर सदा गुरु अथवा दीर्घ माना जावेगा। प्रश्न यह है कि क्या हिन्दी में भी यह व्यवस्था सर्वथा स्वीकृत होगी? हिन्दी में यह विषय वादग्रस्त है। रामप्रसाद को रामप्प्रसाद नहीं कहा जाता, मुख क्रोध से लाल हो गया को मुखक्क्रोध से लाल हो गया नहीं पढ़ा जाएगा। पवित्र प्रयाग को न तो पवित्रप्प्रयाग कहा जाएगा, न कार्य क्षेत्र को कार्यच्क्षेत्र पढ़ा जाएगा। संस्कृत का विद्वान् भले ही ऐसा कह ले अथवा पढ़ ले, परन्तु सर्वसाधारण अथवा हिन्दी या अन्य भाषा का विद्वान् न तो ऐसा कह सकेगा, न पढ़ सकेगा। वह तो वही कहेगा और पढ़ेगा, जो लिखित अक्षरों के आधार से पढ़ा जा सकता है या कहा जा सकता है। संस्कृत का विद्वान भी न तो गोविन्दप्रसाद को गोविन्दप्प्रसाद कहेगा न शिवप्रसाद को शिवप्प्रसाद, क्योंकि सर्वसाधारण के उच्चारण का न तो वह अपलाप कर सकता है, न बोलचाल की भाषा से अनभिज्ञ बनकर उपहास-भाजन बन सकता है। अवधी और ब्रज-भाषा में इस प्रकार का प्रयोग मिलता ही नहीं, क्योंकि वे बोलचाल के रंग में ढली हुई हैं। 'प्रभु तुम कहाँ न प्रभुता करी, के 'न' को दीर्घ बना देंगे तो छन्दो-भंग हो जाएगा। हिन्दी-भाषा की प्रकृति पर यदि विचार करेंगे और लिपि-प्रणाली की यदि रक्षा करेंगे, यदि यह चाहेंगे कि जो लिखा है वही पढ़ा जावे, थोड़ी विद्या-बुध्दि का मनुष्य भी जिस वाक्य को जिस प्रकार पढ़ता है, उसका उच्चारण उसी प्रकार होता रहे तो संयुक्त वर्ण के पहले के अक्षर को हिन्दी में दीर्घ पढ़ने की प्रणाली गृहीत नहीं हो सकती, उसमें एक प्रकार की दुरूहता है। अधिकांश हिन्दी के विद्वानों की यही सम्मति है। परन्तु हिन्दी के कुछ विद्वान् उक्त प्रणाली के पक्षपाती हैं और अपनी रचनाओं में उसकी रक्षा पूर्णतया करते हैं। संयुक्ताक्षर के पहले का अक्षर स्वभावत: दीर्घ हो जाता है जैसे-गल्प, अल्प, उत्तर, विप्र, देवस्थान, शुभ्र, सुन्दर, गर्व, पर्व, किझित, महत्तम, मुद.र आदि। ऐसे शब्दों के विषय में कोई तर्क-वितर्क नहीं है, गद्य-पद्य दोनों में इनका प्रयोग सुविधा के साथ हो सकता है और होता भी है। परन्तु कुछ समस्त शब्दों में ही झगड़ा पड़ता है और वाद उन्हीं के विषय में है। ऐसे शब्द देवव्रत, धर्म्मच्युति, गर्वप्रहरी, सुकृति-स्वरूपा आदि हैं। संस्कृत में उनका उच्चारण देवव्व्रत, धर्मच्चयुति, गर्वप्प्रहारी और सुकृति-स्स्वरूपा होगा। संस्कृत के पण्डित भाषा में भी इनका उच्चारण इसी प्रकार करेंगे। परन्तु हिन्दी-भाषा भिज्ञ इनका उच्चारण उसी रूप में करेंगे जिस रूप में वे लिखे हुए हैं। अब तक यह विषय वादग्रस्त है। गद्य में तो संयुक्त शब्दों के पहले के अक्षर को दीर्घ बनाने में कोई अन्तर न पड़ेगा, किन्तु पद्य में विशेष कर मात्रिक-छन्दों में उसके दीर्घ उच्चारण करने में छन्दो-भंग होगा, यदि पद्यकर्त्ता ने उसको दीर्घ मानकर ही उसका प्रयोग नहीं किया है। परन्तु केवल भाषा का ज्ञान रखनेवाला ऐसा न कर सकेगा; हाँ, संस्कृतज्ञ ऐसा कर सकेगा। किन्तु हिन्दी कविता करनेवालों में संस्कृतज्ञ इने- गिने ही हैं। इसीलिए इस प्रकार के प्रयोग के विरोधी ही अधिक हैं, और अधिक सम्मति उन्हीं के पक्ष में है। मेरा विचार यह है कि विकल्प से यदि इस प्रयोग को मान लिया जावे तो वह उपयोगी होगा। जहाँ छन्दोगति बिगड़ती हो वहाँ समास न किया जावे, और जहाँ छन्दोगति को सहायता मिलती हो वहाँ समास कर दिया जावे। प्राय: ऐसा ही किया भी जाता है। परन्तु समास न करनेवालों की ही संख्या अधिक है, क्योंकि सुविधा इसी में है।
वज्र-भाषा और अवधी का यह नियम है-
'लघु गुरु गुरु लघु होत है निज इच्छा अनुसार।
गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे समर्थ महाकवि भी लिखते हैं-
बन्दों गुरु पद पदुम परागा। सरस सुवास सुरुचि अनुरागा॥
अमिय मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भवरुज परिवारू॥
पराग को परागा, अनुराग को अनुरागा, चारु को चारू और परिवार को पारिवारू कर दिया गया है।
प्रज्ञाचक्षु सूरदासजी लिखते हैं-
जसुदा हरि पालने झुलावै।
दुलरावै हलराइ मल्हावै जोई सोई कछु गावै।
मेरे लाल को आउ निंदरिया काहे न आनि सोआवै॥
जसोदा को जसुदा, जोई के 'जो' को सोई के 'सो' को और मेरे के 'मे' को लघु कर दिया गया है। गोस्वामी जी के पद्य में लघु को दीर्घ बनाया गया है।
उर्दू में तो शब्दों के तोड़ने-मरोड़ने की परवा ही नहीं की जाती। एक शे'र को देखिए-
कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश को।
यह ख़लिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता॥
जिन शब्दों के नीचे लकीर खिंची हुई हैं वे बेतरह तोड़े-मरोड़े गये हैं। लघु को गुरु बनाने तक तो ठिकाना था, पर उक्त शे'र में अक्षर तक उड़ गये हैं, शेर का असली रूप यह होगा-
कई मेर दिल स पूछे, तर तीर नीमकश को।
य खलिश कहाँ स होती ज जिगर क पार होता।
खड़ी बोली की कविता में न तो लघु को दीर्घ बनाया जाता है और न दीर्घ को लघु। उर्दू की कविता के समान उसमें शब्दों का संहार भी नहीं होता। परन्तु कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको उसने स्वीकार कर लिया है। 'अमृत' शब्द तीन मात्र का है, परन्तु कभी-कभी उसको लिखा जाता है। 'अमृत' ही, परन्तु पढ़ा जाता है 'अम्मृत'। बोलचाल में उसका उच्चारण इसी रूप में होता है। बहुत लोगों का यह विचार है कि 'मृ' संयुक्त वर्ण है इसलिए उसके आदि के अक्षर ('अ') का गुरु होना स्वाभाविक है। इसलिए दो 'म' अमृत में नहीं लिखा जाता। परन्तु 'ऋ' युक्त वर्ण संयुक्त वर्ण नहीं माना जाता, इसलिए यह विचार ठीक नहीं है। परन्तु उच्चारण लोगों को भ्रम में डाल देता है। इसलिए उसका प्रयोग प्राय: अमृत के रूप में ही होता है। कभी-कभी छन्दो-गति की रक्षा के लिए 'अमृत' भी लिखा जाता है। संस्कृत का हलन्त वर्ण हिन्दी में विशेष कर कविता में प्राय: हलन्त नहीं लिखा दिखलाता, उसको सस्वर ही लिखते हैं। 'विद्वान' को इसी रूप में लिखेंगे, इसके 'न' को हलन्त न करेंगे। इसमें सुविधा समझी जाती है। संस्कृत में वर्ण-वृत्त का प्रचार है, उसमें हलन्त वर्ण को गणना के समय वर्ण माना ही नहीं जाता-
'रामम् रामानुजम् सीताम् भरतम् भरतानुजम्।
सुग्रीवम् बालि सूनुम् च प्रणमामि पुन: पुन:॥
अनुष्टुप छन्द का एक-एक चरण आठ वर्ण का होता है। यदि इस पद्य में वर्णों की गणना करके देखें तो ज्ञात हो जाएगा कि सब हलन्त वर्ण गणना में नहीं आते। परन्तु मात्रिक छन्दों में वह लघु माना ही जावेगा, इसलिए उसे हलन्त न करने की प्रणाली चल पड़ी है। परन्तु यह प्रणाली भी वाद-ग्रस्त है। हिन्दी-लेखक प्रायश: पद्य में हलन्त न लिखने के पक्षपाती हैं, परन्तु संस्कृत के विद्वान् उसके लिखे जाने के पक्ष में हैं। व्रज-भाषा और अवधी में भी हलन्त वर्ण को सस्वर कर देते हैं, जैसे-मर्म को मरम, भ्रम को भरम, गर्व को गरब, पर्व को परब, आदि। हिन्दी में चंचल लड़की, दिव्य ज्योति, स्वच्छ सड़क, सरस बातें, सुन्दर कली, कहने और लिखने की प्रण्ली है। कुछ लोग समझते हैं कि इस प्रकार लिखना अशुध्द है। चंचला लड़की, दिव्या ज्योति, स्वच्छा सड़क, सरसा बातें और सुन्दरी कली लिखना शुध्द होगा। किन्तु यह अज्ञान है। संस्कृत-नियम से भी प्रथम प्रयोग शुध्द है। मुनिवर पाणिनि का निम्नलिखित सूत्र इसका प्रमाण है-
'पुंवत् कर्म्मधारय जातीय देशेषु'
दूसरी बात यह कि संस्कृत के सब नियम यथातथ्य हिन्दी में नहीं माने जाते, उनमें अन्तर होता ही रहता है। आत्मा, पवन, वायु संस्कृत में पुल्लिंग हैं, किन्तु हिन्दी में वे स्त्री-लिंग लिखे जाते हैं। भारतेन्दु जी जैसे हिन्दी भाषा के प्रगल्भ विद्वान् लिखते हैं-
'सन सन लगी सीरी पौन चलन,
सहृदयवर बिहारीलाल कहते हैं-
'तुमहूँ लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय'
कविवर वृन्द का यह कथन है-
बिना डुलाए ना मिलै ज्यों पंखा की पौन]
मैं पहले कह आया हूँ कि हिन्दी-भाषा की जो विशेषतायें हैं उन्हें सुरक्षित रखना होगा, वास्तवता यही है अन्यथा उसमें कोई नियम न रह जावेगा। समय परिवर्तनशील है, उसके साथ संस्कृति, भाषा, विचार, रहन-सहन, रंग-ढंग, वेश-भूषा आदि सब परिवत्तित होते हैं। परन्तु उसकी भी सीमा है और उसके भीतर भी नियम हैं। वैदिक-काल से अब तक भाषा में परिवर्त्तन होते आये हैं। संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत के उपरान्त अपभ्रंश; अपभ्रंश से हिन्दी का प्रादुर्भाव हुआ। एक संस्कृत से कितनी प्राकृत भाषाएँ बनीं और परस्पर उनमें कितना रूपान्तर हुआ, यह भी अविदित नहीं है। अन्य भाषाओं को छोड़ दीजिए, हिन्दी को ही गवेषणा-दृष्टि से देखिये तो उसके ही अनेक रूप दृष्टिगत होते हैं। शौरसेनी के अन्यतम रूप अवधी, व्रज-भाषा और खड़ी बोली हैं, किन्तु इन्हीं में कितना विभेद दिखलाता है। 'अवधी' जिसमें गोस्वामीजी का लोक-पूज्य रामचरितमानस सा लोकोत्तर ग्रंथ है, जायसी का मनोहर ग्रन्थ पद्मावत है, आज उतनी आदृत नहीं है। जो वज्र-भाषा अपने ही प्रान्त में नहीं, अन्य प्रान्तों में भी सम्मानित थी; पंजाब से बंगाल तक, राजस्थान से मध्य हिन्द तक जिसकी विजय-वैजयन्ती उड़ रही थी, जो प्रज्ञाचक्षु सूरदास की अलौकिक रचना ही से अलंकृत नहीं है, समादरणीय सन्तों और बड़े-बड़े कवियों अथवा महाकवियों की कृतियों से भी मालामाल है। पाँच सौ वर्ष से भी अधिक जिसकी विजय-दुंदुभी का निनाद होता रहा है, आज वह भी विशाल कविता क्षेत्र से उपेक्षित है, यहाँ तक कि खड़ी बोली कविता में उसके किसी शब्द का आ जाना भी अच्छा नहीं समझा जाता। इन दिनों कविता-क्षेत्र पर खड़ी बोली का साम्राज्य है और उसकी विशेषताओं की ओर इन दिनों सबकी दृष्टि है। हिन्दी-भाषा के अन्तर्गत व्रज-भाषा, अवधी, बिहारी, राजस्थानी, बुन्देलखण्डी और मध्य हिन्द की सभी प्रचलित बोलियाँ हैं। किन्तु इस समय प्रधानता खड़ी बोली की है। यथा काल जैसे शौरसेनी और व्रज-भाषा का प्रसार था, वैसा ही आज खड़ी बोली का बोल-बाला है। आज दिन कौन सा प्रान्त है, जहाँ खड़ी बोली का प्रसार और विस्तार नहीं। हिन्दी-भाषा के गद्य रूप में जिसका आधार खड़ी बोली है, भारतवर्ष के किस प्रधान नगर से साप्ताहिक और दैनिक पत्र नहीं निकलते। उसके पद्य-ग्रंथों का आदर भारत व्यापी है इसलिए खड़ी बोली आज दिन मँज गयी है और उसका रूप परिमार्जित हो गया है। व्रज-भाषा और अवधी आदि कुछ बोलियाँ अब भी समादरणीय हैं, अब भी उनमें सत्कविता करने वाले सज्जन हैं, विशेष कर व्रज-भाषा में। परन्तु उन पर अधिकतर प्रान्तीयता का रंग चढ़ा हुआ है। यदि इस समय भारत-व्यापिनी कोई भाषा है तो खड़ी बोली ही है। पचास वर्ष में वह जितनी समुन्नत हुई, उतनी उन्नति करते किसी भाषा को नहीं देखा गया। उर्दू के प्रेमी जो कहें, पर वह हिन्दी की रूपान्तर मात्र है और उसी की गोद में पली है। और इसीलिए कुछ प्रान्तों में समाद्रित भी है। हिन्दी-भाषा के योग्य एवं गण्यमान्य विबुधों ने खड़ी बोली को जो रूप दिया है और जिस प्रकार उसे सर्व गुणालंकृत बनाया है वह उल्लेखनीय ही नहीं अभिनन्दनीय भी है। अब भी उसमें देश काल की आवश्यकताओं पर दृष्टि रखकर उचित परिवर्तन होते रहते हैं। वास्तव बात यह है कि खड़ी बोली की हिन्दी का स्वरूप इस समय सन्तोषजनक और सर्वांग पुष्ट है। इधर थोड़े दिनों से कुछ लोगों की उच्छृंखलता बढ़ गयी है, मनमानी होने लगी है। मुहावरे भी गढ़े जाने लगे हैं और कुछ मनमाने प्रयोग भी होने लगे हैं, किन्तु इसके कारण अनभिज्ञता, अपरिपक्वता और प्रान्तीयता हैं। भाषा में ही नहीं, भावों में भी कतर-ब्योंत हो रहा है, आसमान के तारे तोड़े जा रहे हैं, स्वतन्त्रता के नाम पर मनस्विता का डिंडिम नाद कर कला को विकल बनाया जा रहा है या प्रतिभा उद्यान में नये फूल खिलाए जा रहे हैं। किन्तु ए मानस-उदधि की वे तरंगें हैं जो किसी समय विशेष रूप में तरंगित होकर फिर यथाकाल अपने यथार्थ रूप में विलीन हो जाती हैं। भाषा का प्रवाह सदा ऐसा ही रहा है और रहेगा। परन्तु काल का नियंत्रण भी अपना प्रभाव रखता है, उसकी शक्ति भी अनिवार्य है।
मैंने हिन्दी-भाषा के आधुनिक रूप (खड़ी बोली) के प्रधान प्रधान सिध्दान्तों के विषय में जो थोड़े में कहा है, वह दिग्दर्शन मात्र है। अधिक विस्तार सम्भव न था। उन्हीं पर दृष्टि रखकर मैंने 'वैदेही-वनवास' के पद्यों की रचना की है। कवि-कर्म की दुरूहता मैंने पहले ही निरूपण की है, मनुष्य भूल और भ्रान्ति रहित होता नहीं। महाकवि भी इनसे सुरक्षित नहीं रह सके। कवितागत दोष इतने व्यापक हैं कि उनसे बड़े-बड़े प्रतिभावान् भी नहीं बच सके। मैं साधारण विद्या, बुध्दि का मनुष्य हूँ, इन सब बातों से रहित कैसे हो सकता हूँ। विबुधवृन्द और सहृदय सज्जनों से सविनय यही निवेदन है कि ग्रंथ में यदि कुछ गुण हों तो वे उन्हें अपनी सहज सदाशयता का प्रसाद समझेंगे, दोष-ही-दोष मिलें तो अपनी उदात्त चित्त-वृत्ति पर दृष्टि रखकर एक अल्प विषयामति को क्षमा दान करने की कृपा करेंगे।
दोहा
जिसके सेवन से बने पामर नर-सिरमौर।
राम रसायन से सरस है न रसायन और॥