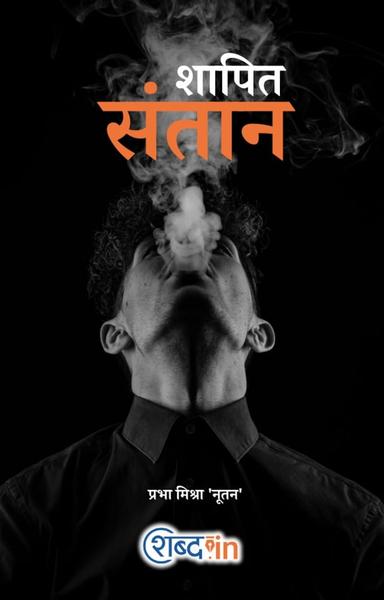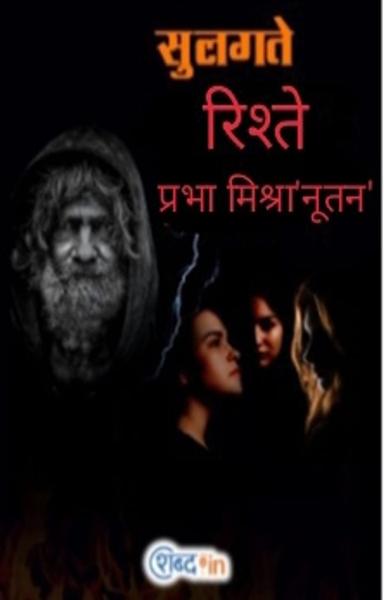तब न था विश्वास,
कि हममें वो सुवास,
जो गृह आंगन का,
उपवन महका सकें।
कीर्ति फैला सकें,
सम्मान दिला सकें।
गर्व से सिर ऊंचा उठा सकें।
सुत पाने की चाह में,
हम आ गये सारी।
तो!कंधों पर,
इतने हो गये भारी?
उन्हें कुछ देना अर्थ,
और हमें देना व्यर्थ लगा?
स्वप्न पंखों को काट कर,
कुंठित हमारा विकास कर,
मां बाप तुम्हें बस,
अपना बेटा ही समर्थ लगा?
आज जरावस्था लिये,
खडे़ हुये जिनके समक्ष।
उनके सामने तो,
सबसे बडा़ प्रश्न यक्ष,
कि बंटवारा आरपार हो।
हिस्से बस एक पडे़,
दूजे से उद्धार हो।
जो एक सुत में खेले।
वो मजबूरी में झेले।
सुध लो कोख में मारने वालों,
जिनकी चाह में,चल रही आरी।
वो कलियुग के अंकुर हैं,
बस ऐसे ही होंगे संस्कारी।
जिनकी चाह में ,सोचते हो,
कि इसे मार दें।
क्या पता उन्हीं मे से एक,
आकर तुम्हें तार दे।
प्रभा मिश्रा 'नूतन'