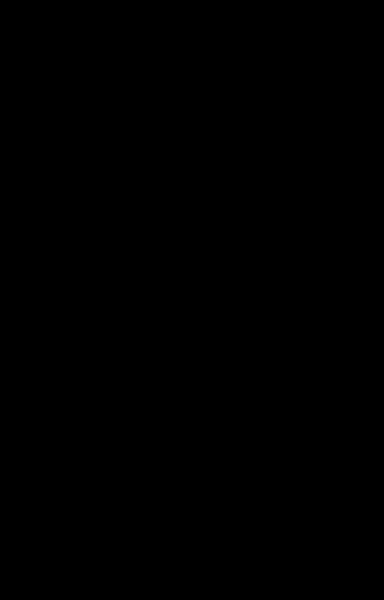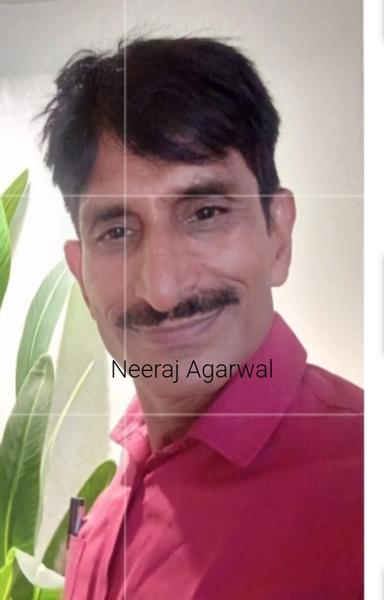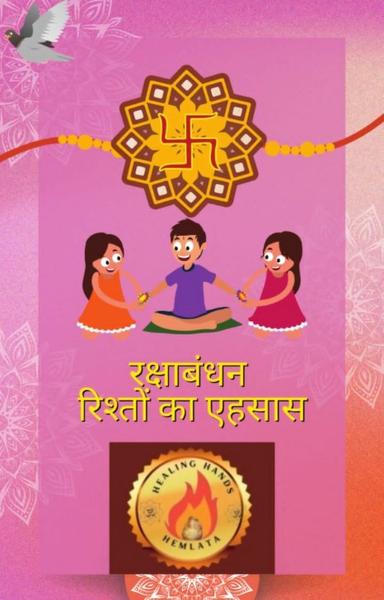1 अगस्त 2018 के जनसत्ता में आलोक मेहता का लेख ‘विश्वास का पुल’ पढ़ा। इसमें सर सैयद अहमद खां के जिस वक्तव्य को उद्धृत किया गया है उससे उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पक्ष उजागर होता है, जबकि उनके व्यक्तित्व के कई और पक्ष हैं जिन्हें हमारे बुद्धिजीवी अपनी सुविधानुसार प्रकाश में नहीं लाते। यही कारण है कि साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा होने में कठिनाई खड़ी होती है। एम एस जैन ने अपनी पुस्तक ‘आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक’ में सर सैयद के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। जैन लिखते हैं कि “सर सैयद भारतीय राजनीति में प्रथम नेता थे जिन्होंने धर्म को अपनी राजनीति का आधार बनाया।” वह कांग्रेस की स्थापना के घोर विरोधी थे। उन्होंने कांग्रेस आंदोलन को “बंगाली मित्रों द्वारा मुसलमानों को कुचलने का प्रयास बताया।” उन्होंने कांग्रेस का संगठित रूप से विरोध करने के लिए ‘इंडियन पैट्रिऑटिक एसोसिएशन’ की स्थापना की जिसका सर्वप्रमुख उद्देश्य था ‘कांग्रेस द्वारा किए गए समस्त प्रयत्नों का खंडन करना।’ जब फिर भी बात नहीं बनी, तो 1893 में ‘मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन’ की स्थापना की जो सर सैयद के राजनीतिक चिंतन का ही परिणाम थी। इसने वे सब मांगें प्रस्तुत कीं जिन्हें 1906 में मुस्लिम लीग ने भी प्रस्तुत किया था। वह उत्तर-पश्चिमी प्रांत में व्यवस्थापिका सभा में हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर रखना चाहते थे, चाहे हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से बहुत अधिक क्यों न हो। उनका तर्क था कि “मुसलमानों का भूतकालीन ऐतिहासिक योगदान और आधुनिक राजनीतिक महत्व किसी प्रकार हिंदुओं से कम नहीं था।” इसी के साथ उन्होंने मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक प्रणाली के आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति की स्थापना की मांग की। वह लोकतंत्र को भी मजहबी चश्मे से देखते थे जिसको लेकर उन्होंने कहा कि “इस्लाम ने किसी गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना नहीं की थी।”
वह एक साथ हिंदू विरोधी और ईसाई प्रेमी दिखना चाहते थे। सर सैयद ने कहा कि “कोई मुसलमान इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि ईश्वर ने कहा है कि ईसाइयों के अतिरिक्त किसी धर्म के अनुयायी मुसलमानों के मित्र नहीं हो सकते।” उन्होंने भारतीय राजनीतिक दलों के गठन का आधार धर्म घोषित किया था और यह बताया था कि “भारतीय संसद में दो दल — हिंदू एवं मुसलमान — ही होंगे।”
हिंदी-उर्दू विवाद में भी उन्होंने घी डालने का काम किया। ‘हयात-ए-जावेद’ के लेखक अलताफ हुसैन हाली इस वाद-विवाद की शुरुआत के लिए सर सैयद के साम्प्रदायिक होने को उत्तरदायी ठहराते हैं। सर सैयद के अलगाववादी विचार उनके जीवन में बहुत आरंभ में ही आ गए थे। उदाहरण के लिए, 1876 में ही उन्होंने कहा कि “इसमें [भारत में] रहने वालों के धार्मिक मतभेद इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने किसी अन्य शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था……….जिस प्रकार रात-दिन तथा काली-सफेदी का आपस में मिल जाना कठिन था उससे कुछ अधिक कठिन था कि भारत के विभिन्न धर्म आपस में संगठित हो जाएं।”
सर सैयद अंततः एक प्रभावशाली नेता ही नहीं बल्कि अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता भी थे। कालांतर में यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का ऐसा संगठित विरोध करने लगा कि तंग आकर बहुत सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम अलीगढ़ को छोड़कर दिल्ली आ गए और जामिया मिलिया इस्लामिया (मुस्लिम विश्वविद्यालय) के होकर रह गए।
अब प्रश्न उठता है कि जिस वक्तव्य की बात इस लेख में की गई वैसा वक्तव्य सर सैयद ने क्यों दिया? तो इसका उत्तर जैन देते हैं — “अपनी मुसलमान कौम से कम धन उपलब्ध होने के कारण सर सैयद के समक्ष मुख्य समस्या मुसलमानों की प्रगति में हिंदुओं से सहयोग लेना थी। हिंदुओं की प्रगति या आंदोलन में सहयोग देना मुसलमानों का, उनके अनुसार, कोई कर्तव्य नहीं था। सर सैयद ने जब कभी अपने कुछ निश्चित मुहावरों का प्रयोग किया, वह उसी समय किया जब उन्हें हिंदुओं से अलीगढ़ कालेज के लिए आर्थिक सहायता लेनी हो या दी हुई सहायता के लिए धन्यवाद देना हो।”
लेखक निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग , वित्त मंत्रालय ,भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं। लेख में व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं ।
4 सितम्बर 2018