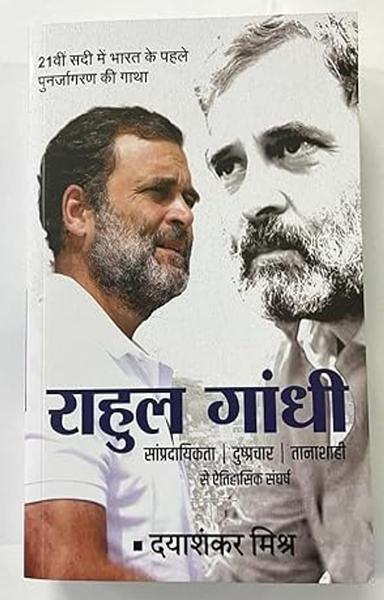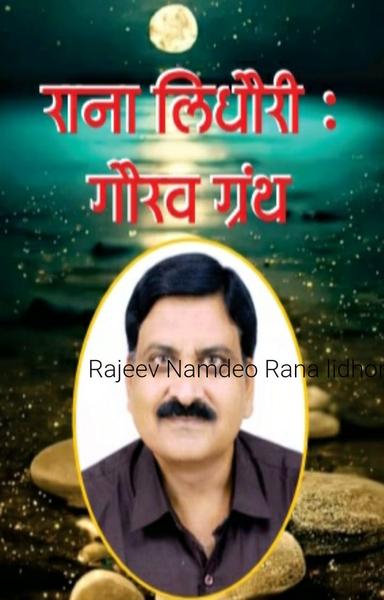मैं कहां जाऊं
किसी स्वर्ग जैसा
अब नर्क कहां बचा है यहां
जहां कशिश से भरी आंखों में
ग़ालिब की गजलें महकती हों
जहां मेरी जर्जर कमीज़ की जेब से
कोई सादा कागज निकल आता हो
कहां जाऊं मैं
ताकि किसी अदृश्य उद्देश्य के लिए
संसद की दीवारें न ढहे
और दायित्व के पंखों को बांधकर
कोई सार्थक और गंभीर पहल
कम से कम सामने हो मौजूद मेरे
तीली और मिथक की अस्मिता में
जरूरत से कुछ ज्यादा ही
स्मृति कोश की सारी स्मृतियां
आंच की हदों को छोड़कर
किसी हंस के समान
मानसरोवर में तैरना चाहती है
और महास्वपन के पटाक्षेप पर
जब गले से निकलती है सिटी
तब जाने की समस्त संभावनाएं
नर्क के दरवाजे पर ही अटकी है
और खाली हाथ
पेट की दोनों जेबों में कसमसा रहे हैं
कहां जाऊं मैं
रात के घने अंधकार से निकलकर
मैं कहां जाऊं?