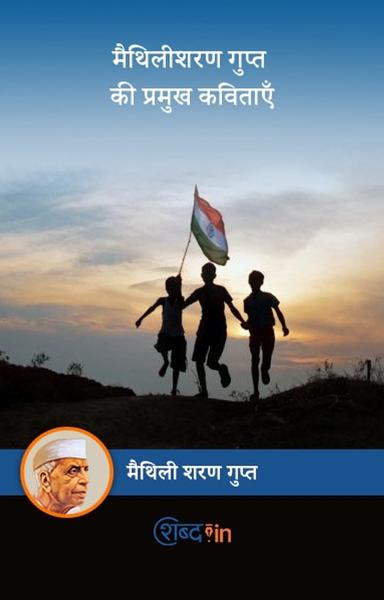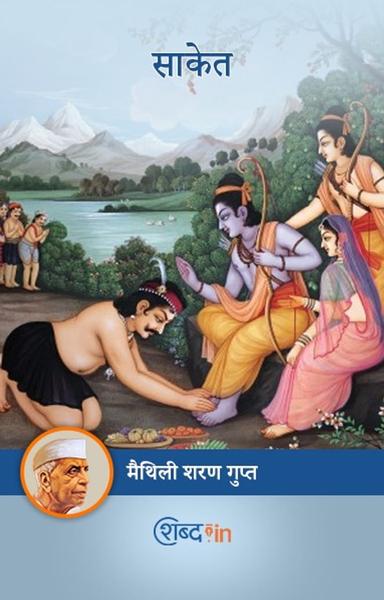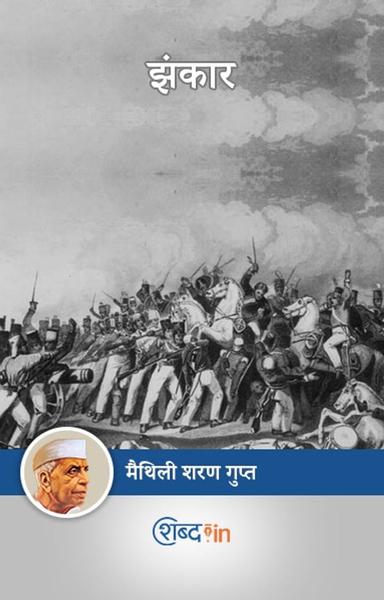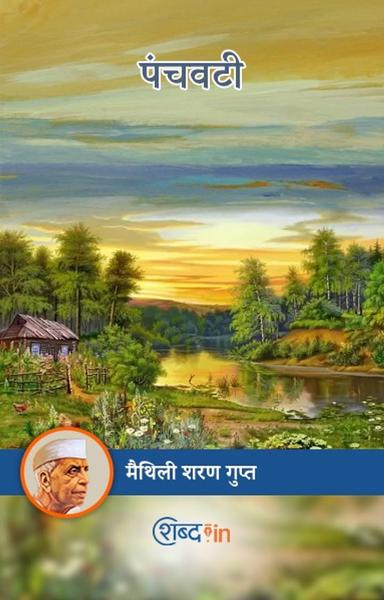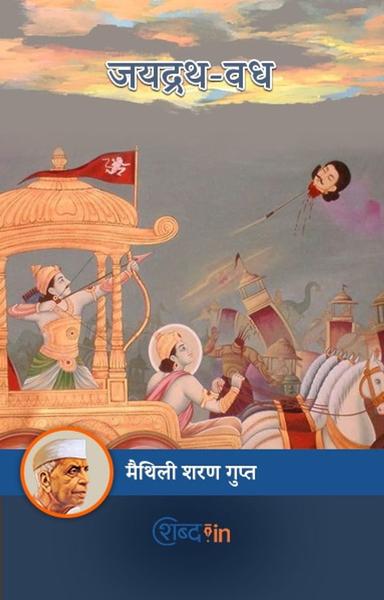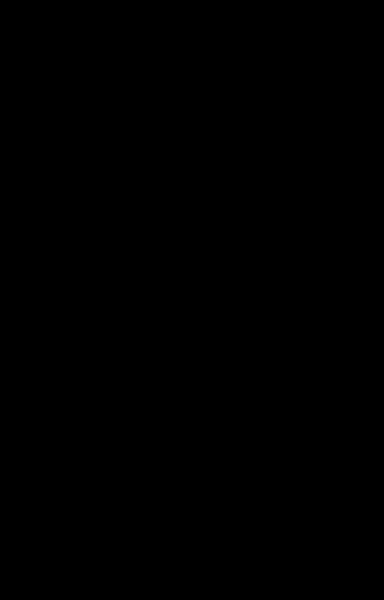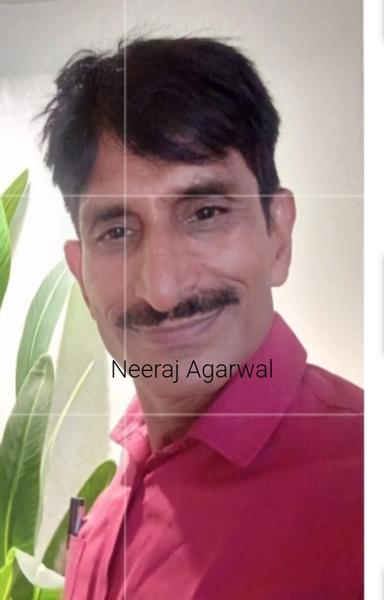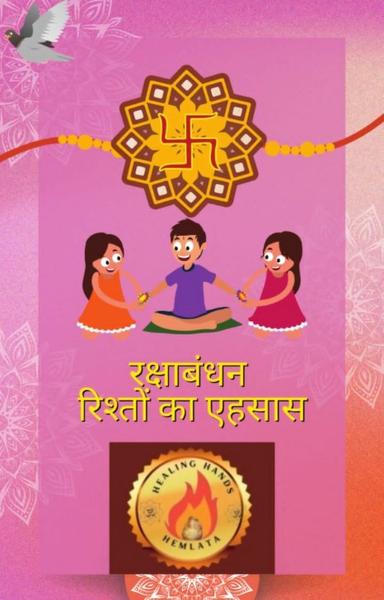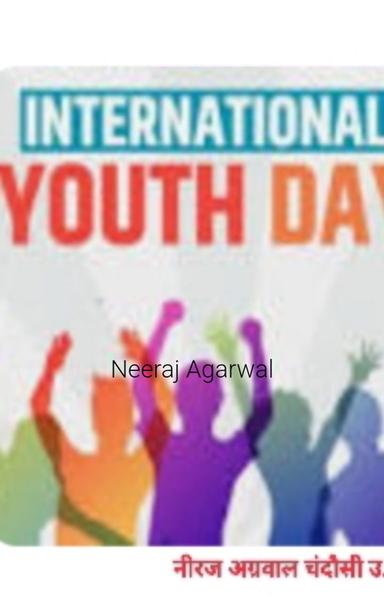यद्यपि उड़ा बैठे कमाई बाप-दादों की सभी,
पर ऐंठ वह अपनी भला हम छोड़ सकते हैं कभी ?
भूषण विके, ऋण मी बढे, पर धन्य सब कोई कहे;
होली जले भीतर न क्यों, बाहर दिवाली ही रहे !!! ।।२८६।।
गुण, ज्ञान, गौरव, मान, धन यद्यपि सभी कुछ खो चुके,
गजमुक्त शून्य कपित्थ-सम नि:सार अब हम हो चुके ।
पर हैं दबाते दीनता श्वेताम्बरों में भूल से !
सम्भव कभी है अग्नि को भी दाब रखना तूल से ? ।।२८७।।
दबती कहीं आडम्बरों से बहुत दिन तक दीनता ?
मिलता नहीं फिर क़र्ज़ भी, होती यहाँ तक हीनता ।
उद्योग तो हम क्या करेंगे जो अपव्यय कर रहे,
पर हाँ, हमारे हाथ से हैं दीन-दुर्बल मर रहे ।।२८८।।
अब आय तो है घट गई, पर व्यय हमारा बढ़ गया,
तिस पर विदेशी सभ्यता का भूत हम पर चढ़ गया।
ऋण-भार दिन दिन बढ़ रहा है दब रहे हैं हम यहाँ,
देता जिन्हें हो, कुछ नहीं भी पास उनके है कहाँ ? ।।२८९।।