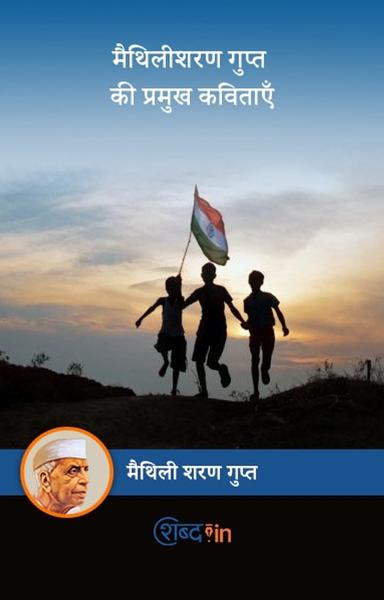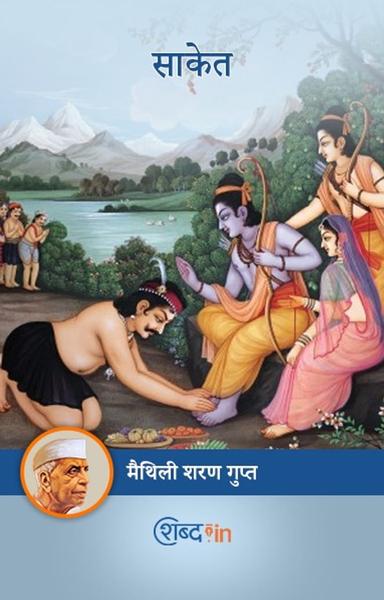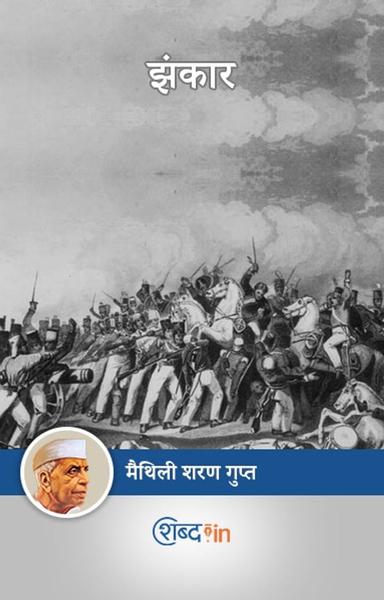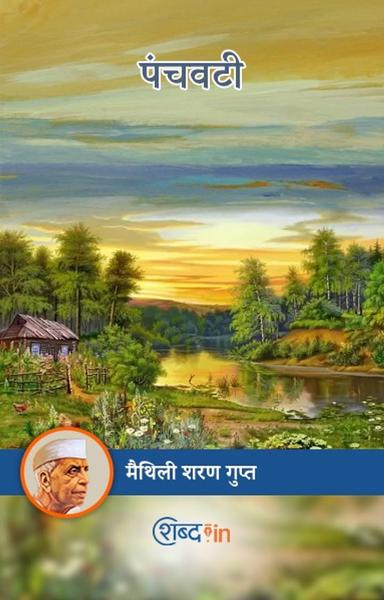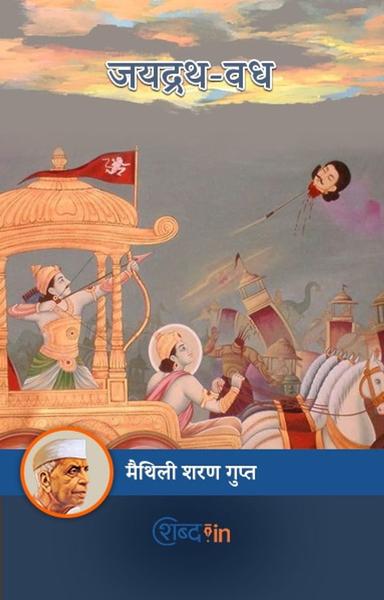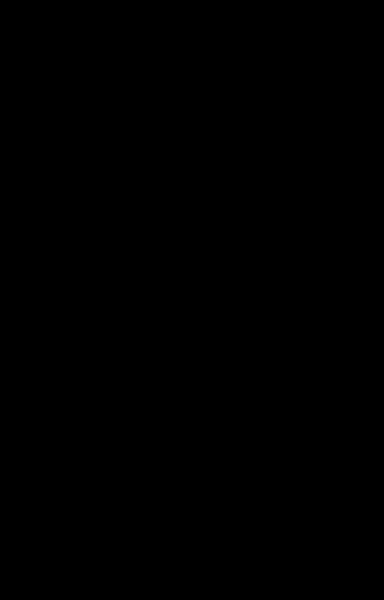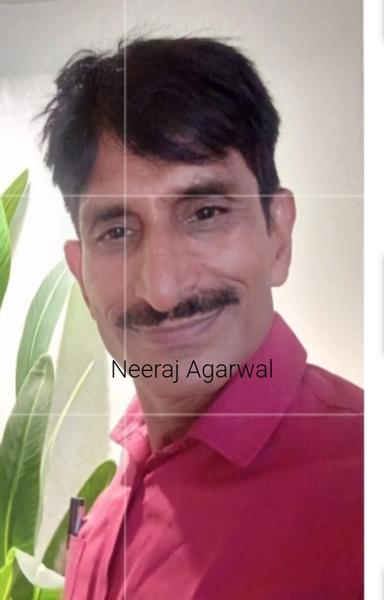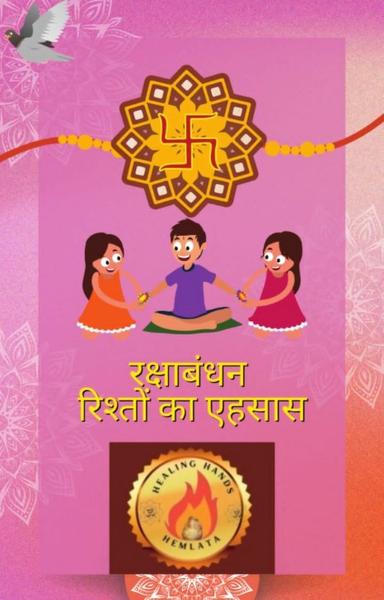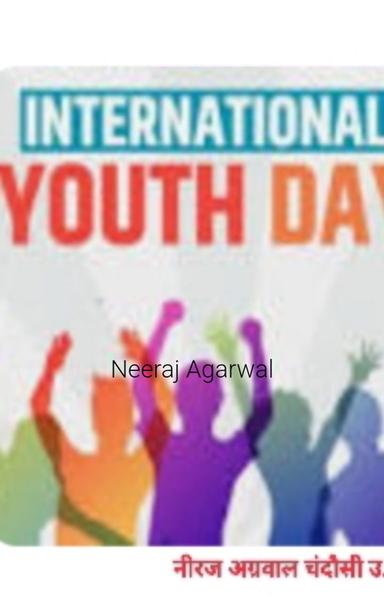है और औपन्यासिकों का एक नृतन दल यहाँ,
फैला रहा है जो निरन्तर और भी हलचल यहाँ!
दौरात्म्य ही अब लोक-रुचि पर हो रहा है सब कहीं,
हा स्वार्थ ! तेरी जय, अरे, तू क्या करा सकता नहीं? ॥१६३॥
ये रुचि-विघातक ग्रन्थ ज्यों ही सैर करने को छुए,
स्वीया हुईं कुलटा बहुत, अनुकूल बहुधा शठ हुए !
ये भाव हम गिरते हुओं पर और पत्थर-से गिरे,
दब कर हृदय जिनसे हमारे हो गये जर्जर निरे !!॥१६४।।
जो उपन्यास यहाँ सु-शिक्षा-प्रद कहा कर बिक रहे
उनमें अधिक अविचार की ही नींव पर हैं टिक रहे ।
उनके कु-पात्रों में नरक की आग ऐसी जागती-
अपनी सु-रुचि भी पाठकों की दूर जिससे मागती ! ॥१६५।।
साद्यन्त उनमें असम्भवता घन-घटा सी छा रही,
दुर्भाव की दुर्गन्धि उनसे अन्त तक है आ रही ।
आई कहानी भी न कहनी और हम इतना बके,
'जीवन-प्रभात' न 'चन्द्रशेखर' एक भी हम लिख सके ! ॥१६६।।
लिक्खाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य-रत्न कहा रहे,
वे वीर वैतरणी नदी का हैं प्रवाह बहा रहे ।
वे हैं नरक के दूत किंवा सूत हैं कलिराज के !
वे मित्ररूपी शत्रु ही हैं देश और समाज के ॥१६७।।
क्या मुँह दिखानेंगे भला परलोक में वे ही कहें ?
जो कुछ नहीं आता उन्हें तो मौन ही फिर वे रहें !
पर मौन वे कैसे रहें, निरुपाय क्या भूखों मरें ?
मर जाय क्यों न समाज सारा, पाकटें उनकी भरें !!॥१६८||