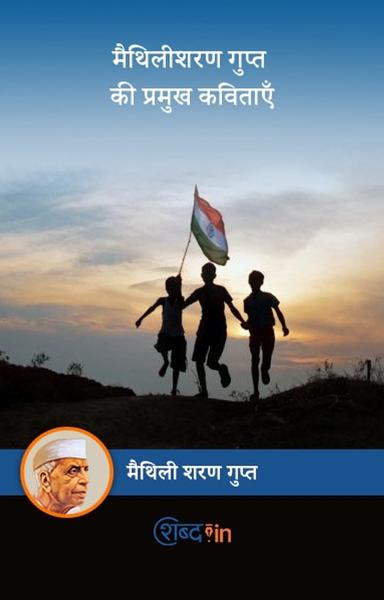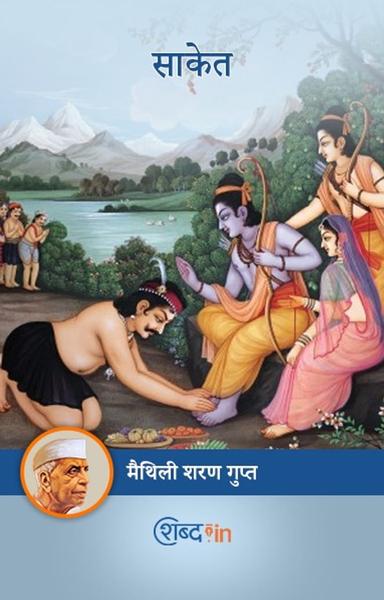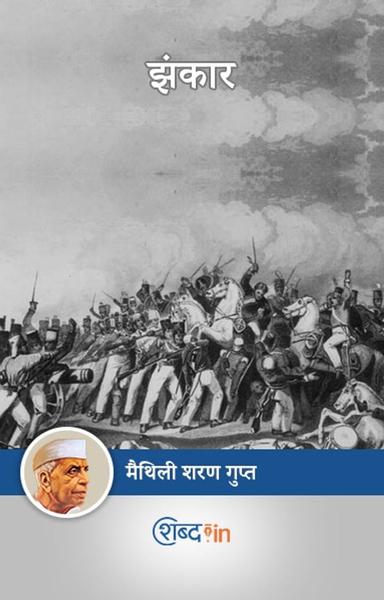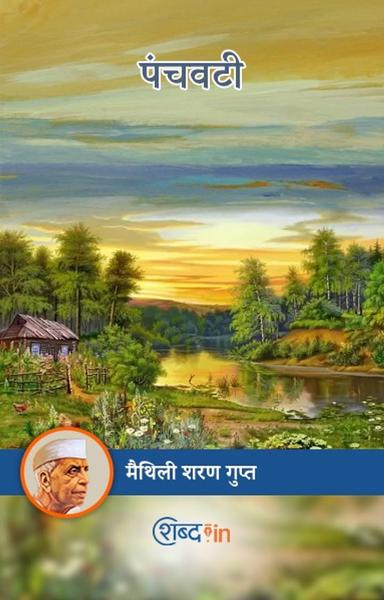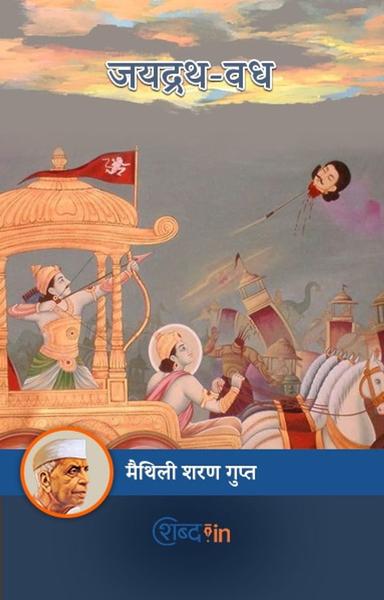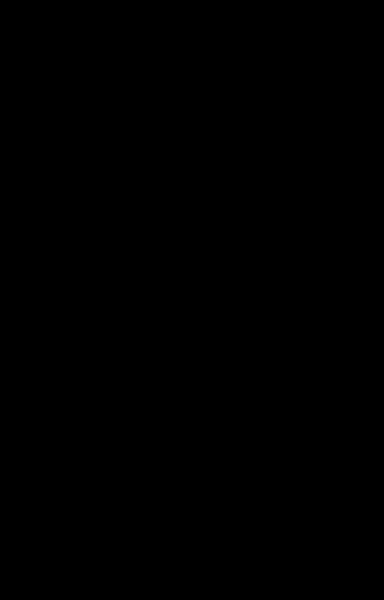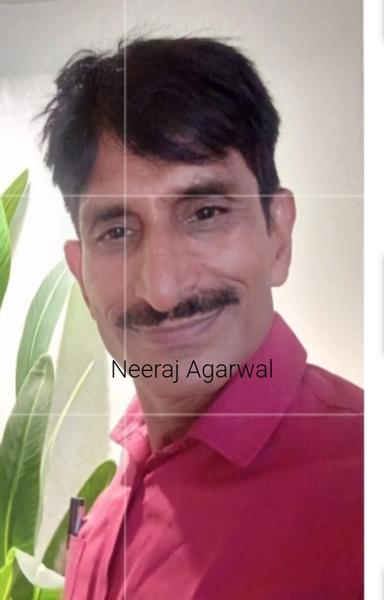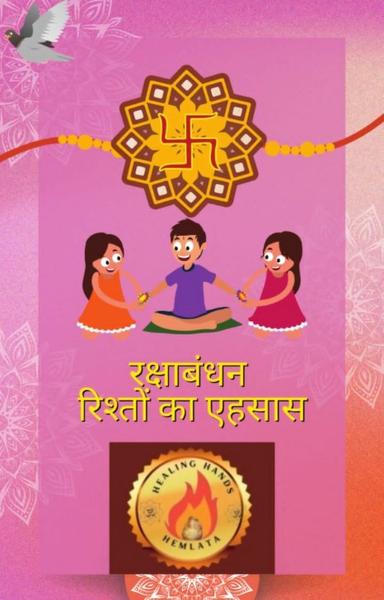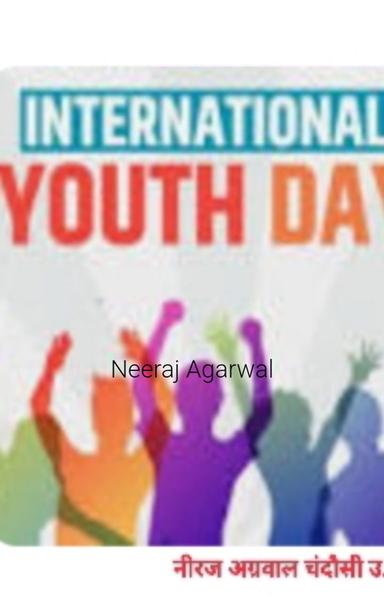अब पूर्व की-सी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है,
पर क्या इसीसे अब हमारी घट रही सम्पत्ति है ?
यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बन्द हो-
तो देश फिर सम्पन्न हो, क्रन्दन रुके, अनन्द ही ॥ २८ ॥
वह उर्वरापन भूमि का कम हो गया है, क्यों न हो ?
होता नहीं कुछ यत्न उसका, यत्न कैसे हो, कहो ?
करते नहीं कर्षक परिश्रम, और वे कैसे करें ?
कर-वृद्धि है जब साथ तब क्यों वे वृथा श्रम कर मरें? ॥ २९॥
सौ में पचासी जन यहाँ निर्वाह कृषि पर कर रहे,
पाकर करोड़ों अर्द्ध भोजन सर्द आहें भर रहे।
जब पेट की ही पड़ रही फिर और की क्या बात है,
'होती नहीं है भक्ति भूखे' उक्ति यह विख्यात है ॥ ३०॥
कृषि-कर्म की उत्कर्षता सर्वत्र विश्रुत है सही,
पर देख अपने कर्षकों को चित्त में आता यही-
हा दैव ! क्या जीते हुए आजन्म मरना था उन्हें ?
भिक्षुक बनाते, पर विधे ! कर्षक न करना था उन्हें ॥ ३१ ॥
कृषि में अपेक्षा वृष्टि की रहती हमें अब है सदा,
होता जहाँ वैषम्य उसमें क्या कहें फिर अपदा।
रहता अवर्षण से अहो! अब जो हमारा हाल है,
दृष्टान्त उसका इन दिनों गुजरात का दुष्काल है॥३२॥
था एक ऐसा भी समय पड़ता अकाल न था यहाँ,
हो या न हो वर्षा जलाशय थे यथेष्ट जहाँ तहाँ।
भारत पढ़ो, देवर्षि ने है क्या युधिष्ठिर से कहा—
“कृषि-कार्य्यावर्षा की अपेक्षा के बिना तो हो रहा है?"॥३३॥
केवल अवर्षण ही नहीं, अति वृष्टि का भी कष्ट है;
बढ़ कर प्रलय-सम प्रबल जल सर्वस्व करता नष्ट है !
"दैवोऽपि दुर्बलघातक:" अथवा अभाग्य कहें इसे ?
किंवा कहो, निज कर्म का मिलता नहीं है फल किसे ? ॥३४॥
अब ऋतु-विपर्यय तो यहाँ आवास ही-सा है किये,
होती प्रकृति में भी विकृति हा ! भाग्यहीनों के लिए।
हेमन्त में बहुधा घनों में पूर्ण रहता व्योम है,
पावस-निशाओं में तथा हँसता शरद का सोम है ! ॥ ३५॥
हो जाय अन्छी भी फ़सल पर लाभ कृषकों को कहाँ ?
खाते, स्ववाई, बीज-ऋण से हैं रंगे रक्खे यहाँ ।
आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अन्त में,
अधपेट रह कर फिर उन्हें है काम्पना हेमन्त में ! ॥ ३६ ॥
पानी बना कर रक्त का, कृषि कृषक करते हैं यहाँ,
फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ ।
सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्न वह निरुपाय है,
बस चार पैसे से अधिक पड़ती न दौनिक आय है ! ॥ ३७ ॥
जब अन्य देशों के कृषक सम्पत्ति में भरपूर हैं-
लाते कि जिनसे आठ रुपया रोज के मज़दूर हैं।
तब चार पैसे रोज़ ही पाते यहाँ कृर्षक अहो !
कैसे चले संसार उनका, किस तरह निर्वाह हो ? ॥ ३८॥
बीता नहीं बहु काल उस औरङ्गजेबी को अभी -
करके स्मरण जिसका कि हिन्दू काँप उठते हैं सभी।
उस दुःसमय का चावलों का आठ मन का भाव है,
पर आठ सेर नहीं रहा अब, क्या अपूर्व अभाव है ! ॥ ३९॥
होती नहीं है कृषि यहाँ पूरी तरह से अब कभी,
यद्यपि शुभाशा चित्त में होती हमें हैं जब कभी ।
पाला कहीं, ओले कहीं, लगता कहीं कुछ रोग है,
पहले शुभाशा, फिर निराशा, दैव ! कैसा योग है ? ॥४०॥
बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा-सा जल रहा,
है चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा !
देखा, कृषक शोणित सुखा कर हल तथापि चला रहे,
किस लेाभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे ! ॥४१॥
मध्याह्न है, उनकी स्त्रियाँ ले रेटियों पहुंची वहीं,
हैं रोटियां रूखी, खबर है शाक की हमको नहीं !
सन्तेाष से खाकर उन्हें वे, काम में फिर लग गये,
भर पेट भोजन पा गये तो भाग्य माने जग गये ! ॥ ४२ ॥
उन कृषक-वधुओं की दशा पर नित्य रोती है दया,
हिम-ताप-वृष्टि-सहिष्णु जिनका रंग काला पड़ गया।
नारी-सुलभ-सुकुमारता उनमें नहीं है नाम को,
वे कर्कशांगी क्यों न हों, देखो न उनके काम को !! ॥४३॥
गोबर उठाती, थापती हैं, भोगती आयास वे,
कृषि काटतीं, लेतीं परोहे, खोदती हैं घास वे।
गृह-कार्य जितने और हैं करती वही सम्पन्न हैं,
तो भी कदाचित् ही कभी भर पेट पाती अन्न हैं ॥४४॥
कुछ रात रहते जागकर चक्की चलाने बैठतीं,
हम सच कहेंगे, उस समय वे गीत गाने बैठतीं।
पर क्या कहें, उस गीत से क्या लाभ पाने बैठतीं,
वे सुख बुलाने बैठती, या दुख भुलाने बैठतीं ! ॥४५॥
घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा,
घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा।
तो भी कृषक मैदान में करते निरन्तर काम हैं,
किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं ? ॥४६॥
बाहर निकलना मौत है, आधी अँधेरी रात है,
आ: शीत कैसा पड़ रहा है, थरथराता गात है।
तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते,
वह लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी त्यागते ! ॥४७॥
यह अन्न तो लेंगे विदेशी, लाभ क्या उनको कहो ?
मिलता उन्हें जो अर्द्ध भोजन विघ्न उसमें भी न हो !
कहते इसी से हैं कि क्या आजन्म मरना था उन्हें,
भिक्षुक बनाते पर विधे! कर्षक न करना था उन्हें ! ॥४८॥
हैं वे असभ्य तथा अशिक्षित, भाव उनके भ्रष्ट हैं ;
दुख-भार से सुविचार मानो हो गये सब नष्ट हैं !
अपनी समुन्नति के उन्हें कोई उपाय न सूझते,
अपना हिताहित भी न कुछ वे हैं समझते बूझते ॥४९॥
सज्ञान कैसे हों, उन्हें संयोग ही मिलता नहीं,
विख्यात कमलालय कमल भी दिन बिना खिलता नहीं !
है पेट से ही पेट की पड़ती उन्हें, वे क्या करें !
वे ग्वाल हो जीते रहें, या छात्र बन भूखों मरें? ॥ ५० ॥
सम्प्रति कहाँ क्या हो रहा है, कुछ न उनको ज्ञान है,
है वायु कैसा चल रहा, इसका न कुछ भी ध्यान है !
मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है,
शशि-सूर्य्य हैं, फिर भी कहीं उसमें नहीं आलोक है! ॥ ५१ ॥
भरपेट भोजन ही चरम सुख वे अकिंचन मानते,
पर, साथ ही दुर्भाग्य-वश दुर्लभ उसे हैं जानते !
दिन दुःख के हैं भर रहे करते हुए सन्तोष वे,
लाचार हैं, निज भाग्य को ही दे रहे हैं दोष वे ! ॥ ५२ ॥
उनको निरन्तर दुःख ने अब कर दिया यों दीन है-
सुख-कल्पना तक से हुआ उनका हृदय अब हीन है।
आलोक का अनुभव कभी जन्मान्ध कर सकते नहीं,
मरु-जन्तु सहसा सुरसरी का ध्यान धर सकते नहीं ॥ ५३ ॥
ग्रामीण गीत यदा कदा वे गान करते हैं सही,
है फाग उनका राग बहुधा और उत्सव भी वही।
पर चित्त को वे दीन जन किस भाँति बहलाया करें?
क्या आँसुओं से ही उसे वे नित्य नहलाया करें ? ॥ ५४ ॥
तुम सभ्य हो, 'मार्केट' जिनका सात सागर पार है,
पर ग्राम की वह हाट ही उनका 'बड़ा बाजार' है।
तुम हो विदेशों से मँगाते माल लाखों का यहाँ,
पर वे अकिंचन नमक-गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ ॥ ५५ ॥
करते सहर्ष प्रदर्शिनी की सैर तुम कौतुक भरी,
(क्या लाभ उससे हो उठाते, बात है यह दूसरी।)
वे हो सका तो ग्राम्य मेले देखकर ही धन्य हैं,
मनिहार की दूकान से जिनमें सुदृश्य न अन्य हैं ॥ ५६ ॥
तुम दार्शनिक हो, ईश का अस्तित्व सत्य न मानते,
हैं भूत-प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते।
हा दैव ! इस ऋषि-भूमि का यह आज कैसा हाल है !
तू काल ! सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है ॥ ५७ ॥
पाठक ! न यह कह बैठना-छेड़ा कहाँ का राग है,
यह फूल कैसा है कि इसमें गन्ध है न पराग है?
है यह कथा नीरस तदपि इसमें हमारा भाग है,
निकले बिना बाहर नहीं रहती हृदय की आग है ॥ ५८ ॥