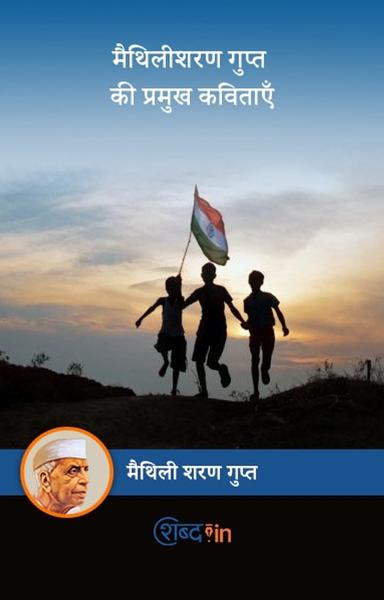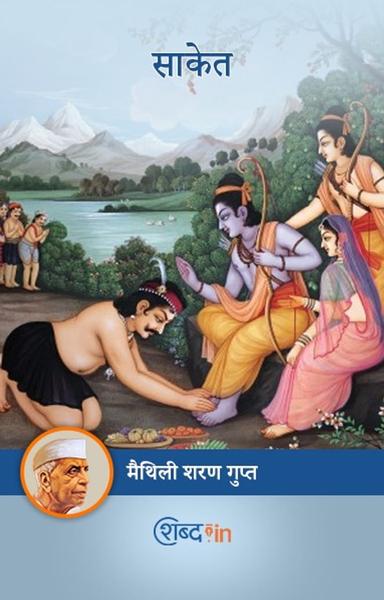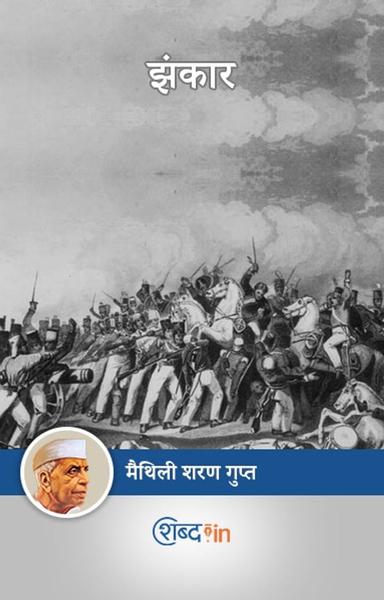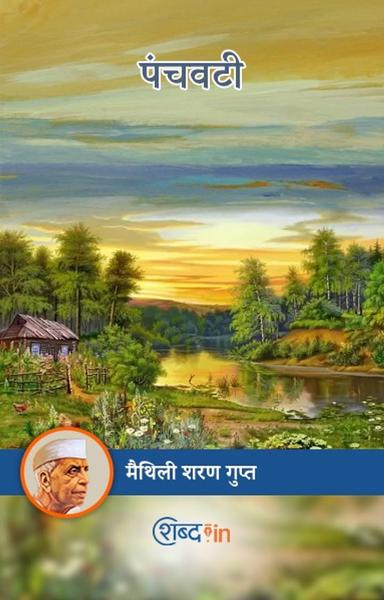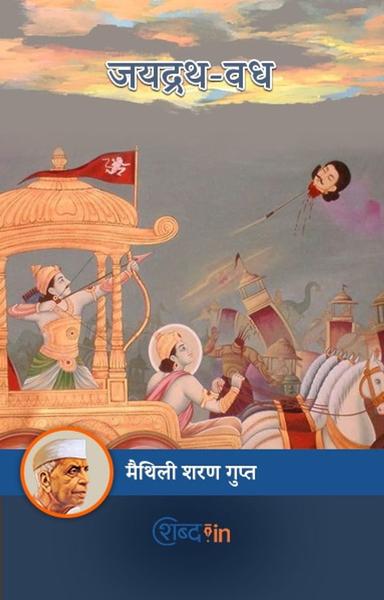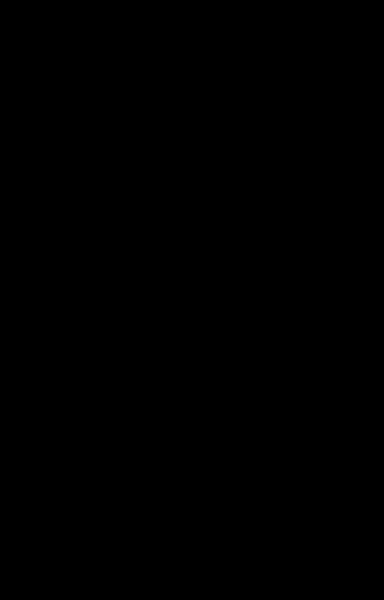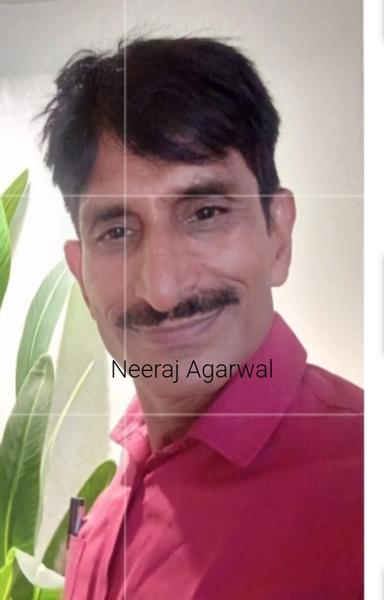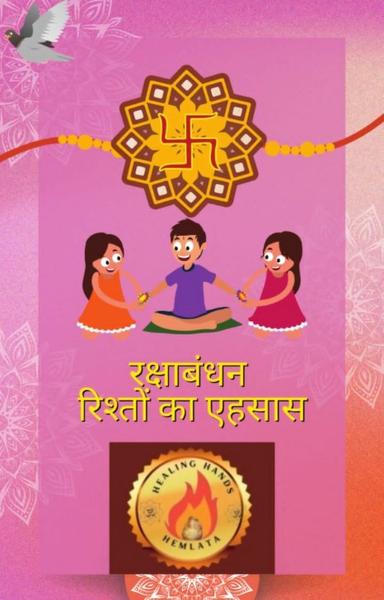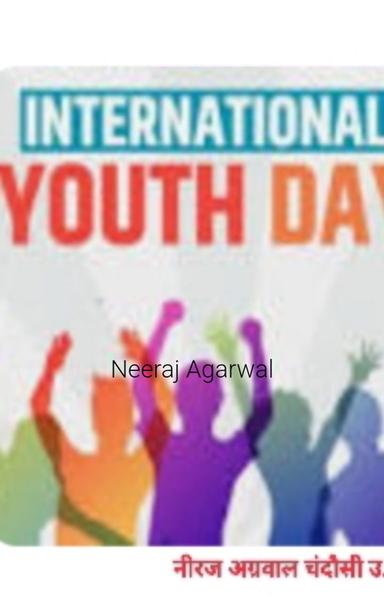थे कर्मवीर कि मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे,
थे युद्धवीर कि काल से भी हम कभी डरते न थे।
थे दानवीर कि देह का भी लोभ हम करते न थे,
थे धर्मवीर कि प्राण के भी मोह पर मरते न थे ॥१२३॥
वे सूर्यवंशी चन्द्रवंशी वीर थे कैसे बली,
जो थे अकेले ही मचाते शत्रु-दल में खलबली।
होते न वे यदि चक्रवर्ती भूप दिग्विजयी यहाँ-
होते भला फिर 'अश्वमेध' कि 'राजसूय' कहो कहाँ? ॥१२४॥
थे भीम-तुल्य महाबली, अर्जुन-समान महारथी,
श्रीकृष्ण लीलामय हुए थे आप जिनके सारथी।
उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है,
जीवन-समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है ॥१२५॥
हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था?
जो शब्द-वेधी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था?
हाँ, मत्स्य जैसे लक्ष्य-वेधक धीर-धन्वी थे यहाँ,
रिपु को गिराकर अस्त्र पीछे लौट आते थे कहाँ ?॥१२६॥
थी चञ्चला की-सी चमक या शीघ्रता सन्धान की,
कृतहस्तता ऐसी कि गति थी हाथ में ही बाण की ।
मुँह खोल कुत्ता भूँकने में बन्द फिर जब तक करे-
भर जाय मुख तूणीर-सा, पर बात क्या जो वह मरे !॥१२७॥
जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकन्दर की चली-
वह चन्द्रगुप्त महीप था कैसा अपूर्व महाबली ?
जिससे कि सिल्यूकस समर में हार तो था ले गया,
कान्धार आदिक देश देकर निज सुता था दे गया !॥१२८॥
जो एक सौ सौ से लड़े ऐसे यहाँ पर वीर थे,
सम्मुख समर में शैल-सम रहते सदा हम धीर थे।
शङ्का न थी, जब जब समर का साज भारत ने सजा-
जावा, सुमात्रा, चीन, लङ्का सब कहीं डंका बजा ॥१२९॥
मोहे विदेशी वीर भी जिस वीरता के गान से,
जिस पर बने हैं ग्रन्थ 'रासो' और 'राजस्थान'-से ।
थी उष्णता वह उस हमारे शेष शोणित की अहा !
जो था महाभारत-समर में नष्ट होते बच रहा ॥१३०॥
रक्षक यवन साम्राज्य के भी राजपूत रहे यहाँ,
पड़ती कठिनता थी जहाँ जाते वही तो थे वहाँ ।
नृप मान-कृत काबुल-विजय की बात सबको ज्ञात है,
दृढ़ता शिवाजी के निकट जयसिंह की विख्यात है ॥१३१॥
क्षत्राणियाँ भी शत्रुओं से हैं यहाँ निर्भय लड़ीं,
इतिहास में जिनकी कथायें हैं अनेक भरी पड़ीं ।
देकर विदा युद्धार्थ पति को प्रेमवल्ली-सी खिली,
यदि फिर न भेंट हुई यहाँ तो स्वर्ग में झट जा मिलीं ॥१३२॥
वह सामरिक सिद्धान्त भी औदार्य-पूर्ण पवित्र था-
थी युद्ध में ही शत्रुता, अन्यत्र बैरी मित्र था !
जय-लोभ में भी छल-कपट आने न पाता पास था,
प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था ॥१३३॥
पाते न थे जय युद्ध में ही हम सुयश के साथ में,
इन्द्रिय तथा मन भी निरन्तर थे हमारे हाथ में ।
हम धर्म्म-धनु से भक्ति-शर भी छोड़ने में सिद्ध थे,
अतएव अक्षर-लक्ष्य भी करते निरन्तर विद्ध थे ॥१३४॥
यद्यपि रहे हम वीर ऐसे-विश्व को जय कर सकें,
ऐसे नहीं थे जो समर में शक को भी डर सकें।
परराज्य को तो थे सदा हम तुच्छ तृण-सा मानते,
लाचार होकर ही कभी लङ्का-सदृश रण ठानते ॥१३५॥