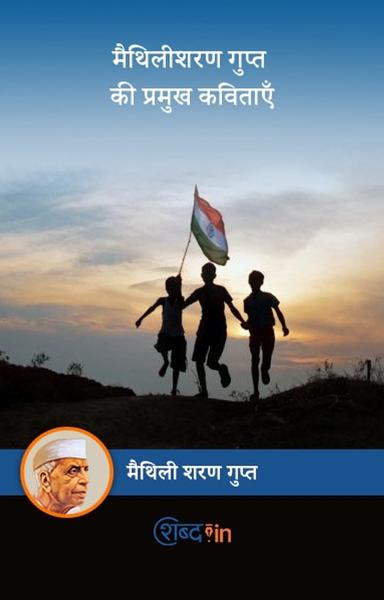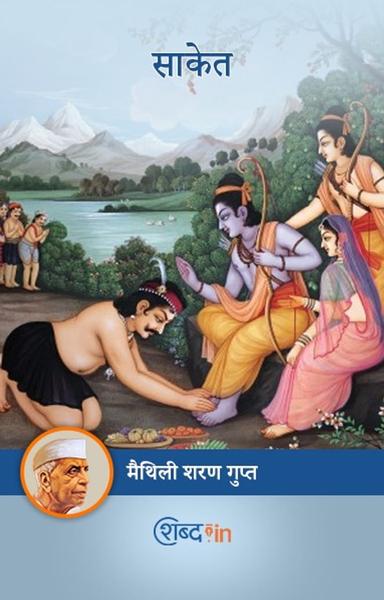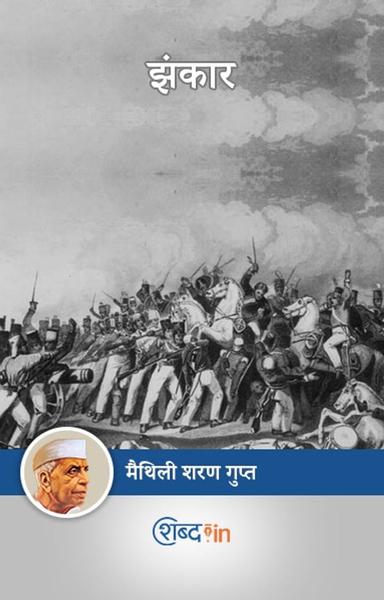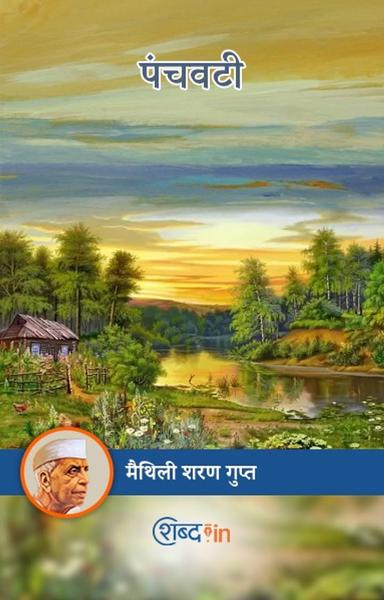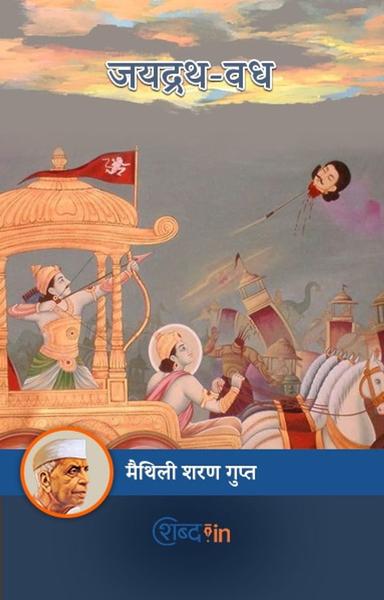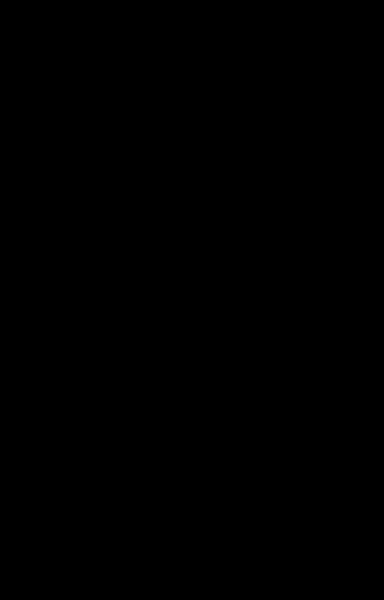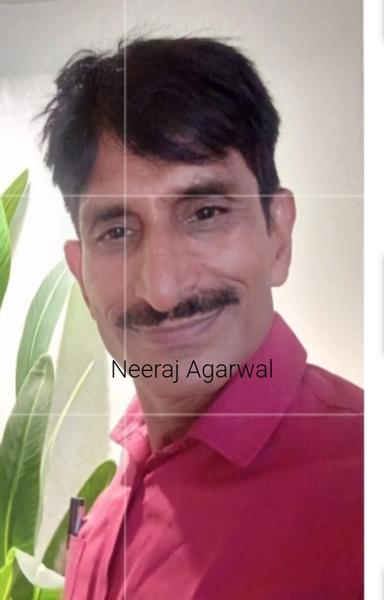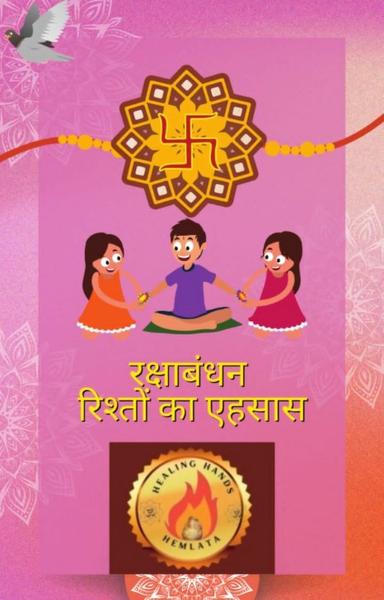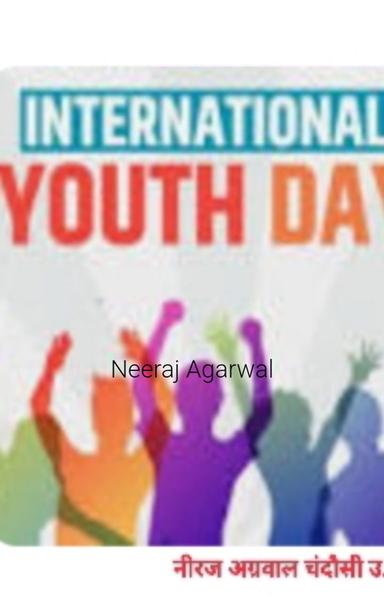हा ! आज शिक्षा-मार्ग भी सङ्कीर्ण होकर क्लिष्ट है,
कुलपति-सहित उन गुरुकुलों का ध्यान ही अवशिष्ट है।
बिकने लगी विद्या यहाँ अब, शक्ति हो तो क्रय करो,
यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूर्ख रह कर ही मरो!॥१३८॥
ऐसी अमुविधा में कहो वे दीन कैसे पढ़ सके ?
इस ओर वे लाखों अकिञ्चन किस तरह से बढ़ सके ?
अधपेट रह कर काटते हैं मास के दिन तीस वे,
पावें कहाँ से पुस्तकें, लावें कहाँ से फीस वे ? ॥१३९।।
वह आधुनिक शिक्षा किसी विध प्राप्त भी कुछ कर सको-
तो लाभ क्या, बस क्लर्क बन कर पेट अपना भर सको !
लिखते रहो जो सिर झुका सुन अफसरों की गालियाँ !
तो दे सकेगी रात को दो रोटियाँ घरवालियाँ ! ॥१४०॥
अब नौकरो ही के लिए विद्या पढ़ी जाती यहाँ,
बी० ए० न हों हम तो भला डिप्टीगरी रक्खी कहाँ ?
किस स्वर्ग का सोपान है तू हाय री, डिप्टीगरी!
सीमा समुन्नति की हमारी, चित्त में तू ही भरी !! ॥१४१।।
शिक्षार्थ क्षात्र विदेश भी जाते अवश्य कभी कभी,
पर वक्तृता ही झाड़ते हैं लौट कर प्राय: सभी !
है काम कितनों का यही पहले यहाँ मिस्टर बने,
इंगलैंड जाकर फिर वहाँ वान्वीर वारिस्टर बने ॥१४२॥
वे वीर हाय ! स्वदेश का करते यही उपकार हैं-
दो भाइयों के युद्ध में होते वही आधार हैं !
उनके भरोसे पर यहाँ अभियोग चलते हैं बड़े,
हारें कि जीतें आप, उनके किन्तु पौबारह पड़े ! ॥१४३॥
जाकर विदेश अनेक अब तक युवक अपने आ चुके,
पर देश के वाणिज्य-हित की ओर कितने हैं झुके ?
हैं कारखाने कौन-से उनके प्रयत्नों से चले ?
क्या क्या सु-फल निज देश में उनसे अभी तक हैं फले?॥१४४।।
अमरीकनों के पात्र जूठे साफ कर पण्डित हुए,
सच्चे स्वदेशी मान से फिर भी नहीं मण्डित हुए!
दृष्टान्त बनते हैं अधिक वे इस कहावत के लिए-
"बारह बरस दिल्ली रहे पर भाड़ ही झोंका किये ! ॥१४५॥
दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहाँ,
हैं मुख्य दो ही जीविकाएँ-मृत्यता, भिक्षा यहाँ!
या तो कहीं बन कर मुहरिर पेट का पालन करो,
या मिल सके तो भीख माँगो, अन्यथा भूखों मरो !॥१४५॥
बिगड़े हमारे अब सभी स्वाधीन वे व्यवसाय हैं,
भिक्षा तथा बस मृत्यता ही आज शेष उपाय हैं।
पर हाय ! दुर्लभ हो रही है प्राप्ति इनकी भी यहाँ,
यह कौन जाने इस पतन का अन्त अब होगा कहाँ !॥१४७।।
वह साम्प्रतिक शिक्षा हमारे सर्वथा प्रतिकूल है,
हममें, हमारे देश के प्रति, द्वेष-मति की मूल है।
हममें विदेशी-भाव भर के वह भुलाती है हमें,
सब स्वास्थ्य का संहार करके वह रुलाती है हमें !! ||१४८||
होती नहीं उससे हमें निज धर्म में अनुरक्ति है,
होने न देती पूर्वजों पर वह हमारी भक्ति है ।
उसमें विदेशी मान का ही मोह-पूर्ण महत्व है,
फल अन्त में उसका वही दासत्व है, दासत्व है !॥१४९।।
हम मूर्ख और असभ्य थे, उससे विदित होता यही,
इस मर्म को कि हमी जगद्गुरु थे, छिपाती है वही ।
"फ्री थाट" हो वह वेद के बदले रटाती है हमें,
देखो, हटा कर असलियत से वह घटाती है हमें ॥१५०||
क्या लाभ है उन हिस्ट्रियों को कण्ठ करने से भला-
रटते हुए जिनको हमारा बैठ जाता है गला ?
हा ! स्वेद बन कर व्यर्थ ही बहता हमारा रक्त है,
सन्-संवतों के फेर में बरवाद होता वक्त है ! ॥१५१॥
दुर्भाग्य से अब एक तो वह ब्रह्मचर्याश्रम नहीं,
तिस पर परिश्रम व्यर्थ यह पड़ता हमें कुछ कम नहीं !
फिर शीघ्र ही चश्मा हमारे चक्षु चाहें क्यों नहीं ?
हम रुग्ण होकर आमरण दुख से कराहें क्यों नहीं ? ॥१५२॥
है व्यर्थ वह शिक्षा कि जिससे देश की उन्नति न हो,
जापान के विद्यार्थियों की सूक्ति है कैसी अहो !-
"साहब ! हमें यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखलाइए,
बेलून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए" ॥१५३।।
करके सु-शिक्षा की उपेक्षा यों पतित हम हो रहे,
हो प्राप्त पशुता को स्वयं मनुजत्व अपना खो रहे।
आहार, निद्रा आदि में नर और पशु क्या सम नहीं ?
है ज्ञान का बस भेद सो भूले उसे क्या हम नहीं ?॥१५४॥
धर्मोपदेशक विश्व में जाते जहाँ से थे सदा,
शिक्षार्थ आते थे जहाँ संसार के जन सर्वदा ।
अज्ञान के अनुचर वहाँ अब फिर रहे फूले हुए,
हम आज अपने आपको भी हैं स्वयं भूले हुए॥१५५॥
अपमान हाय ! सरस्वती का कर रहे हम लोग हैं,
पर साथ ही इस धृष्टता का पा रहे फल-भोग हैं !
निज देवता के कोप में कल्याण किसका है भला,
हम मोह-मुग्ध फँसा रहे हैं आप ही अपना गला ॥१५६॥