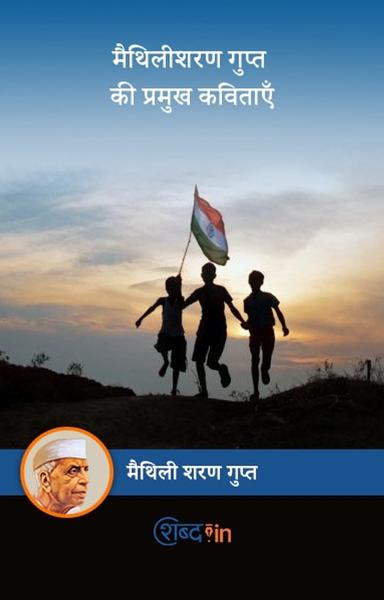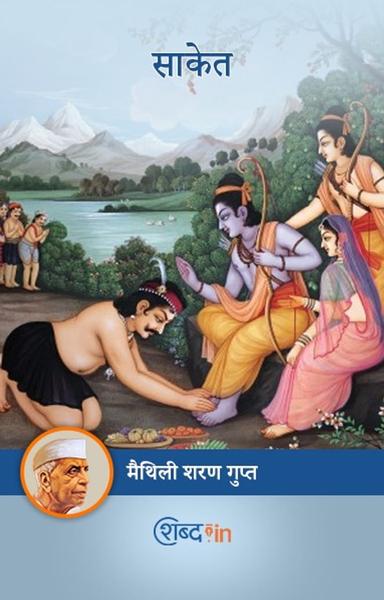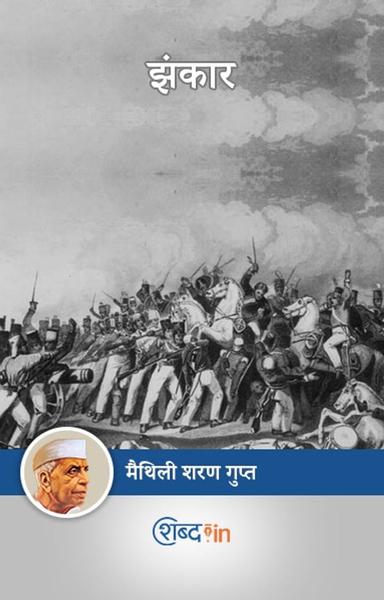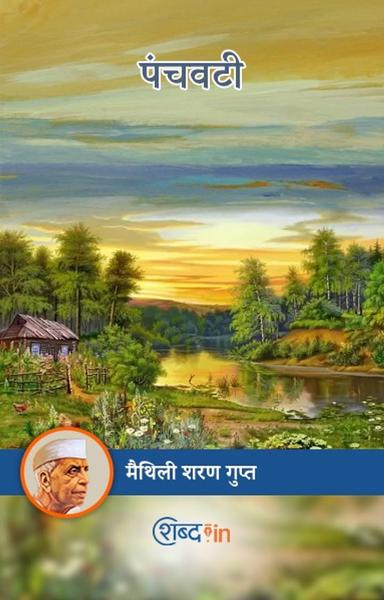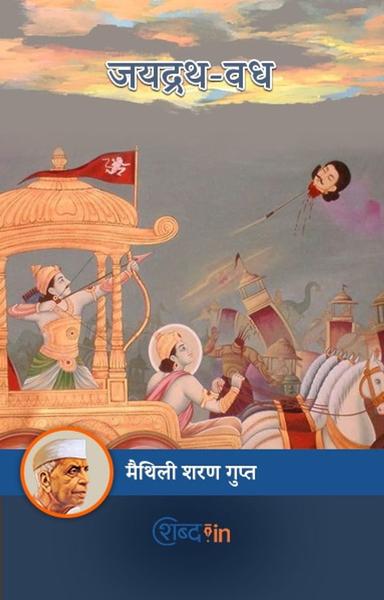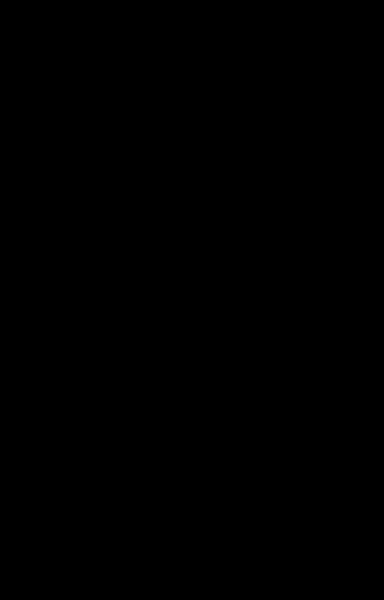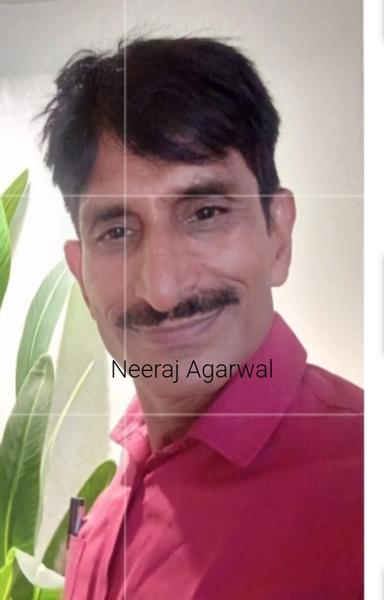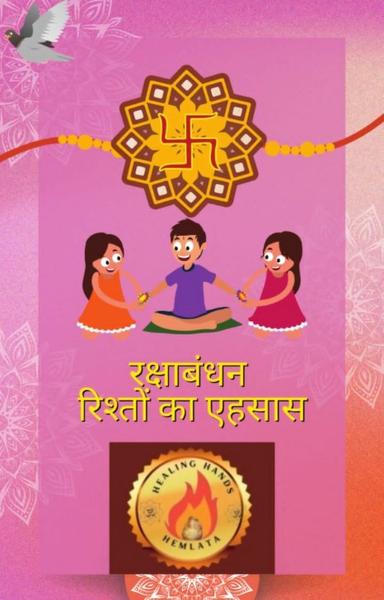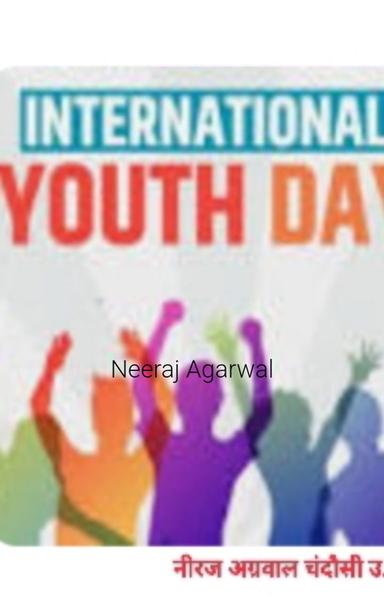व्यभिचार ऐसा बढ़ रहा है, देख लो, चाहे जहाँ;
जैसा शहर, अनुरूप उसके एक 'चकला' है वहाँ ?
जाकर जहाँ हम धर्म्म खोते सदैव सहर्ष हैं,
होते पतित, कङ्गाल, रोगी सैकड़ों प्रतिवर्ष हैं ।।२८२।।
वह कौन धन है, दुर्व्यसन में हम जिसे खोते नहीं ?
उत्सव हमारे बारवधुओं के विना होते नहीं !
सर्वत्र डोंडी पिट रही है अब उन्हीं के नाम की,
मानो अधिष्ठात्री वही हैं अब यहाँ शुभ-काम की !! ॥२८३॥
था शेष लिखने के लिए क्या इस अभागे को यही ?
भगवान् ! भारतवर्ष की कैसी अधोगति हो रही है !
यदि अन्त हो जाता हमारा त्यागते ही शील के ,
तो आज टीके तो न लगते आर्य्याकुल को नील के ।।२८४।।
हा ! वे तपोधन ऋषि कहाँ, सन्तान हम उनकी कहाँ ?
थी पुण्यभूमि प्रसिद्ध जो हा ! आज ऐसा अघ वहाँ !
बस दीप से कज्जल सदृश निज पूर्वजों से हम हुए,
वे लोक में आलोक थे पर हम निविड़तर तम हुए !! ।।२८५।।