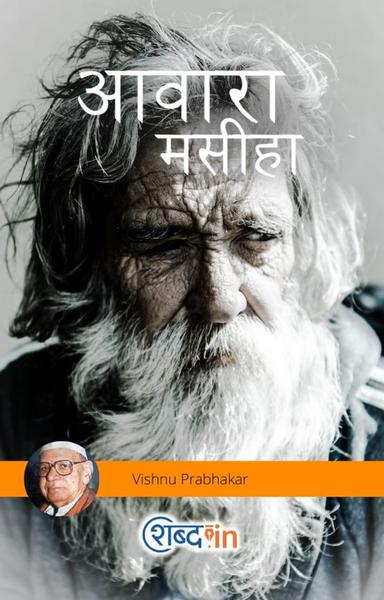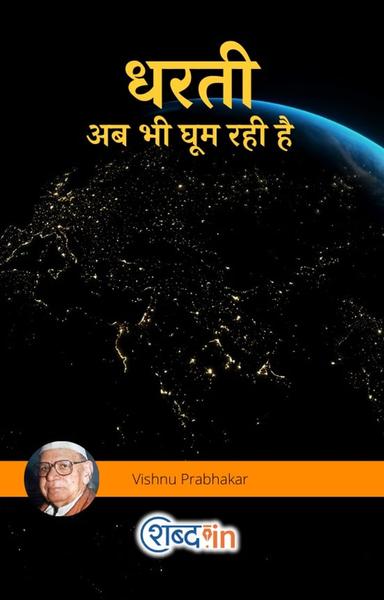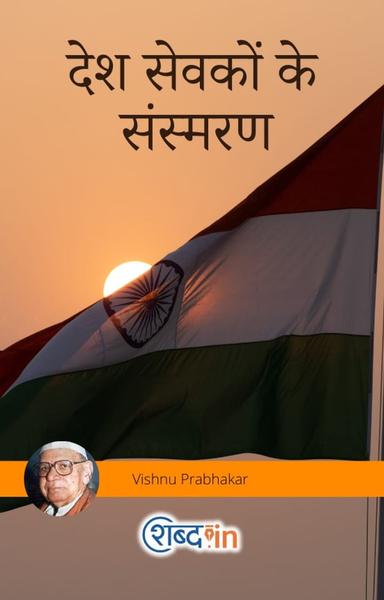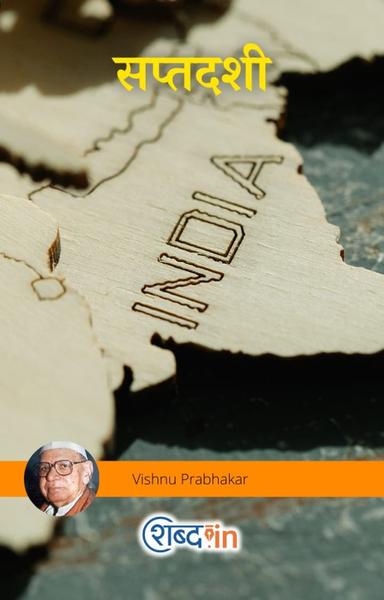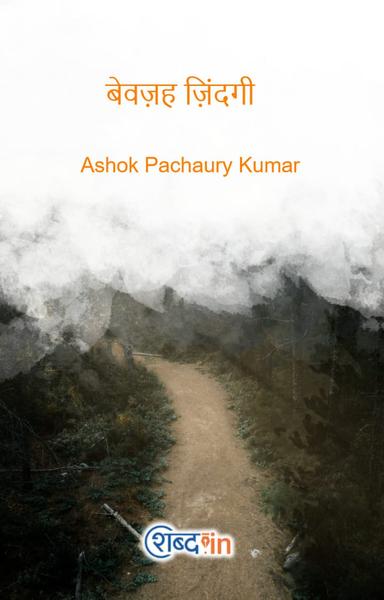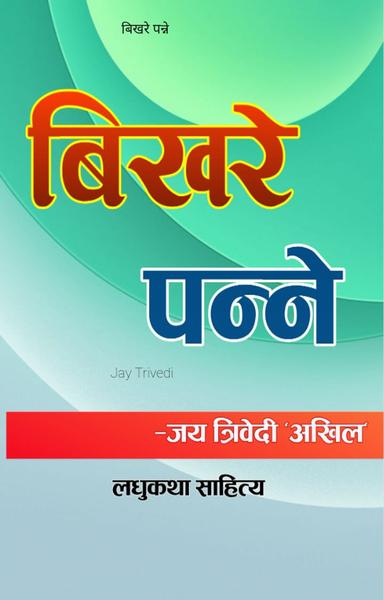इस जीवन का अन्त न जाने कहा जाकर होता कि अचानक भागलपुर से एक तार आया। लिखा था—तुम्हारे पिता की मुत्यु हो गई है। जल्दी आओ।
जिस समय उसने भागलपुर छोड़ा था घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके आने के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। मोतीलाल पागलों की तरह इधर-उधर घूमते रहते। फटी चट्टी, कीचड़ से भरा हुआ बदन, सिर पर बढ़ी हुई जटा, पेट में अन्न नहीं, हाथ में पैसा नहीं ऐसी स्थिति में स्वप्नविहारी मनुष्य पागल ही हो सकता है।
इन्हीं दिनों उनके चचिया ससुर अघोरनाथ भागलपुर आए। दोनों सहपाठी रह चुके थे। मोतीलाल उनसे मिलने ससुराल पहुंचे। खूब शीत पड़ रहा था। बदन पर वस्त्र नहीं था, अघोरनाथ पिता-पुत्र दोनों से खुश नहीं थे। लेकिन बचपन के साथी की ऐसी दशा देखकर वह द्रवित हो आये। पूछा, “तुम यह घर छोड़कर क्यों चले गए मोतीलाल?”
“अच्छा नहीं लगता था, छोटे काका ।”
“इतनी ठण्ड में कपड़ा क्यों नहीं पहनते?" "हैं नहीं।”
“शरत् कहां हे?””
“झगड़ा करके कहीं भाग गया है। "
“आजकल कुछ काम-वाम हे?”
"नही।”
“तब कैसे चलता है?”
मोतीलाल ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। आंखे डबडबा आई, टप टप आंसू गिरने लगे और वह जाने के लिए उठकर खड़े हो गए। तब बदन के वस्त्र उन्हें पहनाकर अघोरनाथ ने एक नोट उनके हाथ में थमा दिया। मोतीलाल के चेहरे पर मुस्कराहट खिल आई। पूछा, “कितने दिन है छोटे काका?"
हैं। "
“कल ही चला जाऊंगा।”
मोतीलाल ने पांव की तरल लेकर कहा, “अब और मिलना नहीं होगा। उम्र पूरी हो गई
सचमुच ही मिलना न हो पाया। कुछ दिनों बाद मन में अजस्त्र प्यार भरे धरती के अयोग्य, स्वप्नदर्शी मोतीलाल विपरीत परिस्थितियों की ठोकरें खाते-खाते जर्जर होकर स्वर्गवासी हो गए।
पिता की मृत्यु का समाचार पाकर शरत् बहुत दुखी हुआ। वह उनसे लडकर आया था और यहां के इस बोहेमियन जीवन में कौन कह सकता है कि उसने उन्हें कितनी बार याद किया था, लेकिन अब जब वह नहीं रहे तो उसे उनके अगाध स्नेह की याद आने लगी। वह उसी क्षण भागलपुर के लिए रवाना हो गया।
उसकी अनुपस्थिति में मामा मणीन्द्रनाथ मे अन्तिम संस्कार किया था । श्राद्ध के अवसर पर भी उसी ने सहायता की। वह उसका सहपाठी था, परन्तु पुरातनपंथी गांगुली परिवार का सच्चा पुत्र भी था। उसे शरत् के जीवन से घृणा थी। फिर भी जिस व्यक्ति के श्राद्ध का प्रश्न था वह गांगुली परिवार का दामाद था। उसी के अनुरूप वह सम्पन्न होना चाहिए। इसीलिए उसने सहायता की।
मां पहले ही चली गई थी। पिता भी चले गए। बड़ी बहन दूसरे घर की थी। शेष रह गए थे, तीन छोटे भाई बहन और वह स्वयं उसे अपनी चिन्ता नहीं थी । चिन्ता थी इन अबोध बालकों की। छोटी बहन सुशीला को मकान मालकिन बहुत प्यार करती थी। उसने उसे अपने पास रख लिया। छोटा भाई प्रभास 11 12 वर्ष का था। शरत् उसे आसनसोल ले गया। वहां उसका एक मित्र रेलवे में काम करता था। काम सीखने के लिए प्रभास को वह उसी के पास छोड़ आया।
अब रह गया प्रकाश, उसे किसके पास छोड़े। कोई भी उसका अपना नहीं था। बहुत सोचा और अन्त में छोटे नाना अघोरनाथ की शरण उसने ली। वह शरत् से बहुत नाराज़ थे। लेकिन शरत् को नानी पर भरोसा था। न जाने कितनी बार उन्होंने शरत् की प्राणरक्षा की थी। प्रकाश को लेकर वह जलपाईगुड़ी पहुंचा। उसने नाना के चरण पकड़ लिए। स्वाभाविक था कि वह पहले कुछ नाराज हुए, लेकिन एक तो मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी थी, दूसरे पत्नी का भी आग्रह था, वह इनकार नहीं कर सके।
छोटी नानी के कारण शरत् की एक बार फिर रक्षा हुई। नाना ने कुछ उपेक्षा के साथ और नानी ने कुछ प्यार के साथ उससे कहा, “अब घर का दायित्व तुम पर है। तुम्हें कुछ करना चाहिए।"
शरत् ने उत्तर दिया, “वही करने जा रहा हूं।"
भाई-बहनों की ओर से निश्चित होकर उसने बिहार को अन्तिम नमस्कार किया और जीविका की तलाश में कलकत्ता पहुंचा। नाते के कई मामा वहां पर रहते थे। उपेन्द्रनाथ से उसकी कुछ घनिष्टता भी थी। उसे भी साहित्य में अनुराग था। एक दूसरे मामा लालमोहन यहां वकालत करते थे। भागलपुर की कचहरी के मुकदमों की अपील कलकत्ता हाईकोर्ट में ही होती थी, लालमोहन वहीं काम करते थे। निश्चय हुआ कि इन्हीं के पास रहकर नौकरी की तलाश की जाए। एक वयस्क व्यक्ति के लिए खर्च पत्ते के वास्ते अभिभावकों के आगे हाथ फैलाने में कुण्ठा होती है। इस कुण्ठा से मुक्तिपाने के लिए शरत् हिन्दी की अर्जियों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने लगा। उसके बदले में उसे खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाते थे।
किन्तु आइन अदालत की भाषा से उसका कोई विशेष परिचय नहीं था, इसलिए इस काम में उसका मन अधिक दिन नहीं लग सक्ता था। इसके अतिरिक्त उसे घर की साग-सब्ज़ी भी लानी पड़ती थी। साधारण नौकरों जैसे और भी काम करने पड़ते थे। अपमान भी कम नहीं होता था। घर के अन्दर जाते समय भागलपुर की तरह यहां भी उसे खांसकर जाना होता था। एक बार वह मामा के ब्रुश से बाल ठीक कर रहा था कि अचानक वे वहां आ गये। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने एक बार शरत् की ओर देखा और फिर उस ब्रुश को उठाकर बाहर फेंक दिया। मानो उन्होंने कहा, “जिस ब्रुश को तुम इस्तेमाल कर चुके हो वह मेरे योग्य नहीं रहा । "
इस घृणा और अपमान के कारण उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। अक्सर सोचता था कि दूसरे के घर पर रहकर ऐसा अपमान पाने से तो सड़क, जंगल, रेगिस्तान कहीं भी रह जाना अच्छा है। उसकी बड़ी बहन कलकत्ते के पास गोविन्दपुर गांव में रहती थी । प्रयत्न किया कि उसके पास जाकर रह सके, गिरीन्द्रनाथ को लिखे एक पत्र से ऐसा लगता है कि वह वहां जाकर रहा भी था। परन्तु वहां भाइयों में झगड़े आरम्भ हो गये थे। इसलिए मुकर्जी महाशय इस स्थिति में नहीं थे कि उसके लिए कुछ कर पाते। उन्होंने पत्नी से कहा, "तुम तो जानती ही हो कि यह गांव है। शरत् का यहां रहना सम्भव नहीं हो सकेगा। गांव के लोग आलोचना करेंगे।”
“तो ...?” अनिला भाई के प्रति करुणा से भर उठी, कुछ कह न सकी।
मुकर्जी महाशय ने कहा, “उसे कहो, कहीं और चला जाए। खर्चे का प्रबन्ध मैं कर दूंगा।”
उन्होंने कुछ सहायता की भी थी, परन्तु उसके लिए कलकत्ता में रहना असंभव हो गया। कहां जाए, यह सोचते-सोचते उसे अपने मौसा अघोरनाथ चट्टोपाध्याय की याद हो आई। वे रंगून में एडवोकेट थे। कई वर्ष पहले वे भागलपुर आये थे तो मोतीलाल से उन्होंने कहा था, “लड़के को कालेज में क्यों भेजते हो? मेरे साथ रंगून भेज दो। पढ़-लिखकर वकील बनने में देर नहीं लगेगी। भविष्य में काफी पैसा भी पैदा कर सकेगा।”
कई कारणों से तब उसका जाना नहीं हो सका था। परन्तु अब उसके सामने जीविका का प्रश्न था । कलकत्ता में बहुत से लोगों ने बर्मा के बारे में उसे नाना प्रकार की कहानियां सुनाई थीं। बताया था कि अमुक व्यक्ति बर्मा में नौकरी करके बहुत धनवान हो गया है। वहां राह-घाट में रुपये बिखरे पड़े हैं। केवल समेटने भर की देर है । जहाज़ से उतरते ही बंगालियों को साहब लोग कंधो पर उठा ले जाते है और नौकरी पर लगा देते हैं।
ये बातें सुन-सुनकर शरत् के भीतर का घुमक्कड़ उसे परेशान करने लगा। वह किसी तरह बर्मा पहुंचने के लिए लालायित हो उठा। इसी समय अचानक अघोरनाथ कलकत्ता आये और लालमोहन के पास ही ठहरे। शरत् को उन्होंने ऐसी-ऐसी रोमांटिक कहानियां सुनाई कि उसने निश्चय कर लिया — अब वह बर्मा ही जाएगा।
ऐसी अनिश्चित और विपरीत, परिस्थितियों में भी उसकी साहित्य साधना मौन रूप से चल रही थी। 'चरित्रहीन' का सृजन आरम्भ हो चुका था। वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, पर शायद उस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। सौरीन्द्र मोहन भी नहीं। भागलपुर का उसका यह पुराना मित्र यहीं रहता था। वह उससे बहुत प्रभावित था। प्रतिदिन संध्या के समय वह शरत के पास आता और फिर दोनों मित्र घूमने के लिए निकल पड़ते। अक्सर वे साहित्य चर्चा करते।
एक दिन सौरीन ने कहा, “शरत्! स्टार थियेटर में क्षीरोदप्रसाद का नाटक 'सावित्री' चल रहा है! तुम उसे अवश्य देखो। "
शरत् उसे देखने गया, लेकिन लौटकर उसने सौरीन्द्र को आड़े हाथों लिया, बोला, “बाप रे बाप, तुम्हें यह नाटक कैसे अच्छा लगा ? सत्यवान के मरने तक तो बहुत बुरा नहीं था। अमृत मित्र ने माण्डव्य का अभिनय भी अच्छा ही किया, लेकिन सत्यवान को जो रूप था, उसे देखकर लगता था कि वह सावित्री का छोटा भाई है। उसके मरने पर सावित्री ने मृत देह को गोद में लेकर गाना गाया। उस अवस्था में क्या कोई मनुष्य गाना गा सकता है?”
सौरीन्द्र ने उत्तर दिया, “उसको तुम ठीक स्वर-लय वाला गाना क्यों मानते हो? उस अवस्था में मनुष्य चिल्लाकर रोता है, 'अजी तुम कहां चले गये? मेरा क्या होगा?' इत्यादि- इत्यादि । शोक के उसी आवेग को नाटककार गान के छन्द के स्वर में प्रकट करता है।
शरत् ने कहा, “ऐसा होने पर भी क्या दो-दो गाने होंगे? एक ही बहुत था। मुझे यह सब बहुत बुरा लगा। गाने से तो करुण रस का श्राद्ध ही हो जाता है। ट्रेजेडी भी उत्पन्न नहीं हो सकती।”
मुजफ्फरपुर का उसका मित्र प्रमथनाथ भट्ट भी यहीं पाथुरेघाटा में राजा सौरीन्द्रमोहन ठाकुर के निजी सचिव के रूप में काम करता था। अक्सर उसके पास जाकर वह अपनी कृतियों पर चर्चा करता। इसके अतिरिक्त सुरेन्द्र और गिरीन्द्र भी अब कलकत्ता में ही पढ़ रहे थे। वे भी उससे मिलने आया करते थे। दिन सहसा गिरीन्द्र ने कहा, “शरत्, तुम 'कुन्तलीन पुरस्कार' के लिए गल्प क्यों नहीं लिखते? पच्चीस रुपये मिलते हैं।"
शरत् ने पूछा, "यह 'कुन्तलीन पुरस्कार' क्या है?"
गिरीन्द्र बोला, “स्वदेशी का युग है। सभी देशप्रेमी स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उन्हें देना चाहिए । 'कुन्तलीन' एक सुगन्धित स्वदेशी तेल है। बहू बाज़ार के एच० बसु उसके निर्माता हैं। इसके प्रचार के लिए ही यह प्रतियोगिता चलाई गई है। नामी लेखक इसका निर्णय करते हैं। ये कहानियां पुस्तक रूप में भी छपती हैं।”
शरत् ने कहा, “स्वदेशी की बात तो ठीक है, लेकिन कहानी लिखना, और फिर पुरस्कार के लिए, मेरे लिए बिलकुल सम्भव नहीं है। इतने बड़े-बड़े लेखकों के सामने मुझे कौन पूछेगा ?”
गिरीन्द्र बोला, “तुम नही जानते। तुम बहुत अच्छी कहानियां लिखते हो। जरूर लिखो। तुम्हें पुरस्कार मिलेगा।”
लेकिन जैसा कि उसका स्वभाव था, वह तुरन्त ही इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। मामा लोग आग्रह करते रहे और वह टालता रहा । आखिर अन्तिम दिन आ पहुंचा। गिरीन्द्र ने फिर कहा, “तुम कहानी क्यों नहीं लिखते? पुरस्कार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कहानी लिखो।”
अन्त में वह लिखने के लिए तैयार है गया। उस दिन उसने जो कहानी लिखी उसका नाम था 'मन्दिर'। उसे समाप्त करते न करते संध्या घिर आई, वह इसलिए गिरीन्द्र को लेकर तुरन्त 'कुन्तलीन' के कार्यालय में पहुंचा। व्यवस्थापक बसु महोदय ने कहा, “अन्तिम दिन के अन्तिम क्षण कहानी लेकर आये हो !”
शरत् बोला, “यदि समय नहीं है तो मैं कहानी लेने के लिए आग्रह नहीं करूंगा।”
बसु मुस्कराये। बोले, “नही, नहीं, अन्तिम क्षण तो है ही। लाओ, मैं कहानी ले लूंगा।” कहानी देकर शरत् ने स्वस्ति की सांस ली। लेकिन उस कहानी पर लेखक के रूप में उसने अपना नाम नहीं दिया था। उसे विश्वास नहीं था कि वह पुरस्कार पा सकेगा। न पाने पर जो लज्जा और व्यथा होती उसी से बचने के लिए वह कहानी उसने अपने मामा सुरेन्द्रनाथ के नाम से भेजी। उससे कहा, “मैंने यह कहानी तुम्हारे नाम से दी है। यदि भाग्य से पारितोषिक मिल जाए तो मोहित सेन द्वारा प्रकाशित रवीन्द्रनाथ की काव्य-ग्रन्थावली मुझे भेज देना।”
शायद यह उसके नाम का प्रभाव था कि जब प्रतियोगिता का फल प्रकाशित हुआ तो प्रथम पुरस्कार बंगाली टोला, भागलपुर के श्री सुरेन्द्रनाथ गांगोपाध्याय को मिला। मित्रों ने उसे हार्दिक बधाई दी, लेकिन उसका मन ग्लानि से भर उठा। वह जानता था कि वह इस यश और बधाई का अधिकारी नहीं हैं। लेकिन जो सचमुच अधिकारी था, वह शरत् तो तब तक कलकत्ता छोड़ चुका था। डेढ़ सौ गल्पों मे प्रथम स्थान प्राप्त करना कम सौभाग्य की बात नहीं थी, लेकिन उदासीन शरत् तो अपने को छिपाने में ही आनन्द पाता था।
रंगून जाने की बात भी उसने किसी से नहीं कही। उसे डर था कि उसके मित्र उसे जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके सामने पूरा जीवन पड़ा था ! उसके भाई-बहन थे। उनका भार अब वह किस पर छोड़ सकता था। उसे किसी तरह जीविका अर्जन करनी ही चाहिए। केवल अपने एक मामा देवी को ही उसने अपने इस निश्चय की सूचना दी थी। उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। किसी तरह उसने किसी से भाड़े के रुपये उधार लिये और एक दिन सवेरे चार बजे भवानीपुर के घर से स्टीमर घाट की ओर चल पड़ा। बस अकेला देवी ही उसके साथ था। भाड़ा चुकाकर उसकी जेब में एक-दो रुपये शेष रह गये। वह नहीं जानता था कि अब वह फिर भारत लौट भी सकेगा या नही इस पलायन के साथ-साथ उसके जीवन रूपी नाटक का एक अंक जैसे समाप्त हो गया। उसकी आयु छब्बीस वर्ष की हो चुकी थी । यौवन का सूय मध्याकाश में था, लेकिन जैसे ठण्डे और घने कुहरे ने उसे आच्छादित कर दिया था 'श्रीकान्त' की तरह दूसरे की इच्छा से दूसरे के घर में वर्ष के बाद वर्ष रहकर वह अपने शरीर को कैशौर्य से यौवन की ओर धकेलता रहा था, लेकिन मन को न जाने किस रसातल की ओर खदेड़ता रहा। उसका वह मन कभी लौटकर नहीं आया।
और इस प्रकार वह उच्छृंखल, आवारा, अर्द्धशिक्षित और धनहीन व्यक्ति किसी बंधुही - लक्ष्यहीन प्रवास के लिए निकल पड़ा।
मां की मृत्यु के बाद उससे कोई यह पूछने वाला भी नहीं था कि तुमने खाया भी है या नहीं। कोई उसकी राह देखता हुआ प्रतीक्षा नहीं करता था। किसी को यह जानने की इच्छा नहीं थी कि उसके पास पहनने को है या नहीं। अपनी इच्छा से वह अभिनय, गाने-बजाने, नाना खेलों, ताम्रकूट आदि के सेवन और सेवा में रस लेता था। यह सभी कार्य नाना के परिवार में न करने योग्य थे। इसलिए अपमान की मात्रा भी बड़ी थी। वह इस अपमान को न पहचानता हो, यह बात नहीं थी। परन्तु वह यह भी जानता था कि धर्मशास्त्र में जिस आचार संहिता की चर्चा है, वह सब युगों के लिए नहीं होती। जैसे युग पलटते हैं, वैसे ही संहिताएं भी पलटती हैं। इसलिए वह अपमान उसकी शक्ति बन गया था। इसीलिए उसके दिशाहारा मन के भीतर जो सौंदर्य और साहित्य सृष्टि के बीज अंकुरित हो चुके थे उनके विकास में यह जीवन सहायक हुआ। उसने दुख को केवल भोक्ता होकर सहा ही नहीं था, दृष्टा होकर देखा भी था।
दासता का अन्त करने वाले राष्ट्रपति लिंकन से उसकी तुलना बहुत संगत नहीं है, परन्तु अपने प्रारम्भिक जीवन में वे दोनों आश्चर्यजनक रूप से कुछ प्रवृत्तियों में समान थे। शारीरिक शक्ति प्रदर्शन, विनोदप्रियता, अध्ययन, कहानी कहने की कला और प्रेम की व्यथा का दोनों को खूब अनुभव था। लार्ड चार्लवुड ने लिखा है, “उसने अराजक विचारधाराओं वाले कुछ लेखकों का अध्ययन किया जिनमें टामसपेन, वाल्तेयर और बोलने प्रमुख थे....... मुर्गे लड़ाना, शारीरिक शक्ति प्रदर्शन, कुन्हाड़ी हथौड़ा या आरे के उपयोगी कौशल या नकल करने की मज़ाकिया प्रवृत्ति इन दिनों बदस्तूर जारी रही। उसमें एकान्तप्रियता या अपने में खो जाने की प्रवृत्ति पनप उठी।.....(प्रियतमा की मृत्यु) का लिंकन पर गहरा और चिरस्थायी प्रभाव पड़ा।
शर की प्रियतमा की मृत्यु तो नहीं हुई थी पर बिछोह सम्पूर्ण था। उस बिछोह का उसके जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उसने कहीं लिखा है, “सच्चा प्रेम मिलाता ही नहीं दूर भी करता है।”
क्या वह इसीलिए तो दूर नहीं जा रहा था?