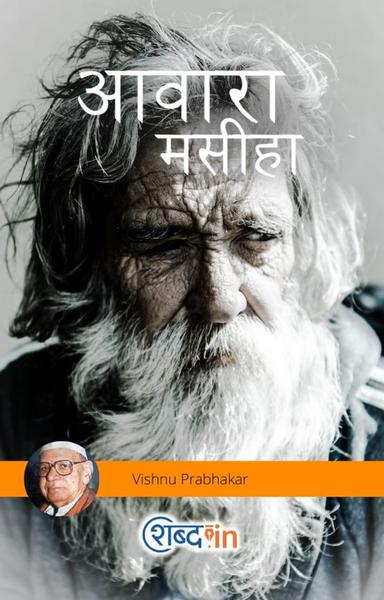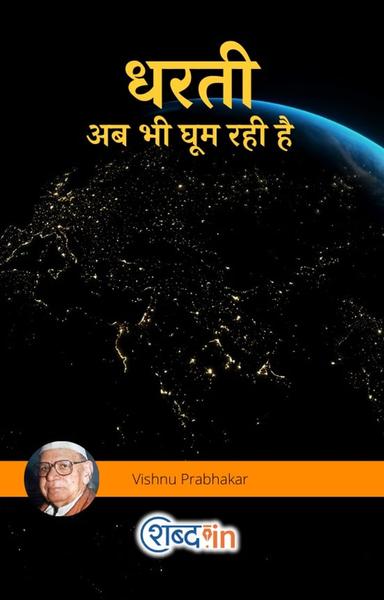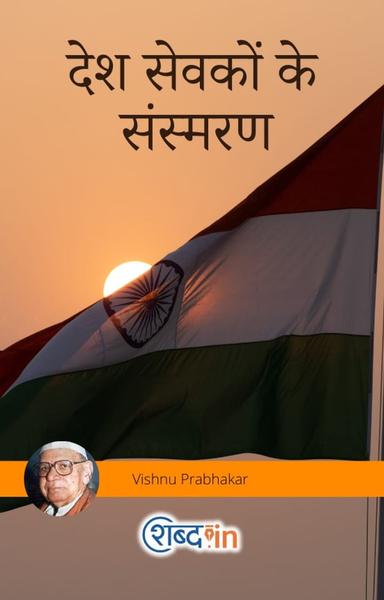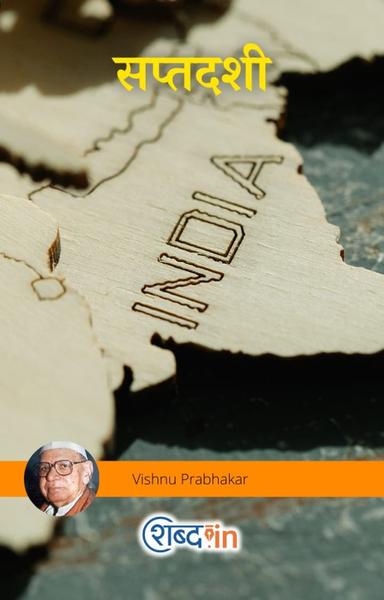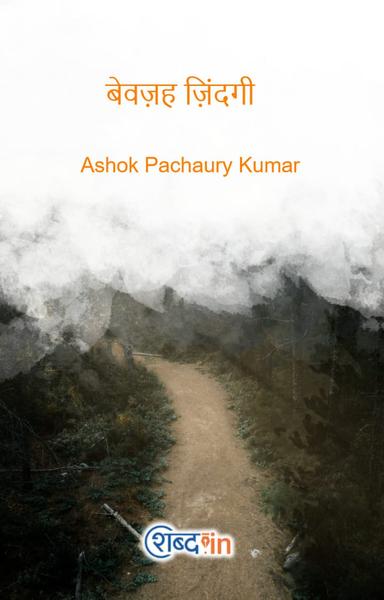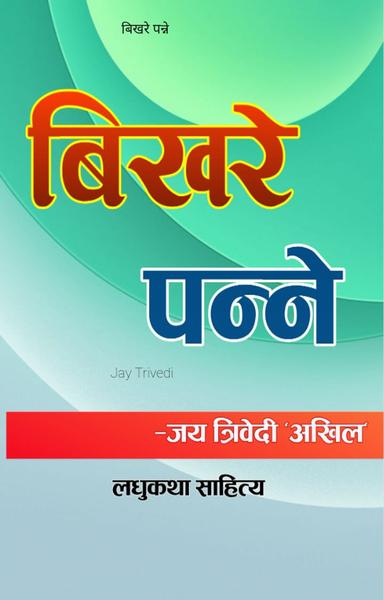वह अपने को निरीश्वरवादी कहकर प्रचारित करता था, लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन वैरागी का मन था। वह बहुत पढ़ता था । समाज विज्ञान, यौन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दर्शन, कुछ भी तो नहीं छूटा था। मणीन्द्रकुमार मित्र के साथ पाश्चात्य दार्शनिकों को लेकर उसकी खूब चर्चा चलती थी। इसी दर्शन प्रेम के कारण वह स्थानीय रामकृष्ण मिशन के स्वामी रामकृष्णानन्द के सम्पर्क में आया। प्रारम्भ में वह वहां मिस्त्री पल्ली के निवासियों के साथ कीर्तन में भाग लेने के लिए जाया करता था। बाद में वह कभी-कभी उनके साथ ईश्वर-संबंधी चर्चा भी करने लगा। उस दिन उसने स्वामीजी से पूछा, “अच्छा, स्वामीजी आप ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते?"
स्वामीजी बोले, “ठाकुर ने कहा है, समुद्र में रत्न हैं, यत्न करने की आवश्यकता है। संसार में ईश्वर है, साधना करनी चाहिए। काई से ढके तालाब के सामने खड़े होकर यदि जल लेना चाहो तो काई को हटाना होगा। इसी प्रकार माया से ढके हुए नेत्र लेकर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। सबसे पहले माया से मुक्त होना है।”
शरत् ने जिज्ञासा की, “माया क्या चीज़ है?”
स्वामीजी बोले, “विषय, वस्तु और कामिनी - कंचन में डूबे रहना ही माया है। इनके मोह को छिन्न-भिन्न करके सरलप्राण होकर पुकारने पर मन शुद्ध होगा। उसकी दया होगी।” शरतचन्द्र ने पूछा, “सुना जाता है वे मंगलमय हैं। ऐसा होने पर पृथ्वी पर इतना दुख क्यों है?"
स्वामीजी मुस्कराए, उत्तर दिया, “इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है। वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है। दुख ही सबसे बढ़के इस पृथ्वी की प्रिय वस्तु है। नहीं तो उसको याद ही क्यों करोगे। उसकी महिमा की उपलब्धि का अवसर कैसे पाओगे?”
शरत् सहसा अनमना हो उठा। कई क्षण बाद बोला, “अच्छा, अदृष्ट दैव और पुरुषकार का अर्थ क्या है?”
स्वामीजी बोले, “पूर्व जन्म में अर्जित फल का नाम अदृष्ट है। अवश्य ही वर्तमान जीवन के कुछ अंशों का उसके साथ सम्बन्ध है, जिसको हम चलती भाषा में कर्म कहते हैं। दैव तथा पुरुषकार, दोनों एक ही हैं। एक को छोड़कर दूसरे की गति नहीं। इसलिए दैव की साधना में पुरुषकार आवश्यक है। इसी तरह पुरुषकार साधना में दैव या भगवत्कृपा आवश्यक है।"
शरत् फिर मौन हो गया। कई क्षण बाद बोला, “गेरुवा वस्त्र बिना पहने क्या संन्यासी हुआ जा सकता है?"
स्वामीजी ने उत्तर दिया, "धर्म का सम्बन्ध मन से है। गेरुआ न पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। मनुष्य मन से ही बन्धन में आता है। मन के कारण ही मुक्त होता है। इसलिए पहले मन चाहिए, बाद में बाहर की सहायता । मन यदि अच्छा है तो बाहर के गेरुए वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं तो ढोंग की ही सृष्टि होगी।" 1
इसी प्रकार यह विचार विनिमय दिन पर दिन चलता रहता था और सब व्यसनों के बावजूद उसका वैरागी मन चुपचाप सच्चे ईश्वर की खोज की ओर उन्मुख होता आ रहा था। सहसा तभी रंगून में प्लेग फूट पड़ी। मित्र महोदय के घर भी चूहे मरने लगे। वह भय से कांप उठे और तुरन्त वह घर छोड़कर शहर से दूर एक छोटे से घर में रहने चले गये । शरत् उनके साथ नहीं जा सका। वह दफ्तर के बाबुओं के मेस में जाकर रहने लगा।
प्लेग का यह आक्रमण इतना भयानक था कि हर व्यक्ति किसी दूसरे की चिन्ता किए बिना भाग खड़ा हुआ। रोगी अकेल तड़प-तड़प कर समाप्त होने लगे। शरत् असहाय लोगों की सहायता करने में सदा आगे रहता आया था। यहां भी आगे रहा। जहां 'पिलेग' शब्द सुनकर बड़े से बड़ा साहसी भी अपने प्रिय से प्रिय जन को छोड़ देता था, वहां शरत् एक अजनबी के पास भी पहुंच जाता था। औषधि आदि खरीद देने तक में उसे संकोच नहीं होता था। राजू की पाठशाला में मानवीय करुणा का जो पाठ उसने पढ़ा था, उसे वह कभी भूल नहीं सका।
न जाने कैसे-कैसे अनुभव उसे हुए और वर्षों बाद ये ही अनुभव चित्र प्रस्फुटित हुए 'श्रीकान्त' में। अचानक एक दिन उसे भी बुखार हो आया। उसका साथी पहले ही रोगग्रस्त हो चुका था। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के सिर पर आइस बैग रखते रहे, लेकिन साथी की अवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही थी । बीच-बीच में उसे होश आ जाता था। अपना अन्त निकट जानकर उसने शरत् से कहा, "मेरे ट्रंक में कुछ गिन्नियां हैं, वे मेरी पत्नी को भेज देना।”
शरत् को विश्वास था कि मेस के दूसरे लोग उनकी सहायता करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। डरते-डरते उसने बराबर के कमरे में झांका, पाया कि दो व्यक्ति तकिये पर सिर रखे सोए पड़े हैं। लेकिन वह नींद हज़ार चिल्लाने पर भी अब टूटने वाली नहीं थी। लौटकर अपने साथी को देखा तो वह छटपटा रहा था। दो क्षण बाद वह भी सो गया। यह सोना भी वैसे ही था, जिसमें जागा नहीं जाता।
उस रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन पुलिस को बुलाने, तार देने और शवदाह की व्यवस्था करने में संध्या हो गई । तबियत अब भी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन जाये तो कहां जाये? सौभाग्य से उसका बुखार प्लेग का बुखार नहीं निकला। कुछ दिन बाद वह ठीक हो गया। लेकिन ये दिन उसने कैसे और कहां बिताये, कोई भी ठीक-ठीक नहीं जानता ।
जहां निम्न वर्ग के लोग रहते थे, बीच-बीच में वह वहीं मिस्त्री पल्ली में जाकर रहता था। उसके अन्तर का हीन भाव उसे सभ्य समाज से दूर इन तथाकथित छोटे लोगों के बीच में ही आनन्द देता था। देश में वह जाति - बहिष्कृत था। उसके रिश्तेदार उसे अपनाने से हिचकते थे। भद्र लोगों की दृष्टि में वह चरित्रहीन था। यहां भी उच्च वर्ग के बंगाली उससे नफरत करते थे। वे मानते थे कि ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, जो अधार्मिकता और अधःपतन की ओर ले जाते हों । निश्चय ही उसके अन्तर में उनसे बदला लेने की भावना जाग उठी थी। इसीलिए वह निम्न वर्ग के लोगों को और भी अधिक प्यार करने लगा था।
उसकी इस प्रवृत्ति से अध्ययन और लिखने की रुचि को बहुत बल मिला। दफ्तर के बाद वह चुपचाप वहा की सुप्रसिद्ध बनार्ड लाइब्रेरी के एक कोने में जाकर बैठ जाता और पढ़ता रहता। उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी । किस अलमारी में, कौन-सी किताब, कहां रखी है; वह यह जानता था। एक-एक पुस्तक उसने पढ़ डाली थी। एक-एक पुस्तक को वह इस तरह प्यार करता था मानो वह उसकी अन्तरंग मित्र हो । इन दिनों तास्ताय उसका प्रिय लेखक था। विशेषकर 'अन्नाकेरिनिना' और 'रिज़रेक्शन' का प्रणेता होने के कारण। 'अन्नाकेरिनिना' तो उसने पचास बार पढ़ी थी। इस साधना की छाप उसके साहित्य पर स्पष्ट देखी जा सकती है। 'नारी का मूल्य', 'नारी का इतिहास', इनकी सामग्री उसने यहीं से एकत्रित की थी।
जब वह सदा के लिए कलकत्ता जा रहा था तब उसने कहा था, “मैं इस लायब्रेरी के कारण ही रंगून छोड़ना नहीं चाहता । कलकत्ता की इम्पीरियल लायब्रेरी में इतनी स्वतंत्रता कहां मिलेगी?”
'अधिकार' में जो कवि है उसके बारे में सव्यसाची कहता है, 'तुम लोग कोई उसे पहचानती नही, भारती, उस जैसा वास्तविक गुणी आदमी सहसा कहीं ढूंढ़े नहीं मिल सकता। अपने टूटे बेहाला मात्र की पूंजी से ऐसी कोई जगह नहीं, जहां वह न गया हो । इसके सिवा बड़ा भारी विद्वान है वह कहां किस पुरतक में क्या लिखा है, उसके सिवा हम लोगों में और कोई आदमी ऐसा नहीं जो बता सकता हो।"
शरत् को भी कौन पहचानता था!
इन्हीं दिनों वह 'चरित्रहीन' लिख रहा था । यद्यपि उसका आरम्भ भारत में ही हो चुका था, लेकिन मेस जीवन की अभिज्ञता उसे यहीं प्राप्त हुई । 'चरित्रहीन' का नायक सतीश मेस में ही रहता है। दिन-भर के काम के बाद जब रात को लालटेन जलाकर वह लिखने बैठता तो उसके संगी-साथी बहुत चिढ़ते । चिल्ला-चिल्लाकर कहते, "देखो, देखो, यह बनेंगे लेखक। आधी रात में लालटेन जलाकर बैठे हैं। उहूं, पचास रुपल्ली के क्लर्क और ख्वाब देखते हैं लेखक बनने के। यह मुंह और मसूर की दाल।”
और वे ठहाका मारकर हंस पड़तें । लालटेन बुझा देते। कभी-कभी बकाबकी भी हो जाती। यह सब देखकर एक दिन उसने स्थायी रूप से मिस्त्री पल्ली में जाकर रहने का निश्चय कर लिया। वह स्थान शहर से दो मील दूर 'बोटाटांग पोजान डंग' रोड पर था। धान, काठ, डॉकयार्ड और ढलाई के कारखाने के अनेक बंगाली मिस्त्री वहां रहते थे। उसका मकान सड़क के किनारे पर ही था। उस पार विस्तृत मैदान फैला पड़ा था। जहां उसका अन्त होता था वहां से आरम्भ होती थी अर्द्धचन्द्राकार पोजान डंग की खाड़ी। यह दृश्य बहुत ही सुन्दर था। बालकनी में खड़े होकर देर तक वह उस दृश्य में डूबा रहता ।
यहां आने पर मित्र मंडली से उसका सम्बन्ध बहुत कम हो गया। जो बहुत अंतरंग थे वे ही यहां आ पाते थे, नहीं तो मिस्त्री पल्ली के कारीगर ही उसके साथी थे। वे आपस में खूब लड़ते-झगड्ते और शरत् को उनका पंच बनना पड़ता । छुट्टी के लिए प्रार्थना-पत्र, घर भेजने के लिए चिट्ठी और मनीआर्डर, सब लिखना जैसे उसका नियम हो गया था। जब वे लोग बीमार हो जाते तो वह होम्योपैथ दवाओं का बैग उठाकर घर-घर उनकी परिचर्या करता फिरता ।
लेकिन अभी यहां रहते हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उसका मित्र बंगचन्द्र दे बीमार हो गया। बहुत समय तक शरत् उसके साथ मेस में रहता रहा था। वह उसके उन कुछ मित्रों में से था, जिन्हें वह केवल प्यार ही कर सकता था। वह पूर्वी बंगाल का रहने वाला एक उच्च शिक्षाप्राप्त और अध्ययनशील व्यक्ति था । अंग्रेज़ी पत्रों में उसके लेख छपते थे, लेकिन ज्ञान की प्यास उसकी जितनी अनन्त थी, शरीर की प्यास भी उतनी ही उग्र थी। जितनी मुक्तता से वह हास-परिहास में रस लेता था, उतनी ही मुक्तता से शराब भी पीता था। दोनों प्रकार इन समान गुणों के कारण उन दोनों में गहरी प्रीति हो गई थी।
शरत् बंगचन्द्र को देहाती बंगाली कहकर चिढ़ाता और तब बंगचन्द्र खूब बकाबकी करता। बंगचन्द्र नवीनचन्द्र का परमभक्त था और शरत् उपासक था कविगुरु रवीन्द्रनाथ का। दोनों की कविताओं को लेकर उनके वाद विवाद का अन्त ही नहीं आता था। लेकिन जब शरत् तर्क न करके कविगुरु की यह कविता पढ़ता - "तोमार कथा हेथा केहो तो बॅले ना करे शुधू मिछे कोलाहल सुधा सागरेर तीरेते बसिया, पान करे शुधू हलाहल । “ तो बंगचन्द्र मौन हो जाता।
पूर्व और पश्चिम बंगाल की प्रतिस्पर्धा सर्वविदित है, लेकिन इसी कारण उन दोनों में कभी एक क्षण के लिए भी मनमुटाव नहीं हुआ। बकाबकी, हास-परिहास, पीना - पिलाना और गहन दार्शनिक विषयों पर वाद-विवाद सब एक साथ और समान रूप से चलता था। बंगचन्द्र ने शरत् की प्रतिभा को पहचान लिया था और शरत् बंगचन्द्र के ज्ञान से प्रभावित था, परन्तु उनकी अटूट मित्रता का कारण थी उनकी निविड़ मानवता ।
इसलिए बंगचन्द्र की बीमारी का समाचार पाकर शरत् तुरन्त मेस पहुंचा। रोग सचमुच सांघातिक था। आस-पास के सभी बन्धु बान्धव उसे छोड़कर चले गये थे, लेकिन शरत् ने जी-जान से उसकी सेवा की। वह ज़रा स्वस्थ हुआ तो अपने घर ले आया। अकेला था, उसके लिए दवा लाता, पानी गर्म करके सिकाई करता, साबूदाना बनाकर खिलाता और इस सबके बीच में हास-परिहास तथा बकाबकी का क्रम भी अबाध गति से चलता रहता । परन्तु इतना कुछ करके भी वह अपने मित्र के प्राण नहीं बचा सका । एक दिन उसकी गोद में सिर रखकर बंगचन्द्र दे ने उसकी ओर देखते हुए सदा के लिए अपने नेत्र मूंद लिए। अपने इस प्रिय मित्र की मृत्यु से शरत् बहुत दुखी हुआ। उस दिन उसके हृदय पर एक बार फिर मर्मान्तक चोट लगी। समाप्त हो गया हास-परिहास और गाना बजाना । रह गया केवल एकाकीपन, चिन्तन और साहित्य-सृजन । वैरागी मन और वैरागी हो उठा।