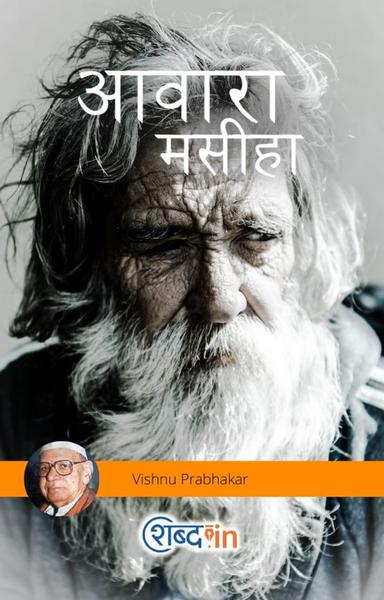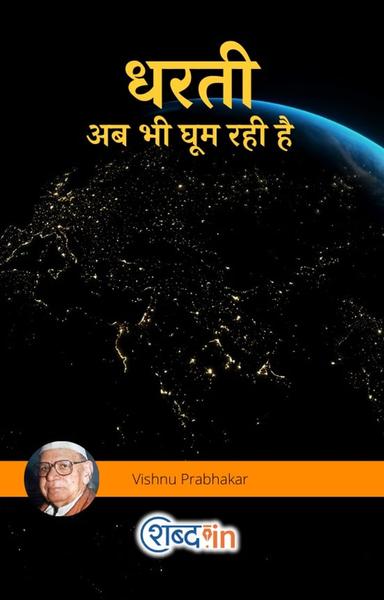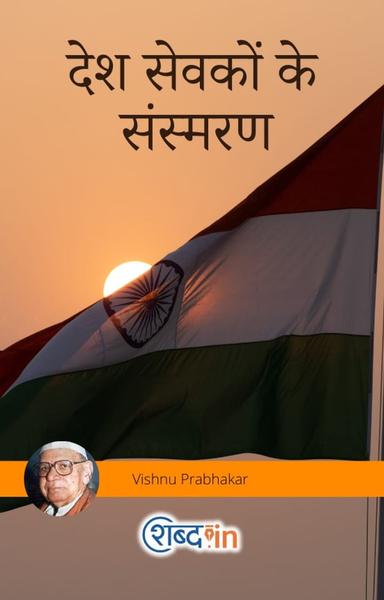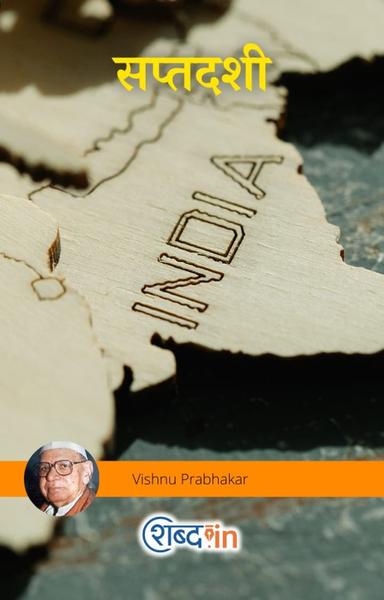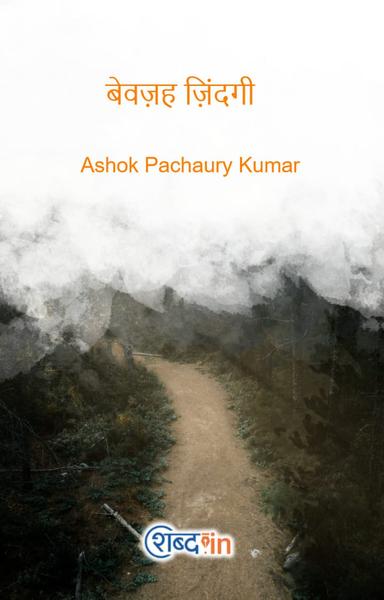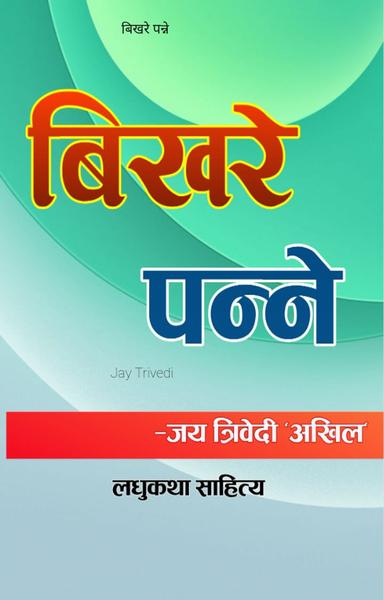अपनी रचनाओं के कारण शरत् बाबू विद्यार्थियों में विशेष रूप से लोकप्रिय थे। लेकिन विश्वविद्यालय और कालेजों से उनका संबंध अभी भी घनिष्ठ नहीं हुआ था। उस दिन अचानक प्रेजिडेन्सी कालेज की बंगला साहित्य सभा के सम्पादक ने निश्चय किया कि इस बार अवश्य कुछ नया करके दिखाना है। सभी लोग 'शरत् ग्रंथावली' पढ़ते हैं। क्या उन्हीं शरत् को नहीं बुलाया जा सकता?
बस एक दिन दो विद्यार्थी पहुंचे बाजे शिवपुर । किसी तरह कुते की यातना से मुक्ति पाकर देखा कि घर के संकरे बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटा नंगे वदन एक व्यक्ति हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। एक साड़ी को लुंगी की तरह बांधे हुए है। जनेऊ माला की तरह गले में अटका है। खिचड़ी बाल कंधे तक आ गए हैं। दोनों ने नमस्कार किया। उत्तर में दो तीक्षा आखें उठी । शुष्क गले से पूछा, "कहां से आना हुआ?
"प्रेजिडेन्सी कालेज से।”
"क्या काम है?. "
बेचारे विद्यार्थी इस शुष्क व्यवहार के लिए शायद प्रस्तुत नहीं थे । प्रयोजन बताया कि साहित्य सभा का अध्यक्ष बनाने की प्रार्थना लेकर आए हैं। शरत् बाबू ने तुरन्त इंकार कर दिया, “मैं किसी सभा-वभा में नहीं आता। उस दिन एक स्कूल के लोग आये थे, मैं नहीं गया।"
विद्यार्थियों को जैसे आघात लगा । बोले, हम किसी स्कूल से नहीं आए, प्रेजिडेन्सी कालेज से आए हैं।"
शरत् बाबू ने कहा, 'एक ही बात हैं। वह छोटा स्कूल है, तुम्हारा बड़ा हो सकता है किन्तु.. .. वहां जाकर मैं क्या करूंगा ? बंगाल में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर मुझे बोलना नहीं आता। एक काम करो। जलधर सेन को ले जाओ। वह साहित्यकार भी हैं और रायबहादुर भी।"
विद्यार्थियों ने समझाने की चेष्टा की कि उन्हें न रायबहादुरी से प्रेम है और न सामाजिक प्रतिष्ठा से वे 'उनके कारण' ही उनके पास आए हैं।
हों?"
अब शरत् बाबू ने कुछ गम्भीर होकर कहा, “क्या तुम मेरी पुस्तक उस्तक भी पढ़ते
"तुरन्त एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, “आप अपनी कोई भी पुस्तक ले लें। कहीं से पूछ लें। सब याद है।"
शरत बाबू ने कहा, "मैं तो समझा था पढ़े-लिखे लड़के हो । बंगला नहीं पढ़ते होंगे। 'कांटिनेण्टल लिटरेचर' पढते होंगे। शिक्षित वर्ग में आजकल वही व्यापार चलता है।"
वह युग कांटिनेण्टल साहित्य का ही था। पर विद्यार्थियों ने कहा, आप ठीक खबर नहीं रखते। तरुण समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है।"
और तरुणोचित आवेश में वे न जाने क्या-क्या कहते रहे और वे चुपचाप सुनते रहे। उनके चुप होने पर भी वे कई क्षण चुप रहे। फिर बोले, “मैं तो यह नहीं समझता था। मेरे पास तुम्हारे जैसे विद्यार्थी कहां आते हैं? बड़े-बड़े लोग आते हैं। कहते हैं, 'यह करो, यह मत करो। बंकिम ने जैसे पाप के क्षय और पुण्य की जयपताका फहराई है, ऐसा ही आप भी करो। आप पाप को ऐसे अंकित करते हैं जैसे वह कोई बहादुरी हो । “
ऐसे पथ प्रदर्शन से उन्हें बडी चिढ थी। वह अपनी स्वाधीन चिन्ताधारा पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं चाहते थे और न स्वयं ही किसी का रहबर बनने की उनकी इच्छा थी। इसीलिए सभा सोसाइटियों में जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था पर आज वार्ताका क्रम कुछ ऐसा चला कि कुछ क्षण बाद नरम होकर वह बोले, “अच्छा आ जाऊंगा । किन्तु क्या बोलना होगा?"
"जो आप चाहें। "
“बहुत भीड तो नहीं होगी?"
“भीड कहां? केवल हम ही होंगे?"
"अच्छा ठहरो । तारीख लिख लूं।"
दीवार पर लगे कलेण्डर में तारीख अंकित करने के बाद वे सहज स्नेह से बाते करने लगे। अपने अतीत की न जाने कितनी कहानियां उन्होंने उन दोनों विद्यार्थियों को सुनाई। एक ने पूछा “लोग कहते हैं, 'श्रीकान्त ' आपकी जीवनी है, क्या यह सत्य है?"
शरत् हंसे बोले, "तुम क्या कहते हो?"
“हम कैसे जानेंगे, हम तो पूछते है।"
वह फिर गम्भीर हो गए। कहा, “उपन्यास लिखने बैठने पर कोई हूबहू अपनी कथा नहीं लिखता । उसी तरह अपने को छोड़कर कोई सार्थक सृष्टि भी नहीं होती। “
विद्यार्थी ने फिर पूछा, “आपके साहित्य में पतिताएं बहुत हैं। इसका क्या कोई विशेष कारण है?"
सहसा वे अनमने हो उठे। उनकी तीक्षा दृष्टि उदासी से भर आई। नली मुंह से निकालकर हाथ में ले ली। कहा, नहीं जानता, विशेष कारण क्या है। मैं बहुतों को जानता हूं। अपनी आखों से देखा है। उनमें ऐसी वस्तु है जो बड़ों-बड़ों में नहीं है। त्याग, धर्म, दया, माया, प्रेम, मनुष्य में जो कुछ अच्छा है, उसका उनमें अभाव नहीं है। भद्रता के मोह में पड़कर इसे अस्वीकार करूं तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? कोई मनुष्य केवल काला ही है, उसमें कोई सुधरने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं होता। '
वे जैसे कहीं खो गए थे। इस तरह बोल रहे थे, जैसे अपने से ही बातें कर रहे हों। किसी ने उनके कमरे की दीवार पर बदूक और रुद्राक्ष माला को एक साथ देखकर कहा था, "इसी आपात असंगति में शरत्चन्द्र के व्यक्तित्व और साहित्य साधना का रहस्य छिपा है। '
लेकिन फिर भी क्या सहजभाव से वे उस सभा में जा सके। ठीक समय पर 'ना' कर बैठे। किसी तरह अनुनय-विनय, आवेदन निवेदन और अन्त में विक्षोभ-प्रदर्शन के बाद ही उन्हें ले जाया जा सका। वहां भीड़-सी भीड़ थी। उनको देखने को लोग पागल रहते थे, पर वे थे कि आतंकित हो उठे। बोले, 'यह क्या किया? इतने मनुष्य!'
लेकिन जब खड़े हुए तो अपनी रचना-प्रक्रिया और साहित्य सृजन की पृष्ठभूमि की विस्तार से चर्चा करते हुए तरुणों को अपना पृष्ठपोषक स्वीकार किया।
तरुण विद्यार्थी उन दिनों देशभक्ति और क्रान्ति की भावना से भरे हुए थे। शरत्चन्द्र में उन्होंने न केवल एक प्रसिद्ध लेखक को देखा बल्कि एक ऐसे क्रान्तिकारी को भी पाया जो उनका पथ-प्रदर्शक बन सकता था। केवल तरुणों ने ही नहीं, उस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी जगत्तारिणी स्वर्णपदक देकर उनका सम्मान किया। इससे पहले केवल रवीन्द्रनाथ ही यह सम्मान प्राप्त कर चुके थे। वे केवल एफ०ए० तक पड़े थे, परन्तु विश्वविद्यालय ने एक बार उन्हें बी०ए० परीक्षा के बंगला भाषा के प्रश्नपत्र का रचयिता भी नियुक्त किया था।
इसी समय योरोप से यह समाचार आया कि इस वर्ष नोबल पुरस्कार किसी भारतीय को मिलने वाला है। डा० सर मोहम्मद इकबाल और श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ शरत्चन्द्र का नाम भी लोगों की जिहा पर था। इसी बात की चर्चा करते हुए इलाचन्द्र जोशी ने एक दिन उनसे पूछा, "यह सब सुनकर आपको कैसा लगता है?"
शरत् बाबू ने उत्तर दिया, 'यदि पुरस्कार मिल गया तो अच्छा ही है और न भी मिला तो मुझे कोई विशेष खेद नहीं होगा। संसार के सभी प्रतिभाशाली लेखकों को नोबल पुरस्कार मिल ही जायेगा यह निश्चित नहीं है। फिर भी यह बात माननी पड़ेगी कि यह पुरस्कार किसी भी लेखक के लिए प्रलोभनीय है। "
जोशीजी ने पूछा, प्रलोभनीय किस अर्थ में?
"शरतचन्द्र बोले, "जिसे यह पुरस्कार मिल जाता है, उसकी ख्याति सारे संसार में फैल जाती है और इतनी बड़ी ख्याति का प्रलोभन न हो ऐसा कोई कवि या लेखक हो सकता है, यह मैं नहीं मानता। मैं इतना बड़ा ढोंगी नही बनना चाहता कि तुझसे कह दूं कि मुझे इसका कोई भी प्रलोभन नहीं है। "
सम्मान बढ रहा था। साथ ही सभा समितियों में बुलाने का आग्रह भी। अगले वर्ष उन्होंने बंगीय साहित्य परिषद नदिया शाखा के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कृष्णनगर में हुआ। वहां वे श्री ललितकुमार चटर्जी के निवास स्थान पर ठहरे थे। चटर्जी महोदय एक सुप्रसिद्ध वकील ही नहीं थे सर आशुतोष मुकर्जी के समधी भी थे।
नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय भी कृष्ण नगर के ही रहने वाले थे। इसलिए दिलीपकुमार भी ललित बाबू के मित्र थे। उन्हीं के कारण शरत् बाबू इस अधिवेशन की अध्यक्षता करन के लिए तैयार हुए थे। स्वीकृति के बाद भी उन लोगो को आशा नहीं थी कि वे आ ही जायेंगे । फिर भी ठीक समय वे लोग शरत् बाबू को लेने के लिए स्टेशन पर आए। नगर के और भी अनेक सम्भ्रान्त व्यक्ति साथ में थे। ट्रेन आई, यात्री उतरे लेकिन शरत् बाबू किसी भी कम्पार्टमेण्ट के द्वार पर दिखाई नहीं दिए। अन्दर ढूंढने पर पाया कि वे एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए शान्त भाव से गुड़गुड़ी पी रहे हैं। सामने नौकर खड़ा है। जो अब तक चिन्तामग्न थे, वे सब व्यक्ति प्रसन्न हो उठे। बड़े आदर से उन्हें नीचे उतारा और विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया।
ललित बाबू के घर पर ही बहुत-से लोग आ गये थे। शरत् बाबू दिन भर हुक्का और चाय पीते रहे। कहानियां सुना सुनाकर सबको हंसाते रहे। सभी को उन्होंने व्यस्त रखा। दूसरे दिन भी इस क्रम में कोई व्याघात नहीं पड़ा। ललित बाबू जानना चाहते थे कि उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण लिख लिया है या नहीं। पता लगा, नहीं लिखा है। उन्होंने दिलीपकुमार से कहा “जानते हो, ये बहुत नर्वस स्वभाव के व्यक्ति हैं। भीड़ का सामना नहीं कर सकते। अब यह देखना तुम्हारा काम है कि ये अपना अध्यक्षीय भाषण लिख लेते हैं।”
कचहरी से वे तीन बजे लौटे। देखा, शरत् बाबू अभी तक मजलिस लगाए बैठे हैं। सभा दो घण्टे बाद ही तो होने वाली है। अब कहीं याद दिलाने पर शरत् बाबू कागज़ - कलम लेकर कमरे में गए। ललित बाबू की चिन्ता का पार नहीं था। इतने थोड़े समय में क्या वे कुछ लिख पायेंगे, लेकिन साढ़े चार बजे तक शरत् बाबू अपना भाषण लिख चुके थे। ठीक समय पर वे लोग कृष्ण नगर कालेज के सभा भवन में पहुंच गए। स्थानीय भद्र लोगों से वह भवन खचाखच भरा हुआ था। तरुण विशेष रूप से बहुत उत्तेजित थे। शरत् बाबू ने जब बोलना शुरू किया तो सहसा शान्ति छा गई । अन्त तक छाई रही। भाषण सुनकर सभी लोग बहुत सन्तुष्ट हुए। इतने थोड़े समय में इतना सुन्दर संक्षिप्त सारगर्भित भाषण लिख डाला था उन्होंने
इसी सभा में दिलीपकुमार राय ने अपना प्रबन्ध 'शरत् साहित्य में आदर्शवाद' पढ़ा और निरुपमा देवी का यह गीत गाया - बाहिरेर न ओ तूमि, आमादेरि आमादेरि एकजन।'
सभा के बाद भोजन की सभा का आयोजन था । मखमल के आसन पर अध्यक्ष को आसीन करके सब लोग दिलीपकुमार राय की प्रशंसा करने लगे। किसी ने गाने की प्रशंसा की, किसी ने अभिनन्दन की तो किसी ने आवृत्ति की । शरत् बीच में बोले, “रुको, मण्टू का गाना चमत्कार, आवृत्ति चमत्कार, उच्छवास चमत्कार, सब चमत्कार। किन्तु सबसे अधिक चमत्कार जो वस्तु है, उसे कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं।”
सब चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। वे उसी गम्भीरता से बोले, “वह सबसे अधिक चमत्कार वस्तु है, इनकी तिल्ली । साधुभाषा में उसे जिगर कहते हैं। वृन्दावन, दिल्ली, आगरा, सभी जगह हम लोग साथ रहे हैं। मैं जो कुछ भी खाता वह मुझे बदहजमी कर देता। ये जो भी खाते वह इनकी शक्ति बन जाता। इतने इतने बैलून जितने परांवठे, ईंट के परिमाण जितनी मलाई, पहाड़ जितना ऊंचा पुलाव, कोफता, कोरमा, सीक- कबाब । पता नहीं सब कहां चला जाता था? किसी से भी इन्हें कोई बदहजमी नहीं हुई। इसीलिए कहता हूं कि इनकी सबसे बड़ी सम्पदा गाना या लिखना या आवृत्ति नहीं है, इनका जिगर है ।"
एक दिन इन्हीं दिलीपकुमार राय ने शरत् बाबू को उस्ताद अब्दुल करीम का गाना सुनने के लिए आमन्त्रित किया था। जब वे बुलाने के लिए आए तो वे बड़े गम्भीरता से बोले, एक शर्त पर चल सकता हूं, मुझे यह विश्वास दिला दीजिए... ..."
"क्या विश्वास?"
“कि वे रुक तो जायेंगे।”
सुनकर दिलीपकुमार एकदम अट्टहास कर उठे। शरत् कभी स्वय बड़ा अच्छा गाते थे। लेकिन शास्त्रीय संगीत से, विशेषकर उस्तादों से उनको कोई प्रेम नहीं था। एक दिन किसी मित्र के आग्रह पर वे गाना सुनने के लिए गए भी पक्का राग था। आलाप के साथ उस्ताद एक ही वाक्य बार-बार दोहराते थे। 'सैयां तू कहां गैयां, आ रे मोरे सैयां तू कहां गैयां रे ।' 5
बहुत देर तक सुनते रहे, लेकिन अन्त तक वे चुप नहीं रह सके। हुक्के की गुड़गुड़ी मुह से निकालकर वे जोर से बोले, “अरे तेरा सैयां काशी मित्तर के घर गैयां, उसे बाद क्या हुआ बताओ न !”
दिलीपकुमार से जो कुछ उन्होंने कहा था, उसका संबंध इसी घटना से था। जहां भी वे जाते, जहां भी वे बैठते, उस मजलिस में इस तरह हंसी के फबारे फूटते रहते।
उन्होंने संगीत में रुकने की बात कही थी, परन्तु जहां तक हास-परिहास की वृत्ति का संबंध है वह स्वयं भी रुकना नहीं जानते थे। उस दिन 'भारतवर्ष के कार्यालय में केवल कर्मचारी ही थे, कर्ता कोई नहीं था। शरत् बाबू उसी समय वहां पहुंचे। अफीम खाने का समय था। उन्होंने जैसे ही गोली मुंह में डाली, कर्मचारी उन्हें देखने लगे। वे बोले, “तुम भी खाओगे? मेरे जैसा लेखक बनना चाहते हो तो जरूर खाओ।" और नाना प्रकार के प्रलोभन देकर थोड़ी-थोड़ी सभी को खिलाई। फिर हरिदास को पत्र लिखा कि उनके सभी कर्मचारी लेखक बनने के मोह में अफीम खाकर नशे में टूल रहे हैं। अगर अभी उनके लिए मिठाई का प्रबन्ध नहीं कर देते तो हाथ में हथकड़ी पड़ सकती है।
हरिदास सब कुछ समझ गए और उन्होंने दस रुपये भेज दिए ।
लेकिन एक बात जो उनके मित्रों को बहुत परेशान करती थी, वह थी उनकी लोगों को अकारण ही कुद्ध कर देने की प्रवृत्ति । किसी के भी बारे में झूठ-मूठ प्रचार कर देते थे या परेशान करने के लिए ऐसा-वैसा कह देते थे। कविगुरु रवीन्द्रनाथ तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था। उस दिन ‘रसचक्र' की बैठक में उन्होंने सहसा बड़ी गम्भीरता से कहा, “तुमने सुना, आजकल रामानन्द चटर्जी और गुरुदेव में बोलचाल बन्द है।”
"सच? क्या बात है?"
" रामानन्द योरोप गए थे न दाढ़ी के कारण लोगों ने उन्हें रवीन्द्रनाथ समझ लिया । उस कविगुरु को यह पता लगा तो उन्होंने रामानन्द चटर्जी से कहा कि वे अपनी दाढ़ी कटवा दें। वे तैयार नहीं हुए। भला इतने दिनों के परिश्रम से बढ़ाई दाढ़ी कैसे कटवाई जा सकती है। तब कविगुरु ने प्रस्ताव किया कि यदि दाढ़ी कटवाना संभव नहीं है तो वे मेंहदी लगाया करें। यह सुनकर रामानन्द बाबू कुद्ध हो उठे। बोले, मैं क्या मुसलमान हूं?"
“बस तब से उनकी बोलचाल बन्द है।"
'रसचक्र' के अधिकांश सदस्य शरत् बाबू के बीरबली स्वभाव से परिचित थे। इस परिहास पर वे खूब हंसे। पर यह भी सच है कि इसी कारण जो उनसे अपरिचित थे, उनके बारे में बुरी धारणा बना लेते थे। या जो उनके विरोधी थे वे इसका अनुचित लाभ उठाते थे। किन्तु वे जरा भी परेशान नहीं होते। मित्र तर्क करते और वे हंसते रहते। यह सब वे रस लेने के विचार से ही करते थे। वे लोग देखते तो पाते उनकी आखों में छेड़-छाड़ करने की वृत्ति है। इसलिए जब सत्य प्रकट होता तो संबंधित व्यक्ति हंस पड़ते थे। लेकिन सभी तो इतने उदार नहीं होते कि जानें कि आदमी अपनी दुर्बलताओं के साथ ही बड़ा होता है। उनसे कटकर नहीं ।
इसी वर्ष मुंशीगंज में, बंगीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। उसकी साहित्य शाखा की अध्यक्षता की थी शरत् बाबू ने। उस समय वे ढाका भी गए थे और अपने प्रिय मित्र उपन्यासकार चारुचन्द्र बंदोपाध्याय के घर पर ठहरे थे। वहां के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुरेशचन्द्र घटक स्वयं साहित्यिक थे। वे उन्हें अपने पास ले जाना चाहते थे। ढाका विश्वविद्यालय के इतिहास के अध्यापक डा० रमेशचन्द्र मजूमदार मुंशीगंज में ही उन्हें अपने घर पर ठहरने का निमंत्रण दे चुके थे। लेकिन शरत् बाबू ने सबसे यही कहा “मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।"
“आपका घर यहां है?"
“हां, चारु मेरा बचपन का दोस्त है। उसका घर मेरा घर है। उसकी पत्नी मेरी जितनी देखभाल करती है, उतनी तुम नहीं कर सकोगे।"
वे किसी के पास जाकर नहीं ठहरे। फिर भी बारी-बारी उनके घर चरणधूलि डालने का निमन्त्रण उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। मजूमदार महाशय के घर जब मजलिस जमी तो कितनी कहानियां सुनाईं, कितने प्याले चाय पी और कितना तम्बाकू खाया, इसका हिसाब किसी के पास नहीं हो सकता। जिस रात सुरेशचन्द्र के यहां निमन्त्रण था, उसी रात को अपूर्वचन्द्र कुमार के घर जाना था। बातों के धनी शरत् बाबू को यह सब कैसे याद रहता । बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद स्वयं कुमार रात में 11 बजे उन्हें लेने के लिए आए।
शरत् बाबू ने कहा, “लोगों को मुझसे बात करने में आनन्द आता है, तो मैं कृपण क्यों होऊं?"
उनके घर से वे रात के ढाई बजे लौटे तो चारु बाबू ने कहा, “शरत्, समय के संबंध में तुम्हें कुछ ध्यान देना चाहिए।"
उन्हें तुरन्त उत्तर मिला, “देखो, चारु, मनुष्य घड़ी का दास हो, यह मैं कभी नहीं चाह सकता। तुम दासता से घृणा करते हो, तब भी मुझसे कहते हो कि घड़ी का दास बनूं। वह मैं नहीं करूंगा।"
आवारापन से शायद उन्हें मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसने उनके जीवन पर जो छाप लगा दी थी उससे वे कभी भी मुक्त नहीं हो सके। वे तथाकथित सभ्य समाज के सुसंस्कृत व्यक्ति कभी नहीं बन सके। उस समय भी, जब वह बंगला साहित्य के महान उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित और समादृत हो चुके थे, उन्होंने अपने को अभिजात वर्ग का व्यक्ति कहकर परिचित कराने की जरा भी चेष्टा नहीं की । यही कहा "मै न तो बहुत पढ़ा-लिखा हूं न मेरा ज्ञान ही कुछ अधिक है। मुझे जो पढ़ना चाहते हैं उसका कारण यही है कि मैंने अपनी रचनाओं में वही चित्रित किया है जो मैंने अपनी आंखों से देखा और मन से अनुभव किया है।” अभिजात की के विरोध में वे ब्रात्य ही बने रहे। कई वर्ष पूर्व प्रमथ चौधरी ने जब उन्हें अपनी एक पुस्तक समर्पित की थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि "मेरे जैसे दुश्चरित्र को पुस्तक समर्पित करने के लिए समाज चौधरी महाशय को क्षमा नहीं करेगा। वे ठहरे परम विद्वान, समाज के चौधरी और मैं ठहरा शरत् चाटूज्जे ।”
लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था वह उतना ही गम्भीर और महत्त्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को और अपने साहित्य के थीम को स्पष्ट किया है। साहित्य में आर्ट और दुर्नीति क्या है उसकी विशद व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, “साहित्य की सुशिक्षा, नीति और लाभालाभ का अंश ही अब तक मैं व्यक्त करता आया हूं। जो चीज इससे भी बड़ी है इसका आनन्द, इसका सौन्दर्य - उसकी आलोचना करने का समय अनेक कारणों से मुझे नहीं मिला। केवल एक बात कह रखना चाहता हूं कि आनन्द और सौन्दर्य केवल बाहर की वस्तु नहीं है। केवल सृष्टि करने की त्रुटि ही है, उसे ग्रहण करने की अक्षमता नहीं यह बात किसी तरह सच नहीं है। आज यह शायद असुन्दर और आनन्दहीन जान पड़े, किन्तु यही इसकी आखिरी बात नहीं है, आधुनिक साहित्य के सम्बन्ध में यह सत्य याद रखने की जरूरत है।
“और एक बात कहकर ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। अंग्रेजी में आईडियलिस्टिक आदशवादी) और रियलिस्टिक (यथार्थवादी) दो शब्द हैं। हाल में किसी- किसी ने यह अभियोग लगाया है कि आधुनिक बंगला साहित्य अत्यधिक यथार्थवादी हो चला है। मैं कहता हूं एक को 'बाद देकर' दूसरा नहीं होता । " कम से कम जिसे उपन्यास कहते हैं, वह नहीं होता। हां, कौन किधर कितना झुककर चलेगा, यह साहित्यिक शक्ति और रुचि पर निर्भर करता है। किन्तु एक शिकायत यह की जा सकती है कि पहले की तरह राजे-रजवाड़ों और जमींदारों के दुख- दैन्य- द्वन्द्व-हीन जीवन के इतिहास को लेकर आधुनिक साहित्यसेवी को सन्तोष नहीं होता उसका मन नहीं भरता । वह नीचे स्तर में उतर गया है । यह अफसोस की बात नहीं है । बल्कि इस अभिशप्त और तमाम दुखों के देश में, अपने अभियान को छोड़कर रूसी साहित्य की तरह जिस दिन वह और भी समाज के नीचे के स्तर में उतरकर उनके दुख और वेदना के बीच खड़ा हो सकेगा, उस दिन यह साहित्य-साधना केवल स्वदेश में ही नहीं विश्व - साहित्य में भी अपना स्थान कर ले सकेगी।.
आदर-अभ्यर्थना का यह जो क्रम आरम्भ हुआ वह फिर नहीं टूटा। उसमें कई महान गुण थे, फिर भी हमेशा डर लगा रहता था कि कही उनकी कमजोरियां, जो कम नहीं थीं, उनके कार्य को नष्ट न कर दें। लेकिन यह डर निर्मूल था, नियति ने उनके लिए यही पथ निश्चित किया था जिस पर वे निरन्तर भूल और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे गरीबी से उठकर आये थे । शिक्षा भी उन्हें कम ही मिली थी। परन्तु जीवन की पाठशाला में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए थे, उनके कारण मनुष्य को समझने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई थी। भले ही व्यवहार उनका अब भी अटपटा ही था। यह अटपटापन उन्हें अक्सर मुसीबत में डाल देता था, परन्तु मस्तिष्क का संतुलन कभी नहीं खोने देता था। जानने से भी अधिक वे मनुष्य को प्यार करते थे।