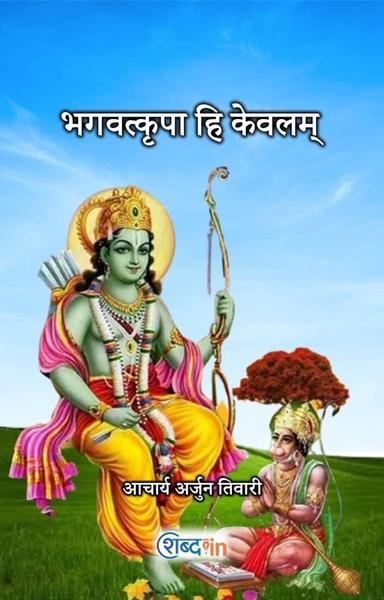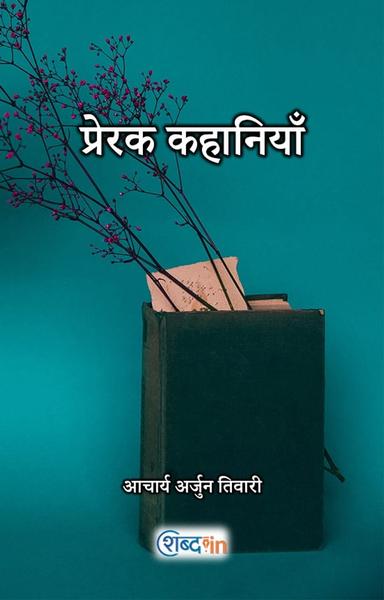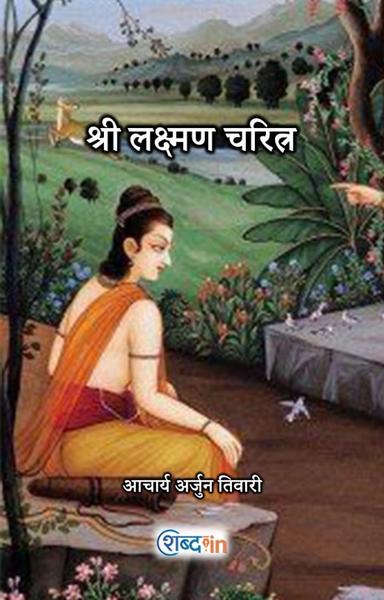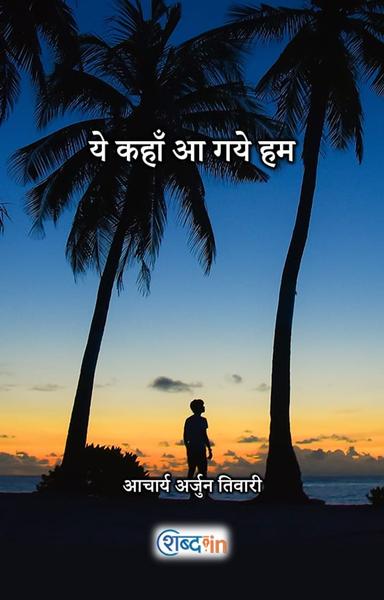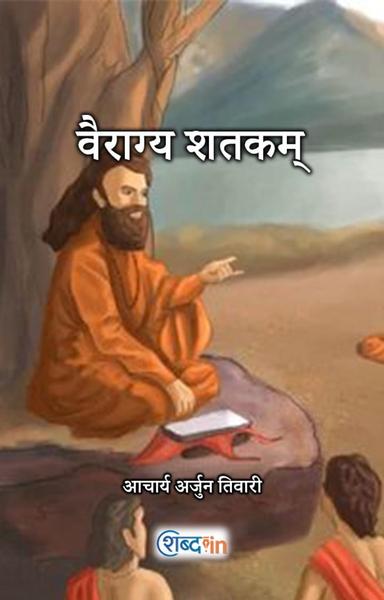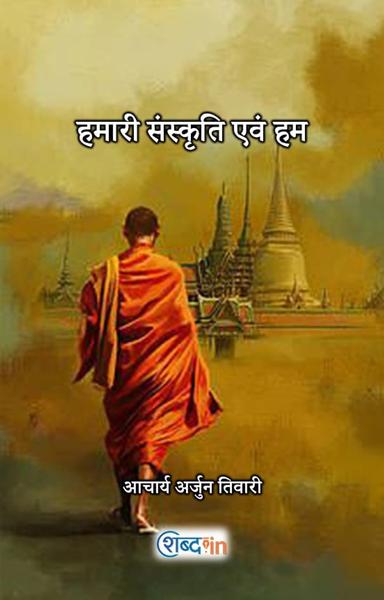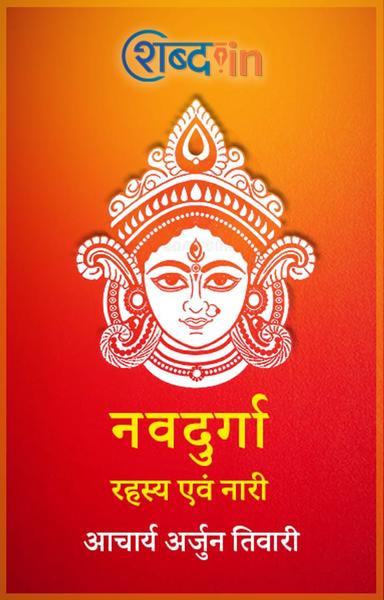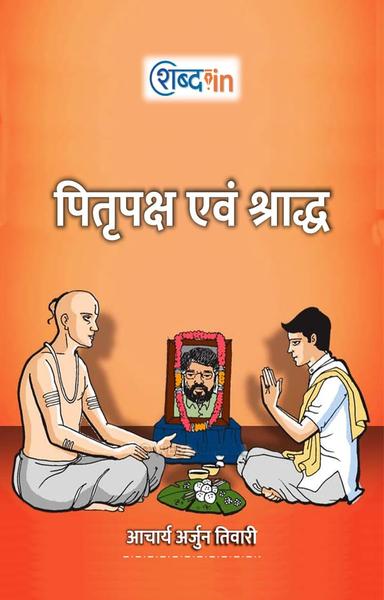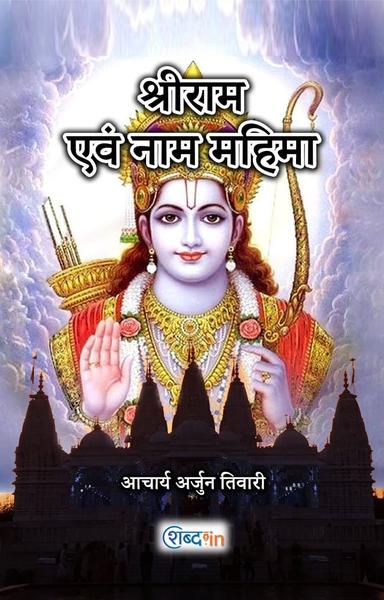भगवत्कृपा - भाग - ११५ (एक सौ पन्द्रह)
26 जुलाई 2022
17 बार देखा गया
यह संपूर्ण जगत भगवतद्विभूति के द्वारा जीवन धारण कर रहा है ! *भगवत्कृपा* की धारा - प्रपात वर्षा हो रही है ! एक औंधे प्याले के समान मनुष्य का क्षुद्र मन उस *कृपा की* पूर्णता का अनुभव करने में असमर्थ है !
*निसिदिन बरसत है यहां , भगवत्कृपा महान !*
*जान न पाता मूढ़ मन , बन मूरख अज्ञान !!*
*बन मूरख अज्ञान , कृपा को समझ न पाता !*
*फंसि माया परपंच , ईश को दोष लगाता !!*
*कह अर्जुन आचार्य आंख को , खोल देख नादान !*
*निसिदिन बरसत है यहां , भगवत्कृपा महान !!*
(स्वरचित)
योग मार्ग में नवागंतुक साधक जिसे नौ सिखुआ कहा जा सकता है , वह बहुधा *भगवत्कृपा* की प्राप्ति और पुरुषार्थ (साधना) इन दोनों विरोधी भावनाओं का पोषण करते हैं ! उनका तर्क होता है कि यदि *भगवत्कृपा* से ही मनुष्य चरम प्रगति करने में समर्थ हो हो सकता है तो वह पुरुषार्थ क्यों करें ? इसके विपरीत यदि वह अपने पुरुषार्थ से ही सफल होता है तो *भगवत्कृपा* की बात ही क्यों की जाए ? तथापि योग दर्शन के सिद्धांतों को गंभीर दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषार्थ और *भगवत्कृपा* , भाग्य तथा संकल्प की स्वतंत्रता के समान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ! पुरुषार्थ मनुष्य के अहंभाव की चेतना के आसपास से प्रारंभ होता है और उस अवस्था को लक्ष्य में रखकर अग्रसर होता है जिस अवस्था में पहुंचने पर अंतरात्मा , इंद्रिय , मन और बुद्धि की सीमा में अावद्ध नहीं रहता और इस प्रकार परमात्मा के साथ अभेदभाव का अनुभव करता है दूसरी और मनुष्य के अस्तित्व में ईश्वरीय सत्ता की बढ़ती हुई अभिव्यक्ति *भगवत्कृपा* है
*पुरुषार्थ मानव हृदय में , नहिं भेद रखता है जरा !*
*यह ही अभेदभाव , साधक को बनाता है खरा !!*
*सब कुछ समर्पित करें प्रभु को , पुण्य अथवा पाप ही !*
*पुरुषार्थ आकर्षित करें , भगवत्कृपा को आप ही !!*
(स्वरचित)
वास्तविक पुरुषार्थ मनुष्य के भीतर अभेदभाव को विकसित करता है अवैधभावापन्न व्यक्ति लौकिक जीवन के एकत्व अर्थात ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है ! साधक के व्यवहारिक जीवन में उसका पुरुषार्थ *भगवत्कृपा* को आकर्षित करता है तथा *भगवत्कृपा* उसके पुरुषार्थ को संपन्न और पूर्ण बनाती है ! अपनी प्रगति के उच्चतर में उसको यह तथ्य ज्ञात हो जाता है कि *भगवत्कृपा* और पुरुषार्थ में कोई भी भेद नहीं है ! ईश्वर वाह्यसत्ता नहीं है वह सारी सृष्टि को परिव्याप्त करने वाली अंतरतम सत्ता है , इसलिए जीवन में अंतःकेंद्र की ओर अग्रसर होने के प्रयत्न में सदा भीतरी खिंचाव के द्वारा सहायता मिलती है ! यह भीतरी खिंचाव और कुछ नहीं बल्कि *भगवत्कृपा* ही है ! जब हमें *भगवत् कृपा* की चाहत होती है तब हम अपनी दृष्टि को अपने भीतर गहराई तक दौड़ाते हैं ! जब हम भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं तब हम अपनी ही अंतरतम सत्ता को आत्मसमर्पण करते हैं ! आत्मसमर्पण की प्रक्रिया जब प्रयत्न के द्वारा फलीभूत होने लगती है तब वही पुरुषार्थ कहलाती है , परंतु जब अनायास फलीभूत होने लगती है तब उसे हम *भगवत्कृपा* कहते हैं

आचार्य अर्जुन तिवारी
51 फ़ॉलोअर्स
आचार्य अर्जुन तिवारी पुराण प्रवक्ता / यज्ञाचार्य ग्राम व पोस्ट - बड़ागाँव (रेलवे स्टेशन) तहसील - सोहावल थाना - रौनाही जनपद - श्री अयोध्या जी पिन - २२४१२६ बचपन से ही भगवत्पथ के पथिक बनने की चाह में कुछ लिखना प्रारम्भ किया ! शनै: शनै: कीर्तन - रामायण का आश्रय लेते हुए अपनी शिक्षा आचार्य तक पूरी की तथा पिताजी से ज्ञानार्जन करके पुराणों की कथाओं का अध्ययन करते हुए व्यासपीठ पर पुराणों का प्रवचन एवं ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म सम्पन्न करवाते हुए लेखन के क्षेत्र में भी सूक्ष्म प्रयास करते रहे ! आज हमारी कई पुस्तकें शब्दनगरी के प्लेटफॉर्म प्रकाशित हैं ! D
प्रतिक्रिया दे
167
रचनाएँ
!! भगवत्कृपा हि केवलम् !!
0.0
इस संसार में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे सब भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं ! बिना भगवत्कृपा के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है ! इसलिए चराचर जगत में भगवत्कृपा का दर्शन करते हुए इस जीवन एवं जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं को भगवत्कृपा का प्रसाद मानते हुए हमें स्वीकार करना चाहिए
1
भगवत्कृपा - भाग - एक
20 मई 2022
4
0
0
2
भगवत्कृपा - भाग - २ (दो)
20 मई 2022
1
0
0
3
भगवत्कृपा - भाग - ३ (तीन)
20 मई 2022
1
0
0
4
भगवत्कृपा - भाग - ४ (चार)
20 मई 2022
1
0
0
5
भगवत्कृपा -भाग - ५ (पाँच)
21 मई 2022
1
0
0
6
भगवत्कृपा - भाग - ६ (छ:)
21 मई 2022
1
0
0
7
भगवत्कृपा - भाग - ७ (सात)
21 मई 2022
1
0
0
8
भगवत्कृपा - भाग - ८ (आठ)
21 मई 2022
0
0
0
9
भगवत्कृपा - भाग - ९ (नौ)
21 मई 2022
0
0
0
10
भगवत्कृपा - भाग - १० (दस)
21 मई 2022
0
0
0
11
भगवत्कृपा - भाग - ११ (ग्यारह)
21 मई 2022
1
0
0
12
भगवत्कृपा - भाग - १२ (बारह)
22 मई 2022
1
0
0
13
भगवत्कृपा - भाग - १३ (तेरह)
22 मई 2022
1
0
0
14
भगवत्कृपा - भाग - १४ - (चौदह)
22 मई 2022
0
0
0
15
भगवत्कृपा - भाग - १५ (पन्द्रह)
23 मई 2022
0
0
0
16
भगवत्कृपा - भाग - १६ (सोलह)
23 मई 2022
0
0
0
17
भगवत्कृपा - भाग - १७ (सत्रह)
24 मई 2022
1
1
0
18
भगवत्कृपा -भाग १८ (अठारह)
24 मई 2022
1
0
0
19
भगवत्कृपा - भाग १९ (उन्नीस)
25 मई 2022
0
0
0
20
भगवत्कृपा - भाग - २० (बीस)
25 मई 2022
0
0
0
21
भगवत्कृपा - भाग - २१ (इक्कीस)
25 मई 2022
0
0
0
22
भगवत्कृपा - भाग २२ (बाईस)
26 मई 2022
0
0
0
23
भगवत्कृपा - भाग - २३ (तेईस)
26 मई 2022
0
0
0
24
भगवत्कृपा - भाग - २४ (चौबीस)
26 मई 2022
0
0
0
25
भगवत्कृपा - भाग - २५ (पच्चीस)
27 मई 2022
0
0
0
26
भगवत्कृपा- भाग - २६ (छब्बीस)
27 मई 2022
0
0
0
27
भगवत्कृपा - भाग - २७ (सत्ताईस)
27 मई 2022
0
0
0
28
भगवत्कृपा - भाग - २८ (अट्ठाईस)
27 मई 2022
0
0
0
29
भगवत्कृपा - भाग - २९ (उनतीस)
27 मई 2022
0
0
0
30
भगवत्कृपा - भाग - ३० (तीस)
27 मई 2022
0
0
0
31
भगवत्कृपा - भाग - ३१ (इकतीस)
28 मई 2022
0
0
0
32
भगवत्कृपा - भाग - ३२ (बत्तीस)
29 मई 2022
0
0
0
33
भगवत्कृपा - भाग - ३३ (तैंतीस)
29 मई 2022
0
0
0
34
भगवत्कृपा - भाग - ३४ (चौंतीस)
29 मई 2022
0
0
0
35
भगवत्कृपा - भाग - ३५ (पैंतीस)
29 मई 2022
0
0
0
36
भगवत्कृपा - भाग - ३६ (छत्तीस)
29 मई 2022
0
0
0
37
भगवत्कृपा - भाग - ३७ (सैंतीस)
30 मई 2022
0
0
0
38
भगवत्कृपा - भाग - ३८ (अड़तीस)
30 मई 2022
1
1
2
39
भगवत्कृपा - भाग - ३९ (उनतालीस)
30 मई 2022
0
0
0
40
भगवत्कृपा - भाग - ४० (चालीस)
30 मई 2022
0
0
0
41
भगवत्कृपा - भाग ४१ (इकतालीस)
2 जून 2022
0
0
0
42
भगवत्कृपा - भाग - ४२ (बयालीस)
2 जून 2022
0
0
0
43
भगवत्कृपा - भाग - ४३ (तिरालीस)
2 जून 2022
0
0
0
44
भगवत्कृपा - भाग - ४४ (चौरालीस)
3 जून 2022
0
0
0
45
भगवत्कृपा - भाग - ४५ (पैंतालीस)
3 जून 2022
0
0
0
46
भगवत्कृपा - भाग - ४६ (छियालीस)
3 जून 2022
0
0
0
47
भगवत्कृपा - भाग - ४७ (सैंतालीस)
3 जून 2022
1
1
0
48
भगवत्कृपा - भाग - ४८ (अड़तालीस)
4 जून 2022
0
0
0
49
भगवत्कृपा - भाग - ४९ (उनचास)
15 जून 2022
0
0
0
50
भगवत्कृपा - भाग - ५० (पचास)
15 जून 2022
0
0
0
51
भगवत्कृपा - भाग - इक्यावन (५१)
15 जून 2022
0
0
0
52
भगवत्कृपा - भाग - ५२ (बावन)
15 जून 2022
0
0
0
53
भगवत्कृपा - भाग ५३ (तिरपन)
15 जून 2022
0
0
0
54
भगवत्कृपा - भाग - ५४ (चौव्वन)
16 जून 2022
0
0
0
55
भगवत्कृपा - भाग - ५५ (पचपन)
16 जून 2022
0
0
0
56
भगवत्कृपा - भाग - ५६ (छप्पन)
16 जून 2022
0
0
0
57
भगवत्कृपा - भाग - ५७ (सत्तावन)
16 जून 2022
0
0
0
58
भगवत्कृपा - भाग - ५८ (अट्ठावन)
16 जून 2022
0
0
0
59
भगवत्कृपा - भाग - ५९ (उनसठ)
16 जून 2022
0
0
0
60
भगवत्कृपा - भाग - ६० (साठ)
17 जून 2022
0
0
0
61
भगवत्कृपा - भाग - ६१ (इकसठ)
17 जून 2022
0
0
0
62
भगवत्कृपा - भाग - ६२ (बासठ)
18 जून 2022
0
0
0
63
भगवत्कृपा - भाग - ६३ (तिरसठ)
18 जून 2022
1
1
0
64
भगवत्कृपा- भाग - ६४ (चौंसठ)
19 जून 2022
2
1
0
65
भगवत्कृपा -;भाग - ६५ (पैंसठ)
20 जून 2022
0
0
0
66
भगवत्कृपा - भाग - ६६ (छियासठ)
21 जून 2022
0
0
0
67
भगवत्कृपा -भाग - ६७ (सड़सठ)
21 जून 2022
0
0
0
68
भगवत्कृपा - भाग ६८ (अड़सठ)
21 जून 2022
0
0
0
69
भगवत्कृपा - भाग - ६९ (उनहत्तर)
22 जून 2022
0
0
0
70
भगवत्कृपा - भाग - ७० (सत्तर)
22 जून 2022
0
0
0
71
भगवत्कृपा - भाग - ७१ (इकहत्तर)
23 जून 2022
0
0
0
72
भगवत्कृपा - भाग ७२ (बहत्तर)
24 जून 2022
0
0
0
73
भगवत्कृपा - भाग - ७३ (तिहत्तर)
25 जून 2022
0
0
0
74
भगवत्कृपा - भाग - ७४ (चौहत्तर)
26 जून 2022
0
0
0
75
भगवत्कृपा - भाग - ७५ (पचहत्तर)
26 जून 2022
0
0
0
76
भगवत्कृपा - भाग - ७६ (छिहत्तर)
27 जून 2022
0
0
0
77
भगवत्कृपा - भाग - ७७ (सतहत्तर)
29 जून 2022
0
0
0
78
भगवत्कृपा - भाग - ७८ (अठहत्तर)
3 जुलाई 2022
0
0
0
79
भगवत्कृपा - भाग - ७९ ( उन्यासी )
3 जुलाई 2022
0
0
0
80
भगवत्कृपा - भाग - ८० (अस्सी)
3 जुलाई 2022
0
0
0
81
भगवत्कृपा - भाग - ८१ (इक्यासी)
4 जुलाई 2022
0
0
0
82
भगवत्कृपा - भाग - ८२ (बयासी)
4 जुलाई 2022
0
0
0
83
भगवत्कृपा - भाग - ८३ (तिरासी)
4 जुलाई 2022
0
0
0
84
भगवत्कृपा - भाग - ८४ (चौरासी)
5 जुलाई 2022
0
0
0
85
भगवत्कृपा भाग - ८५ (पचासी)
5 जुलाई 2022
0
0
0
86
भगवत्कृपा - भाग - ८६ (छियासी)
5 जुलाई 2022
0
0
0
87
भगवत्कृपा - भाग - ८७ (सत्तासी)
5 जुलाई 2022
0
0
0
88
भगवत्कृपा - भाग - ८८ (अट्ठासी)
5 जुलाई 2022
0
0
0
89
भगवत्कृपा - भाग - ८९ (नवासी)
5 जुलाई 2022
0
0
0
90
भगवत्कृपा - भाग - ९० ( नब्बे )
5 जुलाई 2022
0
0
0
91
भगवत्कृपा - भाग - ९१ (इक्यानबे)
6 जुलाई 2022
0
0
0
92
भगवत्कृपा - भाग - ९२ (बानबे)
6 जुलाई 2022
0
0
0
93
भगवत्कृपा - भाग - ९३ (तिरानबे)
6 जुलाई 2022
0
0
0
94
भगवत्कृपा - भाग - ९४ (चौरानबे)
6 जुलाई 2022
0
0
0
95
भगवत्कृपा - भाग ९५ (पंचानबे)
6 जुलाई 2022
0
0
0
96
भगवत्कृपा - भाग - ९६ (छियानबे)
11 जुलाई 2022
0
0
0
97
भगवत्कृपा - भाग - ९७ (सत्तानबे)
11 जुलाई 2022
0
0
0
98
भगवत्कृपा - भाग - ९८ (अट्ठानबे)
11 जुलाई 2022
0
0
0
99
भगवत्कृपा - भाग ९९ (निन्यानबे)
14 जुलाई 2022
0
0
0
100
भगवत्कृपा - भाग - १०० (सौ)
14 जुलाई 2022
0
0
0
101
भगवत्कृपा - भाग - १०१ (एक सौ एक)
14 जुलाई 2022
0
0
0
102
भगवत्कृपा - भाग - १०२ (एक सौ दो)
14 जुलाई 2022
0
0
0
103
भगवत्कृपा - भाग - १०३ (एक सौ तीन)
15 जुलाई 2022
0
0
0
104
भगवत्कृपा - भाग - १०४ (एक सौ चार)
15 जुलाई 2022
0
0
0
105
भगवत्कृपा - भाग - १०५ (एक सौ पाँच)
15 जुलाई 2022
0
0
0
106
भगवत्कृपा - भाग - १०६ (एक सौ छ:)
15 जुलाई 2022
0
0
0
107
भगवत्कृपा - भाग - १०७ (एक सौ सात)
15 जुलाई 2022
0
0
0
108
भगवत्कृपा - भाग - १०८ (एक सौ आठ)
15 जुलाई 2022
0
0
0
109
भगवत्कृपा - भाग - १०९ (एक सौ नौ)
20 जुलाई 2022
0
0
0
110
भगवत्कृपा - भाग - ११० (एक सौ दस)
21 जुलाई 2022
0
0
0
111
भगवत्कृपा - भग - १११ (एक सौ ग्यारह)
22 जुलाई 2022
0
0
0
112
भगवत्कृपा - भाग - ११२ (एक सौ बारह)
22 जुलाई 2022
0
0
0
113
भगवत्कृपा - भाग - ११३ (एक सौ तेरह)
22 जुलाई 2022
0
0
0
114
भगवत्कृपा - भाग - ११४ (एक सौ चौदह)
22 जुलाई 2022
0
0
0
115
भगवत्कृपा - भाग - ११५ (एक सौ पन्द्रह)
26 जुलाई 2022
0
0
0
116
भगवत्कृपा - भाग - ११६ (एक सौ सोलह)
26 जुलाई 2022
0
0
0
117
भगवत्कृपा - भाग - ११७ (एक सौ सत्रह)
26 जुलाई 2022
0
0
0
118
भगवत्कृपा - भाग - ११८ (एक सौ अठारह)
26 जुलाई 2022
0
0
0
119
भगवत्कृपा - भाग - ११९ (एक सौ उन्नीस)
30 जुलाई 2022
0
0
0
120
भगवत्कृपा - भाग - १२० (एक सौ बीस)
30 जुलाई 2022
0
0
0
121
भगवत्कृपा - भाग - १२१ (एक सौ इक्कीस)
30 जुलाई 2022
0
0
0
122
भगवत्कृपा - भाग - १२२ (एक सौ बाईस)
7 अगस्त 2022
0
0
0
123
भगवत्कृपा - भाग - १२३ (एक सौ तेईस)
7 अगस्त 2022
0
0
0
124
भगवत्कृपा - भाग - १२४ (एक सौ चौबीस)
7 अगस्त 2022
0
0
0
125
भगवत्कृपा - भाग - १२५ (एक सौ पच्चीस)
7 अगस्त 2022
0
0
0
126
भगवत्कृपा - भाग - १२६ (एक सौ छब्बीस)
8 अगस्त 2022
0
0
0
127
भगवत्कृपा - भाग -;१२७ (एक सौ सत्ताईस)
8 अगस्त 2022
0
0
0
128
भगवत्कृपा - भाग - १२८ (एक सौ अट्ठाईस)
15 अगस्त 2022
0
0
0
129
भगवत्कृपा - भाग - १२९ (एक सौ उनतीस)
24 अगस्त 2022
0
0
0
130
भगवत्कृपा - भाग - १३० (एक सौ तीस)
24 अगस्त 2022
0
0
0
131
भगवत्कृपा - भाग - १३१ (एक सौ इकतीस)
24 अगस्त 2022
0
0
0
132
भगवत्कृपा -;भाग - १३२ (एक सौ बत्तीस)
26 अगस्त 2022
0
0
0
133
भगवत्कृपा - भाग - १३३
28 अगस्त 2022
0
0
0
134
भगवत्कृपा - भाग - १३४ (एक सौ चौतींस)
29 अगस्त 2022
0
0
0
135
भगवत्कृपा - भाग - १३५ (एक सौ पैंतींस)
29 अगस्त 2022
0
0
0
136
भगवत्कृपा - भाग - १३६ (एक सौ छत्तींस)
29 अगस्त 2022
0
0
0
137
भगवत्कृपा - भाग - १३७ (एक सौ सैंतीस)
5 सितम्बर 2022
0
0
0
138
भगवत्कृपा - भाग - १३८ (एक सौ अड़तीस)
5 सितम्बर 2022
0
0
0
139
भगवत्कृपा - भाग - १३९ (एक सौ उनतालीस)
5 सितम्बर 2022
0
0
0
140
भगवत्कृपा - भाग - १४० (एक सौ चालीस )
5 सितम्बर 2022
0
0
0
141
भगवत्कृपा - भाग - १४१ (एक सौ इकतालीस)
5 सितम्बर 2022
0
0
0
142
भगवत्कृपा - भाग - १४२ (एक सौ बयालीस)
6 सितम्बर 2022
0
0
0
143
भगवत्कृपा - भाग - १४३ (एक सौ तिरालीस)
6 सितम्बर 2022
0
0
0
144
भगवत्कृपा-भाग-१४४ (एक सौ चौरालीस)
8 सितम्बर 2022
0
0
0
145
भगवत्कृपा - भाग - १४५ (एक सौ पैंतालीस)
8 सितम्बर 2022
0
0
0
146
भगवत्कृपा - भाग - १४६ (एक सौ छियालीस)
11 सितम्बर 2022
0
0
0
147
भगवत्कृपा - भाग - १४७ (एक सौ सैंतालीस)
11 सितम्बर 2022
0
0
0
148
भगवत्कृपा - भाग - १४८ (एक सौ अड़तालीस)
11 सितम्बर 2022
0
0
0
149
भगवत्कृपा - भाग - १४९ (एक सौ उनचास )
12 सितम्बर 2022
0
0
0
150
भगवत्कृपा - भाग - १५० (एक सौ पचास)
13 सितम्बर 2022
0
0
0
151
भगवत्कृपा - भाग - १५१ (एक सौ इक्यावन)
13 सितम्बर 2022
0
0
0
152
भगवत्कृपा - भाग - १५२ (एक सौ बावन)
14 सितम्बर 2022
0
0
0
153
भगवत्कृपा - भाग - १५३ (एक सौ तिरपन)
14 सितम्बर 2022
0
0
0
154
भगवत्कृपा - भाग - १५४ (एक सौ चौव्वन)
15 सितम्बर 2022
0
0
0
155
भगवत्कृपा - भाग - १५५ (एक सौ पचपन)
15 सितम्बर 2022
0
0
0
156
भगवत्कृपा - भाग - १५६ (एक सौ छप्पन)
16 सितम्बर 2022
0
0
0
157
भगवत्कृपा - भाग - १५७ (एक सौ सत्तावन)
16 सितम्बर 2022
0
0
0
158
भगवत्कृपा - भाग - १५८ (एक सौ अट्ठावन)
16 सितम्बर 2022
0
0
0
159
भगवत्कृपा - भाग - १५९ (एक सौ उनसठ)
16 सितम्बर 2022
0
0
0
160
भगवत्कृपा - भाग - १६० ( एक सौ साठ )
16 सितम्बर 2022
0
0
0
161
भगवत्कृपा - भाग - १६१ (एक सौ इकसठ)
18 सितम्बर 2022
0
0
0
162
भगवत्कृपा - भाग - १६२ (एक सौ बासठ)
18 सितम्बर 2022
0
0
0
163
भगवत्कृपा - भाग - १६३ (एक सौ तिरसठ)
18 सितम्बर 2022
0
0
0
164
भगवत्कृपा - भाग - १६४
12 अक्टूबर 2022
0
0
0
165
भगवत्कृपा - भाग - १६५ (एक सौ पैसठ
17 अक्टूबर 2022
0
0
0
166
भगवत्कृपा - भाग - १६६ (एक सौ छियासठ )
17 अक्टूबर 2022
0
0
0
167
भगवत्कृपा - भाग - १६७ (एक सौ सड़सठ )
17 अक्टूबर 2022
0
0
0
---
किताब पढ़िए
- हॉरर - भूतप्रेत
- सस्पेंस - थ्रिलर
- स्त्री विमर्श
- प्रेम - रोमांस
- हास्य व्यंग्य
- कॉमिक्स - मीम्स
- जीवनी – संस्मरण
- समीक्षा
- यात्रा वृतांत
- सेल्फ हेल्प
- बाल साहित्य
- स्वास्थ्य - फिटनेस
- इतिहास
- कानून - व्यवस्था
- प्रौद्योगिकी - विज्ञान
- पाक-कला
- व्यापार - धन
- शिक्षा
- खेल – खिलाड़ी
- डायरी
- अन्य
- अनुवाद
- विज्ञान गल्प्
- सामाजिक
- इरोटिक
- पारिवारिक
- धर्म - आध्यात्म
- शिल्प - शौक
- अपराध - जासूसी
- फैशन - लाइफस्टाइल
- ग़ज़ल
- हिंदी नाटक
- हिंदी पत्रिका
- हिंदी क्लासिक
- साहित्य और कथा
- नयी किताबें
- प्रसिद्ध किताबें
- लिस्टेड किताबें
- प्रिंटेड किताबें
- ऑडियो बुक्स
- समीक्षित पुस्तकें
- उपन्यास
- कहानी / कहानी संग्रह
- काव्य / कविता संग्रह
- पत्रिका
- जनरल बुक्स
- पुस्तक प्रतियोगिता
- सभी किताबें...
लेख पढ़िए
- नववर्ष पर कविता
- 2025 से आपकी उम्मीदें
- सामाजिक भावनात्मक शिक्षा
- 2024 की यादें
- ज़ाकिर हुसैन
- बेटियाँ और समाज
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य
- घरेलू हिंसा कानून पर आपकी विवेचना
- नारीवाद का दुरूपयोग
- सपनों का शहर
- सीरिया में तख्तापलट
- वित्तीय साक्षरता का महत्व
- वर्चुअल रियलिटी
- सर्दी की सुबह
- सफलता की सीढ़ियां
- आशाओं का टूटना
- बिना रंग की दुनिया
- बाल विवाह का अभिशाप
- संविधान दिवस
- Ipl auction 2025
- रोजमर्रा
- दीपक श्रीवास्तव नीलपदम
- दीपक नीलपदम्
- दीपक नील पदम्
- दीपकनीलपदम्
- समय
- नया साल
- चिठ्ठियां
- संस्कार
- संघर्ष
- हेल्थ
- पुरुखों की यादें
- सड़क
- लेखक परिचय
- एकात्म मानववाद
- हिंदी दिवस
- जाम
- नं
- सड़क
- सभी लेख...